हैशटैग
#AcharyaShriShantiSagarJiMaharaj1872DevendraKirtiJi

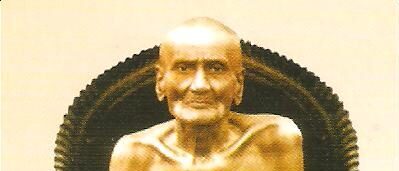
Acharya Shantisagar was one of the greatest Jain teachers and scholars of the 20th century. He was the spiritual leader (acharya) of the Digambara Jain community. For over thirty-five years, from 1920 to his death in 1955, he wandered all over India. He as the first monk in several centuries to revive the tradition of wandering naked without even a begging bowl. He would eat only once a day, receiving food in his bare hands. He was a holy man who led by example and his actions are greatly admired by Jainas throughout the world.

Ref: This chart is taken from the book : Jain Digambaracharya: Prerak Sant avim Vichar, written by Dr.R.K.Jain (Kota)
Acharya,Muni and Aryika Dikshit by Acharya Shri Shanti Sagar Ji Maharaj
1.Muni Shri Vardhaman Sagar Ji Maharaj(South)
2.Muni Shri Chandrakirti Sagar Ji Maharaj
3.Muni Shri Malli Sagar Ji Maharaj
4.Muni Shri Dharm Sagar Ji Maharaj
5.Muni Shri Chandra Sagar Ji Maharaj
6.Muni Shri Uttam Sagar Ji Maharaj
7.Acharya Shri Adi Sagar Ji Maharaj(Shedbalkar)
8.Acharya Shri Nemi Sagar Ji Maharaj
9.Acharya Shri Nami Sagar Ji Maharaj
10.Aryika Shri Vidyavati Mata Ji
गौरवशाली प्रकाशपुंज आचार्य कुंदकुंद स्वामी समंतभद्र, विद्यानंदि, जिनसेन इत्यादि आचार्यों की जन्मभूमि तथा उपदेश से पुनीत विहार भूमि-कर्नाटक देश में आचार्यश्री १०८ शांतिसागर महाराज का जन्म हुआ।
बेलगांव जिले के चिकोड़ी तहसील में दूध-गंगा और वेद-गंगा के संगम के कारण तीर्थरूप ‘‘भोज’’ नामक ग्राम के पास ‘‘येळगुड’’ गांव में विक्रम संवत् १९२९ में (ई. सन् १८७२) आषाढ़ मास के कृष्णपक्ष में षष्ठी तिथि को बुधवार की रात्रि में आचार्यश्री का जन्म हुआ। जन्म नाम ‘‘सातगौंडा’’ था। पिताश्री का नाम भीमगौंडा था, वे पाटील घराने के थे, ‘‘पाटील’’ याने नगर के राजा, ऐसा ही समाज में उनका मान-सम्मानपूर्ण स्थान था। ऊँची पूरी शक्तिशाली देह थी। पराक्रमशीलतापूर्ण नैसर्गिक वृत्ति थी। धीर-वीर गंभीर सहज मनोवृति थी। माता का नाम देवी ‘‘सत्यवती’’ था। वह भी श्रद्धालु, धार्मिक और सदाचार सम्पन्न थीं। भगवान की भक्ति पूजा करना, त्यागीगणों को आहारदान देना, उनकी वैयावृत्य करना, दीन दुखियों को सहायता पहुँचाना आदि कार्यों में विशेष रुचि और पूर्ण सावधान थीं। उस माता का वह सहज स्वभाव था। छोटे-बड़े व्यसनों से दूर पिताजी ने सोलह वर्ष तक दिन में एक ही बार भोजन करने का व्रत लिया था। आचार्यश्री का बाल-जीवन इस प्रकार से सदाचार सम्पन्न माता-पिता की छत्रछाया में व्यतीत हुआ। एक प्रकार से निसर्ग योजना में यह मणिकांचन संयोग ही था।
यद्यपि ये नानी के घर में जन्में थे, फिर भी इनका निवासस्थान-पैतृकस्थान भोजग्राम ही है। आजकल बालकों के जन्म हास्पीटल में होता है, तो भी वह जन्मभूमि न होकर पिता का घर, गाँव ही जन्मभूमि मानी जाती है, ऐसे ही आचार्यश्री की जन्मभूमि या निवास स्थान भोज ही माना जायेगा।
सातगौंडा की विद्यालयीन शिक्षा बहुत कम हुई। वे पाठशाला में तीसरी कक्षा तक पढ़ पाये। शिक्षा के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी आज की अपेक्षा देहातों में अपेक्षाकृत कम थी। संस्कारशील माता-पिता के द्वारा घर में जो कुछ धार्मिक संस्कार हुए, केवल वे ही जीवनाधार बन गये। सत्य-सत्य कहना हो तो जीवन में इस मूल अवस्था में सातगौंडा ने अच्छी वृद्धि ही की जिससे माता-पिता का जीवन धन्य हो गया। पाठशाला में भी सातगौंडा ने एक बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में ही प्रसिद्धि पाई थी।
जब चरित्रनायक सातगौंडा जी ९ साल के हुए, ज्येष्ठ भाई देवगौंडा और आदगौंडा का विवाह सम्पन्न हो रहा था। सातगौंडा का भी विवाह जबरदस्ती ही किया गया। ‘‘संसार विषये सद्य: स्वतो हि मनसो गति:’’। संसार के विषयों में संसारी जीवों की निसर्ग से प्रवृत्ति होती ही है। बच्चों के खेल जैसी प्रक्रिया हो गई। दैव को वह भी स्वीकार नहीं था। विवाह के पश्चात् छ: माह के भीतर ही विवाहिता की इहलोक यात्रा समाप्त हुई। सातगौंडा बाल्यावस्था में विवाहबद्ध होकर भी निसर्ग से बालब्रह्मचारी रहे। ‘‘लाभात् अलाभं बहु मन्यमान:।’’ लाभ से अलाभ को लाभप्रद मानने की बालक सातगौंडा की निसर्ग प्रवृत्ति रही है। अनंतर किये गये आग्रह के वे शिकार नहीं हुए अर्थात् पुन: विवाह नहीं किया।
आत्मानुशासन, समयसार इन दो ग्रंथों का वाचन सातगौंडा प्रारंभ से ही करते थे। विशेषरूप से तत्त्वचिंतन, मनन में काल व्यतीत होता था। आयु के १७वें, १८वें वर्ष में भरी युवावस्था में ही मन में दिगम्बरी दीक्षा लेने के सहज भाव होने लगे परन्तु माता-पिता के दबाववश उस समय वे अपने विचारों को अमल में न ला सके, व्यक्त भी न कर सके। कुछ काल तक उन्हें यथापूर्व घर में ही रहना पड़ा। परन्तु प्रवृत्ति जल से भिन्न कमल की तरह बनी रही। शास्त्र स्वाध्याय की तरह तीर्थक्षेत्रों की भक्ति का भी आचार्यश्री के जीवन में विशेष स्थान रहा। मोक्षमार्ग के पथिक साधक के जीवन में तीर्थयात्रा-दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता ही है। असंगभाव या वीतराग भावों की धारा प्रवाहित करने के लिए दृष्टिसम्पन्न साधु यात्रा को अच्छा निमित्त बना सकता है। सातगौंडा यह कर पाये इसी में परिमार्जित तत्त्वदृष्टि स्पष्ट होती है। विहार का प्रत्येक कदम वीतरागता के लिए था, वीतरागता की ओर था।
इसी अवस्था में पाँच छ: साल और बीत गये। सातगौंडा के मन में निर्गंरथ दीक्षा लेने के विचार तीव्रता से आने लगे। इस बार साहस के साथ माता-पिता के समक्ष उन्होंने अपनी भावना व्यक्त भी की परन्तु पिता जी ने कहा, ‘‘हमारे ये अंतिम दिन हैं, दीक्षा लेकर हमारी मानसिक यातनाएं बढ़ेंगी सो ठीक नहीं होगा-अच्छा नहीं होगा।’’ पिता की आज्ञा तथा पुत्र-कर्तव्य का विकल्प होने से सातगौंडा का दीक्षा लेने का विचार कुछ समय के लिए स्थगित हुआ। शक संवत् १८३३ ई. सन् १९१२ में सातगौंडा की माताजी की इहलोक यात्रा समाप्त हुई। उसके कुछ साल पहले ही पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ था। अब प्रकृतिसिद्ध त्यागमय जीवन और संयमशील बन गया। कोई लगाव भी न रहा। इसी काल में श्रवणबेलगोला-गोमटेश्वर इत्यादि पुण्यक्षेत्रों की दक्षिण यात्रा भी समाप्त कर सातगौंडा शक सं. १८३६ में भोजग्राम में आये।
सातगौंडा ने जीवन के इकतालीस साल पूर्ण होने के उपरांत दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय किया। उस समय कर्नाटक में दिगम्बर स्वामी श्रीदेवेंद्रकीर्ति मुनिराज विहार कर रहे थे। ‘‘कापशी’’ ग्राम के निकट ‘‘उत्तूर’’ नामक देहात है। वहाँ उनका आगमन होने पर सातगौंडा मुनिश्री के समीप पहुँचे और दिगम्बर दीक्षा देने की प्रार्थना की परन्तु श्रीदेवेन्द्रकीर्ति स्वामी ने प्रारंभ में क्षुल्लक पद की ही दीक्षा लेने को कहा। ठीक ही है ‘‘क्रमारम्भो हि सिद्धिकृत्’’ गुरु आज्ञा को प्रमाण माना। शक सम्वत् १८३७ ई. सन् १९१८ में ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि को ‘‘सातगौंडा’’ ने क्षुल्लक पद की दीक्षा धारण की। इस प्रकार स्वतंत्र संयमी जीवन का शुभारंभ हो गया।
उत्तूर ग्राम छोटा था इसलिए गुरु की आज्ञा लेकर क्षुल्लकजी महाराज चातुर्मास के लिए कार्गल आये परन्तु इसी काल में कोगनोली से कुछ नैष्ठिक श्रावक कागल पहुँचे। उन्होंने क्षुल्लक जी से प्रार्थना की कि, ‘‘हमारे कोगनोली ग्राम में आपका पहला चातुर्मास हो।’’ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर क्षुल्लकजी कोगनोली पहुँचे। इस प्रकार क्षुल्लकजी का प्रथम वर्षायोग धारण करने का प्रारंभ कोगनोली से हुआ। ध्यान धारण तथा शांति अनुभवन के लिए कोगनोली का चौमासा अत्यन्त अनुकूल रहा। आचार्यश्री के सहजोद्गार रहे कि ‘‘कोगनोली आमचे आजोळ आहे’’ याने ‘‘कोगनोली हमारी मां का गांव है’’, ननिहाल है। ऐसा ही परस्पर व्यवहार रहा।
क्षुल्लक जी महाराज का चातुर्मास कोगनोली में अपूर्व धर्मप्रभावना के साथ सम्पन्न हुआ। दूसरा चातुर्मास कुम्भोज में और तीसरा चातुर्मास फिर से कोगनोली में हुआ। अनन्तर क्षुल्लकजी ने कर्नाटक प्रांत में विहार शुरू किया। कोगनोली से जैनवाड़ी और वहाँ से बाहुबली क्षेत्र (कुंभोज) में महाराज जी का आगमन हुआ। ‘‘महाराज जी बाहुबली में आये हैं’’ यह वार्ता सुनकर आस-पास के श्रावकगण भी बाहुबली आये। योगायोग से समडोली से कुछ श्रावक लोग इसी समय गिरनार जी की यात्रा के लिए जा रहे थे। उन्होंने महाराज जी से साथ में आने की प्रार्थना की। क्षुल्लक जी महाराज को वाहन में बैठने का त्याग नहीं था। यात्रियों के साथ-साथ गिरनारजी की यात्रा सानन्द सम्पन्न हुई।
श्री गिरनार क्षेत्र का दर्शन करते समय महाराजजी का हृदय उठी हुई वैराग्य भावनाओं से गद्गद् हो उठा। भगवान नेमिनाथ के चरणों के पुन:-पुन: दर्शन कर क्षुल्लकजी के वीतराग भावों में सहज वृद्धि हुई। सावधानी तो पूरी थी ही। उसी समय श्री नेमिनाथ भगवान की चरण साक्षी में स्वयं ऐलक पद को स्वीकार किया। एक कौपीन मात्र परिग्रह के बिना सब वस्त्रादि परिग्रहों को त्याग दिया। नूतन प्रतिमा की प्रतिष्ठा पूर्व प्रतिष्ठित प्रतिमा की साक्षी में होती है और नया व्रत विधान पूर्व में व्रती की साक्षी से ही होना चाहिए ऐसी एक अच्छी प्राचीन परम्परा है। महाराजजी इस परम्परा को तोड़ना नहीं चाहते थे जैसा कि निग्र्रन्थ दीक्षा के समय देखा गया। इस समय उनसे रहा नहीं गया। वैराग्य भावों की वेगवान गति को वे रोक नहीं सके। पूज्य स्वर्गीय अनुभवसमृद्ध श्री वीरसागर जी महाराज ठीक कहते थे। ‘‘गुरु कहे सो करना गुरु करे सो नहीं करना।’’ अस्तु! इस समय वीतरागता का वैराग्यभाव से अपूर्व मिलन होना था, हो गया। श्री गिरनारजी से लौटते समय ऐलकजी ने श्री दक्षिण कुंडलक्षेत्र की वंदना की। श्री पाश्र्वप्रभु भगवान की मूर्ति की साक्षी में ऐलकजी महाराज ने सब वाहनों का आजीवन के लिए परित्याग कर दिया। आगे के लिए विहार का रूप ‘‘पद-विहार’’ ही निश्चित हुआ। ‘‘याजं याजमटन्नवे तीर्थ-स्थानान्यपूजयत्।’’ शुद्ध निर्जंतुक रास्ते से चार हाथ आगे की जमीन को देखकर विहार करते हुए सूर्यप्रकाश में चलने की मुनि की प्रवृत्ति को ईर्यासमिति कहते हैं। गाड़ी या मोटर या रेल सवारी का त्याग त्यागी को इसीलिए होता है। श्री क्षेत्र कुन्डल से विहार करते-करते महाराज जिनमंदिर का दर्शन करते -करते नसलापुर, ऐनापुर, अथणी इस मार्ग से बीजापुर के पास अतिशय क्षेत्र ‘‘बाबानगर’’ को आये। पुण्यक्षेत्र के सहस्रफणी श्री पाश्र्वनाथ भगवान का दर्शन करते हुए लौटकर पुन: ऐनापुर आये। वहाँ वे १५ दिन तक ठहरे। यहां योगायोग से निग्र्रंथ मुनिराज श्री आदिसागर जी महाराज का सत्समागम मिला।
निपाणी संकेश्वर के समीप ‘‘यरनाळ’’ ग्राम में पंचकल्याणक महोत्सव के लिए मुनिराज श्री देवेन्द्रकीर्तिजी पधारे थे। ऐलक सातगौंडा महाराज भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने गुरु श्रीदेवेन्द्रकीर्ति स्वामी को दिगम्बर दीक्षा देने के लिए पुन: प्रार्थना की। एकत्रित जैन समाज को महाराजजी की योग्यता का पूरा परिचय था। वे महाराजजी से प्रभावित भी थे। मुनि दीक्षा के लिए समाजभर ने एक स्वर से अनुमोदना की।
निग्र्रंथ दीक्षा लेने का विचार निश्चित हुआ। दीक्षाकल्याणक के दिन तीर्थंकर भगवान का वन विहार का जुलूस दीक्षा वन में आया। इसी पवित्र समय में ऐलकजी ने भी दीक्षागुरु श्री देवेन्द्रकीर्ति महाराज के पास दिगम्बरी जिनदीक्षा धारण की। ‘नैग्र्रंथ्यं हि तपोऽन्यत्तु संसारस्यैव साधनम्’ यह दृढ़ धारणा थी। भगवान की दीक्षा विधि के साथ ऐलक महाराजजी की भी निग्रंथ दीक्षा विधि सम्पन्न हुई, केशलोंच समारम्भ भी हुआ। ऐलक सातगौंडा मुनि हो गये, यथाजातरूपधारी हुए। मुनि पद का नाम श्री ‘‘शांतिसागर’’ रखा गया। शक् सम्वत् १८४१ फाल्गुन शुक्ला १४ उनकी दीक्षामिति थी। इस पवित्र दिन से महाराज श्री का जीवनरथ अब संयम के राजमार्ग द्वारा मोक्षमहल की ओर अपनी विशिष्ट गति से सदा गतिशील ही रहा। अंतरंग में परिग्रहों से अलिप्तता का भाव सदा के लिए बना रहना और बाह्य में परिग्रह मात्र से स्वयं को दूर रखना यह मुनि की अलौकिक चर्या है। शुद्ध आत्मस्वरूप मग्नता यह उसका अन्तःस्वरूप होता है। देह के प्रति भी ममत्व का लेश नहीं होता, वे विदेही भावों के राजा होते हैं इसीलिए लोग उन्हें महाराज कहते हैं।
पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियों के विषयों पर विजय, छह आवश्यक तथा सात शेष गुण इत्यादि २८ मूलगुणों के ये धारक होते हैं।
यरनाळ में दीक्षासमारंभ समाप्त होने के अनंतर महाराज नसलापुर आये। समाज ने बड़ा आदर किया। भक्तिभावपूर्ण वैयावृत्य किया। उसके बाद महाराज कोगनोली पहुँचे। वहाँ से लौटकर फिर नसलापुर आकर चातुर्मास किया। बाद में महाराज ऐनापुर पहुँचे। यहां जैनसमाज बहुसंख्या में होने से धर्मप्रभावना अच्छी हुई। महाराजजी के विहार काल में कोण्णूर का चातुर्मास बड़ा महत्वपूर्ण रहा। यहां महाराज की जीवनी में अतिशय महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। कोण्णूर ग्राम में प्राचीन गुफाएं बहुसंख्या में हैं। नित्य की तरह गुफा में आचार्यश्री ध्यानस्थ बैठ गये। उसी समय एक नागराज-बड़ा सर्प वहाँ आकर महाराज जी के शरीर पर चढ़कर घूमने लगा। महाराज जी अपने आत्मध्यान में निमग्न थे। ‘नागराज आया है और वह अपने शरीर पर घूम रहा है’ इसका तनिक विकल्प भी महाराज जी को नहीं था। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति की पालना किस प्रकार हो सकती है इसका यह मूर्तिमानरूप दृष्टिगोचर हुआ। महाराज जी के दर्शनार्थ जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन्होंने यह घटना प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखी। वे साश्चर्य दिङ्मूढ़ हो बैठे रहे। वे सांप से डरते थे, सांप भी जनता से घबड़ाता था। महाराज का आश्रय इसीलिए उसने लिया था। महाराज जी का दिव्य आत्मबल देखकर वहाँ आये हुए यात्रियों में से प्रमुख श्रेष्ठी श्रीमान सेठ खुशालचंद जी पहाड़े और ब्र. हीरालाल जी बड़े प्रभावित हुए। दोनों सज्जन विचक्षण थे। दक्षिण यात्रा के लिए निकले हुए यात्री थे। मिरज पहुँचने के बाद पता चला कि निकट ही दिगम्बर साधु हैं। इसलिए परीक्षा के हेतु वे वहाँ पर पहुँचे थे। उनकी अपनी धारण थी इस काल में साधक का होना असंभव है। भरी सभा में ‘क्या आपको अवधिज्ञान है? या आपको ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त है?’’ आदि वैयक्तिक आचारविषयक प्रश्न भी पूछने लगे। कुछ उलाहना का अंश भी जरूर था। सम्मिलित भक्तगणों में कुछ ऐसे जरूर थे जो इन सवालों का जवाब मुट्ठियों से देने के लिए तैयार हो गये। मुनि महाराज ने भक्तों को रोका। एक-एक सवाल का जवाब यथानाम ‘‘शांतिसागर जी’’ ने शांति से ही दिया। समागत दोनों परीक्षक अत्यधिक प्रभावित हुए। उसी समय दीक्षा के लिए तैयार भी हो गये। महाराज जी ने ही उन्हें रोककर यात्रा पूरी करने का और कुटुम्ब परिवार की सम्मति लेने को कहा। जब महाराज बाहुबली (कुम्भोज) आये तब वहां आकर उक्त दोनों सज्जनों ने महाराज जी के पास क्षुल्लक पद की दीक्षा धारण की। दीक्षा के बाद श्री सेठ खुशालचंद जी क्षु. ‘चन्द्रसागर’ तथा ब्र. श्री हीरालाल जी का क्षु. ‘‘वीरसागर’’ नामावंâन हुआ। समडोली के चातुर्मास में आचार्यश्री के पास क्षु. वीरसागर जी ने निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण की। यही महाराज के प्रथम निग्र्रंथ शिष्य थे। आचार्यश्री ने आगे चलकर अपने समाधिकाल में श्री वीरसागर महाराज को ही उन्मुक्त भावों से आचार्यपद प्रदान किया। श्री वीरसागर जी की दीक्षा विधि हुई। कुछ ही समय बाद ऐलक नेमण्णा ने भी मुनिदीक्षा धारण की। नाम श्री ‘नेमिसागर’ रखा गया।
समडोली ग्राम में ही सर्वप्रथम आचार्यश्री का चतुःसंघ स्थापन हुआ। अब तक केवल अकेले महाराज ही निर्ग्रंथ साधु स्वरूप में विहार करते थे। अब संघ सहित विहार होने लगा। संघ ने उनको ‘आचार्य’ पद घोषित किया। आचार्य महाराज का संघ पर वीतराग शासन बराबर चलता था। संघ सहित विहार करते-करते महाराज कुम्भोज से श्री सिद्धक्षेत्र वुंâथलगिरी आये। क्षेत्र पर श्री देशभूषण और कुलभूषण मुनिद्वय के चरण पादुकाओं का पावन दर्शन किया। विहारकाल का उपयोग महाराजश्री जाप्य तथा मंत्र स्मरण के लिए विशेषरूप से कर लेते थे।
(चलता फिरता वीतरागता और विज्ञानता का विश्वविद्यालय)
ई. सन् १९२७ के मार्गशीर्ष वदी प्रतिपदा के दिन श्री सम्मेदशिखर जी क्षेत्र की वंदना और धर्मप्रभावना के उद्देश्य से आचार्यश्री १०८ शांतिसागर जी महाराज की विहारयात्रा संघ सहित बाहुबली (कुम्भोज) क्षेत्र से शुरू हुई।
बम्बई निवासी पुरुषोत्तम श्रीमान् सेठ पूनमचंद जी घासीलाल जी और सुपुत्रगण आचार्यश्री के पास पहुँचे। उन्होंने आचार्यश्री को ससंघ श्रीसम्मेदाचल यात्रा को ले चलने का संकल्प प्रकट किया।
नागपुर में संघ का अपूर्व स्वागत हुआ। जुलूस तीन मील लम्बा निकला था। शहर के बाहर इतवारी में स्वतंत्र ‘शांतिनगर’ की रचना की गयी थी। कांग्रेस के पंडाल से शांतिनगर का पंडाल कुछ छोटा नहीं था। जनता आज भी उस समय की अपूर्व घटनाओं की स्मृति से आनंद का अनुभवन करती है और स्वयं को धन्य मानती है।
संघ की विदाई हृदयद्रावक थी। साश्रुनयनों से श्रावक-श्राविकाओं को अनिवार्यरूप से विदाई देनी पड़ी। ता. ९ जनवरी १९२८ को संघ का नागपुर छोड़कर भंडारा मार्ग से विहार शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के भयंकर जंगलमय विकट मार्ग से निर्बाध होते हुए संघ हजारीबाग आया। बाद में फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन तीर्थराज श्रीसम्मेदशिखर जी सिद्धक्षेत्र को पहुँचा।
यहाँ पर संघपति जी के द्वारा व्यापकरूप में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव द्वारा महती धर्मप्रभावना हुई। भीड़ की सीमा न थी। भारत के कोने-कोने से श्रावक-श्राविकाएं अत्यधिक प्रमाण में पहुँचे। इसी समय हजार से ज्यादा कपड़ों की झोपड़ियां बनवायी गर्इं थीं। धर्मशालाएं खचाखच भर गर्इं।
तीर्थक्षेत्र कमेटी तथा महासभा आदि कई सभाओं के अधिवेशन भी हुए। तीर्थराज जयध्वनि से गूंज उठा था। धर्मशालाओं के बाहर भी यत्र-तत्र लोग अपना स्वतंत्र स्थान जमाए हुए नजर आते थे। नीचे धरती ऊपर आसमान, पूर्ण निर्विकल्प होकर जनता प्रतिष्ठा यात्रा के उन्मुक्त आनन्द रस का पान करती थी। लोग कहते हैं यात्री कहीं तीन लाख से ऊपर होंगे। अस्तु! पंडित आशाधरजी के शब्दों में कहना होगा, ‘‘दलित कलिलीला-विलसितम्’’ यही पर्वतराज का सजीव मनोहारी दृश्य था। अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा में व्यापक तत्व की एकता का होने वाला प्रत्यक्ष दर्शन अलौकिक ही था। निर्विकल्प वस्तु के अनुभव के समय विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव होता ही है ठीक इसी तरह सांस्कृतिक एकता का यह सजीव स्वरूप प्रभावशाली बन गया।
श्री सम्मेदशिखर की वंदना करके वहां से मंदारगिरी, चम्पापुरी, पावापुरी, राजगृही, गुणावां आदि अनेक सिद्धक्षेत्रों की संघ ने यात्रा की।
स्वर्गीय १०८ पायसागर जी महाराज आचार्य श्री को पारसमणि की उपमा देते थे। अपनी जीवनी के आधार से ही समादर की भावनाओं से वे अपने प्रवचनों में आचार्यश्री के विषय में गौरवगाथा गाते थे। स्व. आचार्यश्री वुंâथुसागर महाराज जी आचार्यश्री के शिष्यों में से उद्भट संस्कृतज्ञ प्रवक्ता रहे जिनके द्वारा गुजरात में विशेष प्रभावना हुई। आचार्यश्री वीरसागर जी और शिष्य परम्परा से जो जागरण का कार्य हुआ वह अविस्मरणीय एवं सातिशय ही है।
ता. ६ जनवरी १९३० में संघ धौलपुर स्टेट के राजाखेड़ा शहर में पहुँचा। तीन चार दिन तक महती धर्मप्रभावना हुई। यह धर्मप्रभावना भी एक अजैन भाई को सहन नहीं हुई। एक संगठन बन गया। लाठी, काठी, तलवार आदि शस्त्रास्त्रों के साथ करीब ५०० लोगों के आक्रमण की गुप्त योजना भी बन गई।
मृगमीनसज्जनानां तृणजल-संतोष-विहितवृत्तीनाम् ।
लुब्धक-धीवर-पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति।।
घास पत्ती पर अपना गुजारा करने वाले हिरन, जल में अपना निर्वाह करने वाली मछलियाँ और सन्तोषामृत का पान करने वाले साधु पुरुषों से भी शिकारी, मछलीमार और दुर्जन व्यर्थ ही शत्रुता करते हैं। यह सनातन दुष्टता की परंपरा संसार में चली ही आ रही है। इसका प्रत्युत्तर राजाखेड़ा में आया। छिद्दीलाल ब्राह्मण के नेतृत्व में आक्रमण की तैयारी हो गई थी। संघ का हत्याकाण्ड होने को ही था कि महाराज की अंतरंग स्वच्छता से अंतर्ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी संकेत मिला हो उन्होंने संघस्थ त्यागियों से प्रतिदिन की अपेक्षा शीघ्र आहार करके लौटने को कहा। तदनुसार समस्त त्यागी चर्या करके ९ बजे के भीतर ही मंदिर जी में वापिस लौट आये। आक्रामक लोग नारे लगाते हुए मंदिर जी की ओर बढ़े। जैनियों ने इस प्राणांतक आक्रमण का प्रतिकार भी किया। स्टेट की ओर से पुलिस सहायता भी दौड़ी हुई आयी। पुलिस दल ने आक्रामकों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन महाराज जी ने करुणाभाव प्रदर्शित कर उनको छोड़ देने के लिए पुलिस अधिकारी
मंडल को बाध्य किया।
जातिलिंगविकल्पेन येषां च समयाग्रहः।
तेऽपि न प्राप्नुवंति परम पदमात्मनः।।
अर्थात् जाति और वेष परिवेष का विकल्प साधना में पूरा बाधक एवं हेय होता है। इसी प्रकार तेरहपंथ या बीसपंथ के विकल्पों से आत्मसाधना अर्थात् परमार्थभूत धर्मसाधना अत्यन्त दूर होती है यह धर्मदृष्टि के अभाव का ही परिणाम है। टंकोत्कीर्ण धर्म साधना लुप्तप्राय होती जा रही है और तेरह-बीसपंथ के झगड़े दृढ़मूल बनाए जा रहे हैं और उन्हें धर्माचार का रूप दिया जा रहा है। समाज में आज भी जो भाई तेरह और बीसपंथ के नाम से समय-समय पर वितंडा उपस्थित करते हैं और समाज के स्वास्थ्य को ठेस पहुँचाते हैं उनकी उस प्रवृत्ति को जो समाज के लिए महारोग के समान है, हम समझते हैं आचार्यश्री का सामंजस्य पूर्ण दूरदृष्टिता का व्यवहार एक अद्भुत कल्याणकारी अमृतोपम रसायन हो सकता है।
ईसवी सन् १९३३ का चातुर्मास आचार्य संघ का ब्यावर (राज.) में था।
महाराज जी का अपना दृष्टिकोण हर समस्या को सुलझाने के लिए मूल में व्यापक ही रहता था। योगायोग की घटना है इसी चौमासे में कारंजा गुरुकुल आदि संस्थाओं के संस्थापक और अधिकारी पूज्य ब्र. देवचंद जी दर्शनार्थ ब्यावर पहुँचे। पूज्य आचार्यश्री ने क्षुल्लक दीक्षा के लिए पुन: प्रेरणा की। ब्रह्मचारी जी का स्वयं विकल्प था ही। वे तो इसीलिए ब्यावर पहुँचे थे। साथ में और एक प्रशस्त विकल्प था कि ‘‘यदि संस्था-संचालन होते हुए क्षुल्लक प्रतिमा का दान आचार्यश्री देने को तैयार हों तो हमारी लेने की तैयारी है।’’ इस प्रकार अपना हार्दिक आशय ब्रह्मचारी जी ने प्रगट किया। ५-६ दिन तक उपस्थित पंडितों में काफी बहस हुई। पंडितों का कहना था कि क्षुल्लक प्रतिमा के व्रतधारी संस्था संचालन नहीं कर सकते आचार्यश्री का कहना था कि पूर्व में मुनि संघ में ऐसे मुनि भी रहा करते थे जो जिम्मेदारी के साथ छात्रों का प्रबंध करते थे और ज्ञानदानादि देते थे। यह तो क्षुल्लक प्रतिमा के व्रत श्रावक के व्रत हैं। अंत में आचार्य महाराजजी ने शास्त्राधारों के आधार से अपना निर्णय सिद्ध किया। फलत: श्री ब्र. देवचंद जी ने क्षुल्लक पद के व्रतों को पूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार किया। आचार्य श्री ने स्वयं अपनी आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करते हुए दीक्षा के समय ‘‘समंतभद्र’’ इस भव्य नाम से क्षुल्लकजी को नामांकित किया और पूर्व के समंतभद्र आचार्य की तरह आपके द्वारा धर्म की व्यापक प्रभावना हो इस प्रकार के शुभाशीर्वादों की वर्षा की। कहाँ तो बाल की खाल निकालकर छोटी-छोटी सी बातों की जटिल समस्या बनाने की प्रवृत्ति और कहाँ आचार्यश्री की प्रहरी के समान सजग दिव्य दूरदृष्टिता ?
संघ विहार करता हुआ गजपंथा सिद्धक्षेत्र पर आया। यहाँ पर सम्मिलित सब जैन समाज ने आचार्यश्री को ‘‘चारित्रचक्रवर्ती’’ पद से विभूषित किया। महाराजश्री की आत्मा निरंतर निरूपाधिक आत्मस्वरूप के अमृतोपम महास्वाद को सहज प्रवृत्ति से बराबर लेने में परमानंद का अनुभवन करती थी। उन्हें इस उपाधि से क्या ? वे पूर्ववत् उपाधिशून्य स्वभावमग्न ही थे। साधु परमेष्ठी या आचार्य परमेष्ठी के आंतरिक जीवन का यथार्थ दर्शन यह चक्षु का विषय नहीं होता। वह अपनी शान का अलौकिक ही होता है। जहां जीवनाधार श्वासोच्छ्वास की तरह इन परमेष्ठियों का श्वांस आत्मा को स्वात्मा में स्थिर बनाये रखने के लिए होता है, वहाँ उच्छ्वास विश्व में अपनी आदर्श प्रवृत्ति के द्वारा शांति स्थापना में और धर्मप्रभावना में उत्कृष्ट निमित्त के रूप में उपस्थित होने के लिए होता है। आचार्यश्री की लोकोत्तम, लोकोत्तर अलौकिकता और वैभवशाली विभूतिमत्ता इसी में थी। ‘‘चारित्रचक्रवर्ती’’ उपाधि का महाराज को तो कोई हर्ष विषाद ही नहीं था। ‘‘चारित्र के चक्रवर्ती तो भगवान ही हो सकते हैं। हम तो लास्ट नम्बर के मुनि हैं। हमें उपाधि से क्या ? स्वभाव से निरूपाधिक आत्मा ही हमारी शरण है।’’ समाज ने अपनी गुणग्राहकता और त्याग संयम के प्रति निष्ठा का जो औचित्य-पूर्ण प्रदर्शन किया वह योग्य ही हुआ।
वर्षों से एक प्रशस्त संकल्प चित्त में था, जैसे मां के पेट में बच्चा हो। वह करुणा कोमल चित्त की उद्भट चेतना थी। महाराष्ट्र की जैन जनता प्रायः किस्तकार (किसान) है। धर्मविषयक अज्ञान की भी उनमें बहुलता है। आचार्यश्री का समाज के मानस का गहरा अध्ययन तो अनुभूति पर आधारित था ही। ‘शास्त्रज्ञान’ और तत्त्वविचार’ की ओर इनका मुड़ना बहुत ही कठिन है। प्रथमानुयोगी जनमानस के लिए एक भगवान का दर्शन ही अच्छा निमित्त हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर किसी अच्छे स्थान पर विशालकाय श्री बाहुबली भगवान की विशाल मूर्ति कम से कम २५ फीट की खड़ी कराने का प्रशस्त विकल्प जहां कहीं भी आचार्यश्री पहुँचते थे, प्रकट करते थे परन्तु सिलसिला बैठा नहीं। ‘भावावश्यं भवेदेव न हि केनापि रुध्यते’। होनहार होकर ही रहती है। योगायोग से इसी समय अतिशयक्षेत्र बाहुबली (कुंभोज) में वार्षिकोत्सव होने वाला था। ‘संभव है सत्य संकल्प की पूर्ति हो जाये’ इसी सदाशय से आचार्यश्री के चरण बाहुबली की ओर यकायक बढ़े। १८ मील का विहार वृद्धावस्था में पूरा करते हुए नांद्रे से महाराज श्री क्षेत्र पर संध्या में पहुँचे। पवित्र आन्दोल्लास का वातावरण पैदा हुआ। संस्था के मंत्री श्री सेठ बालचंद देवचंद जी और मुनि श्री समंतभद्र जी से संबोधन करते हुए भरी सभा में आचार्यश्री का निम्न प्रकार समयोचित और समुचित वक्तव्य हुआ। जो आचार्यश्री की पारगामी दृष्टि सम्पन्नता का पूरा सूचक था।
‘तुमची इच्छा येथे हजारो विद्याथ्र्यानी राहावे शिकावे अशी पवित्र आहे हे मी ओळखतो, हा कल्पवृक्ष उभा करून जाते। भगवंताचे दिव्य अधिष्ठान सर्व घडवून आणील। मिळेल तितका मोठा पाषाण मिळवा व लवकर हे पूर्ण करा।मुनिश्री समंतभद्राकडे वळून म्हणाले, ‘तुझी प्रकृति ओळखतो, हे तीर्थक्षेत्र आहे। मुनींनी विहार करावयास पाहिजे असा सर्वसामान्य नियम असला तरी विहार करूनही जे करावयाचे ते येथेच एके ठिकाणी राहून करणे। क्षेत्र आहे। एके ठिकाणी राहाण्यास काहीच हरकत नाही, विकल्प करू नको,काम लवकर पूर्ण करून घे। काम पूर्ण होईल! निश्चित होईल!! हा तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद आहे।’
आपकी आंतरिक पवित्र इच्छा है कि यहाँ पर हजारों विद्यार्थी धर्माध्ययन करते रहें इसका मुझे परिचय है। यह कल्पवृक्ष खड़ा करके जा रहा हूँ। भगवान का दिव्य अधिष्ठान सब काम पूरा कराने में समर्थ है। यथासंभव बड़े पाषाण को प्राप्त कर इस कार्य को पूरा कर लीजिये।’’ मुनि श्री समंतभद्र जी की ओर दृष्टि कर संकेत किया-‘‘आपकी प्रकृति (स्वभाव) को बराबर जानता हूँ। यह तीर्थभूमि है। मुनियों को विहार करते रहना चाहिए इस प्रकार सर्वसामान्य नियम है। फिर भी विहार करते हुए जिस प्रयोजन की पूर्ति करनी है उसे एक स्थान में यहीं पर रहकर कर लो। यह तीर्थक्षेत्र है एक जगह पर रहने के लिए कोई बाधा नहीं है। विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से कार्य शीघ्र पूरा हो सके पूरा प्रयत्न करना। कार्य अवश्य ही पूरा होगा सुनिश्चित पूरा होगा। आप सबको हमारा शुभाशीर्वाद है।’’
पूर्णिमा का शुभ मंगल दिन था। शुभ संकेत के रूप से पच्चीस हजार रुपयों की स्वीकृति भी तत्काल हुई काम लाखों का था। यथाकाल सब काम पूर्ण हुआ। ‘‘पयसा कमलं कमलेन पय: पयसा कमलेन विभाति सर:।’’ पानी से कमल, कमल से पानी और दोनों से सरोवर की शोभा बढ़ती है। ठीक इस कहावत के अनुसार भगवान की मूर्ति से संस्था का अध्यात्म वैभव बढ़ा ही है। अतिशय क्षेत्र की अतिशयता में अच्छी वृद्धि ही हुई। अब तो मूर्ति के प्रांगण में और सिद्धक्षेत्रों की प्रतिकृतियां बनने से यथार्थ में अतिशयता या विशेषता आयी है। महाराज का आशीर्वाद ऐसे फलित हुआ।
वि. सं. २००० (ई. सन् १९४४) की घटना है। आचार्यश्री का चौमासा कुंथलगिरि में था। पं. श्री सुमेरचंद जी दिवाकर से धर्मचर्चा के समय यह पता चला कि अतिशयक्षेत्र मूड़बिद्री में विद्यमान धवला, जयधवला और महाबंध इन सिद्धान्त ग्रंथों में से महाबंध ग्रंथ की ताड़पत्री प्रति के करीब ५००० सूत्रों का भागांश कीटकों का भक्ष्य बनने से नष्टप्राय हुआ। भगवान महावीर के उपदेशों से साक्षात् संबंधित इस जिनवाणी का केवल उपेक्षा मात्र से हुआ विनाश सुनकर आचार्यश्री को अत्यन्त खेद हुआ। आगम का विनाश यह अपूरणीय क्षति है। इनकी भविष्य के लिए सुरक्षा हो तो कैसी हो? इस विषय में पर्याप्त विचार परामर्श हुआ। अंत में निर्णय यह हुआ कि इन ग्रंथराजों के ताम्रपत्र किये जायें और कुछ प्रतियां मुद्रित भी हों।
प्रातःकाल की शास्त्र सभा में आचार्यश्री का वक्तव्य हुआ। संघपति श्रीमान् सेठ दाडिमचंद जी, श्रीमान् सेठ चंदूलाल जी बारामती, श्रीमान् सेठ रामचन्द जी धनजी दावडा आदि सज्जन उपस्थित थे। संघपति जी का कहना था कि जो भी खर्चा हो वे स्वयं करने के लिए तैयार हैं। फिर भी आचार्यश्री के संकेतानुसार दान संकलित हुआ जो करीब डेढ़ लाख हुआ।
‘‘श्री १०८ चा. च. शांतिसागर दि. जैन जिनवाणी जीर्णोद्धार संस्था’’ नामक संस्था का जन्म हुआ। ग्रंथों के मूल ताड़पत्री प्रतियों के फोटो लेने का और देवनागरी प्रति से ताम्रपट्ट कराने का निर्णय हुआ। नियमावली बन गई। कार्य की पूर्ति के लिए ध्रुवनिधि की वृद्धि करने का भी निर्णय हुआ। कार्य की पूर्ति शीघ्र उचितरूप से किस प्रकार हो इस विषय में पत्र द्वारा मुनि श्री समंतभद्र जी से परामर्श किया गया। ‘‘आर्थिक व्यवहार चाहे जिस प्रकार हो यदि कार्य पूरा करना है तो कार्यनिर्वाह की जिम्मेदारी किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के सुपुर्द करनी होगी। हमारी राय में श्रीमान् बालचंद जी देवचंद जी शाह बी.ए.को यह कार्य सौंपा जाये’’ इस सलाह के अनुसार कार्य की व्यवस्था बन गई। आचार्यश्री के संकेत को आज्ञा के रूप में श्री सेठ बालचंद जी ने शिरोधार्य कर कार्य संभाला। प्रतियों के मुद्रण तथा ताम्रपत्र के रूप में टंकोत्कीर्ण का कार्य श्रीमान् विद्यावारिधि पं. खूबचंद जी शास्त्री, श्रीमान् पं. पन्नालाल जी सोनी, श्रीमान् पं. सुमेरचंद जी दिवाकर, श्रीमान् पं.हीरालाल जी शास्त्री, पं. श्री माणिकचंद जी भीसीकर आदि विद्वानों के यथासंभव सहयोग से यह कार्य पूरा हो पाया; जिसमें ९ वर्षों का समय लगा।
कुंथलगिरि दक्षिण का सीमावर्ती सुन्दर सिद्धक्षेत्र है। ‘‘यहाँ पर एक विशालकाय बाहुबली भगवान की मूर्ति हो तो अच्छा होगा।’’ यह भव्य आशय कमेटी के सभी सदस्यों को एकदम पसंद आया। पूज्य आचार्यश्री के समक्ष कार्य पूरा होना असंभव था। महाराज जी ने यम सल्लेखना का नियम कर ही लिया था। इसी अवसर पर एक समाचार विदित हुआ कि दक्षिण में म्हैसूर स्टेट के अंतर्गत ‘‘बस्ती हल्ली’’ देहात में एक १५ फुट ऊँची मनोज्ञ मूर्ति है और वह एक अजैन भाई के खेत में करीब अज्ञात अवस्था में पड़ी हुई है, उसी को लाकर खड़ी करने का विचार किया गया। स्व. श्रीमान् सेठ रावजी देवचंद शहा आदि सज्जन स्वयं वहां पहुँचे। काफी प्रयास किया गया परन्तु सफलता नहीं मिल पायी। केवल फोटो मात्र मिल गया। उसे ही सिर पर रखकर आचार्यश्री ने धन्यता के भाव प्रगट किये। वीतरागता की साधना में परम वीतराग मूर्ति के दर्शन से अद्भुत आनन्द की और धर्मोल्लास की लहर होना सहज था। आचार्यश्री की चर्या पर वह दृग्गोचर हुई। आचार्य महाराज के भव्य भावों की पूर्ति होनी ही चाहिए इस प्रकार का भव्य भाव समीपवर्ती सेवाभावी सरल प्रकृति श्रेष्ठीवर्य श्रीमान् नेमचन्द जी मियाचंद जी गांधी, नातेपुते के चित्त में आया। ‘‘यदि महाराज जी की आज्ञा हो तो इसी क्षेत्र के ऊपर १८-२० फुट ऊँची बाहुबली भगवान की मूर्ति विराजमान करने का मेरा भाव है’’ इसके पश्चात् सन् १९७० में १८ फीट ऊँची बाहुबली भगवान की मूर्ति पहाड़ी के ऊपर पूर्वाभिमुख विराजमान होकर प्रतिष्ठा भी सम्पन्न हो गई। इस प्रकार एक तरह से महाराज के सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हुए।
जैनियों की दक्षिणकाशी फलटन नगरी धर्मकार्यों को उत्साह तथा उल्लास के साथ करती ही आ रही है। सन् १९५२ की घटना है। पूज्यश्री की जीवनी के ८० वर्ष पूरे हुए। इस प्रसंग से हीरक जयंती महोत्सव सम्पन्न करने का निर्णय एक स्वर से किया गया। आचार्यश्री को उत्सवों से कोई हर्ष विषाद नहीं था। एक तरह से त्याग तपस्या का ही यह गौरव होना था। जून की ता. १२, १३, १४ ये तीन दिन विशेष आनन्दोत्सव के रहे। सर्वत्र चहल पहल रही। भारत के कोने-कोने से हजारों भाई फलटण पहुँचे। इंदौर से रावराजा सेठ राजकुमार सिंह जी, रावराजा सेठ हीरालाल जी पहुँचे। बम्बई से सेठ रतनचंद जी, सेठ लालचंद जी, अजमेर से सेठ भागचंद जी, कलकत्ता, देहली, कोल्हापुर, नांदगांव, नागपुर, सिवनी, जबलपुर, बेलगांव, बाहुबली, सांगली, शेडवाल, भोज आदि शहरों से सज्जन उत्सव में सम्मिलित हुए। सभा सम्मेलन हुए, योजनाबद्धरूप से श्रद्धांजलियों का समर्पण हुआ, पूजा प्रभावना हुई। ताम्रपत्रों के ऊपर उत्कीर्ण धवलादि ग्रंथों का हाथियों के ऊपर जुलूस निकालकर वे ग्रंथ भक्तिभावपूर्वक पूज्य आचार्यश्री को समारोह के साथ समर्पण किये गये। छोटे-मोटे सब ही कार्यों में विशेष सातिशय सजीवता दिखलायी देती थी। स्वयं फलटन स्टेट के अधिपति श्रीमान् मालोजीवराव निंबालकर फलटन नगरी का यह अहोभाग्य समझते रहे। हीरक जयंती महोत्सव के निमित्त से एक सचित्र स्मरणिका प्रकाशित हुई। जिससे उत्सव का सचेतन स्वरूप सुस्पष्ट होता है। इस समय महाराजश्री के अनुभव रसपूर्ण हुए। ‘रत्नत्रयधर्म की साधना जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। धर्म से ही शेष पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं सफलता होती है’ ऐसे ही भावपूर्ण वक्तव्य हुए। आचार्यश्री जीवन के क्षणों का मूल्य बराबर जानते थे। उपचार और परमार्थ दोनों का परिज्ञान उन्हें बराबर था। सदा की भांति वे अपनी आत्मसाधना में विशेष तन्मय हुए। रत्नत्रयों के श्रेष्ठ आराधक रत्नत्रयों के अकम्प प्रकाश में अविचलरूप से सुस्थित थे। निग्र्रन्थ साधु की विशेषता के पुण्यदर्शन बराबर होते थे। आचार्य महाराज खूब जानते थे।
तिथिपर्वोत्सवा सर्वे, व्यक्ता येन महात्मना।
अतिथि ते ‘वजानीयात् शेषमभ्यागतं विदुः।।
सब ही तिथियाँ, पर्व और उत्सव सबंधी विकल्पों से ये महर्षि सदा ही दूर होते हैंं इसीलिए इनका यथार्थ नाम ‘अतिथि’ होता है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करने पर आत्मा तो यही कहती है कि महाराज वर्तमान युग के महान सत्पात्र तो रहे ही हैं परन्तु उनके द्वारा जो ज्ञानदान और दृष्टिदान हुआ है उससे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि महाराज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दानी भी रहे। पात्र समझकर जो चढ़ाया गया वह थोड़ा था और दाता समझकर जो कुछ समाज के द्वारा लिया गया वह भी थोड़ा था इस सत्य को स्वीकार करना होगा।
विचार और भावनाओं का समान संयोग आचार्यश्री के जीवन की एक विशेषता थी। भावनाओं में आकर शक्ति को व्यर्थ खोना या व्यर्थ खोने का विकल्प करना यह असंभव था। भविष्य की आशा में वर्तमान को गंवाना वे प्रकाश के बदले में अंधकार को खरीदना जैसा मानते थे। वर्षों से अखण्डरूप से की गयी हजारों मीलों की पदयात्रा, यथासंभव अनुकूल प्रतिकूल आहार का संयोग, उपवासों की धाराप्रवाहिता, वृद्धावस्था, अल्पनिद्रा आदि कारणों से दृष्टि में पूर्व की अपेक्षा अधिकाधिक मंदता का अनुभव होने लगा। वैद्य और डाक्टरों से समय-समय पर बराबर परामर्श होता था। शुद्ध उपचारों का विशुद्ध भावनाओं से अमल भी होता था। दृष्टि विनाश होने के बाद समितियों का पालन और प्राणस्वरूप मुनिचर्या असंभव है, इसलिए साधनों की सुरक्षा सावधानीपूर्वक अप्रमाद भाव से आचार्यश्री प्रारंभ से ही करते रहे। आचार्यश्री विनोद में शरीर की सवारी को घोड़ा कहा करते थे। जब घोड़े से काम लेना है और घोड़ा बराबर काम देता है तो उसे मात्रा में चना देना ही होगा। शरीर की या इन्द्रियों की गुलामी यह कोई अलग चीज होती है। विदेही भावनाओेंं के धनी चारित्र-चक्रवर्ती इस जन्म से प्राप्त घोड़े से ठीक काम लेना बराबर जानते थे। राणाप्रताप के ईमानदार ‘चेतक’ की तरह महाराजश्री की देह ने महाराज की आत्मा का पूरा साथ दिया परन्तु देहधर्म की अपनी प्रकृति है उसे शिथिल और कमजोर पाकर महाराजश्री बिल्कुल सचेत हो गये। शुरू में कांचबिन्दु बतलाया गया और अंत में डा. आरोसकरजी के द्वारा मोतियाबिंद के सुनिश्चित होने पर निर्विकल्परूप से सल्लेखना ही एकमात्र शरण है ऐसी अन्तरंग में दृढ़ धारणा हो गई।
समाधि, सल्लेखना, समाधिमरण, वीरमरण, मृत्यु महोत्सव ये ऐसे सार्थक शब्द हैं जो यह बतलाते हैं कि साधक किन पवित्र भावनाओं से सावधानीपूर्वक मृत्यु का सहज स्वागत करता है। शरीर का गल जाना, विनश जाना यह अटल प्रकृति है। वास्तव में जन्म जितना सत्य होता है उतनी ही मृत्यु सत्य होती है। परन्तु भोगी बहिर्दृष्टि लौकिक पुरुष जन्म का सहर्ष स्वागत करता है, आनन्द मनाता है और मृत्यु से डरता है, मुत्यु के नाममात्र से रोता है, यही विकल्प परायण अज्ञानी की अज्ञानता है। जन्म होना, छोटे से बड़ा होना, परिपुष्ट होना और अंत में गल जाना यही प्राणियों के प्राणों का स्वभाव होता है। जीवन का कोई विश्वास नहीं यह सब कोई कहते हैं और नित्य नये विकल्पों को करते भी जाते हैं, यही अज्ञानियों का अज्ञान है। महाराजजी ने अपने जीवन से पूरा काम लिया था। रसपूर्ण गन्ने का पूरा रस निकाला हुआ था। सारहीन भाग यदि ठीक ढंग से जलता हो तो उसमें शोक वृथा होता है, विकल्प निरर्थक होते हैं। वस्तुतत्त्व के आधार से संकल्प विकल्पों का परित्याग और आत्मस्वरूप स्थिरता यह समाधि या सल्लेखना की आत्मा होती है और आहार के क्रमश: विधिपुरस्सर परित्यागपूर्वक होने वाला देहविसर्जन यह समाधि का कलेवर होता है। शरीर की धारणा बनी रहना यह उपजीवन है और स्वरूप में अकंप स्थिरता यह आत्मा का जीवन है। यह दोनों का सुनिश्चित स्वरूप है वैसे ही जीवन के लिए उपजीवन होता है न कि उपजीवन के लिए जीवन यह पारस्परिक संबंध भी उतना ही निश्चित है। जीवन का यह सम्यग्दर्शन पूज्य महाराज जी की युवावस्था से ही यथार्थरूप में था इसलिए परलोक यात्रा की तैयारी सहर्ष भावना से पूरी हो गई थी। दिनाँक १८-८-५५ को महाराज जी का यम सल्लेखना का ज्यों ही निर्णय प्रगट हुआ, समाज भर को, देश भर को भूचाल जैसा धक्का लगा, जो स्वाभाविक ही था।
अन्न आहार के रूप में अंतिम ग्रास दिनाँक १८-८-५५ को दिया गया। ता. २६-८-५५ को मध्यान्ह में सल्लेखना विधि के अनुसार महाराजश्री के द्वारा क्षमायाचना का, क्षमा के आदान-प्रदान का भाव व्यक्त हुआ। यह सम्पूर्ण दृश्य अभिनव था। सभा में गंभीरता का वातावरण भर आया। उपचार विधि में पूरी परमार्थता किस प्रकार हो सकती है इसका वह मूर्तिमानरूप था। बस अब सदा के लिए अन्नाहार बंद हो गया। केवल पानी मात्र की छूट थी। आगे चलकर पानी का भी दिनाँक २८-८-५५ को परित्याग कर दिया। फिर भी मंदिरों के दर्शन, यथाशक्ति वंदना, अभिषेक, पूजा इत्यादि का अवलोकन, मंत्रस्मरण आदि में कोई खण्ड नहीं रहा। लोगों की बढ़ती हुई भीड़ का क्या कहना ? कुंथलगिरि की उस वीरान पहाड़ी का क्या कहना ? कुंथलगिरि की उस वीरान पहाड़ी में जनसागर उमड़ पड़ा। जिसको भी समाचार मिला और अनुकूलता मिली वह साधकोत्तम महापुरुष के अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचा। महासाधक की वह महायात्रा थी। सम्मिश्र भावनाओं का सम्मिश्र रसरूप दृगोच्चर होता था। जहाँ महाराजश्री स्वाभाविकरूप से सहज भावना से अपूर्व आनन्द रस में उन्मुक्त मन से अधिकाधिक मग्न होते हुए नजर आते थे। स्वनामधन्य शांतिसागर जी अथाह शांति के सागर में निमग्न थे। उसी समय जनता सागर शोक में डूबता हुआ दृष्टिगोचर होता था। वुंâथलगिरी का दृश्य कुछ अपूर्व था। बाहर की दुनिया में जैनाजैन समाचार पत्रों में अनुवूâल प्रतिवूâल समाचार साभिप्राय प्रगट होते ही थे। अपने विकल्पों को सबके लिए छूट होती ही है। व्यक्तिस्वातंत्र्य का युग है। कोई ‘‘जैन साधु की पवित्र महायात्रा’’ लिखता था कोई ‘‘जैन साधूची आत्महत्या’’ लिखता था। युद्ध में मृत्यु हो तो ‘‘वीरमरण’’ कहना। देशभक्त को यदि फाँसी हो तो उसे हुतात्मता कहना, यहां तक ही लौकिक दृष्टि की पहुँच हो सकती है। इससे भी बढ़कर साधक की समाधि हो सकती है इसका इनको क्या पता ? धर्म और अहिंसा जैसी पवित्र पवित्रतम वस्तुओं की वर्षों से समय असमय में बराबर खाल उतारी जाती है वहां सल्लेखना और समाधि जैसी अत्यंत पवित्र लोकोत्तम ‘‘व्रतशिरोरत्न’’ की जो छानबीन की चेष्टा ज्ञानी कहे जाने वाले अज्ञानियों के द्वारा हुई उसका क्या हिसाब ? पवित्रता की विडंबना ही मानो इस युग की विशेषता रही हो। जिसके पास सच्चा माप तोल ही नहीं, सूखी लकड़ियों के साथ गीली को और कोयले को ही तौलने का तराजू हो वह क्या, उनसे रत्नों का और जवाहरात का माप तोल कर सकता है ? धर्मकांटा कोई अलग वस्तु होती है, यही बात सच्ची है।
महाराजश्री की शांत स्वात्मनिर्भरता यथापूर्व हाथी की चाल से कदम कदम पर आगे के लिए बढ़ती ही जा रही थी। दिनाँक २२-८-५५ को महाराजश्री के संकेत से ही श्रीमान् सेठ बालचंद देवचंद शहा का ताम्रपट्ट तथा ग्रंथमालाओं से की गई श्रुतसेवा के लिए सभासंयोजनापूर्वक सत्कार किया गया और मानपत्र समर्पण किया गया। स्वयं महाराजश्री आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए।
शास्त्रों में सामायिक और छेदोपस्थापना का जो भी सूक्ष्म वर्णन आता है, निर्विकल्प शुुद्धात्म स्वरूप मग्नता और विकल्पों में से निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप में मग्न होने का जो सावधान प्रयत्न, इन दोनों अंतरंग प्रक्रियाओं का जराजर्जर तपस्याक्षीण देही महाराज की विदेही सावधान प्रवृत्ति में जो प्रत्यक्ष दर्शन हो पाया वह सुनिश्चित ही अद्भुत, अपूर्व, चैतन्यचमत्कारपूर्ण था। वैसे ही महाराज की निद्रा अत्यल्प थी। अब तो आत्मजागरण का सविशेष स्वरूप था। थकावट से निवृत्त होते ही ॐकार के उच्चारण से जागृति होती थी। उनका संकेत था ‘‘हमे औरों के द्वारा जगाने की आवश्यकता ही नहीं है।’’ हम हमारी आत्मा में, हमारे घर में पूर्ण सावधान हैं। सातिशय आत्मबल का ही प्रभाव समझना होगा। महाराज अंत तक परमात्म स्मरण कर पाये। णमोकार मंत्र का उच्चारण कर पाये। ऊँकार की वही अनुभव रसपूर्ण ध्वनि निकटवर्तियों को अन्त तक बराबर सुनने को मिली। भीतर ही सावधानता का और कौन सा बाहरी रूप हो सकता है? दिनाँक १८-९-५५ को भाद्रपद शुक्ल दूज रविवार प्रातःकाल ठीक ६ बजकर ५० मिनट पर महाराजश्री की परम पवित्र निरामय तपस्या से पुनीत आत्मा ‘‘ॐ सिद्धाय नम:’’ के उच्चारण के साथ अंतिम श्वास ले पायी। मोक्षमार्ग के साधक ने इस पर्याय की अपनी पवित्र जीवन यात्रा इस प्रकार पूरी कर परलोक यात्रा के लिए प्रस्थान कर लिया।
अब भक्तों के लिए आचार्य महाराज की केवल पुण्यस्मृति और तपस्या पुनीत देहमात्र शेष थी। विमान बनाया गया। जयनाद से आकाश गूंज उठा। श्रीमान् सेठ गोविन्दजी रावजी दोशी तथा सौ. कुमुदिनीबाई ने विमान यात्रा का बहुमान किया। विमानयात्रा के बाद दाहसंस्कार निर्धारित उसी स्थान पर हुआ जहां आज भी इस युग पुरुष की चरणपादुकाएं विद्यमान हैं। अब ऊपर से संगमरमर की सर्वांग सुन्दर छत्री भी बन गई है, प्रेरणा लेने वाले भक्तों के लिए चरण आज भी प्रेरणा दे रहे हैं।
(यह प्रकरण चा. च. आ. शांतिसागर शताब्दी स्मृति ग्रंथ से संग्रहीत है। इसमें जन्म तिथि आदि चारित्र चक्रवर्ती ग्रन्थ से ली गई है।)
आचार्यश्री की रत्नत्रय साधना अत्यन्त कठोर थी। वे शरीर को पूर्णरूपेण परद्रव्य समझकर उसे कभी-कभी ही आहार प्रदान करते थे। ३५ वर्ष के दीक्षित जीवन में आचार्यश्री ने २५ वर्ष से भी अधिक दिन उपवास में निकाले हैं जिनकी सूची निम्न प्रकार है-
१) १६ दिन का ३ बार ४८
२) १० दिन का १ बार १०
३) ९ दिन का ६ बार ५४
४) ८ दिन का ७ बार ५६
५) ७ दिन का ६ बार ४२
६) ६ दिन का ६ बार ३६
७) ५ दिन का ६ बार ३०
८) ४ दिन का ६ बार २४
९) अंतिम ३६ दिन तक के उपवास में स्वर्गवास ३६
योग-३३६ दिन
१. चारित्र शुद्धि व्रत १२३४
२. तीस चौबीसी व्रत ७२०
३. कर्मदहन व्रत (तीन बार) ४६८
४. सिंहनिष्क्रीड़ित व्रत (तीन बार) २७०
५. सोलहकारण व्रत (१६/१६) २५६
६. श्रुतपंचमी व्रत ३६
७. विहरमाण व्रत (२० तीर्थंकर व्रत) २०
८. दशलक्षण पर्व १०
९. सिद्धों के व्रत (८) ८
१०. अष्टाह्निका व्रत ८
११. गणधरों के व्रत २००
गणधरों के १४५२ उपवास होते हैं।
आचार्य श्री २०० ही कर पाये थे।
१२. अतिरिक्त व्रत ६३७२
आचार्यश्री ने सन् १९२० में निर्ग्रन्थ मुनि दीक्षा ली। इस समय से लेकर १९५५ तक के ३५ वर्षों में महाराज ने ६३३८ दिन उपवास किया। इसका अर्थ यह है कि ३६ वर्ष के मुनि जीवन के २५ वर्ष ७ मास अनशन में बीते। महाराज इतने दिन निराहार रहे। क्या इस कठोर उग्र तपस्या में आचार्यश्री की कोई बराबरी कर सकता है? नहीं। यह तो उनकी विशिष्ट आत्मशक्ति का प्रतीक है।
स्थान का नाम सन्
१. कागनोली १९२०
२. नसलापुर १९२१
३. ऐनापुर १९२२
४. कोन्नूर १९२३
५. समडोली १९२४
६. कुम्भोज १९२५
७. नांदडी १९२६
८. बाहुबली डोंगर१९२७
९. कटनी १९२८
१०. ललितपुर १९२९
११. मथुरा १९३०
१२. दिल्ली १९३१
१३. जयपुर १९३२
१४. ब्यावर १९३३
१५. उदयपुर १९३४
१६. गोरल १९३५
१७. प्रतापगढ़ १९३६
१८. गजपंथा १९३७
१९. बारामती १९३८
२०. पावागढ़ १९३९
२१. गोरल १९४०
२२. अकलूज १९४१
२३. कौरची १९४२
२४. डिग्गज १९४३
२५. कुंथलगिरि १९४४
२६. फलटन १९४५
२७. कवलाना १९४६
२८. सोलापुर १९४७
२९. फलटन १९४८
३०. कवलाना १९४९
३१. गजपंथा १९५०
३२. बारामती १९५१
३३. लोणंद १९५२
३४. कुंथलगिरि १९५३
३५. फलटण १९५४
३६. कुंथलगिरि १९५५
(१९५५ भादवा सुदी २ को स्वर्गवासी हुए)
http://hi.encyclopediaofjainism.com/index.php/
Image Ref: शालिणी पाटील परिवार
#AcharyaShriShantiSagarJiMaharaj1872DevendraKirtiJi
http://hi.encyclopediaofjainism.com/index.php/
Image Ref: शालिणी पाटील परिवार
चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्री १०८ शांति सागरजी महाराज
| Name | Phone/Mobile 1 | Which Sangh/Maharaji/Aryika Ji you are associated with |
|---|
आचार्य श्री १०८ देवेन्द्र कीर्तिजी महाराज Acharya Shri 108 Devendra Kirtiji Maharaj
Place Name
1. Kaganoli 1920
2. Nasalapur 1921
3. Anapur 1922
4. Konnur 1923
5. Samdoli 1926
4. Kumbhoj 1925
4. Nandi 1926
4. Bahubali donger 1926
4. Katni 1926
10. Lalitpur 1929
11. Mathura 1930
12. Delhi 1931
13. Jaipur 1932
14. Beawar 1933
15. Udaipur 1937
14. Goral 1935
14. Pratapgarh 1937
14. Gajapantha 1937
19. Baramati 1937
20. Pavagarh 1939
21. Goral 1960
22. Akluj 1971
23. Kaurchi 1962
26. Digs 1963
25. Kunthalgiri 1949
26. Fulton 1965
26. Kavalana196
26. Solapur 1949
29. Phaltan19
30. Kavalana 1979
31. Gajapantha 1950
32. Baramati 1951
33. Lonand 1952
37. Kunthalgiri 1953
35. Result 1957
37. Kunthalgiri 1955
http://hi.encyclopediaofjainism.com/index.php/
DevendraKirtiji
https://www.jinaagamsaar.com/aacharya/shantisagarc.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Shantisagar
https://padmavatmedia.newsreach.in/news/450582
https://jainmunilocator.org/munis.php?id=3
http://www.jambudweep.org-Book
https://www.jinaagamsaar.com/aacharya/shantisagarc.phphttp:/
/www.jinvaani.org/acharya-shri-shantisagar-ji.html
Image Ref: Shalini Patil Pariwar
Acharya Shantisagar was one of the greatest Jain teachers and scholars of the 20th century. He was the spiritual leader (acharya) of the Digambara Jain community. For over thirty-five years, from 1920 to his death in 1955, he wandered all over India. He as the first monk in several centuries to revive the tradition of wandering naked without even a begging bowl. He would eat only once a day, receiving food in his bare hands. He was a holy man who led by example and his actions are greatly admired by Jainas throughout the world.

Ref: This chart is taken from the book : Jain Digambaracharya: Prerak Sant avim Vichar, written by Dr.R.K.Jain (Kota)
Acharya,Muni and Aryika Dikshit by Acharya Shri Shanti Sagar Ji Maharaj
1.Muni Shri Vardhaman Sagar Ji Maharaj(South)
2.Muni Shri Chandrakirti Sagar Ji Maharaj
3.Muni Shri Malli Sagar Ji Maharaj
4.Muni Shri Dharm Sagar Ji Maharaj
5.Muni Shri Chandra Sagar Ji Maharaj
6.Muni Shri Uttam Sagar Ji Maharaj
7.Acharya Shri Adi Sagar Ji Maharaj(Shedbalkar)
8.Acharya Shri Nemi Sagar Ji Maharaj
9.Acharya Shri Nami Sagar Ji Maharaj
10.Aryika Shri Vidyavati Mata Ji
Shri ShantiSagar ji Maharaj contributed very much to uphold, strengthen and establish the traditions of Digambar traditions. He revived the character and some beliefs of Digambar Jain sect and that is why he is remembered and respected as the great saints of old age.
He was born in 1871 AD at Belgul village is in Belgaum District of South India.. His mother's name was Shrimati Satyavati (Satyabhama) and father's name was Shri Bhimgonda. His name was kept as Satgonda. From the very childhood, he was reserved detached from homely affairs and took active part in religious celebrations and rituals. He used to go to temple with his mother everyday. Mother always advised him and taught good things. He was, thus, invested with all virtues from his childhood.
Satgonda was married at the age of only nine years with a girl of six years of age but the girl died within six months of marriage. He was then pressed for second marriage but he clearly declined and observed complete, clear and holy celibacy for the whole of his life.
ShantiSagar Ji wanted to adopt Dixa at the age of 17 but he could not do so because his parents did not consent. Thus, he was totally detached with worldly lie right from his age of understanding. He used to sit at the cloth-shop of his father but dealt with total honesty and maintaining absolutely truthful behavior with all. He was careful not to be at lapses of integrity at any stage. Even while working at the shop he kept his mind in the service of the Lord, his prayers, self-study, company of saints and high thoughts. Since he was intending to adopt Dixa, his parents allowed him to observe certain vows, rules and non-eating but directed that he should not leave the house until they were alive. He used to sit at the shop more time but continued to think of eternal element.
At the age of 32, he went to the great pilgrimage of SamedShikharji. His longing for pilgrimage was very deep. In the memory of this pilgrimage he took vows not to eat ghee and edible oil for the whole of his life. He, thus, started his steps on the way of future mendicant ship. On return from pilgrimage he took a vow of only one time dining in a day. His father also took water and meals only for once in a day for 16 years. He accepted meditation-death and left the mortal body while muttering the name of Lord Arihant. Satgonda was of 37 at this time. His mother also passed away after three years by adopting meditation-death.
After this he stayed in house for some years and prepared himself for permanent Dixa. When Digambar Mooniraj Shri Devapa Swamy (Devendra Kirtiji Maharaj) came to Uttoor Village, Satgonda requested before him for Dixa. The learned saint explained him that it was a difficult path to be Nirgranth Dixa-holder (Possession less mendicant) and by sincere adoption of this Dixa, there is no fear for the soul to turn back to worldly affairs. Then after, as per the advice and guidance of Gurudev Devapa Swamy, Shri Satgonda took dixa in 1915 AD at the age of 43 in Uttoor village. He left everything after keeping only two clothes to wear and on begging bowl to ask for alms and to eat. He accepted the position of a minor mendicant. Satgonda was now free from the attachments of house and family. He was now worthless man named ShantiSagar. He kept away his attachments with the region of Bhoj Bhoomi and accepted the whole earth as his own nature place. He now started moving on earth seeking eternal freedom for him and for others. He suffered several large and minor troubles for long time and then he was steady in the quite sea of peace. He, on his way of moving from place to place came to the mountain Girnar that was holy with the footprints of Tirthankar Neminath. In this Holy Land Shri ShantiSagarji Maharaj adopted Elak Dixa as he was very much increased in his feelings of non-attachment.
Once moving in routine course, Maharaj came over to Parnal village where the celebrations of Panch Kalyan Pratishtha Mahotsava of Lord Jinendra-a big religious rite) were going on Digambar mendicant Shri Devendra Kirti Maharaj was also there. Shri ShantiSagarji Maharaj requested for Nirgranth Dixa-Possession less mendicantship by placing his head on his feet. The great teacher mendicant Devendra Kirti Maharaj explained him that this was as painful as walking on the edge of a sword, but ShantiSagarji Maharaj said that he had sufficient power of restraint, celibacy, sympathy, tolerance and truth and therefore, Devendra Kirti Maharaj invested him with the title of Mooni ShantiSagar by granting him higher stage of Dixa in the presence of thousands of followers and disciples on the holy day of Dixa-Kalyanak of Panch Kalyan Pratishtha Mahotsava, Maharaj ShantiSagar was of the age of 45 at this time. While maintaining his vows very strictly, he moved towards the south and expanded religion at all places through which he passed. He advised people to shun evil practices. By time, he became famous. He granted Dixa and vows to several Shravaks (Jain family-holders). In 1834, he regularly established Shraman Sangh at the time of Mooni Dixa of Shri Nemisagarji. The Jain community gave him the title of Acharya at his age of 52; and after 26 years in 1951 at the holy celebrations of Panch Kalyanak Pratishtha Mahotsava at Gajpantha in Maharashtra, Acharya Shri ShantiSagarji was given further award of Charitra Chakravarti.
In 1928, Acharya Shri Shantisagar ji started for the pilgrimage of SamedShikhar along with his disciples and followers. This was the first occasion after many centuries that a large group of possession less mendicants was moving in north India and there was a sharp wave of religious fervor in this region. He was honored at all places and Panch. Kalyanak Celebrations were also held at SamedShikhar. Lacs of devotees arrived there for this celebration from the whole of India. Acharya Shri walked about 35,000 miles in seven years and lacs of devotees had taken advantage of his spiritual knowledge. Maharaj Shri had cleared the way of Mooni-Vihar (movement of mendicants). The number of Acharyas, Moonis, small persons, women and celibates who had taken Dixa at the hands of AcharyaShri was about 3 to 400.
Once AcharyaShri came to know that a big volume of religious teachings collected from the preaching heard from time to time and completed by Swamy BhootBali was written an one thousand years old leaves and trees. It was then very old and was about to be destroyed by insects. He felt importance of preserving it and hence he proposed to get the whole book re-written on copper sheets so that it can remain totally secured for thousands of years. He requested the rich Jains to bear the costs and expenses for this task. Thus, Acharya Shri ShantiSagarji got these Agam books re-written on copper sheets and this was his most important work of his life. It will be noted by golden writings in the history of Shrutoddhar of invaluable books of Jainism i.e.. Re-writing of books, which were written, on leaves of trees by hearing the preaching of Jain saints & mendicants. Acharya had to face many difficulties in his life and he faced all the adverse circumstances with fearlessness, patience and tolerance. He has, thus, established his highest character and we are confirmed of his greatness. AcharyaShri was famous as charitra-chakravarti only because of his achievements and accomplishments for the up-life of Jainism.
Once Acharya Shri was performing Samayik (religious rite) in a cave. At this time, thousands and crores of red ants came up on his body and began to suck his blood by severely painful biting. AcharyaShri did not move for about two hours and went on suffering this pain. Afterwards, some Shravakas saw this and they removed the ants by throwing sugar nearby. Maharaj Shri opened his lips only after all the ants were gone away from him. AcharyaShri was performing noon-Samayik in the cave named Kagnoli. At this time a dangerous black snake came over his body and wrapped him. The snake was for more than 20 minutes in this position pressing the body of Acharyaji. Acharyaji, however, maintained Mauna- (non-speaking) and meditation. There have been many such instances in the life of Acharyaji wherein he has been proved to be victorious over rigorous physical pains and mental worries.
AcharyaShri had created deep impressions on common people by religious preaching and restrained life. Rulers of Sangli, Faltan, Kolhapur, Pratapgadh, Idar, Dholpur and other states used to come to see him. Even several European officers were also attracted towards Acharyaji. His preaching were highly philosophical; his thinking was of the highest level. He considered people of all religious equally. His disciples had also created very good impressions on the people. Acharya Shri ShantiSagarji adopted ultimate vow of Yam-Sannllekhana fast unto death at the closing years of his life. His welcome death was as good as putting up a golden pot on the top of temples. He had adopted 12 year vow of Sannllekhana in the presence of Lord Jinendra in the Gajpantha region and he had stopped taking food since then.
When his eye sight began to weaken in 1955 AD, he thought that it was then different for him to observe several vows like kindness to animals and several rules of daily routine life. He had, therefore, started preparations to adopt Sannllekhana Vow-fast unto death. In the first eight days, he took only two bits of food everyday. Then after he took only juice from black grapes for another eight days and after that he used to take water only. He took water at an interval of four days and sometimes after five and six days. This continued for about two months. When he was absolutely weak and unable even to stand without help from someone, he adopted Yama-Sannllekhana and stopped taking water till the end of his life. He did not take services from others even in his total weakness and continued to be in meditation of soul-salvation and muttering religion phrases and hymns.
In these days he was at Kunthalgiri holy place in Sangli District of Maharashtra. More than one lac of people took his Darshan within two months. People considered them to have been purified with his Darshan and held that their lives were fulfilled. Acharya Shri ShantiSagarji Maharaj breathed his last. It was September 18, 1955 AD. He had touched Jinendra Murti with his hand just before five minutes of his passing away and had moved his head towards his feet. He was muttering "Namah Siddhebhya: -"- respects to the Absolute when he breathed last.
Acharya Shri ShantiSagarji Maharaj was an ideal digambar jain saint who observed rigorous vows and restrained life with total celibacy for about forty years. He had won over his senses and had captured anger, greed, attachments, sensuality, pride desires with six enemies. His life was a lamppost for all mendicants, disciples and followers. He re-incarnated the Digambar traditions
https://www.jinaagamsaar.com/aacharya/shantisagarc.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Shantisagar
https://padmavatmedia.newsreach.in/news/450582
https://jainmunilocator.org/munis.php?id=3
http://www.jambudweep.org-Book
https://www.jinaagamsaar.com/aacharya/shantisagarc.phphttp:/
/www.jinvaani.org/acharya-shri-shantisagar-ji.html
Image Ref: Shalini Patil Pariwar
आचार्य श्री १०८ देवेन्द्र कीर्तिजी महाराज Acharya Shri 108 Devendra Kirtiji Maharaj
आचार्य श्री १०८ देवेन्द्र कीर्तिजी महाराज Acharya Shri 108 Devendra Kirtiji Maharaj
Place Name
1. Kaganoli 1920
2. Nasalapur 1921
3. Anapur 1922
4. Konnur 1923
5. Samdoli 1926
4. Kumbhoj 1925
4. Nandi 1926
4. Bahubali donger 1926
4. Katni 1926
10. Lalitpur 1929
11. Mathura 1930
12. Delhi 1931
13. Jaipur 1932
14. Beawar 1933
15. Udaipur 1937
14. Goral 1935
14. Pratapgarh 1937
14. Gajapantha 1937
19. Baramati 1937
20. Pavagarh 1939
21. Goral 1960
22. Akluj 1971
23. Kaurchi 1962
26. Digs 1963
25. Kunthalgiri 1949
26. Fulton 1965
26. Kavalana196
26. Solapur 1949
29. Phaltan19
30. Kavalana 1979
31. Gajapantha 1950
32. Baramati 1951
33. Lonand 1952
37. Kunthalgiri 1953
35. Result 1957
37. Kunthalgiri 1955
Charitrachakravarthy
#AcharyaShriShantiSagarJiMaharaj1872DevendraKirtiJi
DevendraKirtiji
DevendraKirtiji
1000
Charitrachakravarti Acharya Shri 108 Shanti Sagarji Maharaj
#AcharyaShriShantiSagarJiMaharaj1872DevendraKirtiJi
AcharyaShriShantiSagarJiMaharaj1872DevendraKirtiJi
You cannot copy content of this page