हैशटैग
#devsenjimaharaj

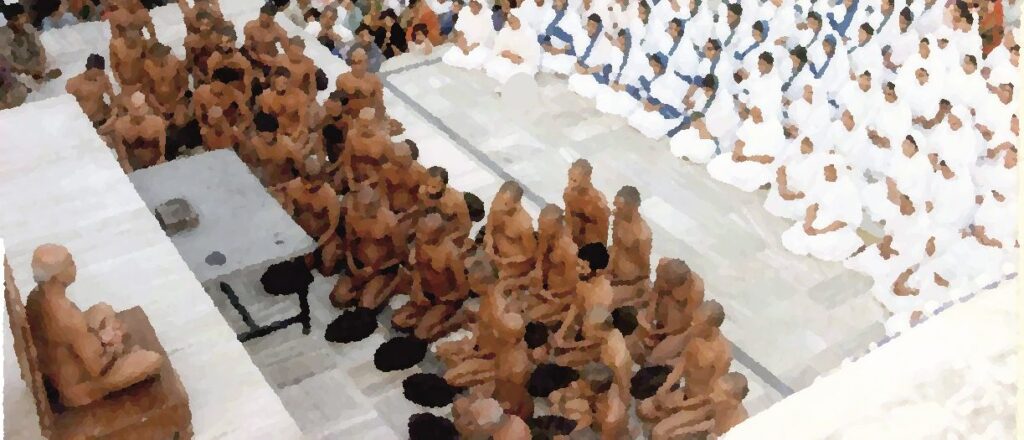
देवसेन नामके कई आचार्योक उल्लेख मिलते हैं। सारस्वसाचार्यों की परंपरा मे देवसेन का भी नाम आता है। एक देवसेन वे हैं, जिन्होंने विक्रम सं. ९९० में दर्शनसारनामक ग्रन्थकी रचना की थी। आलापपद्धति, लघुनयचक्र, आराधनासार और तत्त्वसार नामक ग्रन्थ भी देवसेनके द्वारा रचित हैं। इन सब ग्रन्थोंको दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी कृति माना जाता है। दर्शनसारके अन्त में प्रशस्तिरूप दो गाथाएँ आयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं-
पुव्वायरियकयाइं गाहाइं संचिऊण एयस्थ।
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसतेण।।
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए।
सिरिसासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुनदसमीए।।
अर्थात् पूर्वाचार्योंके द्वारा रची हुई गाथाओंको एकत्र करके यह दर्शनसार नामका ग्रन्थ श्री देवसेनगणिने माघ शुक्ला दशमी, विक्रम सं. ९९०में धारा नगरीमें निवास करते समय पार्श्वनाथ भगवानके मन्दिर में रचा, जो भव्य जीवोंके हृदय में हारके समान शोभा देगा।
तत्त्वसारकी प्रशस्तिमें बताया गया है-
सोऊण तच्चसारं रइयं मुणिणाहदेवसेणेण।
जो सद्दीट्टि भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं।
मुनिनाथ देवसेनने सुनकर तत्वसार रचा, जो सम्यकदृष्टी उसकी भावना करता है वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। आराधनासारके अन्त में बताया है-
ण य मे अस्थि कवितं ण मुणामो छंदलक्खणं कि पि।
णियभावणाणिमित्तं रइय आराहणासारं॥
अमुणियतच्चेण इमं भणियं जं कि पि देवसेणेण।
सोहंतु तं मुणिदा अस्थि हु जइ पवयण-विरुद्धं।।
न मुझे कनिका परिज्ञान है, न जाना और न मान तुगाका ही। अपनी भावनाके निमित्त मैंने आराधनासार रचा है। पूर्णतत्त्वज्ञानसे अपरिचित देवसेनने जो कुछ भी इसमें कहा है यदि उसमें आगमविरुद्ध कथन हो तो मुनीन्द्र उसे शुद्ध कर लें।
इस तरह देवसेनने दर्शनसारमें रचनाकाल और रचना स्थानका निर्देश किया है किन्तु अन्य रचनाओंमें रचना-काल और रचना-स्थानका निर्देश नहीं है। दर्शनसारमें देवसेनने अपनेको देवसेनर्माण कहा है और तत्त्वसारमें मुनिनाथ देवसेन कहा है तथा आराधनासारमें केवल देवसेन। गणि और मुनिनाथपदको एकार्थवाचक मान लेने पर एकरूपता आ सकती है।
भावसंग्रहके अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी रचनामें गुरुके नामका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता है, पर प्रकारान्तरसे गुरुके नामका अध्याहार किया जा सकता है। आराधनासारकी मङ्गलमाथामें "विमल गुणसमिद्ध" पदके द्वारा, दर्शनसारमें "विमलणाणं" पद द्वारा, नयचक्र में "विगयमलं" और "विमलणाण संयुक्तं" पोंके द्वारा गुरुके नामका उल्लेख माना जा सकता है। अत: आराधनासार, दर्शनसार, भाव-संग्रह आदिके रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। दर्शनसार और भाव-संग्रह तो एक ही व्यक्तिकी रचनाएँ हैं क्योंकि श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें दी गयी गाथाओंमेंसे एक गाथा ज्यों-की-त्यों है और अन्य गाथाओंके भाव प्राय: मिलते हैं। यहाँ तुलनाके लिए कुछ गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं। यथा-
छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
सोरठ्ठे उप्पण्णो सेवडसंघो हु वलहीए।।
आसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भद्दबाहुणामेण।
जाणिय सुणिमित्तधरो भणिओ संघो णिओ तेण।।
होहइ यह दुन्भिवखं बारह वरसाणि जाम पुण्णाणि।
देसंतराई गच्छह णिणियसंघेण संजुत्ता।।
सोऊण इमं वयणं णाणादेसेहिं गणहरा सव्वे।
णियणियसंघपउत्ता विहरीमा अत्य सुभिक्खं।।
दर्शनसारमें श्वेताम्बरमतकी उत्पत्ति निम्न प्रकार बतायी है-
छत्तीसे वरिस-सए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
सोर बलहीरा नप्पणो मेवहो संघो।।
सिरिभद्दनाहगणिणो सीसो णामेण संति आइरिओ।
तस्स य सीसो वो जिणचंदो मंदचारितो।
तेण कियं मयमेयं इत्योणं अस्थि तब्भवे मोक्खो।
केवलणाणीण पुणो अद्दक्खाणं तहा रोओं॥
इन गाथाओंकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रन्थोंका रचयिता एक ही व्यक्ति है।
पण्डित परमानन्दजी शास्त्री दिल्लीका अभिमत है कि 'भावसंग्रह' 'दर्शनसार’ के रचयिता देवसेनकी कृति नहीं है, क्योंकि 'दर्शनसार' मूल संघका ग्रंथ है, उसमें काष्ठासंघ, द्रविडसंघ, यापनीयसंघ और माथुरसंघको जैनाभास घोषित किया है। पर 'भावसंग्रह’ केवल मूलसंघका ही मालूम नहीं होता, क्योंकि उसमें "त्रिवर्णाचार’ के समान आचमन, सकलीकरण और पन्चामृताभिषेक आदिका विधान है। इतना ही नहीं, अपितु इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, पवन, यक्ष और ऐशान आदि दिग्पाल देवोंको सशस्त्र और युवतिवाहन सहित आह्वानन करने, बलि, चरु आदि पूजा द्रव्य तथा यज्ञके भागको बीजाक्षरयुक्त मन्त्रोंसे देनेका विधान है। अतएव पं. परमानन्दजीने बताया है कि अपभ्रंश-भाषाके 'सुलोचनारित'के रचयिता देवसेन ही 'भावसंग्रह’ के कर्ता हैं। इनके गुरुका नाम भी विमलसेनगणि है।
श्री प्रेमीजीने भी उनके इस मतको प्रायः स्वीकार करते हुए लिखा है "एक और प्राकृत ग्रन्थ 'भाव संग्रह' है, जो विमलगणिके शिष्य देवसेनका है। यह भी मुद्रित हो चुका है। इसमें कई जगह 'दर्शनसार'की अनेक गाथाएँ उद्धृत हैं। इसपरसे हमने अनुमान किया था कि 'दर्शनसार’ के कर्ता ही इसके कर्ता हैं, परन्तु परमानन्दजी शास्त्रीने (अनेकान्त वर्ष ७ अंक ११-१२ में) इस पर सन्देह किया है और सुलोचनाचरिउके कर्ता तथा भावसंग्रहके कर्ताको एक बतलाया है, जो कि विमलगणिके शिष्य हैं।''
'सुलोचनाचरिउ' में उसके रचना-कालका निर्देश करते हुए लिखा है कि संवत्सरकी श्रावण शुक्ला चतुर्दशीके दिन यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ। पं. परमानन्दजीने ज्योतिष गणनाका प्रमाण देते हुए उक्त कालको विक्रम संवत् ११३२ तथा ११९२ में पड़ता हुआ लिखा है।
पता नहीं पं. परमानन्दजीने किस आधारपर यह ज्योतिष गणना को है। राक्षस-संवत्सर श्रावण शुक्ला चतुर्दशीको ग्रह-लाघवके गणितानुसार वि. सं. १०१२ में आता है। यो राक्षससंवत्सरकी स्थिति वि. सं. ९५२, १०१२, १०७२, ११३२ और ११९२ में आती है, पर श्रावणशुक्ला चतुर्दशीको राक्षस संवत्सरका योग विक्रम सं. १०१२ के अतिरिक्त १३७२ में आता है। इसके बीचके संवत्सरोंमें बार्हस्पत्य गणनानुसार राक्षससंवत्सर और श्रावण शुक्ला चतुर्दशीकी स्थिति एक साथ घटित नहीं होती है। अतः अनुमान है कि दर्शनसार, भावसंग्रह और सुलोचनाचरिउ इन तीनों ग्रंथोंका कर्ता एक देवसेन नहीं है। श्री जगलकिशोर मुख्तारने श्री पं. परमानन्दजीको समालोचना करते हुए लिखा है-
"अतः भावसंग्रहके कर्ता देवसेन उनसे पहले हुए, तब सुलोचनाचरिउके कर्ता देवसेन और पाण्डवपुराणकी गुरुपरम्परावाले देवसेनके साथ उनकी एकता किसी भी तरह स्थापित नहीं की जा सकती और न उन्हें १२वीं १३वों शताब्दीका विद्वान ही ठहराया जा सकता है। इसलिए जब तक भिन्न कर्त्तुत्वका द्योतक कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण सामने न आ जाने, तब तक दर्शनसार और भावसंग्रहको एक ही देवसेनकृत मानने में कोई खास बाधा मालूम नहीं होती"।
मुख्तार साहबके इस कथनसे स्पष्ट है कि सुलोचनाचरिउ १४ वी शतीके किसी देवसेनका है। भावसंग्रह और दर्शनसार एक हो कर्ताकी रचनाएँ हैं।
श्री पं. परमानन्दजी का यह तर्क कि 'दर्शनगार’ मुलसंघका ग्रंथ है और 'भावसंग्रह' मूलसंघसे इतर संघका ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पञ्चामृत अभिषेक आदिकी विधि प्रतिपादित की गयी है, अधिक सबल नहीं है, क्योंकि काष्ठासंघमें, जो कि मूलसंघके समान ही मान्य था, पञ्चामृत- अभिषेक आदिका विधान किया है।
श्री प्रेमीजीने दर्शनसारके अन्तर्गत आये हुए संघोकी समीक्षा करते हुए लिखा है कि दर्शनसारमें आये हुए चार संघोंमें यापनीयसंघको छोड़ शेष तीन संघोंका मूलसंघसे इतना पार्थक्य नहीं है कि वे जैनाभास बतला दिये जायें। दर्शनसारकी रचना वि. सं. ९९० में की है। भावसंग्रह, आराधनासार और तत्त्वसार इनकी रचना दर्शनसारके बाद की गयी है । अत: हमारा अनुमान है कि दर्शनसार देवसेनकी सबसे पहली रचना है। इस रचनाके समयमें वे कट्टर मूलसंघी रहे होंगे। पर पाँच-दस वर्षके बीच उनके विचार और अधिक परिपक्व हुए तथा के काष्ठासंघी आचार्योंके सम्पर्क में पहुँचे, जिससे उन्होंने प्रभावित होकर वि. सं. १००५ के. लगभग भावसंग्नह लिखा।
श्री मुख्तार साहबने श्री पं. नाथूरामजी प्रेमीके मतको उपस्थित करते हुए लिखा है- "इसके प्रारम्भिक अंशमें अन्य ग्रंथोंके उद्धरणोंकी भरमार है, जो मूल ग्रंथकारके द्वारा उद्धत नहीं हुए हैं और अनेक स्थानोंपर- खासकर पांचवें गुणस्थानके वर्णनमें- इसके पद्योंकी स्थिति रयणसार जैसी सन्दिग्ध पायी जाती है। अतः प्राचीन प्रतियोंको खोज करके इसके मूलरूपको सुनिश्चित करनेकी खास जरूरत है।
एक और तर्क भी विचारणीय है कि प्राकृत भाषाके ग्रंथोंकी रचनाके पश्चात ही अपभ्रंशमें रचनाएँ लिखी जाती हैं। कोई भी लेखक प्रथम प्राकृत और संस्कृतमें रचना करता है, तत्पश्चात् अपनशमें। जो लेखक तीनों भाषाओंमें ही रचनाओंका प्रणयन करते हैं, वे प्रथम प्राकृत अनन्तर संस्कृत और तत्पश्चात अपभ्रंशमें ग्रन्थ लिखते हैं। अतएव देवसेनने भी प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशमें रचनाओं का प्रणयन किया होगा। उनकी सरस्वती-आराधनाका काल वि. सं. ९९० (ई सन् ९३३) से वि. सं. १०१२ (ई. सन् ९५५) तक है। अतएव दर्शनसार, भावसंग्रह, आराधनासार, तत्वसार आदि ग्रन्थोंके रचयिता विमलसेनगणिके शिष्य देवसेनगणि हैं।
१. दर्शनसार,
२. भावसंग्रह,
३. आलापपति,
४. लघुनयचक्र,
५. आराधनासार,
६. तत्त्वसार।
१. दर्शनसार- इस लघुकाय ग्रन्थमें कुल ५१ गाथाएँ हैं। प्रथम गाथामें श्लेषमें गरुका स्मरण करते हुए तीर्थंकर महावीरको नमस्कार किया है और पूर्वाचार्यों द्वारा कथित गाधाओंका संग्रह किया है। उत्थानिकाके अनन्तर समस्त इतर दार्शनिक मतोंका प्रवर्त्तक ऋषभदेवके पुत्र मरीचिको माना है। मरीचिने एकान्त, संशय, विपरीत, विनय और अज्ञान इन पांचों एकान्त मार्गों का प्रवर्तन किया है। बताया है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथके तीर्थकालमें सरयू नदीके तटवर्ती पलाश नामक नगरमें पिहितास्रव साधुका शिष्य बुद्धि कीर्तिमुनि हुआ, जो बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था। मत्स्याहारके कारण बह दीक्षासे भ्रष्ट हो गया और रक्ताम्बर धारण कर उसने एकान्तमतका प्रचलन किया। फल, दधि, दुग्ध, शक्कर आदिके समान मांसमें भी जीव नहीं है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करने में कोई पाप नहीं है। उसमें बतलाया की जिस प्रकार जल एक द्रव पदार्थ है, उसके सेवनमें दोष नहीं उसी प्रकार मद्य भी द्रव पदार्थ है, उसके सेवन में भी किसी प्रकारका दोष नहीं है।
एक पाप करता है और फल दुसरा भोगता है। इस प्रकार अनर्गल सिद्धान्तोंका प्रचार कर वह बुद्धकीर्ति नरक गया। कर्ता कोई अन्य व्यक्ति है और फल-भोक्ता कोई अन्य। इस सिद्धान्तमें क्षणिकवादका कथन किया गया है। इस प्रकार मरीचि और बुद्धीर्तिने मिथ्या मतोंका प्रचार किया।
इस अवतारणके पश्चात् श्वेताम्बर मत, विपरीत मत, वाचनिक मत, अज्ञान मत, द्राविड़संघ, यापनीयसंघ, काष्ठासंघ, माधुरसंघ और भिल्लकसंघकी उत्पत्ति एवं समीक्षा की गयी है। काष्ठासंघकी समीक्षा करते हुए वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेन, कुन्दकुन्द, गुणभद्र, विनयसेन, कुमारसेनके निर्देश आये हैं। कुमारसेनको काष्ठासंघका उपदेशक बतलाया है और इस संघका उत्पत्ति काल वि. सं. ७५३ माना है। माथुरसंघकी उत्पत्ति रामसेन द्वारा वि. सं. ९५३ में मथुरा नगरीमें मानी गयी है। भिल्लकसंघकी उत्पत्ति भविष्य-कल्पनाके रूपमें अङ्कित है-
पणमिय वीरजिणिदं सुरसेणणमंसियं विमलणाणं।
बोच्छं दंसणसारं जह कहियं पुव्वसूरीहि।
भरहे तिथयराणं पणमिय देविंदणागरुडाणं।
समएसु होंति केई मिच्छत्तपवट्टगा जीवा॥
सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो।
पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बुड्डकित्तिमुणी।।
णदियडे वरगामे कुमारसमो सत्यपिणः।
कट्ठो दंसणभट्टो जादो सल्लेहणाकाले॥
तत्तो दुसए तीदे महुराए माहुराण गरुणाहो।
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वणियं तेण।
दर्शनसारसे देवसेनके अक्खड़ स्वभावका पता चलता है। उन्होंने अन्तिम गाथामें अपनी स्पष्टता व्यक्त करते हुए लिखा है-
रूसउ तूसउ लोओ सच्चं अक्खंतयस्स साहुस्स।
कि जूयभए साडी विज्जियव्वा णरिदेण।।
सत्य कहने वाले साधुसे कोई रुष्ट हो, चाहे सन्तुष्ट हो, इसकी चिन्ता नहीं। क्या राजाको युका (जूआ) के भयसे वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं।
इससे देवसेनका अक्खड़पना प्रकट होता है।
२. भावसंग्रह
इस ग्रन्यमें ७०१ गाथाएँ हैं। इसमें चौदह गुणस्थानोंका अवलम्बन लेकर विविध विषयोंका निरूपण किया गया है। दो गाथाओं द्वारा १४ गुणस्थानोंके नाम बतला कर मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप प्रतिपादित किया है। मिथ्यात्वके एकान्त, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत इन पांच भेदोंको बतलाकर ब्राह्मण मतको विपरीतमिथ्यादृष्टि कहा है-
मण्णाइ जलेण सुद्धि तित्ति मंसेण पियरवग्गस्स।
पसुकयवहेण सग्गं घम्म गोजोणिफासेण॥
जह जलण्हाणपउता जोवा मुइ णिययपावेण।
तो तत्व वसिय जलयरा सव्वे पावंति दिवलोयं।।
जं कम दिढबद्धं जीवपएसेहि तिविहजोएण।
तं जलफासणिमित्ते कह फट्टइ तित्थाण्हाणेण।।
मलिणो देहो णिच्वं देही पुण णिम्मलो सयारुवी।
को इह जलैण सुज्झइ तम्हा ण्हाणे ण हु सुद्धी॥
जलसे शुद्धि होती है, मांससे पितरोंकी तुसि होती है, पशुबलिसे स्वर्ण मिलता है और गोयोनिके स्पर्शसे धर्म होता है, इन चार ब्राह्मणधर्मके प्रमुख सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए बताया है कि जलस्नानसे यदि समस्त पापोंका प्रक्षालन सम्भव हो, तो नदी, समुद्र और तालाबोंमें रहनेवाले जलचर जीव भी स्वर्गको प्राप्त कर लेंगे। कर्म मैलसे मलिन इस आत्माको जलसे शुद्धि नहीं हो सकती है, जो जलसे शुद्धि मानता है, वह अच्छा विचारक नहीं है। आत्माकी शद्धि तप, इन्द्रियनिग्रह और रत्नत्रयके द्वारा होती है। जिस प्रकार अग्निके संयोगसे स्वर्ण पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार अनशन, ऊनोदर आदि तपोंके करनेसे जीव भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति विषय और कषायमें संलग्न हैं और राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले गृहकार्योंमें आसक्त हैं उनकी जलस्नानसे शुद्धि नहीं हो सकती। कषायरहित, प्रतनियम और शीलसे युक्त व्यक्ति जल स्नानके बिना भी आत्माको पवित्र कर सकता है।
माँसद्वारा पितरोंकी तृप्ति मानने वाला व्यक्ति भी विवेकी नहीं है। हिंसा, कृरता और निर्दयता करने वाला व्यक्ति चारों गतियोंके दुःखोंको उठाता है। जो मांस द्वारा श्राद्ध करके पितरोंकी ताप चाहता है वह व्यक्ति भी बालूसे तेल निकालना चाहता है। अतएव मांसको न तो दान ही माना जा सकता है, और न इससे पितरोंकी तृप्ति ही हो सकती है।
जो श्राद्धद्वारा पितरोंकी तृप्ति मानता है, वह भ्रममें है। किसीके भोजनसे किसीकी तृप्ति नहीं हो सकती। यदि पित्ता भोजन करता है, तो पुत्रका पेट नहीं भरता, और पुत्र भोजन करता है तो पिताका पेट नहीं भरता। जो भोजन करता है, वही तृप्त हो सकता है, अन्य कैसे तुप्त हो सकता है? जो यह मानता है कि पाप करके नरक जाने पर पिताको पिण्डदानद्वारा पुत्र स्वर्ग भेज सकता है, उसके यहाँ जो कार्य करने वाला है उसे फल न मिल कर अन्यको होगा। अतः कृतनाश और अकृताभ्यागम नामक दोष आयगा। इस प्रकार उक्त चारों सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए गीता, महाभारत आदि ग्रन्थोंसे ही समर्थन के लिए प्रमाण उद्धृत किये हैं।
विपरीतमिथ्यात्वके पश्चात् एकान्तमिथ्यात्वकी समीक्षा की गयी है। इस प्रसंगमें क्षणिककान्तवादी बुद्धका खण्डन किया है। वैनायिक मिथ्यात्वके निरसनमें यक्ष, नाग, दुर्गा, चण्डिका आदिके पूजनेका निषेध किया है। संशयमिथ्यात्वका निरूपण करते हुए उदाहरणके हेतु श्वेताम्बर मतका निरसन किया गया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीमुक्ति, केवली कवलाहार और साधुओंका वस्त्र पात्र रखना इन तीनों बातोंकी आलोचना की गयी है। श्वेताम्बर अपने साधुओंको स्थविरकल्पी बतलाते हैं। ग्रन्थकारके मतसे वे स्थविर नहीं, बल्कि गृहस्थकल्पी हैं। जिनकल्प और स्थविरकल्पका विवेचन विस्तार पूर्वक किया है। इस सन्दर्भमें बताया है-
दुद्धरतवस्स भग्गा परिसहविसएहि पौडिया जे य।
जो गिहकप्पो लोए स थविरकप्पो कओ तेहि॥
अर्थात् परीषहसे पीड़ित और दुर्द्धर तपसे भीत बनोने गृहस्थकल्पको स्थविर कल्प बना दिया है। १३७ वी गाथासे श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा दी गयी है। इस कथामें बताया है कि सौराष्ट्र देशकी बलभी नगरी में वि. सं. १३६ में श्वेताम्बर संघकी उत्पत्ति हुई। दर्शनसारमें भी श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिका यही समय अंकित किया गया है।
अज्ञानमिथ्यात्वका कथन करते हुए लिखा है कि भगवान पार्श्वनाथके तीर्थकल्पमें मस्करीपूरण नामक ऋषि हुआ। यह भगवान महावीरके समवचरणमें गया, किन्तु उसके जानेपर भगवानकी वाणो नहीं खिरी। वह रुष्ट होकर समवशरणसे चला आया और कहने लगा-मैं ग्यारह अंगोंका धारी हूँ, फिर भी मेरे जाने पर तीर्थंकर महावीरकी दिव्यध्वनि प्रवाहित नहीं हुई और गौतमके आने पर दिव्यध्वनि होने लगी। गौतमने अभी दीक्षा ली है। वह तो वेदवादी पण्डित है। वह जिनोक्त श्रुतको क्या जाने। अतः उसने अज्ञानसे लोगोंके मध्य मोक्षका उपदेश दिया-
अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणो हु।
देवो ण अत्थि कोई सुण्णं झाएह इच्छाएँ।
अर्थात् अज्ञानसे ही मोक्ष होता है। इसके लिये ध्यान, संयम, तप, सज्ञान की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार पांचों मिथ्यात्वोंकी समीक्षा करनेके पश्चात् चार्वाकके द्वारा मान्य दर्शनकी समीक्षा की है। चार्वाक चैतन्यको भूतोंका विकारमात्र मानता है। ग्रन्थकारने इसे कोलिकाचार्यका मत कहा है-
कउलायरिओ अक्खइ अत्थि ण जीवो हु कस्स तं पावं।
पुण्णं वा कस्स भवे को गच्छइ णरय-सग्गं वा।।
यह कोलिकमत शैवतन्त्रका एकमत है। एक प्रकारसे यह वामाङ्गो है। माँस, मदिराके सेवनके साथ स्त्रिरमण एवं स्वयं शिव-पार्वतीका प्रतिरूपक अपनेको मानना आदि इसके सिद्धान्त हैं। यहाँ हमें ग्रंथकारका भ्रम प्रतीत होता है। कौलिक और चार्वाक ये दोनों मत स्वतन्त्र हैं। दोनोंमें समता इतनी है कि पुण्य-पाप, परलोक आदिकी स्थिति दोनोंमें तुत्य है। कौलिक मतके ग्रन्योंमें वामाचारकी भी पुण्यरूप कहा गया है तथा वाममार्गीधर्माचरणसे स्वर्गादिक सुखोंकी उपलब्धि भी मानी गयी है। शिव और पार्वती रूप कृत्य-अकृत्योंका संकल्प कर लेने पर कहीं कोई बाधा नहीं आती और स्वर्गादिक प्राप्त हो जाते हैं।
चार्वाकमतके पश्चात् सांख्यमतकी समीक्षा की गयी है। बताया है कि जीव सदा अकर्ता है और पुण्य-पापका भोक्ता भी नहीं है। ऐसा लोकमें प्रकट करके बहन और पुत्रीको भी अंगीकार किया गया है। यथा-
जीवो सया भकत्ता भूत्ता ण हु तुम गलस्म।
इय पयडिऊण लोए गहिया वहिणी सधूया वि।।
धूयमायरिवहिणि अण्णावि पुत्तस्थिणि।
आयति य पासवयणुपयडे वि विप्पे।
जह रमियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पे॥
बंभणि-छिपिणि-डोंवि-नडिय-वरुडि-रज्जइ-चम्मारि।
कवले समइ समागमइ तह भूति य परणारि।।
अर्थात् पुत्री, माता, बहन या अन्य कोई भी नारी पुत्रोत्पत्तिको भावनासे कामवचन प्रकट करे, तो कामातुर हो वेदज्ञानी ब्राह्मणको उसका उपभोग करना चाहिये। लेखकने बतलाया है कि कपिलदर्शनमें प्रतिपादित ब्राह्मणी, डोम्बी, नटी, घोबिन, चमारिन आदि परनारियोंके साथ भोग करना उचित है।
स्मृतिकारोंके इस कथनका आशय लेकर कि जो पुरुष स्वयं भागता नारीका भोग नहीं करता उसे बह्महत्याका पाप लगता है; को लक्ष्य में रखकर ही उक्त कथन किया गया है। सांख्यदर्शनके साथ इसका कुछ भी मेल नहीं है। हाँ, कौलिक सम्प्रदायमें उक्त सिद्धान्त अवश्य स्वीकृत है। राजशेखरने अपनी 'कर्पूरमंजरी-सट्टक’ में रण्डा, चण्डा आदिके भोगका औचित्य बतलाया है। अतः कपिलदर्शनका यह सिद्धान्त न होकर, स्मृति या कौलिक सम्प्रदायका सिद्धान्त है। देवसेनने इसी सिद्धान्तकी समीक्षा को है।
तुतीय मिश्रगुणस्थानका कथन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी समालोचना की गयी है। ब्रह्माकी आलोचना करते हुए तिलोत्तमा आदिके उपाख्यानोंको उपस्थित किया है। विष्णकी आलोचनामें उनके विभिन्न अवतारोंकी समीक्षा की गयी है। रुद्रकी आलोचनामें उनके स्वरूप और ब्रह्महत्या आदि कार्योंकी समीक्षा आयी है।
चतुर्थ अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए सात तत्त्वोंका कथन किया गया है। पांच गुणस्थानका स्वरूप २५० गाथाओंके द्वारा बहुत विस्तारसे बतलाया है। इसमें अणुव्रत, गुणव्रत, और शिक्षाव्रतोके साथ अष्टमूलगुणोंका भी उल्लेख आया है। चार प्रकारके ध्यान, देवपूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, आदि श्रावकाचारका भी निरूपण आया है। अभिषेकके समय यम, वरुण, कुवेर, ईशान आदिके आह्वानपूर्वक पन्चामृत-अभिषेक करनेका विधान किया है।
षष्ठ व सप्तम गुणस्थानके स्वरूपकथनमें पिण्डस्थ, पदस्थ रूपस्थ, और रूपातीत ध्यानोंका कथन आया है। शेष गुणस्थानोंका सामान्यतया स्वरूपविवेचन हुआ है। गणस्थानोंके स्वरूपकथनमें देवसेनने पंचसंग्रहप्राकृतसे अनेक गाथाएँ ज्यों-को-त्यों रूपमें ग्रहण की हैं। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने गोम्मटसारमें पंचसंग्रहकी अनेक गाथाएँ ग्रहण की हैं। यहाँ तुलनाके लिए कतिपय सामान गाथाएँ दी जाती हैं-
मिच्छो सासण मिस्सो अविरयसम्मो य देसविरदो य।
विरओ पमत्त इसरो अपुव्व अणियट्टि सुहमो य।।
उपसंत खीणमोहे सजोइकेलिजिणो अजोगी य।
ए चउदस गुणठाणा कमेण सिहा य णायव्या।।
णो इंदिएसु विरोओ णो जीवे थावरे तसे वा पि।
जो सद्दहइ जिणुतं अविरइसम्मो त्ति णायव्वो।
इस प्रकार अनेक गाथाएँ पंचसंग्रहमें प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, भाव संग्रहकी कई गाथाएँ कुछ रूपान्तरके साथ राजशेखरकी कर्पूरमंजरीमें भी मिलती हैं। कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें पंचसंग्रह और धवलाटीकाका मिश्रित रूप है।
जे तसवहाउ विरदो णो विरओ अवखथावरवहाओ।
पडिसमयं सो जोवो बिरयाविरओ जिणेक्कमई।।- गाथा १३
जो तसबहादु बिरदो अविरद तह य थावरवहाओ।
एक्कसमम्मि जीवो विरदाविरदो जिणेवकमाई।।- गाथा ३१
जो तसवहाउ विरओ णो विरओ तह य थावरवहाओ।
एक्कसमर्याम्म जीवो विरयाविरज त्ति जिणु कहई।।- गाथा ३५१
भावसंग्रहपर कुन्दकुन्दाचार्य के पञ्चास्तिकाय ग्रंथका भी प्रभाव है-
जीवो त्ति हवदि वेदा उचओयविसेसिदो पहूं कत्ता।
भोत्ता य देहमेतो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो।।
पाणेहि चदुहिं जीवदि जीवरसदि जो हु जीविदो पुव्वं।
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासो।।
जीवो अणाइ णिच्चो उवओगसंजुदो देहमित्तो य।
कत्ता भोक्ता चेता ण हु मुत्तो सहावउड्ढगई।।
पाणचउक्कपउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पुव्वं।
जोवेइ वट्टमाणं जीवत्तगगुण समावण्णो॥
स्पष्ट है कि भावसंग्रहपर पञ्चास्तिकायका भी प्रभाव है।
३. आराधनासार
एकसी पन्द्रह प्राकृत-गाथाओंमें यह ग्रंथ रचा गया है। आराधनाओंका वर्णन करते हुए बताया है-
आराहणाइसारो तव-दंसण-णाण-चरणसालानी।
सो दुम्भेओ उत्तो ववहारो चेन पप।।
अर्थात् तपाराधना, दर्शनाराधना, झानाराधना और चारित्राराधना इन चारों आराधानाओका सार इसमें गिर रहेगा। माइ माराधनामगर दो प्रकारका है- (१) व्यवहार और (२) परमार्थ। व्यवहार-आराधनाका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि सूत्र और अर्थ द्वारा कथित वस्तुको ग्रहण करना ज्ञानाराधना है। अर्थात् तीर्थंकरकी वाणी द्वारा प्रतिपादित ११ अंग और १४ पूर्वोको अवगत करना ज्ञानाराधना है। मावशुद्धिपूर्वक १३ प्रकारके चारित्रका आचरण करना चारित्राराधना है। १३ प्रकारके चारित्रमें ५ महाव्रत, ५ समिति ओर ३ गप्तीको स्थान दिया गया है। १२ प्रकारके तपोंका आचरण करनेके लिए प्रवृत्त होना तपाराधना है। इस प्रकार व्यवहार-आराधनाका स्वरूप कथन कर निश्चय-आराधनाफा स्वरूप बसलाते हुए लिखा है-
सुद्धणये चउखंध उत्तं आराहणाइ परिसिय!
सम्ववियप्पविमुक्को सुद्धो अप्पा णिरालंबो।।
अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सपरूप इन चारों भेद- विकल्पोंका त्याग कर पञ्चेन्द्रियके विषयसुखसे रहित निर्विकल्प आत्मतत्वका आराधन करना निश्चय-आराधना है। आगे इसीके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन करते हुए बताया है-
सद्दहइ सहावं जाणइ अप्पाणमामणो सुद्धं।
तं चि य अणुचरइ पुणो इंदियविसए णिरोहिता।
अर्थात् स्वस्वरूपका श्रद्धान करना, शुद्ध आत्माको जानना और निज आत्मरूप आचरण करना एवं निज स्वरूप तपश्चरण करना निश्चयाराधना है। निश्चय-आराधनामें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ रुक जाती हैं और आत्मस्वरूप श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और तपाराधना होने लगती है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपरूप आत्मा ही है, जो राग-द्वेष छोड़कर इस शुद्ध आत्माका आराधन करता है उसीकी निश्चय-आराधना होती है।
जीव चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, भ्रमण करेगा और भ्रमण किया है। इसका कारण ज्ञानमयो आत्माराधनको प्राप्त न करना है। मरणकालमें वही व्यक्ति आत्माराधन कर सकता है जो राग-द्वेष रहित है। बताया है-
अप्पसहावे णिरओ वज्जियपरदव्वसंगसुक्खरसो।
णिग्गहियरायदोसो हवई आराहमो मरणे॥
जो रयणत्तयमइओ मुत्तूणं अप्पणो विसूदप्पा।
चितेइ य परवव विराहओ णिच्छयं भणियो।
राग-द्वेषोंको दूर कर और परद्रव्योंके संयोगजन्य सुखका त्याग कर जो आत्मस्वभावमें निरत है वहीं मरण-कालमें आराधक होता है। जो रत्नत्रय मयी विशुद्ध आत्माको छोड़कर परद्रव्योंका चिन्तन करता है वह आराधनाका विराधक माना जाता है। जो न सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्ररूप आत्माकी समझता है और न आत्मासे विलक्षण शरीरादि परद्रव्योंको ही जानता है, उसे न ज्ञानकी प्राप्ति रहती है और न आराधनाकी हो।
जब तक वृद्धावस्था नहीं भाती है, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, बुद्धि नष्ट नहीं होती है, आयरूपी जल समाप्त नहीं होता है तब तक आत्मकल्याणके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचता रहता है कि अभी तो युवावस्था है, विषयसुख-सेवनके दिन हैं वह वृद्धावस्था आने पर कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपरूप आराधनाकी प्राप्ती शारीरिक शक्ति और इन्द्रियोंकी शक्ति रहने पर ही सम्भव है। बताया है-
जरवग्घिणी ण चंपइ जाम ण वियलाइ हुति अक्खाई।
बुद्धी जाम ण णासइ आउजलं जाम ण परिगलाई।
जा उज्जमो ण वियलइ संजम-तत्र-णाण-झाणजोएसु।
तावरिहो सो पुरिसो उत्तमठाणस्स संभवई।
बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रहका त्यागकर अन्तरक कषाय और विकारोंको कुश करनेका प्रयास करना ही वास्तविक आराधना है। कषाएँ अत्यधिक शक्तिशाली हैं। इन्हींके कारण चतुर्गति परिभ्रमण होता है। जब तक कषाय और भोगोंका त्याग नहीं किया जायेगा, तब तक संयमकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है और संयमरहित व्यक्तिके गुण विशुद्ध नहीं हो सकते। बताया है-
जाम ण हणइ कसाए सकसाई णेव संजमी होई।
संजमसहियस्स गुणा ण हूंति सव्वे विसुद्धियरा।
जो परीषहोंको सहन करता हुआ शान्तिभावपूर्वक व्रत, समिति और गुप्तियोंका पालन करता है वह अनादिकालीन काम-क्रोधादिको नष्ट कर देता है। इस प्रसङ्गमें उपसर्ग और परीषहोंको सहन करनेवाले शिवभूति, सूकुमाल और सुकोशलके उदाहरण दिये गये हैं और मनुष्यकृत उपसर्ग सहन करने में गुरुदत्त, पाण्डव और गजकुमारके आख्यान दृष्ट्वान्तके रूपमें प्रस्तुत किये हैं। देवकृत उपसर्गके सहन करने में प्रसिद्ध हुए श्रीदत्त, सुवर्णभद्र आदिके उदाहरण दिये गये हैं। इस प्रकार उदाहरणों और प्रत्युदाहरणों द्वारा सैद्धान्तिक विषयको भी सरस बनानेकी चेष्टा की है।
मन, वचन और कायको वश करनेकी आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा है-
सिक्सह मणवसियरणं सवसीहूएण जेण मणुआणं।
णासंति रार-दोसे तेसिं णासे समो परमो।।
मनको वश में करनेको शिक्षा देनी चाहिए। जिसका मन वशीभूत है वही राग-द्वेषको नाश कर सकता है और राग-द्वेषके नाश करनेसे ही परमपदकी प्राप्ति होती है।
उपशमवान जीव ही मनका निग्रह कर सकता है और मनका निग्रह करनेसे ही आत्मा परमात्मापदकी प्राप्त कर सकती है।
आचार्यने ध्यान, ध्याता और ध्येयका लक्षण बतलाया है और ध्यानके द्वारा ही सकल कर्मोका नाश होता है। अतः राग-द्वेष, मोहका विनाश करने पर ही ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है। जो यह अनुभव करता है कि न मैं देह हूँ, न मन हूँ और न मुझमें दुःख ही है वह क्षपक समभावनासे युक्त होकर दुःखका विनाश कर लेता है। यथा-
णाई देहो ग मणो ण तेण में अत्थि इत्थ दुक्खाई।
समभावणाइ जुत्तो वि सहसु दुक्खं अहो खवय।।
इस प्रकार समस्त परिग्रहका त्यागकर आत्मसाधनामें संलग्न रहनेका निर्देश किया है।
४. तत्त्वसार
इस ग्रन्थमें ७४ गाथा हैं। तत्वके मूलत: दो भेद है- (१) स्वगत तत्व और परगत तत्व। स्वगत तत्व निजात्मा है और परगत तत्वमें परमेष्ठी हैं। स्वगत तत्वके भी दो भेद है- (१) सविकल्पक और (२) निर्विकल्पक। आस्त्रवसहितको सविकल्पक कहते हैं और आस्त्रवरहितको निर्विकल्पक। इन्द्रियविषय- सुख के समाप्त होनेपर मनकीको चंचलता जब अरुवद्ध हो जाती है तब आत्मा अपने स्वरूपमें निर्विकल्प हो जाता है। यथा-
जं पुणु सगयं तच्चं सवियप्प हबइ तह य अवियप्पं।
सवियप्पं सासवयं णिरासर्व विमयसंकप्पं।।
इंदियविसविरामे मणस्स णिल्लूरणं हवे जइया।
तझ्या तं अविअप्प ससख्ये अप्पणो त तु॥
जो अविकल्पक सत्व है वही मोक्षका कारण है। उसीको शुद्ध समझकर ध्यान करना चाहिए।
इस प्रकरणमें श्रमण और योगीकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है- "मन वचन-कायसे जो बाह्म और आभ्यन्सर परिग्रहसे रहित है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है और जिसने जिनलिमा आश्रय ग्रहण किया है वह श्रमण कहलाता है-
बहिरव्भतरगंथा मुक्का जेणेह तिविहजोएण।
सो णिग्गंधी भणिओ जिणलिंगसमासिओ सवणों।।
लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, मित्र-शत्रुको जो समानरूपसे ध्यान करता है वह योगी है। यथा-
लाहालाहे सरिसो सुहदुक्खे तह य जीविए मरणे।
बंधव-अरयसमाणो झाणसमत्थो हु सो जोई॥
जो व्यक्ति आत्माकी सिद्धि करना चाहता है वह ध्यान द्वारा कर्मोंका क्षय कर मोक्षको प्राप्त करे। यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप है, असंख्यात प्रदेशी है और प्रदेशोंके संहार तथा विसर्पणके कारण यह शरीरप्रमाण है जो राग, द्वेष, मोहका त्याग कर जन्म-जरा-मरणसे रहित इस निरञ्जन आत्माका ध्यान करता है वह सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। आत्मामें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न शब्द है। यह तो शुद्ध चेतनस्वरूप निरञ्जन है। यथा-
फासरसरूवगंधा सद्दादीया य जस्स गरिय पुणो।
शुद्धो चेयणभावो णिरंजणो सो अहं भणियो।
व्यवहारनयसे इस आत्मामें कर्म-नोकर्म माने जाते हैं। आत्मा और कर्मका सम्बन्ध दूध-पानीके समान है। जिस प्रकार दूध और पानी अपने-अपने स्वभावसे विकृत होकर एकमें एक मिल जाते हैं उसी प्रकार आत्मा और पौद्गलिक कर्म भी अपने-अपने स्वभावको छोड़ एकमें एक मिल गये हैं। अतएव में शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ज्ञानरूप हूँ, कर्म-नोकर्मसे रहित हूँ, एक हूँ, निरालम्ब हूँ, देहप्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यातदेशिक हूँ, अमर्त हूँ। इस प्रकार चिन्तन कर आत्म स्वरूपको प्राप्त करना चाहिए। जब तक पर द्रव्योंसे चित्त व्यावृत्त नहीं होता तब तक भव्यजीव मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी उग्र तप क्यों न करता रहे। आत्मसिद्धिका मूलकारण राग-द्वेष और विषयसुखसे मुक्ति प्राप्त कर लेना है।
यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है तथा इसमें आत्मानुभूति तथा आत्मसिद्धिका उपाय वर्णित है।
५. लघुनयचक्र
इस ग्रन्थमें ८७ गाथाएँ हैं । नयका स्वरूप, उपयोगिता एवं उसके भेद प्रभेदोंका वर्णन किया है । नयका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-
जं णाणीण वियप्पं सुयभेयं वत्यूयंससंगहण।
ते इह णयं पउत्तं णाणी पुण तेहि णाणेहि॥
जो वस्तुके एक अंशका ग्रहण करता है श्रुतज्ञानका वह भेद नय कहलासा है। नयके बिना वस्तुस्वरूपकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है और नय द्वारा ही स्याद्वादका ज्ञान होता है। अतः नयका ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुकी प्रतिपत्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। नयसे जिन वचनोंका बोध होता है और नयसे ही वस्तुकी प्रतिपत्ति होती है। भूल नय दो है- द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। नयके सामान्यतया नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत ये सात भेद हैं। अन्य भेद निम्न प्रकार हैं-
दव्वत्थं दहमेयं छब्भेयं पज्जयत्थियं यं।
तिविहं च णेगमं तह दुविहं पुण संगहं तत्थ।।
ववहार रिउसुतं दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का।
उत्ता इह णयमेया उपणयभेया वि पभणामो॥
द्वव्यार्थिकके १० भेद, पर्यायार्थिकके ६ भेद, नैगम नयके तीन भेद, संग्रहके दो, व्यवहार और ऋतुसूत्रके दो-दो भेद और शेष नयोंका एक-एक भेद है। उपनयके तीन भेद हैं- (१) सद्भुत, (२) असद्भुत और (३) उपचरित नय। सद्भुतके दो भेद हैं और असद्भुत के तीन तथा उपचरितके तीन। इस प्रकार नयके भेद-प्रभेदोंका कथन कर द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंकी अपेक्षासे वस्तु-विवेचन किया गया है।
६. आलाप-पद्धति
यह संस्कृत-गद्यमें रचित छोटी-सी रचना है। अन्य ग्रंथोंके समान इसका प्रकाशन भी माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमालासे हुआ है। इस ग्रंथमें गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नय, गुण-व्यत्पत्ति, स्वभाव-व्युत्पत्ति, प्रमाणका कथन, निक्षेपको व्युत्पत्ति, नयोंके भेदोंको व्युत्पत्ति एवं अध्यात्मनयोंका कथन किया गया है। आरम्भमें वचनपद्धतिको ही आलापपद्धति कहा है। यह ग्रन्थ निम्नलिमित अधिकारों में विभक्त है-
१. द्वव्याधिकार,
२. गुणाधिकार,
३. पर्यायाधिकार,
४. स्वभावाधिकार,
५. प्रमाणाधिकार,
६. नय-अधिकार,
७. गुण व्युत्पत्ति अधिकार,
८. पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार,
९. स्वभावव्युत्पत्ति-अधिकार,
१०. एकान्तपक्षमें दोष,
११. नययोजना,
१२ प्रमाणकथन,
१३. नयलक्षण और भेद,
१४. निक्षेप व्युत्पत्ति,
१५. नयोंके भेदोंकी व्युत्पत्ति,
१६. अध्यात्मनय।
नामानुसार विषयोंका निरूपण इन अधिकारोंमें किया गया है। जैन सिद्धान्तकी अवगत करनेके लिए यह छोटा-सा ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। द्रव्यके सामान्य और विशेष गुणोंका विवेचन करते हुए लिखा है-
"अस्तित्वं, वस्तुत्त्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्व मचेतनत्वं, मूर्त्तत्वममूर्तत्वं द्रव्याणां दश सामान्यगुणाः। प्रत्येकमष्टावष्टो सर्वेषाम्।”
[एकैकद्रव्ये अष्टौ अष्टौ गुणा भवंति। जीवद्रव्ये अचेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति, पुद्गलद्रव्ये चेतनत्वममूर्तत्वं च नास्ति, धर्माधर्माकाशकालद्रव्येषु चेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति। एवं द्विद्विगुणजिते अष्टौ अष्टौ गुणाः प्रत्येकद्रव्ये भवन्ति।]
ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि स्पर्शरसगंधवर्णा: गतिहेतुत्वं स्थितिहेतुत्वमवगाहन हेतुत्वं वर्तनाहेतुत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं मूर्तस्वममूर्तत्वं द्रव्याणां षोडश विशेष गुणा:।
"अर्थात् अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रभेयत्व, अगुरुलवुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सामान्यगुण हैं। सदेव द्रव्योंके साथ रहते हैं, द्रव्योंसे पृथक् नहीं होते। प्रत्येक द्रव्यमें दश सामान्य गुणोंमेंसे आठ-आठ गुण रहते हैं, दो-दो गुण नहीं होते। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेषगुण हैं।"
इस प्रकार द्रव्य, गुण, स्वभावके अतिरिक्त नय और प्रमाणका भी विवेचन किया है।
सारस्वसाचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।
सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-
१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।
२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।
३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।
४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।
५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।
६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन।
७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन।
सारस्वताचार्यों में सर्वप्रमुख स्वामीसमन्तभद्र हैं। इनकी समकक्षता श्रुत घराचार्यों से की जा सकती है। विभिन्न विषयक ग्रन्थ-रचनामें थे अद्वितीय हैं।
देवसेन नामके कई आचार्योक उल्लेख मिलते हैं। सारस्वसाचार्यों की परंपरा मे देवसेन का भी नाम आता है। एक देवसेन वे हैं, जिन्होंने विक्रम सं. ९९० में दर्शनसारनामक ग्रन्थकी रचना की थी। आलापपद्धति, लघुनयचक्र, आराधनासार और तत्त्वसार नामक ग्रन्थ भी देवसेनके द्वारा रचित हैं। इन सब ग्रन्थोंको दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी कृति माना जाता है। दर्शनसारके अन्त में प्रशस्तिरूप दो गाथाएँ आयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं-
पुव्वायरियकयाइं गाहाइं संचिऊण एयस्थ।
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसतेण।।
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए।
सिरिसासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुनदसमीए।।
अर्थात् पूर्वाचार्योंके द्वारा रची हुई गाथाओंको एकत्र करके यह दर्शनसार नामका ग्रन्थ श्री देवसेनगणिने माघ शुक्ला दशमी, विक्रम सं. ९९०में धारा नगरीमें निवास करते समय पार्श्वनाथ भगवानके मन्दिर में रचा, जो भव्य जीवोंके हृदय में हारके समान शोभा देगा।
तत्त्वसारकी प्रशस्तिमें बताया गया है-
सोऊण तच्चसारं रइयं मुणिणाहदेवसेणेण।
जो सद्दीट्टि भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं।
मुनिनाथ देवसेनने सुनकर तत्वसार रचा, जो सम्यकदृष्टी उसकी भावना करता है वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। आराधनासारके अन्त में बताया है-
ण य मे अस्थि कवितं ण मुणामो छंदलक्खणं कि पि।
णियभावणाणिमित्तं रइय आराहणासारं॥
अमुणियतच्चेण इमं भणियं जं कि पि देवसेणेण।
सोहंतु तं मुणिदा अस्थि हु जइ पवयण-विरुद्धं।।
न मुझे कनिका परिज्ञान है, न जाना और न मान तुगाका ही। अपनी भावनाके निमित्त मैंने आराधनासार रचा है। पूर्णतत्त्वज्ञानसे अपरिचित देवसेनने जो कुछ भी इसमें कहा है यदि उसमें आगमविरुद्ध कथन हो तो मुनीन्द्र उसे शुद्ध कर लें।
इस तरह देवसेनने दर्शनसारमें रचनाकाल और रचना स्थानका निर्देश किया है किन्तु अन्य रचनाओंमें रचना-काल और रचना-स्थानका निर्देश नहीं है। दर्शनसारमें देवसेनने अपनेको देवसेनर्माण कहा है और तत्त्वसारमें मुनिनाथ देवसेन कहा है तथा आराधनासारमें केवल देवसेन। गणि और मुनिनाथपदको एकार्थवाचक मान लेने पर एकरूपता आ सकती है।
भावसंग्रहके अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी रचनामें गुरुके नामका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता है, पर प्रकारान्तरसे गुरुके नामका अध्याहार किया जा सकता है। आराधनासारकी मङ्गलमाथामें "विमल गुणसमिद्ध" पदके द्वारा, दर्शनसारमें "विमलणाणं" पद द्वारा, नयचक्र में "विगयमलं" और "विमलणाण संयुक्तं" पोंके द्वारा गुरुके नामका उल्लेख माना जा सकता है। अत: आराधनासार, दर्शनसार, भाव-संग्रह आदिके रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। दर्शनसार और भाव-संग्रह तो एक ही व्यक्तिकी रचनाएँ हैं क्योंकि श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें दी गयी गाथाओंमेंसे एक गाथा ज्यों-की-त्यों है और अन्य गाथाओंके भाव प्राय: मिलते हैं। यहाँ तुलनाके लिए कुछ गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं। यथा-
छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
सोरठ्ठे उप्पण्णो सेवडसंघो हु वलहीए।।
आसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भद्दबाहुणामेण।
जाणिय सुणिमित्तधरो भणिओ संघो णिओ तेण।।
होहइ यह दुन्भिवखं बारह वरसाणि जाम पुण्णाणि।
देसंतराई गच्छह णिणियसंघेण संजुत्ता।।
सोऊण इमं वयणं णाणादेसेहिं गणहरा सव्वे।
णियणियसंघपउत्ता विहरीमा अत्य सुभिक्खं।।
दर्शनसारमें श्वेताम्बरमतकी उत्पत्ति निम्न प्रकार बतायी है-
छत्तीसे वरिस-सए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
सोर बलहीरा नप्पणो मेवहो संघो।।
सिरिभद्दनाहगणिणो सीसो णामेण संति आइरिओ।
तस्स य सीसो वो जिणचंदो मंदचारितो।
तेण कियं मयमेयं इत्योणं अस्थि तब्भवे मोक्खो।
केवलणाणीण पुणो अद्दक्खाणं तहा रोओं॥
इन गाथाओंकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रन्थोंका रचयिता एक ही व्यक्ति है।
पण्डित परमानन्दजी शास्त्री दिल्लीका अभिमत है कि 'भावसंग्रह' 'दर्शनसार’ के रचयिता देवसेनकी कृति नहीं है, क्योंकि 'दर्शनसार' मूल संघका ग्रंथ है, उसमें काष्ठासंघ, द्रविडसंघ, यापनीयसंघ और माथुरसंघको जैनाभास घोषित किया है। पर 'भावसंग्रह’ केवल मूलसंघका ही मालूम नहीं होता, क्योंकि उसमें "त्रिवर्णाचार’ के समान आचमन, सकलीकरण और पन्चामृताभिषेक आदिका विधान है। इतना ही नहीं, अपितु इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, पवन, यक्ष और ऐशान आदि दिग्पाल देवोंको सशस्त्र और युवतिवाहन सहित आह्वानन करने, बलि, चरु आदि पूजा द्रव्य तथा यज्ञके भागको बीजाक्षरयुक्त मन्त्रोंसे देनेका विधान है। अतएव पं. परमानन्दजीने बताया है कि अपभ्रंश-भाषाके 'सुलोचनारित'के रचयिता देवसेन ही 'भावसंग्रह’ के कर्ता हैं। इनके गुरुका नाम भी विमलसेनगणि है।
श्री प्रेमीजीने भी उनके इस मतको प्रायः स्वीकार करते हुए लिखा है "एक और प्राकृत ग्रन्थ 'भाव संग्रह' है, जो विमलगणिके शिष्य देवसेनका है। यह भी मुद्रित हो चुका है। इसमें कई जगह 'दर्शनसार'की अनेक गाथाएँ उद्धृत हैं। इसपरसे हमने अनुमान किया था कि 'दर्शनसार’ के कर्ता ही इसके कर्ता हैं, परन्तु परमानन्दजी शास्त्रीने (अनेकान्त वर्ष ७ अंक ११-१२ में) इस पर सन्देह किया है और सुलोचनाचरिउके कर्ता तथा भावसंग्रहके कर्ताको एक बतलाया है, जो कि विमलगणिके शिष्य हैं।''
'सुलोचनाचरिउ' में उसके रचना-कालका निर्देश करते हुए लिखा है कि संवत्सरकी श्रावण शुक्ला चतुर्दशीके दिन यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ। पं. परमानन्दजीने ज्योतिष गणनाका प्रमाण देते हुए उक्त कालको विक्रम संवत् ११३२ तथा ११९२ में पड़ता हुआ लिखा है।
पता नहीं पं. परमानन्दजीने किस आधारपर यह ज्योतिष गणना को है। राक्षस-संवत्सर श्रावण शुक्ला चतुर्दशीको ग्रह-लाघवके गणितानुसार वि. सं. १०१२ में आता है। यो राक्षससंवत्सरकी स्थिति वि. सं. ९५२, १०१२, १०७२, ११३२ और ११९२ में आती है, पर श्रावणशुक्ला चतुर्दशीको राक्षस संवत्सरका योग विक्रम सं. १०१२ के अतिरिक्त १३७२ में आता है। इसके बीचके संवत्सरोंमें बार्हस्पत्य गणनानुसार राक्षससंवत्सर और श्रावण शुक्ला चतुर्दशीकी स्थिति एक साथ घटित नहीं होती है। अतः अनुमान है कि दर्शनसार, भावसंग्रह और सुलोचनाचरिउ इन तीनों ग्रंथोंका कर्ता एक देवसेन नहीं है। श्री जगलकिशोर मुख्तारने श्री पं. परमानन्दजीको समालोचना करते हुए लिखा है-
"अतः भावसंग्रहके कर्ता देवसेन उनसे पहले हुए, तब सुलोचनाचरिउके कर्ता देवसेन और पाण्डवपुराणकी गुरुपरम्परावाले देवसेनके साथ उनकी एकता किसी भी तरह स्थापित नहीं की जा सकती और न उन्हें १२वीं १३वों शताब्दीका विद्वान ही ठहराया जा सकता है। इसलिए जब तक भिन्न कर्त्तुत्वका द्योतक कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण सामने न आ जाने, तब तक दर्शनसार और भावसंग्रहको एक ही देवसेनकृत मानने में कोई खास बाधा मालूम नहीं होती"।
मुख्तार साहबके इस कथनसे स्पष्ट है कि सुलोचनाचरिउ १४ वी शतीके किसी देवसेनका है। भावसंग्रह और दर्शनसार एक हो कर्ताकी रचनाएँ हैं।
श्री पं. परमानन्दजी का यह तर्क कि 'दर्शनगार’ मुलसंघका ग्रंथ है और 'भावसंग्रह' मूलसंघसे इतर संघका ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पञ्चामृत अभिषेक आदिकी विधि प्रतिपादित की गयी है, अधिक सबल नहीं है, क्योंकि काष्ठासंघमें, जो कि मूलसंघके समान ही मान्य था, पञ्चामृत- अभिषेक आदिका विधान किया है।
श्री प्रेमीजीने दर्शनसारके अन्तर्गत आये हुए संघोकी समीक्षा करते हुए लिखा है कि दर्शनसारमें आये हुए चार संघोंमें यापनीयसंघको छोड़ शेष तीन संघोंका मूलसंघसे इतना पार्थक्य नहीं है कि वे जैनाभास बतला दिये जायें। दर्शनसारकी रचना वि. सं. ९९० में की है। भावसंग्रह, आराधनासार और तत्त्वसार इनकी रचना दर्शनसारके बाद की गयी है । अत: हमारा अनुमान है कि दर्शनसार देवसेनकी सबसे पहली रचना है। इस रचनाके समयमें वे कट्टर मूलसंघी रहे होंगे। पर पाँच-दस वर्षके बीच उनके विचार और अधिक परिपक्व हुए तथा के काष्ठासंघी आचार्योंके सम्पर्क में पहुँचे, जिससे उन्होंने प्रभावित होकर वि. सं. १००५ के. लगभग भावसंग्नह लिखा।
श्री मुख्तार साहबने श्री पं. नाथूरामजी प्रेमीके मतको उपस्थित करते हुए लिखा है- "इसके प्रारम्भिक अंशमें अन्य ग्रंथोंके उद्धरणोंकी भरमार है, जो मूल ग्रंथकारके द्वारा उद्धत नहीं हुए हैं और अनेक स्थानोंपर- खासकर पांचवें गुणस्थानके वर्णनमें- इसके पद्योंकी स्थिति रयणसार जैसी सन्दिग्ध पायी जाती है। अतः प्राचीन प्रतियोंको खोज करके इसके मूलरूपको सुनिश्चित करनेकी खास जरूरत है।
एक और तर्क भी विचारणीय है कि प्राकृत भाषाके ग्रंथोंकी रचनाके पश्चात ही अपभ्रंशमें रचनाएँ लिखी जाती हैं। कोई भी लेखक प्रथम प्राकृत और संस्कृतमें रचना करता है, तत्पश्चात् अपनशमें। जो लेखक तीनों भाषाओंमें ही रचनाओंका प्रणयन करते हैं, वे प्रथम प्राकृत अनन्तर संस्कृत और तत्पश्चात अपभ्रंशमें ग्रन्थ लिखते हैं। अतएव देवसेनने भी प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशमें रचनाओं का प्रणयन किया होगा। उनकी सरस्वती-आराधनाका काल वि. सं. ९९० (ई सन् ९३३) से वि. सं. १०१२ (ई. सन् ९५५) तक है। अतएव दर्शनसार, भावसंग्रह, आराधनासार, तत्वसार आदि ग्रन्थोंके रचयिता विमलसेनगणिके शिष्य देवसेनगणि हैं।
१. दर्शनसार,
२. भावसंग्रह,
३. आलापपति,
४. लघुनयचक्र,
५. आराधनासार,
६. तत्त्वसार।
१. दर्शनसार- इस लघुकाय ग्रन्थमें कुल ५१ गाथाएँ हैं। प्रथम गाथामें श्लेषमें गरुका स्मरण करते हुए तीर्थंकर महावीरको नमस्कार किया है और पूर्वाचार्यों द्वारा कथित गाधाओंका संग्रह किया है। उत्थानिकाके अनन्तर समस्त इतर दार्शनिक मतोंका प्रवर्त्तक ऋषभदेवके पुत्र मरीचिको माना है। मरीचिने एकान्त, संशय, विपरीत, विनय और अज्ञान इन पांचों एकान्त मार्गों का प्रवर्तन किया है। बताया है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथके तीर्थकालमें सरयू नदीके तटवर्ती पलाश नामक नगरमें पिहितास्रव साधुका शिष्य बुद्धि कीर्तिमुनि हुआ, जो बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था। मत्स्याहारके कारण बह दीक्षासे भ्रष्ट हो गया और रक्ताम्बर धारण कर उसने एकान्तमतका प्रचलन किया। फल, दधि, दुग्ध, शक्कर आदिके समान मांसमें भी जीव नहीं है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करने में कोई पाप नहीं है। उसमें बतलाया की जिस प्रकार जल एक द्रव पदार्थ है, उसके सेवनमें दोष नहीं उसी प्रकार मद्य भी द्रव पदार्थ है, उसके सेवन में भी किसी प्रकारका दोष नहीं है।
एक पाप करता है और फल दुसरा भोगता है। इस प्रकार अनर्गल सिद्धान्तोंका प्रचार कर वह बुद्धकीर्ति नरक गया। कर्ता कोई अन्य व्यक्ति है और फल-भोक्ता कोई अन्य। इस सिद्धान्तमें क्षणिकवादका कथन किया गया है। इस प्रकार मरीचि और बुद्धीर्तिने मिथ्या मतोंका प्रचार किया।
इस अवतारणके पश्चात् श्वेताम्बर मत, विपरीत मत, वाचनिक मत, अज्ञान मत, द्राविड़संघ, यापनीयसंघ, काष्ठासंघ, माधुरसंघ और भिल्लकसंघकी उत्पत्ति एवं समीक्षा की गयी है। काष्ठासंघकी समीक्षा करते हुए वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेन, कुन्दकुन्द, गुणभद्र, विनयसेन, कुमारसेनके निर्देश आये हैं। कुमारसेनको काष्ठासंघका उपदेशक बतलाया है और इस संघका उत्पत्ति काल वि. सं. ७५३ माना है। माथुरसंघकी उत्पत्ति रामसेन द्वारा वि. सं. ९५३ में मथुरा नगरीमें मानी गयी है। भिल्लकसंघकी उत्पत्ति भविष्य-कल्पनाके रूपमें अङ्कित है-
पणमिय वीरजिणिदं सुरसेणणमंसियं विमलणाणं।
बोच्छं दंसणसारं जह कहियं पुव्वसूरीहि।
भरहे तिथयराणं पणमिय देविंदणागरुडाणं।
समएसु होंति केई मिच्छत्तपवट्टगा जीवा॥
सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो।
पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बुड्डकित्तिमुणी।।
णदियडे वरगामे कुमारसमो सत्यपिणः।
कट्ठो दंसणभट्टो जादो सल्लेहणाकाले॥
तत्तो दुसए तीदे महुराए माहुराण गरुणाहो।
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वणियं तेण।
दर्शनसारसे देवसेनके अक्खड़ स्वभावका पता चलता है। उन्होंने अन्तिम गाथामें अपनी स्पष्टता व्यक्त करते हुए लिखा है-
रूसउ तूसउ लोओ सच्चं अक्खंतयस्स साहुस्स।
कि जूयभए साडी विज्जियव्वा णरिदेण।।
सत्य कहने वाले साधुसे कोई रुष्ट हो, चाहे सन्तुष्ट हो, इसकी चिन्ता नहीं। क्या राजाको युका (जूआ) के भयसे वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं।
इससे देवसेनका अक्खड़पना प्रकट होता है।
२. भावसंग्रह
इस ग्रन्यमें ७०१ गाथाएँ हैं। इसमें चौदह गुणस्थानोंका अवलम्बन लेकर विविध विषयोंका निरूपण किया गया है। दो गाथाओं द्वारा १४ गुणस्थानोंके नाम बतला कर मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप प्रतिपादित किया है। मिथ्यात्वके एकान्त, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत इन पांच भेदोंको बतलाकर ब्राह्मण मतको विपरीतमिथ्यादृष्टि कहा है-
मण्णाइ जलेण सुद्धि तित्ति मंसेण पियरवग्गस्स।
पसुकयवहेण सग्गं घम्म गोजोणिफासेण॥
जह जलण्हाणपउता जोवा मुइ णिययपावेण।
तो तत्व वसिय जलयरा सव्वे पावंति दिवलोयं।।
जं कम दिढबद्धं जीवपएसेहि तिविहजोएण।
तं जलफासणिमित्ते कह फट्टइ तित्थाण्हाणेण।।
मलिणो देहो णिच्वं देही पुण णिम्मलो सयारुवी।
को इह जलैण सुज्झइ तम्हा ण्हाणे ण हु सुद्धी॥
जलसे शुद्धि होती है, मांससे पितरोंकी तुसि होती है, पशुबलिसे स्वर्ण मिलता है और गोयोनिके स्पर्शसे धर्म होता है, इन चार ब्राह्मणधर्मके प्रमुख सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए बताया है कि जलस्नानसे यदि समस्त पापोंका प्रक्षालन सम्भव हो, तो नदी, समुद्र और तालाबोंमें रहनेवाले जलचर जीव भी स्वर्गको प्राप्त कर लेंगे। कर्म मैलसे मलिन इस आत्माको जलसे शुद्धि नहीं हो सकती है, जो जलसे शुद्धि मानता है, वह अच्छा विचारक नहीं है। आत्माकी शद्धि तप, इन्द्रियनिग्रह और रत्नत्रयके द्वारा होती है। जिस प्रकार अग्निके संयोगसे स्वर्ण पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार अनशन, ऊनोदर आदि तपोंके करनेसे जीव भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति विषय और कषायमें संलग्न हैं और राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले गृहकार्योंमें आसक्त हैं उनकी जलस्नानसे शुद्धि नहीं हो सकती। कषायरहित, प्रतनियम और शीलसे युक्त व्यक्ति जल स्नानके बिना भी आत्माको पवित्र कर सकता है।
माँसद्वारा पितरोंकी तृप्ति मानने वाला व्यक्ति भी विवेकी नहीं है। हिंसा, कृरता और निर्दयता करने वाला व्यक्ति चारों गतियोंके दुःखोंको उठाता है। जो मांस द्वारा श्राद्ध करके पितरोंकी ताप चाहता है वह व्यक्ति भी बालूसे तेल निकालना चाहता है। अतएव मांसको न तो दान ही माना जा सकता है, और न इससे पितरोंकी तृप्ति ही हो सकती है।
जो श्राद्धद्वारा पितरोंकी तृप्ति मानता है, वह भ्रममें है। किसीके भोजनसे किसीकी तृप्ति नहीं हो सकती। यदि पित्ता भोजन करता है, तो पुत्रका पेट नहीं भरता, और पुत्र भोजन करता है तो पिताका पेट नहीं भरता। जो भोजन करता है, वही तृप्त हो सकता है, अन्य कैसे तुप्त हो सकता है? जो यह मानता है कि पाप करके नरक जाने पर पिताको पिण्डदानद्वारा पुत्र स्वर्ग भेज सकता है, उसके यहाँ जो कार्य करने वाला है उसे फल न मिल कर अन्यको होगा। अतः कृतनाश और अकृताभ्यागम नामक दोष आयगा। इस प्रकार उक्त चारों सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए गीता, महाभारत आदि ग्रन्थोंसे ही समर्थन के लिए प्रमाण उद्धृत किये हैं।
विपरीतमिथ्यात्वके पश्चात् एकान्तमिथ्यात्वकी समीक्षा की गयी है। इस प्रसंगमें क्षणिककान्तवादी बुद्धका खण्डन किया है। वैनायिक मिथ्यात्वके निरसनमें यक्ष, नाग, दुर्गा, चण्डिका आदिके पूजनेका निषेध किया है। संशयमिथ्यात्वका निरूपण करते हुए उदाहरणके हेतु श्वेताम्बर मतका निरसन किया गया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीमुक्ति, केवली कवलाहार और साधुओंका वस्त्र पात्र रखना इन तीनों बातोंकी आलोचना की गयी है। श्वेताम्बर अपने साधुओंको स्थविरकल्पी बतलाते हैं। ग्रन्थकारके मतसे वे स्थविर नहीं, बल्कि गृहस्थकल्पी हैं। जिनकल्प और स्थविरकल्पका विवेचन विस्तार पूर्वक किया है। इस सन्दर्भमें बताया है-
दुद्धरतवस्स भग्गा परिसहविसएहि पौडिया जे य।
जो गिहकप्पो लोए स थविरकप्पो कओ तेहि॥
अर्थात् परीषहसे पीड़ित और दुर्द्धर तपसे भीत बनोने गृहस्थकल्पको स्थविर कल्प बना दिया है। १३७ वी गाथासे श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा दी गयी है। इस कथामें बताया है कि सौराष्ट्र देशकी बलभी नगरी में वि. सं. १३६ में श्वेताम्बर संघकी उत्पत्ति हुई। दर्शनसारमें भी श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिका यही समय अंकित किया गया है।
अज्ञानमिथ्यात्वका कथन करते हुए लिखा है कि भगवान पार्श्वनाथके तीर्थकल्पमें मस्करीपूरण नामक ऋषि हुआ। यह भगवान महावीरके समवचरणमें गया, किन्तु उसके जानेपर भगवानकी वाणो नहीं खिरी। वह रुष्ट होकर समवशरणसे चला आया और कहने लगा-मैं ग्यारह अंगोंका धारी हूँ, फिर भी मेरे जाने पर तीर्थंकर महावीरकी दिव्यध्वनि प्रवाहित नहीं हुई और गौतमके आने पर दिव्यध्वनि होने लगी। गौतमने अभी दीक्षा ली है। वह तो वेदवादी पण्डित है। वह जिनोक्त श्रुतको क्या जाने। अतः उसने अज्ञानसे लोगोंके मध्य मोक्षका उपदेश दिया-
अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणो हु।
देवो ण अत्थि कोई सुण्णं झाएह इच्छाएँ।
अर्थात् अज्ञानसे ही मोक्ष होता है। इसके लिये ध्यान, संयम, तप, सज्ञान की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार पांचों मिथ्यात्वोंकी समीक्षा करनेके पश्चात् चार्वाकके द्वारा मान्य दर्शनकी समीक्षा की है। चार्वाक चैतन्यको भूतोंका विकारमात्र मानता है। ग्रन्थकारने इसे कोलिकाचार्यका मत कहा है-
कउलायरिओ अक्खइ अत्थि ण जीवो हु कस्स तं पावं।
पुण्णं वा कस्स भवे को गच्छइ णरय-सग्गं वा।।
यह कोलिकमत शैवतन्त्रका एकमत है। एक प्रकारसे यह वामाङ्गो है। माँस, मदिराके सेवनके साथ स्त्रिरमण एवं स्वयं शिव-पार्वतीका प्रतिरूपक अपनेको मानना आदि इसके सिद्धान्त हैं। यहाँ हमें ग्रंथकारका भ्रम प्रतीत होता है। कौलिक और चार्वाक ये दोनों मत स्वतन्त्र हैं। दोनोंमें समता इतनी है कि पुण्य-पाप, परलोक आदिकी स्थिति दोनोंमें तुत्य है। कौलिक मतके ग्रन्योंमें वामाचारकी भी पुण्यरूप कहा गया है तथा वाममार्गीधर्माचरणसे स्वर्गादिक सुखोंकी उपलब्धि भी मानी गयी है। शिव और पार्वती रूप कृत्य-अकृत्योंका संकल्प कर लेने पर कहीं कोई बाधा नहीं आती और स्वर्गादिक प्राप्त हो जाते हैं।
चार्वाकमतके पश्चात् सांख्यमतकी समीक्षा की गयी है। बताया है कि जीव सदा अकर्ता है और पुण्य-पापका भोक्ता भी नहीं है। ऐसा लोकमें प्रकट करके बहन और पुत्रीको भी अंगीकार किया गया है। यथा-
जीवो सया भकत्ता भूत्ता ण हु तुम गलस्म।
इय पयडिऊण लोए गहिया वहिणी सधूया वि।।
धूयमायरिवहिणि अण्णावि पुत्तस्थिणि।
आयति य पासवयणुपयडे वि विप्पे।
जह रमियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पे॥
बंभणि-छिपिणि-डोंवि-नडिय-वरुडि-रज्जइ-चम्मारि।
कवले समइ समागमइ तह भूति य परणारि।।
अर्थात् पुत्री, माता, बहन या अन्य कोई भी नारी पुत्रोत्पत्तिको भावनासे कामवचन प्रकट करे, तो कामातुर हो वेदज्ञानी ब्राह्मणको उसका उपभोग करना चाहिये। लेखकने बतलाया है कि कपिलदर्शनमें प्रतिपादित ब्राह्मणी, डोम्बी, नटी, घोबिन, चमारिन आदि परनारियोंके साथ भोग करना उचित है।
स्मृतिकारोंके इस कथनका आशय लेकर कि जो पुरुष स्वयं भागता नारीका भोग नहीं करता उसे बह्महत्याका पाप लगता है; को लक्ष्य में रखकर ही उक्त कथन किया गया है। सांख्यदर्शनके साथ इसका कुछ भी मेल नहीं है। हाँ, कौलिक सम्प्रदायमें उक्त सिद्धान्त अवश्य स्वीकृत है। राजशेखरने अपनी 'कर्पूरमंजरी-सट्टक’ में रण्डा, चण्डा आदिके भोगका औचित्य बतलाया है। अतः कपिलदर्शनका यह सिद्धान्त न होकर, स्मृति या कौलिक सम्प्रदायका सिद्धान्त है। देवसेनने इसी सिद्धान्तकी समीक्षा को है।
तुतीय मिश्रगुणस्थानका कथन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी समालोचना की गयी है। ब्रह्माकी आलोचना करते हुए तिलोत्तमा आदिके उपाख्यानोंको उपस्थित किया है। विष्णकी आलोचनामें उनके विभिन्न अवतारोंकी समीक्षा की गयी है। रुद्रकी आलोचनामें उनके स्वरूप और ब्रह्महत्या आदि कार्योंकी समीक्षा आयी है।
चतुर्थ अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए सात तत्त्वोंका कथन किया गया है। पांच गुणस्थानका स्वरूप २५० गाथाओंके द्वारा बहुत विस्तारसे बतलाया है। इसमें अणुव्रत, गुणव्रत, और शिक्षाव्रतोके साथ अष्टमूलगुणोंका भी उल्लेख आया है। चार प्रकारके ध्यान, देवपूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, आदि श्रावकाचारका भी निरूपण आया है। अभिषेकके समय यम, वरुण, कुवेर, ईशान आदिके आह्वानपूर्वक पन्चामृत-अभिषेक करनेका विधान किया है।
षष्ठ व सप्तम गुणस्थानके स्वरूपकथनमें पिण्डस्थ, पदस्थ रूपस्थ, और रूपातीत ध्यानोंका कथन आया है। शेष गुणस्थानोंका सामान्यतया स्वरूपविवेचन हुआ है। गणस्थानोंके स्वरूपकथनमें देवसेनने पंचसंग्रहप्राकृतसे अनेक गाथाएँ ज्यों-को-त्यों रूपमें ग्रहण की हैं। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने गोम्मटसारमें पंचसंग्रहकी अनेक गाथाएँ ग्रहण की हैं। यहाँ तुलनाके लिए कतिपय सामान गाथाएँ दी जाती हैं-
मिच्छो सासण मिस्सो अविरयसम्मो य देसविरदो य।
विरओ पमत्त इसरो अपुव्व अणियट्टि सुहमो य।।
उपसंत खीणमोहे सजोइकेलिजिणो अजोगी य।
ए चउदस गुणठाणा कमेण सिहा य णायव्या।।
णो इंदिएसु विरोओ णो जीवे थावरे तसे वा पि।
जो सद्दहइ जिणुतं अविरइसम्मो त्ति णायव्वो।
इस प्रकार अनेक गाथाएँ पंचसंग्रहमें प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, भाव संग्रहकी कई गाथाएँ कुछ रूपान्तरके साथ राजशेखरकी कर्पूरमंजरीमें भी मिलती हैं। कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें पंचसंग्रह और धवलाटीकाका मिश्रित रूप है।
जे तसवहाउ विरदो णो विरओ अवखथावरवहाओ।
पडिसमयं सो जोवो बिरयाविरओ जिणेक्कमई।।- गाथा १३
जो तसबहादु बिरदो अविरद तह य थावरवहाओ।
एक्कसमम्मि जीवो विरदाविरदो जिणेवकमाई।।- गाथा ३१
जो तसवहाउ विरओ णो विरओ तह य थावरवहाओ।
एक्कसमर्याम्म जीवो विरयाविरज त्ति जिणु कहई।।- गाथा ३५१
भावसंग्रहपर कुन्दकुन्दाचार्य के पञ्चास्तिकाय ग्रंथका भी प्रभाव है-
जीवो त्ति हवदि वेदा उचओयविसेसिदो पहूं कत्ता।
भोत्ता य देहमेतो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो।।
पाणेहि चदुहिं जीवदि जीवरसदि जो हु जीविदो पुव्वं।
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासो।।
जीवो अणाइ णिच्चो उवओगसंजुदो देहमित्तो य।
कत्ता भोक्ता चेता ण हु मुत्तो सहावउड्ढगई।।
पाणचउक्कपउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पुव्वं।
जोवेइ वट्टमाणं जीवत्तगगुण समावण्णो॥
स्पष्ट है कि भावसंग्रहपर पञ्चास्तिकायका भी प्रभाव है।
३. आराधनासार
एकसी पन्द्रह प्राकृत-गाथाओंमें यह ग्रंथ रचा गया है। आराधनाओंका वर्णन करते हुए बताया है-
आराहणाइसारो तव-दंसण-णाण-चरणसालानी।
सो दुम्भेओ उत्तो ववहारो चेन पप।।
अर्थात् तपाराधना, दर्शनाराधना, झानाराधना और चारित्राराधना इन चारों आराधानाओका सार इसमें गिर रहेगा। माइ माराधनामगर दो प्रकारका है- (१) व्यवहार और (२) परमार्थ। व्यवहार-आराधनाका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि सूत्र और अर्थ द्वारा कथित वस्तुको ग्रहण करना ज्ञानाराधना है। अर्थात् तीर्थंकरकी वाणी द्वारा प्रतिपादित ११ अंग और १४ पूर्वोको अवगत करना ज्ञानाराधना है। मावशुद्धिपूर्वक १३ प्रकारके चारित्रका आचरण करना चारित्राराधना है। १३ प्रकारके चारित्रमें ५ महाव्रत, ५ समिति ओर ३ गप्तीको स्थान दिया गया है। १२ प्रकारके तपोंका आचरण करनेके लिए प्रवृत्त होना तपाराधना है। इस प्रकार व्यवहार-आराधनाका स्वरूप कथन कर निश्चय-आराधनाफा स्वरूप बसलाते हुए लिखा है-
सुद्धणये चउखंध उत्तं आराहणाइ परिसिय!
सम्ववियप्पविमुक्को सुद्धो अप्पा णिरालंबो।।
अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सपरूप इन चारों भेद- विकल्पोंका त्याग कर पञ्चेन्द्रियके विषयसुखसे रहित निर्विकल्प आत्मतत्वका आराधन करना निश्चय-आराधना है। आगे इसीके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन करते हुए बताया है-
सद्दहइ सहावं जाणइ अप्पाणमामणो सुद्धं।
तं चि य अणुचरइ पुणो इंदियविसए णिरोहिता।
अर्थात् स्वस्वरूपका श्रद्धान करना, शुद्ध आत्माको जानना और निज आत्मरूप आचरण करना एवं निज स्वरूप तपश्चरण करना निश्चयाराधना है। निश्चय-आराधनामें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ रुक जाती हैं और आत्मस्वरूप श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और तपाराधना होने लगती है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपरूप आत्मा ही है, जो राग-द्वेष छोड़कर इस शुद्ध आत्माका आराधन करता है उसीकी निश्चय-आराधना होती है।
जीव चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, भ्रमण करेगा और भ्रमण किया है। इसका कारण ज्ञानमयो आत्माराधनको प्राप्त न करना है। मरणकालमें वही व्यक्ति आत्माराधन कर सकता है जो राग-द्वेष रहित है। बताया है-
अप्पसहावे णिरओ वज्जियपरदव्वसंगसुक्खरसो।
णिग्गहियरायदोसो हवई आराहमो मरणे॥
जो रयणत्तयमइओ मुत्तूणं अप्पणो विसूदप्पा।
चितेइ य परवव विराहओ णिच्छयं भणियो।
राग-द्वेषोंको दूर कर और परद्रव्योंके संयोगजन्य सुखका त्याग कर जो आत्मस्वभावमें निरत है वहीं मरण-कालमें आराधक होता है। जो रत्नत्रय मयी विशुद्ध आत्माको छोड़कर परद्रव्योंका चिन्तन करता है वह आराधनाका विराधक माना जाता है। जो न सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्ररूप आत्माकी समझता है और न आत्मासे विलक्षण शरीरादि परद्रव्योंको ही जानता है, उसे न ज्ञानकी प्राप्ति रहती है और न आराधनाकी हो।
जब तक वृद्धावस्था नहीं भाती है, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, बुद्धि नष्ट नहीं होती है, आयरूपी जल समाप्त नहीं होता है तब तक आत्मकल्याणके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचता रहता है कि अभी तो युवावस्था है, विषयसुख-सेवनके दिन हैं वह वृद्धावस्था आने पर कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपरूप आराधनाकी प्राप्ती शारीरिक शक्ति और इन्द्रियोंकी शक्ति रहने पर ही सम्भव है। बताया है-
जरवग्घिणी ण चंपइ जाम ण वियलाइ हुति अक्खाई।
बुद्धी जाम ण णासइ आउजलं जाम ण परिगलाई।
जा उज्जमो ण वियलइ संजम-तत्र-णाण-झाणजोएसु।
तावरिहो सो पुरिसो उत्तमठाणस्स संभवई।
बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रहका त्यागकर अन्तरक कषाय और विकारोंको कुश करनेका प्रयास करना ही वास्तविक आराधना है। कषाएँ अत्यधिक शक्तिशाली हैं। इन्हींके कारण चतुर्गति परिभ्रमण होता है। जब तक कषाय और भोगोंका त्याग नहीं किया जायेगा, तब तक संयमकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है और संयमरहित व्यक्तिके गुण विशुद्ध नहीं हो सकते। बताया है-
जाम ण हणइ कसाए सकसाई णेव संजमी होई।
संजमसहियस्स गुणा ण हूंति सव्वे विसुद्धियरा।
जो परीषहोंको सहन करता हुआ शान्तिभावपूर्वक व्रत, समिति और गुप्तियोंका पालन करता है वह अनादिकालीन काम-क्रोधादिको नष्ट कर देता है। इस प्रसङ्गमें उपसर्ग और परीषहोंको सहन करनेवाले शिवभूति, सूकुमाल और सुकोशलके उदाहरण दिये गये हैं और मनुष्यकृत उपसर्ग सहन करने में गुरुदत्त, पाण्डव और गजकुमारके आख्यान दृष्ट्वान्तके रूपमें प्रस्तुत किये हैं। देवकृत उपसर्गके सहन करने में प्रसिद्ध हुए श्रीदत्त, सुवर्णभद्र आदिके उदाहरण दिये गये हैं। इस प्रकार उदाहरणों और प्रत्युदाहरणों द्वारा सैद्धान्तिक विषयको भी सरस बनानेकी चेष्टा की है।
मन, वचन और कायको वश करनेकी आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा है-
सिक्सह मणवसियरणं सवसीहूएण जेण मणुआणं।
णासंति रार-दोसे तेसिं णासे समो परमो।।
मनको वश में करनेको शिक्षा देनी चाहिए। जिसका मन वशीभूत है वही राग-द्वेषको नाश कर सकता है और राग-द्वेषके नाश करनेसे ही परमपदकी प्राप्ति होती है।
उपशमवान जीव ही मनका निग्रह कर सकता है और मनका निग्रह करनेसे ही आत्मा परमात्मापदकी प्राप्त कर सकती है।
आचार्यने ध्यान, ध्याता और ध्येयका लक्षण बतलाया है और ध्यानके द्वारा ही सकल कर्मोका नाश होता है। अतः राग-द्वेष, मोहका विनाश करने पर ही ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है। जो यह अनुभव करता है कि न मैं देह हूँ, न मन हूँ और न मुझमें दुःख ही है वह क्षपक समभावनासे युक्त होकर दुःखका विनाश कर लेता है। यथा-
णाई देहो ग मणो ण तेण में अत्थि इत्थ दुक्खाई।
समभावणाइ जुत्तो वि सहसु दुक्खं अहो खवय।।
इस प्रकार समस्त परिग्रहका त्यागकर आत्मसाधनामें संलग्न रहनेका निर्देश किया है।
४. तत्त्वसार
इस ग्रन्थमें ७४ गाथा हैं। तत्वके मूलत: दो भेद है- (१) स्वगत तत्व और परगत तत्व। स्वगत तत्व निजात्मा है और परगत तत्वमें परमेष्ठी हैं। स्वगत तत्वके भी दो भेद है- (१) सविकल्पक और (२) निर्विकल्पक। आस्त्रवसहितको सविकल्पक कहते हैं और आस्त्रवरहितको निर्विकल्पक। इन्द्रियविषय- सुख के समाप्त होनेपर मनकीको चंचलता जब अरुवद्ध हो जाती है तब आत्मा अपने स्वरूपमें निर्विकल्प हो जाता है। यथा-
जं पुणु सगयं तच्चं सवियप्प हबइ तह य अवियप्पं।
सवियप्पं सासवयं णिरासर्व विमयसंकप्पं।।
इंदियविसविरामे मणस्स णिल्लूरणं हवे जइया।
तझ्या तं अविअप्प ससख्ये अप्पणो त तु॥
जो अविकल्पक सत्व है वही मोक्षका कारण है। उसीको शुद्ध समझकर ध्यान करना चाहिए।
इस प्रकरणमें श्रमण और योगीकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है- "मन वचन-कायसे जो बाह्म और आभ्यन्सर परिग्रहसे रहित है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है और जिसने जिनलिमा आश्रय ग्रहण किया है वह श्रमण कहलाता है-
बहिरव्भतरगंथा मुक्का जेणेह तिविहजोएण।
सो णिग्गंधी भणिओ जिणलिंगसमासिओ सवणों।।
लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, मित्र-शत्रुको जो समानरूपसे ध्यान करता है वह योगी है। यथा-
लाहालाहे सरिसो सुहदुक्खे तह य जीविए मरणे।
बंधव-अरयसमाणो झाणसमत्थो हु सो जोई॥
जो व्यक्ति आत्माकी सिद्धि करना चाहता है वह ध्यान द्वारा कर्मोंका क्षय कर मोक्षको प्राप्त करे। यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप है, असंख्यात प्रदेशी है और प्रदेशोंके संहार तथा विसर्पणके कारण यह शरीरप्रमाण है जो राग, द्वेष, मोहका त्याग कर जन्म-जरा-मरणसे रहित इस निरञ्जन आत्माका ध्यान करता है वह सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। आत्मामें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न शब्द है। यह तो शुद्ध चेतनस्वरूप निरञ्जन है। यथा-
फासरसरूवगंधा सद्दादीया य जस्स गरिय पुणो।
शुद्धो चेयणभावो णिरंजणो सो अहं भणियो।
व्यवहारनयसे इस आत्मामें कर्म-नोकर्म माने जाते हैं। आत्मा और कर्मका सम्बन्ध दूध-पानीके समान है। जिस प्रकार दूध और पानी अपने-अपने स्वभावसे विकृत होकर एकमें एक मिल जाते हैं उसी प्रकार आत्मा और पौद्गलिक कर्म भी अपने-अपने स्वभावको छोड़ एकमें एक मिल गये हैं। अतएव में शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ज्ञानरूप हूँ, कर्म-नोकर्मसे रहित हूँ, एक हूँ, निरालम्ब हूँ, देहप्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यातदेशिक हूँ, अमर्त हूँ। इस प्रकार चिन्तन कर आत्म स्वरूपको प्राप्त करना चाहिए। जब तक पर द्रव्योंसे चित्त व्यावृत्त नहीं होता तब तक भव्यजीव मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी उग्र तप क्यों न करता रहे। आत्मसिद्धिका मूलकारण राग-द्वेष और विषयसुखसे मुक्ति प्राप्त कर लेना है।
यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है तथा इसमें आत्मानुभूति तथा आत्मसिद्धिका उपाय वर्णित है।
५. लघुनयचक्र
इस ग्रन्थमें ८७ गाथाएँ हैं । नयका स्वरूप, उपयोगिता एवं उसके भेद प्रभेदोंका वर्णन किया है । नयका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-
जं णाणीण वियप्पं सुयभेयं वत्यूयंससंगहण।
ते इह णयं पउत्तं णाणी पुण तेहि णाणेहि॥
जो वस्तुके एक अंशका ग्रहण करता है श्रुतज्ञानका वह भेद नय कहलासा है। नयके बिना वस्तुस्वरूपकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है और नय द्वारा ही स्याद्वादका ज्ञान होता है। अतः नयका ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुकी प्रतिपत्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। नयसे जिन वचनोंका बोध होता है और नयसे ही वस्तुकी प्रतिपत्ति होती है। भूल नय दो है- द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। नयके सामान्यतया नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत ये सात भेद हैं। अन्य भेद निम्न प्रकार हैं-
दव्वत्थं दहमेयं छब्भेयं पज्जयत्थियं यं।
तिविहं च णेगमं तह दुविहं पुण संगहं तत्थ।।
ववहार रिउसुतं दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का।
उत्ता इह णयमेया उपणयभेया वि पभणामो॥
द्वव्यार्थिकके १० भेद, पर्यायार्थिकके ६ भेद, नैगम नयके तीन भेद, संग्रहके दो, व्यवहार और ऋतुसूत्रके दो-दो भेद और शेष नयोंका एक-एक भेद है। उपनयके तीन भेद हैं- (१) सद्भुत, (२) असद्भुत और (३) उपचरित नय। सद्भुतके दो भेद हैं और असद्भुत के तीन तथा उपचरितके तीन। इस प्रकार नयके भेद-प्रभेदोंका कथन कर द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंकी अपेक्षासे वस्तु-विवेचन किया गया है।
६. आलाप-पद्धति
यह संस्कृत-गद्यमें रचित छोटी-सी रचना है। अन्य ग्रंथोंके समान इसका प्रकाशन भी माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमालासे हुआ है। इस ग्रंथमें गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नय, गुण-व्यत्पत्ति, स्वभाव-व्युत्पत्ति, प्रमाणका कथन, निक्षेपको व्युत्पत्ति, नयोंके भेदोंको व्युत्पत्ति एवं अध्यात्मनयोंका कथन किया गया है। आरम्भमें वचनपद्धतिको ही आलापपद्धति कहा है। यह ग्रन्थ निम्नलिमित अधिकारों में विभक्त है-
१. द्वव्याधिकार,
२. गुणाधिकार,
३. पर्यायाधिकार,
४. स्वभावाधिकार,
५. प्रमाणाधिकार,
६. नय-अधिकार,
७. गुण व्युत्पत्ति अधिकार,
८. पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार,
९. स्वभावव्युत्पत्ति-अधिकार,
१०. एकान्तपक्षमें दोष,
११. नययोजना,
१२ प्रमाणकथन,
१३. नयलक्षण और भेद,
१४. निक्षेप व्युत्पत्ति,
१५. नयोंके भेदोंकी व्युत्पत्ति,
१६. अध्यात्मनय।
नामानुसार विषयोंका निरूपण इन अधिकारोंमें किया गया है। जैन सिद्धान्तकी अवगत करनेके लिए यह छोटा-सा ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। द्रव्यके सामान्य और विशेष गुणोंका विवेचन करते हुए लिखा है-
"अस्तित्वं, वस्तुत्त्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्व मचेतनत्वं, मूर्त्तत्वममूर्तत्वं द्रव्याणां दश सामान्यगुणाः। प्रत्येकमष्टावष्टो सर्वेषाम्।”
[एकैकद्रव्ये अष्टौ अष्टौ गुणा भवंति। जीवद्रव्ये अचेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति, पुद्गलद्रव्ये चेतनत्वममूर्तत्वं च नास्ति, धर्माधर्माकाशकालद्रव्येषु चेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति। एवं द्विद्विगुणजिते अष्टौ अष्टौ गुणाः प्रत्येकद्रव्ये भवन्ति।]
ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि स्पर्शरसगंधवर्णा: गतिहेतुत्वं स्थितिहेतुत्वमवगाहन हेतुत्वं वर्तनाहेतुत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं मूर्तस्वममूर्तत्वं द्रव्याणां षोडश विशेष गुणा:।
"अर्थात् अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रभेयत्व, अगुरुलवुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सामान्यगुण हैं। सदेव द्रव्योंके साथ रहते हैं, द्रव्योंसे पृथक् नहीं होते। प्रत्येक द्रव्यमें दश सामान्य गुणोंमेंसे आठ-आठ गुण रहते हैं, दो-दो गुण नहीं होते। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेषगुण हैं।"
इस प्रकार द्रव्य, गुण, स्वभावके अतिरिक्त नय और प्रमाणका भी विवेचन किया है।
सारस्वसाचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।
सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-
१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।
२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।
३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।
४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।
५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।
६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन।
७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन।
सारस्वताचार्यों में सर्वप्रमुख स्वामीसमन्तभद्र हैं। इनकी समकक्षता श्रुत घराचार्यों से की जा सकती है। विभिन्न विषयक ग्रन्थ-रचनामें थे अद्वितीय हैं।
डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।
#devsenjimaharaj
डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।
आचार्य श्री देवसेन (प्राचीन)
| Name | Phone/Mobile 1 | Which Sangh/Maharaji/Aryika Ji you are associated with |
|---|
Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara- 2
देवसेन नामके कई आचार्योक उल्लेख मिलते हैं। सारस्वसाचार्यों की परंपरा मे देवसेन का भी नाम आता है। एक देवसेन वे हैं, जिन्होंने विक्रम सं. ९९० में दर्शनसारनामक ग्रन्थकी रचना की थी। आलापपद्धति, लघुनयचक्र, आराधनासार और तत्त्वसार नामक ग्रन्थ भी देवसेनके द्वारा रचित हैं। इन सब ग्रन्थोंको दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी कृति माना जाता है। दर्शनसारके अन्त में प्रशस्तिरूप दो गाथाएँ आयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं-
पुव्वायरियकयाइं गाहाइं संचिऊण एयस्थ।
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसतेण।।
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए।
सिरिसासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुनदसमीए।।
अर्थात् पूर्वाचार्योंके द्वारा रची हुई गाथाओंको एकत्र करके यह दर्शनसार नामका ग्रन्थ श्री देवसेनगणिने माघ शुक्ला दशमी, विक्रम सं. ९९०में धारा नगरीमें निवास करते समय पार्श्वनाथ भगवानके मन्दिर में रचा, जो भव्य जीवोंके हृदय में हारके समान शोभा देगा।
तत्त्वसारकी प्रशस्तिमें बताया गया है-
सोऊण तच्चसारं रइयं मुणिणाहदेवसेणेण।
जो सद्दीट्टि भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं।
मुनिनाथ देवसेनने सुनकर तत्वसार रचा, जो सम्यकदृष्टी उसकी भावना करता है वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। आराधनासारके अन्त में बताया है-
ण य मे अस्थि कवितं ण मुणामो छंदलक्खणं कि पि।
णियभावणाणिमित्तं रइय आराहणासारं॥
अमुणियतच्चेण इमं भणियं जं कि पि देवसेणेण।
सोहंतु तं मुणिदा अस्थि हु जइ पवयण-विरुद्धं।।
न मुझे कनिका परिज्ञान है, न जाना और न मान तुगाका ही। अपनी भावनाके निमित्त मैंने आराधनासार रचा है। पूर्णतत्त्वज्ञानसे अपरिचित देवसेनने जो कुछ भी इसमें कहा है यदि उसमें आगमविरुद्ध कथन हो तो मुनीन्द्र उसे शुद्ध कर लें।
इस तरह देवसेनने दर्शनसारमें रचनाकाल और रचना स्थानका निर्देश किया है किन्तु अन्य रचनाओंमें रचना-काल और रचना-स्थानका निर्देश नहीं है। दर्शनसारमें देवसेनने अपनेको देवसेनर्माण कहा है और तत्त्वसारमें मुनिनाथ देवसेन कहा है तथा आराधनासारमें केवल देवसेन। गणि और मुनिनाथपदको एकार्थवाचक मान लेने पर एकरूपता आ सकती है।
भावसंग्रहके अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी रचनामें गुरुके नामका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता है, पर प्रकारान्तरसे गुरुके नामका अध्याहार किया जा सकता है। आराधनासारकी मङ्गलमाथामें "विमल गुणसमिद्ध" पदके द्वारा, दर्शनसारमें "विमलणाणं" पद द्वारा, नयचक्र में "विगयमलं" और "विमलणाण संयुक्तं" पोंके द्वारा गुरुके नामका उल्लेख माना जा सकता है। अत: आराधनासार, दर्शनसार, भाव-संग्रह आदिके रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। दर्शनसार और भाव-संग्रह तो एक ही व्यक्तिकी रचनाएँ हैं क्योंकि श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें दी गयी गाथाओंमेंसे एक गाथा ज्यों-की-त्यों है और अन्य गाथाओंके भाव प्राय: मिलते हैं। यहाँ तुलनाके लिए कुछ गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं। यथा-
छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
सोरठ्ठे उप्पण्णो सेवडसंघो हु वलहीए।।
आसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भद्दबाहुणामेण।
जाणिय सुणिमित्तधरो भणिओ संघो णिओ तेण।।
होहइ यह दुन्भिवखं बारह वरसाणि जाम पुण्णाणि।
देसंतराई गच्छह णिणियसंघेण संजुत्ता।।
सोऊण इमं वयणं णाणादेसेहिं गणहरा सव्वे।
णियणियसंघपउत्ता विहरीमा अत्य सुभिक्खं।।
दर्शनसारमें श्वेताम्बरमतकी उत्पत्ति निम्न प्रकार बतायी है-
छत्तीसे वरिस-सए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
सोर बलहीरा नप्पणो मेवहो संघो।।
सिरिभद्दनाहगणिणो सीसो णामेण संति आइरिओ।
तस्स य सीसो वो जिणचंदो मंदचारितो।
तेण कियं मयमेयं इत्योणं अस्थि तब्भवे मोक्खो।
केवलणाणीण पुणो अद्दक्खाणं तहा रोओं॥
इन गाथाओंकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रन्थोंका रचयिता एक ही व्यक्ति है।
पण्डित परमानन्दजी शास्त्री दिल्लीका अभिमत है कि 'भावसंग्रह' 'दर्शनसार’ के रचयिता देवसेनकी कृति नहीं है, क्योंकि 'दर्शनसार' मूल संघका ग्रंथ है, उसमें काष्ठासंघ, द्रविडसंघ, यापनीयसंघ और माथुरसंघको जैनाभास घोषित किया है। पर 'भावसंग्रह’ केवल मूलसंघका ही मालूम नहीं होता, क्योंकि उसमें "त्रिवर्णाचार’ के समान आचमन, सकलीकरण और पन्चामृताभिषेक आदिका विधान है। इतना ही नहीं, अपितु इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, पवन, यक्ष और ऐशान आदि दिग्पाल देवोंको सशस्त्र और युवतिवाहन सहित आह्वानन करने, बलि, चरु आदि पूजा द्रव्य तथा यज्ञके भागको बीजाक्षरयुक्त मन्त्रोंसे देनेका विधान है। अतएव पं. परमानन्दजीने बताया है कि अपभ्रंश-भाषाके 'सुलोचनारित'के रचयिता देवसेन ही 'भावसंग्रह’ के कर्ता हैं। इनके गुरुका नाम भी विमलसेनगणि है।
श्री प्रेमीजीने भी उनके इस मतको प्रायः स्वीकार करते हुए लिखा है "एक और प्राकृत ग्रन्थ 'भाव संग्रह' है, जो विमलगणिके शिष्य देवसेनका है। यह भी मुद्रित हो चुका है। इसमें कई जगह 'दर्शनसार'की अनेक गाथाएँ उद्धृत हैं। इसपरसे हमने अनुमान किया था कि 'दर्शनसार’ के कर्ता ही इसके कर्ता हैं, परन्तु परमानन्दजी शास्त्रीने (अनेकान्त वर्ष ७ अंक ११-१२ में) इस पर सन्देह किया है और सुलोचनाचरिउके कर्ता तथा भावसंग्रहके कर्ताको एक बतलाया है, जो कि विमलगणिके शिष्य हैं।''
'सुलोचनाचरिउ' में उसके रचना-कालका निर्देश करते हुए लिखा है कि संवत्सरकी श्रावण शुक्ला चतुर्दशीके दिन यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ। पं. परमानन्दजीने ज्योतिष गणनाका प्रमाण देते हुए उक्त कालको विक्रम संवत् ११३२ तथा ११९२ में पड़ता हुआ लिखा है।
पता नहीं पं. परमानन्दजीने किस आधारपर यह ज्योतिष गणना को है। राक्षस-संवत्सर श्रावण शुक्ला चतुर्दशीको ग्रह-लाघवके गणितानुसार वि. सं. १०१२ में आता है। यो राक्षससंवत्सरकी स्थिति वि. सं. ९५२, १०१२, १०७२, ११३२ और ११९२ में आती है, पर श्रावणशुक्ला चतुर्दशीको राक्षस संवत्सरका योग विक्रम सं. १०१२ के अतिरिक्त १३७२ में आता है। इसके बीचके संवत्सरोंमें बार्हस्पत्य गणनानुसार राक्षससंवत्सर और श्रावण शुक्ला चतुर्दशीकी स्थिति एक साथ घटित नहीं होती है। अतः अनुमान है कि दर्शनसार, भावसंग्रह और सुलोचनाचरिउ इन तीनों ग्रंथोंका कर्ता एक देवसेन नहीं है। श्री जगलकिशोर मुख्तारने श्री पं. परमानन्दजीको समालोचना करते हुए लिखा है-
"अतः भावसंग्रहके कर्ता देवसेन उनसे पहले हुए, तब सुलोचनाचरिउके कर्ता देवसेन और पाण्डवपुराणकी गुरुपरम्परावाले देवसेनके साथ उनकी एकता किसी भी तरह स्थापित नहीं की जा सकती और न उन्हें १२वीं १३वों शताब्दीका विद्वान ही ठहराया जा सकता है। इसलिए जब तक भिन्न कर्त्तुत्वका द्योतक कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण सामने न आ जाने, तब तक दर्शनसार और भावसंग्रहको एक ही देवसेनकृत मानने में कोई खास बाधा मालूम नहीं होती"।
मुख्तार साहबके इस कथनसे स्पष्ट है कि सुलोचनाचरिउ १४ वी शतीके किसी देवसेनका है। भावसंग्रह और दर्शनसार एक हो कर्ताकी रचनाएँ हैं।
श्री पं. परमानन्दजी का यह तर्क कि 'दर्शनगार’ मुलसंघका ग्रंथ है और 'भावसंग्रह' मूलसंघसे इतर संघका ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पञ्चामृत अभिषेक आदिकी विधि प्रतिपादित की गयी है, अधिक सबल नहीं है, क्योंकि काष्ठासंघमें, जो कि मूलसंघके समान ही मान्य था, पञ्चामृत- अभिषेक आदिका विधान किया है।
श्री प्रेमीजीने दर्शनसारके अन्तर्गत आये हुए संघोकी समीक्षा करते हुए लिखा है कि दर्शनसारमें आये हुए चार संघोंमें यापनीयसंघको छोड़ शेष तीन संघोंका मूलसंघसे इतना पार्थक्य नहीं है कि वे जैनाभास बतला दिये जायें। दर्शनसारकी रचना वि. सं. ९९० में की है। भावसंग्रह, आराधनासार और तत्त्वसार इनकी रचना दर्शनसारके बाद की गयी है । अत: हमारा अनुमान है कि दर्शनसार देवसेनकी सबसे पहली रचना है। इस रचनाके समयमें वे कट्टर मूलसंघी रहे होंगे। पर पाँच-दस वर्षके बीच उनके विचार और अधिक परिपक्व हुए तथा के काष्ठासंघी आचार्योंके सम्पर्क में पहुँचे, जिससे उन्होंने प्रभावित होकर वि. सं. १००५ के. लगभग भावसंग्नह लिखा।
श्री मुख्तार साहबने श्री पं. नाथूरामजी प्रेमीके मतको उपस्थित करते हुए लिखा है- "इसके प्रारम्भिक अंशमें अन्य ग्रंथोंके उद्धरणोंकी भरमार है, जो मूल ग्रंथकारके द्वारा उद्धत नहीं हुए हैं और अनेक स्थानोंपर- खासकर पांचवें गुणस्थानके वर्णनमें- इसके पद्योंकी स्थिति रयणसार जैसी सन्दिग्ध पायी जाती है। अतः प्राचीन प्रतियोंको खोज करके इसके मूलरूपको सुनिश्चित करनेकी खास जरूरत है।
एक और तर्क भी विचारणीय है कि प्राकृत भाषाके ग्रंथोंकी रचनाके पश्चात ही अपभ्रंशमें रचनाएँ लिखी जाती हैं। कोई भी लेखक प्रथम प्राकृत और संस्कृतमें रचना करता है, तत्पश्चात् अपनशमें। जो लेखक तीनों भाषाओंमें ही रचनाओंका प्रणयन करते हैं, वे प्रथम प्राकृत अनन्तर संस्कृत और तत्पश्चात अपभ्रंशमें ग्रन्थ लिखते हैं। अतएव देवसेनने भी प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशमें रचनाओं का प्रणयन किया होगा। उनकी सरस्वती-आराधनाका काल वि. सं. ९९० (ई सन् ९३३) से वि. सं. १०१२ (ई. सन् ९५५) तक है। अतएव दर्शनसार, भावसंग्रह, आराधनासार, तत्वसार आदि ग्रन्थोंके रचयिता विमलसेनगणिके शिष्य देवसेनगणि हैं।
१. दर्शनसार,
२. भावसंग्रह,
३. आलापपति,
४. लघुनयचक्र,
५. आराधनासार,
६. तत्त्वसार।
१. दर्शनसार- इस लघुकाय ग्रन्थमें कुल ५१ गाथाएँ हैं। प्रथम गाथामें श्लेषमें गरुका स्मरण करते हुए तीर्थंकर महावीरको नमस्कार किया है और पूर्वाचार्यों द्वारा कथित गाधाओंका संग्रह किया है। उत्थानिकाके अनन्तर समस्त इतर दार्शनिक मतोंका प्रवर्त्तक ऋषभदेवके पुत्र मरीचिको माना है। मरीचिने एकान्त, संशय, विपरीत, विनय और अज्ञान इन पांचों एकान्त मार्गों का प्रवर्तन किया है। बताया है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथके तीर्थकालमें सरयू नदीके तटवर्ती पलाश नामक नगरमें पिहितास्रव साधुका शिष्य बुद्धि कीर्तिमुनि हुआ, जो बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था। मत्स्याहारके कारण बह दीक्षासे भ्रष्ट हो गया और रक्ताम्बर धारण कर उसने एकान्तमतका प्रचलन किया। फल, दधि, दुग्ध, शक्कर आदिके समान मांसमें भी जीव नहीं है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करने में कोई पाप नहीं है। उसमें बतलाया की जिस प्रकार जल एक द्रव पदार्थ है, उसके सेवनमें दोष नहीं उसी प्रकार मद्य भी द्रव पदार्थ है, उसके सेवन में भी किसी प्रकारका दोष नहीं है।
एक पाप करता है और फल दुसरा भोगता है। इस प्रकार अनर्गल सिद्धान्तोंका प्रचार कर वह बुद्धकीर्ति नरक गया। कर्ता कोई अन्य व्यक्ति है और फल-भोक्ता कोई अन्य। इस सिद्धान्तमें क्षणिकवादका कथन किया गया है। इस प्रकार मरीचि और बुद्धीर्तिने मिथ्या मतोंका प्रचार किया।
इस अवतारणके पश्चात् श्वेताम्बर मत, विपरीत मत, वाचनिक मत, अज्ञान मत, द्राविड़संघ, यापनीयसंघ, काष्ठासंघ, माधुरसंघ और भिल्लकसंघकी उत्पत्ति एवं समीक्षा की गयी है। काष्ठासंघकी समीक्षा करते हुए वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेन, कुन्दकुन्द, गुणभद्र, विनयसेन, कुमारसेनके निर्देश आये हैं। कुमारसेनको काष्ठासंघका उपदेशक बतलाया है और इस संघका उत्पत्ति काल वि. सं. ७५३ माना है। माथुरसंघकी उत्पत्ति रामसेन द्वारा वि. सं. ९५३ में मथुरा नगरीमें मानी गयी है। भिल्लकसंघकी उत्पत्ति भविष्य-कल्पनाके रूपमें अङ्कित है-
पणमिय वीरजिणिदं सुरसेणणमंसियं विमलणाणं।
बोच्छं दंसणसारं जह कहियं पुव्वसूरीहि।
भरहे तिथयराणं पणमिय देविंदणागरुडाणं।
समएसु होंति केई मिच्छत्तपवट्टगा जीवा॥
सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो।
पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बुड्डकित्तिमुणी।।
णदियडे वरगामे कुमारसमो सत्यपिणः।
कट्ठो दंसणभट्टो जादो सल्लेहणाकाले॥
तत्तो दुसए तीदे महुराए माहुराण गरुणाहो।
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वणियं तेण।
दर्शनसारसे देवसेनके अक्खड़ स्वभावका पता चलता है। उन्होंने अन्तिम गाथामें अपनी स्पष्टता व्यक्त करते हुए लिखा है-
रूसउ तूसउ लोओ सच्चं अक्खंतयस्स साहुस्स।
कि जूयभए साडी विज्जियव्वा णरिदेण।।
सत्य कहने वाले साधुसे कोई रुष्ट हो, चाहे सन्तुष्ट हो, इसकी चिन्ता नहीं। क्या राजाको युका (जूआ) के भयसे वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं।
इससे देवसेनका अक्खड़पना प्रकट होता है।
२. भावसंग्रह
इस ग्रन्यमें ७०१ गाथाएँ हैं। इसमें चौदह गुणस्थानोंका अवलम्बन लेकर विविध विषयोंका निरूपण किया गया है। दो गाथाओं द्वारा १४ गुणस्थानोंके नाम बतला कर मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप प्रतिपादित किया है। मिथ्यात्वके एकान्त, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत इन पांच भेदोंको बतलाकर ब्राह्मण मतको विपरीतमिथ्यादृष्टि कहा है-
मण्णाइ जलेण सुद्धि तित्ति मंसेण पियरवग्गस्स।
पसुकयवहेण सग्गं घम्म गोजोणिफासेण॥
जह जलण्हाणपउता जोवा मुइ णिययपावेण।
तो तत्व वसिय जलयरा सव्वे पावंति दिवलोयं।।
जं कम दिढबद्धं जीवपएसेहि तिविहजोएण।
तं जलफासणिमित्ते कह फट्टइ तित्थाण्हाणेण।।
मलिणो देहो णिच्वं देही पुण णिम्मलो सयारुवी।
को इह जलैण सुज्झइ तम्हा ण्हाणे ण हु सुद्धी॥
जलसे शुद्धि होती है, मांससे पितरोंकी तुसि होती है, पशुबलिसे स्वर्ण मिलता है और गोयोनिके स्पर्शसे धर्म होता है, इन चार ब्राह्मणधर्मके प्रमुख सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए बताया है कि जलस्नानसे यदि समस्त पापोंका प्रक्षालन सम्भव हो, तो नदी, समुद्र और तालाबोंमें रहनेवाले जलचर जीव भी स्वर्गको प्राप्त कर लेंगे। कर्म मैलसे मलिन इस आत्माको जलसे शुद्धि नहीं हो सकती है, जो जलसे शुद्धि मानता है, वह अच्छा विचारक नहीं है। आत्माकी शद्धि तप, इन्द्रियनिग्रह और रत्नत्रयके द्वारा होती है। जिस प्रकार अग्निके संयोगसे स्वर्ण पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार अनशन, ऊनोदर आदि तपोंके करनेसे जीव भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति विषय और कषायमें संलग्न हैं और राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले गृहकार्योंमें आसक्त हैं उनकी जलस्नानसे शुद्धि नहीं हो सकती। कषायरहित, प्रतनियम और शीलसे युक्त व्यक्ति जल स्नानके बिना भी आत्माको पवित्र कर सकता है।
माँसद्वारा पितरोंकी तृप्ति मानने वाला व्यक्ति भी विवेकी नहीं है। हिंसा, कृरता और निर्दयता करने वाला व्यक्ति चारों गतियोंके दुःखोंको उठाता है। जो मांस द्वारा श्राद्ध करके पितरोंकी ताप चाहता है वह व्यक्ति भी बालूसे तेल निकालना चाहता है। अतएव मांसको न तो दान ही माना जा सकता है, और न इससे पितरोंकी तृप्ति ही हो सकती है।
जो श्राद्धद्वारा पितरोंकी तृप्ति मानता है, वह भ्रममें है। किसीके भोजनसे किसीकी तृप्ति नहीं हो सकती। यदि पित्ता भोजन करता है, तो पुत्रका पेट नहीं भरता, और पुत्र भोजन करता है तो पिताका पेट नहीं भरता। जो भोजन करता है, वही तृप्त हो सकता है, अन्य कैसे तुप्त हो सकता है? जो यह मानता है कि पाप करके नरक जाने पर पिताको पिण्डदानद्वारा पुत्र स्वर्ग भेज सकता है, उसके यहाँ जो कार्य करने वाला है उसे फल न मिल कर अन्यको होगा। अतः कृतनाश और अकृताभ्यागम नामक दोष आयगा। इस प्रकार उक्त चारों सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए गीता, महाभारत आदि ग्रन्थोंसे ही समर्थन के लिए प्रमाण उद्धृत किये हैं।
विपरीतमिथ्यात्वके पश्चात् एकान्तमिथ्यात्वकी समीक्षा की गयी है। इस प्रसंगमें क्षणिककान्तवादी बुद्धका खण्डन किया है। वैनायिक मिथ्यात्वके निरसनमें यक्ष, नाग, दुर्गा, चण्डिका आदिके पूजनेका निषेध किया है। संशयमिथ्यात्वका निरूपण करते हुए उदाहरणके हेतु श्वेताम्बर मतका निरसन किया गया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीमुक्ति, केवली कवलाहार और साधुओंका वस्त्र पात्र रखना इन तीनों बातोंकी आलोचना की गयी है। श्वेताम्बर अपने साधुओंको स्थविरकल्पी बतलाते हैं। ग्रन्थकारके मतसे वे स्थविर नहीं, बल्कि गृहस्थकल्पी हैं। जिनकल्प और स्थविरकल्पका विवेचन विस्तार पूर्वक किया है। इस सन्दर्भमें बताया है-
दुद्धरतवस्स भग्गा परिसहविसएहि पौडिया जे य।
जो गिहकप्पो लोए स थविरकप्पो कओ तेहि॥
अर्थात् परीषहसे पीड़ित और दुर्द्धर तपसे भीत बनोने गृहस्थकल्पको स्थविर कल्प बना दिया है। १३७ वी गाथासे श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा दी गयी है। इस कथामें बताया है कि सौराष्ट्र देशकी बलभी नगरी में वि. सं. १३६ में श्वेताम्बर संघकी उत्पत्ति हुई। दर्शनसारमें भी श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिका यही समय अंकित किया गया है।
अज्ञानमिथ्यात्वका कथन करते हुए लिखा है कि भगवान पार्श्वनाथके तीर्थकल्पमें मस्करीपूरण नामक ऋषि हुआ। यह भगवान महावीरके समवचरणमें गया, किन्तु उसके जानेपर भगवानकी वाणो नहीं खिरी। वह रुष्ट होकर समवशरणसे चला आया और कहने लगा-मैं ग्यारह अंगोंका धारी हूँ, फिर भी मेरे जाने पर तीर्थंकर महावीरकी दिव्यध्वनि प्रवाहित नहीं हुई और गौतमके आने पर दिव्यध्वनि होने लगी। गौतमने अभी दीक्षा ली है। वह तो वेदवादी पण्डित है। वह जिनोक्त श्रुतको क्या जाने। अतः उसने अज्ञानसे लोगोंके मध्य मोक्षका उपदेश दिया-
अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणो हु।
देवो ण अत्थि कोई सुण्णं झाएह इच्छाएँ।
अर्थात् अज्ञानसे ही मोक्ष होता है। इसके लिये ध्यान, संयम, तप, सज्ञान की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार पांचों मिथ्यात्वोंकी समीक्षा करनेके पश्चात् चार्वाकके द्वारा मान्य दर्शनकी समीक्षा की है। चार्वाक चैतन्यको भूतोंका विकारमात्र मानता है। ग्रन्थकारने इसे कोलिकाचार्यका मत कहा है-
कउलायरिओ अक्खइ अत्थि ण जीवो हु कस्स तं पावं।
पुण्णं वा कस्स भवे को गच्छइ णरय-सग्गं वा।।
यह कोलिकमत शैवतन्त्रका एकमत है। एक प्रकारसे यह वामाङ्गो है। माँस, मदिराके सेवनके साथ स्त्रिरमण एवं स्वयं शिव-पार्वतीका प्रतिरूपक अपनेको मानना आदि इसके सिद्धान्त हैं। यहाँ हमें ग्रंथकारका भ्रम प्रतीत होता है। कौलिक और चार्वाक ये दोनों मत स्वतन्त्र हैं। दोनोंमें समता इतनी है कि पुण्य-पाप, परलोक आदिकी स्थिति दोनोंमें तुत्य है। कौलिक मतके ग्रन्योंमें वामाचारकी भी पुण्यरूप कहा गया है तथा वाममार्गीधर्माचरणसे स्वर्गादिक सुखोंकी उपलब्धि भी मानी गयी है। शिव और पार्वती रूप कृत्य-अकृत्योंका संकल्प कर लेने पर कहीं कोई बाधा नहीं आती और स्वर्गादिक प्राप्त हो जाते हैं।
चार्वाकमतके पश्चात् सांख्यमतकी समीक्षा की गयी है। बताया है कि जीव सदा अकर्ता है और पुण्य-पापका भोक्ता भी नहीं है। ऐसा लोकमें प्रकट करके बहन और पुत्रीको भी अंगीकार किया गया है। यथा-
जीवो सया भकत्ता भूत्ता ण हु तुम गलस्म।
इय पयडिऊण लोए गहिया वहिणी सधूया वि।।
धूयमायरिवहिणि अण्णावि पुत्तस्थिणि।
आयति य पासवयणुपयडे वि विप्पे।
जह रमियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पे॥
बंभणि-छिपिणि-डोंवि-नडिय-वरुडि-रज्जइ-चम्मारि।
कवले समइ समागमइ तह भूति य परणारि।।
अर्थात् पुत्री, माता, बहन या अन्य कोई भी नारी पुत्रोत्पत्तिको भावनासे कामवचन प्रकट करे, तो कामातुर हो वेदज्ञानी ब्राह्मणको उसका उपभोग करना चाहिये। लेखकने बतलाया है कि कपिलदर्शनमें प्रतिपादित ब्राह्मणी, डोम्बी, नटी, घोबिन, चमारिन आदि परनारियोंके साथ भोग करना उचित है।
स्मृतिकारोंके इस कथनका आशय लेकर कि जो पुरुष स्वयं भागता नारीका भोग नहीं करता उसे बह्महत्याका पाप लगता है; को लक्ष्य में रखकर ही उक्त कथन किया गया है। सांख्यदर्शनके साथ इसका कुछ भी मेल नहीं है। हाँ, कौलिक सम्प्रदायमें उक्त सिद्धान्त अवश्य स्वीकृत है। राजशेखरने अपनी 'कर्पूरमंजरी-सट्टक’ में रण्डा, चण्डा आदिके भोगका औचित्य बतलाया है। अतः कपिलदर्शनका यह सिद्धान्त न होकर, स्मृति या कौलिक सम्प्रदायका सिद्धान्त है। देवसेनने इसी सिद्धान्तकी समीक्षा को है।
तुतीय मिश्रगुणस्थानका कथन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी समालोचना की गयी है। ब्रह्माकी आलोचना करते हुए तिलोत्तमा आदिके उपाख्यानोंको उपस्थित किया है। विष्णकी आलोचनामें उनके विभिन्न अवतारोंकी समीक्षा की गयी है। रुद्रकी आलोचनामें उनके स्वरूप और ब्रह्महत्या आदि कार्योंकी समीक्षा आयी है।
चतुर्थ अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए सात तत्त्वोंका कथन किया गया है। पांच गुणस्थानका स्वरूप २५० गाथाओंके द्वारा बहुत विस्तारसे बतलाया है। इसमें अणुव्रत, गुणव्रत, और शिक्षाव्रतोके साथ अष्टमूलगुणोंका भी उल्लेख आया है। चार प्रकारके ध्यान, देवपूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, आदि श्रावकाचारका भी निरूपण आया है। अभिषेकके समय यम, वरुण, कुवेर, ईशान आदिके आह्वानपूर्वक पन्चामृत-अभिषेक करनेका विधान किया है।
षष्ठ व सप्तम गुणस्थानके स्वरूपकथनमें पिण्डस्थ, पदस्थ रूपस्थ, और रूपातीत ध्यानोंका कथन आया है। शेष गुणस्थानोंका सामान्यतया स्वरूपविवेचन हुआ है। गणस्थानोंके स्वरूपकथनमें देवसेनने पंचसंग्रहप्राकृतसे अनेक गाथाएँ ज्यों-को-त्यों रूपमें ग्रहण की हैं। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने गोम्मटसारमें पंचसंग्रहकी अनेक गाथाएँ ग्रहण की हैं। यहाँ तुलनाके लिए कतिपय सामान गाथाएँ दी जाती हैं-
मिच्छो सासण मिस्सो अविरयसम्मो य देसविरदो य।
विरओ पमत्त इसरो अपुव्व अणियट्टि सुहमो य।।
उपसंत खीणमोहे सजोइकेलिजिणो अजोगी य।
ए चउदस गुणठाणा कमेण सिहा य णायव्या।।
णो इंदिएसु विरोओ णो जीवे थावरे तसे वा पि।
जो सद्दहइ जिणुतं अविरइसम्मो त्ति णायव्वो।
इस प्रकार अनेक गाथाएँ पंचसंग्रहमें प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, भाव संग्रहकी कई गाथाएँ कुछ रूपान्तरके साथ राजशेखरकी कर्पूरमंजरीमें भी मिलती हैं। कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें पंचसंग्रह और धवलाटीकाका मिश्रित रूप है।
जे तसवहाउ विरदो णो विरओ अवखथावरवहाओ।
पडिसमयं सो जोवो बिरयाविरओ जिणेक्कमई।।- गाथा १३
जो तसबहादु बिरदो अविरद तह य थावरवहाओ।
एक्कसमम्मि जीवो विरदाविरदो जिणेवकमाई।।- गाथा ३१
जो तसवहाउ विरओ णो विरओ तह य थावरवहाओ।
एक्कसमर्याम्म जीवो विरयाविरज त्ति जिणु कहई।।- गाथा ३५१
भावसंग्रहपर कुन्दकुन्दाचार्य के पञ्चास्तिकाय ग्रंथका भी प्रभाव है-
जीवो त्ति हवदि वेदा उचओयविसेसिदो पहूं कत्ता।
भोत्ता य देहमेतो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो।।
पाणेहि चदुहिं जीवदि जीवरसदि जो हु जीविदो पुव्वं।
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासो।।
जीवो अणाइ णिच्चो उवओगसंजुदो देहमित्तो य।
कत्ता भोक्ता चेता ण हु मुत्तो सहावउड्ढगई।।
पाणचउक्कपउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पुव्वं।
जोवेइ वट्टमाणं जीवत्तगगुण समावण्णो॥
स्पष्ट है कि भावसंग्रहपर पञ्चास्तिकायका भी प्रभाव है।
३. आराधनासार
एकसी पन्द्रह प्राकृत-गाथाओंमें यह ग्रंथ रचा गया है। आराधनाओंका वर्णन करते हुए बताया है-
आराहणाइसारो तव-दंसण-णाण-चरणसालानी।
सो दुम्भेओ उत्तो ववहारो चेन पप।।
अर्थात् तपाराधना, दर्शनाराधना, झानाराधना और चारित्राराधना इन चारों आराधानाओका सार इसमें गिर रहेगा। माइ माराधनामगर दो प्रकारका है- (१) व्यवहार और (२) परमार्थ। व्यवहार-आराधनाका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि सूत्र और अर्थ द्वारा कथित वस्तुको ग्रहण करना ज्ञानाराधना है। अर्थात् तीर्थंकरकी वाणी द्वारा प्रतिपादित ११ अंग और १४ पूर्वोको अवगत करना ज्ञानाराधना है। मावशुद्धिपूर्वक १३ प्रकारके चारित्रका आचरण करना चारित्राराधना है। १३ प्रकारके चारित्रमें ५ महाव्रत, ५ समिति ओर ३ गप्तीको स्थान दिया गया है। १२ प्रकारके तपोंका आचरण करनेके लिए प्रवृत्त होना तपाराधना है। इस प्रकार व्यवहार-आराधनाका स्वरूप कथन कर निश्चय-आराधनाफा स्वरूप बसलाते हुए लिखा है-
सुद्धणये चउखंध उत्तं आराहणाइ परिसिय!
सम्ववियप्पविमुक्को सुद्धो अप्पा णिरालंबो।।
अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सपरूप इन चारों भेद- विकल्पोंका त्याग कर पञ्चेन्द्रियके विषयसुखसे रहित निर्विकल्प आत्मतत्वका आराधन करना निश्चय-आराधना है। आगे इसीके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन करते हुए बताया है-
सद्दहइ सहावं जाणइ अप्पाणमामणो सुद्धं।
तं चि य अणुचरइ पुणो इंदियविसए णिरोहिता।
अर्थात् स्वस्वरूपका श्रद्धान करना, शुद्ध आत्माको जानना और निज आत्मरूप आचरण करना एवं निज स्वरूप तपश्चरण करना निश्चयाराधना है। निश्चय-आराधनामें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ रुक जाती हैं और आत्मस्वरूप श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और तपाराधना होने लगती है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपरूप आत्मा ही है, जो राग-द्वेष छोड़कर इस शुद्ध आत्माका आराधन करता है उसीकी निश्चय-आराधना होती है।
जीव चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, भ्रमण करेगा और भ्रमण किया है। इसका कारण ज्ञानमयो आत्माराधनको प्राप्त न करना है। मरणकालमें वही व्यक्ति आत्माराधन कर सकता है जो राग-द्वेष रहित है। बताया है-
अप्पसहावे णिरओ वज्जियपरदव्वसंगसुक्खरसो।
णिग्गहियरायदोसो हवई आराहमो मरणे॥
जो रयणत्तयमइओ मुत्तूणं अप्पणो विसूदप्पा।
चितेइ य परवव विराहओ णिच्छयं भणियो।
राग-द्वेषोंको दूर कर और परद्रव्योंके संयोगजन्य सुखका त्याग कर जो आत्मस्वभावमें निरत है वहीं मरण-कालमें आराधक होता है। जो रत्नत्रय मयी विशुद्ध आत्माको छोड़कर परद्रव्योंका चिन्तन करता है वह आराधनाका विराधक माना जाता है। जो न सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्ररूप आत्माकी समझता है और न आत्मासे विलक्षण शरीरादि परद्रव्योंको ही जानता है, उसे न ज्ञानकी प्राप्ति रहती है और न आराधनाकी हो।
जब तक वृद्धावस्था नहीं भाती है, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, बुद्धि नष्ट नहीं होती है, आयरूपी जल समाप्त नहीं होता है तब तक आत्मकल्याणके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचता रहता है कि अभी तो युवावस्था है, विषयसुख-सेवनके दिन हैं वह वृद्धावस्था आने पर कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपरूप आराधनाकी प्राप्ती शारीरिक शक्ति और इन्द्रियोंकी शक्ति रहने पर ही सम्भव है। बताया है-
जरवग्घिणी ण चंपइ जाम ण वियलाइ हुति अक्खाई।
बुद्धी जाम ण णासइ आउजलं जाम ण परिगलाई।
जा उज्जमो ण वियलइ संजम-तत्र-णाण-झाणजोएसु।
तावरिहो सो पुरिसो उत्तमठाणस्स संभवई।
बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रहका त्यागकर अन्तरक कषाय और विकारोंको कुश करनेका प्रयास करना ही वास्तविक आराधना है। कषाएँ अत्यधिक शक्तिशाली हैं। इन्हींके कारण चतुर्गति परिभ्रमण होता है। जब तक कषाय और भोगोंका त्याग नहीं किया जायेगा, तब तक संयमकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है और संयमरहित व्यक्तिके गुण विशुद्ध नहीं हो सकते। बताया है-
जाम ण हणइ कसाए सकसाई णेव संजमी होई।
संजमसहियस्स गुणा ण हूंति सव्वे विसुद्धियरा।
जो परीषहोंको सहन करता हुआ शान्तिभावपूर्वक व्रत, समिति और गुप्तियोंका पालन करता है वह अनादिकालीन काम-क्रोधादिको नष्ट कर देता है। इस प्रसङ्गमें उपसर्ग और परीषहोंको सहन करनेवाले शिवभूति, सूकुमाल और सुकोशलके उदाहरण दिये गये हैं और मनुष्यकृत उपसर्ग सहन करने में गुरुदत्त, पाण्डव और गजकुमारके आख्यान दृष्ट्वान्तके रूपमें प्रस्तुत किये हैं। देवकृत उपसर्गके सहन करने में प्रसिद्ध हुए श्रीदत्त, सुवर्णभद्र आदिके उदाहरण दिये गये हैं। इस प्रकार उदाहरणों और प्रत्युदाहरणों द्वारा सैद्धान्तिक विषयको भी सरस बनानेकी चेष्टा की है।
मन, वचन और कायको वश करनेकी आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा है-
सिक्सह मणवसियरणं सवसीहूएण जेण मणुआणं।
णासंति रार-दोसे तेसिं णासे समो परमो।।
मनको वश में करनेको शिक्षा देनी चाहिए। जिसका मन वशीभूत है वही राग-द्वेषको नाश कर सकता है और राग-द्वेषके नाश करनेसे ही परमपदकी प्राप्ति होती है।
उपशमवान जीव ही मनका निग्रह कर सकता है और मनका निग्रह करनेसे ही आत्मा परमात्मापदकी प्राप्त कर सकती है।
आचार्यने ध्यान, ध्याता और ध्येयका लक्षण बतलाया है और ध्यानके द्वारा ही सकल कर्मोका नाश होता है। अतः राग-द्वेष, मोहका विनाश करने पर ही ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है। जो यह अनुभव करता है कि न मैं देह हूँ, न मन हूँ और न मुझमें दुःख ही है वह क्षपक समभावनासे युक्त होकर दुःखका विनाश कर लेता है। यथा-
णाई देहो ग मणो ण तेण में अत्थि इत्थ दुक्खाई।
समभावणाइ जुत्तो वि सहसु दुक्खं अहो खवय।।
इस प्रकार समस्त परिग्रहका त्यागकर आत्मसाधनामें संलग्न रहनेका निर्देश किया है।
४. तत्त्वसार
इस ग्रन्थमें ७४ गाथा हैं। तत्वके मूलत: दो भेद है- (१) स्वगत तत्व और परगत तत्व। स्वगत तत्व निजात्मा है और परगत तत्वमें परमेष्ठी हैं। स्वगत तत्वके भी दो भेद है- (१) सविकल्पक और (२) निर्विकल्पक। आस्त्रवसहितको सविकल्पक कहते हैं और आस्त्रवरहितको निर्विकल्पक। इन्द्रियविषय- सुख के समाप्त होनेपर मनकीको चंचलता जब अरुवद्ध हो जाती है तब आत्मा अपने स्वरूपमें निर्विकल्प हो जाता है। यथा-
जं पुणु सगयं तच्चं सवियप्प हबइ तह य अवियप्पं।
सवियप्पं सासवयं णिरासर्व विमयसंकप्पं।।
इंदियविसविरामे मणस्स णिल्लूरणं हवे जइया।
तझ्या तं अविअप्प ससख्ये अप्पणो त तु॥
जो अविकल्पक सत्व है वही मोक्षका कारण है। उसीको शुद्ध समझकर ध्यान करना चाहिए।
इस प्रकरणमें श्रमण और योगीकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है- "मन वचन-कायसे जो बाह्म और आभ्यन्सर परिग्रहसे रहित है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है और जिसने जिनलिमा आश्रय ग्रहण किया है वह श्रमण कहलाता है-
बहिरव्भतरगंथा मुक्का जेणेह तिविहजोएण।
सो णिग्गंधी भणिओ जिणलिंगसमासिओ सवणों।।
लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, मित्र-शत्रुको जो समानरूपसे ध्यान करता है वह योगी है। यथा-
लाहालाहे सरिसो सुहदुक्खे तह य जीविए मरणे।
बंधव-अरयसमाणो झाणसमत्थो हु सो जोई॥
जो व्यक्ति आत्माकी सिद्धि करना चाहता है वह ध्यान द्वारा कर्मोंका क्षय कर मोक्षको प्राप्त करे। यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप है, असंख्यात प्रदेशी है और प्रदेशोंके संहार तथा विसर्पणके कारण यह शरीरप्रमाण है जो राग, द्वेष, मोहका त्याग कर जन्म-जरा-मरणसे रहित इस निरञ्जन आत्माका ध्यान करता है वह सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। आत्मामें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न शब्द है। यह तो शुद्ध चेतनस्वरूप निरञ्जन है। यथा-
फासरसरूवगंधा सद्दादीया य जस्स गरिय पुणो।
शुद्धो चेयणभावो णिरंजणो सो अहं भणियो।
व्यवहारनयसे इस आत्मामें कर्म-नोकर्म माने जाते हैं। आत्मा और कर्मका सम्बन्ध दूध-पानीके समान है। जिस प्रकार दूध और पानी अपने-अपने स्वभावसे विकृत होकर एकमें एक मिल जाते हैं उसी प्रकार आत्मा और पौद्गलिक कर्म भी अपने-अपने स्वभावको छोड़ एकमें एक मिल गये हैं। अतएव में शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ज्ञानरूप हूँ, कर्म-नोकर्मसे रहित हूँ, एक हूँ, निरालम्ब हूँ, देहप्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यातदेशिक हूँ, अमर्त हूँ। इस प्रकार चिन्तन कर आत्म स्वरूपको प्राप्त करना चाहिए। जब तक पर द्रव्योंसे चित्त व्यावृत्त नहीं होता तब तक भव्यजीव मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी उग्र तप क्यों न करता रहे। आत्मसिद्धिका मूलकारण राग-द्वेष और विषयसुखसे मुक्ति प्राप्त कर लेना है।
यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है तथा इसमें आत्मानुभूति तथा आत्मसिद्धिका उपाय वर्णित है।
५. लघुनयचक्र
इस ग्रन्थमें ८७ गाथाएँ हैं । नयका स्वरूप, उपयोगिता एवं उसके भेद प्रभेदोंका वर्णन किया है । नयका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-
जं णाणीण वियप्पं सुयभेयं वत्यूयंससंगहण।
ते इह णयं पउत्तं णाणी पुण तेहि णाणेहि॥
जो वस्तुके एक अंशका ग्रहण करता है श्रुतज्ञानका वह भेद नय कहलासा है। नयके बिना वस्तुस्वरूपकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है और नय द्वारा ही स्याद्वादका ज्ञान होता है। अतः नयका ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुकी प्रतिपत्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। नयसे जिन वचनोंका बोध होता है और नयसे ही वस्तुकी प्रतिपत्ति होती है। भूल नय दो है- द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। नयके सामान्यतया नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत ये सात भेद हैं। अन्य भेद निम्न प्रकार हैं-
दव्वत्थं दहमेयं छब्भेयं पज्जयत्थियं यं।
तिविहं च णेगमं तह दुविहं पुण संगहं तत्थ।।
ववहार रिउसुतं दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का।
उत्ता इह णयमेया उपणयभेया वि पभणामो॥
द्वव्यार्थिकके १० भेद, पर्यायार्थिकके ६ भेद, नैगम नयके तीन भेद, संग्रहके दो, व्यवहार और ऋतुसूत्रके दो-दो भेद और शेष नयोंका एक-एक भेद है। उपनयके तीन भेद हैं- (१) सद्भुत, (२) असद्भुत और (३) उपचरित नय। सद्भुतके दो भेद हैं और असद्भुत के तीन तथा उपचरितके तीन। इस प्रकार नयके भेद-प्रभेदोंका कथन कर द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंकी अपेक्षासे वस्तु-विवेचन किया गया है।
६. आलाप-पद्धति
यह संस्कृत-गद्यमें रचित छोटी-सी रचना है। अन्य ग्रंथोंके समान इसका प्रकाशन भी माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमालासे हुआ है। इस ग्रंथमें गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नय, गुण-व्यत्पत्ति, स्वभाव-व्युत्पत्ति, प्रमाणका कथन, निक्षेपको व्युत्पत्ति, नयोंके भेदोंको व्युत्पत्ति एवं अध्यात्मनयोंका कथन किया गया है। आरम्भमें वचनपद्धतिको ही आलापपद्धति कहा है। यह ग्रन्थ निम्नलिमित अधिकारों में विभक्त है-
१. द्वव्याधिकार,
२. गुणाधिकार,
३. पर्यायाधिकार,
४. स्वभावाधिकार,
५. प्रमाणाधिकार,
६. नय-अधिकार,
७. गुण व्युत्पत्ति अधिकार,
८. पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार,
९. स्वभावव्युत्पत्ति-अधिकार,
१०. एकान्तपक्षमें दोष,
११. नययोजना,
१२ प्रमाणकथन,
१३. नयलक्षण और भेद,
१४. निक्षेप व्युत्पत्ति,
१५. नयोंके भेदोंकी व्युत्पत्ति,
१६. अध्यात्मनय।
नामानुसार विषयोंका निरूपण इन अधिकारोंमें किया गया है। जैन सिद्धान्तकी अवगत करनेके लिए यह छोटा-सा ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। द्रव्यके सामान्य और विशेष गुणोंका विवेचन करते हुए लिखा है-
"अस्तित्वं, वस्तुत्त्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्व मचेतनत्वं, मूर्त्तत्वममूर्तत्वं द्रव्याणां दश सामान्यगुणाः। प्रत्येकमष्टावष्टो सर्वेषाम्।”
[एकैकद्रव्ये अष्टौ अष्टौ गुणा भवंति। जीवद्रव्ये अचेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति, पुद्गलद्रव्ये चेतनत्वममूर्तत्वं च नास्ति, धर्माधर्माकाशकालद्रव्येषु चेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति। एवं द्विद्विगुणजिते अष्टौ अष्टौ गुणाः प्रत्येकद्रव्ये भवन्ति।]
ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि स्पर्शरसगंधवर्णा: गतिहेतुत्वं स्थितिहेतुत्वमवगाहन हेतुत्वं वर्तनाहेतुत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं मूर्तस्वममूर्तत्वं द्रव्याणां षोडश विशेष गुणा:।
"अर्थात् अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रभेयत्व, अगुरुलवुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सामान्यगुण हैं। सदेव द्रव्योंके साथ रहते हैं, द्रव्योंसे पृथक् नहीं होते। प्रत्येक द्रव्यमें दश सामान्य गुणोंमेंसे आठ-आठ गुण रहते हैं, दो-दो गुण नहीं होते। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेषगुण हैं।"
इस प्रकार द्रव्य, गुण, स्वभावके अतिरिक्त नय और प्रमाणका भी विवेचन किया है।
सारस्वसाचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।
सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-
१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।
२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।
३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।
४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।
५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।
६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन।
७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन।
सारस्वताचार्यों में सर्वप्रमुख स्वामीसमन्तभद्र हैं। इनकी समकक्षता श्रुत घराचार्यों से की जा सकती है। विभिन्न विषयक ग्रन्थ-रचनामें थे अद्वितीय हैं।
Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara- 2
Acharya Shri Devsen Ji
#devsenjimaharaj
15000
Acharya Shri Devsen (Prachin)
#devsenjimaharaj
devsenjimaharaj
You cannot copy content of this page