हैशटैग
#kartikeymaharaj

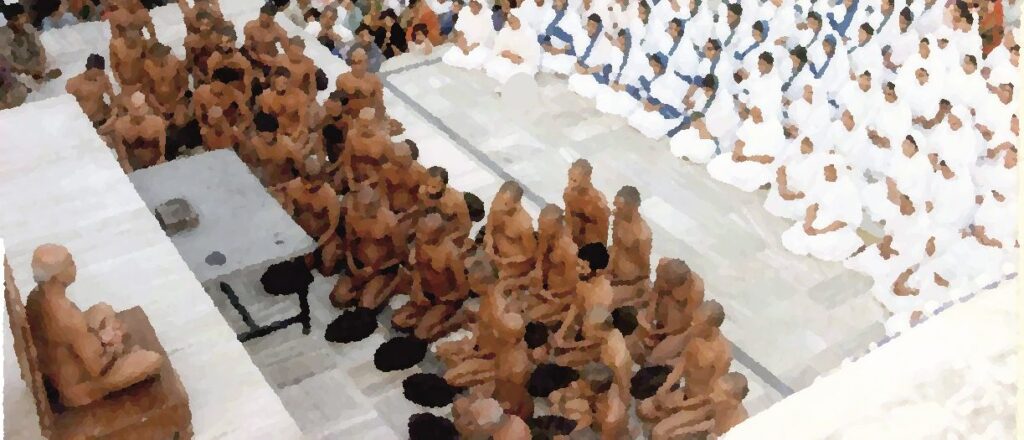
श्रुतधराचार्यों की परंपरामें आचार्य कार्तिकेय का नाम आता है। कुमार या कार्तिकेयके सम्बन्ध में अभी तक निर्विवाद सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। हरिषेण, श्रीचन्द्र और ब्रम्हनेमिदत्तके कथाकोषोंमें बताया गया है कि कार्तिकेयने कुमारावस्थामें ही मुनि दीक्षा धारण की थी। इनकी बहनका विवाह रोहेड नगरके राजा क्रौञ्चके साथ हुआ था और उन्होंने दारुण उपसर्ग सहन कर स्वर्गलोकको प्राप्त किया। ये अग्निनामक राजाके पुत्र थे।
'तस्वार्थवातिकमें' अनुत्तरोपपाददशांगके वर्णन-प्रसंगमें दारुण उपसर्ग सहन करनेवालोंमें कार्तिकेयका भी नाम आया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि कार्तिकेय नामके कोई उग्र तपस्वी हुए हैं। ग्रंथके अन्तमें जो प्रशस्ति गाथाएँ दी गयी हैं वे निम्न प्रकार है-
जिणवयणभावणठ्ठ, सामिकुमारेण परमसद्धाए।
रइया अणुवेहाओ, चंचलमणरुंभणठ्ठ च।।
वारसअणुवेक्खाओ, भणिया हु जिणागमारगुसारेण।
जो पढइ सुणइ भावइ, सो पावइ सासयं सोक्खं।
तिहयणपहाणसामि, कुमारकालेण तवियतवयरणं।
वसुपुज्जसुयं मल्लि, चरमत्तिय सथुवे णिच्चं।।
यह अनुप्रेक्षानामक ग्रंथ स्वामी कुमारने श्रद्धापूर्वक जिनवचनकी प्रभावना तथा चंचल मनको रोकने के लिए बनाया।
ये बारह अनुप्रेक्षाएँ जिनागमके अनुसार कहा है, जो भव्य जीव इनको पढ़ता, सुनता और भावना करता है, वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। यह भावनारूप कर्तव्य अर्थका उपदेशक है। अतः भव्य जीवोंको इन्हें पढ़ना, सुनना और इनका चितन करना चाहिए।
कुमार-कालमें दीक्षा ग्रहण करनेवाले वासुपूज्याजिन, मल्लिजिन, नेमिनाथजिन, पार्श्वनाथजिन एवं वर्धमान इन पांचों बाल-यातियोंका में सदैव स्तवन करता हूँ।
इन प्रशस्ति-गाथाओंसे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं-
१. वारस अनुप्रेक्षाके रचयिता स्वामी कुमार हैं।
२. ये स्वामी कुमार बालब्रह्मचारी थे। इसी कारण इन्होंने अन्त्य मंगलके रूपमें पांच बाल-यतियोंको नमस्कार किया है।
३. चन्चल मन एवं विषय-वासनाओंके विरोधकेलिए ये अनुप्रेक्षाएँ लिखी गई है।
मथुराके एक अभिलेखमें उच्चनागरके कुमारनन्दिका उल्लेख आया है- क्षुणे उच्चैनगिरस्यायंकुमारनन्दिशिष्यस्य मित्रस्य।
एक अन्य अभिलेखमें भी कुमारनन्दिका नाम प्राप्त होता है।
इन अभिलेखोम कुमारनन्दिका नाम आया है और उन्हें नागर शाखाका आचार्य कहा है। इस शाखाका अस्तित्व ई. सनकी आरंभिक शताब्दीयोमें था और इस शाखाके आचार्योंने सरस्वती-आन्दोलनमें ग्रन्थ-निर्माणका कार्य किया। अतः कुमारनन्दि और स्वामी कुमार यदि एक व्यक्ति हों, तो उनका समय ई. सन् की आरम्भिक शताब्दी माना जा सकता है। पर अभी तक उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इन दोनांका अभिन्नत्व सिद्ध नहीं है।
संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि स्वामी कार्तिकेय प्रतिभाशाली, आगम पारगामी और अपने समयके प्रसिद्ध आचार्य हैं। यो परम्परासे कार्तिकेयकी द्वादश अनुप्रेक्षाएँ मानी जाती हैं। इस ग्रन्थमें कहीं पर भी कातिकेयका नाम नहीं आया है और न ग्रन्थको ही कार्तिकेयानुप्रेक्षा कहा गया है। ग्रन्थके प्रतिज्ञा और समाप्ति वाक्योंमें ग्रन्थका नाम सामान्यत: 'अणुपेहा' या 'अणुपेक्खा' और विशेषतः 'बारस अणुवेक्खा' नाम आया है। भट्टारक शुभचन्द्रने इस ग्रन्थपर विक्रम संवत् १६१३ (ई. सन् १५७६) में संस्कृत टीका लिखी है। इस टीकामें अनेक स्थानोंपर ग्रन्थका नाम कार्तिकेयानुप्रेक्षा दिया है और ग्रन्थकारका नाम कार्तिकेय मुनि प्रकट किया है।
बहुत सम्भव है कि कार्तिकेयशब्द कुमार या स्वामी कुमारका पर्यायवाची यहाँ व्यवहत किया गया हो। यह सत्य है कि शुभचन्द्र भट्टारक के पूर्व अन्य किसी भी पन्धमें बारस-अणुवेक्खाके रचयिताका नाम कार्तिकेय नहीं आया है। शुभचन्द्रने ३९४ संख्यक गाथाकी टीकामें कार्तिकेय मुनिका उदाहरण प्रस्तुत किया है। लिखा है- "स्वामीकार्तिकेयमुनिः क्रौञ्चराजकृतोपसर्ग सोढ्वा साम्य परिणामेन समाधिमरणेम देवलोकं प्राप्त।" स्पष्ट है कि स्वामी कातिकेय मुनि क्रौञ्चराजकृत उपसर्गको समभावसे सहकर समाधिपूर्वक मरणके द्वारा देव लोकको प्राप्त हुए।
भगवती आराधनाकी गाथा-संख्या १५४९ में क्रौञ्च द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए एक व्यक्तिका निर्देश आया है। साथमें उपसर्गस्थान रोहेडक और शक्ति हथियारका भी उल्लेख है। पर कार्तिकेय नामका स्पष्ट निर्देश नहीं है। उस व्यक्तिको अग्निदयितः' लिखा है, जिसका अर्थ अग्निप्रिय है। मूलाराधनादर्पणमें लिखा है- "रोहेडयम्मि रोहेटकनाम्नि नगरे। सत्तोए शक्त्या शस्त्रविशेषेण क्रौञ्चनाम्ना राज्ञा। अग्गिदइदो अग्निराजनाम्नो राज्ञः पुत्रः कार्तिकेय संज्ञः।" अर्थात् रोहेडनगरमें क्रौञ्च राजाने अग्निराजाके पुत्र कार्तिकेय मुनिको शक्तिनामक शस्त्रसे मारा था और मुनिराजने उस दुःखको समत्तापूर्वक सहनकर रनत्रयकी प्राप्ति की थी। इस टीकासे प्रकट होता है कि कार्तिकेयने कुमारावस्थामें मुनिदीक्षा ली थी। बताया गया है कि कार्तिकेयकी बहन रोहेड नगरके क्रौञ्च राजाके साथ विवाहित थी। राजा किसी कारणवश कार्तिकेयसे असन्तुष्ट हो गया और उसने कार्तिकेय को दारुण उपसर्ग दिये। इन उपसर्गोको समत्तासे सहनकर कार्तिकेयने देवलोक प्राप्त किया। इस कथाके आधारपर इतना तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थके रचयिता कार्तिकेय सम्भव है और ग्रंथका नाम भी कार्तिकेयानुप्रेक्षा कल्पित नहीं है।
मूलाचार, भगवती-आराधना और कुन्दकुन्दकृत 'बारह अणुवेक्खा' में बारह भावनाओंका क्रम और उनकी प्रतिपादक गाथाएँ एक ही हैं। यहाँतक कि उनके नाम भी एक हो हैं। किन्तु कार्तिकेयको 'बारहअणुवेक्खा’ में न वह क्रम है और न वे नाम हैं। इसमें क्रम और नाम तत्वार्थसूत्रकी तरह हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्त्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, चोधिदुर्लभ और धर्म इस क्रम तथा नामोसे १२ भावनाएँ आयी हैं। ठीक यही क्रम और नाम कार्तिकेयको 'अणुवेक्खामें’ हैं। अतएव इस भिन्नतासे कार्तिकेय न केवल वट्टकेर, शिवार्य और कुन्दकुन्दके उत्तरवर्ती प्रतीत हाते हैं, अपितु तत्वार्थसूत्रकारके भी उत्तरवर्ती जान पड़ते हैं।
परन्तु यहीं कहा जा सकता है कि तत्त्वार्थसूत्रकारके समक्ष भी कोई क्रम रहा है, तभी उन्होंने अपने ग्रन्थमें उस क्रमको निबद्ध किया है। साथ ही यह भी सम्भावना है कि भावनाओंके दोनों ही क्रम प्रचलित रहे हों, एक क्रमको कुन्दकुन्द, शिवार्य, वट्टकेर आदिने अपनाया और दूसरे क्रमको स्वामी कार्तिकेय, गृद्धपिच्छ आदिने। अतः भावनाक्रमके अपनानेके आधारपर कार्तिकेयके समयका निर्धारण नहीं किया जा सकता और न उनके 'बारह अणुवेक्वा' ग्रंथकी अर्वाचीनता ही सिद्ध की जा सकती है।
स्वामि कात्तिकेयके समयका विचार करते हुए डॉ. ए. एन. उपाध्येने 'बारस-अणुवेक्खा'का अन्तःपरीक्षणकर बतलाया है कि इस ग्रन्थकी २७९ वीं गाथामें 'णिसुणहि' और 'भावहि' ये दो पद अपभ्रंशके आ घुसे हैं, जो वर्तमान काल तृतीय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं। यह गाथा 'जोइन्दु'के योगसारके ६५ वे दोहेके साथ मिलती-जुलती है और दोहा तथा गाथा दोनोंका भाव भी एक है। अतएव इस गाथाको 'जोइन्दु के दोहेका परिवर्तित रूप माना जा सकता है। यथा-
विरला जाणहि तत्तु बहु विरला णिसुणहि तत्तु।
विरला झायहिं तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु॥
विरला णिसुणहि तच्चं विरला जाणंति तच्चदो तच्चं।
विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणा होदि।।
अतः इन दोनों संधार्भोन्के तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर कार्तिकेयका समय जोइन्दुके पश्चात् होना चाहिए।
श्री जुगलकिशोर मुख्तारने डॉ. उपाध्येके इस अभिमतका परोक्षण करते हुए लिखा है कि "यह गाथा कार्तिकेय द्वारा लिखित नहीं है। जिस लोक भावनाके प्रकरणमें यह आयी है, वहाँ इसकी संगति नहीं बैठती।" आचार्य मुख्तारने अपने कथनको पुष्टिके लिए गाथाओंका क्रम भी उपस्थित किया है। उन्होंने लिखा है- "स्वामीकुमारने ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके बनाया है, समुचित प्रतीत नहीं होता- खासकर उस हालतमें जबकि ग्रन्थ भरमें अपभ्रंष भाषाका और कोई प्रयोग भी न पाया जाता हो। बहुत सम्भव है कि किसी दूसरे विद्वानने दोहेको गाथाका रूप देकर उसे अपनी ग्रंथ-प्रतिमें नोट किया हो, और यह भी सम्भब है कि यह गाथा साधारणसे पाठभेदके साथ अधिक प्राचीन हो, और योगेन्दुने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवर्तनके साथ अपना उक्त दोहा बनाया हो; क्योंकि योगेन्दुके परमार्थप्रकाश आदि ग्रन्थोंमें और भी कितने ही दोहे ऐसे पाये जाते हैं, जो भावपाहुड तथा समाधितंत्रादिके पद्योंपरसे परिवर्तन करके बनाये गये हैं और जिसे डॉ. साहबने स्वयं स्वीकार किया है। जब कि स्वामीकुमारके इस ग्रन्थकी ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आयी। "
आचार्य मुख्तार साहबका यह निष्कर्ष उचित्त मालूम होता है, क्योंकि योगसारका विषय क्रमबद्ध रूपसे नहीं है। इसमें कुन्दकुन्दकी अनेक गाथाओंका रूपान्तरण मिलता है। कुन्दकुन्दने कर्मविमुक्त आत्माको परमात्मा बतलाते हुए; उसे ज्ञानी, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णू, चतुर्मुख और बुद्ध कहा है। योगसारमें भी उसके जिन, बुद्ध, विष्णु, शिव आदि नाम बतलाये है। इसके अतिरिक्त जो इन्दुने कुन्दकुन्दके समान हो निश्चय और व्यवहार नयों द्वारा आत्माका कथन किया है। योगसार और परमार्थप्रकाश इन दोनोंका विषय समान होने पर भी योगसार संग्रहग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। इसमें कई तथ्य छूट भी गये हैं। दोहा ९९-१०३ द्वारा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसाम्पराय संयमका स्वरूप बतलाया है। यहाँ यथाख्यात चारित्रका स्वरूप छूट गया है। अतएव योगसारके दोहेका परिवर्तीत रूप कार्तिकेयानुप्रेक्षामें होनेके आधारपर कातिकेयको अर्वाचीन बताना युक्त नहीं है।
आचार्य जुगलकिशोर मुख्तारने समय-निर्णय करते हुये लिखा है- "मेरी समझमें यह ग्रंथ उमास्वातिके तत्वार्थ सूत्रसे अधिक बादका नहीं, उसके निकटवर्ती किसी समयका होना चाहिये, और उसके कर्ता वे अग्निपुत्र कार्तिकेय मुनि नहीं हैं, जो साधारणत: इसके कर्ता समझे जाते हैं, और क्राँच राजाके द्वारा उपसर्गको प्राप्त हए थे, बल्कि स्वामीकुमार नामके आचार्य ही है, जिस नामका उल्लेख उन्होंने स्वयं 'अन्त्यमंगल'की गाथामें श्लेष रूपसे किया है।
आचार्य जुगलकिशोर मुख्तारके उक्त मतसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्तिकेय गृद्धपिच्छके समकालीन अथवा कुछ उत्तरकालोन हैं। अर्थात् वि. सं. को दूसरी-तीसरी शती उनका समय होना चाहिए।
द्वादशानुप्रेक्षामें कुल ४८९ गाथाएँ हैं। इनमें अघ्र व, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, अस्त्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधदुर्लभ और धर्म इन बारह अनुषेक्षाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। प्रसंगवश जीव, अजीव, अस्त्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वोंका स्वरूप भी वर्णीत है। जीवसमास तथा मार्गणाके निरूपणके साथ, द्वादगवत, पात्रोंके भेद, दाताके सात गुण, दानकी श्रेष्ठता, माहात्म्य, सल्लेखना, दश धर्म, सम्यक्त्वके आठ अंग, बारह प्रकारके तप एवं ध्यानके भेद-प्रभेदोंका निरूपण किया गया है। आचार्यका स्वरूप एवं आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया इस ग्रन्थमें विस्तारपूर्वक वर्णीत है।
अघ्रुवानुप्रेक्षामें ४-२२ गाथाएँ हैं। अशरणानुप्रेक्षाम २३-३१; संसारानुप्रेक्षामें ३२-७३; एकात्वानुप्रेक्षामें ७४-७९; अन्यत्वानुप्रेक्षामें ८०-८२: अशु चित्वानुप्रेक्षामें ८३-८७; आस्त्रवानुप्रेक्षामें ८८-१४; संवरानुप्रेक्षामें ९५-१०१, निर्जरानुप्रेक्षामें १०२-११४, लोकानुप्रेक्षामें ११५-२८३; बोधिदुर्लभानुप्रक्षामें २८४-३०१ एवं धर्मानुप्रंक्षामें ३०२-४३५ गाथाएँ हैं। ४३६ गाथासे अन्ततक द्वादश तपोंका वर्णन आया है। अघ्रुवानुप्रेक्षामें समस्त वस्तुओंकी अनित्यता बतलाते हुए वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक कहा है। सामान्य द्रव्यरूप है, और विशेष गुण पर्यायरूप। द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है किन्तु पर्यायकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य हैं। यह संसारका प्राणी पर्यायबुद्धि है, जिससे पर्यायोंको उत्पन्न और नष्ट होते देखकर हर्ष-विषाद करता है, और उसको नित्य रखना चाहता है। यह शरीर जीव-पुद्गलको संयोग जनित पर्याय है धन-धान्यादिक पुद्गल परणुओंकी स्कन्ध पर्याय है। इनके संयोग और वियोग नियमसे अवश्य है, जो स्थिरताकी बुद्धि करता है, वह मोहजनित भावके कारण संक्लेश प्राप्त करता है।
संसारकी समस्त अवस्थाएँ विरोधी भावोंसे युक्त हैं। जब जन्म होता है, तब उसे स्थिर समझकर हर्ष उत्पन्न होता है, मरण होनेपर नाश मानकर शोक करता है। इस प्रकार इष्टकी प्राप्तिमें हर्ष, अप्राप्तीमें विषाद तथा अनिष्ट प्राप्तिमें विषाद, अप्राप्तीमें हर्ष करता है, यह भी सब मोहका माहात्म्य है। आचार्य सादृश्यमूलक उपमा प्रस्तुतकर परिवार, वन्धुवर्ग, स्त्री, पुत्र, मित्र, धनधान्यादिकी अनित्यताका चित्रण करते हुए कहते है-
अथिरं परियण-सवर्ण, पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावण्णं।
गिह-गोहणाइ सव्वं, णव-घण-विदेण सारित्थ।।
परिवार, बन्धुवर्ग, पुत्र, स्त्री, मित्र, सौन्दर्य, गृह, धन, पशु सम्पत्ति इत्यादि सभी वस्तुएँ नवीन मेध-समूहके ममान अस्थिर हैं। इन्द्रियोंके विषय, भृत्य, अश्व, गज, रथ आदि सभी पदार्थ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं।
पुण्यके उदयसे प्राप्त होने वाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी भी नित्य नहीं हैं, तब वह पुण्यहीन अथवा अल्पपुण्यवाले व्यक्तियोंसे केसे प्रेम करेगी? कविने इसी को समझाते हुए लिखा है-
कत्थ वि ण रमइ लच्छी, कुलीण-धीरे वि पंडिए सूरे।
पुज्जे धम्मिट्ठे वि य, सरूव-सुयणे महासत्ते।
अर्थात् यह लक्ष्मी कुलवान, धैर्यवान, पंडित, सुघट, पूज्य, धर्मात्मा, रूपवान, सुजन, महापराक्रमी इत्यादि किसी भी पुरुषसे प्रेम नहीं करती, यह जल की तरंगोंके समान चंचल है। इसका निवास एक स्थानपर अधिक समय तक नहीं रहता। इस प्रकार आचार्य स्वामिकुमारने संसार, शरीर, भोग और लक्ष्मीकी अस्थिरताके चिन्तनको अघ्रुवानुप्रेक्षा कहा है।
अशरण भावनामें बताया है कि मरण करते समय कोई भी प्राणीकी शरण नहीं। जिस प्रकार वनमें सिंह मृगके बच्चेको जब पैरके नीचे दबा लेता है, तब कोई भो उसकी रक्षा नहीं कर सकता , देव , तप आदि सभी मुत्युसे रक्षा करने में असमर्थ है। रक्षा करनेके लिए जितने उपाय किये जाते हैं, वे सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। आयुके क्षय होनेपर कोई एक क्षणके लिए भी आयुदान नहीं सकता-
आउक्खयेण मरणं आउं दाउं ण सक्कदे को वि।
तम्हा देविदो वि य, मरगाउ ण सक्खदे को वि।
आयुकर्मके क्षयसे मरण होता है और आयुकर्मको कोई देनेमें समर्थ नहीं, अतएव देवेन्द्र भी मृत्युसे किसीकी रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार अशरण रूप चिन्तनका समावेश अशरण-भावनामें होता है।
संसार-अनुप्रेक्षामें बताया है कि संसार-परिभ्रमणका कारण मिथ्यात्व और कषाय है। इन दोनोंके निमित्तसे ही जीव चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता है। हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रहरूप भावनाके कारण विभिन्न गत्तियोंमें इस जीवको परिभ्रमण करना पड़ता है| आचार्यने इस भावनामें चतुरंगतिके दुःखोंका वर्णन भी संक्षेपमें किया है। मनुष्यगतिके हाखोंका प्रतिपादन करते हुए संसार स्वभावका विश्लेषण विश्लेषण किया है-
कस्स वि दुटुकलितं, कस्स वि दुव्वसणवसणिओ पुत्तो।
कस्स वि अरिसमबंधू, कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ।।
मरदि सुपुत्तो कस्स वि, कस्स वि महिला विणस्सदे इट्ठा।
कस्स वि अग्गीपलितं, गिहं कुडंबं च डज्झेई।।
संसारमें सुख नहीं है। इस मनुष्यगतिमें नानाप्रकारके दुःख हैं। किसीकी स्त्री दुराचारिणी है, किसीका पुत्र व्यसनी है, किसीका भाई शत्रुके समान कलहकारी है। एवं किसीकी पुत्री दुश्चरित्रा है। इस प्रकार संसारकी विषम परिस्थिति मनुष्यको सुखका कण भी प्रदान नहीं करती है।
किसीके पुत्रका मरण हो जाता है, किसीकी भार्याका मरण हो जाता है और किसीके घर एवं कुटुम्ब जलकर भस्म हो जाते हैं। इसप्रकार मनुष्यगतिमें अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करता हुआ यह जीव धर्माचरणबुद्धिके अभावके कारण कष्ट प्राप्त करता है। मनुष्यगतिकी तो बात ही क्या, देवगति में भी नानाप्रकारके दुःख इस प्राणीको सहन करने पड़ते हैं। इसप्रकार संसारानुप्रेक्षामें, संसारके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंचपरावर्तनोंका वर्णन आया है|
एकत्त्वानुप्रेक्षामें बताया गया है कि जीव अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही नाना प्रकारके कष्टोंको सहन करता है| नानाप्रकारकी पर्याएँ यह जीव घारणकर सांसारिक कष्टोंको भोगता है। रोग, शोक जन्य अनेक प्रकारके कष्टोंको अकेला ही भोगता है। पुण्यार्जनकर अकेला ही स्वर्ग जाता है और पापार्जन द्वारा अकेला ही नरक प्राप्त करता है। अपना दुःख अपनेको ही भोगना पड़ता है, उसका कोई भी हिस्सेदार नहीं है। इसप्रकार एकत्वभावनामें आचार्यने जीवको शरीरसे भिन्न बताया है-
सव्वायरेण जाणह, एवर्क जावं सरीरदो भिण्णं।
अम्हि दु मुणिदे जीवे, होदि असेसं खणे हेय।।
अर्थात सब प्रकारके प्रयत्नकर शरीरसे भिन्न अकेलं जीनको अवगत करना चाहिये। यह जीव समस्त परद्रव्योंसे भिन्न है। अत: स्वयं ही कर्ता और भोक्ता है। इसप्रकार एकत्वानुप्रेक्षामें अकेले जीवको ही कर्ता और भोक्ता होनेके चिन्तनका वर्णन किया है।
अन्यत्वानुप्रेक्षामें शरीरसे आत्माको भिन्न अनुभव करनेका वर्णन किया है। सभी बाह्य पदार्थ आत्मस्वरूपसे भिन्न हैं। आत्मा ज्ञानदर्शन सुखरूप है और यह संसारके समस्त पुद्गलादि पदार्थोंके स्वरूपसे भिन्न है। इसप्रकार अन्यत्वानुप्रेक्षामें आत्माके भिन्न स्वरूपके चिन्तनका कथन आया है।
अशुचित्वानुप्रेक्षामें शरीरको समस्त अपवित्र वस्तुओंका समूह मानकर विरक्त होने का संदेश दिया गया है। शारीर अत्यन्त अपवित्र है। इसके सम्पर्कमें आनेवाले चन्दन, कर्पूर, केसर आदि सुगन्धित पदार्थ भी दुर्गन्धित हो जाते हैं। अतः इसकी अशुचिताका चिन्तन करना अशुचित्वानप्रेक्षा है।
आस्रवानुप्रेक्षामें आस्त्रवके स्वरूप, कारण, भेद एवं उसके महत्वके चिन्तन का वर्णन आया है। मन, वचन, कायका निमित्त प्राप्तकर जीवके प्रदेशोंका चंचल होना योग हैं, इसीको आस्त्रव कहते हैं। बन्धका कारण आस्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके निमित्तसे बन्ध होता है। यह आस्त्रव पुण्य और पापरूप होता है। शुभास्रव पुण्यरूप है और अशुभास्रव पापरूप है। इमी सन्दर्भमें कषायोंके तीव्र और मन्द भेदोंका भी विवेचन आया है। आस्त्रवानुप्रेक्षामें आस्त्रवके स्वरूपका विचार करते हुये उससे अलिप्त रहने का उपदेश है।
संवरानुप्रक्षामें संवरके स्वरूप और कारणोंका विवेचन करते हुए सम्यक्त्व, व्रत, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिगहजय आदिका चिन्तन आवश्यक माना है। इसी सन्दर्भमें आर्त और रौद्र परिणतिके त्यागका भी कथन किया है, जो व्यक्ति इन्द्रियों के विषयोंसे विरक्त होता हआ संवररूप परिणतिको प्राप्त करता है उसीके संवरभावना होती है।
निर्जराभावनाका विवेचन करते हुये बताया है कि जो अहंकार रहित होकर तप करता है, उसीके निर्जरानुप्रेक्षा होती है। ख्याति, लाभ, पूजा और इन्द्रियोंके विषयभोग बन्धके निमित्त है। निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है। आचार्यने प्रारम्भमें ही वैराग्य-भावनाकी उद्दीप्तीका वर्णन करते हुए कहा है-
वारसविहेण तवसा, णियाणरहियस्स णिज्जरा होदि।
वेरम्गभावणादो, णिरहंकारस्स णाणिस्स।।
निदानरहित, अहंकाररहित, ज्ञानीके बारह प्रकारके तपसे तथा वैराग्य भावनासे निर्जरा होती है। समभावसे निर्जराकी वृद्धि होती है। निर्जरा दो प्रकारकी है- सविपाक और अविपाक। कर्म अपनी स्थितिको पूर्णकर, उदयरस देकर खिर जाते हैं उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा सब जीवोंके होती है। और तपके कारण जो कर्म स्थिति पूर्ण हुये बिना ही खिर जाते हैं, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। सविपाक निर्जरा कार्यकारी नहीं है। अविपाक निर्जरा हो कार्यकारी है। अतएव इन्द्रियों ओर कषायोंका निग्रह करके परम वीतरागभावरूप आत्मध्यानमें लीन होना उत्कृष्ट निर्जरा है।
लोकानुप्रेक्षामें लोकके स्वरूप और आकार-प्रकारका विस्तारसे वर्णन है। आकाशद्रव्यका क्षेत्र अनन्त है और उसके बहुमध्य देशमें स्थित लोक है। यह किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। जीवादि द्रव्योका परस्पर एक क्षेत्रावगाह होनेसे यह लोक कहलाता है। वस्तुतः द्रव्योंका समुदाय लोक कहा जाता है। लोक द्रव्य की दृष्टिसे नित्य है, पर परिवर्तनशील पर्यायों की अपेक्षासे परिणामी है। यह पूर्व-पश्चिम दिशामें नीचेके भागमें सात राजु चौड़ा है। वहाँसे अनुक्रमसे घटता हुआ मध्यलोकमें एक राजु रहता है। पुनः ऊपर अनुक्रमसे बढ़ता-बनता ब्रह्म स्वर्ग तक पाँच राजु चौड़ा हो जाता है, पश्चात् घटते-घटते अन्नमें एक राजु रह जाता है। इसप्रकार खड़े किये गये डेढ मृदंगकी तरह लोकका पूर्व-पश्चिम में आकार होता है। उत्तर-दक्षिणमें भी सात राजु विस्तार है। मेरुके नीचे भी सात राजु अधोलोक है। लोकशब्दका अर्थ बतलाते हुए लिखा है-
दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ।
तस्स सिहरम्मि सिद्धा, अंतविहीणा विरायंते।।
जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक कहलाता है। लोकमें जीव, पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ: द्रव्योंका निवास है। इस अनुप्रेक्षामें इन छहों द्रव्योंका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लोकानुप्रेक्षामें द्रव्योंके स्वभाव-गुणको बतलाते हुये, शरीरसे भिन्न आत्माकी अनुभूति करनेका चित्रण किया है। इस भावनामें गुणस्थानोंके स्वरूप और भेदोंका भी कथन आया है तथा सप्त नयोंकी अपेक्षासे जीवादि पदार्थोंका विवेचन भी किया गया है।
बोधिदुर्लभभावनामें आत्मज्ञानकी दुलभतापर प्रकाश डाला गया है। आरम्भमें बतलाया गया है कि संसारमें समस्त पदार्थोंकी प्राप्ति सुलभ है, पर आत्मज्ञानकी प्राप्ति होना अत्यन्त दुष्कर है। सम्यक्त्वके बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिसे मन्द कर्मोदयसे रत्नत्रय भी प्राप्त हो गया हो, वह व्यक्ति यदि तीव्र कषायके अधीन रहे, तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वह दुर्गति का पात्र बनता है। प्रथम तो मनुष्यगतिकी प्राप्ति ही दुर्लभ है और इस पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी सम्यक्त्वका मिलना दुष्कर है। सम्यक्त्व प्राप्त होनेपर भो सम्यक् बोधका मिलना और भी कठिन है। इसप्रकार स्वामिकार्तिकेयने वोधिकी दुर्लभताका कथन करते हुये रत्नत्रयके स्वरूप आदि पर प्रकाश डाला है।
धर्मानुप्रेक्षामें धर्मका यथार्थ स्वरूप अतीन्द्रिय बतलाया है। धर्मका वास्तविक रूप सर्वज्ञता है। सर्वज्ञताके अस्तित्वमें किसीप्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता है। इस घर्मानुप्रेक्षामें कर्मबन्धके चक्रवालका भी विश्लेषण आया है। बताया गया है कि सर्वज्ञदेव सब द्रव्य, क्षण, काल भावोंकी अवस्थाको जानते हैं। सर्वज्ञके ज्ञानमें सब कुछ प्रकाशित होता है। उनके ज्ञानमें जिस प्रकारके पदार्थोकी पर्यायें प्रतिविम्बित होती हैं, उन पर्याय जन्य फल वैसा ही घटित होता है। उसमें कोई किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं कर सकता है। निम्न दोनों गाथाओंसे पर्यायोंकी नियत स्थिति सिद्ध होती है-
जं जस्स जम्मि देसे, जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि।
णादं, जिणेण णियदं, जम्म वा अहव मरणं वा॥
तं तस्स तम्मि देसे, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि।
को सक्कदि वारेदूं, ईदा वा अह जिणिदो वा।।
जो जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जन्म-मरण, दुःख-सुख, रोग-दारिद्र आदि सर्वज्ञदेवके द्वारा जाने गये हैं, वे नियमसे ही उस प्राणोकी उसी देशमें , उसी कालमें और उसो विधानसे प्राप्त होते हैं। इन्द्र, जिनेन्द्र या तीर्थंकरदेव अन्य कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकते। इस प्रकारके निश्चयसे सब द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन द्रव्यों और इनकी समस्त पर्यायोंका जो श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यकदृष्टी है। यह स्मरणीय है कि जीव मिथ्यात्वकर्मके, उपशम, क्षयोपशम या क्षयके बिना तत्त्वार्थको ग्रहण नहीं कर पाता। इसप्रकार धर्मानुप्रेक्षामें व्यवहारधर्म और निश्चयधर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।
१८६ गाथाओं में इस अनुप्रेक्षाका वर्णन आया है। अनशनादि बारह तप भी इसी वर्णनसंदर्भ में समाविष्ट हैं। बारह व्रतोंके निरूपणमें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंका क्रम वही है, जो कुन्दकुन्दके 'चारित्रपाहुड में पाया जाता है। भेद केवल इतना ही है कि अन्तिम शिक्षाव्रत संल्लेखना नहीं, किंतु देशावकाशिक ग्रहण किया गया है। यह गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंकी व्यवस्था तत्त्वार्थसूत्रसे संख्याक्रममें भिन्न है, और श्रावक प्रज्ञाप्राप्तिकी व्यवस्थाके तुल्य है।
इस प्रकार धर्मानुप्रेक्षामें तपों और व्रत्तोंका विस्तारपूर्वक कथन आया है। श्रावकधर्म और मुनिधर्मको संक्षेपमें अवगत करनेके लिए यह ग्रंथ उपयोगी है।
स्वामी कार्तिकेयकी रचना-शक्ति शिवार्य और कुन्दकुन्दके समान है। विषयको सरल और सुबोध बनानेके लिए उपमानोंका प्रयोग पद-पदपर किया गया है। लेखक जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है, उस तथ्यको बड़ी हो द्रुधताके साथ उपस्थित कर देता है। प्रश्नोत्तर-शैलीमें लिखी गयी गाथाएँ तो विशेष रोचक और महत्वपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणार्थ दो गाथाओंकी उपस्थित कर लेखककी रचना-प्रतिभाका परिचय प्रस्तुत किया जाता है-
को ण वसो इत्थिजणे, कस्स ण मयणेण खंडियं माणं।
को इंदिएहिण जियो, को ण कसाएहि संतत्तो।
सो ण वसो इस्थिजणे, सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण।
जो ण य गिण्हदि गंर्थ, अब्भंतर बाहिरं सव्व।
इस लोकमें स्त्रीजनके वशमें कौन नहीं? कामने किसका मान खण्डित नहीं किया? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन सतप्त नहीं हुआ? ग्रन्थकारने इन समस्त प्रश्नोंका उत्तर तर्कपूर्ण और सुबोध शैलीमें अंकित किया है। वह कहता है, जो मनुष्य बाह्य और आनन्तर संमस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो स्त्रीजनके वश में होता है, न कामके अधीन होता है और न मोह और इन्द्रियों के द्वारा हो जोता जा सकता है।
इस ग्रन्थकी अभिव्यंजना बड़ी ही सशक है। ग्रन्थकारने छोटी-सी गाथामें बड़े-बड़े तथ्योंको संजो कर सहजरूपमें अभिव्यक्त किया है। भाषा सरल और परिमार्जित है। शैलीमें अर्थसौष्ठव, स्वच्छता, प्रेषणीयता, सूत्रात्मकता अलंकारात्मकता समवेत है।
श्रुतधराचार्यसे अभिप्राय हमारा उन आचार्यों से है, जिन्होंने सिद्धान्त, साहित्य, कमराहिम, बायाससाहित्यका साथ दिगम्बर आचार्यों के चारित्र और गुणोंका जोबन में निर्वाह करते हुए किया है। यों तो प्रथमानुयोग, करणा नुयोग, चरणानुयोग और ध्यानुयोगका पूर्व परम्पराके भाधारपर प्रन्धरूपमें प्रणयन करनेका कार्य सभी आचार्य करते रहे हैं, पर केवली और श्रुत केवलियोंकी परम्पराको प्राप्त कर जो अंग या पूर्वो के एकदेशशाता आचार्य हुए हैं उनका इतिवृत्त श्रुतधर आचार्यों को परम्पराके अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायगा | अतएव इन आचार्यों में गुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवाल, यति वृषम, उच्चारणाचार्य, आयमंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, गृपिच्छाचार्य और बप्पदेवकी गणना की जा सकती है ।
श्रुतधराचार्य युगसंस्थापक और युगान्तरकारी आचार्य है। इन्होंने प्रतिभाके कोण होनेपर नष्ट होतो हुई श्रुतपरम्पराको मूर्त रूप देनेका कार्य किया है। यदि श्रतधर आचार्य इस प्रकारका प्रयास नहीं करते तो आज जो जिनवाणी अवशिष्ट है, वह दिखलायी नहीं पड़ती। श्रुतधराचार्य दिगम्बर आचार्यों के मूलगुण और उत्तरगुणों से युक्त थे और परम्पराको जीवित रखनेको दृष्टिसे वे ग्रन्थ-प्रणयनमें संलग्न रहते थे 1 श्रुतकी यह परम्परा अर्थश्रुत और द्रव्यश्रुतके रूपमें ई. सन् पूर्वकी शताब्दियोंसे आरम्भ होकर ई. सनकी चतुर्थ पंचम शताब्दी तक चलती रही है ।अतएव श्रुतघर परम्परामें कर्मसिद्धान्त, लोका. नुयोग एवं सूत्र रूपमें ऐसा निबद साहित्य, जिसपर उत्तरकालमें टीकाएँ, विव त्तियाँ एवं भाष्य लिखे गये हैं, का निरूपण समाविष्ट रहेगा।
श्रुतधराचार्यों की परंपरामें आचार्य कार्तिकेय का नाम आता है। कुमार या कार्तिकेयके सम्बन्ध में अभी तक निर्विवाद सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। हरिषेण, श्रीचन्द्र और ब्रम्हनेमिदत्तके कथाकोषोंमें बताया गया है कि कार्तिकेयने कुमारावस्थामें ही मुनि दीक्षा धारण की थी। इनकी बहनका विवाह रोहेड नगरके राजा क्रौञ्चके साथ हुआ था और उन्होंने दारुण उपसर्ग सहन कर स्वर्गलोकको प्राप्त किया। ये अग्निनामक राजाके पुत्र थे।
'तस्वार्थवातिकमें' अनुत्तरोपपाददशांगके वर्णन-प्रसंगमें दारुण उपसर्ग सहन करनेवालोंमें कार्तिकेयका भी नाम आया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि कार्तिकेय नामके कोई उग्र तपस्वी हुए हैं। ग्रंथके अन्तमें जो प्रशस्ति गाथाएँ दी गयी हैं वे निम्न प्रकार है-
जिणवयणभावणठ्ठ, सामिकुमारेण परमसद्धाए।
रइया अणुवेहाओ, चंचलमणरुंभणठ्ठ च।।
वारसअणुवेक्खाओ, भणिया हु जिणागमारगुसारेण।
जो पढइ सुणइ भावइ, सो पावइ सासयं सोक्खं।
तिहयणपहाणसामि, कुमारकालेण तवियतवयरणं।
वसुपुज्जसुयं मल्लि, चरमत्तिय सथुवे णिच्चं।।
यह अनुप्रेक्षानामक ग्रंथ स्वामी कुमारने श्रद्धापूर्वक जिनवचनकी प्रभावना तथा चंचल मनको रोकने के लिए बनाया।
ये बारह अनुप्रेक्षाएँ जिनागमके अनुसार कहा है, जो भव्य जीव इनको पढ़ता, सुनता और भावना करता है, वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। यह भावनारूप कर्तव्य अर्थका उपदेशक है। अतः भव्य जीवोंको इन्हें पढ़ना, सुनना और इनका चितन करना चाहिए।
कुमार-कालमें दीक्षा ग्रहण करनेवाले वासुपूज्याजिन, मल्लिजिन, नेमिनाथजिन, पार्श्वनाथजिन एवं वर्धमान इन पांचों बाल-यातियोंका में सदैव स्तवन करता हूँ।
इन प्रशस्ति-गाथाओंसे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं-
१. वारस अनुप्रेक्षाके रचयिता स्वामी कुमार हैं।
२. ये स्वामी कुमार बालब्रह्मचारी थे। इसी कारण इन्होंने अन्त्य मंगलके रूपमें पांच बाल-यतियोंको नमस्कार किया है।
३. चन्चल मन एवं विषय-वासनाओंके विरोधकेलिए ये अनुप्रेक्षाएँ लिखी गई है।
मथुराके एक अभिलेखमें उच्चनागरके कुमारनन्दिका उल्लेख आया है- क्षुणे उच्चैनगिरस्यायंकुमारनन्दिशिष्यस्य मित्रस्य।
एक अन्य अभिलेखमें भी कुमारनन्दिका नाम प्राप्त होता है।
इन अभिलेखोम कुमारनन्दिका नाम आया है और उन्हें नागर शाखाका आचार्य कहा है। इस शाखाका अस्तित्व ई. सनकी आरंभिक शताब्दीयोमें था और इस शाखाके आचार्योंने सरस्वती-आन्दोलनमें ग्रन्थ-निर्माणका कार्य किया। अतः कुमारनन्दि और स्वामी कुमार यदि एक व्यक्ति हों, तो उनका समय ई. सन् की आरम्भिक शताब्दी माना जा सकता है। पर अभी तक उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इन दोनांका अभिन्नत्व सिद्ध नहीं है।
संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि स्वामी कार्तिकेय प्रतिभाशाली, आगम पारगामी और अपने समयके प्रसिद्ध आचार्य हैं। यो परम्परासे कार्तिकेयकी द्वादश अनुप्रेक्षाएँ मानी जाती हैं। इस ग्रन्थमें कहीं पर भी कातिकेयका नाम नहीं आया है और न ग्रन्थको ही कार्तिकेयानुप्रेक्षा कहा गया है। ग्रन्थके प्रतिज्ञा और समाप्ति वाक्योंमें ग्रन्थका नाम सामान्यत: 'अणुपेहा' या 'अणुपेक्खा' और विशेषतः 'बारस अणुवेक्खा' नाम आया है। भट्टारक शुभचन्द्रने इस ग्रन्थपर विक्रम संवत् १६१३ (ई. सन् १५७६) में संस्कृत टीका लिखी है। इस टीकामें अनेक स्थानोंपर ग्रन्थका नाम कार्तिकेयानुप्रेक्षा दिया है और ग्रन्थकारका नाम कार्तिकेय मुनि प्रकट किया है।
बहुत सम्भव है कि कार्तिकेयशब्द कुमार या स्वामी कुमारका पर्यायवाची यहाँ व्यवहत किया गया हो। यह सत्य है कि शुभचन्द्र भट्टारक के पूर्व अन्य किसी भी पन्धमें बारस-अणुवेक्खाके रचयिताका नाम कार्तिकेय नहीं आया है। शुभचन्द्रने ३९४ संख्यक गाथाकी टीकामें कार्तिकेय मुनिका उदाहरण प्रस्तुत किया है। लिखा है- "स्वामीकार्तिकेयमुनिः क्रौञ्चराजकृतोपसर्ग सोढ्वा साम्य परिणामेन समाधिमरणेम देवलोकं प्राप्त।" स्पष्ट है कि स्वामी कातिकेय मुनि क्रौञ्चराजकृत उपसर्गको समभावसे सहकर समाधिपूर्वक मरणके द्वारा देव लोकको प्राप्त हुए।
भगवती आराधनाकी गाथा-संख्या १५४९ में क्रौञ्च द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए एक व्यक्तिका निर्देश आया है। साथमें उपसर्गस्थान रोहेडक और शक्ति हथियारका भी उल्लेख है। पर कार्तिकेय नामका स्पष्ट निर्देश नहीं है। उस व्यक्तिको अग्निदयितः' लिखा है, जिसका अर्थ अग्निप्रिय है। मूलाराधनादर्पणमें लिखा है- "रोहेडयम्मि रोहेटकनाम्नि नगरे। सत्तोए शक्त्या शस्त्रविशेषेण क्रौञ्चनाम्ना राज्ञा। अग्गिदइदो अग्निराजनाम्नो राज्ञः पुत्रः कार्तिकेय संज्ञः।" अर्थात् रोहेडनगरमें क्रौञ्च राजाने अग्निराजाके पुत्र कार्तिकेय मुनिको शक्तिनामक शस्त्रसे मारा था और मुनिराजने उस दुःखको समत्तापूर्वक सहनकर रनत्रयकी प्राप्ति की थी। इस टीकासे प्रकट होता है कि कार्तिकेयने कुमारावस्थामें मुनिदीक्षा ली थी। बताया गया है कि कार्तिकेयकी बहन रोहेड नगरके क्रौञ्च राजाके साथ विवाहित थी। राजा किसी कारणवश कार्तिकेयसे असन्तुष्ट हो गया और उसने कार्तिकेय को दारुण उपसर्ग दिये। इन उपसर्गोको समत्तासे सहनकर कार्तिकेयने देवलोक प्राप्त किया। इस कथाके आधारपर इतना तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थके रचयिता कार्तिकेय सम्भव है और ग्रंथका नाम भी कार्तिकेयानुप्रेक्षा कल्पित नहीं है।
मूलाचार, भगवती-आराधना और कुन्दकुन्दकृत 'बारह अणुवेक्खा' में बारह भावनाओंका क्रम और उनकी प्रतिपादक गाथाएँ एक ही हैं। यहाँतक कि उनके नाम भी एक हो हैं। किन्तु कार्तिकेयको 'बारहअणुवेक्खा’ में न वह क्रम है और न वे नाम हैं। इसमें क्रम और नाम तत्वार्थसूत्रकी तरह हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्त्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, चोधिदुर्लभ और धर्म इस क्रम तथा नामोसे १२ भावनाएँ आयी हैं। ठीक यही क्रम और नाम कार्तिकेयको 'अणुवेक्खामें’ हैं। अतएव इस भिन्नतासे कार्तिकेय न केवल वट्टकेर, शिवार्य और कुन्दकुन्दके उत्तरवर्ती प्रतीत हाते हैं, अपितु तत्वार्थसूत्रकारके भी उत्तरवर्ती जान पड़ते हैं।
परन्तु यहीं कहा जा सकता है कि तत्त्वार्थसूत्रकारके समक्ष भी कोई क्रम रहा है, तभी उन्होंने अपने ग्रन्थमें उस क्रमको निबद्ध किया है। साथ ही यह भी सम्भावना है कि भावनाओंके दोनों ही क्रम प्रचलित रहे हों, एक क्रमको कुन्दकुन्द, शिवार्य, वट्टकेर आदिने अपनाया और दूसरे क्रमको स्वामी कार्तिकेय, गृद्धपिच्छ आदिने। अतः भावनाक्रमके अपनानेके आधारपर कार्तिकेयके समयका निर्धारण नहीं किया जा सकता और न उनके 'बारह अणुवेक्वा' ग्रंथकी अर्वाचीनता ही सिद्ध की जा सकती है।
स्वामि कात्तिकेयके समयका विचार करते हुए डॉ. ए. एन. उपाध्येने 'बारस-अणुवेक्खा'का अन्तःपरीक्षणकर बतलाया है कि इस ग्रन्थकी २७९ वीं गाथामें 'णिसुणहि' और 'भावहि' ये दो पद अपभ्रंशके आ घुसे हैं, जो वर्तमान काल तृतीय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं। यह गाथा 'जोइन्दु'के योगसारके ६५ वे दोहेके साथ मिलती-जुलती है और दोहा तथा गाथा दोनोंका भाव भी एक है। अतएव इस गाथाको 'जोइन्दु के दोहेका परिवर्तित रूप माना जा सकता है। यथा-
विरला जाणहि तत्तु बहु विरला णिसुणहि तत्तु।
विरला झायहिं तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु॥
विरला णिसुणहि तच्चं विरला जाणंति तच्चदो तच्चं।
विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणा होदि।।
अतः इन दोनों संधार्भोन्के तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर कार्तिकेयका समय जोइन्दुके पश्चात् होना चाहिए।
श्री जुगलकिशोर मुख्तारने डॉ. उपाध्येके इस अभिमतका परोक्षण करते हुए लिखा है कि "यह गाथा कार्तिकेय द्वारा लिखित नहीं है। जिस लोक भावनाके प्रकरणमें यह आयी है, वहाँ इसकी संगति नहीं बैठती।" आचार्य मुख्तारने अपने कथनको पुष्टिके लिए गाथाओंका क्रम भी उपस्थित किया है। उन्होंने लिखा है- "स्वामीकुमारने ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके बनाया है, समुचित प्रतीत नहीं होता- खासकर उस हालतमें जबकि ग्रन्थ भरमें अपभ्रंष भाषाका और कोई प्रयोग भी न पाया जाता हो। बहुत सम्भव है कि किसी दूसरे विद्वानने दोहेको गाथाका रूप देकर उसे अपनी ग्रंथ-प्रतिमें नोट किया हो, और यह भी सम्भब है कि यह गाथा साधारणसे पाठभेदके साथ अधिक प्राचीन हो, और योगेन्दुने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवर्तनके साथ अपना उक्त दोहा बनाया हो; क्योंकि योगेन्दुके परमार्थप्रकाश आदि ग्रन्थोंमें और भी कितने ही दोहे ऐसे पाये जाते हैं, जो भावपाहुड तथा समाधितंत्रादिके पद्योंपरसे परिवर्तन करके बनाये गये हैं और जिसे डॉ. साहबने स्वयं स्वीकार किया है। जब कि स्वामीकुमारके इस ग्रन्थकी ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आयी। "
आचार्य मुख्तार साहबका यह निष्कर्ष उचित्त मालूम होता है, क्योंकि योगसारका विषय क्रमबद्ध रूपसे नहीं है। इसमें कुन्दकुन्दकी अनेक गाथाओंका रूपान्तरण मिलता है। कुन्दकुन्दने कर्मविमुक्त आत्माको परमात्मा बतलाते हुए; उसे ज्ञानी, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णू, चतुर्मुख और बुद्ध कहा है। योगसारमें भी उसके जिन, बुद्ध, विष्णु, शिव आदि नाम बतलाये है। इसके अतिरिक्त जो इन्दुने कुन्दकुन्दके समान हो निश्चय और व्यवहार नयों द्वारा आत्माका कथन किया है। योगसार और परमार्थप्रकाश इन दोनोंका विषय समान होने पर भी योगसार संग्रहग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। इसमें कई तथ्य छूट भी गये हैं। दोहा ९९-१०३ द्वारा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसाम्पराय संयमका स्वरूप बतलाया है। यहाँ यथाख्यात चारित्रका स्वरूप छूट गया है। अतएव योगसारके दोहेका परिवर्तीत रूप कार्तिकेयानुप्रेक्षामें होनेके आधारपर कातिकेयको अर्वाचीन बताना युक्त नहीं है।
आचार्य जुगलकिशोर मुख्तारने समय-निर्णय करते हुये लिखा है- "मेरी समझमें यह ग्रंथ उमास्वातिके तत्वार्थ सूत्रसे अधिक बादका नहीं, उसके निकटवर्ती किसी समयका होना चाहिये, और उसके कर्ता वे अग्निपुत्र कार्तिकेय मुनि नहीं हैं, जो साधारणत: इसके कर्ता समझे जाते हैं, और क्राँच राजाके द्वारा उपसर्गको प्राप्त हए थे, बल्कि स्वामीकुमार नामके आचार्य ही है, जिस नामका उल्लेख उन्होंने स्वयं 'अन्त्यमंगल'की गाथामें श्लेष रूपसे किया है।
आचार्य जुगलकिशोर मुख्तारके उक्त मतसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्तिकेय गृद्धपिच्छके समकालीन अथवा कुछ उत्तरकालोन हैं। अर्थात् वि. सं. को दूसरी-तीसरी शती उनका समय होना चाहिए।
द्वादशानुप्रेक्षामें कुल ४८९ गाथाएँ हैं। इनमें अघ्र व, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, अस्त्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधदुर्लभ और धर्म इन बारह अनुषेक्षाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। प्रसंगवश जीव, अजीव, अस्त्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वोंका स्वरूप भी वर्णीत है। जीवसमास तथा मार्गणाके निरूपणके साथ, द्वादगवत, पात्रोंके भेद, दाताके सात गुण, दानकी श्रेष्ठता, माहात्म्य, सल्लेखना, दश धर्म, सम्यक्त्वके आठ अंग, बारह प्रकारके तप एवं ध्यानके भेद-प्रभेदोंका निरूपण किया गया है। आचार्यका स्वरूप एवं आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया इस ग्रन्थमें विस्तारपूर्वक वर्णीत है।
अघ्रुवानुप्रेक्षामें ४-२२ गाथाएँ हैं। अशरणानुप्रेक्षाम २३-३१; संसारानुप्रेक्षामें ३२-७३; एकात्वानुप्रेक्षामें ७४-७९; अन्यत्वानुप्रेक्षामें ८०-८२: अशु चित्वानुप्रेक्षामें ८३-८७; आस्त्रवानुप्रेक्षामें ८८-१४; संवरानुप्रेक्षामें ९५-१०१, निर्जरानुप्रेक्षामें १०२-११४, लोकानुप्रेक्षामें ११५-२८३; बोधिदुर्लभानुप्रक्षामें २८४-३०१ एवं धर्मानुप्रंक्षामें ३०२-४३५ गाथाएँ हैं। ४३६ गाथासे अन्ततक द्वादश तपोंका वर्णन आया है। अघ्रुवानुप्रेक्षामें समस्त वस्तुओंकी अनित्यता बतलाते हुए वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक कहा है। सामान्य द्रव्यरूप है, और विशेष गुण पर्यायरूप। द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है किन्तु पर्यायकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य हैं। यह संसारका प्राणी पर्यायबुद्धि है, जिससे पर्यायोंको उत्पन्न और नष्ट होते देखकर हर्ष-विषाद करता है, और उसको नित्य रखना चाहता है। यह शरीर जीव-पुद्गलको संयोग जनित पर्याय है धन-धान्यादिक पुद्गल परणुओंकी स्कन्ध पर्याय है। इनके संयोग और वियोग नियमसे अवश्य है, जो स्थिरताकी बुद्धि करता है, वह मोहजनित भावके कारण संक्लेश प्राप्त करता है।
संसारकी समस्त अवस्थाएँ विरोधी भावोंसे युक्त हैं। जब जन्म होता है, तब उसे स्थिर समझकर हर्ष उत्पन्न होता है, मरण होनेपर नाश मानकर शोक करता है। इस प्रकार इष्टकी प्राप्तिमें हर्ष, अप्राप्तीमें विषाद तथा अनिष्ट प्राप्तिमें विषाद, अप्राप्तीमें हर्ष करता है, यह भी सब मोहका माहात्म्य है। आचार्य सादृश्यमूलक उपमा प्रस्तुतकर परिवार, वन्धुवर्ग, स्त्री, पुत्र, मित्र, धनधान्यादिकी अनित्यताका चित्रण करते हुए कहते है-
अथिरं परियण-सवर्ण, पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावण्णं।
गिह-गोहणाइ सव्वं, णव-घण-विदेण सारित्थ।।
परिवार, बन्धुवर्ग, पुत्र, स्त्री, मित्र, सौन्दर्य, गृह, धन, पशु सम्पत्ति इत्यादि सभी वस्तुएँ नवीन मेध-समूहके ममान अस्थिर हैं। इन्द्रियोंके विषय, भृत्य, अश्व, गज, रथ आदि सभी पदार्थ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं।
पुण्यके उदयसे प्राप्त होने वाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी भी नित्य नहीं हैं, तब वह पुण्यहीन अथवा अल्पपुण्यवाले व्यक्तियोंसे केसे प्रेम करेगी? कविने इसी को समझाते हुए लिखा है-
कत्थ वि ण रमइ लच्छी, कुलीण-धीरे वि पंडिए सूरे।
पुज्जे धम्मिट्ठे वि य, सरूव-सुयणे महासत्ते।
अर्थात् यह लक्ष्मी कुलवान, धैर्यवान, पंडित, सुघट, पूज्य, धर्मात्मा, रूपवान, सुजन, महापराक्रमी इत्यादि किसी भी पुरुषसे प्रेम नहीं करती, यह जल की तरंगोंके समान चंचल है। इसका निवास एक स्थानपर अधिक समय तक नहीं रहता। इस प्रकार आचार्य स्वामिकुमारने संसार, शरीर, भोग और लक्ष्मीकी अस्थिरताके चिन्तनको अघ्रुवानुप्रेक्षा कहा है।
अशरण भावनामें बताया है कि मरण करते समय कोई भी प्राणीकी शरण नहीं। जिस प्रकार वनमें सिंह मृगके बच्चेको जब पैरके नीचे दबा लेता है, तब कोई भो उसकी रक्षा नहीं कर सकता , देव , तप आदि सभी मुत्युसे रक्षा करने में असमर्थ है। रक्षा करनेके लिए जितने उपाय किये जाते हैं, वे सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। आयुके क्षय होनेपर कोई एक क्षणके लिए भी आयुदान नहीं सकता-
आउक्खयेण मरणं आउं दाउं ण सक्कदे को वि।
तम्हा देविदो वि य, मरगाउ ण सक्खदे को वि।
आयुकर्मके क्षयसे मरण होता है और आयुकर्मको कोई देनेमें समर्थ नहीं, अतएव देवेन्द्र भी मृत्युसे किसीकी रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार अशरण रूप चिन्तनका समावेश अशरण-भावनामें होता है।
संसार-अनुप्रेक्षामें बताया है कि संसार-परिभ्रमणका कारण मिथ्यात्व और कषाय है। इन दोनोंके निमित्तसे ही जीव चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता है। हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रहरूप भावनाके कारण विभिन्न गत्तियोंमें इस जीवको परिभ्रमण करना पड़ता है| आचार्यने इस भावनामें चतुरंगतिके दुःखोंका वर्णन भी संक्षेपमें किया है। मनुष्यगतिके हाखोंका प्रतिपादन करते हुए संसार स्वभावका विश्लेषण विश्लेषण किया है-
कस्स वि दुटुकलितं, कस्स वि दुव्वसणवसणिओ पुत्तो।
कस्स वि अरिसमबंधू, कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ।।
मरदि सुपुत्तो कस्स वि, कस्स वि महिला विणस्सदे इट्ठा।
कस्स वि अग्गीपलितं, गिहं कुडंबं च डज्झेई।।
संसारमें सुख नहीं है। इस मनुष्यगतिमें नानाप्रकारके दुःख हैं। किसीकी स्त्री दुराचारिणी है, किसीका पुत्र व्यसनी है, किसीका भाई शत्रुके समान कलहकारी है। एवं किसीकी पुत्री दुश्चरित्रा है। इस प्रकार संसारकी विषम परिस्थिति मनुष्यको सुखका कण भी प्रदान नहीं करती है।
किसीके पुत्रका मरण हो जाता है, किसीकी भार्याका मरण हो जाता है और किसीके घर एवं कुटुम्ब जलकर भस्म हो जाते हैं। इसप्रकार मनुष्यगतिमें अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करता हुआ यह जीव धर्माचरणबुद्धिके अभावके कारण कष्ट प्राप्त करता है। मनुष्यगतिकी तो बात ही क्या, देवगति में भी नानाप्रकारके दुःख इस प्राणीको सहन करने पड़ते हैं। इसप्रकार संसारानुप्रेक्षामें, संसारके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंचपरावर्तनोंका वर्णन आया है|
एकत्त्वानुप्रेक्षामें बताया गया है कि जीव अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही नाना प्रकारके कष्टोंको सहन करता है| नानाप्रकारकी पर्याएँ यह जीव घारणकर सांसारिक कष्टोंको भोगता है। रोग, शोक जन्य अनेक प्रकारके कष्टोंको अकेला ही भोगता है। पुण्यार्जनकर अकेला ही स्वर्ग जाता है और पापार्जन द्वारा अकेला ही नरक प्राप्त करता है। अपना दुःख अपनेको ही भोगना पड़ता है, उसका कोई भी हिस्सेदार नहीं है। इसप्रकार एकत्वभावनामें आचार्यने जीवको शरीरसे भिन्न बताया है-
सव्वायरेण जाणह, एवर्क जावं सरीरदो भिण्णं।
अम्हि दु मुणिदे जीवे, होदि असेसं खणे हेय।।
अर्थात सब प्रकारके प्रयत्नकर शरीरसे भिन्न अकेलं जीनको अवगत करना चाहिये। यह जीव समस्त परद्रव्योंसे भिन्न है। अत: स्वयं ही कर्ता और भोक्ता है। इसप्रकार एकत्वानुप्रेक्षामें अकेले जीवको ही कर्ता और भोक्ता होनेके चिन्तनका वर्णन किया है।
अन्यत्वानुप्रेक्षामें शरीरसे आत्माको भिन्न अनुभव करनेका वर्णन किया है। सभी बाह्य पदार्थ आत्मस्वरूपसे भिन्न हैं। आत्मा ज्ञानदर्शन सुखरूप है और यह संसारके समस्त पुद्गलादि पदार्थोंके स्वरूपसे भिन्न है। इसप्रकार अन्यत्वानुप्रेक्षामें आत्माके भिन्न स्वरूपके चिन्तनका कथन आया है।
अशुचित्वानुप्रेक्षामें शरीरको समस्त अपवित्र वस्तुओंका समूह मानकर विरक्त होने का संदेश दिया गया है। शारीर अत्यन्त अपवित्र है। इसके सम्पर्कमें आनेवाले चन्दन, कर्पूर, केसर आदि सुगन्धित पदार्थ भी दुर्गन्धित हो जाते हैं। अतः इसकी अशुचिताका चिन्तन करना अशुचित्वानप्रेक्षा है।
आस्रवानुप्रेक्षामें आस्त्रवके स्वरूप, कारण, भेद एवं उसके महत्वके चिन्तन का वर्णन आया है। मन, वचन, कायका निमित्त प्राप्तकर जीवके प्रदेशोंका चंचल होना योग हैं, इसीको आस्त्रव कहते हैं। बन्धका कारण आस्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके निमित्तसे बन्ध होता है। यह आस्त्रव पुण्य और पापरूप होता है। शुभास्रव पुण्यरूप है और अशुभास्रव पापरूप है। इमी सन्दर्भमें कषायोंके तीव्र और मन्द भेदोंका भी विवेचन आया है। आस्त्रवानुप्रेक्षामें आस्त्रवके स्वरूपका विचार करते हुये उससे अलिप्त रहने का उपदेश है।
संवरानुप्रक्षामें संवरके स्वरूप और कारणोंका विवेचन करते हुए सम्यक्त्व, व्रत, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिगहजय आदिका चिन्तन आवश्यक माना है। इसी सन्दर्भमें आर्त और रौद्र परिणतिके त्यागका भी कथन किया है, जो व्यक्ति इन्द्रियों के विषयोंसे विरक्त होता हआ संवररूप परिणतिको प्राप्त करता है उसीके संवरभावना होती है।
निर्जराभावनाका विवेचन करते हुये बताया है कि जो अहंकार रहित होकर तप करता है, उसीके निर्जरानुप्रेक्षा होती है। ख्याति, लाभ, पूजा और इन्द्रियोंके विषयभोग बन्धके निमित्त है। निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है। आचार्यने प्रारम्भमें ही वैराग्य-भावनाकी उद्दीप्तीका वर्णन करते हुए कहा है-
वारसविहेण तवसा, णियाणरहियस्स णिज्जरा होदि।
वेरम्गभावणादो, णिरहंकारस्स णाणिस्स।।
निदानरहित, अहंकाररहित, ज्ञानीके बारह प्रकारके तपसे तथा वैराग्य भावनासे निर्जरा होती है। समभावसे निर्जराकी वृद्धि होती है। निर्जरा दो प्रकारकी है- सविपाक और अविपाक। कर्म अपनी स्थितिको पूर्णकर, उदयरस देकर खिर जाते हैं उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा सब जीवोंके होती है। और तपके कारण जो कर्म स्थिति पूर्ण हुये बिना ही खिर जाते हैं, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। सविपाक निर्जरा कार्यकारी नहीं है। अविपाक निर्जरा हो कार्यकारी है। अतएव इन्द्रियों ओर कषायोंका निग्रह करके परम वीतरागभावरूप आत्मध्यानमें लीन होना उत्कृष्ट निर्जरा है।
लोकानुप्रेक्षामें लोकके स्वरूप और आकार-प्रकारका विस्तारसे वर्णन है। आकाशद्रव्यका क्षेत्र अनन्त है और उसके बहुमध्य देशमें स्थित लोक है। यह किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। जीवादि द्रव्योका परस्पर एक क्षेत्रावगाह होनेसे यह लोक कहलाता है। वस्तुतः द्रव्योंका समुदाय लोक कहा जाता है। लोक द्रव्य की दृष्टिसे नित्य है, पर परिवर्तनशील पर्यायों की अपेक्षासे परिणामी है। यह पूर्व-पश्चिम दिशामें नीचेके भागमें सात राजु चौड़ा है। वहाँसे अनुक्रमसे घटता हुआ मध्यलोकमें एक राजु रहता है। पुनः ऊपर अनुक्रमसे बढ़ता-बनता ब्रह्म स्वर्ग तक पाँच राजु चौड़ा हो जाता है, पश्चात् घटते-घटते अन्नमें एक राजु रह जाता है। इसप्रकार खड़े किये गये डेढ मृदंगकी तरह लोकका पूर्व-पश्चिम में आकार होता है। उत्तर-दक्षिणमें भी सात राजु विस्तार है। मेरुके नीचे भी सात राजु अधोलोक है। लोकशब्दका अर्थ बतलाते हुए लिखा है-
दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ।
तस्स सिहरम्मि सिद्धा, अंतविहीणा विरायंते।।
जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक कहलाता है। लोकमें जीव, पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ: द्रव्योंका निवास है। इस अनुप्रेक्षामें इन छहों द्रव्योंका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लोकानुप्रेक्षामें द्रव्योंके स्वभाव-गुणको बतलाते हुये, शरीरसे भिन्न आत्माकी अनुभूति करनेका चित्रण किया है। इस भावनामें गुणस्थानोंके स्वरूप और भेदोंका भी कथन आया है तथा सप्त नयोंकी अपेक्षासे जीवादि पदार्थोंका विवेचन भी किया गया है।
बोधिदुर्लभभावनामें आत्मज्ञानकी दुलभतापर प्रकाश डाला गया है। आरम्भमें बतलाया गया है कि संसारमें समस्त पदार्थोंकी प्राप्ति सुलभ है, पर आत्मज्ञानकी प्राप्ति होना अत्यन्त दुष्कर है। सम्यक्त्वके बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिसे मन्द कर्मोदयसे रत्नत्रय भी प्राप्त हो गया हो, वह व्यक्ति यदि तीव्र कषायके अधीन रहे, तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वह दुर्गति का पात्र बनता है। प्रथम तो मनुष्यगतिकी प्राप्ति ही दुर्लभ है और इस पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी सम्यक्त्वका मिलना दुष्कर है। सम्यक्त्व प्राप्त होनेपर भो सम्यक् बोधका मिलना और भी कठिन है। इसप्रकार स्वामिकार्तिकेयने वोधिकी दुर्लभताका कथन करते हुये रत्नत्रयके स्वरूप आदि पर प्रकाश डाला है।
धर्मानुप्रेक्षामें धर्मका यथार्थ स्वरूप अतीन्द्रिय बतलाया है। धर्मका वास्तविक रूप सर्वज्ञता है। सर्वज्ञताके अस्तित्वमें किसीप्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता है। इस घर्मानुप्रेक्षामें कर्मबन्धके चक्रवालका भी विश्लेषण आया है। बताया गया है कि सर्वज्ञदेव सब द्रव्य, क्षण, काल भावोंकी अवस्थाको जानते हैं। सर्वज्ञके ज्ञानमें सब कुछ प्रकाशित होता है। उनके ज्ञानमें जिस प्रकारके पदार्थोकी पर्यायें प्रतिविम्बित होती हैं, उन पर्याय जन्य फल वैसा ही घटित होता है। उसमें कोई किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं कर सकता है। निम्न दोनों गाथाओंसे पर्यायोंकी नियत स्थिति सिद्ध होती है-
जं जस्स जम्मि देसे, जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि।
णादं, जिणेण णियदं, जम्म वा अहव मरणं वा॥
तं तस्स तम्मि देसे, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि।
को सक्कदि वारेदूं, ईदा वा अह जिणिदो वा।।
जो जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जन्म-मरण, दुःख-सुख, रोग-दारिद्र आदि सर्वज्ञदेवके द्वारा जाने गये हैं, वे नियमसे ही उस प्राणोकी उसी देशमें , उसी कालमें और उसो विधानसे प्राप्त होते हैं। इन्द्र, जिनेन्द्र या तीर्थंकरदेव अन्य कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकते। इस प्रकारके निश्चयसे सब द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन द्रव्यों और इनकी समस्त पर्यायोंका जो श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यकदृष्टी है। यह स्मरणीय है कि जीव मिथ्यात्वकर्मके, उपशम, क्षयोपशम या क्षयके बिना तत्त्वार्थको ग्रहण नहीं कर पाता। इसप्रकार धर्मानुप्रेक्षामें व्यवहारधर्म और निश्चयधर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।
१८६ गाथाओं में इस अनुप्रेक्षाका वर्णन आया है। अनशनादि बारह तप भी इसी वर्णनसंदर्भ में समाविष्ट हैं। बारह व्रतोंके निरूपणमें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंका क्रम वही है, जो कुन्दकुन्दके 'चारित्रपाहुड में पाया जाता है। भेद केवल इतना ही है कि अन्तिम शिक्षाव्रत संल्लेखना नहीं, किंतु देशावकाशिक ग्रहण किया गया है। यह गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंकी व्यवस्था तत्त्वार्थसूत्रसे संख्याक्रममें भिन्न है, और श्रावक प्रज्ञाप्राप्तिकी व्यवस्थाके तुल्य है।
इस प्रकार धर्मानुप्रेक्षामें तपों और व्रत्तोंका विस्तारपूर्वक कथन आया है। श्रावकधर्म और मुनिधर्मको संक्षेपमें अवगत करनेके लिए यह ग्रंथ उपयोगी है।
स्वामी कार्तिकेयकी रचना-शक्ति शिवार्य और कुन्दकुन्दके समान है। विषयको सरल और सुबोध बनानेके लिए उपमानोंका प्रयोग पद-पदपर किया गया है। लेखक जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है, उस तथ्यको बड़ी हो द्रुधताके साथ उपस्थित कर देता है। प्रश्नोत्तर-शैलीमें लिखी गयी गाथाएँ तो विशेष रोचक और महत्वपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणार्थ दो गाथाओंकी उपस्थित कर लेखककी रचना-प्रतिभाका परिचय प्रस्तुत किया जाता है-
को ण वसो इत्थिजणे, कस्स ण मयणेण खंडियं माणं।
को इंदिएहिण जियो, को ण कसाएहि संतत्तो।
सो ण वसो इस्थिजणे, सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण।
जो ण य गिण्हदि गंर्थ, अब्भंतर बाहिरं सव्व।
इस लोकमें स्त्रीजनके वशमें कौन नहीं? कामने किसका मान खण्डित नहीं किया? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन सतप्त नहीं हुआ? ग्रन्थकारने इन समस्त प्रश्नोंका उत्तर तर्कपूर्ण और सुबोध शैलीमें अंकित किया है। वह कहता है, जो मनुष्य बाह्य और आनन्तर संमस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो स्त्रीजनके वश में होता है, न कामके अधीन होता है और न मोह और इन्द्रियों के द्वारा हो जोता जा सकता है।
इस ग्रन्थकी अभिव्यंजना बड़ी ही सशक है। ग्रन्थकारने छोटी-सी गाथामें बड़े-बड़े तथ्योंको संजो कर सहजरूपमें अभिव्यक्त किया है। भाषा सरल और परिमार्जित है। शैलीमें अर्थसौष्ठव, स्वच्छता, प्रेषणीयता, सूत्रात्मकता अलंकारात्मकता समवेत है।
श्रुतधराचार्यसे अभिप्राय हमारा उन आचार्यों से है, जिन्होंने सिद्धान्त, साहित्य, कमराहिम, बायाससाहित्यका साथ दिगम्बर आचार्यों के चारित्र और गुणोंका जोबन में निर्वाह करते हुए किया है। यों तो प्रथमानुयोग, करणा नुयोग, चरणानुयोग और ध्यानुयोगका पूर्व परम्पराके भाधारपर प्रन्धरूपमें प्रणयन करनेका कार्य सभी आचार्य करते रहे हैं, पर केवली और श्रुत केवलियोंकी परम्पराको प्राप्त कर जो अंग या पूर्वो के एकदेशशाता आचार्य हुए हैं उनका इतिवृत्त श्रुतधर आचार्यों को परम्पराके अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायगा | अतएव इन आचार्यों में गुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवाल, यति वृषम, उच्चारणाचार्य, आयमंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, गृपिच्छाचार्य और बप्पदेवकी गणना की जा सकती है ।
श्रुतधराचार्य युगसंस्थापक और युगान्तरकारी आचार्य है। इन्होंने प्रतिभाके कोण होनेपर नष्ट होतो हुई श्रुतपरम्पराको मूर्त रूप देनेका कार्य किया है। यदि श्रतधर आचार्य इस प्रकारका प्रयास नहीं करते तो आज जो जिनवाणी अवशिष्ट है, वह दिखलायी नहीं पड़ती। श्रुतधराचार्य दिगम्बर आचार्यों के मूलगुण और उत्तरगुणों से युक्त थे और परम्पराको जीवित रखनेको दृष्टिसे वे ग्रन्थ-प्रणयनमें संलग्न रहते थे 1 श्रुतकी यह परम्परा अर्थश्रुत और द्रव्यश्रुतके रूपमें ई. सन् पूर्वकी शताब्दियोंसे आरम्भ होकर ई. सनकी चतुर्थ पंचम शताब्दी तक चलती रही है ।अतएव श्रुतघर परम्परामें कर्मसिद्धान्त, लोका. नुयोग एवं सूत्र रूपमें ऐसा निबद साहित्य, जिसपर उत्तरकालमें टीकाएँ, विव त्तियाँ एवं भाष्य लिखे गये हैं, का निरूपण समाविष्ट रहेगा।
डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।
#kartikeymaharaj
डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।
आचार्य श्री कार्तिकेय महाराजजी
| Name | Phone/Mobile 1 | Which Sangh/Maharaji/Aryika Ji you are associated with |
|---|---|---|
| Sangh Common Number | +919844033717 | #VardhamanSagarJiMaharaj1950DharmSagarJi |
| Hemal Jain | +918690943133 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi |
| Abhi Bantu | +919575455473 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi |
| Purnima Didi | +918552998307 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi |
| Varna Manish Bhai | +919352199164 | #KanaknandiJiMaharajKunthusagarji |
| Ankit Test | +919730016352 | #AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj |
| Santosh Khule | +919850774639 | #PavitrasagarJiMaharaj1949SanmatiSagarJi1927 |
| Madhok Shaha | +919928058345 | #KanaknandiJiMaharajKunthusagarji |
| Siddharth jain Baddu | +917987281995 | #AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj, #VishalSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi |
| Akshay Adadande | +919765069127 | #AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj, #NiyamSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi |
| Mayur Jain | +918484845108 | #SundarSagarJiMaharaj1976SanmatiSagarJi, #VibhavSagarJiMaharaj1976ViragSagarJi, #PrabhavsagarjiPavitrasagarJiMaharaj1949, #MayanksagarjiRayansagarJiMaharaj1955 |
Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara_2.
श्रुतधराचार्यों की परंपरामें आचार्य कार्तिकेय का नाम आता है। कुमार या कार्तिकेयके सम्बन्ध में अभी तक निर्विवाद सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। हरिषेण, श्रीचन्द्र और ब्रम्हनेमिदत्तके कथाकोषोंमें बताया गया है कि कार्तिकेयने कुमारावस्थामें ही मुनि दीक्षा धारण की थी। इनकी बहनका विवाह रोहेड नगरके राजा क्रौञ्चके साथ हुआ था और उन्होंने दारुण उपसर्ग सहन कर स्वर्गलोकको प्राप्त किया। ये अग्निनामक राजाके पुत्र थे।
'तस्वार्थवातिकमें' अनुत्तरोपपाददशांगके वर्णन-प्रसंगमें दारुण उपसर्ग सहन करनेवालोंमें कार्तिकेयका भी नाम आया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि कार्तिकेय नामके कोई उग्र तपस्वी हुए हैं। ग्रंथके अन्तमें जो प्रशस्ति गाथाएँ दी गयी हैं वे निम्न प्रकार है-
जिणवयणभावणठ्ठ, सामिकुमारेण परमसद्धाए।
रइया अणुवेहाओ, चंचलमणरुंभणठ्ठ च।।
वारसअणुवेक्खाओ, भणिया हु जिणागमारगुसारेण।
जो पढइ सुणइ भावइ, सो पावइ सासयं सोक्खं।
तिहयणपहाणसामि, कुमारकालेण तवियतवयरणं।
वसुपुज्जसुयं मल्लि, चरमत्तिय सथुवे णिच्चं।।
यह अनुप्रेक्षानामक ग्रंथ स्वामी कुमारने श्रद्धापूर्वक जिनवचनकी प्रभावना तथा चंचल मनको रोकने के लिए बनाया।
ये बारह अनुप्रेक्षाएँ जिनागमके अनुसार कहा है, जो भव्य जीव इनको पढ़ता, सुनता और भावना करता है, वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। यह भावनारूप कर्तव्य अर्थका उपदेशक है। अतः भव्य जीवोंको इन्हें पढ़ना, सुनना और इनका चितन करना चाहिए।
कुमार-कालमें दीक्षा ग्रहण करनेवाले वासुपूज्याजिन, मल्लिजिन, नेमिनाथजिन, पार्श्वनाथजिन एवं वर्धमान इन पांचों बाल-यातियोंका में सदैव स्तवन करता हूँ।
इन प्रशस्ति-गाथाओंसे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं-
१. वारस अनुप्रेक्षाके रचयिता स्वामी कुमार हैं।
२. ये स्वामी कुमार बालब्रह्मचारी थे। इसी कारण इन्होंने अन्त्य मंगलके रूपमें पांच बाल-यतियोंको नमस्कार किया है।
३. चन्चल मन एवं विषय-वासनाओंके विरोधकेलिए ये अनुप्रेक्षाएँ लिखी गई है।
मथुराके एक अभिलेखमें उच्चनागरके कुमारनन्दिका उल्लेख आया है- क्षुणे उच्चैनगिरस्यायंकुमारनन्दिशिष्यस्य मित्रस्य।
एक अन्य अभिलेखमें भी कुमारनन्दिका नाम प्राप्त होता है।
इन अभिलेखोम कुमारनन्दिका नाम आया है और उन्हें नागर शाखाका आचार्य कहा है। इस शाखाका अस्तित्व ई. सनकी आरंभिक शताब्दीयोमें था और इस शाखाके आचार्योंने सरस्वती-आन्दोलनमें ग्रन्थ-निर्माणका कार्य किया। अतः कुमारनन्दि और स्वामी कुमार यदि एक व्यक्ति हों, तो उनका समय ई. सन् की आरम्भिक शताब्दी माना जा सकता है। पर अभी तक उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इन दोनांका अभिन्नत्व सिद्ध नहीं है।
संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि स्वामी कार्तिकेय प्रतिभाशाली, आगम पारगामी और अपने समयके प्रसिद्ध आचार्य हैं। यो परम्परासे कार्तिकेयकी द्वादश अनुप्रेक्षाएँ मानी जाती हैं। इस ग्रन्थमें कहीं पर भी कातिकेयका नाम नहीं आया है और न ग्रन्थको ही कार्तिकेयानुप्रेक्षा कहा गया है। ग्रन्थके प्रतिज्ञा और समाप्ति वाक्योंमें ग्रन्थका नाम सामान्यत: 'अणुपेहा' या 'अणुपेक्खा' और विशेषतः 'बारस अणुवेक्खा' नाम आया है। भट्टारक शुभचन्द्रने इस ग्रन्थपर विक्रम संवत् १६१३ (ई. सन् १५७६) में संस्कृत टीका लिखी है। इस टीकामें अनेक स्थानोंपर ग्रन्थका नाम कार्तिकेयानुप्रेक्षा दिया है और ग्रन्थकारका नाम कार्तिकेय मुनि प्रकट किया है।
बहुत सम्भव है कि कार्तिकेयशब्द कुमार या स्वामी कुमारका पर्यायवाची यहाँ व्यवहत किया गया हो। यह सत्य है कि शुभचन्द्र भट्टारक के पूर्व अन्य किसी भी पन्धमें बारस-अणुवेक्खाके रचयिताका नाम कार्तिकेय नहीं आया है। शुभचन्द्रने ३९४ संख्यक गाथाकी टीकामें कार्तिकेय मुनिका उदाहरण प्रस्तुत किया है। लिखा है- "स्वामीकार्तिकेयमुनिः क्रौञ्चराजकृतोपसर्ग सोढ्वा साम्य परिणामेन समाधिमरणेम देवलोकं प्राप्त।" स्पष्ट है कि स्वामी कातिकेय मुनि क्रौञ्चराजकृत उपसर्गको समभावसे सहकर समाधिपूर्वक मरणके द्वारा देव लोकको प्राप्त हुए।
भगवती आराधनाकी गाथा-संख्या १५४९ में क्रौञ्च द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए एक व्यक्तिका निर्देश आया है। साथमें उपसर्गस्थान रोहेडक और शक्ति हथियारका भी उल्लेख है। पर कार्तिकेय नामका स्पष्ट निर्देश नहीं है। उस व्यक्तिको अग्निदयितः' लिखा है, जिसका अर्थ अग्निप्रिय है। मूलाराधनादर्पणमें लिखा है- "रोहेडयम्मि रोहेटकनाम्नि नगरे। सत्तोए शक्त्या शस्त्रविशेषेण क्रौञ्चनाम्ना राज्ञा। अग्गिदइदो अग्निराजनाम्नो राज्ञः पुत्रः कार्तिकेय संज्ञः।" अर्थात् रोहेडनगरमें क्रौञ्च राजाने अग्निराजाके पुत्र कार्तिकेय मुनिको शक्तिनामक शस्त्रसे मारा था और मुनिराजने उस दुःखको समत्तापूर्वक सहनकर रनत्रयकी प्राप्ति की थी। इस टीकासे प्रकट होता है कि कार्तिकेयने कुमारावस्थामें मुनिदीक्षा ली थी। बताया गया है कि कार्तिकेयकी बहन रोहेड नगरके क्रौञ्च राजाके साथ विवाहित थी। राजा किसी कारणवश कार्तिकेयसे असन्तुष्ट हो गया और उसने कार्तिकेय को दारुण उपसर्ग दिये। इन उपसर्गोको समत्तासे सहनकर कार्तिकेयने देवलोक प्राप्त किया। इस कथाके आधारपर इतना तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थके रचयिता कार्तिकेय सम्भव है और ग्रंथका नाम भी कार्तिकेयानुप्रेक्षा कल्पित नहीं है।
मूलाचार, भगवती-आराधना और कुन्दकुन्दकृत 'बारह अणुवेक्खा' में बारह भावनाओंका क्रम और उनकी प्रतिपादक गाथाएँ एक ही हैं। यहाँतक कि उनके नाम भी एक हो हैं। किन्तु कार्तिकेयको 'बारहअणुवेक्खा’ में न वह क्रम है और न वे नाम हैं। इसमें क्रम और नाम तत्वार्थसूत्रकी तरह हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्त्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, चोधिदुर्लभ और धर्म इस क्रम तथा नामोसे १२ भावनाएँ आयी हैं। ठीक यही क्रम और नाम कार्तिकेयको 'अणुवेक्खामें’ हैं। अतएव इस भिन्नतासे कार्तिकेय न केवल वट्टकेर, शिवार्य और कुन्दकुन्दके उत्तरवर्ती प्रतीत हाते हैं, अपितु तत्वार्थसूत्रकारके भी उत्तरवर्ती जान पड़ते हैं।
परन्तु यहीं कहा जा सकता है कि तत्त्वार्थसूत्रकारके समक्ष भी कोई क्रम रहा है, तभी उन्होंने अपने ग्रन्थमें उस क्रमको निबद्ध किया है। साथ ही यह भी सम्भावना है कि भावनाओंके दोनों ही क्रम प्रचलित रहे हों, एक क्रमको कुन्दकुन्द, शिवार्य, वट्टकेर आदिने अपनाया और दूसरे क्रमको स्वामी कार्तिकेय, गृद्धपिच्छ आदिने। अतः भावनाक्रमके अपनानेके आधारपर कार्तिकेयके समयका निर्धारण नहीं किया जा सकता और न उनके 'बारह अणुवेक्वा' ग्रंथकी अर्वाचीनता ही सिद्ध की जा सकती है।
स्वामि कात्तिकेयके समयका विचार करते हुए डॉ. ए. एन. उपाध्येने 'बारस-अणुवेक्खा'का अन्तःपरीक्षणकर बतलाया है कि इस ग्रन्थकी २७९ वीं गाथामें 'णिसुणहि' और 'भावहि' ये दो पद अपभ्रंशके आ घुसे हैं, जो वर्तमान काल तृतीय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं। यह गाथा 'जोइन्दु'के योगसारके ६५ वे दोहेके साथ मिलती-जुलती है और दोहा तथा गाथा दोनोंका भाव भी एक है। अतएव इस गाथाको 'जोइन्दु के दोहेका परिवर्तित रूप माना जा सकता है। यथा-
विरला जाणहि तत्तु बहु विरला णिसुणहि तत्तु।
विरला झायहिं तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु॥
विरला णिसुणहि तच्चं विरला जाणंति तच्चदो तच्चं।
विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणा होदि।।
अतः इन दोनों संधार्भोन्के तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर कार्तिकेयका समय जोइन्दुके पश्चात् होना चाहिए।
श्री जुगलकिशोर मुख्तारने डॉ. उपाध्येके इस अभिमतका परोक्षण करते हुए लिखा है कि "यह गाथा कार्तिकेय द्वारा लिखित नहीं है। जिस लोक भावनाके प्रकरणमें यह आयी है, वहाँ इसकी संगति नहीं बैठती।" आचार्य मुख्तारने अपने कथनको पुष्टिके लिए गाथाओंका क्रम भी उपस्थित किया है। उन्होंने लिखा है- "स्वामीकुमारने ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके बनाया है, समुचित प्रतीत नहीं होता- खासकर उस हालतमें जबकि ग्रन्थ भरमें अपभ्रंष भाषाका और कोई प्रयोग भी न पाया जाता हो। बहुत सम्भव है कि किसी दूसरे विद्वानने दोहेको गाथाका रूप देकर उसे अपनी ग्रंथ-प्रतिमें नोट किया हो, और यह भी सम्भब है कि यह गाथा साधारणसे पाठभेदके साथ अधिक प्राचीन हो, और योगेन्दुने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवर्तनके साथ अपना उक्त दोहा बनाया हो; क्योंकि योगेन्दुके परमार्थप्रकाश आदि ग्रन्थोंमें और भी कितने ही दोहे ऐसे पाये जाते हैं, जो भावपाहुड तथा समाधितंत्रादिके पद्योंपरसे परिवर्तन करके बनाये गये हैं और जिसे डॉ. साहबने स्वयं स्वीकार किया है। जब कि स्वामीकुमारके इस ग्रन्थकी ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आयी। "
आचार्य मुख्तार साहबका यह निष्कर्ष उचित्त मालूम होता है, क्योंकि योगसारका विषय क्रमबद्ध रूपसे नहीं है। इसमें कुन्दकुन्दकी अनेक गाथाओंका रूपान्तरण मिलता है। कुन्दकुन्दने कर्मविमुक्त आत्माको परमात्मा बतलाते हुए; उसे ज्ञानी, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णू, चतुर्मुख और बुद्ध कहा है। योगसारमें भी उसके जिन, बुद्ध, विष्णु, शिव आदि नाम बतलाये है। इसके अतिरिक्त जो इन्दुने कुन्दकुन्दके समान हो निश्चय और व्यवहार नयों द्वारा आत्माका कथन किया है। योगसार और परमार्थप्रकाश इन दोनोंका विषय समान होने पर भी योगसार संग्रहग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। इसमें कई तथ्य छूट भी गये हैं। दोहा ९९-१०३ द्वारा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसाम्पराय संयमका स्वरूप बतलाया है। यहाँ यथाख्यात चारित्रका स्वरूप छूट गया है। अतएव योगसारके दोहेका परिवर्तीत रूप कार्तिकेयानुप्रेक्षामें होनेके आधारपर कातिकेयको अर्वाचीन बताना युक्त नहीं है।
आचार्य जुगलकिशोर मुख्तारने समय-निर्णय करते हुये लिखा है- "मेरी समझमें यह ग्रंथ उमास्वातिके तत्वार्थ सूत्रसे अधिक बादका नहीं, उसके निकटवर्ती किसी समयका होना चाहिये, और उसके कर्ता वे अग्निपुत्र कार्तिकेय मुनि नहीं हैं, जो साधारणत: इसके कर्ता समझे जाते हैं, और क्राँच राजाके द्वारा उपसर्गको प्राप्त हए थे, बल्कि स्वामीकुमार नामके आचार्य ही है, जिस नामका उल्लेख उन्होंने स्वयं 'अन्त्यमंगल'की गाथामें श्लेष रूपसे किया है।
आचार्य जुगलकिशोर मुख्तारके उक्त मतसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्तिकेय गृद्धपिच्छके समकालीन अथवा कुछ उत्तरकालोन हैं। अर्थात् वि. सं. को दूसरी-तीसरी शती उनका समय होना चाहिए।
द्वादशानुप्रेक्षामें कुल ४८९ गाथाएँ हैं। इनमें अघ्र व, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, अस्त्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधदुर्लभ और धर्म इन बारह अनुषेक्षाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। प्रसंगवश जीव, अजीव, अस्त्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वोंका स्वरूप भी वर्णीत है। जीवसमास तथा मार्गणाके निरूपणके साथ, द्वादगवत, पात्रोंके भेद, दाताके सात गुण, दानकी श्रेष्ठता, माहात्म्य, सल्लेखना, दश धर्म, सम्यक्त्वके आठ अंग, बारह प्रकारके तप एवं ध्यानके भेद-प्रभेदोंका निरूपण किया गया है। आचार्यका स्वरूप एवं आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया इस ग्रन्थमें विस्तारपूर्वक वर्णीत है।
अघ्रुवानुप्रेक्षामें ४-२२ गाथाएँ हैं। अशरणानुप्रेक्षाम २३-३१; संसारानुप्रेक्षामें ३२-७३; एकात्वानुप्रेक्षामें ७४-७९; अन्यत्वानुप्रेक्षामें ८०-८२: अशु चित्वानुप्रेक्षामें ८३-८७; आस्त्रवानुप्रेक्षामें ८८-१४; संवरानुप्रेक्षामें ९५-१०१, निर्जरानुप्रेक्षामें १०२-११४, लोकानुप्रेक्षामें ११५-२८३; बोधिदुर्लभानुप्रक्षामें २८४-३०१ एवं धर्मानुप्रंक्षामें ३०२-४३५ गाथाएँ हैं। ४३६ गाथासे अन्ततक द्वादश तपोंका वर्णन आया है। अघ्रुवानुप्रेक्षामें समस्त वस्तुओंकी अनित्यता बतलाते हुए वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक कहा है। सामान्य द्रव्यरूप है, और विशेष गुण पर्यायरूप। द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है किन्तु पर्यायकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य हैं। यह संसारका प्राणी पर्यायबुद्धि है, जिससे पर्यायोंको उत्पन्न और नष्ट होते देखकर हर्ष-विषाद करता है, और उसको नित्य रखना चाहता है। यह शरीर जीव-पुद्गलको संयोग जनित पर्याय है धन-धान्यादिक पुद्गल परणुओंकी स्कन्ध पर्याय है। इनके संयोग और वियोग नियमसे अवश्य है, जो स्थिरताकी बुद्धि करता है, वह मोहजनित भावके कारण संक्लेश प्राप्त करता है।
संसारकी समस्त अवस्थाएँ विरोधी भावोंसे युक्त हैं। जब जन्म होता है, तब उसे स्थिर समझकर हर्ष उत्पन्न होता है, मरण होनेपर नाश मानकर शोक करता है। इस प्रकार इष्टकी प्राप्तिमें हर्ष, अप्राप्तीमें विषाद तथा अनिष्ट प्राप्तिमें विषाद, अप्राप्तीमें हर्ष करता है, यह भी सब मोहका माहात्म्य है। आचार्य सादृश्यमूलक उपमा प्रस्तुतकर परिवार, वन्धुवर्ग, स्त्री, पुत्र, मित्र, धनधान्यादिकी अनित्यताका चित्रण करते हुए कहते है-
अथिरं परियण-सवर्ण, पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावण्णं।
गिह-गोहणाइ सव्वं, णव-घण-विदेण सारित्थ।।
परिवार, बन्धुवर्ग, पुत्र, स्त्री, मित्र, सौन्दर्य, गृह, धन, पशु सम्पत्ति इत्यादि सभी वस्तुएँ नवीन मेध-समूहके ममान अस्थिर हैं। इन्द्रियोंके विषय, भृत्य, अश्व, गज, रथ आदि सभी पदार्थ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं।
पुण्यके उदयसे प्राप्त होने वाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी भी नित्य नहीं हैं, तब वह पुण्यहीन अथवा अल्पपुण्यवाले व्यक्तियोंसे केसे प्रेम करेगी? कविने इसी को समझाते हुए लिखा है-
कत्थ वि ण रमइ लच्छी, कुलीण-धीरे वि पंडिए सूरे।
पुज्जे धम्मिट्ठे वि य, सरूव-सुयणे महासत्ते।
अर्थात् यह लक्ष्मी कुलवान, धैर्यवान, पंडित, सुघट, पूज्य, धर्मात्मा, रूपवान, सुजन, महापराक्रमी इत्यादि किसी भी पुरुषसे प्रेम नहीं करती, यह जल की तरंगोंके समान चंचल है। इसका निवास एक स्थानपर अधिक समय तक नहीं रहता। इस प्रकार आचार्य स्वामिकुमारने संसार, शरीर, भोग और लक्ष्मीकी अस्थिरताके चिन्तनको अघ्रुवानुप्रेक्षा कहा है।
अशरण भावनामें बताया है कि मरण करते समय कोई भी प्राणीकी शरण नहीं। जिस प्रकार वनमें सिंह मृगके बच्चेको जब पैरके नीचे दबा लेता है, तब कोई भो उसकी रक्षा नहीं कर सकता , देव , तप आदि सभी मुत्युसे रक्षा करने में असमर्थ है। रक्षा करनेके लिए जितने उपाय किये जाते हैं, वे सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। आयुके क्षय होनेपर कोई एक क्षणके लिए भी आयुदान नहीं सकता-
आउक्खयेण मरणं आउं दाउं ण सक्कदे को वि।
तम्हा देविदो वि य, मरगाउ ण सक्खदे को वि।
आयुकर्मके क्षयसे मरण होता है और आयुकर्मको कोई देनेमें समर्थ नहीं, अतएव देवेन्द्र भी मृत्युसे किसीकी रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार अशरण रूप चिन्तनका समावेश अशरण-भावनामें होता है।
संसार-अनुप्रेक्षामें बताया है कि संसार-परिभ्रमणका कारण मिथ्यात्व और कषाय है। इन दोनोंके निमित्तसे ही जीव चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता है। हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रहरूप भावनाके कारण विभिन्न गत्तियोंमें इस जीवको परिभ्रमण करना पड़ता है| आचार्यने इस भावनामें चतुरंगतिके दुःखोंका वर्णन भी संक्षेपमें किया है। मनुष्यगतिके हाखोंका प्रतिपादन करते हुए संसार स्वभावका विश्लेषण विश्लेषण किया है-
कस्स वि दुटुकलितं, कस्स वि दुव्वसणवसणिओ पुत्तो।
कस्स वि अरिसमबंधू, कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ।।
मरदि सुपुत्तो कस्स वि, कस्स वि महिला विणस्सदे इट्ठा।
कस्स वि अग्गीपलितं, गिहं कुडंबं च डज्झेई।।
संसारमें सुख नहीं है। इस मनुष्यगतिमें नानाप्रकारके दुःख हैं। किसीकी स्त्री दुराचारिणी है, किसीका पुत्र व्यसनी है, किसीका भाई शत्रुके समान कलहकारी है। एवं किसीकी पुत्री दुश्चरित्रा है। इस प्रकार संसारकी विषम परिस्थिति मनुष्यको सुखका कण भी प्रदान नहीं करती है।
किसीके पुत्रका मरण हो जाता है, किसीकी भार्याका मरण हो जाता है और किसीके घर एवं कुटुम्ब जलकर भस्म हो जाते हैं। इसप्रकार मनुष्यगतिमें अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करता हुआ यह जीव धर्माचरणबुद्धिके अभावके कारण कष्ट प्राप्त करता है। मनुष्यगतिकी तो बात ही क्या, देवगति में भी नानाप्रकारके दुःख इस प्राणीको सहन करने पड़ते हैं। इसप्रकार संसारानुप्रेक्षामें, संसारके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंचपरावर्तनोंका वर्णन आया है|
एकत्त्वानुप्रेक्षामें बताया गया है कि जीव अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही नाना प्रकारके कष्टोंको सहन करता है| नानाप्रकारकी पर्याएँ यह जीव घारणकर सांसारिक कष्टोंको भोगता है। रोग, शोक जन्य अनेक प्रकारके कष्टोंको अकेला ही भोगता है। पुण्यार्जनकर अकेला ही स्वर्ग जाता है और पापार्जन द्वारा अकेला ही नरक प्राप्त करता है। अपना दुःख अपनेको ही भोगना पड़ता है, उसका कोई भी हिस्सेदार नहीं है। इसप्रकार एकत्वभावनामें आचार्यने जीवको शरीरसे भिन्न बताया है-
सव्वायरेण जाणह, एवर्क जावं सरीरदो भिण्णं।
अम्हि दु मुणिदे जीवे, होदि असेसं खणे हेय।।
अर्थात सब प्रकारके प्रयत्नकर शरीरसे भिन्न अकेलं जीनको अवगत करना चाहिये। यह जीव समस्त परद्रव्योंसे भिन्न है। अत: स्वयं ही कर्ता और भोक्ता है। इसप्रकार एकत्वानुप्रेक्षामें अकेले जीवको ही कर्ता और भोक्ता होनेके चिन्तनका वर्णन किया है।
अन्यत्वानुप्रेक्षामें शरीरसे आत्माको भिन्न अनुभव करनेका वर्णन किया है। सभी बाह्य पदार्थ आत्मस्वरूपसे भिन्न हैं। आत्मा ज्ञानदर्शन सुखरूप है और यह संसारके समस्त पुद्गलादि पदार्थोंके स्वरूपसे भिन्न है। इसप्रकार अन्यत्वानुप्रेक्षामें आत्माके भिन्न स्वरूपके चिन्तनका कथन आया है।
अशुचित्वानुप्रेक्षामें शरीरको समस्त अपवित्र वस्तुओंका समूह मानकर विरक्त होने का संदेश दिया गया है। शारीर अत्यन्त अपवित्र है। इसके सम्पर्कमें आनेवाले चन्दन, कर्पूर, केसर आदि सुगन्धित पदार्थ भी दुर्गन्धित हो जाते हैं। अतः इसकी अशुचिताका चिन्तन करना अशुचित्वानप्रेक्षा है।
आस्रवानुप्रेक्षामें आस्त्रवके स्वरूप, कारण, भेद एवं उसके महत्वके चिन्तन का वर्णन आया है। मन, वचन, कायका निमित्त प्राप्तकर जीवके प्रदेशोंका चंचल होना योग हैं, इसीको आस्त्रव कहते हैं। बन्धका कारण आस्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके निमित्तसे बन्ध होता है। यह आस्त्रव पुण्य और पापरूप होता है। शुभास्रव पुण्यरूप है और अशुभास्रव पापरूप है। इमी सन्दर्भमें कषायोंके तीव्र और मन्द भेदोंका भी विवेचन आया है। आस्त्रवानुप्रेक्षामें आस्त्रवके स्वरूपका विचार करते हुये उससे अलिप्त रहने का उपदेश है।
संवरानुप्रक्षामें संवरके स्वरूप और कारणोंका विवेचन करते हुए सम्यक्त्व, व्रत, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिगहजय आदिका चिन्तन आवश्यक माना है। इसी सन्दर्भमें आर्त और रौद्र परिणतिके त्यागका भी कथन किया है, जो व्यक्ति इन्द्रियों के विषयोंसे विरक्त होता हआ संवररूप परिणतिको प्राप्त करता है उसीके संवरभावना होती है।
निर्जराभावनाका विवेचन करते हुये बताया है कि जो अहंकार रहित होकर तप करता है, उसीके निर्जरानुप्रेक्षा होती है। ख्याति, लाभ, पूजा और इन्द्रियोंके विषयभोग बन्धके निमित्त है। निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है। आचार्यने प्रारम्भमें ही वैराग्य-भावनाकी उद्दीप्तीका वर्णन करते हुए कहा है-
वारसविहेण तवसा, णियाणरहियस्स णिज्जरा होदि।
वेरम्गभावणादो, णिरहंकारस्स णाणिस्स।।
निदानरहित, अहंकाररहित, ज्ञानीके बारह प्रकारके तपसे तथा वैराग्य भावनासे निर्जरा होती है। समभावसे निर्जराकी वृद्धि होती है। निर्जरा दो प्रकारकी है- सविपाक और अविपाक। कर्म अपनी स्थितिको पूर्णकर, उदयरस देकर खिर जाते हैं उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा सब जीवोंके होती है। और तपके कारण जो कर्म स्थिति पूर्ण हुये बिना ही खिर जाते हैं, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। सविपाक निर्जरा कार्यकारी नहीं है। अविपाक निर्जरा हो कार्यकारी है। अतएव इन्द्रियों ओर कषायोंका निग्रह करके परम वीतरागभावरूप आत्मध्यानमें लीन होना उत्कृष्ट निर्जरा है।
लोकानुप्रेक्षामें लोकके स्वरूप और आकार-प्रकारका विस्तारसे वर्णन है। आकाशद्रव्यका क्षेत्र अनन्त है और उसके बहुमध्य देशमें स्थित लोक है। यह किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। जीवादि द्रव्योका परस्पर एक क्षेत्रावगाह होनेसे यह लोक कहलाता है। वस्तुतः द्रव्योंका समुदाय लोक कहा जाता है। लोक द्रव्य की दृष्टिसे नित्य है, पर परिवर्तनशील पर्यायों की अपेक्षासे परिणामी है। यह पूर्व-पश्चिम दिशामें नीचेके भागमें सात राजु चौड़ा है। वहाँसे अनुक्रमसे घटता हुआ मध्यलोकमें एक राजु रहता है। पुनः ऊपर अनुक्रमसे बढ़ता-बनता ब्रह्म स्वर्ग तक पाँच राजु चौड़ा हो जाता है, पश्चात् घटते-घटते अन्नमें एक राजु रह जाता है। इसप्रकार खड़े किये गये डेढ मृदंगकी तरह लोकका पूर्व-पश्चिम में आकार होता है। उत्तर-दक्षिणमें भी सात राजु विस्तार है। मेरुके नीचे भी सात राजु अधोलोक है। लोकशब्दका अर्थ बतलाते हुए लिखा है-
दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ।
तस्स सिहरम्मि सिद्धा, अंतविहीणा विरायंते।।
जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक कहलाता है। लोकमें जीव, पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ: द्रव्योंका निवास है। इस अनुप्रेक्षामें इन छहों द्रव्योंका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लोकानुप्रेक्षामें द्रव्योंके स्वभाव-गुणको बतलाते हुये, शरीरसे भिन्न आत्माकी अनुभूति करनेका चित्रण किया है। इस भावनामें गुणस्थानोंके स्वरूप और भेदोंका भी कथन आया है तथा सप्त नयोंकी अपेक्षासे जीवादि पदार्थोंका विवेचन भी किया गया है।
बोधिदुर्लभभावनामें आत्मज्ञानकी दुलभतापर प्रकाश डाला गया है। आरम्भमें बतलाया गया है कि संसारमें समस्त पदार्थोंकी प्राप्ति सुलभ है, पर आत्मज्ञानकी प्राप्ति होना अत्यन्त दुष्कर है। सम्यक्त्वके बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिसे मन्द कर्मोदयसे रत्नत्रय भी प्राप्त हो गया हो, वह व्यक्ति यदि तीव्र कषायके अधीन रहे, तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वह दुर्गति का पात्र बनता है। प्रथम तो मनुष्यगतिकी प्राप्ति ही दुर्लभ है और इस पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी सम्यक्त्वका मिलना दुष्कर है। सम्यक्त्व प्राप्त होनेपर भो सम्यक् बोधका मिलना और भी कठिन है। इसप्रकार स्वामिकार्तिकेयने वोधिकी दुर्लभताका कथन करते हुये रत्नत्रयके स्वरूप आदि पर प्रकाश डाला है।
धर्मानुप्रेक्षामें धर्मका यथार्थ स्वरूप अतीन्द्रिय बतलाया है। धर्मका वास्तविक रूप सर्वज्ञता है। सर्वज्ञताके अस्तित्वमें किसीप्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता है। इस घर्मानुप्रेक्षामें कर्मबन्धके चक्रवालका भी विश्लेषण आया है। बताया गया है कि सर्वज्ञदेव सब द्रव्य, क्षण, काल भावोंकी अवस्थाको जानते हैं। सर्वज्ञके ज्ञानमें सब कुछ प्रकाशित होता है। उनके ज्ञानमें जिस प्रकारके पदार्थोकी पर्यायें प्रतिविम्बित होती हैं, उन पर्याय जन्य फल वैसा ही घटित होता है। उसमें कोई किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं कर सकता है। निम्न दोनों गाथाओंसे पर्यायोंकी नियत स्थिति सिद्ध होती है-
जं जस्स जम्मि देसे, जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि।
णादं, जिणेण णियदं, जम्म वा अहव मरणं वा॥
तं तस्स तम्मि देसे, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि।
को सक्कदि वारेदूं, ईदा वा अह जिणिदो वा।।
जो जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जन्म-मरण, दुःख-सुख, रोग-दारिद्र आदि सर्वज्ञदेवके द्वारा जाने गये हैं, वे नियमसे ही उस प्राणोकी उसी देशमें , उसी कालमें और उसो विधानसे प्राप्त होते हैं। इन्द्र, जिनेन्द्र या तीर्थंकरदेव अन्य कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकते। इस प्रकारके निश्चयसे सब द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन द्रव्यों और इनकी समस्त पर्यायोंका जो श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यकदृष्टी है। यह स्मरणीय है कि जीव मिथ्यात्वकर्मके, उपशम, क्षयोपशम या क्षयके बिना तत्त्वार्थको ग्रहण नहीं कर पाता। इसप्रकार धर्मानुप्रेक्षामें व्यवहारधर्म और निश्चयधर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।
१८६ गाथाओं में इस अनुप्रेक्षाका वर्णन आया है। अनशनादि बारह तप भी इसी वर्णनसंदर्भ में समाविष्ट हैं। बारह व्रतोंके निरूपणमें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंका क्रम वही है, जो कुन्दकुन्दके 'चारित्रपाहुड में पाया जाता है। भेद केवल इतना ही है कि अन्तिम शिक्षाव्रत संल्लेखना नहीं, किंतु देशावकाशिक ग्रहण किया गया है। यह गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंकी व्यवस्था तत्त्वार्थसूत्रसे संख्याक्रममें भिन्न है, और श्रावक प्रज्ञाप्राप्तिकी व्यवस्थाके तुल्य है।
इस प्रकार धर्मानुप्रेक्षामें तपों और व्रत्तोंका विस्तारपूर्वक कथन आया है। श्रावकधर्म और मुनिधर्मको संक्षेपमें अवगत करनेके लिए यह ग्रंथ उपयोगी है।
स्वामी कार्तिकेयकी रचना-शक्ति शिवार्य और कुन्दकुन्दके समान है। विषयको सरल और सुबोध बनानेके लिए उपमानोंका प्रयोग पद-पदपर किया गया है। लेखक जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है, उस तथ्यको बड़ी हो द्रुधताके साथ उपस्थित कर देता है। प्रश्नोत्तर-शैलीमें लिखी गयी गाथाएँ तो विशेष रोचक और महत्वपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणार्थ दो गाथाओंकी उपस्थित कर लेखककी रचना-प्रतिभाका परिचय प्रस्तुत किया जाता है-
को ण वसो इत्थिजणे, कस्स ण मयणेण खंडियं माणं।
को इंदिएहिण जियो, को ण कसाएहि संतत्तो।
सो ण वसो इस्थिजणे, सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण।
जो ण य गिण्हदि गंर्थ, अब्भंतर बाहिरं सव्व।
इस लोकमें स्त्रीजनके वशमें कौन नहीं? कामने किसका मान खण्डित नहीं किया? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन सतप्त नहीं हुआ? ग्रन्थकारने इन समस्त प्रश्नोंका उत्तर तर्कपूर्ण और सुबोध शैलीमें अंकित किया है। वह कहता है, जो मनुष्य बाह्य और आनन्तर संमस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो स्त्रीजनके वश में होता है, न कामके अधीन होता है और न मोह और इन्द्रियों के द्वारा हो जोता जा सकता है।
इस ग्रन्थकी अभिव्यंजना बड़ी ही सशक है। ग्रन्थकारने छोटी-सी गाथामें बड़े-बड़े तथ्योंको संजो कर सहजरूपमें अभिव्यक्त किया है। भाषा सरल और परिमार्जित है। शैलीमें अर्थसौष्ठव, स्वच्छता, प्रेषणीयता, सूत्रात्मकता अलंकारात्मकता समवेत है।
श्रुतधराचार्यसे अभिप्राय हमारा उन आचार्यों से है, जिन्होंने सिद्धान्त, साहित्य, कमराहिम, बायाससाहित्यका साथ दिगम्बर आचार्यों के चारित्र और गुणोंका जोबन में निर्वाह करते हुए किया है। यों तो प्रथमानुयोग, करणा नुयोग, चरणानुयोग और ध्यानुयोगका पूर्व परम्पराके भाधारपर प्रन्धरूपमें प्रणयन करनेका कार्य सभी आचार्य करते रहे हैं, पर केवली और श्रुत केवलियोंकी परम्पराको प्राप्त कर जो अंग या पूर्वो के एकदेशशाता आचार्य हुए हैं उनका इतिवृत्त श्रुतधर आचार्यों को परम्पराके अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायगा | अतएव इन आचार्यों में गुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवाल, यति वृषम, उच्चारणाचार्य, आयमंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, गृपिच्छाचार्य और बप्पदेवकी गणना की जा सकती है ।
श्रुतधराचार्य युगसंस्थापक और युगान्तरकारी आचार्य है। इन्होंने प्रतिभाके कोण होनेपर नष्ट होतो हुई श्रुतपरम्पराको मूर्त रूप देनेका कार्य किया है। यदि श्रतधर आचार्य इस प्रकारका प्रयास नहीं करते तो आज जो जिनवाणी अवशिष्ट है, वह दिखलायी नहीं पड़ती। श्रुतधराचार्य दिगम्बर आचार्यों के मूलगुण और उत्तरगुणों से युक्त थे और परम्पराको जीवित रखनेको दृष्टिसे वे ग्रन्थ-प्रणयनमें संलग्न रहते थे 1 श्रुतकी यह परम्परा अर्थश्रुत और द्रव्यश्रुतके रूपमें ई. सन् पूर्वकी शताब्दियोंसे आरम्भ होकर ई. सनकी चतुर्थ पंचम शताब्दी तक चलती रही है ।अतएव श्रुतघर परम्परामें कर्मसिद्धान्त, लोका. नुयोग एवं सूत्र रूपमें ऐसा निबद साहित्य, जिसपर उत्तरकालमें टीकाएँ, विव त्तियाँ एवं भाष्य लिखे गये हैं, का निरूपण समाविष्ट रहेगा।
Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara_2.
Acharya Shri Kartikey Maharaj Ji (Prachin)
#kartikeymaharaj
15000
Acharya Shri Kartikey Maharajji (Prachin)
#kartikeymaharaj
kartikeymaharaj
You cannot copy content of this page