हैशटैग
#samantbhadramaharaj

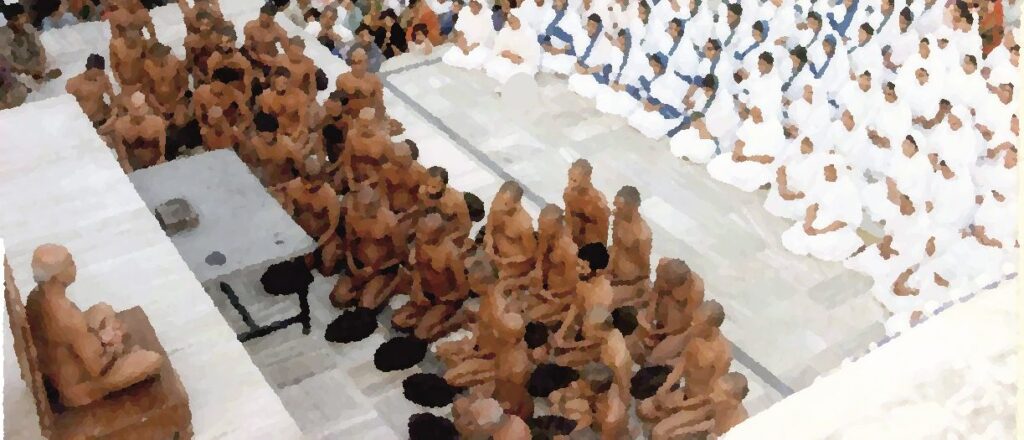
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्ति रश्मयः।
वज्रन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलबोद्धता जनाः'।।
समन्तभद्रादिमहाकवीश्वराः कुवादिविद्याजयलब्धकीर्तयः।
सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकाक्षिणि।।
श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुम्मरसञ्चयम्।
मुनिवन्ध जनानन्दं नमामि वचनश्रिये॥
सारस्वताचार्योंमें सबसे प्रमुख और आद्य आचार्य समन्तभद्र है। जिस प्रकार गृद्धपिच्छाचार्य संस्कृतके प्रथम सूत्रकार है, उसी प्रकार जैन वांडमयमें स्वामी समन्तभद्र प्रथम संस्कृत-कवि और प्रथम स्तुतिकार हैं। ये कवि होनेके साथ प्रकाण्ड दार्शनिक और गम्भीर चिन्तक भी हैं। इन्हें हम श्रुतधर आचार्यपरम्परा और सारस्वत आचार्यपरम्पराको जोड़नेवाली अटूट श्रृंखला कह सकते हैं। इनका व्यक्तित्व श्रुतधर आचार्यो से कम नहीं है।
स्तोत्र-काव्यका सूत्रपात आचार्य समन्तभद्रसे ही होता है। ये स्तोत्र-कवि होने के साथ ऐसे तर्ककुशल मनीषी हैं, जिनकी दार्शनिक रचनाओंपर अकलंक और विद्यानन्द जैसे उदभट आचार्यों ने टीका और विवृत्तियों लिखकर मौलिक ग्रन्थ रचयिताका यश प्राप्त किया है| वीतरागी तीर्थकरकी स्तुतियोंमें दार्शनिक मान्यताओंका समावेश करना असाधारण प्रतिभाका ही फल है।
आदिपुराणमें आचार्य जिगोनने जन्हें वापद हामिल, कवित्व और गमकत्व इन चार विशेषणोंसे युक्त बताया है। इतना ही नहीं, जिनसेनने इनको कवि-वेधा कहकर कवियोंको उत्पन्न करनेवाला विधाता भी लिखा है-
कवीनां गमकानाञ्च वादिनां वाग्मिनामपि।
यशः सामन्तभद्रीयं मूनि चूडामधीयते।।
नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ।
यद्धचोवज्जपातेन निभिन्ना: कुमतादयः।।
मैं कवि समन्तभद्रको नमस्कार करता हूँ, जो कवियोंसे ब्रह्मा हैं, और जिनके वचनरूप वज्ज्रपातसे मिथ्यामतरूपी पर्वत चूर-चूर हो जाते हैं।
स्वतन्त्र कविता करनेवाले कवि, शिष्योंको मर्मतक पहुँचानेवाले गमक, शास्त्रार्थ करनेवाले वादी और मनोहर व्याख्यान देनेवाले वाग्मियोंके मस्तक पर समन्तभद्रस्वामीका यश चुडामणिके समान आचरण करनेवाला है| वादोभसिंहने अपने 'गद्यचिन्तामणि' ग्रन्थमें समन्तभद्रस्वामीकी तार्किक प्रतिमा एवं शास्त्रार्थ करनेकी क्षमताकी सुन्दर व्यंजना को है। समन्तभद्रके समक्षा बड़े-बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका महत्व समाप्त हो जाता था और प्रतिवादी मौन होकर उनके समक्ष स्तब्ध रह जाते थे।
सरस्वतीस्वैरविहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः।
जयन्ति वाग्वनिपातपाटितप्रतीपरादान्तमहीघ्रकोटयः।।
श्रीसमन्तभद्र मुनीश्वर सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि थे। उनके वचनरूपी वज्ज्रके निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चोटियाँ चूर-चूर हो गयी थीं। उन्होंने जिनशासनकी गौरवमयी पताकाको नीले आकाशमें फहरानेका कार्य किया था। परवादी-पंचानन बर्द्धमानसूरिने समन्तभद्रको 'महाकवीश्वर' और 'सुतर्कशास्त्रामृससागर' कहकर उनसे कवित्वशक्ति प्राप्त करनेकी प्रार्थना की है-
समन्तभद्रादिमहाकवारवराः कुवादिविद्याजयलब्धकोत्तयः।
सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांक्षिणि||
श्रवणबेलगोलाके शिलालेख न. १०५ में समन्तभद्र की सुन्दर उक्तियोंको वादीरुपी हस्तियोंको वश करनेके लिए वज्राकुंश कहा गया है तथा बतलाया है कि समन्तभद्र के प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी दुर्वादोंकी वार्तासे भी रहित हो गयी थी।
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभवज्राकुशसूक्तिजालः।
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वन्ध्यास दुव्र्वादुकवार्तयापि।।
स्यात्कारमुद्रित-समस्त-पदार्थपूर्णत्रैलोक्य-हम्मखिलं स खलु व्यक्ति।
दुव्वादुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं सामन्तभद्र-वचन-स्फुटरनदीपः।।
ज्ञानार्णवके रचयिता शुभचन्द्राचार्यने समन्तभद्रको 'कबीन्द्र- भास्वान' विशेषणके साथ स्मरण करते हुये उन्हें श्रेष्ठ कवीश्वर कहा है-
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरममयः।
वज्रन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलवोद्धता जनाः।।
अजितसेनका 'अलंकारचिन्तामणि' और ब्रह्म अजितके 'हनुमच्चरित्' एवं श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं. ५४ और अभिलेख नं. १०८ में समन्तभद्रका स्मरण महाकविके रूपमें किया गया है।
इस प्रकार जैन वाडमयमें समन्तभद्र पूर्ण तेजस्वी विज्ञान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादिविजेता और कविवेधके रूपमें स्मरण किये गये हैं। जैन धर्म और जैनसिदान्तके मर्मज विद्वान होनेके साथ तर्क, व्याकरण, छन्द, अलंकार एवं काव्य-कोषादि विषयोंमे पूर्णतया निष्णात थे। अपनी अलौकिक प्रतीभा द्वारा इन्होंने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्रायः समस्त विषयोंको आत्मसात् कर लिया था। संस्कृत, प्राकृत आदि विभिन्न भाषाओंके पारंगत विद्वान थे। स्तुतिविद्याग्रंथसे इनके शब्दाधिपत्यपर पूरा प्रकाश पड़ता है।
दक्षिण भारतमें उच्च कोटिके संस्कृत-ज्ञानको प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और प्रसारण देने वालोंमें समंतभद्रका नाम उल्लेखनीय है। आप ऐसे युगसंस्थापक हैं, जिन्होंने जैन विद्याके क्षेत्रमें एक नया आलोक विकीर्ण किया है। अपने समयके प्रचलित नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद,ब्रह्माद्वैतवाद, पुरुष एवं प्रकृतिवाद आदिकी समीक्षाकर स्यादवाद-सिद्धांतको प्रतिष्ठा की है। 'अलंकारचिन्तामणि’ में 'कविकुन्जर', 'मुनिबंध' और 'जनानन्द' आदि विशेषणों द्वारा अभिहित किया गया है। श्रवणबेल्गोला के शिलालेखोमी में तो इन्हें जीनशाषण प्रणेता और भद्र मूर्ती कहा गया है। इस प्रकार वाङ्मयसे समत्तभद्रके शास्त्रीय ज्ञान और प्रभाव का परिचय प्राप्त होता है।
समत्तभद्रका जन्म दक्षिमभारतमें हुआ था। इन्हें चोल राजवंशका राजकुमार अनुमित किया जाता है। इनके पिता उरगपुर (उरैपुर) के क्षत्रिय राजा थे। यह स्थान कावेरी नदीके तटपर फणिमण्डलके अंतर्गत अत्यंत समृद्धिशाली माना गया है। श्रवणबेलगोलाके दौरवलि जिनदास शास्त्रीके भण्डारमें पायी जाने वाली आप्तमीमांसाकी प्रतिके अतमें लिखा है- "इति फणिमंडलालंकारस्योरगपुराधिपसुनोः श्रीस्वामीसमन्तभद्रमुनेः कृतो आप्तमीमांसायाम्" इस प्रशस्ति वाक्यसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र स्वामीका जन्म क्षत्रियवंशमें हुआ था और उनका जन्मस्थान उरगपुर है। 'राजावलिकथे’ में आपका जन्म उत्कलिका ग्राममें होना लिखा है, जो प्रायः उरगपुरके अंतर्गत हो रहा होगा। आचार्य जुगलकिशोर मख्तारका अनुमान है कि यह उरगपुर उरैपुरका ही संस्कृत अथवा श्रुतमधुर नाम है, चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी थी। ‘त्रिचिनापोली’ का ही प्राचीन नाम उरयूर था। यह नगर कावेरीके तटपर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा ही समृद्धशाली जनपद था।
इनका जन्म नाम शांतिवर्मा बताया जाता है। 'स्तुतिविद्या' अथवा 'जिनस्तुतिशतम्’ में, जिसका अपर नाम जिनशतक' अथवा 'जिनशतकालंकार' है, "गत्वैकस्तुतमेव'' आदि पद्य आया है। इस पद्ममें कवि और काव्यका नाम चित्रबद्धरूपमें अंकित है। इस काव्यके छह आरे और नव वलय वाली चित्ररचना परसे 'शांतिवर्मकृतम्' और 'जिनस्तुतिशतम्' ये दो पद निकलते हैं। लिखा है- "षडरं नववलयं चक्रमालिख्य सप्तमवलये शांतिवर्मकृतं इति भवति।” "चतुर्थवलये जिनस्तुतिशतं इति च भवति अतः कवि-काव्यनामगर्भ चक्रवृत्तं भवति। इससे स्पष्ट है कि आचार्य समन्तभद्रने ‘जिनस्तुतिशतम्’ का रचयिता शांतिवर्मा कहा है, जो उनका स्वयं नामांतर संभव है। यह सत्य है कि यह नाम मुनि अवस्थाका नहीं हो सकता, क्योंकि वर्मान्त नाम मुनियोके नहीं होते। संभव है कि माता-पिताके द्वारा रखा गया यह समन्तभद्रका जन्मनाम हो। 'स्तुतिविद्या' किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित न होकर समन्तभद्रकी ही कृति मानी जाती है। टीकाकार महाकवि नरसिंहने- "ताकिकचूडामणि श्रीमत् समन्तभद्राचार्यविरचित" सूचित किया है और अन्य आचार्य और विद्वानोंने भी इसे समत्तभद्रकी कृति कहा है। अतएव समन्तभद्रका जन्मनाम शांतिवर्मा रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है।
मुनि-दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात् जब ये मणुवकहल्ली स्थानमें विचरण कर रहे थे कि उन्हें भस्मक व्याधि नामक भयानक रोग हो गया, जिससे दिगम्बर मुनिपदका निर्वाह उन्हें अशक्य प्रतीत हुआ। अतएव उन्होंने गुरुसे समाधिमरण धारण करनेको अनुमति मांगी| गुरुने भविष्णु शिष्यको बादेश देते हुए कहा- "आपसे धर्म और साहित्यकी बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं, अत: आप दीक्षा छोड़कर रोग-शमनका उपाय करें। रोग दूर होनेपर पुन: दीक्षा ग्रहण कर लें"। गुरुके इस आदेशानुसार समन्तभद्र रोगोपचारके हेतु नाग्यपदको छोड़कर सन्यासी बन गये और इधर-उधर विचरण करने लगे। पश्चात वाराणसीमें शिवकोटि राजाके भीमलिंग नामक शिवालयमें जाकर राजाको आर्शीवाद दिया और शिवजीको अर्पण किये जाने वाले नैवेद्यको शिवजीको ही खिला देनेकी घोषणा की। राजा इससे प्रसन्न हुआ और उन्हें शिवजीको नैवेद्य भक्षण करानेकी अनुमति दे दी। समन्तभन्न अनुमति प्राप्त कर शिवालयके किंवाड़ बन्द कर उस नैवेद्यको स्वयं ही भक्षण कर रोगको शांत करने लगे। शनैः शनै: उनकी व्याधिका उपशम होने लगा और भोगको सामग्री बचने लगी। राजाको इसपर सन्देह हुआ। अत्तः गुप्तरूपसे उसने शिवालयके भीतर कुछ व्यक्तियों को छिपा दिया। समन्तभद्रको नेवेद्यका भक्षण करते हुए छिपे व्यक्तियोंने देख लिया। समन्तभद्रने इसे उपसर्ग समझ कर चर्तुविशति तीर्थ करोंकी स्तुति आरंभ की। राजा शिवकोटिके डरानेपर भी समन्तभद्र एकाग्रचित्तसे स्तवन करते रहे, जब ये चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति कर रहे थे कि भीमलिंग शिवकी पिण्डी विदीर्ण हो गयी और मध्यसे चन्द्रप्रभ स्वामीका मनोज्ञ स्वर्णनिम्न प्रकट हो गया। समन्तभद्रके इस महात्म्यको देखकर शिक्कोटि राजा अपने भाई शिवायन सहित आश्चर्य चकित हुआ। समन्तभद्रने वर्धमान पर्यन्त चतुर्विशशति तीर्थंकरोंकी स्तुति पूर्ण हो जानेपर राजाको आशीर्वाद दिया।
यह कथानक 'राजाबलिकथे’ में उपलब्ध है। सेनगणकी पट्टावलिसे भी इस विषयका समर्थन होता है। पट्टावलिमें भीमलिंग शिवालयमें शिवकोटि राजाके समन्तभद्र द्वारा चमत्कृत्त और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है। साथ ही उसे नवतिलिंग देशका राजा सूचित किया है, जिसकी राजधानी सम्भवतः काञ्ची रही होगी। यहाँ यह अनुमान लगाना भी अनुचित नहीं है कि सम्भवत: यह घटना काशीकी न होकर काञ्चीको है। काञ्चीको दक्षिण काशी भी कहा जाता रहा है- "नर्वातलिंगदेशाभिरामद्राक्षाभिरामभोमलिङ्गस्चयन्वादिस्तोटकोस्कोरण ? रुद्रसान्द्रचदिकाविशदयशःश्रीचन्द्रजिनेन्द्रसइर्शनसमुत्पन्नकौतू हलकलितशिवकोटिमहाराजतपोराज्यस्थापकाचार्यश्रीमत्समन्तभद्रस्वामिनाम्”
इस तथ्यका समर्थन श्रवणबेलगोलाके एक अभिलेखसे भी होता है। अभिलेख में समन्तभद्र स्वामीके भस्मक रोगका निर्देश आया है। आपत्काल समाप्त होने पर उन्होंने पुनः मुनि-दीक्षा ग्रहण की। बताया है-
"वन्द्यो भस्मक-भस्म-सात्कृति-पटुः पद्मावतीदेवता-
दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभः।
आचार्यस्स समन्तभद्रगणभृधेनेह काले कली,
जैन वत्र्म समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तान्मुहः।।"
अर्थात् जो अपने भस्मक रोगको भस्मसात् करनेमें चतुर हैं, पद्मावती नामक देवीकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपने मन्त्रवचनोंसे चन्द्रप्रभको प्रकट किया और जिनके द्वारा यह कल्णाणकारी जैन मार्ग इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुभा, वे गणनायक आचार्य समन्तभद्र बार-बार वन्दना किये जाने योग्य हैं।
यह अभिलेख शक संवत् १०२२ का है। अतः समन्तभद्रकी भस्मक व्याधि की कथा ई. सन्के १०वी, ११वीं शताब्दी में प्रचलित रही है।
ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशमें भी शिवकोटि राजाका उल्लेख है। राजाके शिवालयमें शिव-नैवेद्यसे भस्मक-व्याधिकी शान्ति और चन्द्रप्रभजिनेन्द्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बका प्रादुर्भूत होना साथ-साथ वर्णित है। यह भी बताया गया है कि शिवकोधि महाराजने जिनदीक्षा भी धारण की थी।
ब्रह्मनेमिदत्तने शिवकोटिको काञ्चो अथवा नव तैलङ्ग देशका राजा न लिखकर वाराणसीका राजा लिखा है। भारतीय इतिहासके आलोडनसे न तो काशीके शिवकोटि राजाका ही उल्लेख मिलता है और न काञ्चीके ही।
प्रा. ए. चक्रवतीने पञ्चास्तिकायकी अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें बताया है कि काञ्चीका एक पल्लवराजा शिवस्कन्ध वर्मा था, जिसने 'मायदाबोलु' का दान-पत्र लिखाया है। इस राजाका समय विष्णुगोपसे पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी है। यदि यही शिवकोटि रहा हो, तो समन्तभद्र के साथ इसका सम्बन्ध घटित हो सकता है। 'राजाबलि कथे', 'पट्टावलि, एवं श्रवणबेलगोलाके अभिलेखमें शिवकोटिका निर्देश जिस रूपमें किया गया है उस रूपके अध्ययनसे उसके अस्तित्वसे इंकार नहीं किया जा सकता है।
ब्रह्म नेमिदत्तने समन्तभद्रकी कथामें काशीका उल्लेख किया है। पर यह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। कथाके ऐसे भी कुछ अंश है जो यथार्थ नहीं मालूम होते। कथामें आया है- "काञ्चोमें उस समय भस्मक व्याधिको नाश करनेके लिए स्निग्ध भोजनोंकी सम्प्राप्तिका अभाव था। अत: वे काञ्ची छोड़कर उत्तरकी ओर चल दिये। वे पुपड़ेन्द्रनगरमें पहुंचे। यहाँ बौद्धोंकी महती दानशाला देखकर उन्होंने बौद्ध भिक्षुका रूप धारण किया। पर जब वहाँ भी महाव्याधिका उपशम नहीं हुआ तो वे वहाँसे निकलकर अनेक नगरों में घूमते हुए दशपुर नगरमें पहुंचे। यहाँ भागवतोंका उन्नत मठ देखकर वे विशिष्ट आहारप्राप्तिकी इच्छासे बौद्ध भिक्षुका वेष त्याग वैष्णव संन्यासी बन गये। यहाँके विशिष्ट आहार द्वारा भी जब उनकी भस्मक व्याधि शान्त न हुई, तो वे नाना देशोंमें घूमते हुए वाराणसी पहुंचे और वहीं उन्होंने योगि-लिङ्ग धारण करके शिवकोटि राजाके शिवालयमें प्रवेश किया। यहां घी-दूध-दही-मिष्टान्न आदि नाना प्रकारके नेवेद्य शिवके भोगके लिए तैयार किये जाते थे। समन्त भद्रने शिवकोटि राजासे निवेदन किया कि वे अपनी दिव्यशक्ति द्वारा समस्त नेवेद्यको शिवको खिला सकते हैं। राजाका आदेश प्राप्त कर समन्तभद्रने मन्दिरके कपाट बन्द कर समस्त नैवेद्य स्वयं ग्रहण किया और आचमनके पश्चात् किवाड़ खोल दिये। राजा शिवकोटिको महान आश्चर्य हआ कि मनोंकी परिमाणमें उपस्थित किया गया नैवेद्य साक्षात् शिवने ही अवतरित होकर ग्रहण किया है। योगिराजकी शक्ति अपूर्व है, अतएव उनको शिवालयका प्रधान पुरोहित नियुक्त किया। समन्तभद्र प्रतिदिन नैवेद्य प्राप्त करने लगे और शनैः शनैः उनकी मस्मक व्याधि शान्त होने लगी। मन्दिरके प्रमुख पुरोहितोंने ईर्ष्यावश समन्तभद्रकी देखरेख की और राजाको सूचना दी कि तथाकथित योगि शिवको नैवेद्य न ग्रहण कराकर स्वयं नैवेद्य ग्रहण कर लेता है। राजाके आदेशानुसार एक दिन समन्तभद्रको भोजन करते हुए पकड़ लिया गया और उनसे शिवको नमस्कार करनेके लिए कहा। समन्तभद्रने उत्तर दिया, "रागी देषी देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता है। राजाने आज्ञा दी कि अपना सामर्थ्य दिखलाकर स्ववचनको सिद्ध करो।
रात्रिमें समन्तभद्रको वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, क्योंकि प्रातःकाल ही उनको अपनी परीक्षा उत्तीर्ण होना था। उनकी चिन्ताके कारण अम्बिका देवीका आसन कम्पित हुआ और वह दौड़कर समन्तभद्र के समक्ष उपस्थित हुई और उन्हें आश्वासन दिया। प्रात:काल होनेपर अपार भीड़ एकत्र हुई और समन्तभदने अपना स्वयंभूस्तोत्र आरम्भ किया। जिस समय वे चन्द्रप्रभ भगवानको स्तुति करते हा 'तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम्' यह वाक्य पढ़ रहे थे, उसी समय वह शिवलिङ्ग खण्ड-खण्ड हो गया और उसके स्थानपर चन्द्रप्रभ भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा प्रकट हुई। राजा शिवकोटि समन्तभद्रके इस महत्वको देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने समन्तभद्रसे उनका परिचय पूछा। समन्तभद्रने उत्तर देते हुए कहा-
"काच्या नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुलम्बिशे पाण्डुपिण्डः।
पुण्ड्रेण्डे शाक्यभिक्षुर्दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिवाट्।।
वाराणस्यामभूवं शशकरधवलः पाण्डुराङ्गस्तपस्वी।
राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिग्रन्थवादी।।"
मैं काञ्ची में नग्नदिगम्बर यत्तिके रूपमें रहा, शरीरमें रोग होनेपर पुण्डनगरीमें बौद्ध भिक्षु बनकर मैंने निवास किया। पश्चात् दशपुर नगरमें मिष्टान्न भोजी परिवाजक बनकर रहा। अनन्तर वाराणसी में आकर शैव तपस्वी बना। है राजन् ! मैं जैननिर्ग्रंथवादी-स्याद्वादी हूँ। यहाँ जिसकी शक्ति वाद करनेकी हो वह मेरे सम्मुख आकर वाद करे। द्वितीय पद्यमें आया है-
पुर्ण पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठपक-विषये काञ्चीपुरे वैदिशे।
प्राप्तोऽहं करहाटक बहुभट विद्योत्कटं ससूट
वादार्थी विचराम्यहन्नरपते शाई लविक्रीडितम्।।
मैंने पहले पाटलिपुत्र नगरमें वादकी भेरी बजाई। पुनः मालवा, सिन्ध देश, ढक्क-ढाका(बंगाल), काञ्चीपुर और वैदिश-विदिशा-भेलसाके आसपासके प्रदेशोंमें भेरी बजाई। अब बड़े-बड़े वीरोंसे युक्त इस करहाटक-कराड, जिला सतारा, नगरको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हे राजन् ! मैं वाद करनेके लिए सिंहके समान इतस्ततः क्रिड़ा करता फिरता हूँ।
राजा शिवकोटिको समन्तभद्रका चमत्कारक उक्त आख्यान सुनकर विरक्ति हो गयी और वह अपने पुत्र श्रीकण्ठको राज्य देकर प्रवजित हो गया। समन्तभद्रने भी गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त ले पुनः दीक्षा ग्रहण की।
ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकथा-कोषकी उक्त कथा प्रभाचन्द्र के गद्यात्मक लिखे गये कथाकोषके आधारपर लिखी गयी है। बुद्धिवादीकी दष्टिसे उक्स कथाका परीक्षण करनेपर समस्त तथ्य बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी इसना तो स्पष्ट है कि समन्तभद्रको भस्मक व्याधि हई थी और उसका शमन किसी शिवकोटिनामक राजाके शिवालयमें जानेपर हुआ था। हमारा अनुमान है कि यह घटना दक्षिण काशी अर्थात् काञ्चीकी होनी चाहिए।
समन्तभद्रको गुरु-शिष्यपरम्परा के सम्बन्धमें अभी सक निर्णीत रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। समस्त जैन वाडमय समन्तभद्रके सम्बन्ध में प्रशंसात्मक उक्तियां मिलती हैं। समन्तभद्र वर्धमान स्वामीके तीर्थको सहस्त्रगुनी वृद्धि करने वाले हुए और इन्हें श्रुतकेचलिऋद्धि प्राप्त थी। चन्नरायपट्टण ताल्लुकेके अभिलेख न. १४९में श्रुतकेवली-संतानको उन्नत करने वाले समन्त भद्र बताये गये हैं-
"श्रुतकेवलिगलु पलवरूप
अतीतर आद् इम्बलिक्के तत्सन्तानो
न्नतियं समन्तभद्र
वृतिपर् अलेन्दरू समस्तविद्यानिधिगल।।"
यह अभिलेख शक संवत् १०४७का है। इसमें समन्तभद्रको श्रुतकेलियोंके समान कहा गया है। एक अभिलेखमें बताया है कि श्रुतकेलियों और अन्य आचार्योंके पश्चात् समन्तभद्रस्वामी श्रीवर्धमानस्वामीके तीर्थकी सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए अभ्युदरको प्राप्त हुए।
"श्रीवर्धमानस्वामिगलु तीत्थंदोलु केवलिगलु ऋद्धीप्राप्तरुं श्रुतकेवलिगलुं पलरूं सिद्धसाध्यर् आगे तत्___त्यंमं सहस्त्रगणं माहि समन्तभद्र-स्वा मिगलु सन्दर___।"
इन अभिलेखोंसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि समन्तभद्र श्रुतधरोंकी परम्पराके आचार्य थे| इन्हें जो श्रुतपरम्परा प्राप्त हुई थी, उस श्रुतपरम्पराको इन्होंने बहुत ही वृद्धिगत किया।
विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके विद्वान् कवि हस्तिमल्ल और 'अय्यप्पार्यने' श्रीमूलसंघव्योसनेन्दु विशेषण द्वारा इनकी मूलसंघरूपी आकाशका चन्द्रमा बताया है। इससे स्पष्ट है कि समन्तभद्र मूलसंघके आचार्य थे।
श्रवणबेलगोलके अभिलेखोंसे ज्ञात होता है कि भद्रबाहू श्रुतकेवलीके शिष्य चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मुनिके वंशज पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्द मुनिराज, उनके वंशज गृद्धपिच्छाचार्य और गृद्धपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छाचार्य और उनके वंशज समन्तभद्र हुए। अभिलेख में बताया है-
"श्रीगृद्धपिच्छ-मुनिपस्य बलाकपिच्छ:
शिष्योऽजनिऽष्टभुवनत्रयत्तिकोतिः।
चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-मौलि-
माला-शिलीमुख-विराजितपादपनः।।
एवं महाचार्यपरम्परायां स्यात्कारमुद्राङ्किततत्वदोपः।
भद्रस्समन्ताद्गुणतो गणीशस्समन्तभद्रोऽजनि वादिसिंहः।।"
इन पद्योंसे विदित है कि समन्तभद्र कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छाचार्य आदि महान् आचार्योंकी परम्रामें हुए थे।
सेनगणकी पट्टावलीमें समन्तभद्रको सेनगणका आचार्य सूचित किया है। यद्यपि इस पट्टावलीमें आचार्योंकी क्रमबद्ध परम्परा अंकित नहीं की गयी है, तो भी इतना स्पष्ट है कि समन्तभद्रको उसमें सेनगणका आचार्य परिगणित किया है।
श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं. १०८ में नन्दिसेन आदि चार प्रकारके संघ भेदका भट्टाकलंकदेवके स्वर्गारोहणके पश्चात् उल्लेख है। परन्तु समन्तभद्र अकलंकदेवसे बहुत पहले हो चुके हैं। अकलंकदेवसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके गणोंका कोई उल्लेख भी दिखलाई नहीं पड़ता है। यद्यपि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार एवं अभिलेख नं. १०५में इन चारों संघोका प्रवर्तक अर्हदबलि आचार्यको लिखा है। पर श्रुतावतार अकलंकदेवसे पश्चात्ययर्ती रचना है।
तिरूमकूडल नरसिपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं. १०५में समन्तभद्रको द्रमिल संघके अन्तर्गत नन्दिसंघकी अरूंगल शाखाका विद्वान सूचित किया है।
अतः यह निश्चयपूर्वक कह सकना कठिन है कि समन्तभद्र अमुक गण या संघके थे। इतना तथ्य है कि समन्तभद्र गृद्धविच्छाचार्यके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' मंगलस्तोत्रमें स्तुत आप्तके मीमांसक होनेसे वे उनके तथा कुन्दकुन्दके अन्वयमें हुये है।
आचार्य समन्तभद्रके समयके सम्बन्धमें विद्धानोंने पर्याप्त उहापोह किया है। मि. लेविस राईसका अनुमान है कि समन्तभद्र ई. की प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें हुए हैं।
"कर्नाटक पानीले नामक ग्रंथके रचयिता आर नरसिंहाचार्यने समन्तभद्रका समय शक संवत् ६० (ई. सन् १३८) के लगभग माना है। उनके प्रमाण भी राईसके समान ही हैं।
श्रीयुत् एम. एस. रामस्वामी आयंगरने अपनी 'Studies in South Indian Jainism' नामक पुस्तक में लिखा है- "समन्तभद्र उन प्रख्यात दिगम्बर लेखकोंकी श्रेणीमें सबसे प्रथम थे, जिन्होंने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें महान् प्राधान्य प्राप्त किया।"
मध्यकालीन भारतीय न्यायके इतिहास (हिस्ट्री ऑफ दी मिडिझायल स्कूल ऑफ इण्डियन लाजिक) में डॉ. सतीशचन्द्र विद्याभूषणने यह अनुमान प्रकट किया है कि समन्तभद्र ई. सन् ६००के लगभग हुए हैं। उन्होंने अपने इस कथनके लिए कोई तर्क नहीं दिया। केवल इतना ही बतलाया है कि बौद्ध तार्किक धर्मकीर्तीका समकालीन कुमारिलभट्ट है और इनका समय ई. सन् सातवीं शताब्दी है। कुमारिलने समन्तभद्रका निर्देश किया है। अतः कुमारिलके पूर्व समन्तभद्रका समय मानना उचित है।
सिद्धसेनने अपने न्यायावतारमें समन्तभद्रके रत्नकरण्डकश्रावकाचारका निम्नलिखित पद्य उद्धत्त किया है.-
"आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमदृष्टेष्टविरोधकम्।
तत्त्वोपदेशकृतसाचं शास्त्रं कापथपट्टनम्॥"
इस पद्यको लेकर विवाद है। पंडिस सुखलालजीका मत है कि यह न्याया वतारका मुल पद्म है। वहींसे यह रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें गया है। पर विचार करनेसे यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। यतः रत्नकरण्डनावकाचारमें जिस स्थान पर यह पद्य आया है वहाँ वह क्रमबद्धरूपमें नियोजित है। समन्तभद्रने सम्यग्दर्शनकी परिभाषा हुये आप्त आजमगाम जोरजोतने सानो सम्यादर्शन कहा है। इस प्रसंगमें उन्होंने सर्व प्रथम आप्तका स्वरूप बतलाया है और तत्पश्चात् आगमका। शास्त्रका स्वरूप बतलाते हुए उक्तं पद्य लिखा है। इसके अनन्तर तपोभृतक स्वरूप बतलाया है। अतः क्रमबद्धताको देखते हुए उक्त पद्यका उद्भवस्थान समन्तभद्रका रत्नकरण्डश्रावकाचार है। वह अन्यत्र से उद्धूत नहीं है। परन्तु यह स्थिति न्यायावतारमें नहीं है। न्यायावतारमें स्वार्थानुमानका लक्षणनिरूपणके पश्चात् शाब्द- आगम प्रमाणका कथन करने के लिए एक पद्य, जिसमें शाब्दका पूरा लक्षण आ गया है, निबद्ध कर इस पद्यको उपस्थित किया है, जिसे वहाँसे अलग कर देनेपर ग्रन्थका भङ्ग भी नहीं होता। परन्तु रत्नकरण्डवावकाचारमें से उसे हटा देने पर ग्रंथ भङ्ग हो जाता है। अत: इस पद्यको न्यायाक्तारमें मूल ग्रन्थरचयिताका नहीं माना जा सकता है। न्यायावतारमें शब्दप्रमाणका लक्षण निम्न प्रकार है-
दुष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्परमार्थाभिधायिनः।
तत्वग्राहितयोत्पन्नं मान शाब्दं प्रकीतितम्।।
इस पद्मके पश्चात् ही उक्त आप्तोपज्ञ' आदि पद्य दिया है, जो व्यर्थ, पुनरूक्त और अनावश्यक है। आचार्य श्री जुगलकिशोरने अपने 'स्वामी समन्तभद्र' शीर्षक प्रबन्धमें विस्तारसे इसपर विचार किया है। अतएव न्यायावतारमें उल्लिखित उक्त पद्मके आधार पर समन्तभद्रको उसके कर्ता सिद्धसेनसे उत्तरवर्ती बतलाना समुचित नहीं है।
स्वामी समन्तभद्रके समयपर विचार करनेवाले जैन विचारकोंमें दो विचार धाराएँ उपलब्ध हैं। प्रथम विचारधाराके प्रवर्तक पंडित नाथरामजी प्रेमी हैं और उसके समर्थक डॉ. हीरालालजी आदि हैं। प्रेमीजीने स्वामी समन्तभद्रका समय छठी शताब्दी माना है। उनका तर्क है कि 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' मंगलाचरण सूत्रकार उमास्वामीका न होकर सर्वार्थसिद्धिटीकाकार देवनन्दि-पूज्यपादका है और इसी मंगलाचरणके आधार पर स्वामी समन्तभद्रने 'आप्तमीमांसा' नामक ग्रन्थकी रचना की है। अतएव इनका समय देवनन्दि पूज्यपाद (ई. ५वीं शती) के अनन्तर होना चाहिये। प्रेमीजीके इस मतका समर्थन कुछ मिन्न युक्तियों द्वारा आचार्य श्रीसुखलालजी संघवी एवं डॉ. महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य भी किया है। पति सुखलालमोने समन्तभद्रपर प्रसिद्ध बौद्ध तार्किक धर्मकीर्तीका प्रभाव अनुमित कर उनका समय धर्मकीर्तीके उपरान्त बतलाया है। पं. महेन्द्रकुमारजीने 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' मंगलाचरणको देवनन्दि-पूज्यपादका सिद्ध कर उसपर आप्तमीमांसा लिखनेवाले समन्तभद्रका समय उनके बाद अर्थात् छठी शताब्दी माना है।
किन्तु उल्लेखनीय है कि जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ९, किरण १ में 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ शीर्षकसे जो उन्होंने निबन्ध लिखा था और जिसके आधार पर आचार्य समन्तभद्रका उक्त छठी शताब्दी समय निर्धारित किया था, जिसका उल्लेख न्यायकुमुदचन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें किया था, उसपर डॉ. दरबारीलालजी काठियाने 'तत्वार्थसूत्रका मंगलाचरण' शर्षिक दो विस्तृत निबन्धों द्वारा 'अनेकान्त' वर्ष ५, किरण ६,७ तथा १०,११ में गहरा विचार करके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' मंगलस्तोत्रको तत्वार्थसूत्रकार आचार्य गृद्धपिच्छका सिद्ध किया है। फलतः डॉ. महेन्द्रकुमारजीने अपने पुराने विचारमें परिवर्तन कर समन्तभद्रका समय ‘सिद्धिविनिश्चयटीकाकी’ प्रस्तावना एवं 'जैन दर्शन' ग्रन्थोंमें ई. सन् द्वितीय शताब्दी स्वीकार कर लिया है, जो आचार्य मुख्तार आदि विद्वानोंकी दृढ़ मान्यता है।
आचार्य श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने समन्तभद्रके साहित्यका गम्भीर आलोचन कर उनका समय विक्रमकी द्वितीय शती माना है। इनके इस मतका समर्थन डॉ. ज्योति प्रसाद जैनने अनेक युक्तियोस किया है। उन्होंने लिखा है-स्वामी समन्तभद्रका समय १२०-१८५ ई. निर्णित होता है और यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म पूर्वतटवर्ती नागराज्य संघके अन्तर्गत उरगपूर (वर्तमान त्रिचनापल्ली)के नागवंशी चोल नरेश कीलिकवर्मनके कनिष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी सर्ववर्मन (शेषनाग) के अनुज राजकुमार शांतिवर्मनके रूपमें सम्भवतया ई. सन् १२०के लगभग हुआ था, सन् १३८ ई. (पट्टावलि प्रसत्त शक सं.६०)में उन्होंने मुनिदीक्षा ली और १८५ ई. के लगभग वे स्वर्गस्थ हुए प्रतीत होते हैं। अतएव समन्तभद्रका समय अनेक प्रमाणोंके आधार पर ईस्वी सनकी द्वितीय शती अवगत होती है।
इनके चित्रालंकार सम्बन्धी स्तुतिविद्याके आधार पर जो यह कहा जाता है कि समन्तभद्र अलंकृत काव्ययुगके कवि है और इनका समय भारनिके आस-पास मानना चाहिये। यह तर्क भी अधिक सबल नहीं है। एकाक्षरी या द्वयक्षरी या अन्य चित्रकाव्योंकी परम्परा वैदिक कालसे ही यत्त्किचित रूपमें प्राप्त होने लगती है। दक्षिण भारत में चित्रकाव्योंकी परम्परा बहुत प्राचीन समयसे चली जा रही है। समन्तभद्गने चित्रकाव्यका प्रयोग उसी परम्पराके आधारपर किया है। अत: उसके आधापर पर उनका समय अर्वाचीन बतलाना युक्त नहीं है। अतएव संक्षेपमें समन्तभद्रका समय ई. सन् द्वितीय शताब्दी है और ‘मोक्ष मार्गस्य नेतारं' को आचार्य विद्यानन्दने सुत्रकार गृद्धपिच्छका ही मंगलाचरण माना है, सर्वार्थसिद्धिकार पूज्यपाद देवनन्दिका नहीं।
संस्कृत काव्यका प्रारम्भ ही स्तुति-काव्यसे हुआ है। जिसप्रकार वैदिक ऋषियोंने स्वानुभूति-जीवनकी जीवन्तधारा और सौंदर्यभावनाको स्तुति काव्यकी पटभूमिपर ही अंकित किया है, उसीप्रकार स्वामी समन्तभद्रने भी दर्शन, सिद्धान्त एवं न्यायसम्बन्धी मान्यताओंको स्तुति-काव्यके माध्यमसे अभिव्यक्त किया है। अतएव स्तुतियोंकी विभिन्न परम्परामें आद्य जैन स्तुतिकार समन्तभद्रने बौद्धिक चिन्तन और मानवजीवनको प्रोज्जवल कल्पनाको स्तुति-कायके रूपमें हो मूर्तिमत्ता प्रदान की है। इनके द्वारा रचित स्तुतियों में तरल भावनाओंके साथ मस्तिष्कका चिन्तनभी समवेत है। समन्तमद्र द्वारा लिखित निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती हैं-
१. बृहत् स्वम्भूस्तोत्र
२. स्तुतिविद्या-जिनशतक
३. देवागमस्तोत्र-आसमीमांसा
४. युक्त्यनुशासन
५. रत्नकरण्डकश्रावकाचार
६. जीवसिद्धि
७. तस्वानुशासन
८. प्राकृतव्याकरण
९. प्रमाणपदार्थ
१०. कर्मप्राभृसटीका
११. गन्धहस्तिमहाभाष्य
१. बृहत् स्वम्भूस्तोत्र- इसका अपर नाम स्वम्भूस्तोत्र अथवा चातुर्विशांती स्तोत्र भी है। इसमें ऋषभदेवसे लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरोंकी क्रमशः स्तुतियां है। इस स्तोत्रके भक्तीरसमें गम्भीर अनुभूति एवं तर्कणायुक्त चिन्तन निबद्ध है। अतः इसे सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि कहा जा सकता है। इस 'स्तोत्र’ के संस्कृत टीकाकार प्रमाचन्द्रने इसे 'नि:शेषजिनोक्तधर्म' कहा है। इसमें कुल पद्योंकी संख्या निम्न प्रकार है-
१. श्रीऋषभजिन स्तवन, पद्य ५,
२. श्रीअजितजिन स्तवन, पद्य ५,
३. श्री सम्भवज्जीन स्तवन, पद्य ५,
४. श्रीअभिनन्दनजिन स्तवन पद्य ५,
५. श्रीसुमतिजिन स्तवन पद्य ५,
६. श्रीपद्मप्रभजिन स्तवन पद्य ५,
७. श्रासुपार्श्वजिन स्तवन पद्य ५,
८. श्रीचन्द्रप्रभजिन स्तवन पद्य ५,
९. श्रीसुविधजिन स्तवन पद्य ५,
१०. श्रीशीतलजिन स्तवन पद्य ५,
११, श्रीश्रेयोजिन स्तवन पद्य ५,
१२. श्रीवासुपूज्यजिन स्तवन पद्य ५,
१३. श्रीविमल जिनस्तवन पद्य ५,
१४. श्रीअनन्तजिन स्तवन पद्य ५.
१५.श्रीधर्मजिन स्तवन पद्य ५,
१६. श्रीशान्तिजिन स्तवन पद्य ५.
१७. श्रीकुंथुजिन स्तवन पद्य ५,
१८, श्रीअरजिन स्तवन पद्य २०,
१९ श्रीमल्लिजिन स्तवन पद्य, ५,
२० श्रीमुनिसुव्रतजिन स्तवन पद्य ५,
२१. श्रीनमिजिन स्तवन पद्य ५,
२२. श्रीअरिष्टनेमिजिन स्तवन पद्य १०,
२३. श्री पाश्वजिन स्तवन पद्य ५,
२४. श्रीवीरजिन स्तवन पद्य ८ = १४३।
इस स्तोत्रमें कविने प्रबन्ध-पद्धतिके बीजोंको निहित कर इतिवृत्त सम्बन्धी अनेक तथ्योंको प्रस्तुत किया है। प्रथम तीर्थंकरको प्रजापतिके रूप में असि, मषि, कृषि,सेवा, शिल्प और वाणिज्यका उपदेष्टा कहा है। इस स्तोत्रमें आये हुए ‘निर्दय भस्मसात्कियाम’ पदसे सम्मतः आचार्यने अपनी भस्मक व्याधिका संकेत किया है तथा सम्भवनाथको स्तुतिमें सम्भवजीनको वैद्यका रूपक देकर अपनी जीवनघटनाओंकी ओर संकेत किया है। इसी प्रकार “यस्याङ्ग-लक्ष्मो परिवेश भिन्न तमस्तमोरेखि रश्मिभिन्नम् पदसे राजा शिवकोटिके शिवालयमें घटित हुई घटनाका संकेत प्राप्त होता है।
समस्तभद्रने बाद (शास्त्रार्थ) द्वारा जैन सिद्धान्तोंका प्रचार किया था। श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोंके अनुसार पाटलिपुत्र, ढक्क, मालव, कांची आदि देशोंमें उन्होंने शास्त्रार्थ कर जिनसिद्धान्तोंकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। इस ओर भी उनका संकेत "स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदाऽवलिप्ता वाकसिह-नादेविमदा वभूवुः" पद्यांशसे मिलता है।
शान्तिनाथतीर्थकरने चक्रवर्तीत्वपद प्राप्त किया था और उन्होंने षट्खण्डकी दिग्विजयकर समस्त राजाओंको करद बनाया था। उनके राज्यकालमें प्रजा अत्यन्त सुखी और समृद्ध थी। इस बातकी सूचना निम्नलिखित पद्यांशोंसे प्राप्त होती है-
"चक्रण यः शत्रु-मवरण जित्वा नृप सर्व-नरेन्द्र-चक्रम्"
"विधाय रक्षा परतः प्रजानां राजा धीरं योऽप्रतिम-प्रतापः"
मल्लिजिन आजन्म ब्रह्मचारी थे। उनकी गणना बालयतियोंमें है। इसी प्रकार अरिष्ट नेमिको भी बालयति कहा गया है। इन दोनों तीर्थकरोंके स्तवन में 'महर्षी' या 'ऋषि' शब्दके प्रयोग आये हैं, जो इन तीर्थकरोंके बालयतित्वको अभिव्क्त करते हैं।
पार्श्वनाथस्तोत्रमें तीर्थकर पाश्वनाथके मुनिजीवनमें तपश्चर्या करते समय वेरी कमठ द्वारा किये उपसर्ग तथा पद्यावती और धरणेन्द्र द्वारा उसके निवारण का वर्णन निम्नलिखित पद्योंमें किया है-
"तमाल-नीलैः सघनुस्तडिद्गुणैःप्रकीर्ण-भीमाशनि-वायु-वृष्टिभिः।
बलाहकैवरि-वशैरुपद्रुतो महामना यो न चचाल योगतः॥
बृहत्फणा-मण्डल-मण्डपेन यं स्फुर-तरित्पिड-रुचोपसर्गिणम।
जुगूह नागो धरणो धराधरं विराग-संध्या-तडिदम्बुदो यथा।"
इस प्रकार इस स्तोत्र-काव्यमें प्रबन्धात्मक बीजसूत्र सर्वत्र विद्यमान हैं।
स्तोत्रसाहित्यका निर्माता वही सफल माना जाता है, जो स्तोत्रोंके मध्यमें प्रबन्धात्मक बीजोंकी योजना करता है, इस योजनासे स्तोत्र तो बनते ही हैं, साथ ही उनमें प्रेषणीयता विशेष उत्पन्न होती है। समन्तभदाचार्यने वैदिक मन्त्रोंके समान ही प्रबन्धगर्भित स्तोत्रोंका प्रणयनकर दार्शनिक और काव्यात्मक क्षेत्रमें नये चरणचिन्ह उपस्थित किये हैं।
वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, वसन्ततिलका, रथोद्धता, पथ्यावक्त्र-अनुष्टुप, सुभद्रिका-मालतीमिश्रित, वानवासिका, वेतासीय, शिखरिणी, उदगता एवं आर्यागीति इन तेरह प्रकारके छन्दोंका प्रयोग पाया जाता है। अलंकार-योजनाकी दृष्टिसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्सरन्यास, उदाहरण, दृष्टान्त एवं अन्योक्ति प्रभृति अलंकार उल्लेख्य हैं। अतिशयोक्तिका निम्न उदाहरण ध्यातव्य है-
तव रूपस्य सौन्दर्य दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्।
द्वयक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव वहु-विस्मयः।।
यहाँ भगवान के सौन्दर्यको दो नेत्रोंसे देखने में अतृप्तिका अनुभव करते हुए इन्दने सहत्र नेत्र धारणकर भगवानके रूप-सौन्दर्यका अवलोकन कर आश्चर्य प्राप्त किया है। इस संन्दर्भमें अतिशयोक्ति हैं।
सुखाभिलाषाऽनलदाहमूच्छित मनो निजं मानमयाऽमृत्ताम्बुभिः।
व्यविध्यपस्त्वं विषदाहमोहितं यथा भिषम्मन्त्रगुणैः स्वविग्रहम्।।
जिसप्रकार वैद्य विषदाहसे मुर्चीत हुए अपने शरीरको विषापहारमन्त्रके गुणोंसे उसकी अमोघशक्तियोंसे निर्दिष एवं मुर्चा रहित कर देता है, उसीप्रकार हे शोत्तलजिन ! आपने सांसारिक सुखोंकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूछित हुए अपने आत्माको ज्ञानमय अमृतके सिञ्चनसे मूच्छारहित-शान्त किया है।
स चन्द्रमा भव्यकुमुद्धतीनां विपन्नदोषाभ्रकलखुलेपः।
व्याकोश-याङ-न्याय-मयूखमाल: पूयात्पवित्रो भगवाम्मनो मे।।
यहाँ-'भव्यकुमुदतीनां' और 'दोषाभ्र-कलखु-लेपः' में रूपककी योजना है। इन रूपकोंने भावोंको सहज ग्राह्य तो बनाया ही है, साथ ही चन्द्रप्रभ भगवानके गुणोंका प्रभाव भी दिखलाया है। भव्यकुमुदनियोंको विकसित करनेके लिए चन्द्रप्रभ चन्द्रमा है।
पद्मप्रभः पद्यपलाश-लेश्यः पद्यालयालिजितचारुमूर्ती:।
बभौ भवान् भव्य-पयोरुहाणां पद्माकराणामिव पद्यबन्धुः।।
पद्ममत्रके समान द्रव्यलेश्याके धारक हे पद्मप्रभजिन! आपको सुन्दरमूर्ति पदमालय-लक्ष्मीसे आलिङ्गित रही है और आप भव्यकमलोंको विकसित करनेके लिए उसी तरह भासमान हुए हैं, जिसप्रकार सूर्य कमलसमूहका विकास करता हुआ सुशोभित होता है।
संक्षेपमें स्तोत्रकाव्यमें एकान्ततत्वकी समीक्षापूर्वक स्पाद्वादनयसे अनेकान्तामृततत्वको स्थापना की गयी है।
२. स्तुतिविद्या
जिनशतक और जिनशतकालंकार भी इसके नाम आये हैं। इसमें चित्रकाव्य और बन्धरचनाका अपूर्व कौशल समाहित है। शतककाव्योंमें इसकी गणना की गयी है। सौ पद्योमें किसी एक विषयसे सम्बद्ध रचना लिखना असाधारण बात मानी जातो थी। प्रस्तुत जिनशतकमें चौबीस तीर्थंकरोंकी चित्रबन्धोंमें स्तुति की गयी है। भावपक्ष और कलापक्ष दोनों नैतिक एवं धार्मिक उपदेशके उपस्कारक बनकर आये हैं। समन्तभद्रकी काव्यकला इस स्तोत्रमें आद्यन्त व्याप्त है। मुरजादि चक्रबन्धकी रचनाके कारण चित्र काव्यका उत्कर्ष इस स्तोत्रकाव्यमें पूर्णतया वर्तमान है।
समन्तभद्रकी इस कृतिसे स्पष्ट है कि चित्रकाव्यका विकास माघोत्तरकाल में नहीं हुआ, बल्कि माघ कविसे कई सौ वर्ष पूर्व हो चुका है। चित्र, श्लेष और यमकका समावेश वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता है, अत: यह सम्भव है कि दाक्षिणत्य भाषाओंके विशिष्ट सम्पर्कके कारण समन्तभद्रने चित्र-श्लेष और यमकका पर्याप्त विकास कर उक्त काव्यकी रचना की। इस कृतिमें मुरजबन्ध, अर्धभ्रम, गतप्रत्यागतार्घ, चक्रबन्ध, अनुलोम, प्रतिलोम क्रम एवं सर्वतोभद्र आदि चित्रोंका प्रयोग आया है। एकाक्षर पद्योंको सुन्दरता कलाकी दक्षिसे अत्यन्त प्रशंसनीय है।
कुछ विद्वानोंका इस कृतिको देखकर यह अनुमान है कि जिस कृत्रिम शैलीमें समन्तभद्रने स्तुतिविद्याका प्रमयन किया है वह कृत्रिम शैली ई. सनकी चौथी शताब्दीसे विकसित होती है। अत: कृत्रिम शैलीके कारण यह कृति द्वितीय-तृतीय शतीकी रचना नहीं हो सकती। विचार करनेपर उक्त मत निभ्रन्ति प्रतीत नहीं होता, यतः कृत्रिम शैलीके विकासका मूल कारण आर्यभाषाके साथ द्रविड भाषाका सम्पर्क है। द्राविड़-परिवारकी भाषाओंमें चित्र, श्लेष और चमकको अधिक क्षमता है। अत: समन्तभद्रने दाक्षिणात्य होनेके कारण ही इस शैलीका प्रयोग किया है।
इस स्तोत्रमें कुल ११६ पद्य हैं और अन्तिम पद्यमें "कविकाव्यनामगर्म- चक्रवृत्तम" है। जिसके बाहरके षष्ट वलयमें 'शान्तिवर्मकृतम्' और चतुर्थ वलयमें 'जिनस्तुतिशतम्' की उपलब्धि होती है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकका एक साथ प्रयोग काव्यकलाकी दृष्टिसे श्लाघनीय है। यहाँ उदाहरणार्थ काव्यलिंगको प्रस्तुत किया जा रहा है-
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यच्र्चनं चापि ते
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षि संप्रेक्षते।
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरा नतिपरं सेवेव्दशी येन ते
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृतो तेनैव तेजःपते॥
जिनेन्द्र भगवानकी आराधना करनेवाले मनुष्यकी आत्मा आत्मीय तेजसे जगमगा उठती है। वह सर्वोत्कृष्ट पुरुष गिना आने लगता है। तथा उसके महान पुण्यका बन्ध होता है। यहाँ स्मरण, पूजन, अञ्जलि-बन्धन, कथा-श्रवण, दर्शन आदिका क्रमशः नियोजन होनेसे परिसंख्या-अलंकार है। आचार्यने हेतु-वाक्यों का प्रयोग कर काव्यलिंगकी भी योजना की है। इस प्रकार यह स्तुति-विद्या स्तोत्र-काव्य और दर्शनगुणोंसे युक्त है। और है सविवेक भकि-रचना।
३. आप्तमीमांसा या देवागमस्तोत्र
स्तोत्रके रूपमें तर्क और आगमपरम्पराकी कसौटीपर आप्त-सर्वज्ञदेवकी मीमांसा की गयी है। समन्तभद्र अन्धश्रदालु नहीं हैं, वे श्रद्धाको तर्ककी कसौटीपर कसकर युक्ति-आगमद्वारा आप्तकी विवेचना करते हैं। आप्त विषयक मूल्यांकनमें सर्वज्ञाभाववादी मीमांसक, भावैकान्तवादी सांख्य, एकान्तपर्यायवादी बौद्ध एवं सर्वथा उभयवादी वैशेषिकका तर्कपूर्वक विवेचन करते हए निराकरण किया गया है। प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्साभावका सप्तभंगीन्यायद्वारा समर्थन कर वीरशासनकी महत्ता प्रतिपादित की है। सर्वथा अद्वैतवाद, द्वैतवाद, कर्मद्वैत, फलद्वैत, लोकद्वैत प्रभृतिका निरसन कर अनेकान्तात्मकता सिद्ध की गयी है। इसमें अनेकान्तवादका स्वस्थ स्वरूप विद्यमान है। उदाहरणके लिए-
"द्रव्यपर्यायोरेक्यं तयोरव्यतिरेकतः।
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावत:॥
संज्ञासंख्याविशेषाच्च स्वलक्षनविशेषतः।
प्रयोजनादिभेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा॥"
द्रख्य और पर्याय कथंचित् एक हैं, क्योंकि वे भिन्न उपलब्ध नहीं होते तथा वे कथंचित् अनेक हैं क्योंकि परिणाम, संज्ञा, संख्या, आदिका भेद है। देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदिको सिद्धि अनेकान्तके द्वारा हि होती है। एकान्त वादियोंको समस्त तपस्याओंका अनेकान्तवदके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
इस स्तोत्रमें ११५ पद्य हैं। 'देवागम' पदद्वारा स्तोत्रका आरम्भ होनेके कारण यह 'देवागम' स्तोत्र भी कहा जाता है। समन्तभद्रकी परीक्षाप्रधान दृष्टि इस स्तोत्रकाव्य में समाहित है। कवित्वकी दृष्टिसे यह काव्य बोझिल है। काव्य रस-दर्शनकी चट्टानके भीतर प्रवेश करनेपर ही क्वचित् प्राप्त होता है, अप्रस्तुत विधानका भी अभाव है। जीवन और जगतकी विभिन्न समस्याओंका समाधान इस स्तोत्रकाव्यमें अवश्य वर्तमान है।
४. युक्त्यनुशसन- वीरके सर्वोदय तीर्थका महत्व प्रतिपादित करने के लिए उनकी स्तुति की गयी है। युक्तिपूर्णक महावीरके शासनका मण्डन और विरुद्धमतोंका खण्डन किया गया है। समस्त जिनशासनको केवल १४ पद्योंमें ही समाविष्ट कर दिया है| अर्थगौरवकी दृष्टिसे यह काव्य उत्तम है, 'गागरमें सागर'को भर देनेकी कहावत चरितार्थ होती है। महावीरके तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा है-
"सर्वान्तवत्तद् गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मियोऽनपेक्षम्।
सर्वापदामन्तकरं निरन्सं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव॥"
इसप्रकार महावीरके तीर्थको ही समस्त विपत्तियोंका अन्त करनेवाला सर्वोदय तीर्थ कहा है।
५. रतनकरण्यश्रावकाचार- जीवन और आचारकी व्याख्या इस ग्रंथमें की गयी है। १५० पद्योंमें विस्तारपूर्वक सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक चारित्रका विवेचन करते हुए कुन्दकुन्दके निर्देशानुसार सल्लेखनाको श्रावकके व्रतोंमें स्थान दिया है। अन्तमें श्रावककी एकादश प्रतिमाएँ वर्णित है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवालने समोचीन धर्मशास्त्र- रत्नकरण्डश्रावकाधारको भूमिकामें लिखा है- "स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न केवल जैनमार्गको सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न किया है। (जैन वत्म समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तात् मुहः), किन्तु शुद्धमानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यको नैतिक धरातलपर प्रतिष्ठित करनेके लिए बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके इस दृष्टिकोणमें मानव-मात्रकी रुचि हो सकती है। समन्तभद्रकी दृष्टिमें मनकी साधना हृदयका परिवर्तन सच्ची साधना है। बाह्य आचार तो आडम्बरोंसे भरे भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना है कि मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है (कारिका-३३) किसीने चाहे चाण्डाल योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु यदि उसमें सम्यक् दर्शनका उदय हो गया है तो देवता ऐसे व्यक्तिको देव समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढंके हुए किन्तु अन्तरमें दहकते हुए अंगारकी तरह होता है।"
इस ग्रंथकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-
१. श्रावकके अष्टमूलगुणोंका विवेचन
२. अर्हतपूजनका वैयावृत्यके अन्तर्गत स्थान
३. व्रतोंमें प्रसिद्धि पानेवालोंके नामोल्लेख
४. मोही मुनिको अपेक्षा निर्मोही श्रावककी श्रेष्ठता
५. सम्यकदर्शनसम्पन्न मातंगको देवतुल्य कहकर उदार दृष्टिकोणका उपन्यास।
६.कुन्दकुन्द और उमास्वामीको श्रावकधर्म सम्बन्धी मान्यताओंको आत्मसातकर स्वतन्त्र रूपमें श्रावकधर्मसम्बन्धी ग्रंथका प्रणयन।
इस कृतिमें कर्ताके रूपमी सुमन्त्भद्रका कही भी उपलब्ध नहीं है। टीकाकार प्रभाचन्द्रने इसे समन्तभद्रकृत लिखा है। अत: डाॅ. हीरालाल जैन आप्तमीमांसामें निरूपित आप्तके लक्षणकी शैलीकी अपेक्षा इसकी शैलीमें भिन्नता प्राप्तकर और पार्श्वनाथचरितकी उत्थानिकामें योगीन्द्रकी रचनाके निर्देशको पाकर इसे योगीन्द्रदेवकी रचना मानते हैं। ग्रंथके उपान्त्य श्लोकमें 'बौतकलड’, विद्या' और 'सर्वार्थसिद्धि' शब्दोंको तत्तद् आचार्य और ग्रन्थोंका सूचक मानकर आठवीं-ग्यारहवीं शतीके मध्यकी रचना इसे स्वीकार करते हैं।
अतः डॉ. जैनके मतानुसार यह कृति आप्तमीमांसाके रचयिता स्वामी समन्तभद्रकी नहीं है। भले ही कोई दूसरा समन्तभद्र इसका रचयिता रहा हो। डॉ. साहबने उक्त मन्तव्यको प्रकट करनेके लिए एक निबन्ध अनेकान्त, वर्ष ८, किरण १-३. पृ. २६-३३, ८६-९० और १२५-१३२ में लिखा था, जिसका प्रतिवाद डॉ. प्रो. दरबारीलाल कोठियाने अनेकान्त वर्ष ८ किरण ४-५ में किया है। डॉ. कोठियाने डॉ. जैनके तर्कोका उत्तर देते हुए प्रस्तुत कृतिको आचार्य समन्तभद्रकी ही रचना सिद्ध किया है। मैं इस विवादमें न पड़कर इतना अवश्य कहूँगा कि समन्तभद्रके अन्य ग्रंथोंके समान इस ग्रन्थके भी दो नाम उपलब्ध हैं- १. समीचोन धर्मशास्त्र ओर २. वर्ण्य विषयके अनुसार रत्नकरण्डकश्रावकाचार। स्वामी समन्तभद्रकी यह शेली है कि वे अपने प्रत्येक ग्रन्थके दो नाम रखते हैं. प्रथम नामका निर्देश प्रथम पद्यके प्रारम्भिक वाक्यमें कर देते हैं और दूसरेका निर्देश ग्रंथके वर्ण्य विषयके आधारपर रहता है।
यह निर्विवाद सत्य है कि इस ग्रन्थमें प्रतिपादित विषय बहुत प्राचीन है। श्रुतधर कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुड, प्रवचनसार, दर्शनपाहुड, सीलपाहुड आदिसे विषयको सूत्ररूपमें ग्रहणकर नये रूपमें श्रावकाचारसम्बन्धी सिद्धान्तोंका प्रणयन किया है। अत: विद्वानोंके मध्य मूलगुणसम्बन्धी जो प्रश्न उठाया जाता है उसका समाधान यहाँ सम्भव है। जब समन्तभद्रने श्रावकाचारका प्रणयन नये रूपमें किया, तो उन्होंने बहुत्त-सी ऐसी बातोंको भी इस ग्रंथमें स्थान दिया, जो पहलेसे प्रचलित नहीं थीं। हमारा तो दृढ़ मत है कि तृतीय अध्याय की यह ६६ वीं कारिका प्रक्षिप्त है। पोछेके किसी विद्वान्ने प्रतिलिपि करते समय अहिंसाणुव्रतके विशुद्धयर्थ इस कारिकाको जोड़ दिया है। यहाँसे इसे हटा देनेपर भी ग्रंथके वर्ण्य विषयमें किसीप्रकारकी कमी नहीं आती। यह कारिका एक प्रकारसे विषयका पुनरुक्तीकरण ही करती है। मद्य, मांस, मधु के त्याग तथा पंचाणुव्रतोंके पालनको अष्टमूलगुण कहा गया है। अहिंसाणुव्रत के लक्षणमें संस्कारपूर्वक मन-वचन-काय, कृत, कारित, अनुमोदनारूप व्यापारसे द्वीन्द्रियादि प्राणियोंका घात न करना अहिंसाणुव्रत है। इस परिभाषाके अन्तर्गत मद्य, मांस, मधुका त्याग स्वयमेव समाविष्ट हो जाता है। पंचाणुव्रतोंकी चर्चा तो स्पष्टरूपसे पुनरुक्त है ही। अतएव वर्ण्य-विषयकी दृष्टिसे इस पद्यकी कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि आचार्य समन्तभन्द्रको अष्टमूलगुणोंका निर्देश करना अभीष्ट होता, तो वे इस पद्यको अहिंसाणुव्रतके लक्षणके आस-पास निबद्ध करते। अहिंसादि व्रतोंका पालन करनेवाले व्यक्तियोंके नामोल्लेखके पश्चात इस कारिकाका संयोजन अनुपयोगी जैसा प्रतीत होता है। यदि यह तर्क दिया जाय कि अणुव्रतोंका वर्णन करनेके पश्चात् मूलगुणोंका निर्देश आवश्यक था, तो यह तर्क भी बहुत सबल नहीं है। अणुव्रत और गुणव्रतोंके बीच इस पद्यका स्थान नहीं होना चाहिए। अतएव हमारी दृष्टिसे यह पद्य प्रक्षिप्त है।
अनेक आचार्योंने बताया है कि कोई नदी और समुद्रके स्नानको धर्म समझता है, कोई मिट्टी और पत्थरके स्तूपाकार ढेर बनाकर धर्मको इतिश्री मानता है। कोई पहाडसे कूदकर प्राणान्त कर लेने अथवा अग्निमें शरीरको जला देने में ही कल्याण मानता है । ये सब बातें लोकमूढ़ता है-
"आपगा-सागर-स्नानमुच्चयः सिकताऽश्मनाम्।
गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते।।"
उपयुक्त पद्यमें गतानुगतिक रूपसे अनुसरण किये जानेवाले मूढ़तापूर्ण दृष्टिकोणोंका विवेचन किया है और (१) आपगासागरस्नान, (२) सिकताऽ श्मनामुच्चयः, (३) गिरिपात, (४) अग्निपातको लोकमूढ़ता कहा है। भारतीय संस्कृतिके विकासक्रमका विचार करनेसे अवगत होता है कि उक्त ये चारों प्रथाएँ ई. सन्के पूर्व अत्यधिक रूपमें प्रचलित थीं। उत्तरकालमें इन प्रथाओंमेंसे एक-दोको छोड़कर शेष सभीका लोप हो गया। ऋग्वेदकालमें जीवन तथा जीवन भोगोंके प्रति आसक्तिकी प्रवृत्ति वर्तमान थी। अत: इस युगमें संन्यास और आत्मबलका निर्देश नहीं मिलता। प्रो. हिलब्रैटने दीक्षाविधिमें प्रयुक्त होनेवाले अग्निपातसे अग्निपात द्वारा आत्मबलिका अनुमान किया है। शतपथब्राह्मणमें बताया गया है कि पुरुषमेध गवं सर्वमेध्यत्रमें समस्त सम्पत्तिका त्याग कर साधक मृत्युका वरण करने के लिए बन जाता है। परिव्राजककी क्रियाओंका विवेचन करते हुए जाबालोपनिषदमें विभिन्न रूपोंमें किये जानेवाले आत्मघातोंको धार्मिक रूप दिया गया है-
'वीराध्वाने वा अनाशके वा अपां प्रवेशे बा अग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा।'
स्पष्ट है कि अग्निपात, जलपात और अनशनव्रतद्वारा आत्महत्या करना धार्मिक विधानमें शामिल किया गया है।
हिन्दी विश्वकोषमें आत्मघातोंका निरूपण करते हुए लिखा है कि वैध, अवैध, ज्ञानकृत और अज्ञानकृत ये चार भेद आत्मघातफे हैं। मनु एवं वृद्धगर्गने लिखा है कि जब मनुष्य अत्यन्त वृद्ध हो जाये और चिकित्सा करानेपर भी आरोग्यकी सम्भावना न हो, तो शौचादिक्रियाओंके लुप्त होने की आशंका उत्पन्न होनेसे, उच्च स्थानसे गिरकर, अग्निमें कूदकर, अनशनसे रहकर या जलमें डूबकर प्राण छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्राण छोडनेपर त्रिरात्रका अशौच माना जाता है।
उपर्युक्त सन्दर्भाशसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र द्वारा विवेचित लोक-मूढ़ताएं ब्राह्मण और उपनिषद् काल में प्रचलित थीं। धर्मशास्त्रोंके अशौच प्रकरणमें इन मान्यताओंका समावेश पाया जाता है।
'आपगासागरस्नान' की सांस्कृतिक व्याख्यामें प्रवेश करने पर ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ोंके प्राप्त भग्नवशेषोंमें उपलब्ध हुए स्नानागारोंसे हड़प्पाके सांस्कृतिक जीवनमें जलकी महत्ताका परिचय मिलता है। विद्वानोंने बताया है कि इसका आर्योंके सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। सरोवरों, नदियों और समुद्रोंके जलमें स्नान करनेकी प्रथा तथा सूर्योदयके पूर्व और भोजनके पूर्व स्नान करनेकी विधिपर धार्मिक मोहर इस बातका प्रमाण है कि सिन्धु घाटीकी सभ्यतामें भी स्नानको सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त था। आर्योंके जीवनमें नदियोंका नित्य बहता हुआ निर्मल जल ही उनके लिए स्वर्गकी पवित्रता एवं पावनताका परिचायक था। सिन्धु, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपासा, शत्तद्रु, यमुना, गंगा एवं ब्रह्मापुत्र आदि नदियोंने धार्मिक प्रेरणाके कारण ही आर्योंके जीवनको उर्वर बनाया था। अतएव नदियोंमें स्नान करनेको पवित्र भावनाके साथ उनमें डूबकर आत्मघात करनेकी प्रथा भी धर्मके नामपर ब्राह्मणकालमें प्रचलित थी। जलमात्रमें स्नान करना या असमर्थ अवस्थामें डूबकर प्राणघात करना धार्मिकताका चिह्न था । ई. पूर्व द्वितीय-तृतीय शताब्दीसे लेकर ई. सन प्रथम-द्वितीय शताब्दी तक इस प्रथाका बहुत प्रचार रहा है। जब संन्यासविधि पूर्णतया विकसित हो गयी, और आत्मशोधनके लिए ध्यान, संयमका मूल्य बढ़ गया, तो उक प्रथाका शनैः-शनैः ह्रास होने लगा। स्वामी समन्तभद्रके समय में इस प्रथाका जोर-शोरके साथ प्रचार था। अतः उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें इसकी समीक्षा की है। यहाँ यह स्मरणीय है कि लोक मूढ़ताओंका रूप समयानुसार बदलता रहता है।
धर्मके नामपर स्तूप निर्माणको प्रथाका आरम्भ बौद्धकालसे हुआ है बुद्धके अस्थि-अवशेषको स्तूपके भीतर रखा जाता था और इन स्तूपोंकी धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करनेके लिए पूजा की जाती थी। सम्राट अशोकने तथा उसके उत्तर वर्ती सम्राट् सम्प्रतिने स्तुप और अभिलेखोंका आरम्भ धार्मिक स्मृतिके साथ धर्म-प्रेरणाके लिए कराया। अशोकके नूप में सम्प्रमियरूप पोरन इस प्रकार मिश्रित हो गये हैं कि उनका पृथक्करण सहज सम्भव नहीं है। इसका प्रधान कारण यह है कि धर्म और सदाचारके सामान्य नियम इन दोनों सम्राटोंको समानरूपसे ही अभिप्रेत थे। ये स्तूप ठोस गुम्बदके आकारके होते थे और इनके ऊपर छत्र भी बनाये जाते थे। अशोक निर्मित स्तूपोंमें सांचीका स्तूप अत्यन्त प्रसिद्ध है। कुशाणकालके पूर्व बुद्धकी उपासना इन स्मारक चिन्होंमें प्रयुक्त प्रतीक रूपोंमें ही होती थी। छत्र, पांव, पुष्प, चन्द्र या चक्रके प्रतीकोंमें ही बुद्धकी स्मृति अन्तर्निहित थी। महायान सम्प्रदायके आविर्भावके पश्चात् बुद्ध-प्रतिमाओंके निर्माणकी प्रथाका आरम्भ हुआ।
जब स्तुपनिर्माणका महत्व जनसाधारणमें प्रचलित हुआ, तो स्तूपोंके प्रतिनिषिस्वरूप 'सिकताश्मनामुच्चयः'का प्रचार हुआ। बालू या कंकड़ोंका स्तूपाकार ढेर लगाकर देवकी उपासना होने लगी। यह प्रथा कुषाणकालके पूर्व तक प्रचलित रही। समन्तभद्रके समय में इसका बाहुल्य था। अतएव उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें इस प्रथाकी ओर संकेत किया है। कुषाणकालके पश्चात् कुछ ही शताब्दियोंमें मूर्तिकलाका विकास होनेसे उक्त मान्यता क्षीण हो गयी। अतएव रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें 'सिकताश्मनामुच्चयः'का जो प्रयोग आया है, वह उसको प्राचीनताका सूचक है।
गिरिपातप्रथाका निर्देश समन्तभद्रने किया है। सांस्कृतिकदृष्टिसे इस प्रथाका विकास और प्रसार ई. सन पूर्वकी शताब्दियोंसे ई. सन्की आरम्भिक शताब्दियों तक ही प्राप्त होता है। योग-क्रियाओंको सम्पादित करने में असमर्थ व्यक्ति गिरिपातद्वारा मुक्तिलाभ करता था। अतएव प्राचीन धर्मशास्त्रके लेखकोंने इस प्रथाकी समीक्षा की है। हरिभद्रकी 'समराइचकहा’ के द्वितीय भवमें भी यह प्रथा उल्लिखित है। अतः समन्तभद्रने लोकमूढ़ताका जो वर्णन किया है वह उनकी प्राचीनताका सूचक है।
समन्तभद्ने प्रथम अध्यायकी चौबीसवीं कारिकामें 'पाषण्डि-मूढ़ता' की समीक्षा की है। यह ‘पाषण्डी’ शब्द विचारणीय है। धर्मके अर्थमें इसका प्रयोग प्राचीन साहित्यमें ही उपलब्ध होता है। अशोकके अभिलेखोंके साथ आचार्य कुन्दकुन्दके समयसारमें भी इस शब्दका प्रयोग आया है। कुन्दकुन्दने लिखा है-
"पाखंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि।
चित्त वदंति मुढा लिंगमिणं मोक्खमग्गो ति।।"
"ण वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिहिमयाणि लिंगाणि।"
अशोकने भी गिरिनारके छठे अभिलेखमें 'पाषण्डि' शब्दका प्रयोग धर्म या सम्प्रदायके अर्थ में किया है। लिखा है- 'सब-पासंडापि मे पूजित विविधाय पूजाय' इससे स्पष्ट है कि 'पाषंड-मूढता' का निरूपण समन्तभद्रकी प्राचीनताका द्योतक है। आरम्भमें 'पाषंडी' शब्द पवित्रताके अर्थ में प्रचलित था, पर शनै:- शनै: इस शब्दका अर्थ अपकृर्षित होने लगा और यह आडम्बरपूर्ण जीवन व्यतीत करनेके अर्थमें प्रचलित हुआ।
जहाँ तक हमारा अध्ययन है पाँचवी, छठी शताब्दीके किसी भी साहित्यमें पाषंडीका प्रयोग धर्मके अर्थ में नहीं आया है। अतः समन्तभद्रके समयपर तो इससे प्रकाश पड़ता ही है, साथ ही रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्राचीनतापर भी प्रकाश पड़ता है।
एक अन्य विचारणीय विषय यह भी है कि मूढ़ताओंकी समीक्षा धम्मपद, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। धर्मशास्त्रके निर्माताओंने मूढ़ताओंकी समीक्षा ई. सन पूर्वसे ही आरम्भ कर दी थी। अतः समन्तभद्रको रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें इन मूढ़ताओंकी समीक्षाके लिये धम्मपदादि ग्रंथोंसे भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। समन्तभद्ने इनकी समीक्षा उसो शैलीमें की है जो शैली 'धम्मपद’ में मिलती है। अतः मूढ़ताओंके विवेचनसन्दर्भसे रत्नकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता प्राचीन समन्तभद्र ही सिद्ध होते हैं। 'धम्मपद' में बताया है-
"न नग्गचरिया न जटा न पंका नानासका थण्डिलसायिका वा।
रजोवजल्लं उककुटिकप्पधानं सोधेन्ति मच्चं अवितिण्ण कंखं।"
अर्थात् जिस पुरुषका सन्देह समाप्त नहीं हुआ है उसकी शुद्धि न नंगे रहनेसे, न जटासे, न कीचड़ लपेटनेसे, न उपवास करनेसे, न कठिन भूमि पर शयन करनेसे, न धूल लपेटनेसे और न उकडू बैठनेसे होती है।
लोक-मूढत्ताएँ विकसित होकर पांचवीं- छठी शताब्दीके साहित्यमें आडम्बरपूर्ण जीवनके विश्लेषणके रूपमें आयी हैं। अपभ्रंश साहित्यमें इन लोक-मूढ़ताओंका रूप बाह्याडम्बर या बाह्य वेशके रूप में उपस्थित है।
रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्राचीनताका एक सबल प्रमाण यह भी है कि इस ग्रन्थके कई पद्य मनुस्मृत्तिके वर्तमान संस्करणमें पाये जाते हैं। मनुस्मृतिका वर्तमान संस्करण ई. सन्की दूसरी-तीसरी शतीका है। यद्यपि यह संस्करण भी किसी प्राचीन मनुस्मृतिके आधार पर प्रस्तुत किया गया है, तो भी इसमें द्वितीय और तृतीय शतीकी अनेक रचनाओंके पद्य, वाक्यांश और पदांश उपलब्ध हैं। मनुस्मृति संग्रहग्रंथ है, इसका प्रमाण मनुस्मृतिमें भृगु द्वारा 'प्रोक्त वक्तव्यों’ का पद्यरूपमें निबद्ध करना है। श्रीपाण्डुरंग वामनकाणेने इसका संकलनकाल दूसरी शताब्दी माना है। तुलनाके लिए पद्य प्रस्तुत किये जाते हैं-
सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम।
देवा देवं विदुभंस्मगूढांगारान्तरोजसम्।।
सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिविण्णः।
पञ्चगुरुचरमशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्मः॥
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबद्धयते।
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते॥
इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यम्न चान्यथा।
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्माउँऽसंशया रुचिः॥
इदं शरणमज्ञानमिदमेव विजानताम्।
इदमन्विच्छतांस्वमिदमानन्त्यमिच्छताम्।।
अतएव विषयकी प्राचीनताकी दृष्टिसे रत्नकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता प्राचीन समन्तभद्र ही हैं। मनुस्मृति और रत्नकरण्डकश्रावकाचारके प्रकरणोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि रत्नकरण्डसे ही उक्त पद्य मनुस्मृति में संग्रहीत हैं। पद्योंमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है।
जीवसिद्धि, तत्त्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, प्रमाणपदार्थ, कर्मप्राभृतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य ये रचनाएं उपलब्ध नहीं है। अत: इनके सबन्धमें विवेचन करना संभाव नहीं। इन रचनाओंके केवल निर्देश ही जहाँ-तहाँ मिलते हैं। अतएव अब हम आचार्य समन्तभद्की काव्य-प्रतिमा एवं वैदुष्यपर प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं।
समन्तभद्र अत्यन्त प्रतिभाशाली और स्वसमय, परसमयके ज्ञाता सारस्वत हैं। इन्होंने एकान्तवादियोंका निरसन कर अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा दार्शनिक शैलीमें की है। भाव और अभावरूप विरोधी युगलधार्मोंको लेकर सप्तभंगात्मक वस्तुको सिद्ध किया है। क्रियाभेद, कारकभेद, पुण्य-पापरूप कर्मद्वैत, सुख-दुख-रूप फलद्वैत, इहलोक-परलोकरूप लोकद्वैत, विद्या-अविद्यारूप ज्ञानद्वैत और बन्ध-मोक्षरुप जीवकी शुद्धाशुद्ध अवस्थाओंका चित्रण किया गया है। बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शनोंकी मूल मान्यताओंका अध्ययन कर उनकी यथार्थ समीक्षा समन्तभद्रने की है। हम यहाँ उदाहरणके लिए वैशेषिकोंके परमाणुवादको लेते हैं। वैशेषिकोंमें कोई परमाणुओंमें पाक-अग्नि संयोग होकर द्वयणुकादि अवयवीमें क्रमशः पाक मानते हैं और कोई परमाणुओंमें किसी भी प्रकारकी विकृति न होनेसे उनमें पाक-अग्निसंयोग न मान कर केवल द्वयणुकादिमें पाक स्वीकार करते हैं। जो परमाणुओं में पाक नहीं मानते उनका कहना है कि परमाणु नित्य हैं और इसलिए वे द्वयणुकादि सभी अवस्थाओंमें एकरूप बने रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकारकी अन्यता नहीं होती, अपितु सर्वदा अनन्यता विद्यमान रहती है। इसी मान्यताको आचार्य समन्तभद्रने 'अणुओंका अनन्यतैकान्त' कहा है। इस मान्यतामें दोषोद्घाटन करते हुए बताया है कि यदि अणु द्वयणुकादि संघातदशामें भी उसी प्रकारके बने रहते हैं, जिस प्रकार वे विभागके समय है, तो वे असंहत ही रहेंगे और इस अवस्थामें अवयवीरूप पृथ्वी आदि चारों भूत भ्रान्त हो जायेंगे, जिससे अवयवीरूप कार्य भी भ्रान्त सिद्ध होगा। इस प्रकार वैशेषिकोंके अनन्यतैकान्तकी समीक्षा कर अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा की है।
समन्तभद्रकी कारिकाओंके अवलोकनसे उनका विभिन्न दर्शनोंका पाण्डित्य अभिव्यक्त होता है। प्रमाण, समायाफल, प्रमाणका निम पिच समन्तभद्रने बहुत ही सूक्ष्मतासे किया है। इन्होंने सद्-असद्वादकी तरह द्वेत अद्वैतवाद, शाश्वत-अशाश्वतवाद, वक्तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद, अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-बहिरर्थवाद, देव-पुरुषार्थवाद, पाप-पुण्यवाद और बन्ध-मोक्षकारणवादका विवेचन किया है।
डॉ. दरबारीलाल कोठियाने समन्तभद्र के उपादानोंका निर्देश करते हुए लिखा है कि उन्होंने जैनदर्शनको निम्नलिखित सिद्धान्त प्रदान किये हैं-
१. प्रमाणका स्वपराभासलक्षण
२. प्रमाणके क्रमभावि और अक्रमभावि भेदोंकी परिकल्पना
३. प्रमाणके साक्षात् और परम्परा फलोंका निरूपण
४. प्रमाणका विषय
५. नयका स्वरूप
६. हेतुका स्वरूप
७. स्याद्वादका स्वरूप
८. वाच्यका स्वरूप
९. वाचकका स्वरूप
१०. अभावका वस्तुधर्मनिरूपण एवं भावान्तरकथन
११. तत्वका अनेकान्तरूप प्रतिपादन
१२. अनेकान्तका स्वरूप
१३. अनेकान्तमें भी अनेकान्तकी योजना
१४. जैनदर्शनमें अवस्तुका स्वरूप
१५. स्यात् निपातका स्वरूप
१६. अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि
१७. युक्तियोंसे स्याद्वादकी व्यवस्था
१८. आप्तका तार्किक स्वरूप
१९. वस्तु-द्रव्य-प्रमेयका स्वरूप
काव्य-चमत्कारकी दृष्टिसे भी समन्तभद्र अपने क्षेत्रमें अद्वितीय हैं। इन्होंने चित्र और श्लेष काव्यका प्रारम्भ कर भारवि और माघके लिये काव्य-क्षेत्रका विकास किया है। कवि समन्तभद्रने अपने स्तोत्र-काव्योंमें शब्द और अर्थ इन दोनोंकी गम्भीरताका अपूर्व समन्वयं बनाये रखनेकी सफल चेष्टा की है। शब्द-संघति, अलंकार-वैचित्र्य, कल्पनासम्पत्ति एवं तार्किक प्रतिभाका समवाय एकत्र प्राप्य है। प्रबन्धकाच्य न लिखने पर भी कतिपय पद्योंमें प्रौढ़ प्रबन्धात्माकता पायी जाती है। इतिवृत्तात्मक धार्मिक तथ्योंका समावेश भी काव्य शैलीमें मनोरमरूपमें हुआ है। कविप्रतिभा और दार्शनिकताका मणि-कांचन संयोग श्लाघ्य है। उत्प्रेक्षाद्वारा आराध्य पद्मप्रभका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-
"शरीर-रश्मि-प्रसरः प्रभोस्तै बालार्क-रश्मिन्छविराऽऽलिलेप।
मराऽमराऽकोण सभा प्रभा वा शैलस्य पद्माभमणे: स्वसानुम्।।"
अर्थात् हे प्रभो ! प्रातःकालीन सूर्यकिरणोंकी छविके समान रक्तवर्णकी आभावाले आपके शरीरकी किरणोंके विस्तारने मनुष्य और देवताओंसे भरी हुई समवशरण सभाको इस प्रकार अलिप्त किया है, जैसे पद्मकान्तमणि पर्वतकी प्रभा अपने पाश्वंभागको आलिप्त करती है।
इस पद्यमें पद्मप्रभ तीर्थंकरकी रक्तवर्ण कान्ति द्वारा समवशरणसभाके व्याप्त किये जानेको उत्प्रेक्षा पद्यकान्तमणिके पर्वतकी प्रभासे की गयी है।
कवि समन्तभद्र उपमा-अलंकारके व्यवहारमें भी पटु हैं। उन्होंने भगवान् आदिनाथको अज्ञानान्धकारका विनाश करने के लिए चन्द्रमाका उपमान प्रदान किया है। कुछ पद्यों में प्रयुक्त उपमान नवीन प्रतीत होते हैं। यथा-
"येन प्रणीतं पृथु धर्म-तीर्थ ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम्।
गाङ्ग हृदं चन्दन-पड-शोतं गज-प्रवेका इव घर्मतप्ताः।।''
जिन्होंने उस महान् और ज्येष्ठ धर्मतीर्थका प्रणयन किया है, जिसका आश्रय पाकर भव्यजनं दुःख-सन्तापपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्यके सन्तापसे सन्तप्त हुए बड़े-बड़े हाथी चन्दनलेपके समान शीतल गङ्गाको प्राप्त कर सूर्यके आतापजन्य दुःखको मिटा डालते हैं।
यहाँ गंगाजलका उपमान चन्दनलेप है और धर्मतीर्थका उपमान गंगाजल है। जनका उपमान गज है। इस प्रकार इस पद्यमें संसार-आतापकी शान्तिके लिए धर्मतीर्थका सामर्थ्य विभिन्न उपमानों द्वारा दिखलाया गया है।
चन्द्रप्रभजिनकी स्तुति करते हुए उनको संसारका अद्वितीय चन्द्रमा कहा है तथा उपमा द्वारा आराध्यको रूपाकृतिका मनोरम चित्र अंकित किया है-
चन्द्रप्रभ चन्द्र-मरीचि-गौर चन्द्र द्वितीयं जगतोव कान्तम्।
वन्देऽभिवानद राहतामृषीन्द्र जिनं जित-स्वान्त-कषाय-बन्धम।
चन्द्रकिरणके समान गौरवर्णसे युक्त चन्द्रप्रभजिन जगत्में द्वितीय चन्द्रमाके समान दीप्तिमान हैं, जिन्होंने अपने अन्तःकरणके कषायबन्धनको जीत अकषायपद प्राप्त किया है और जो ऋद्विधारी मुनियोंके स्वामी तथा महात्माओं द्वारा वन्दनीय हैं।
इस पद्यमें 'चन्द्रमरीचिगौर' उपमान है, इस उपमान द्वारा चन्द्रप्रभतीर्थ करके गौरवर्ण शरीरकी आकृतिका सुन्दर अंकन किया है।
चन्द्रप्रभजिनके प्रवचनको सिंहका रूपक और एकान्तवादियोंको मदोन्मत्त गजका रूपक देकर कविने आराध्यके उपदेशकी महत्ता प्रदर्शित की है। इस प्रसंगमें रूपक-अलंकारकी योजना बहुत ही तर्कसंगत है। यथा-
"स्व-पक्ष-सोस्थित्य-मदाऽवलिप्ता वाकसिह-नादेविमदा वभूवुः।
प्रवादिनो यस्य मदार्दगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादैः।।"
जिनके प्रवचनरूप सिंहनादोंको सुनकर अपने मतकी सुस्थित्तिका घमण्ड रखनेवाले प्रवादिजन उसी प्रकार निर्मद हुए हैं, जिस प्रकार मद झरते हुए उन्मत्त हाथी केसरी- सिंहकी गर्जनाको सुनकर निर्मद हो जाते हैं।
चन्दन, चन्द्रकिरण, गंगाजल और मुक्ताओंकी हारयष्टीकी शीतलताका निषेध कर शीतलनाथ तीर्थंकरके वचनोंको आचार्य समन्तभद्रने शीतल सिद्ध किया है। प्रस्तुत सन्दर्भमै व्यतिरेक-अलंकार द्वारा उपमेयमें गुणाधिक्यका आरोप कर उपमानोंमें न्यून गुणका समावेश किया है। शीतलनाथ तीर्थंकरके सद्गुणोंका उत्कर्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुणत्व ही उत्कर्षापकर्षका आधार है। अत: तीर्थंकरकी अमृतवाणीको शीतलताका चरम साधन मानकर उपमानोंके साधारण धर्मसे आधिक्य दिखलाया गया है। वाणीमें शीतलता और माधुर्यके साथ अमृतत्व भी है, जिससे वह चन्दन, चन्द्रकिरण आदिकी अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करने की क्षमता रखती है। यथा-
"न शीतलाश्चन्दमचन्द्ररश्मयो न गाजमम्भो न च हारयष्ट्यः।
यथा मुनेस्तेऽनय! वाक्य-रश्मयःशमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चिताम्॥"
हे अनघ ! निरवद्य निर्दोष श्रीशीतलजिन ! आप जैसे प्रत्यक्षज्ञानी मुनिकी प्रशमजलसे आप्लावित वाक्यरश्मियां संसार-तापको दूर करने के हेतु उतनी शीतल हैं, जितनी न तो चन्द्रकिरणे शीतल हैं, न चन्दन है, न गङ्गाजल श्वीतल है और न मोतियोंकी हारयष्ट्रि ही। तात्पर्य यह है कि शीतलजिनकी अमृतवाणी चन्दन, चन्द्रकिरण, गङ्गाजल और मुक्ताहारष्टिसे अधिक शीतल और सुखप्रद है।
कविताका विषय हृदयकी अनुभूति है। अनुभूतिकी अवस्था में समस्त स्नायुमण्डल तदनुकूल रूप धारण करता है और उच्चरित वाक्यावलिमें अपूर्व प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। अनुभूतिके समयमें हृदयकी प्रधानत: दो अवस्थाएँ होती है। ये अवस्थाएं हैं- १. उल्लास और २. विह्वलता। कवि जब उल्लसित होता है, तो वह गाता है। यही कारण है कि स्तोत्रोंके समय में कविकी तन्मयता चरमसीमाको पहुँच जाती है। आराध्यके चरणोंमें वीतरागताकी प्राप्तिके लिए कवि अपनेको समर्पित कर देता है। भाव जहाँ उसके हृदयको उल्लसित और उद्वेलित करते हैं, वहाँ रमणीय वाक्यावलिके शब्द उसके हृदयको चमत्कारसे भर देते हैं।
चित्रकाव्यमें हृदयकी भावावस्था उतनी द्रवित नहीं होती, जितनी चमत्कारकी योजना होनेसे कोतुहल। अतएव संस्कृतकाव्यमें सर्वप्रथम चित्र, श्लेष और यमकका प्रादुर्भाव हुआ। भावावस्थामें स्थायित्व नहीं रहता है, यतः भाव क्षणभरमें उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, पर चमत्कृत्त दशा अधिक समय तक विद्यमान रहती है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियोंने भी वैदिक मन्त्रोंके प्रयोगमें शब्दरमणीयताको स्थान दिया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक प्रभृति अलंकारोंके साथ श्लेष और यमक भो उपलब्ध हैं।
स्वामी समन्तभदने स्तुतिविद्यामें हृदयको भावावस्थाको अधिक क्षणोंतक बनाये रखने के लिए शब्दोंको रम्यक्रिडाको स्थान दिया है। इसके बिना हृदयमें कौतूहलको स्थिति प्रबल अंगके साथ जागृत नहीं की जा सकती है। सवेदनाओंको शब्दोंकी रम्यताके गर्भसे प्रस्फुटितकर कौतूहल स्थिति तक पहुँचा देना है। आचार्य समन्तभद्रके चित्रबन्ध केवल शाब्दी रमणीयताका ही सृजन नहीं करते हैं, अपितु इनमें वक्रोक्ति और स्वभावोक्तियोंका चमत्कार भी निहित है।
'तकार' व्यज्जन द्वारा निम्नलिखित पद्यका गुम्फन किया है। श्लोकके प्रथमपादमें जो अक्षर हैं, वे ही सब अगले पादोंमें यत्र-तत्र व्यवस्थित हैं। साध्यरूपमें यहाँ शाब्दी क्रीडा नहीं है, अपितु साधनके रूप में है, जिससे शब्दचमत्कार "परिच्छित्ति’ की योजना द्वारा निमित हुआ है।
ततोतित्ता तु तेतीतस्तोतृतोतीतितोतुतः।
ततोतातिततोतोते ततता ते ततोततः।
हे भगवन् ! आपने ज्ञानावरणादि कर्मोको नष्ट कर केवलज्ञानादि विशेषगुणों को प्राप्त किया है, तथा आप परिग्रहहित स्वतन्त्र है। अतः आप पूज्य और सुरक्षित है। आपने ज्ञानावरणादि कर्मोके विस्तृत-अनादिकालिक सम्बन्धको नष्ट कर दिया है। अतः आपका विशालता-प्रभुता स्पष्ट है-आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं।
एक-एक व्यंजनके अक्षरक्रमसे प्रत्येक पादका ग्रंथन कर चित्रालकारकी योजना द्वारा भावाभिव्यक्ति की गयी है। यहाँ शब्दचमत्कारके साथ अर्थ चमत्कार भी प्राप्य है-
येयायायाययेयाय नानाननाननानन।
ममाममाममामामिताततीतिततोतितः।।
हे भगवन् ! आपका मोक्षमार्ग उन्हीं जीवोंको प्राप्त हो सकता है, जो कि पुण्यबन्धके सम्मुख हैं अथवा जिन्होंने पुण्यबन्ध कर लिया है। समवशरणमें आपके चार मुख दिखलाई पड़ते हैं। आप केवलज्ञानसे युक्त हैं तथा ममताभावसे-मोहपरिणामोंसे रहित है, तो भी आप सांसारिक बड़ी-बड़ी व्याधियोंको नष्ट कर देते हैं। हे प्रभो ! मेरे भी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दीजिए।
चन्द्रप्रभ और शीतलजिन स्तुति करते हुए मुजंबन्धोंकी योजनामें व्यतिरेक और श्लेष अलंकारको दिव्य आभाका मिश्रण उपलब्ध होता है-
"प्रकाशयन समुद्भूतस्त्वमुर्धाकलालयः।
विकासयन् समुद्भूतः कुमुदं कमलाप्रियः||"
हे प्रभो ! आप चन्द्ररूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा उदय होते ही आकाशको प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भी समस्त लोकाकाश और अलोकाकाशको प्रकाशित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार मुगलांछनसे युक्त है, उसी प्रकार आप भी मनोहर अर्द्धचन्द्रसे युक्त हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार सोलह कलाओंका आलय-गृह होता है, उसी तरह आप भी केवलज्ञानादि अनेक कलाओंके आलय-स्थान हैं। चन्द्रमा जिस तरह कुमुदों-नीलकुमुदोंको विकसित करता हुआ उदित होता है, उसी तरह आप भी पृथ्वीके समस्त प्रणियोंको आनन्दित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार कमलाप्रिय--कमलतृशात्रु होता है, उसी प्रकार आप भी कमलाप्रिय- केवलज्ञानादि लक्ष्मीके प्रिय है।
श्लेषके समान ही उपर्युक्त पद्यमें व्यतिरेक अलंकार भी है। इस अलंकारके प्रकाशमें चन्द्रमाकी अपेक्षा तीर्थंकर चन्द्रप्रभकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है। चन्द्रप्रभ गुणोंका उत्कर्ष और चन्द्रमामें अपकर्ष दिखलाया गया है।
श्रेयोजिनकी स्तुति में 'अर्द्धभ्रम'का प्रयोग किया है। इसमें औष्ठय वर्णोंका अभाव है, और चतुर्थ पादके समस्त अक्षरोंको अन्य तीन पादोंमें समाहित किया है-
"हरतीज्याहिता तान्ति रक्षार्थायस्य नेदिता।
तीर्थदिश्रेयसे नेताज्यायः श्रेयस्पयस्य हि॥"
कुछ ऐसे भी पद्य हैं, जिन्हें क्रमके साथ विपरीत क्रमसे भी पढ़ा जा सकता है, और विपरीत क्रमसे पढ़नेपर भिन्नार्थक पद्य ही बन जाता है। कविने स्वयं ही अनुलोम-प्रतिलोमक्रमसे श्लोकोंका प्रणयन किया है। यथा-
"रक्षमाक्षर वामेश शमी चारुरुचानुत:।
भो विमोनशनाजोरुनभ्रेन विजरामयः।।"
इसी पद्यको प्रतिलोमक्रमसे पढ़नेपर निम्नलिखित पद्य निर्मित होता है।
"यमराज विनम्रन रजोनाशन भो विभो।
तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर||"
शब्द और अर्थ चमत्कारके साथ नादानुक्रति भी विद्यमान है। विधायक कल्पना द्वारा आराध्यकी शरीराकृतिके साथ गुणोंका समवाय भी अभिव्यक्त हुआ है।
इस प्रकार आचार्य समन्तभद्रने जैनन्यायको तार्किकरूप प्रदान करनेके साथ संस्कृतकाव्यको निम्नलिखित तत्व प्रदान किये हैं-
१. चित्रालंकारका प्रारम्भ
२. श्लेष और यमकों द्वारा काव्यशैलीका उदात्तीकरण
३.शतककाव्यका सूत्रपात
४. स्तवनोंमें बाह्य चित्रणकी अपेक्षा अन्तरंग गुणों एवं अनेकान्तात्मक सिद्धान्तोंकी बहुलता
५. दर्शन और काव्यभावनाका मणि-कांचनसंयोग
आचार्य समन्तभद्रके उक्त काव्यतत्त्वोंका संस्कृतकाव्यतत्वोंपर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। जब संस्कृतकाव्यका प्रणयन मध्यदेशसे स्थानान्तरित हो गुजरात, कश्मीर और दक्षिणभारतमें प्रविष्ट हुआ, तो समन्तभद्रके काव्य सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित हो गये। भारविमें एकाएक चित्र और श्लेषका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, अपितु समन्तभद्रके काव्यसिद्धान्तोंका उनपर प्रभाव है। मलाबार निवासी वासुदेव कविने यमक और श्लेष सम्बन्धी जिन प्रसिद्ध काव्यों की रचना की है, उनके लिए वे शैलीके क्षेत्रम समन्तभद्रके ऋणी हैं। कवि कुज्जर द्वारा लिखित राघवपाण्डवीय पर भी समन्तभद्रकी शैलोका प्रभाव है। अत: संक्षेपमें दर्शन, आचार, तर्क, न्याय आदि क्षेत्रोंम प्रस्तुत किये गये ग्रंथोंकी दृष्टिसे समन्तभद्र ऐसे सारस्वताचार्य है, जिन्होंने कुन्दकुन्दादि आचार्योंके वचनोंको ग्रहण कर, सर्वज्ञकी वाणीको एक नये रूपमें प्रस्तुत किया है।
सारस्वताचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।
सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-
१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।
२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।
३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।
४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।
५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।
६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन ।
७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन ।
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्ति रश्मयः।
वज्रन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलबोद्धता जनाः'।।
समन्तभद्रादिमहाकवीश्वराः कुवादिविद्याजयलब्धकीर्तयः।
सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकाक्षिणि।।
श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुम्मरसञ्चयम्।
मुनिवन्ध जनानन्दं नमामि वचनश्रिये॥
सारस्वताचार्योंमें सबसे प्रमुख और आद्य आचार्य समन्तभद्र है। जिस प्रकार गृद्धपिच्छाचार्य संस्कृतके प्रथम सूत्रकार है, उसी प्रकार जैन वांडमयमें स्वामी समन्तभद्र प्रथम संस्कृत-कवि और प्रथम स्तुतिकार हैं। ये कवि होनेके साथ प्रकाण्ड दार्शनिक और गम्भीर चिन्तक भी हैं। इन्हें हम श्रुतधर आचार्यपरम्परा और सारस्वत आचार्यपरम्पराको जोड़नेवाली अटूट श्रृंखला कह सकते हैं। इनका व्यक्तित्व श्रुतधर आचार्यो से कम नहीं है।
स्तोत्र-काव्यका सूत्रपात आचार्य समन्तभद्रसे ही होता है। ये स्तोत्र-कवि होने के साथ ऐसे तर्ककुशल मनीषी हैं, जिनकी दार्शनिक रचनाओंपर अकलंक और विद्यानन्द जैसे उदभट आचार्यों ने टीका और विवृत्तियों लिखकर मौलिक ग्रन्थ रचयिताका यश प्राप्त किया है| वीतरागी तीर्थकरकी स्तुतियोंमें दार्शनिक मान्यताओंका समावेश करना असाधारण प्रतिभाका ही फल है।
आदिपुराणमें आचार्य जिगोनने जन्हें वापद हामिल, कवित्व और गमकत्व इन चार विशेषणोंसे युक्त बताया है। इतना ही नहीं, जिनसेनने इनको कवि-वेधा कहकर कवियोंको उत्पन्न करनेवाला विधाता भी लिखा है-
कवीनां गमकानाञ्च वादिनां वाग्मिनामपि।
यशः सामन्तभद्रीयं मूनि चूडामधीयते।।
नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ।
यद्धचोवज्जपातेन निभिन्ना: कुमतादयः।।
मैं कवि समन्तभद्रको नमस्कार करता हूँ, जो कवियोंसे ब्रह्मा हैं, और जिनके वचनरूप वज्ज्रपातसे मिथ्यामतरूपी पर्वत चूर-चूर हो जाते हैं।
स्वतन्त्र कविता करनेवाले कवि, शिष्योंको मर्मतक पहुँचानेवाले गमक, शास्त्रार्थ करनेवाले वादी और मनोहर व्याख्यान देनेवाले वाग्मियोंके मस्तक पर समन्तभद्रस्वामीका यश चुडामणिके समान आचरण करनेवाला है| वादोभसिंहने अपने 'गद्यचिन्तामणि' ग्रन्थमें समन्तभद्रस्वामीकी तार्किक प्रतिमा एवं शास्त्रार्थ करनेकी क्षमताकी सुन्दर व्यंजना को है। समन्तभद्रके समक्षा बड़े-बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका महत्व समाप्त हो जाता था और प्रतिवादी मौन होकर उनके समक्ष स्तब्ध रह जाते थे।
सरस्वतीस्वैरविहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः।
जयन्ति वाग्वनिपातपाटितप्रतीपरादान्तमहीघ्रकोटयः।।
श्रीसमन्तभद्र मुनीश्वर सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि थे। उनके वचनरूपी वज्ज्रके निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चोटियाँ चूर-चूर हो गयी थीं। उन्होंने जिनशासनकी गौरवमयी पताकाको नीले आकाशमें फहरानेका कार्य किया था। परवादी-पंचानन बर्द्धमानसूरिने समन्तभद्रको 'महाकवीश्वर' और 'सुतर्कशास्त्रामृससागर' कहकर उनसे कवित्वशक्ति प्राप्त करनेकी प्रार्थना की है-
समन्तभद्रादिमहाकवारवराः कुवादिविद्याजयलब्धकोत्तयः।
सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांक्षिणि||
श्रवणबेलगोलाके शिलालेख न. १०५ में समन्तभद्र की सुन्दर उक्तियोंको वादीरुपी हस्तियोंको वश करनेके लिए वज्राकुंश कहा गया है तथा बतलाया है कि समन्तभद्र के प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी दुर्वादोंकी वार्तासे भी रहित हो गयी थी।
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभवज्राकुशसूक्तिजालः।
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वन्ध्यास दुव्र्वादुकवार्तयापि।।
स्यात्कारमुद्रित-समस्त-पदार्थपूर्णत्रैलोक्य-हम्मखिलं स खलु व्यक्ति।
दुव्वादुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं सामन्तभद्र-वचन-स्फुटरनदीपः।।
ज्ञानार्णवके रचयिता शुभचन्द्राचार्यने समन्तभद्रको 'कबीन्द्र- भास्वान' विशेषणके साथ स्मरण करते हुये उन्हें श्रेष्ठ कवीश्वर कहा है-
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरममयः।
वज्रन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलवोद्धता जनाः।।
अजितसेनका 'अलंकारचिन्तामणि' और ब्रह्म अजितके 'हनुमच्चरित्' एवं श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं. ५४ और अभिलेख नं. १०८ में समन्तभद्रका स्मरण महाकविके रूपमें किया गया है।
इस प्रकार जैन वाडमयमें समन्तभद्र पूर्ण तेजस्वी विज्ञान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादिविजेता और कविवेधके रूपमें स्मरण किये गये हैं। जैन धर्म और जैनसिदान्तके मर्मज विद्वान होनेके साथ तर्क, व्याकरण, छन्द, अलंकार एवं काव्य-कोषादि विषयोंमे पूर्णतया निष्णात थे। अपनी अलौकिक प्रतीभा द्वारा इन्होंने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्रायः समस्त विषयोंको आत्मसात् कर लिया था। संस्कृत, प्राकृत आदि विभिन्न भाषाओंके पारंगत विद्वान थे। स्तुतिविद्याग्रंथसे इनके शब्दाधिपत्यपर पूरा प्रकाश पड़ता है।
दक्षिण भारतमें उच्च कोटिके संस्कृत-ज्ञानको प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और प्रसारण देने वालोंमें समंतभद्रका नाम उल्लेखनीय है। आप ऐसे युगसंस्थापक हैं, जिन्होंने जैन विद्याके क्षेत्रमें एक नया आलोक विकीर्ण किया है। अपने समयके प्रचलित नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद,ब्रह्माद्वैतवाद, पुरुष एवं प्रकृतिवाद आदिकी समीक्षाकर स्यादवाद-सिद्धांतको प्रतिष्ठा की है। 'अलंकारचिन्तामणि’ में 'कविकुन्जर', 'मुनिबंध' और 'जनानन्द' आदि विशेषणों द्वारा अभिहित किया गया है। श्रवणबेल्गोला के शिलालेखोमी में तो इन्हें जीनशाषण प्रणेता और भद्र मूर्ती कहा गया है। इस प्रकार वाङ्मयसे समत्तभद्रके शास्त्रीय ज्ञान और प्रभाव का परिचय प्राप्त होता है।
समत्तभद्रका जन्म दक्षिमभारतमें हुआ था। इन्हें चोल राजवंशका राजकुमार अनुमित किया जाता है। इनके पिता उरगपुर (उरैपुर) के क्षत्रिय राजा थे। यह स्थान कावेरी नदीके तटपर फणिमण्डलके अंतर्गत अत्यंत समृद्धिशाली माना गया है। श्रवणबेलगोलाके दौरवलि जिनदास शास्त्रीके भण्डारमें पायी जाने वाली आप्तमीमांसाकी प्रतिके अतमें लिखा है- "इति फणिमंडलालंकारस्योरगपुराधिपसुनोः श्रीस्वामीसमन्तभद्रमुनेः कृतो आप्तमीमांसायाम्" इस प्रशस्ति वाक्यसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र स्वामीका जन्म क्षत्रियवंशमें हुआ था और उनका जन्मस्थान उरगपुर है। 'राजावलिकथे’ में आपका जन्म उत्कलिका ग्राममें होना लिखा है, जो प्रायः उरगपुरके अंतर्गत हो रहा होगा। आचार्य जुगलकिशोर मख्तारका अनुमान है कि यह उरगपुर उरैपुरका ही संस्कृत अथवा श्रुतमधुर नाम है, चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी थी। ‘त्रिचिनापोली’ का ही प्राचीन नाम उरयूर था। यह नगर कावेरीके तटपर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा ही समृद्धशाली जनपद था।
इनका जन्म नाम शांतिवर्मा बताया जाता है। 'स्तुतिविद्या' अथवा 'जिनस्तुतिशतम्’ में, जिसका अपर नाम जिनशतक' अथवा 'जिनशतकालंकार' है, "गत्वैकस्तुतमेव'' आदि पद्य आया है। इस पद्ममें कवि और काव्यका नाम चित्रबद्धरूपमें अंकित है। इस काव्यके छह आरे और नव वलय वाली चित्ररचना परसे 'शांतिवर्मकृतम्' और 'जिनस्तुतिशतम्' ये दो पद निकलते हैं। लिखा है- "षडरं नववलयं चक्रमालिख्य सप्तमवलये शांतिवर्मकृतं इति भवति।” "चतुर्थवलये जिनस्तुतिशतं इति च भवति अतः कवि-काव्यनामगर्भ चक्रवृत्तं भवति। इससे स्पष्ट है कि आचार्य समन्तभद्रने ‘जिनस्तुतिशतम्’ का रचयिता शांतिवर्मा कहा है, जो उनका स्वयं नामांतर संभव है। यह सत्य है कि यह नाम मुनि अवस्थाका नहीं हो सकता, क्योंकि वर्मान्त नाम मुनियोके नहीं होते। संभव है कि माता-पिताके द्वारा रखा गया यह समन्तभद्रका जन्मनाम हो। 'स्तुतिविद्या' किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित न होकर समन्तभद्रकी ही कृति मानी जाती है। टीकाकार महाकवि नरसिंहने- "ताकिकचूडामणि श्रीमत् समन्तभद्राचार्यविरचित" सूचित किया है और अन्य आचार्य और विद्वानोंने भी इसे समत्तभद्रकी कृति कहा है। अतएव समन्तभद्रका जन्मनाम शांतिवर्मा रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है।
मुनि-दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात् जब ये मणुवकहल्ली स्थानमें विचरण कर रहे थे कि उन्हें भस्मक व्याधि नामक भयानक रोग हो गया, जिससे दिगम्बर मुनिपदका निर्वाह उन्हें अशक्य प्रतीत हुआ। अतएव उन्होंने गुरुसे समाधिमरण धारण करनेको अनुमति मांगी| गुरुने भविष्णु शिष्यको बादेश देते हुए कहा- "आपसे धर्म और साहित्यकी बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं, अत: आप दीक्षा छोड़कर रोग-शमनका उपाय करें। रोग दूर होनेपर पुन: दीक्षा ग्रहण कर लें"। गुरुके इस आदेशानुसार समन्तभद्र रोगोपचारके हेतु नाग्यपदको छोड़कर सन्यासी बन गये और इधर-उधर विचरण करने लगे। पश्चात वाराणसीमें शिवकोटि राजाके भीमलिंग नामक शिवालयमें जाकर राजाको आर्शीवाद दिया और शिवजीको अर्पण किये जाने वाले नैवेद्यको शिवजीको ही खिला देनेकी घोषणा की। राजा इससे प्रसन्न हुआ और उन्हें शिवजीको नैवेद्य भक्षण करानेकी अनुमति दे दी। समन्तभन्न अनुमति प्राप्त कर शिवालयके किंवाड़ बन्द कर उस नैवेद्यको स्वयं ही भक्षण कर रोगको शांत करने लगे। शनैः शनै: उनकी व्याधिका उपशम होने लगा और भोगको सामग्री बचने लगी। राजाको इसपर सन्देह हुआ। अत्तः गुप्तरूपसे उसने शिवालयके भीतर कुछ व्यक्तियों को छिपा दिया। समन्तभद्रको नेवेद्यका भक्षण करते हुए छिपे व्यक्तियोंने देख लिया। समन्तभद्रने इसे उपसर्ग समझ कर चर्तुविशति तीर्थ करोंकी स्तुति आरंभ की। राजा शिवकोटिके डरानेपर भी समन्तभद्र एकाग्रचित्तसे स्तवन करते रहे, जब ये चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति कर रहे थे कि भीमलिंग शिवकी पिण्डी विदीर्ण हो गयी और मध्यसे चन्द्रप्रभ स्वामीका मनोज्ञ स्वर्णनिम्न प्रकट हो गया। समन्तभद्रके इस महात्म्यको देखकर शिक्कोटि राजा अपने भाई शिवायन सहित आश्चर्य चकित हुआ। समन्तभद्रने वर्धमान पर्यन्त चतुर्विशशति तीर्थंकरोंकी स्तुति पूर्ण हो जानेपर राजाको आशीर्वाद दिया।
यह कथानक 'राजाबलिकथे’ में उपलब्ध है। सेनगणकी पट्टावलिसे भी इस विषयका समर्थन होता है। पट्टावलिमें भीमलिंग शिवालयमें शिवकोटि राजाके समन्तभद्र द्वारा चमत्कृत्त और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है। साथ ही उसे नवतिलिंग देशका राजा सूचित किया है, जिसकी राजधानी सम्भवतः काञ्ची रही होगी। यहाँ यह अनुमान लगाना भी अनुचित नहीं है कि सम्भवत: यह घटना काशीकी न होकर काञ्चीको है। काञ्चीको दक्षिण काशी भी कहा जाता रहा है- "नर्वातलिंगदेशाभिरामद्राक्षाभिरामभोमलिङ्गस्चयन्वादिस्तोटकोस्कोरण ? रुद्रसान्द्रचदिकाविशदयशःश्रीचन्द्रजिनेन्द्रसइर्शनसमुत्पन्नकौतू हलकलितशिवकोटिमहाराजतपोराज्यस्थापकाचार्यश्रीमत्समन्तभद्रस्वामिनाम्”
इस तथ्यका समर्थन श्रवणबेलगोलाके एक अभिलेखसे भी होता है। अभिलेख में समन्तभद्र स्वामीके भस्मक रोगका निर्देश आया है। आपत्काल समाप्त होने पर उन्होंने पुनः मुनि-दीक्षा ग्रहण की। बताया है-
"वन्द्यो भस्मक-भस्म-सात्कृति-पटुः पद्मावतीदेवता-
दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभः।
आचार्यस्स समन्तभद्रगणभृधेनेह काले कली,
जैन वत्र्म समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तान्मुहः।।"
अर्थात् जो अपने भस्मक रोगको भस्मसात् करनेमें चतुर हैं, पद्मावती नामक देवीकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपने मन्त्रवचनोंसे चन्द्रप्रभको प्रकट किया और जिनके द्वारा यह कल्णाणकारी जैन मार्ग इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुभा, वे गणनायक आचार्य समन्तभद्र बार-बार वन्दना किये जाने योग्य हैं।
यह अभिलेख शक संवत् १०२२ का है। अतः समन्तभद्रकी भस्मक व्याधि की कथा ई. सन्के १०वी, ११वीं शताब्दी में प्रचलित रही है।
ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशमें भी शिवकोटि राजाका उल्लेख है। राजाके शिवालयमें शिव-नैवेद्यसे भस्मक-व्याधिकी शान्ति और चन्द्रप्रभजिनेन्द्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बका प्रादुर्भूत होना साथ-साथ वर्णित है। यह भी बताया गया है कि शिवकोधि महाराजने जिनदीक्षा भी धारण की थी।
ब्रह्मनेमिदत्तने शिवकोटिको काञ्चो अथवा नव तैलङ्ग देशका राजा न लिखकर वाराणसीका राजा लिखा है। भारतीय इतिहासके आलोडनसे न तो काशीके शिवकोटि राजाका ही उल्लेख मिलता है और न काञ्चीके ही।
प्रा. ए. चक्रवतीने पञ्चास्तिकायकी अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें बताया है कि काञ्चीका एक पल्लवराजा शिवस्कन्ध वर्मा था, जिसने 'मायदाबोलु' का दान-पत्र लिखाया है। इस राजाका समय विष्णुगोपसे पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी है। यदि यही शिवकोटि रहा हो, तो समन्तभद्र के साथ इसका सम्बन्ध घटित हो सकता है। 'राजाबलि कथे', 'पट्टावलि, एवं श्रवणबेलगोलाके अभिलेखमें शिवकोटिका निर्देश जिस रूपमें किया गया है उस रूपके अध्ययनसे उसके अस्तित्वसे इंकार नहीं किया जा सकता है।
ब्रह्म नेमिदत्तने समन्तभद्रकी कथामें काशीका उल्लेख किया है। पर यह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। कथाके ऐसे भी कुछ अंश है जो यथार्थ नहीं मालूम होते। कथामें आया है- "काञ्चोमें उस समय भस्मक व्याधिको नाश करनेके लिए स्निग्ध भोजनोंकी सम्प्राप्तिका अभाव था। अत: वे काञ्ची छोड़कर उत्तरकी ओर चल दिये। वे पुपड़ेन्द्रनगरमें पहुंचे। यहाँ बौद्धोंकी महती दानशाला देखकर उन्होंने बौद्ध भिक्षुका रूप धारण किया। पर जब वहाँ भी महाव्याधिका उपशम नहीं हुआ तो वे वहाँसे निकलकर अनेक नगरों में घूमते हुए दशपुर नगरमें पहुंचे। यहाँ भागवतोंका उन्नत मठ देखकर वे विशिष्ट आहारप्राप्तिकी इच्छासे बौद्ध भिक्षुका वेष त्याग वैष्णव संन्यासी बन गये। यहाँके विशिष्ट आहार द्वारा भी जब उनकी भस्मक व्याधि शान्त न हुई, तो वे नाना देशोंमें घूमते हुए वाराणसी पहुंचे और वहीं उन्होंने योगि-लिङ्ग धारण करके शिवकोटि राजाके शिवालयमें प्रवेश किया। यहां घी-दूध-दही-मिष्टान्न आदि नाना प्रकारके नेवेद्य शिवके भोगके लिए तैयार किये जाते थे। समन्त भद्रने शिवकोटि राजासे निवेदन किया कि वे अपनी दिव्यशक्ति द्वारा समस्त नेवेद्यको शिवको खिला सकते हैं। राजाका आदेश प्राप्त कर समन्तभद्रने मन्दिरके कपाट बन्द कर समस्त नैवेद्य स्वयं ग्रहण किया और आचमनके पश्चात् किवाड़ खोल दिये। राजा शिवकोटिको महान आश्चर्य हआ कि मनोंकी परिमाणमें उपस्थित किया गया नैवेद्य साक्षात् शिवने ही अवतरित होकर ग्रहण किया है। योगिराजकी शक्ति अपूर्व है, अतएव उनको शिवालयका प्रधान पुरोहित नियुक्त किया। समन्तभद्र प्रतिदिन नैवेद्य प्राप्त करने लगे और शनैः शनैः उनकी मस्मक व्याधि शान्त होने लगी। मन्दिरके प्रमुख पुरोहितोंने ईर्ष्यावश समन्तभद्रकी देखरेख की और राजाको सूचना दी कि तथाकथित योगि शिवको नैवेद्य न ग्रहण कराकर स्वयं नैवेद्य ग्रहण कर लेता है। राजाके आदेशानुसार एक दिन समन्तभद्रको भोजन करते हुए पकड़ लिया गया और उनसे शिवको नमस्कार करनेके लिए कहा। समन्तभद्रने उत्तर दिया, "रागी देषी देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता है। राजाने आज्ञा दी कि अपना सामर्थ्य दिखलाकर स्ववचनको सिद्ध करो।
रात्रिमें समन्तभद्रको वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, क्योंकि प्रातःकाल ही उनको अपनी परीक्षा उत्तीर्ण होना था। उनकी चिन्ताके कारण अम्बिका देवीका आसन कम्पित हुआ और वह दौड़कर समन्तभद्र के समक्ष उपस्थित हुई और उन्हें आश्वासन दिया। प्रात:काल होनेपर अपार भीड़ एकत्र हुई और समन्तभदने अपना स्वयंभूस्तोत्र आरम्भ किया। जिस समय वे चन्द्रप्रभ भगवानको स्तुति करते हा 'तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम्' यह वाक्य पढ़ रहे थे, उसी समय वह शिवलिङ्ग खण्ड-खण्ड हो गया और उसके स्थानपर चन्द्रप्रभ भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा प्रकट हुई। राजा शिवकोटि समन्तभद्रके इस महत्वको देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने समन्तभद्रसे उनका परिचय पूछा। समन्तभद्रने उत्तर देते हुए कहा-
"काच्या नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुलम्बिशे पाण्डुपिण्डः।
पुण्ड्रेण्डे शाक्यभिक्षुर्दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिवाट्।।
वाराणस्यामभूवं शशकरधवलः पाण्डुराङ्गस्तपस्वी।
राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिग्रन्थवादी।।"
मैं काञ्ची में नग्नदिगम्बर यत्तिके रूपमें रहा, शरीरमें रोग होनेपर पुण्डनगरीमें बौद्ध भिक्षु बनकर मैंने निवास किया। पश्चात् दशपुर नगरमें मिष्टान्न भोजी परिवाजक बनकर रहा। अनन्तर वाराणसी में आकर शैव तपस्वी बना। है राजन् ! मैं जैननिर्ग्रंथवादी-स्याद्वादी हूँ। यहाँ जिसकी शक्ति वाद करनेकी हो वह मेरे सम्मुख आकर वाद करे। द्वितीय पद्यमें आया है-
पुर्ण पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठपक-विषये काञ्चीपुरे वैदिशे।
प्राप्तोऽहं करहाटक बहुभट विद्योत्कटं ससूट
वादार्थी विचराम्यहन्नरपते शाई लविक्रीडितम्।।
मैंने पहले पाटलिपुत्र नगरमें वादकी भेरी बजाई। पुनः मालवा, सिन्ध देश, ढक्क-ढाका(बंगाल), काञ्चीपुर और वैदिश-विदिशा-भेलसाके आसपासके प्रदेशोंमें भेरी बजाई। अब बड़े-बड़े वीरोंसे युक्त इस करहाटक-कराड, जिला सतारा, नगरको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हे राजन् ! मैं वाद करनेके लिए सिंहके समान इतस्ततः क्रिड़ा करता फिरता हूँ।
राजा शिवकोटिको समन्तभद्रका चमत्कारक उक्त आख्यान सुनकर विरक्ति हो गयी और वह अपने पुत्र श्रीकण्ठको राज्य देकर प्रवजित हो गया। समन्तभद्रने भी गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त ले पुनः दीक्षा ग्रहण की।
ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकथा-कोषकी उक्त कथा प्रभाचन्द्र के गद्यात्मक लिखे गये कथाकोषके आधारपर लिखी गयी है। बुद्धिवादीकी दष्टिसे उक्स कथाका परीक्षण करनेपर समस्त तथ्य बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी इसना तो स्पष्ट है कि समन्तभद्रको भस्मक व्याधि हई थी और उसका शमन किसी शिवकोटिनामक राजाके शिवालयमें जानेपर हुआ था। हमारा अनुमान है कि यह घटना दक्षिण काशी अर्थात् काञ्चीकी होनी चाहिए।
समन्तभद्रको गुरु-शिष्यपरम्परा के सम्बन्धमें अभी सक निर्णीत रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। समस्त जैन वाडमय समन्तभद्रके सम्बन्ध में प्रशंसात्मक उक्तियां मिलती हैं। समन्तभद्र वर्धमान स्वामीके तीर्थको सहस्त्रगुनी वृद्धि करने वाले हुए और इन्हें श्रुतकेचलिऋद्धि प्राप्त थी। चन्नरायपट्टण ताल्लुकेके अभिलेख न. १४९में श्रुतकेवली-संतानको उन्नत करने वाले समन्त भद्र बताये गये हैं-
"श्रुतकेवलिगलु पलवरूप
अतीतर आद् इम्बलिक्के तत्सन्तानो
न्नतियं समन्तभद्र
वृतिपर् अलेन्दरू समस्तविद्यानिधिगल।।"
यह अभिलेख शक संवत् १०४७का है। इसमें समन्तभद्रको श्रुतकेलियोंके समान कहा गया है। एक अभिलेखमें बताया है कि श्रुतकेलियों और अन्य आचार्योंके पश्चात् समन्तभद्रस्वामी श्रीवर्धमानस्वामीके तीर्थकी सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए अभ्युदरको प्राप्त हुए।
"श्रीवर्धमानस्वामिगलु तीत्थंदोलु केवलिगलु ऋद्धीप्राप्तरुं श्रुतकेवलिगलुं पलरूं सिद्धसाध्यर् आगे तत्___त्यंमं सहस्त्रगणं माहि समन्तभद्र-स्वा मिगलु सन्दर___।"
इन अभिलेखोंसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि समन्तभद्र श्रुतधरोंकी परम्पराके आचार्य थे| इन्हें जो श्रुतपरम्परा प्राप्त हुई थी, उस श्रुतपरम्पराको इन्होंने बहुत ही वृद्धिगत किया।
विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके विद्वान् कवि हस्तिमल्ल और 'अय्यप्पार्यने' श्रीमूलसंघव्योसनेन्दु विशेषण द्वारा इनकी मूलसंघरूपी आकाशका चन्द्रमा बताया है। इससे स्पष्ट है कि समन्तभद्र मूलसंघके आचार्य थे।
श्रवणबेलगोलके अभिलेखोंसे ज्ञात होता है कि भद्रबाहू श्रुतकेवलीके शिष्य चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मुनिके वंशज पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्द मुनिराज, उनके वंशज गृद्धपिच्छाचार्य और गृद्धपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छाचार्य और उनके वंशज समन्तभद्र हुए। अभिलेख में बताया है-
"श्रीगृद्धपिच्छ-मुनिपस्य बलाकपिच्छ:
शिष्योऽजनिऽष्टभुवनत्रयत्तिकोतिः।
चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-मौलि-
माला-शिलीमुख-विराजितपादपनः।।
एवं महाचार्यपरम्परायां स्यात्कारमुद्राङ्किततत्वदोपः।
भद्रस्समन्ताद्गुणतो गणीशस्समन्तभद्रोऽजनि वादिसिंहः।।"
इन पद्योंसे विदित है कि समन्तभद्र कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छाचार्य आदि महान् आचार्योंकी परम्रामें हुए थे।
सेनगणकी पट्टावलीमें समन्तभद्रको सेनगणका आचार्य सूचित किया है। यद्यपि इस पट्टावलीमें आचार्योंकी क्रमबद्ध परम्परा अंकित नहीं की गयी है, तो भी इतना स्पष्ट है कि समन्तभद्रको उसमें सेनगणका आचार्य परिगणित किया है।
श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं. १०८ में नन्दिसेन आदि चार प्रकारके संघ भेदका भट्टाकलंकदेवके स्वर्गारोहणके पश्चात् उल्लेख है। परन्तु समन्तभद्र अकलंकदेवसे बहुत पहले हो चुके हैं। अकलंकदेवसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके गणोंका कोई उल्लेख भी दिखलाई नहीं पड़ता है। यद्यपि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार एवं अभिलेख नं. १०५में इन चारों संघोका प्रवर्तक अर्हदबलि आचार्यको लिखा है। पर श्रुतावतार अकलंकदेवसे पश्चात्ययर्ती रचना है।
तिरूमकूडल नरसिपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं. १०५में समन्तभद्रको द्रमिल संघके अन्तर्गत नन्दिसंघकी अरूंगल शाखाका विद्वान सूचित किया है।
अतः यह निश्चयपूर्वक कह सकना कठिन है कि समन्तभद्र अमुक गण या संघके थे। इतना तथ्य है कि समन्तभद्र गृद्धविच्छाचार्यके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' मंगलस्तोत्रमें स्तुत आप्तके मीमांसक होनेसे वे उनके तथा कुन्दकुन्दके अन्वयमें हुये है।
आचार्य समन्तभद्रके समयके सम्बन्धमें विद्धानोंने पर्याप्त उहापोह किया है। मि. लेविस राईसका अनुमान है कि समन्तभद्र ई. की प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें हुए हैं।
"कर्नाटक पानीले नामक ग्रंथके रचयिता आर नरसिंहाचार्यने समन्तभद्रका समय शक संवत् ६० (ई. सन् १३८) के लगभग माना है। उनके प्रमाण भी राईसके समान ही हैं।
श्रीयुत् एम. एस. रामस्वामी आयंगरने अपनी 'Studies in South Indian Jainism' नामक पुस्तक में लिखा है- "समन्तभद्र उन प्रख्यात दिगम्बर लेखकोंकी श्रेणीमें सबसे प्रथम थे, जिन्होंने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें महान् प्राधान्य प्राप्त किया।"
मध्यकालीन भारतीय न्यायके इतिहास (हिस्ट्री ऑफ दी मिडिझायल स्कूल ऑफ इण्डियन लाजिक) में डॉ. सतीशचन्द्र विद्याभूषणने यह अनुमान प्रकट किया है कि समन्तभद्र ई. सन् ६००के लगभग हुए हैं। उन्होंने अपने इस कथनके लिए कोई तर्क नहीं दिया। केवल इतना ही बतलाया है कि बौद्ध तार्किक धर्मकीर्तीका समकालीन कुमारिलभट्ट है और इनका समय ई. सन् सातवीं शताब्दी है। कुमारिलने समन्तभद्रका निर्देश किया है। अतः कुमारिलके पूर्व समन्तभद्रका समय मानना उचित है।
सिद्धसेनने अपने न्यायावतारमें समन्तभद्रके रत्नकरण्डकश्रावकाचारका निम्नलिखित पद्य उद्धत्त किया है.-
"आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमदृष्टेष्टविरोधकम्।
तत्त्वोपदेशकृतसाचं शास्त्रं कापथपट्टनम्॥"
इस पद्यको लेकर विवाद है। पंडिस सुखलालजीका मत है कि यह न्याया वतारका मुल पद्म है। वहींसे यह रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें गया है। पर विचार करनेसे यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। यतः रत्नकरण्डनावकाचारमें जिस स्थान पर यह पद्य आया है वहाँ वह क्रमबद्धरूपमें नियोजित है। समन्तभद्रने सम्यग्दर्शनकी परिभाषा हुये आप्त आजमगाम जोरजोतने सानो सम्यादर्शन कहा है। इस प्रसंगमें उन्होंने सर्व प्रथम आप्तका स्वरूप बतलाया है और तत्पश्चात् आगमका। शास्त्रका स्वरूप बतलाते हुए उक्तं पद्य लिखा है। इसके अनन्तर तपोभृतक स्वरूप बतलाया है। अतः क्रमबद्धताको देखते हुए उक्त पद्यका उद्भवस्थान समन्तभद्रका रत्नकरण्डश्रावकाचार है। वह अन्यत्र से उद्धूत नहीं है। परन्तु यह स्थिति न्यायावतारमें नहीं है। न्यायावतारमें स्वार्थानुमानका लक्षणनिरूपणके पश्चात् शाब्द- आगम प्रमाणका कथन करने के लिए एक पद्य, जिसमें शाब्दका पूरा लक्षण आ गया है, निबद्ध कर इस पद्यको उपस्थित किया है, जिसे वहाँसे अलग कर देनेपर ग्रन्थका भङ्ग भी नहीं होता। परन्तु रत्नकरण्डवावकाचारमें से उसे हटा देने पर ग्रंथ भङ्ग हो जाता है। अत: इस पद्यको न्यायाक्तारमें मूल ग्रन्थरचयिताका नहीं माना जा सकता है। न्यायावतारमें शब्दप्रमाणका लक्षण निम्न प्रकार है-
दुष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्परमार्थाभिधायिनः।
तत्वग्राहितयोत्पन्नं मान शाब्दं प्रकीतितम्।।
इस पद्मके पश्चात् ही उक्त आप्तोपज्ञ' आदि पद्य दिया है, जो व्यर्थ, पुनरूक्त और अनावश्यक है। आचार्य श्री जुगलकिशोरने अपने 'स्वामी समन्तभद्र' शीर्षक प्रबन्धमें विस्तारसे इसपर विचार किया है। अतएव न्यायावतारमें उल्लिखित उक्त पद्मके आधार पर समन्तभद्रको उसके कर्ता सिद्धसेनसे उत्तरवर्ती बतलाना समुचित नहीं है।
स्वामी समन्तभद्रके समयपर विचार करनेवाले जैन विचारकोंमें दो विचार धाराएँ उपलब्ध हैं। प्रथम विचारधाराके प्रवर्तक पंडित नाथरामजी प्रेमी हैं और उसके समर्थक डॉ. हीरालालजी आदि हैं। प्रेमीजीने स्वामी समन्तभद्रका समय छठी शताब्दी माना है। उनका तर्क है कि 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' मंगलाचरण सूत्रकार उमास्वामीका न होकर सर्वार्थसिद्धिटीकाकार देवनन्दि-पूज्यपादका है और इसी मंगलाचरणके आधार पर स्वामी समन्तभद्रने 'आप्तमीमांसा' नामक ग्रन्थकी रचना की है। अतएव इनका समय देवनन्दि पूज्यपाद (ई. ५वीं शती) के अनन्तर होना चाहिये। प्रेमीजीके इस मतका समर्थन कुछ मिन्न युक्तियों द्वारा आचार्य श्रीसुखलालजी संघवी एवं डॉ. महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य भी किया है। पति सुखलालमोने समन्तभद्रपर प्रसिद्ध बौद्ध तार्किक धर्मकीर्तीका प्रभाव अनुमित कर उनका समय धर्मकीर्तीके उपरान्त बतलाया है। पं. महेन्द्रकुमारजीने 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' मंगलाचरणको देवनन्दि-पूज्यपादका सिद्ध कर उसपर आप्तमीमांसा लिखनेवाले समन्तभद्रका समय उनके बाद अर्थात् छठी शताब्दी माना है।
किन्तु उल्लेखनीय है कि जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ९, किरण १ में 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ शीर्षकसे जो उन्होंने निबन्ध लिखा था और जिसके आधार पर आचार्य समन्तभद्रका उक्त छठी शताब्दी समय निर्धारित किया था, जिसका उल्लेख न्यायकुमुदचन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें किया था, उसपर डॉ. दरबारीलालजी काठियाने 'तत्वार्थसूत्रका मंगलाचरण' शर्षिक दो विस्तृत निबन्धों द्वारा 'अनेकान्त' वर्ष ५, किरण ६,७ तथा १०,११ में गहरा विचार करके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' मंगलस्तोत्रको तत्वार्थसूत्रकार आचार्य गृद्धपिच्छका सिद्ध किया है। फलतः डॉ. महेन्द्रकुमारजीने अपने पुराने विचारमें परिवर्तन कर समन्तभद्रका समय ‘सिद्धिविनिश्चयटीकाकी’ प्रस्तावना एवं 'जैन दर्शन' ग्रन्थोंमें ई. सन् द्वितीय शताब्दी स्वीकार कर लिया है, जो आचार्य मुख्तार आदि विद्वानोंकी दृढ़ मान्यता है।
आचार्य श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने समन्तभद्रके साहित्यका गम्भीर आलोचन कर उनका समय विक्रमकी द्वितीय शती माना है। इनके इस मतका समर्थन डॉ. ज्योति प्रसाद जैनने अनेक युक्तियोस किया है। उन्होंने लिखा है-स्वामी समन्तभद्रका समय १२०-१८५ ई. निर्णित होता है और यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म पूर्वतटवर्ती नागराज्य संघके अन्तर्गत उरगपूर (वर्तमान त्रिचनापल्ली)के नागवंशी चोल नरेश कीलिकवर्मनके कनिष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी सर्ववर्मन (शेषनाग) के अनुज राजकुमार शांतिवर्मनके रूपमें सम्भवतया ई. सन् १२०के लगभग हुआ था, सन् १३८ ई. (पट्टावलि प्रसत्त शक सं.६०)में उन्होंने मुनिदीक्षा ली और १८५ ई. के लगभग वे स्वर्गस्थ हुए प्रतीत होते हैं। अतएव समन्तभद्रका समय अनेक प्रमाणोंके आधार पर ईस्वी सनकी द्वितीय शती अवगत होती है।
इनके चित्रालंकार सम्बन्धी स्तुतिविद्याके आधार पर जो यह कहा जाता है कि समन्तभद्र अलंकृत काव्ययुगके कवि है और इनका समय भारनिके आस-पास मानना चाहिये। यह तर्क भी अधिक सबल नहीं है। एकाक्षरी या द्वयक्षरी या अन्य चित्रकाव्योंकी परम्परा वैदिक कालसे ही यत्त्किचित रूपमें प्राप्त होने लगती है। दक्षिण भारत में चित्रकाव्योंकी परम्परा बहुत प्राचीन समयसे चली जा रही है। समन्तभद्गने चित्रकाव्यका प्रयोग उसी परम्पराके आधारपर किया है। अत: उसके आधापर पर उनका समय अर्वाचीन बतलाना युक्त नहीं है। अतएव संक्षेपमें समन्तभद्रका समय ई. सन् द्वितीय शताब्दी है और ‘मोक्ष मार्गस्य नेतारं' को आचार्य विद्यानन्दने सुत्रकार गृद्धपिच्छका ही मंगलाचरण माना है, सर्वार्थसिद्धिकार पूज्यपाद देवनन्दिका नहीं।
संस्कृत काव्यका प्रारम्भ ही स्तुति-काव्यसे हुआ है। जिसप्रकार वैदिक ऋषियोंने स्वानुभूति-जीवनकी जीवन्तधारा और सौंदर्यभावनाको स्तुति काव्यकी पटभूमिपर ही अंकित किया है, उसीप्रकार स्वामी समन्तभद्रने भी दर्शन, सिद्धान्त एवं न्यायसम्बन्धी मान्यताओंको स्तुति-काव्यके माध्यमसे अभिव्यक्त किया है। अतएव स्तुतियोंकी विभिन्न परम्परामें आद्य जैन स्तुतिकार समन्तभद्रने बौद्धिक चिन्तन और मानवजीवनको प्रोज्जवल कल्पनाको स्तुति-कायके रूपमें हो मूर्तिमत्ता प्रदान की है। इनके द्वारा रचित स्तुतियों में तरल भावनाओंके साथ मस्तिष्कका चिन्तनभी समवेत है। समन्तमद्र द्वारा लिखित निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती हैं-
१. बृहत् स्वम्भूस्तोत्र
२. स्तुतिविद्या-जिनशतक
३. देवागमस्तोत्र-आसमीमांसा
४. युक्त्यनुशासन
५. रत्नकरण्डकश्रावकाचार
६. जीवसिद्धि
७. तस्वानुशासन
८. प्राकृतव्याकरण
९. प्रमाणपदार्थ
१०. कर्मप्राभृसटीका
११. गन्धहस्तिमहाभाष्य
१. बृहत् स्वम्भूस्तोत्र- इसका अपर नाम स्वम्भूस्तोत्र अथवा चातुर्विशांती स्तोत्र भी है। इसमें ऋषभदेवसे लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरोंकी क्रमशः स्तुतियां है। इस स्तोत्रके भक्तीरसमें गम्भीर अनुभूति एवं तर्कणायुक्त चिन्तन निबद्ध है। अतः इसे सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि कहा जा सकता है। इस 'स्तोत्र’ के संस्कृत टीकाकार प्रमाचन्द्रने इसे 'नि:शेषजिनोक्तधर्म' कहा है। इसमें कुल पद्योंकी संख्या निम्न प्रकार है-
१. श्रीऋषभजिन स्तवन, पद्य ५,
२. श्रीअजितजिन स्तवन, पद्य ५,
३. श्री सम्भवज्जीन स्तवन, पद्य ५,
४. श्रीअभिनन्दनजिन स्तवन पद्य ५,
५. श्रीसुमतिजिन स्तवन पद्य ५,
६. श्रीपद्मप्रभजिन स्तवन पद्य ५,
७. श्रासुपार्श्वजिन स्तवन पद्य ५,
८. श्रीचन्द्रप्रभजिन स्तवन पद्य ५,
९. श्रीसुविधजिन स्तवन पद्य ५,
१०. श्रीशीतलजिन स्तवन पद्य ५,
११, श्रीश्रेयोजिन स्तवन पद्य ५,
१२. श्रीवासुपूज्यजिन स्तवन पद्य ५,
१३. श्रीविमल जिनस्तवन पद्य ५,
१४. श्रीअनन्तजिन स्तवन पद्य ५.
१५.श्रीधर्मजिन स्तवन पद्य ५,
१६. श्रीशान्तिजिन स्तवन पद्य ५.
१७. श्रीकुंथुजिन स्तवन पद्य ५,
१८, श्रीअरजिन स्तवन पद्य २०,
१९ श्रीमल्लिजिन स्तवन पद्य, ५,
२० श्रीमुनिसुव्रतजिन स्तवन पद्य ५,
२१. श्रीनमिजिन स्तवन पद्य ५,
२२. श्रीअरिष्टनेमिजिन स्तवन पद्य १०,
२३. श्री पाश्वजिन स्तवन पद्य ५,
२४. श्रीवीरजिन स्तवन पद्य ८ = १४३।
इस स्तोत्रमें कविने प्रबन्ध-पद्धतिके बीजोंको निहित कर इतिवृत्त सम्बन्धी अनेक तथ्योंको प्रस्तुत किया है। प्रथम तीर्थंकरको प्रजापतिके रूप में असि, मषि, कृषि,सेवा, शिल्प और वाणिज्यका उपदेष्टा कहा है। इस स्तोत्रमें आये हुए ‘निर्दय भस्मसात्कियाम’ पदसे सम्मतः आचार्यने अपनी भस्मक व्याधिका संकेत किया है तथा सम्भवनाथको स्तुतिमें सम्भवजीनको वैद्यका रूपक देकर अपनी जीवनघटनाओंकी ओर संकेत किया है। इसी प्रकार “यस्याङ्ग-लक्ष्मो परिवेश भिन्न तमस्तमोरेखि रश्मिभिन्नम् पदसे राजा शिवकोटिके शिवालयमें घटित हुई घटनाका संकेत प्राप्त होता है।
समस्तभद्रने बाद (शास्त्रार्थ) द्वारा जैन सिद्धान्तोंका प्रचार किया था। श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोंके अनुसार पाटलिपुत्र, ढक्क, मालव, कांची आदि देशोंमें उन्होंने शास्त्रार्थ कर जिनसिद्धान्तोंकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। इस ओर भी उनका संकेत "स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदाऽवलिप्ता वाकसिह-नादेविमदा वभूवुः" पद्यांशसे मिलता है।
शान्तिनाथतीर्थकरने चक्रवर्तीत्वपद प्राप्त किया था और उन्होंने षट्खण्डकी दिग्विजयकर समस्त राजाओंको करद बनाया था। उनके राज्यकालमें प्रजा अत्यन्त सुखी और समृद्ध थी। इस बातकी सूचना निम्नलिखित पद्यांशोंसे प्राप्त होती है-
"चक्रण यः शत्रु-मवरण जित्वा नृप सर्व-नरेन्द्र-चक्रम्"
"विधाय रक्षा परतः प्रजानां राजा धीरं योऽप्रतिम-प्रतापः"
मल्लिजिन आजन्म ब्रह्मचारी थे। उनकी गणना बालयतियोंमें है। इसी प्रकार अरिष्ट नेमिको भी बालयति कहा गया है। इन दोनों तीर्थकरोंके स्तवन में 'महर्षी' या 'ऋषि' शब्दके प्रयोग आये हैं, जो इन तीर्थकरोंके बालयतित्वको अभिव्क्त करते हैं।
पार्श्वनाथस्तोत्रमें तीर्थकर पाश्वनाथके मुनिजीवनमें तपश्चर्या करते समय वेरी कमठ द्वारा किये उपसर्ग तथा पद्यावती और धरणेन्द्र द्वारा उसके निवारण का वर्णन निम्नलिखित पद्योंमें किया है-
"तमाल-नीलैः सघनुस्तडिद्गुणैःप्रकीर्ण-भीमाशनि-वायु-वृष्टिभिः।
बलाहकैवरि-वशैरुपद्रुतो महामना यो न चचाल योगतः॥
बृहत्फणा-मण्डल-मण्डपेन यं स्फुर-तरित्पिड-रुचोपसर्गिणम।
जुगूह नागो धरणो धराधरं विराग-संध्या-तडिदम्बुदो यथा।"
इस प्रकार इस स्तोत्र-काव्यमें प्रबन्धात्मक बीजसूत्र सर्वत्र विद्यमान हैं।
स्तोत्रसाहित्यका निर्माता वही सफल माना जाता है, जो स्तोत्रोंके मध्यमें प्रबन्धात्मक बीजोंकी योजना करता है, इस योजनासे स्तोत्र तो बनते ही हैं, साथ ही उनमें प्रेषणीयता विशेष उत्पन्न होती है। समन्तभदाचार्यने वैदिक मन्त्रोंके समान ही प्रबन्धगर्भित स्तोत्रोंका प्रणयनकर दार्शनिक और काव्यात्मक क्षेत्रमें नये चरणचिन्ह उपस्थित किये हैं।
वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, वसन्ततिलका, रथोद्धता, पथ्यावक्त्र-अनुष्टुप, सुभद्रिका-मालतीमिश्रित, वानवासिका, वेतासीय, शिखरिणी, उदगता एवं आर्यागीति इन तेरह प्रकारके छन्दोंका प्रयोग पाया जाता है। अलंकार-योजनाकी दृष्टिसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्सरन्यास, उदाहरण, दृष्टान्त एवं अन्योक्ति प्रभृति अलंकार उल्लेख्य हैं। अतिशयोक्तिका निम्न उदाहरण ध्यातव्य है-
तव रूपस्य सौन्दर्य दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्।
द्वयक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव वहु-विस्मयः।।
यहाँ भगवान के सौन्दर्यको दो नेत्रोंसे देखने में अतृप्तिका अनुभव करते हुए इन्दने सहत्र नेत्र धारणकर भगवानके रूप-सौन्दर्यका अवलोकन कर आश्चर्य प्राप्त किया है। इस संन्दर्भमें अतिशयोक्ति हैं।
सुखाभिलाषाऽनलदाहमूच्छित मनो निजं मानमयाऽमृत्ताम्बुभिः।
व्यविध्यपस्त्वं विषदाहमोहितं यथा भिषम्मन्त्रगुणैः स्वविग्रहम्।।
जिसप्रकार वैद्य विषदाहसे मुर्चीत हुए अपने शरीरको विषापहारमन्त्रके गुणोंसे उसकी अमोघशक्तियोंसे निर्दिष एवं मुर्चा रहित कर देता है, उसीप्रकार हे शोत्तलजिन ! आपने सांसारिक सुखोंकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूछित हुए अपने आत्माको ज्ञानमय अमृतके सिञ्चनसे मूच्छारहित-शान्त किया है।
स चन्द्रमा भव्यकुमुद्धतीनां विपन्नदोषाभ्रकलखुलेपः।
व्याकोश-याङ-न्याय-मयूखमाल: पूयात्पवित्रो भगवाम्मनो मे।।
यहाँ-'भव्यकुमुदतीनां' और 'दोषाभ्र-कलखु-लेपः' में रूपककी योजना है। इन रूपकोंने भावोंको सहज ग्राह्य तो बनाया ही है, साथ ही चन्द्रप्रभ भगवानके गुणोंका प्रभाव भी दिखलाया है। भव्यकुमुदनियोंको विकसित करनेके लिए चन्द्रप्रभ चन्द्रमा है।
पद्मप्रभः पद्यपलाश-लेश्यः पद्यालयालिजितचारुमूर्ती:।
बभौ भवान् भव्य-पयोरुहाणां पद्माकराणामिव पद्यबन्धुः।।
पद्ममत्रके समान द्रव्यलेश्याके धारक हे पद्मप्रभजिन! आपको सुन्दरमूर्ति पदमालय-लक्ष्मीसे आलिङ्गित रही है और आप भव्यकमलोंको विकसित करनेके लिए उसी तरह भासमान हुए हैं, जिसप्रकार सूर्य कमलसमूहका विकास करता हुआ सुशोभित होता है।
संक्षेपमें स्तोत्रकाव्यमें एकान्ततत्वकी समीक्षापूर्वक स्पाद्वादनयसे अनेकान्तामृततत्वको स्थापना की गयी है।
२. स्तुतिविद्या
जिनशतक और जिनशतकालंकार भी इसके नाम आये हैं। इसमें चित्रकाव्य और बन्धरचनाका अपूर्व कौशल समाहित है। शतककाव्योंमें इसकी गणना की गयी है। सौ पद्योमें किसी एक विषयसे सम्बद्ध रचना लिखना असाधारण बात मानी जातो थी। प्रस्तुत जिनशतकमें चौबीस तीर्थंकरोंकी चित्रबन्धोंमें स्तुति की गयी है। भावपक्ष और कलापक्ष दोनों नैतिक एवं धार्मिक उपदेशके उपस्कारक बनकर आये हैं। समन्तभद्रकी काव्यकला इस स्तोत्रमें आद्यन्त व्याप्त है। मुरजादि चक्रबन्धकी रचनाके कारण चित्र काव्यका उत्कर्ष इस स्तोत्रकाव्यमें पूर्णतया वर्तमान है।
समन्तभद्रकी इस कृतिसे स्पष्ट है कि चित्रकाव्यका विकास माघोत्तरकाल में नहीं हुआ, बल्कि माघ कविसे कई सौ वर्ष पूर्व हो चुका है। चित्र, श्लेष और यमकका समावेश वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता है, अत: यह सम्भव है कि दाक्षिणत्य भाषाओंके विशिष्ट सम्पर्कके कारण समन्तभद्रने चित्र-श्लेष और यमकका पर्याप्त विकास कर उक्त काव्यकी रचना की। इस कृतिमें मुरजबन्ध, अर्धभ्रम, गतप्रत्यागतार्घ, चक्रबन्ध, अनुलोम, प्रतिलोम क्रम एवं सर्वतोभद्र आदि चित्रोंका प्रयोग आया है। एकाक्षर पद्योंको सुन्दरता कलाकी दक्षिसे अत्यन्त प्रशंसनीय है।
कुछ विद्वानोंका इस कृतिको देखकर यह अनुमान है कि जिस कृत्रिम शैलीमें समन्तभद्रने स्तुतिविद्याका प्रमयन किया है वह कृत्रिम शैली ई. सनकी चौथी शताब्दीसे विकसित होती है। अत: कृत्रिम शैलीके कारण यह कृति द्वितीय-तृतीय शतीकी रचना नहीं हो सकती। विचार करनेपर उक्त मत निभ्रन्ति प्रतीत नहीं होता, यतः कृत्रिम शैलीके विकासका मूल कारण आर्यभाषाके साथ द्रविड भाषाका सम्पर्क है। द्राविड़-परिवारकी भाषाओंमें चित्र, श्लेष और चमकको अधिक क्षमता है। अत: समन्तभद्रने दाक्षिणात्य होनेके कारण ही इस शैलीका प्रयोग किया है।
इस स्तोत्रमें कुल ११६ पद्य हैं और अन्तिम पद्यमें "कविकाव्यनामगर्म- चक्रवृत्तम" है। जिसके बाहरके षष्ट वलयमें 'शान्तिवर्मकृतम्' और चतुर्थ वलयमें 'जिनस्तुतिशतम्' की उपलब्धि होती है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकका एक साथ प्रयोग काव्यकलाकी दृष्टिसे श्लाघनीय है। यहाँ उदाहरणार्थ काव्यलिंगको प्रस्तुत किया जा रहा है-
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यच्र्चनं चापि ते
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षि संप्रेक्षते।
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरा नतिपरं सेवेव्दशी येन ते
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृतो तेनैव तेजःपते॥
जिनेन्द्र भगवानकी आराधना करनेवाले मनुष्यकी आत्मा आत्मीय तेजसे जगमगा उठती है। वह सर्वोत्कृष्ट पुरुष गिना आने लगता है। तथा उसके महान पुण्यका बन्ध होता है। यहाँ स्मरण, पूजन, अञ्जलि-बन्धन, कथा-श्रवण, दर्शन आदिका क्रमशः नियोजन होनेसे परिसंख्या-अलंकार है। आचार्यने हेतु-वाक्यों का प्रयोग कर काव्यलिंगकी भी योजना की है। इस प्रकार यह स्तुति-विद्या स्तोत्र-काव्य और दर्शनगुणोंसे युक्त है। और है सविवेक भकि-रचना।
३. आप्तमीमांसा या देवागमस्तोत्र
स्तोत्रके रूपमें तर्क और आगमपरम्पराकी कसौटीपर आप्त-सर्वज्ञदेवकी मीमांसा की गयी है। समन्तभद्र अन्धश्रदालु नहीं हैं, वे श्रद्धाको तर्ककी कसौटीपर कसकर युक्ति-आगमद्वारा आप्तकी विवेचना करते हैं। आप्त विषयक मूल्यांकनमें सर्वज्ञाभाववादी मीमांसक, भावैकान्तवादी सांख्य, एकान्तपर्यायवादी बौद्ध एवं सर्वथा उभयवादी वैशेषिकका तर्कपूर्वक विवेचन करते हए निराकरण किया गया है। प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्साभावका सप्तभंगीन्यायद्वारा समर्थन कर वीरशासनकी महत्ता प्रतिपादित की है। सर्वथा अद्वैतवाद, द्वैतवाद, कर्मद्वैत, फलद्वैत, लोकद्वैत प्रभृतिका निरसन कर अनेकान्तात्मकता सिद्ध की गयी है। इसमें अनेकान्तवादका स्वस्थ स्वरूप विद्यमान है। उदाहरणके लिए-
"द्रव्यपर्यायोरेक्यं तयोरव्यतिरेकतः।
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावत:॥
संज्ञासंख्याविशेषाच्च स्वलक्षनविशेषतः।
प्रयोजनादिभेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा॥"
द्रख्य और पर्याय कथंचित् एक हैं, क्योंकि वे भिन्न उपलब्ध नहीं होते तथा वे कथंचित् अनेक हैं क्योंकि परिणाम, संज्ञा, संख्या, आदिका भेद है। देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदिको सिद्धि अनेकान्तके द्वारा हि होती है। एकान्त वादियोंको समस्त तपस्याओंका अनेकान्तवदके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
इस स्तोत्रमें ११५ पद्य हैं। 'देवागम' पदद्वारा स्तोत्रका आरम्भ होनेके कारण यह 'देवागम' स्तोत्र भी कहा जाता है। समन्तभद्रकी परीक्षाप्रधान दृष्टि इस स्तोत्रकाव्य में समाहित है। कवित्वकी दृष्टिसे यह काव्य बोझिल है। काव्य रस-दर्शनकी चट्टानके भीतर प्रवेश करनेपर ही क्वचित् प्राप्त होता है, अप्रस्तुत विधानका भी अभाव है। जीवन और जगतकी विभिन्न समस्याओंका समाधान इस स्तोत्रकाव्यमें अवश्य वर्तमान है।
४. युक्त्यनुशसन- वीरके सर्वोदय तीर्थका महत्व प्रतिपादित करने के लिए उनकी स्तुति की गयी है। युक्तिपूर्णक महावीरके शासनका मण्डन और विरुद्धमतोंका खण्डन किया गया है। समस्त जिनशासनको केवल १४ पद्योंमें ही समाविष्ट कर दिया है| अर्थगौरवकी दृष्टिसे यह काव्य उत्तम है, 'गागरमें सागर'को भर देनेकी कहावत चरितार्थ होती है। महावीरके तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा है-
"सर्वान्तवत्तद् गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मियोऽनपेक्षम्।
सर्वापदामन्तकरं निरन्सं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव॥"
इसप्रकार महावीरके तीर्थको ही समस्त विपत्तियोंका अन्त करनेवाला सर्वोदय तीर्थ कहा है।
५. रतनकरण्यश्रावकाचार- जीवन और आचारकी व्याख्या इस ग्रंथमें की गयी है। १५० पद्योंमें विस्तारपूर्वक सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक चारित्रका विवेचन करते हुए कुन्दकुन्दके निर्देशानुसार सल्लेखनाको श्रावकके व्रतोंमें स्थान दिया है। अन्तमें श्रावककी एकादश प्रतिमाएँ वर्णित है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवालने समोचीन धर्मशास्त्र- रत्नकरण्डश्रावकाधारको भूमिकामें लिखा है- "स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न केवल जैनमार्गको सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न किया है। (जैन वत्म समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तात् मुहः), किन्तु शुद्धमानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यको नैतिक धरातलपर प्रतिष्ठित करनेके लिए बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके इस दृष्टिकोणमें मानव-मात्रकी रुचि हो सकती है। समन्तभद्रकी दृष्टिमें मनकी साधना हृदयका परिवर्तन सच्ची साधना है। बाह्य आचार तो आडम्बरोंसे भरे भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना है कि मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है (कारिका-३३) किसीने चाहे चाण्डाल योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु यदि उसमें सम्यक् दर्शनका उदय हो गया है तो देवता ऐसे व्यक्तिको देव समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढंके हुए किन्तु अन्तरमें दहकते हुए अंगारकी तरह होता है।"
इस ग्रंथकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-
१. श्रावकके अष्टमूलगुणोंका विवेचन
२. अर्हतपूजनका वैयावृत्यके अन्तर्गत स्थान
३. व्रतोंमें प्रसिद्धि पानेवालोंके नामोल्लेख
४. मोही मुनिको अपेक्षा निर्मोही श्रावककी श्रेष्ठता
५. सम्यकदर्शनसम्पन्न मातंगको देवतुल्य कहकर उदार दृष्टिकोणका उपन्यास।
६.कुन्दकुन्द और उमास्वामीको श्रावकधर्म सम्बन्धी मान्यताओंको आत्मसातकर स्वतन्त्र रूपमें श्रावकधर्मसम्बन्धी ग्रंथका प्रणयन।
इस कृतिमें कर्ताके रूपमी सुमन्त्भद्रका कही भी उपलब्ध नहीं है। टीकाकार प्रभाचन्द्रने इसे समन्तभद्रकृत लिखा है। अत: डाॅ. हीरालाल जैन आप्तमीमांसामें निरूपित आप्तके लक्षणकी शैलीकी अपेक्षा इसकी शैलीमें भिन्नता प्राप्तकर और पार्श्वनाथचरितकी उत्थानिकामें योगीन्द्रकी रचनाके निर्देशको पाकर इसे योगीन्द्रदेवकी रचना मानते हैं। ग्रंथके उपान्त्य श्लोकमें 'बौतकलड’, विद्या' और 'सर्वार्थसिद्धि' शब्दोंको तत्तद् आचार्य और ग्रन्थोंका सूचक मानकर आठवीं-ग्यारहवीं शतीके मध्यकी रचना इसे स्वीकार करते हैं।
अतः डॉ. जैनके मतानुसार यह कृति आप्तमीमांसाके रचयिता स्वामी समन्तभद्रकी नहीं है। भले ही कोई दूसरा समन्तभद्र इसका रचयिता रहा हो। डॉ. साहबने उक्त मन्तव्यको प्रकट करनेके लिए एक निबन्ध अनेकान्त, वर्ष ८, किरण १-३. पृ. २६-३३, ८६-९० और १२५-१३२ में लिखा था, जिसका प्रतिवाद डॉ. प्रो. दरबारीलाल कोठियाने अनेकान्त वर्ष ८ किरण ४-५ में किया है। डॉ. कोठियाने डॉ. जैनके तर्कोका उत्तर देते हुए प्रस्तुत कृतिको आचार्य समन्तभद्रकी ही रचना सिद्ध किया है। मैं इस विवादमें न पड़कर इतना अवश्य कहूँगा कि समन्तभद्रके अन्य ग्रंथोंके समान इस ग्रन्थके भी दो नाम उपलब्ध हैं- १. समीचोन धर्मशास्त्र ओर २. वर्ण्य विषयके अनुसार रत्नकरण्डकश्रावकाचार। स्वामी समन्तभद्रकी यह शेली है कि वे अपने प्रत्येक ग्रन्थके दो नाम रखते हैं. प्रथम नामका निर्देश प्रथम पद्यके प्रारम्भिक वाक्यमें कर देते हैं और दूसरेका निर्देश ग्रंथके वर्ण्य विषयके आधारपर रहता है।
यह निर्विवाद सत्य है कि इस ग्रन्थमें प्रतिपादित विषय बहुत प्राचीन है। श्रुतधर कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुड, प्रवचनसार, दर्शनपाहुड, सीलपाहुड आदिसे विषयको सूत्ररूपमें ग्रहणकर नये रूपमें श्रावकाचारसम्बन्धी सिद्धान्तोंका प्रणयन किया है। अत: विद्वानोंके मध्य मूलगुणसम्बन्धी जो प्रश्न उठाया जाता है उसका समाधान यहाँ सम्भव है। जब समन्तभद्रने श्रावकाचारका प्रणयन नये रूपमें किया, तो उन्होंने बहुत्त-सी ऐसी बातोंको भी इस ग्रंथमें स्थान दिया, जो पहलेसे प्रचलित नहीं थीं। हमारा तो दृढ़ मत है कि तृतीय अध्याय की यह ६६ वीं कारिका प्रक्षिप्त है। पोछेके किसी विद्वान्ने प्रतिलिपि करते समय अहिंसाणुव्रतके विशुद्धयर्थ इस कारिकाको जोड़ दिया है। यहाँसे इसे हटा देनेपर भी ग्रंथके वर्ण्य विषयमें किसीप्रकारकी कमी नहीं आती। यह कारिका एक प्रकारसे विषयका पुनरुक्तीकरण ही करती है। मद्य, मांस, मधु के त्याग तथा पंचाणुव्रतोंके पालनको अष्टमूलगुण कहा गया है। अहिंसाणुव्रत के लक्षणमें संस्कारपूर्वक मन-वचन-काय, कृत, कारित, अनुमोदनारूप व्यापारसे द्वीन्द्रियादि प्राणियोंका घात न करना अहिंसाणुव्रत है। इस परिभाषाके अन्तर्गत मद्य, मांस, मधुका त्याग स्वयमेव समाविष्ट हो जाता है। पंचाणुव्रतोंकी चर्चा तो स्पष्टरूपसे पुनरुक्त है ही। अतएव वर्ण्य-विषयकी दृष्टिसे इस पद्यकी कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि आचार्य समन्तभन्द्रको अष्टमूलगुणोंका निर्देश करना अभीष्ट होता, तो वे इस पद्यको अहिंसाणुव्रतके लक्षणके आस-पास निबद्ध करते। अहिंसादि व्रतोंका पालन करनेवाले व्यक्तियोंके नामोल्लेखके पश्चात इस कारिकाका संयोजन अनुपयोगी जैसा प्रतीत होता है। यदि यह तर्क दिया जाय कि अणुव्रतोंका वर्णन करनेके पश्चात् मूलगुणोंका निर्देश आवश्यक था, तो यह तर्क भी बहुत सबल नहीं है। अणुव्रत और गुणव्रतोंके बीच इस पद्यका स्थान नहीं होना चाहिए। अतएव हमारी दृष्टिसे यह पद्य प्रक्षिप्त है।
अनेक आचार्योंने बताया है कि कोई नदी और समुद्रके स्नानको धर्म समझता है, कोई मिट्टी और पत्थरके स्तूपाकार ढेर बनाकर धर्मको इतिश्री मानता है। कोई पहाडसे कूदकर प्राणान्त कर लेने अथवा अग्निमें शरीरको जला देने में ही कल्याण मानता है । ये सब बातें लोकमूढ़ता है-
"आपगा-सागर-स्नानमुच्चयः सिकताऽश्मनाम्।
गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते।।"
उपयुक्त पद्यमें गतानुगतिक रूपसे अनुसरण किये जानेवाले मूढ़तापूर्ण दृष्टिकोणोंका विवेचन किया है और (१) आपगासागरस्नान, (२) सिकताऽ श्मनामुच्चयः, (३) गिरिपात, (४) अग्निपातको लोकमूढ़ता कहा है। भारतीय संस्कृतिके विकासक्रमका विचार करनेसे अवगत होता है कि उक्त ये चारों प्रथाएँ ई. सन्के पूर्व अत्यधिक रूपमें प्रचलित थीं। उत्तरकालमें इन प्रथाओंमेंसे एक-दोको छोड़कर शेष सभीका लोप हो गया। ऋग्वेदकालमें जीवन तथा जीवन भोगोंके प्रति आसक्तिकी प्रवृत्ति वर्तमान थी। अत: इस युगमें संन्यास और आत्मबलका निर्देश नहीं मिलता। प्रो. हिलब्रैटने दीक्षाविधिमें प्रयुक्त होनेवाले अग्निपातसे अग्निपात द्वारा आत्मबलिका अनुमान किया है। शतपथब्राह्मणमें बताया गया है कि पुरुषमेध गवं सर्वमेध्यत्रमें समस्त सम्पत्तिका त्याग कर साधक मृत्युका वरण करने के लिए बन जाता है। परिव्राजककी क्रियाओंका विवेचन करते हुए जाबालोपनिषदमें विभिन्न रूपोंमें किये जानेवाले आत्मघातोंको धार्मिक रूप दिया गया है-
'वीराध्वाने वा अनाशके वा अपां प्रवेशे बा अग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा।'
स्पष्ट है कि अग्निपात, जलपात और अनशनव्रतद्वारा आत्महत्या करना धार्मिक विधानमें शामिल किया गया है।
हिन्दी विश्वकोषमें आत्मघातोंका निरूपण करते हुए लिखा है कि वैध, अवैध, ज्ञानकृत और अज्ञानकृत ये चार भेद आत्मघातफे हैं। मनु एवं वृद्धगर्गने लिखा है कि जब मनुष्य अत्यन्त वृद्ध हो जाये और चिकित्सा करानेपर भी आरोग्यकी सम्भावना न हो, तो शौचादिक्रियाओंके लुप्त होने की आशंका उत्पन्न होनेसे, उच्च स्थानसे गिरकर, अग्निमें कूदकर, अनशनसे रहकर या जलमें डूबकर प्राण छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्राण छोडनेपर त्रिरात्रका अशौच माना जाता है।
उपर्युक्त सन्दर्भाशसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र द्वारा विवेचित लोक-मूढ़ताएं ब्राह्मण और उपनिषद् काल में प्रचलित थीं। धर्मशास्त्रोंके अशौच प्रकरणमें इन मान्यताओंका समावेश पाया जाता है।
'आपगासागरस्नान' की सांस्कृतिक व्याख्यामें प्रवेश करने पर ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ोंके प्राप्त भग्नवशेषोंमें उपलब्ध हुए स्नानागारोंसे हड़प्पाके सांस्कृतिक जीवनमें जलकी महत्ताका परिचय मिलता है। विद्वानोंने बताया है कि इसका आर्योंके सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। सरोवरों, नदियों और समुद्रोंके जलमें स्नान करनेकी प्रथा तथा सूर्योदयके पूर्व और भोजनके पूर्व स्नान करनेकी विधिपर धार्मिक मोहर इस बातका प्रमाण है कि सिन्धु घाटीकी सभ्यतामें भी स्नानको सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त था। आर्योंके जीवनमें नदियोंका नित्य बहता हुआ निर्मल जल ही उनके लिए स्वर्गकी पवित्रता एवं पावनताका परिचायक था। सिन्धु, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपासा, शत्तद्रु, यमुना, गंगा एवं ब्रह्मापुत्र आदि नदियोंने धार्मिक प्रेरणाके कारण ही आर्योंके जीवनको उर्वर बनाया था। अतएव नदियोंमें स्नान करनेको पवित्र भावनाके साथ उनमें डूबकर आत्मघात करनेकी प्रथा भी धर्मके नामपर ब्राह्मणकालमें प्रचलित थी। जलमात्रमें स्नान करना या असमर्थ अवस्थामें डूबकर प्राणघात करना धार्मिकताका चिह्न था । ई. पूर्व द्वितीय-तृतीय शताब्दीसे लेकर ई. सन प्रथम-द्वितीय शताब्दी तक इस प्रथाका बहुत प्रचार रहा है। जब संन्यासविधि पूर्णतया विकसित हो गयी, और आत्मशोधनके लिए ध्यान, संयमका मूल्य बढ़ गया, तो उक प्रथाका शनैः-शनैः ह्रास होने लगा। स्वामी समन्तभद्रके समय में इस प्रथाका जोर-शोरके साथ प्रचार था। अतः उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें इसकी समीक्षा की है। यहाँ यह स्मरणीय है कि लोक मूढ़ताओंका रूप समयानुसार बदलता रहता है।
धर्मके नामपर स्तूप निर्माणको प्रथाका आरम्भ बौद्धकालसे हुआ है बुद्धके अस्थि-अवशेषको स्तूपके भीतर रखा जाता था और इन स्तूपोंकी धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करनेके लिए पूजा की जाती थी। सम्राट अशोकने तथा उसके उत्तर वर्ती सम्राट् सम्प्रतिने स्तुप और अभिलेखोंका आरम्भ धार्मिक स्मृतिके साथ धर्म-प्रेरणाके लिए कराया। अशोकके नूप में सम्प्रमियरूप पोरन इस प्रकार मिश्रित हो गये हैं कि उनका पृथक्करण सहज सम्भव नहीं है। इसका प्रधान कारण यह है कि धर्म और सदाचारके सामान्य नियम इन दोनों सम्राटोंको समानरूपसे ही अभिप्रेत थे। ये स्तूप ठोस गुम्बदके आकारके होते थे और इनके ऊपर छत्र भी बनाये जाते थे। अशोक निर्मित स्तूपोंमें सांचीका स्तूप अत्यन्त प्रसिद्ध है। कुशाणकालके पूर्व बुद्धकी उपासना इन स्मारक चिन्होंमें प्रयुक्त प्रतीक रूपोंमें ही होती थी। छत्र, पांव, पुष्प, चन्द्र या चक्रके प्रतीकोंमें ही बुद्धकी स्मृति अन्तर्निहित थी। महायान सम्प्रदायके आविर्भावके पश्चात् बुद्ध-प्रतिमाओंके निर्माणकी प्रथाका आरम्भ हुआ।
जब स्तुपनिर्माणका महत्व जनसाधारणमें प्रचलित हुआ, तो स्तूपोंके प्रतिनिषिस्वरूप 'सिकताश्मनामुच्चयः'का प्रचार हुआ। बालू या कंकड़ोंका स्तूपाकार ढेर लगाकर देवकी उपासना होने लगी। यह प्रथा कुषाणकालके पूर्व तक प्रचलित रही। समन्तभद्रके समय में इसका बाहुल्य था। अतएव उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें इस प्रथाकी ओर संकेत किया है। कुषाणकालके पश्चात् कुछ ही शताब्दियोंमें मूर्तिकलाका विकास होनेसे उक्त मान्यता क्षीण हो गयी। अतएव रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें 'सिकताश्मनामुच्चयः'का जो प्रयोग आया है, वह उसको प्राचीनताका सूचक है।
गिरिपातप्रथाका निर्देश समन्तभद्रने किया है। सांस्कृतिकदृष्टिसे इस प्रथाका विकास और प्रसार ई. सन पूर्वकी शताब्दियोंसे ई. सन्की आरम्भिक शताब्दियों तक ही प्राप्त होता है। योग-क्रियाओंको सम्पादित करने में असमर्थ व्यक्ति गिरिपातद्वारा मुक्तिलाभ करता था। अतएव प्राचीन धर्मशास्त्रके लेखकोंने इस प्रथाकी समीक्षा की है। हरिभद्रकी 'समराइचकहा’ के द्वितीय भवमें भी यह प्रथा उल्लिखित है। अतः समन्तभद्रने लोकमूढ़ताका जो वर्णन किया है वह उनकी प्राचीनताका सूचक है।
समन्तभद्ने प्रथम अध्यायकी चौबीसवीं कारिकामें 'पाषण्डि-मूढ़ता' की समीक्षा की है। यह ‘पाषण्डी’ शब्द विचारणीय है। धर्मके अर्थमें इसका प्रयोग प्राचीन साहित्यमें ही उपलब्ध होता है। अशोकके अभिलेखोंके साथ आचार्य कुन्दकुन्दके समयसारमें भी इस शब्दका प्रयोग आया है। कुन्दकुन्दने लिखा है-
"पाखंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि।
चित्त वदंति मुढा लिंगमिणं मोक्खमग्गो ति।।"
"ण वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिहिमयाणि लिंगाणि।"
अशोकने भी गिरिनारके छठे अभिलेखमें 'पाषण्डि' शब्दका प्रयोग धर्म या सम्प्रदायके अर्थ में किया है। लिखा है- 'सब-पासंडापि मे पूजित विविधाय पूजाय' इससे स्पष्ट है कि 'पाषंड-मूढता' का निरूपण समन्तभद्रकी प्राचीनताका द्योतक है। आरम्भमें 'पाषंडी' शब्द पवित्रताके अर्थ में प्रचलित था, पर शनै:- शनै: इस शब्दका अर्थ अपकृर्षित होने लगा और यह आडम्बरपूर्ण जीवन व्यतीत करनेके अर्थमें प्रचलित हुआ।
जहाँ तक हमारा अध्ययन है पाँचवी, छठी शताब्दीके किसी भी साहित्यमें पाषंडीका प्रयोग धर्मके अर्थ में नहीं आया है। अतः समन्तभद्रके समयपर तो इससे प्रकाश पड़ता ही है, साथ ही रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्राचीनतापर भी प्रकाश पड़ता है।
एक अन्य विचारणीय विषय यह भी है कि मूढ़ताओंकी समीक्षा धम्मपद, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। धर्मशास्त्रके निर्माताओंने मूढ़ताओंकी समीक्षा ई. सन पूर्वसे ही आरम्भ कर दी थी। अतः समन्तभद्रको रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें इन मूढ़ताओंकी समीक्षाके लिये धम्मपदादि ग्रंथोंसे भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। समन्तभद्ने इनकी समीक्षा उसो शैलीमें की है जो शैली 'धम्मपद’ में मिलती है। अतः मूढ़ताओंके विवेचनसन्दर्भसे रत्नकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता प्राचीन समन्तभद्र ही सिद्ध होते हैं। 'धम्मपद' में बताया है-
"न नग्गचरिया न जटा न पंका नानासका थण्डिलसायिका वा।
रजोवजल्लं उककुटिकप्पधानं सोधेन्ति मच्चं अवितिण्ण कंखं।"
अर्थात् जिस पुरुषका सन्देह समाप्त नहीं हुआ है उसकी शुद्धि न नंगे रहनेसे, न जटासे, न कीचड़ लपेटनेसे, न उपवास करनेसे, न कठिन भूमि पर शयन करनेसे, न धूल लपेटनेसे और न उकडू बैठनेसे होती है।
लोक-मूढत्ताएँ विकसित होकर पांचवीं- छठी शताब्दीके साहित्यमें आडम्बरपूर्ण जीवनके विश्लेषणके रूपमें आयी हैं। अपभ्रंश साहित्यमें इन लोक-मूढ़ताओंका रूप बाह्याडम्बर या बाह्य वेशके रूप में उपस्थित है।
रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्राचीनताका एक सबल प्रमाण यह भी है कि इस ग्रन्थके कई पद्य मनुस्मृत्तिके वर्तमान संस्करणमें पाये जाते हैं। मनुस्मृतिका वर्तमान संस्करण ई. सन्की दूसरी-तीसरी शतीका है। यद्यपि यह संस्करण भी किसी प्राचीन मनुस्मृतिके आधार पर प्रस्तुत किया गया है, तो भी इसमें द्वितीय और तृतीय शतीकी अनेक रचनाओंके पद्य, वाक्यांश और पदांश उपलब्ध हैं। मनुस्मृति संग्रहग्रंथ है, इसका प्रमाण मनुस्मृतिमें भृगु द्वारा 'प्रोक्त वक्तव्यों’ का पद्यरूपमें निबद्ध करना है। श्रीपाण्डुरंग वामनकाणेने इसका संकलनकाल दूसरी शताब्दी माना है। तुलनाके लिए पद्य प्रस्तुत किये जाते हैं-
सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम।
देवा देवं विदुभंस्मगूढांगारान्तरोजसम्।।
सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिविण्णः।
पञ्चगुरुचरमशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्मः॥
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबद्धयते।
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते॥
इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यम्न चान्यथा।
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्माउँऽसंशया रुचिः॥
इदं शरणमज्ञानमिदमेव विजानताम्।
इदमन्विच्छतांस्वमिदमानन्त्यमिच्छताम्।।
अतएव विषयकी प्राचीनताकी दृष्टिसे रत्नकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता प्राचीन समन्तभद्र ही हैं। मनुस्मृति और रत्नकरण्डकश्रावकाचारके प्रकरणोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि रत्नकरण्डसे ही उक्त पद्य मनुस्मृति में संग्रहीत हैं। पद्योंमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है।
जीवसिद्धि, तत्त्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, प्रमाणपदार्थ, कर्मप्राभृतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य ये रचनाएं उपलब्ध नहीं है। अत: इनके सबन्धमें विवेचन करना संभाव नहीं। इन रचनाओंके केवल निर्देश ही जहाँ-तहाँ मिलते हैं। अतएव अब हम आचार्य समन्तभद्की काव्य-प्रतिमा एवं वैदुष्यपर प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं।
समन्तभद्र अत्यन्त प्रतिभाशाली और स्वसमय, परसमयके ज्ञाता सारस्वत हैं। इन्होंने एकान्तवादियोंका निरसन कर अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा दार्शनिक शैलीमें की है। भाव और अभावरूप विरोधी युगलधार्मोंको लेकर सप्तभंगात्मक वस्तुको सिद्ध किया है। क्रियाभेद, कारकभेद, पुण्य-पापरूप कर्मद्वैत, सुख-दुख-रूप फलद्वैत, इहलोक-परलोकरूप लोकद्वैत, विद्या-अविद्यारूप ज्ञानद्वैत और बन्ध-मोक्षरुप जीवकी शुद्धाशुद्ध अवस्थाओंका चित्रण किया गया है। बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शनोंकी मूल मान्यताओंका अध्ययन कर उनकी यथार्थ समीक्षा समन्तभद्रने की है। हम यहाँ उदाहरणके लिए वैशेषिकोंके परमाणुवादको लेते हैं। वैशेषिकोंमें कोई परमाणुओंमें पाक-अग्नि संयोग होकर द्वयणुकादि अवयवीमें क्रमशः पाक मानते हैं और कोई परमाणुओंमें किसी भी प्रकारकी विकृति न होनेसे उनमें पाक-अग्निसंयोग न मान कर केवल द्वयणुकादिमें पाक स्वीकार करते हैं। जो परमाणुओं में पाक नहीं मानते उनका कहना है कि परमाणु नित्य हैं और इसलिए वे द्वयणुकादि सभी अवस्थाओंमें एकरूप बने रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकारकी अन्यता नहीं होती, अपितु सर्वदा अनन्यता विद्यमान रहती है। इसी मान्यताको आचार्य समन्तभद्रने 'अणुओंका अनन्यतैकान्त' कहा है। इस मान्यतामें दोषोद्घाटन करते हुए बताया है कि यदि अणु द्वयणुकादि संघातदशामें भी उसी प्रकारके बने रहते हैं, जिस प्रकार वे विभागके समय है, तो वे असंहत ही रहेंगे और इस अवस्थामें अवयवीरूप पृथ्वी आदि चारों भूत भ्रान्त हो जायेंगे, जिससे अवयवीरूप कार्य भी भ्रान्त सिद्ध होगा। इस प्रकार वैशेषिकोंके अनन्यतैकान्तकी समीक्षा कर अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा की है।
समन्तभद्रकी कारिकाओंके अवलोकनसे उनका विभिन्न दर्शनोंका पाण्डित्य अभिव्यक्त होता है। प्रमाण, समायाफल, प्रमाणका निम पिच समन्तभद्रने बहुत ही सूक्ष्मतासे किया है। इन्होंने सद्-असद्वादकी तरह द्वेत अद्वैतवाद, शाश्वत-अशाश्वतवाद, वक्तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद, अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-बहिरर्थवाद, देव-पुरुषार्थवाद, पाप-पुण्यवाद और बन्ध-मोक्षकारणवादका विवेचन किया है।
डॉ. दरबारीलाल कोठियाने समन्तभद्र के उपादानोंका निर्देश करते हुए लिखा है कि उन्होंने जैनदर्शनको निम्नलिखित सिद्धान्त प्रदान किये हैं-
१. प्रमाणका स्वपराभासलक्षण
२. प्रमाणके क्रमभावि और अक्रमभावि भेदोंकी परिकल्पना
३. प्रमाणके साक्षात् और परम्परा फलोंका निरूपण
४. प्रमाणका विषय
५. नयका स्वरूप
६. हेतुका स्वरूप
७. स्याद्वादका स्वरूप
८. वाच्यका स्वरूप
९. वाचकका स्वरूप
१०. अभावका वस्तुधर्मनिरूपण एवं भावान्तरकथन
११. तत्वका अनेकान्तरूप प्रतिपादन
१२. अनेकान्तका स्वरूप
१३. अनेकान्तमें भी अनेकान्तकी योजना
१४. जैनदर्शनमें अवस्तुका स्वरूप
१५. स्यात् निपातका स्वरूप
१६. अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि
१७. युक्तियोंसे स्याद्वादकी व्यवस्था
१८. आप्तका तार्किक स्वरूप
१९. वस्तु-द्रव्य-प्रमेयका स्वरूप
काव्य-चमत्कारकी दृष्टिसे भी समन्तभद्र अपने क्षेत्रमें अद्वितीय हैं। इन्होंने चित्र और श्लेष काव्यका प्रारम्भ कर भारवि और माघके लिये काव्य-क्षेत्रका विकास किया है। कवि समन्तभद्रने अपने स्तोत्र-काव्योंमें शब्द और अर्थ इन दोनोंकी गम्भीरताका अपूर्व समन्वयं बनाये रखनेकी सफल चेष्टा की है। शब्द-संघति, अलंकार-वैचित्र्य, कल्पनासम्पत्ति एवं तार्किक प्रतिभाका समवाय एकत्र प्राप्य है। प्रबन्धकाच्य न लिखने पर भी कतिपय पद्योंमें प्रौढ़ प्रबन्धात्माकता पायी जाती है। इतिवृत्तात्मक धार्मिक तथ्योंका समावेश भी काव्य शैलीमें मनोरमरूपमें हुआ है। कविप्रतिभा और दार्शनिकताका मणि-कांचन संयोग श्लाघ्य है। उत्प्रेक्षाद्वारा आराध्य पद्मप्रभका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-
"शरीर-रश्मि-प्रसरः प्रभोस्तै बालार्क-रश्मिन्छविराऽऽलिलेप।
मराऽमराऽकोण सभा प्रभा वा शैलस्य पद्माभमणे: स्वसानुम्।।"
अर्थात् हे प्रभो ! प्रातःकालीन सूर्यकिरणोंकी छविके समान रक्तवर्णकी आभावाले आपके शरीरकी किरणोंके विस्तारने मनुष्य और देवताओंसे भरी हुई समवशरण सभाको इस प्रकार अलिप्त किया है, जैसे पद्मकान्तमणि पर्वतकी प्रभा अपने पाश्वंभागको आलिप्त करती है।
इस पद्यमें पद्मप्रभ तीर्थंकरकी रक्तवर्ण कान्ति द्वारा समवशरणसभाके व्याप्त किये जानेको उत्प्रेक्षा पद्यकान्तमणिके पर्वतकी प्रभासे की गयी है।
कवि समन्तभद्र उपमा-अलंकारके व्यवहारमें भी पटु हैं। उन्होंने भगवान् आदिनाथको अज्ञानान्धकारका विनाश करने के लिए चन्द्रमाका उपमान प्रदान किया है। कुछ पद्यों में प्रयुक्त उपमान नवीन प्रतीत होते हैं। यथा-
"येन प्रणीतं पृथु धर्म-तीर्थ ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम्।
गाङ्ग हृदं चन्दन-पड-शोतं गज-प्रवेका इव घर्मतप्ताः।।''
जिन्होंने उस महान् और ज्येष्ठ धर्मतीर्थका प्रणयन किया है, जिसका आश्रय पाकर भव्यजनं दुःख-सन्तापपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्यके सन्तापसे सन्तप्त हुए बड़े-बड़े हाथी चन्दनलेपके समान शीतल गङ्गाको प्राप्त कर सूर्यके आतापजन्य दुःखको मिटा डालते हैं।
यहाँ गंगाजलका उपमान चन्दनलेप है और धर्मतीर्थका उपमान गंगाजल है। जनका उपमान गज है। इस प्रकार इस पद्यमें संसार-आतापकी शान्तिके लिए धर्मतीर्थका सामर्थ्य विभिन्न उपमानों द्वारा दिखलाया गया है।
चन्द्रप्रभजिनकी स्तुति करते हुए उनको संसारका अद्वितीय चन्द्रमा कहा है तथा उपमा द्वारा आराध्यको रूपाकृतिका मनोरम चित्र अंकित किया है-
चन्द्रप्रभ चन्द्र-मरीचि-गौर चन्द्र द्वितीयं जगतोव कान्तम्।
वन्देऽभिवानद राहतामृषीन्द्र जिनं जित-स्वान्त-कषाय-बन्धम।
चन्द्रकिरणके समान गौरवर्णसे युक्त चन्द्रप्रभजिन जगत्में द्वितीय चन्द्रमाके समान दीप्तिमान हैं, जिन्होंने अपने अन्तःकरणके कषायबन्धनको जीत अकषायपद प्राप्त किया है और जो ऋद्विधारी मुनियोंके स्वामी तथा महात्माओं द्वारा वन्दनीय हैं।
इस पद्यमें 'चन्द्रमरीचिगौर' उपमान है, इस उपमान द्वारा चन्द्रप्रभतीर्थ करके गौरवर्ण शरीरकी आकृतिका सुन्दर अंकन किया है।
चन्द्रप्रभजिनके प्रवचनको सिंहका रूपक और एकान्तवादियोंको मदोन्मत्त गजका रूपक देकर कविने आराध्यके उपदेशकी महत्ता प्रदर्शित की है। इस प्रसंगमें रूपक-अलंकारकी योजना बहुत ही तर्कसंगत है। यथा-
"स्व-पक्ष-सोस्थित्य-मदाऽवलिप्ता वाकसिह-नादेविमदा वभूवुः।
प्रवादिनो यस्य मदार्दगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादैः।।"
जिनके प्रवचनरूप सिंहनादोंको सुनकर अपने मतकी सुस्थित्तिका घमण्ड रखनेवाले प्रवादिजन उसी प्रकार निर्मद हुए हैं, जिस प्रकार मद झरते हुए उन्मत्त हाथी केसरी- सिंहकी गर्जनाको सुनकर निर्मद हो जाते हैं।
चन्दन, चन्द्रकिरण, गंगाजल और मुक्ताओंकी हारयष्टीकी शीतलताका निषेध कर शीतलनाथ तीर्थंकरके वचनोंको आचार्य समन्तभद्रने शीतल सिद्ध किया है। प्रस्तुत सन्दर्भमै व्यतिरेक-अलंकार द्वारा उपमेयमें गुणाधिक्यका आरोप कर उपमानोंमें न्यून गुणका समावेश किया है। शीतलनाथ तीर्थंकरके सद्गुणोंका उत्कर्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुणत्व ही उत्कर्षापकर्षका आधार है। अत: तीर्थंकरकी अमृतवाणीको शीतलताका चरम साधन मानकर उपमानोंके साधारण धर्मसे आधिक्य दिखलाया गया है। वाणीमें शीतलता और माधुर्यके साथ अमृतत्व भी है, जिससे वह चन्दन, चन्द्रकिरण आदिकी अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करने की क्षमता रखती है। यथा-
"न शीतलाश्चन्दमचन्द्ररश्मयो न गाजमम्भो न च हारयष्ट्यः।
यथा मुनेस्तेऽनय! वाक्य-रश्मयःशमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चिताम्॥"
हे अनघ ! निरवद्य निर्दोष श्रीशीतलजिन ! आप जैसे प्रत्यक्षज्ञानी मुनिकी प्रशमजलसे आप्लावित वाक्यरश्मियां संसार-तापको दूर करने के हेतु उतनी शीतल हैं, जितनी न तो चन्द्रकिरणे शीतल हैं, न चन्दन है, न गङ्गाजल श्वीतल है और न मोतियोंकी हारयष्ट्रि ही। तात्पर्य यह है कि शीतलजिनकी अमृतवाणी चन्दन, चन्द्रकिरण, गङ्गाजल और मुक्ताहारष्टिसे अधिक शीतल और सुखप्रद है।
कविताका विषय हृदयकी अनुभूति है। अनुभूतिकी अवस्था में समस्त स्नायुमण्डल तदनुकूल रूप धारण करता है और उच्चरित वाक्यावलिमें अपूर्व प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। अनुभूतिके समयमें हृदयकी प्रधानत: दो अवस्थाएँ होती है। ये अवस्थाएं हैं- १. उल्लास और २. विह्वलता। कवि जब उल्लसित होता है, तो वह गाता है। यही कारण है कि स्तोत्रोंके समय में कविकी तन्मयता चरमसीमाको पहुँच जाती है। आराध्यके चरणोंमें वीतरागताकी प्राप्तिके लिए कवि अपनेको समर्पित कर देता है। भाव जहाँ उसके हृदयको उल्लसित और उद्वेलित करते हैं, वहाँ रमणीय वाक्यावलिके शब्द उसके हृदयको चमत्कारसे भर देते हैं।
चित्रकाव्यमें हृदयकी भावावस्था उतनी द्रवित नहीं होती, जितनी चमत्कारकी योजना होनेसे कोतुहल। अतएव संस्कृतकाव्यमें सर्वप्रथम चित्र, श्लेष और यमकका प्रादुर्भाव हुआ। भावावस्थामें स्थायित्व नहीं रहता है, यतः भाव क्षणभरमें उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, पर चमत्कृत्त दशा अधिक समय तक विद्यमान रहती है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियोंने भी वैदिक मन्त्रोंके प्रयोगमें शब्दरमणीयताको स्थान दिया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक प्रभृति अलंकारोंके साथ श्लेष और यमक भो उपलब्ध हैं।
स्वामी समन्तभदने स्तुतिविद्यामें हृदयको भावावस्थाको अधिक क्षणोंतक बनाये रखने के लिए शब्दोंको रम्यक्रिडाको स्थान दिया है। इसके बिना हृदयमें कौतूहलको स्थिति प्रबल अंगके साथ जागृत नहीं की जा सकती है। सवेदनाओंको शब्दोंकी रम्यताके गर्भसे प्रस्फुटितकर कौतूहल स्थिति तक पहुँचा देना है। आचार्य समन्तभद्रके चित्रबन्ध केवल शाब्दी रमणीयताका ही सृजन नहीं करते हैं, अपितु इनमें वक्रोक्ति और स्वभावोक्तियोंका चमत्कार भी निहित है।
'तकार' व्यज्जन द्वारा निम्नलिखित पद्यका गुम्फन किया है। श्लोकके प्रथमपादमें जो अक्षर हैं, वे ही सब अगले पादोंमें यत्र-तत्र व्यवस्थित हैं। साध्यरूपमें यहाँ शाब्दी क्रीडा नहीं है, अपितु साधनके रूप में है, जिससे शब्दचमत्कार "परिच्छित्ति’ की योजना द्वारा निमित हुआ है।
ततोतित्ता तु तेतीतस्तोतृतोतीतितोतुतः।
ततोतातिततोतोते ततता ते ततोततः।
हे भगवन् ! आपने ज्ञानावरणादि कर्मोको नष्ट कर केवलज्ञानादि विशेषगुणों को प्राप्त किया है, तथा आप परिग्रहहित स्वतन्त्र है। अतः आप पूज्य और सुरक्षित है। आपने ज्ञानावरणादि कर्मोके विस्तृत-अनादिकालिक सम्बन्धको नष्ट कर दिया है। अतः आपका विशालता-प्रभुता स्पष्ट है-आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं।
एक-एक व्यंजनके अक्षरक्रमसे प्रत्येक पादका ग्रंथन कर चित्रालकारकी योजना द्वारा भावाभिव्यक्ति की गयी है। यहाँ शब्दचमत्कारके साथ अर्थ चमत्कार भी प्राप्य है-
येयायायाययेयाय नानाननाननानन।
ममाममाममामामिताततीतिततोतितः।।
हे भगवन् ! आपका मोक्षमार्ग उन्हीं जीवोंको प्राप्त हो सकता है, जो कि पुण्यबन्धके सम्मुख हैं अथवा जिन्होंने पुण्यबन्ध कर लिया है। समवशरणमें आपके चार मुख दिखलाई पड़ते हैं। आप केवलज्ञानसे युक्त हैं तथा ममताभावसे-मोहपरिणामोंसे रहित है, तो भी आप सांसारिक बड़ी-बड़ी व्याधियोंको नष्ट कर देते हैं। हे प्रभो ! मेरे भी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दीजिए।
चन्द्रप्रभ और शीतलजिन स्तुति करते हुए मुजंबन्धोंकी योजनामें व्यतिरेक और श्लेष अलंकारको दिव्य आभाका मिश्रण उपलब्ध होता है-
"प्रकाशयन समुद्भूतस्त्वमुर्धाकलालयः।
विकासयन् समुद्भूतः कुमुदं कमलाप्रियः||"
हे प्रभो ! आप चन्द्ररूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा उदय होते ही आकाशको प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भी समस्त लोकाकाश और अलोकाकाशको प्रकाशित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार मुगलांछनसे युक्त है, उसी प्रकार आप भी मनोहर अर्द्धचन्द्रसे युक्त हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार सोलह कलाओंका आलय-गृह होता है, उसी तरह आप भी केवलज्ञानादि अनेक कलाओंके आलय-स्थान हैं। चन्द्रमा जिस तरह कुमुदों-नीलकुमुदोंको विकसित करता हुआ उदित होता है, उसी तरह आप भी पृथ्वीके समस्त प्रणियोंको आनन्दित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार कमलाप्रिय--कमलतृशात्रु होता है, उसी प्रकार आप भी कमलाप्रिय- केवलज्ञानादि लक्ष्मीके प्रिय है।
श्लेषके समान ही उपर्युक्त पद्यमें व्यतिरेक अलंकार भी है। इस अलंकारके प्रकाशमें चन्द्रमाकी अपेक्षा तीर्थंकर चन्द्रप्रभकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है। चन्द्रप्रभ गुणोंका उत्कर्ष और चन्द्रमामें अपकर्ष दिखलाया गया है।
श्रेयोजिनकी स्तुति में 'अर्द्धभ्रम'का प्रयोग किया है। इसमें औष्ठय वर्णोंका अभाव है, और चतुर्थ पादके समस्त अक्षरोंको अन्य तीन पादोंमें समाहित किया है-
"हरतीज्याहिता तान्ति रक्षार्थायस्य नेदिता।
तीर्थदिश्रेयसे नेताज्यायः श्रेयस्पयस्य हि॥"
कुछ ऐसे भी पद्य हैं, जिन्हें क्रमके साथ विपरीत क्रमसे भी पढ़ा जा सकता है, और विपरीत क्रमसे पढ़नेपर भिन्नार्थक पद्य ही बन जाता है। कविने स्वयं ही अनुलोम-प्रतिलोमक्रमसे श्लोकोंका प्रणयन किया है। यथा-
"रक्षमाक्षर वामेश शमी चारुरुचानुत:।
भो विमोनशनाजोरुनभ्रेन विजरामयः।।"
इसी पद्यको प्रतिलोमक्रमसे पढ़नेपर निम्नलिखित पद्य निर्मित होता है।
"यमराज विनम्रन रजोनाशन भो विभो।
तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर||"
शब्द और अर्थ चमत्कारके साथ नादानुक्रति भी विद्यमान है। विधायक कल्पना द्वारा आराध्यकी शरीराकृतिके साथ गुणोंका समवाय भी अभिव्यक्त हुआ है।
इस प्रकार आचार्य समन्तभद्रने जैनन्यायको तार्किकरूप प्रदान करनेके साथ संस्कृतकाव्यको निम्नलिखित तत्व प्रदान किये हैं-
१. चित्रालंकारका प्रारम्भ
२. श्लेष और यमकों द्वारा काव्यशैलीका उदात्तीकरण
३.शतककाव्यका सूत्रपात
४. स्तवनोंमें बाह्य चित्रणकी अपेक्षा अन्तरंग गुणों एवं अनेकान्तात्मक सिद्धान्तोंकी बहुलता
५. दर्शन और काव्यभावनाका मणि-कांचनसंयोग
आचार्य समन्तभद्रके उक्त काव्यतत्त्वोंका संस्कृतकाव्यतत्वोंपर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। जब संस्कृतकाव्यका प्रणयन मध्यदेशसे स्थानान्तरित हो गुजरात, कश्मीर और दक्षिणभारतमें प्रविष्ट हुआ, तो समन्तभद्रके काव्य सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित हो गये। भारविमें एकाएक चित्र और श्लेषका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, अपितु समन्तभद्रके काव्यसिद्धान्तोंका उनपर प्रभाव है। मलाबार निवासी वासुदेव कविने यमक और श्लेष सम्बन्धी जिन प्रसिद्ध काव्यों की रचना की है, उनके लिए वे शैलीके क्षेत्रम समन्तभद्रके ऋणी हैं। कवि कुज्जर द्वारा लिखित राघवपाण्डवीय पर भी समन्तभद्रकी शैलोका प्रभाव है। अत: संक्षेपमें दर्शन, आचार, तर्क, न्याय आदि क्षेत्रोंम प्रस्तुत किये गये ग्रंथोंकी दृष्टिसे समन्तभद्र ऐसे सारस्वताचार्य है, जिन्होंने कुन्दकुन्दादि आचार्योंके वचनोंको ग्रहण कर, सर्वज्ञकी वाणीको एक नये रूपमें प्रस्तुत किया है।
सारस्वताचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।
सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-
१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।
२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।
३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।
४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।
५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।
६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन ।
७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन ।
डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।
#samantbhadramaharaj
डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।
आचार्य श्री समन्तभद्र महाराजजी (प्राचीन)
| Name | Phone/Mobile 1 | Which Sangh/Maharaji/Aryika Ji you are associated with |
|---|
Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara_2.
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्ति रश्मयः।
वज्रन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलबोद्धता जनाः'।।
समन्तभद्रादिमहाकवीश्वराः कुवादिविद्याजयलब्धकीर्तयः।
सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकाक्षिणि।।
श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुम्मरसञ्चयम्।
मुनिवन्ध जनानन्दं नमामि वचनश्रिये॥
सारस्वताचार्योंमें सबसे प्रमुख और आद्य आचार्य समन्तभद्र है। जिस प्रकार गृद्धपिच्छाचार्य संस्कृतके प्रथम सूत्रकार है, उसी प्रकार जैन वांडमयमें स्वामी समन्तभद्र प्रथम संस्कृत-कवि और प्रथम स्तुतिकार हैं। ये कवि होनेके साथ प्रकाण्ड दार्शनिक और गम्भीर चिन्तक भी हैं। इन्हें हम श्रुतधर आचार्यपरम्परा और सारस्वत आचार्यपरम्पराको जोड़नेवाली अटूट श्रृंखला कह सकते हैं। इनका व्यक्तित्व श्रुतधर आचार्यो से कम नहीं है।
स्तोत्र-काव्यका सूत्रपात आचार्य समन्तभद्रसे ही होता है। ये स्तोत्र-कवि होने के साथ ऐसे तर्ककुशल मनीषी हैं, जिनकी दार्शनिक रचनाओंपर अकलंक और विद्यानन्द जैसे उदभट आचार्यों ने टीका और विवृत्तियों लिखकर मौलिक ग्रन्थ रचयिताका यश प्राप्त किया है| वीतरागी तीर्थकरकी स्तुतियोंमें दार्शनिक मान्यताओंका समावेश करना असाधारण प्रतिभाका ही फल है।
आदिपुराणमें आचार्य जिगोनने जन्हें वापद हामिल, कवित्व और गमकत्व इन चार विशेषणोंसे युक्त बताया है। इतना ही नहीं, जिनसेनने इनको कवि-वेधा कहकर कवियोंको उत्पन्न करनेवाला विधाता भी लिखा है-
कवीनां गमकानाञ्च वादिनां वाग्मिनामपि।
यशः सामन्तभद्रीयं मूनि चूडामधीयते।।
नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ।
यद्धचोवज्जपातेन निभिन्ना: कुमतादयः।।
मैं कवि समन्तभद्रको नमस्कार करता हूँ, जो कवियोंसे ब्रह्मा हैं, और जिनके वचनरूप वज्ज्रपातसे मिथ्यामतरूपी पर्वत चूर-चूर हो जाते हैं।
स्वतन्त्र कविता करनेवाले कवि, शिष्योंको मर्मतक पहुँचानेवाले गमक, शास्त्रार्थ करनेवाले वादी और मनोहर व्याख्यान देनेवाले वाग्मियोंके मस्तक पर समन्तभद्रस्वामीका यश चुडामणिके समान आचरण करनेवाला है| वादोभसिंहने अपने 'गद्यचिन्तामणि' ग्रन्थमें समन्तभद्रस्वामीकी तार्किक प्रतिमा एवं शास्त्रार्थ करनेकी क्षमताकी सुन्दर व्यंजना को है। समन्तभद्रके समक्षा बड़े-बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका महत्व समाप्त हो जाता था और प्रतिवादी मौन होकर उनके समक्ष स्तब्ध रह जाते थे।
सरस्वतीस्वैरविहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः।
जयन्ति वाग्वनिपातपाटितप्रतीपरादान्तमहीघ्रकोटयः।।
श्रीसमन्तभद्र मुनीश्वर सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि थे। उनके वचनरूपी वज्ज्रके निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चोटियाँ चूर-चूर हो गयी थीं। उन्होंने जिनशासनकी गौरवमयी पताकाको नीले आकाशमें फहरानेका कार्य किया था। परवादी-पंचानन बर्द्धमानसूरिने समन्तभद्रको 'महाकवीश्वर' और 'सुतर्कशास्त्रामृससागर' कहकर उनसे कवित्वशक्ति प्राप्त करनेकी प्रार्थना की है-
समन्तभद्रादिमहाकवारवराः कुवादिविद्याजयलब्धकोत्तयः।
सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांक्षिणि||
श्रवणबेलगोलाके शिलालेख न. १०५ में समन्तभद्र की सुन्दर उक्तियोंको वादीरुपी हस्तियोंको वश करनेके लिए वज्राकुंश कहा गया है तथा बतलाया है कि समन्तभद्र के प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी दुर्वादोंकी वार्तासे भी रहित हो गयी थी।
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभवज्राकुशसूक्तिजालः।
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वन्ध्यास दुव्र्वादुकवार्तयापि।।
स्यात्कारमुद्रित-समस्त-पदार्थपूर्णत्रैलोक्य-हम्मखिलं स खलु व्यक्ति।
दुव्वादुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं सामन्तभद्र-वचन-स्फुटरनदीपः।।
ज्ञानार्णवके रचयिता शुभचन्द्राचार्यने समन्तभद्रको 'कबीन्द्र- भास्वान' विशेषणके साथ स्मरण करते हुये उन्हें श्रेष्ठ कवीश्वर कहा है-
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरममयः।
वज्रन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलवोद्धता जनाः।।
अजितसेनका 'अलंकारचिन्तामणि' और ब्रह्म अजितके 'हनुमच्चरित्' एवं श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं. ५४ और अभिलेख नं. १०८ में समन्तभद्रका स्मरण महाकविके रूपमें किया गया है।
इस प्रकार जैन वाडमयमें समन्तभद्र पूर्ण तेजस्वी विज्ञान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादिविजेता और कविवेधके रूपमें स्मरण किये गये हैं। जैन धर्म और जैनसिदान्तके मर्मज विद्वान होनेके साथ तर्क, व्याकरण, छन्द, अलंकार एवं काव्य-कोषादि विषयोंमे पूर्णतया निष्णात थे। अपनी अलौकिक प्रतीभा द्वारा इन्होंने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्रायः समस्त विषयोंको आत्मसात् कर लिया था। संस्कृत, प्राकृत आदि विभिन्न भाषाओंके पारंगत विद्वान थे। स्तुतिविद्याग्रंथसे इनके शब्दाधिपत्यपर पूरा प्रकाश पड़ता है।
दक्षिण भारतमें उच्च कोटिके संस्कृत-ज्ञानको प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और प्रसारण देने वालोंमें समंतभद्रका नाम उल्लेखनीय है। आप ऐसे युगसंस्थापक हैं, जिन्होंने जैन विद्याके क्षेत्रमें एक नया आलोक विकीर्ण किया है। अपने समयके प्रचलित नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद,ब्रह्माद्वैतवाद, पुरुष एवं प्रकृतिवाद आदिकी समीक्षाकर स्यादवाद-सिद्धांतको प्रतिष्ठा की है। 'अलंकारचिन्तामणि’ में 'कविकुन्जर', 'मुनिबंध' और 'जनानन्द' आदि विशेषणों द्वारा अभिहित किया गया है। श्रवणबेल्गोला के शिलालेखोमी में तो इन्हें जीनशाषण प्रणेता और भद्र मूर्ती कहा गया है। इस प्रकार वाङ्मयसे समत्तभद्रके शास्त्रीय ज्ञान और प्रभाव का परिचय प्राप्त होता है।
समत्तभद्रका जन्म दक्षिमभारतमें हुआ था। इन्हें चोल राजवंशका राजकुमार अनुमित किया जाता है। इनके पिता उरगपुर (उरैपुर) के क्षत्रिय राजा थे। यह स्थान कावेरी नदीके तटपर फणिमण्डलके अंतर्गत अत्यंत समृद्धिशाली माना गया है। श्रवणबेलगोलाके दौरवलि जिनदास शास्त्रीके भण्डारमें पायी जाने वाली आप्तमीमांसाकी प्रतिके अतमें लिखा है- "इति फणिमंडलालंकारस्योरगपुराधिपसुनोः श्रीस्वामीसमन्तभद्रमुनेः कृतो आप्तमीमांसायाम्" इस प्रशस्ति वाक्यसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र स्वामीका जन्म क्षत्रियवंशमें हुआ था और उनका जन्मस्थान उरगपुर है। 'राजावलिकथे’ में आपका जन्म उत्कलिका ग्राममें होना लिखा है, जो प्रायः उरगपुरके अंतर्गत हो रहा होगा। आचार्य जुगलकिशोर मख्तारका अनुमान है कि यह उरगपुर उरैपुरका ही संस्कृत अथवा श्रुतमधुर नाम है, चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी थी। ‘त्रिचिनापोली’ का ही प्राचीन नाम उरयूर था। यह नगर कावेरीके तटपर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा ही समृद्धशाली जनपद था।
इनका जन्म नाम शांतिवर्मा बताया जाता है। 'स्तुतिविद्या' अथवा 'जिनस्तुतिशतम्’ में, जिसका अपर नाम जिनशतक' अथवा 'जिनशतकालंकार' है, "गत्वैकस्तुतमेव'' आदि पद्य आया है। इस पद्ममें कवि और काव्यका नाम चित्रबद्धरूपमें अंकित है। इस काव्यके छह आरे और नव वलय वाली चित्ररचना परसे 'शांतिवर्मकृतम्' और 'जिनस्तुतिशतम्' ये दो पद निकलते हैं। लिखा है- "षडरं नववलयं चक्रमालिख्य सप्तमवलये शांतिवर्मकृतं इति भवति।” "चतुर्थवलये जिनस्तुतिशतं इति च भवति अतः कवि-काव्यनामगर्भ चक्रवृत्तं भवति। इससे स्पष्ट है कि आचार्य समन्तभद्रने ‘जिनस्तुतिशतम्’ का रचयिता शांतिवर्मा कहा है, जो उनका स्वयं नामांतर संभव है। यह सत्य है कि यह नाम मुनि अवस्थाका नहीं हो सकता, क्योंकि वर्मान्त नाम मुनियोके नहीं होते। संभव है कि माता-पिताके द्वारा रखा गया यह समन्तभद्रका जन्मनाम हो। 'स्तुतिविद्या' किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित न होकर समन्तभद्रकी ही कृति मानी जाती है। टीकाकार महाकवि नरसिंहने- "ताकिकचूडामणि श्रीमत् समन्तभद्राचार्यविरचित" सूचित किया है और अन्य आचार्य और विद्वानोंने भी इसे समत्तभद्रकी कृति कहा है। अतएव समन्तभद्रका जन्मनाम शांतिवर्मा रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है।
मुनि-दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात् जब ये मणुवकहल्ली स्थानमें विचरण कर रहे थे कि उन्हें भस्मक व्याधि नामक भयानक रोग हो गया, जिससे दिगम्बर मुनिपदका निर्वाह उन्हें अशक्य प्रतीत हुआ। अतएव उन्होंने गुरुसे समाधिमरण धारण करनेको अनुमति मांगी| गुरुने भविष्णु शिष्यको बादेश देते हुए कहा- "आपसे धर्म और साहित्यकी बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं, अत: आप दीक्षा छोड़कर रोग-शमनका उपाय करें। रोग दूर होनेपर पुन: दीक्षा ग्रहण कर लें"। गुरुके इस आदेशानुसार समन्तभद्र रोगोपचारके हेतु नाग्यपदको छोड़कर सन्यासी बन गये और इधर-उधर विचरण करने लगे। पश्चात वाराणसीमें शिवकोटि राजाके भीमलिंग नामक शिवालयमें जाकर राजाको आर्शीवाद दिया और शिवजीको अर्पण किये जाने वाले नैवेद्यको शिवजीको ही खिला देनेकी घोषणा की। राजा इससे प्रसन्न हुआ और उन्हें शिवजीको नैवेद्य भक्षण करानेकी अनुमति दे दी। समन्तभन्न अनुमति प्राप्त कर शिवालयके किंवाड़ बन्द कर उस नैवेद्यको स्वयं ही भक्षण कर रोगको शांत करने लगे। शनैः शनै: उनकी व्याधिका उपशम होने लगा और भोगको सामग्री बचने लगी। राजाको इसपर सन्देह हुआ। अत्तः गुप्तरूपसे उसने शिवालयके भीतर कुछ व्यक्तियों को छिपा दिया। समन्तभद्रको नेवेद्यका भक्षण करते हुए छिपे व्यक्तियोंने देख लिया। समन्तभद्रने इसे उपसर्ग समझ कर चर्तुविशति तीर्थ करोंकी स्तुति आरंभ की। राजा शिवकोटिके डरानेपर भी समन्तभद्र एकाग्रचित्तसे स्तवन करते रहे, जब ये चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति कर रहे थे कि भीमलिंग शिवकी पिण्डी विदीर्ण हो गयी और मध्यसे चन्द्रप्रभ स्वामीका मनोज्ञ स्वर्णनिम्न प्रकट हो गया। समन्तभद्रके इस महात्म्यको देखकर शिक्कोटि राजा अपने भाई शिवायन सहित आश्चर्य चकित हुआ। समन्तभद्रने वर्धमान पर्यन्त चतुर्विशशति तीर्थंकरोंकी स्तुति पूर्ण हो जानेपर राजाको आशीर्वाद दिया।
यह कथानक 'राजाबलिकथे’ में उपलब्ध है। सेनगणकी पट्टावलिसे भी इस विषयका समर्थन होता है। पट्टावलिमें भीमलिंग शिवालयमें शिवकोटि राजाके समन्तभद्र द्वारा चमत्कृत्त और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है। साथ ही उसे नवतिलिंग देशका राजा सूचित किया है, जिसकी राजधानी सम्भवतः काञ्ची रही होगी। यहाँ यह अनुमान लगाना भी अनुचित नहीं है कि सम्भवत: यह घटना काशीकी न होकर काञ्चीको है। काञ्चीको दक्षिण काशी भी कहा जाता रहा है- "नर्वातलिंगदेशाभिरामद्राक्षाभिरामभोमलिङ्गस्चयन्वादिस्तोटकोस्कोरण ? रुद्रसान्द्रचदिकाविशदयशःश्रीचन्द्रजिनेन्द्रसइर्शनसमुत्पन्नकौतू हलकलितशिवकोटिमहाराजतपोराज्यस्थापकाचार्यश्रीमत्समन्तभद्रस्वामिनाम्”
इस तथ्यका समर्थन श्रवणबेलगोलाके एक अभिलेखसे भी होता है। अभिलेख में समन्तभद्र स्वामीके भस्मक रोगका निर्देश आया है। आपत्काल समाप्त होने पर उन्होंने पुनः मुनि-दीक्षा ग्रहण की। बताया है-
"वन्द्यो भस्मक-भस्म-सात्कृति-पटुः पद्मावतीदेवता-
दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभः।
आचार्यस्स समन्तभद्रगणभृधेनेह काले कली,
जैन वत्र्म समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तान्मुहः।।"
अर्थात् जो अपने भस्मक रोगको भस्मसात् करनेमें चतुर हैं, पद्मावती नामक देवीकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपने मन्त्रवचनोंसे चन्द्रप्रभको प्रकट किया और जिनके द्वारा यह कल्णाणकारी जैन मार्ग इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुभा, वे गणनायक आचार्य समन्तभद्र बार-बार वन्दना किये जाने योग्य हैं।
यह अभिलेख शक संवत् १०२२ का है। अतः समन्तभद्रकी भस्मक व्याधि की कथा ई. सन्के १०वी, ११वीं शताब्दी में प्रचलित रही है।
ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशमें भी शिवकोटि राजाका उल्लेख है। राजाके शिवालयमें शिव-नैवेद्यसे भस्मक-व्याधिकी शान्ति और चन्द्रप्रभजिनेन्द्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बका प्रादुर्भूत होना साथ-साथ वर्णित है। यह भी बताया गया है कि शिवकोधि महाराजने जिनदीक्षा भी धारण की थी।
ब्रह्मनेमिदत्तने शिवकोटिको काञ्चो अथवा नव तैलङ्ग देशका राजा न लिखकर वाराणसीका राजा लिखा है। भारतीय इतिहासके आलोडनसे न तो काशीके शिवकोटि राजाका ही उल्लेख मिलता है और न काञ्चीके ही।
प्रा. ए. चक्रवतीने पञ्चास्तिकायकी अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें बताया है कि काञ्चीका एक पल्लवराजा शिवस्कन्ध वर्मा था, जिसने 'मायदाबोलु' का दान-पत्र लिखाया है। इस राजाका समय विष्णुगोपसे पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी है। यदि यही शिवकोटि रहा हो, तो समन्तभद्र के साथ इसका सम्बन्ध घटित हो सकता है। 'राजाबलि कथे', 'पट्टावलि, एवं श्रवणबेलगोलाके अभिलेखमें शिवकोटिका निर्देश जिस रूपमें किया गया है उस रूपके अध्ययनसे उसके अस्तित्वसे इंकार नहीं किया जा सकता है।
ब्रह्म नेमिदत्तने समन्तभद्रकी कथामें काशीका उल्लेख किया है। पर यह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। कथाके ऐसे भी कुछ अंश है जो यथार्थ नहीं मालूम होते। कथामें आया है- "काञ्चोमें उस समय भस्मक व्याधिको नाश करनेके लिए स्निग्ध भोजनोंकी सम्प्राप्तिका अभाव था। अत: वे काञ्ची छोड़कर उत्तरकी ओर चल दिये। वे पुपड़ेन्द्रनगरमें पहुंचे। यहाँ बौद्धोंकी महती दानशाला देखकर उन्होंने बौद्ध भिक्षुका रूप धारण किया। पर जब वहाँ भी महाव्याधिका उपशम नहीं हुआ तो वे वहाँसे निकलकर अनेक नगरों में घूमते हुए दशपुर नगरमें पहुंचे। यहाँ भागवतोंका उन्नत मठ देखकर वे विशिष्ट आहारप्राप्तिकी इच्छासे बौद्ध भिक्षुका वेष त्याग वैष्णव संन्यासी बन गये। यहाँके विशिष्ट आहार द्वारा भी जब उनकी भस्मक व्याधि शान्त न हुई, तो वे नाना देशोंमें घूमते हुए वाराणसी पहुंचे और वहीं उन्होंने योगि-लिङ्ग धारण करके शिवकोटि राजाके शिवालयमें प्रवेश किया। यहां घी-दूध-दही-मिष्टान्न आदि नाना प्रकारके नेवेद्य शिवके भोगके लिए तैयार किये जाते थे। समन्त भद्रने शिवकोटि राजासे निवेदन किया कि वे अपनी दिव्यशक्ति द्वारा समस्त नेवेद्यको शिवको खिला सकते हैं। राजाका आदेश प्राप्त कर समन्तभद्रने मन्दिरके कपाट बन्द कर समस्त नैवेद्य स्वयं ग्रहण किया और आचमनके पश्चात् किवाड़ खोल दिये। राजा शिवकोटिको महान आश्चर्य हआ कि मनोंकी परिमाणमें उपस्थित किया गया नैवेद्य साक्षात् शिवने ही अवतरित होकर ग्रहण किया है। योगिराजकी शक्ति अपूर्व है, अतएव उनको शिवालयका प्रधान पुरोहित नियुक्त किया। समन्तभद्र प्रतिदिन नैवेद्य प्राप्त करने लगे और शनैः शनैः उनकी मस्मक व्याधि शान्त होने लगी। मन्दिरके प्रमुख पुरोहितोंने ईर्ष्यावश समन्तभद्रकी देखरेख की और राजाको सूचना दी कि तथाकथित योगि शिवको नैवेद्य न ग्रहण कराकर स्वयं नैवेद्य ग्रहण कर लेता है। राजाके आदेशानुसार एक दिन समन्तभद्रको भोजन करते हुए पकड़ लिया गया और उनसे शिवको नमस्कार करनेके लिए कहा। समन्तभद्रने उत्तर दिया, "रागी देषी देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता है। राजाने आज्ञा दी कि अपना सामर्थ्य दिखलाकर स्ववचनको सिद्ध करो।
रात्रिमें समन्तभद्रको वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, क्योंकि प्रातःकाल ही उनको अपनी परीक्षा उत्तीर्ण होना था। उनकी चिन्ताके कारण अम्बिका देवीका आसन कम्पित हुआ और वह दौड़कर समन्तभद्र के समक्ष उपस्थित हुई और उन्हें आश्वासन दिया। प्रात:काल होनेपर अपार भीड़ एकत्र हुई और समन्तभदने अपना स्वयंभूस्तोत्र आरम्भ किया। जिस समय वे चन्द्रप्रभ भगवानको स्तुति करते हा 'तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम्' यह वाक्य पढ़ रहे थे, उसी समय वह शिवलिङ्ग खण्ड-खण्ड हो गया और उसके स्थानपर चन्द्रप्रभ भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा प्रकट हुई। राजा शिवकोटि समन्तभद्रके इस महत्वको देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने समन्तभद्रसे उनका परिचय पूछा। समन्तभद्रने उत्तर देते हुए कहा-
"काच्या नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुलम्बिशे पाण्डुपिण्डः।
पुण्ड्रेण्डे शाक्यभिक्षुर्दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिवाट्।।
वाराणस्यामभूवं शशकरधवलः पाण्डुराङ्गस्तपस्वी।
राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिग्रन्थवादी।।"
मैं काञ्ची में नग्नदिगम्बर यत्तिके रूपमें रहा, शरीरमें रोग होनेपर पुण्डनगरीमें बौद्ध भिक्षु बनकर मैंने निवास किया। पश्चात् दशपुर नगरमें मिष्टान्न भोजी परिवाजक बनकर रहा। अनन्तर वाराणसी में आकर शैव तपस्वी बना। है राजन् ! मैं जैननिर्ग्रंथवादी-स्याद्वादी हूँ। यहाँ जिसकी शक्ति वाद करनेकी हो वह मेरे सम्मुख आकर वाद करे। द्वितीय पद्यमें आया है-
पुर्ण पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठपक-विषये काञ्चीपुरे वैदिशे।
प्राप्तोऽहं करहाटक बहुभट विद्योत्कटं ससूट
वादार्थी विचराम्यहन्नरपते शाई लविक्रीडितम्।।
मैंने पहले पाटलिपुत्र नगरमें वादकी भेरी बजाई। पुनः मालवा, सिन्ध देश, ढक्क-ढाका(बंगाल), काञ्चीपुर और वैदिश-विदिशा-भेलसाके आसपासके प्रदेशोंमें भेरी बजाई। अब बड़े-बड़े वीरोंसे युक्त इस करहाटक-कराड, जिला सतारा, नगरको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हे राजन् ! मैं वाद करनेके लिए सिंहके समान इतस्ततः क्रिड़ा करता फिरता हूँ।
राजा शिवकोटिको समन्तभद्रका चमत्कारक उक्त आख्यान सुनकर विरक्ति हो गयी और वह अपने पुत्र श्रीकण्ठको राज्य देकर प्रवजित हो गया। समन्तभद्रने भी गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त ले पुनः दीक्षा ग्रहण की।
ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकथा-कोषकी उक्त कथा प्रभाचन्द्र के गद्यात्मक लिखे गये कथाकोषके आधारपर लिखी गयी है। बुद्धिवादीकी दष्टिसे उक्स कथाका परीक्षण करनेपर समस्त तथ्य बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी इसना तो स्पष्ट है कि समन्तभद्रको भस्मक व्याधि हई थी और उसका शमन किसी शिवकोटिनामक राजाके शिवालयमें जानेपर हुआ था। हमारा अनुमान है कि यह घटना दक्षिण काशी अर्थात् काञ्चीकी होनी चाहिए।
समन्तभद्रको गुरु-शिष्यपरम्परा के सम्बन्धमें अभी सक निर्णीत रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। समस्त जैन वाडमय समन्तभद्रके सम्बन्ध में प्रशंसात्मक उक्तियां मिलती हैं। समन्तभद्र वर्धमान स्वामीके तीर्थको सहस्त्रगुनी वृद्धि करने वाले हुए और इन्हें श्रुतकेचलिऋद्धि प्राप्त थी। चन्नरायपट्टण ताल्लुकेके अभिलेख न. १४९में श्रुतकेवली-संतानको उन्नत करने वाले समन्त भद्र बताये गये हैं-
"श्रुतकेवलिगलु पलवरूप
अतीतर आद् इम्बलिक्के तत्सन्तानो
न्नतियं समन्तभद्र
वृतिपर् अलेन्दरू समस्तविद्यानिधिगल।।"
यह अभिलेख शक संवत् १०४७का है। इसमें समन्तभद्रको श्रुतकेलियोंके समान कहा गया है। एक अभिलेखमें बताया है कि श्रुतकेलियों और अन्य आचार्योंके पश्चात् समन्तभद्रस्वामी श्रीवर्धमानस्वामीके तीर्थकी सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए अभ्युदरको प्राप्त हुए।
"श्रीवर्धमानस्वामिगलु तीत्थंदोलु केवलिगलु ऋद्धीप्राप्तरुं श्रुतकेवलिगलुं पलरूं सिद्धसाध्यर् आगे तत्___त्यंमं सहस्त्रगणं माहि समन्तभद्र-स्वा मिगलु सन्दर___।"
इन अभिलेखोंसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि समन्तभद्र श्रुतधरोंकी परम्पराके आचार्य थे| इन्हें जो श्रुतपरम्परा प्राप्त हुई थी, उस श्रुतपरम्पराको इन्होंने बहुत ही वृद्धिगत किया।
विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके विद्वान् कवि हस्तिमल्ल और 'अय्यप्पार्यने' श्रीमूलसंघव्योसनेन्दु विशेषण द्वारा इनकी मूलसंघरूपी आकाशका चन्द्रमा बताया है। इससे स्पष्ट है कि समन्तभद्र मूलसंघके आचार्य थे।
श्रवणबेलगोलके अभिलेखोंसे ज्ञात होता है कि भद्रबाहू श्रुतकेवलीके शिष्य चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मुनिके वंशज पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्द मुनिराज, उनके वंशज गृद्धपिच्छाचार्य और गृद्धपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छाचार्य और उनके वंशज समन्तभद्र हुए। अभिलेख में बताया है-
"श्रीगृद्धपिच्छ-मुनिपस्य बलाकपिच्छ:
शिष्योऽजनिऽष्टभुवनत्रयत्तिकोतिः।
चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-मौलि-
माला-शिलीमुख-विराजितपादपनः।।
एवं महाचार्यपरम्परायां स्यात्कारमुद्राङ्किततत्वदोपः।
भद्रस्समन्ताद्गुणतो गणीशस्समन्तभद्रोऽजनि वादिसिंहः।।"
इन पद्योंसे विदित है कि समन्तभद्र कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छाचार्य आदि महान् आचार्योंकी परम्रामें हुए थे।
सेनगणकी पट्टावलीमें समन्तभद्रको सेनगणका आचार्य सूचित किया है। यद्यपि इस पट्टावलीमें आचार्योंकी क्रमबद्ध परम्परा अंकित नहीं की गयी है, तो भी इतना स्पष्ट है कि समन्तभद्रको उसमें सेनगणका आचार्य परिगणित किया है।
श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं. १०८ में नन्दिसेन आदि चार प्रकारके संघ भेदका भट्टाकलंकदेवके स्वर्गारोहणके पश्चात् उल्लेख है। परन्तु समन्तभद्र अकलंकदेवसे बहुत पहले हो चुके हैं। अकलंकदेवसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके गणोंका कोई उल्लेख भी दिखलाई नहीं पड़ता है। यद्यपि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार एवं अभिलेख नं. १०५में इन चारों संघोका प्रवर्तक अर्हदबलि आचार्यको लिखा है। पर श्रुतावतार अकलंकदेवसे पश्चात्ययर्ती रचना है।
तिरूमकूडल नरसिपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं. १०५में समन्तभद्रको द्रमिल संघके अन्तर्गत नन्दिसंघकी अरूंगल शाखाका विद्वान सूचित किया है।
अतः यह निश्चयपूर्वक कह सकना कठिन है कि समन्तभद्र अमुक गण या संघके थे। इतना तथ्य है कि समन्तभद्र गृद्धविच्छाचार्यके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' मंगलस्तोत्रमें स्तुत आप्तके मीमांसक होनेसे वे उनके तथा कुन्दकुन्दके अन्वयमें हुये है।
आचार्य समन्तभद्रके समयके सम्बन्धमें विद्धानोंने पर्याप्त उहापोह किया है। मि. लेविस राईसका अनुमान है कि समन्तभद्र ई. की प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें हुए हैं।
"कर्नाटक पानीले नामक ग्रंथके रचयिता आर नरसिंहाचार्यने समन्तभद्रका समय शक संवत् ६० (ई. सन् १३८) के लगभग माना है। उनके प्रमाण भी राईसके समान ही हैं।
श्रीयुत् एम. एस. रामस्वामी आयंगरने अपनी 'Studies in South Indian Jainism' नामक पुस्तक में लिखा है- "समन्तभद्र उन प्रख्यात दिगम्बर लेखकोंकी श्रेणीमें सबसे प्रथम थे, जिन्होंने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें महान् प्राधान्य प्राप्त किया।"
मध्यकालीन भारतीय न्यायके इतिहास (हिस्ट्री ऑफ दी मिडिझायल स्कूल ऑफ इण्डियन लाजिक) में डॉ. सतीशचन्द्र विद्याभूषणने यह अनुमान प्रकट किया है कि समन्तभद्र ई. सन् ६००के लगभग हुए हैं। उन्होंने अपने इस कथनके लिए कोई तर्क नहीं दिया। केवल इतना ही बतलाया है कि बौद्ध तार्किक धर्मकीर्तीका समकालीन कुमारिलभट्ट है और इनका समय ई. सन् सातवीं शताब्दी है। कुमारिलने समन्तभद्रका निर्देश किया है। अतः कुमारिलके पूर्व समन्तभद्रका समय मानना उचित है।
सिद्धसेनने अपने न्यायावतारमें समन्तभद्रके रत्नकरण्डकश्रावकाचारका निम्नलिखित पद्य उद्धत्त किया है.-
"आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमदृष्टेष्टविरोधकम्।
तत्त्वोपदेशकृतसाचं शास्त्रं कापथपट्टनम्॥"
इस पद्यको लेकर विवाद है। पंडिस सुखलालजीका मत है कि यह न्याया वतारका मुल पद्म है। वहींसे यह रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें गया है। पर विचार करनेसे यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। यतः रत्नकरण्डनावकाचारमें जिस स्थान पर यह पद्य आया है वहाँ वह क्रमबद्धरूपमें नियोजित है। समन्तभद्रने सम्यग्दर्शनकी परिभाषा हुये आप्त आजमगाम जोरजोतने सानो सम्यादर्शन कहा है। इस प्रसंगमें उन्होंने सर्व प्रथम आप्तका स्वरूप बतलाया है और तत्पश्चात् आगमका। शास्त्रका स्वरूप बतलाते हुए उक्तं पद्य लिखा है। इसके अनन्तर तपोभृतक स्वरूप बतलाया है। अतः क्रमबद्धताको देखते हुए उक्त पद्यका उद्भवस्थान समन्तभद्रका रत्नकरण्डश्रावकाचार है। वह अन्यत्र से उद्धूत नहीं है। परन्तु यह स्थिति न्यायावतारमें नहीं है। न्यायावतारमें स्वार्थानुमानका लक्षणनिरूपणके पश्चात् शाब्द- आगम प्रमाणका कथन करने के लिए एक पद्य, जिसमें शाब्दका पूरा लक्षण आ गया है, निबद्ध कर इस पद्यको उपस्थित किया है, जिसे वहाँसे अलग कर देनेपर ग्रन्थका भङ्ग भी नहीं होता। परन्तु रत्नकरण्डवावकाचारमें से उसे हटा देने पर ग्रंथ भङ्ग हो जाता है। अत: इस पद्यको न्यायाक्तारमें मूल ग्रन्थरचयिताका नहीं माना जा सकता है। न्यायावतारमें शब्दप्रमाणका लक्षण निम्न प्रकार है-
दुष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्परमार्थाभिधायिनः।
तत्वग्राहितयोत्पन्नं मान शाब्दं प्रकीतितम्।।
इस पद्मके पश्चात् ही उक्त आप्तोपज्ञ' आदि पद्य दिया है, जो व्यर्थ, पुनरूक्त और अनावश्यक है। आचार्य श्री जुगलकिशोरने अपने 'स्वामी समन्तभद्र' शीर्षक प्रबन्धमें विस्तारसे इसपर विचार किया है। अतएव न्यायावतारमें उल्लिखित उक्त पद्मके आधार पर समन्तभद्रको उसके कर्ता सिद्धसेनसे उत्तरवर्ती बतलाना समुचित नहीं है।
स्वामी समन्तभद्रके समयपर विचार करनेवाले जैन विचारकोंमें दो विचार धाराएँ उपलब्ध हैं। प्रथम विचारधाराके प्रवर्तक पंडित नाथरामजी प्रेमी हैं और उसके समर्थक डॉ. हीरालालजी आदि हैं। प्रेमीजीने स्वामी समन्तभद्रका समय छठी शताब्दी माना है। उनका तर्क है कि 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' मंगलाचरण सूत्रकार उमास्वामीका न होकर सर्वार्थसिद्धिटीकाकार देवनन्दि-पूज्यपादका है और इसी मंगलाचरणके आधार पर स्वामी समन्तभद्रने 'आप्तमीमांसा' नामक ग्रन्थकी रचना की है। अतएव इनका समय देवनन्दि पूज्यपाद (ई. ५वीं शती) के अनन्तर होना चाहिये। प्रेमीजीके इस मतका समर्थन कुछ मिन्न युक्तियों द्वारा आचार्य श्रीसुखलालजी संघवी एवं डॉ. महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य भी किया है। पति सुखलालमोने समन्तभद्रपर प्रसिद्ध बौद्ध तार्किक धर्मकीर्तीका प्रभाव अनुमित कर उनका समय धर्मकीर्तीके उपरान्त बतलाया है। पं. महेन्द्रकुमारजीने 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' मंगलाचरणको देवनन्दि-पूज्यपादका सिद्ध कर उसपर आप्तमीमांसा लिखनेवाले समन्तभद्रका समय उनके बाद अर्थात् छठी शताब्दी माना है।
किन्तु उल्लेखनीय है कि जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ९, किरण १ में 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ शीर्षकसे जो उन्होंने निबन्ध लिखा था और जिसके आधार पर आचार्य समन्तभद्रका उक्त छठी शताब्दी समय निर्धारित किया था, जिसका उल्लेख न्यायकुमुदचन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें किया था, उसपर डॉ. दरबारीलालजी काठियाने 'तत्वार्थसूत्रका मंगलाचरण' शर्षिक दो विस्तृत निबन्धों द्वारा 'अनेकान्त' वर्ष ५, किरण ६,७ तथा १०,११ में गहरा विचार करके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' मंगलस्तोत्रको तत्वार्थसूत्रकार आचार्य गृद्धपिच्छका सिद्ध किया है। फलतः डॉ. महेन्द्रकुमारजीने अपने पुराने विचारमें परिवर्तन कर समन्तभद्रका समय ‘सिद्धिविनिश्चयटीकाकी’ प्रस्तावना एवं 'जैन दर्शन' ग्रन्थोंमें ई. सन् द्वितीय शताब्दी स्वीकार कर लिया है, जो आचार्य मुख्तार आदि विद्वानोंकी दृढ़ मान्यता है।
आचार्य श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने समन्तभद्रके साहित्यका गम्भीर आलोचन कर उनका समय विक्रमकी द्वितीय शती माना है। इनके इस मतका समर्थन डॉ. ज्योति प्रसाद जैनने अनेक युक्तियोस किया है। उन्होंने लिखा है-स्वामी समन्तभद्रका समय १२०-१८५ ई. निर्णित होता है और यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म पूर्वतटवर्ती नागराज्य संघके अन्तर्गत उरगपूर (वर्तमान त्रिचनापल्ली)के नागवंशी चोल नरेश कीलिकवर्मनके कनिष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी सर्ववर्मन (शेषनाग) के अनुज राजकुमार शांतिवर्मनके रूपमें सम्भवतया ई. सन् १२०के लगभग हुआ था, सन् १३८ ई. (पट्टावलि प्रसत्त शक सं.६०)में उन्होंने मुनिदीक्षा ली और १८५ ई. के लगभग वे स्वर्गस्थ हुए प्रतीत होते हैं। अतएव समन्तभद्रका समय अनेक प्रमाणोंके आधार पर ईस्वी सनकी द्वितीय शती अवगत होती है।
इनके चित्रालंकार सम्बन्धी स्तुतिविद्याके आधार पर जो यह कहा जाता है कि समन्तभद्र अलंकृत काव्ययुगके कवि है और इनका समय भारनिके आस-पास मानना चाहिये। यह तर्क भी अधिक सबल नहीं है। एकाक्षरी या द्वयक्षरी या अन्य चित्रकाव्योंकी परम्परा वैदिक कालसे ही यत्त्किचित रूपमें प्राप्त होने लगती है। दक्षिण भारत में चित्रकाव्योंकी परम्परा बहुत प्राचीन समयसे चली जा रही है। समन्तभद्गने चित्रकाव्यका प्रयोग उसी परम्पराके आधारपर किया है। अत: उसके आधापर पर उनका समय अर्वाचीन बतलाना युक्त नहीं है। अतएव संक्षेपमें समन्तभद्रका समय ई. सन् द्वितीय शताब्दी है और ‘मोक्ष मार्गस्य नेतारं' को आचार्य विद्यानन्दने सुत्रकार गृद्धपिच्छका ही मंगलाचरण माना है, सर्वार्थसिद्धिकार पूज्यपाद देवनन्दिका नहीं।
संस्कृत काव्यका प्रारम्भ ही स्तुति-काव्यसे हुआ है। जिसप्रकार वैदिक ऋषियोंने स्वानुभूति-जीवनकी जीवन्तधारा और सौंदर्यभावनाको स्तुति काव्यकी पटभूमिपर ही अंकित किया है, उसीप्रकार स्वामी समन्तभद्रने भी दर्शन, सिद्धान्त एवं न्यायसम्बन्धी मान्यताओंको स्तुति-काव्यके माध्यमसे अभिव्यक्त किया है। अतएव स्तुतियोंकी विभिन्न परम्परामें आद्य जैन स्तुतिकार समन्तभद्रने बौद्धिक चिन्तन और मानवजीवनको प्रोज्जवल कल्पनाको स्तुति-कायके रूपमें हो मूर्तिमत्ता प्रदान की है। इनके द्वारा रचित स्तुतियों में तरल भावनाओंके साथ मस्तिष्कका चिन्तनभी समवेत है। समन्तमद्र द्वारा लिखित निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती हैं-
१. बृहत् स्वम्भूस्तोत्र
२. स्तुतिविद्या-जिनशतक
३. देवागमस्तोत्र-आसमीमांसा
४. युक्त्यनुशासन
५. रत्नकरण्डकश्रावकाचार
६. जीवसिद्धि
७. तस्वानुशासन
८. प्राकृतव्याकरण
९. प्रमाणपदार्थ
१०. कर्मप्राभृसटीका
११. गन्धहस्तिमहाभाष्य
१. बृहत् स्वम्भूस्तोत्र- इसका अपर नाम स्वम्भूस्तोत्र अथवा चातुर्विशांती स्तोत्र भी है। इसमें ऋषभदेवसे लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरोंकी क्रमशः स्तुतियां है। इस स्तोत्रके भक्तीरसमें गम्भीर अनुभूति एवं तर्कणायुक्त चिन्तन निबद्ध है। अतः इसे सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि कहा जा सकता है। इस 'स्तोत्र’ के संस्कृत टीकाकार प्रमाचन्द्रने इसे 'नि:शेषजिनोक्तधर्म' कहा है। इसमें कुल पद्योंकी संख्या निम्न प्रकार है-
१. श्रीऋषभजिन स्तवन, पद्य ५,
२. श्रीअजितजिन स्तवन, पद्य ५,
३. श्री सम्भवज्जीन स्तवन, पद्य ५,
४. श्रीअभिनन्दनजिन स्तवन पद्य ५,
५. श्रीसुमतिजिन स्तवन पद्य ५,
६. श्रीपद्मप्रभजिन स्तवन पद्य ५,
७. श्रासुपार्श्वजिन स्तवन पद्य ५,
८. श्रीचन्द्रप्रभजिन स्तवन पद्य ५,
९. श्रीसुविधजिन स्तवन पद्य ५,
१०. श्रीशीतलजिन स्तवन पद्य ५,
११, श्रीश्रेयोजिन स्तवन पद्य ५,
१२. श्रीवासुपूज्यजिन स्तवन पद्य ५,
१३. श्रीविमल जिनस्तवन पद्य ५,
१४. श्रीअनन्तजिन स्तवन पद्य ५.
१५.श्रीधर्मजिन स्तवन पद्य ५,
१६. श्रीशान्तिजिन स्तवन पद्य ५.
१७. श्रीकुंथुजिन स्तवन पद्य ५,
१८, श्रीअरजिन स्तवन पद्य २०,
१९ श्रीमल्लिजिन स्तवन पद्य, ५,
२० श्रीमुनिसुव्रतजिन स्तवन पद्य ५,
२१. श्रीनमिजिन स्तवन पद्य ५,
२२. श्रीअरिष्टनेमिजिन स्तवन पद्य १०,
२३. श्री पाश्वजिन स्तवन पद्य ५,
२४. श्रीवीरजिन स्तवन पद्य ८ = १४३।
इस स्तोत्रमें कविने प्रबन्ध-पद्धतिके बीजोंको निहित कर इतिवृत्त सम्बन्धी अनेक तथ्योंको प्रस्तुत किया है। प्रथम तीर्थंकरको प्रजापतिके रूप में असि, मषि, कृषि,सेवा, शिल्प और वाणिज्यका उपदेष्टा कहा है। इस स्तोत्रमें आये हुए ‘निर्दय भस्मसात्कियाम’ पदसे सम्मतः आचार्यने अपनी भस्मक व्याधिका संकेत किया है तथा सम्भवनाथको स्तुतिमें सम्भवजीनको वैद्यका रूपक देकर अपनी जीवनघटनाओंकी ओर संकेत किया है। इसी प्रकार “यस्याङ्ग-लक्ष्मो परिवेश भिन्न तमस्तमोरेखि रश्मिभिन्नम् पदसे राजा शिवकोटिके शिवालयमें घटित हुई घटनाका संकेत प्राप्त होता है।
समस्तभद्रने बाद (शास्त्रार्थ) द्वारा जैन सिद्धान्तोंका प्रचार किया था। श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोंके अनुसार पाटलिपुत्र, ढक्क, मालव, कांची आदि देशोंमें उन्होंने शास्त्रार्थ कर जिनसिद्धान्तोंकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। इस ओर भी उनका संकेत "स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदाऽवलिप्ता वाकसिह-नादेविमदा वभूवुः" पद्यांशसे मिलता है।
शान्तिनाथतीर्थकरने चक्रवर्तीत्वपद प्राप्त किया था और उन्होंने षट्खण्डकी दिग्विजयकर समस्त राजाओंको करद बनाया था। उनके राज्यकालमें प्रजा अत्यन्त सुखी और समृद्ध थी। इस बातकी सूचना निम्नलिखित पद्यांशोंसे प्राप्त होती है-
"चक्रण यः शत्रु-मवरण जित्वा नृप सर्व-नरेन्द्र-चक्रम्"
"विधाय रक्षा परतः प्रजानां राजा धीरं योऽप्रतिम-प्रतापः"
मल्लिजिन आजन्म ब्रह्मचारी थे। उनकी गणना बालयतियोंमें है। इसी प्रकार अरिष्ट नेमिको भी बालयति कहा गया है। इन दोनों तीर्थकरोंके स्तवन में 'महर्षी' या 'ऋषि' शब्दके प्रयोग आये हैं, जो इन तीर्थकरोंके बालयतित्वको अभिव्क्त करते हैं।
पार्श्वनाथस्तोत्रमें तीर्थकर पाश्वनाथके मुनिजीवनमें तपश्चर्या करते समय वेरी कमठ द्वारा किये उपसर्ग तथा पद्यावती और धरणेन्द्र द्वारा उसके निवारण का वर्णन निम्नलिखित पद्योंमें किया है-
"तमाल-नीलैः सघनुस्तडिद्गुणैःप्रकीर्ण-भीमाशनि-वायु-वृष्टिभिः।
बलाहकैवरि-वशैरुपद्रुतो महामना यो न चचाल योगतः॥
बृहत्फणा-मण्डल-मण्डपेन यं स्फुर-तरित्पिड-रुचोपसर्गिणम।
जुगूह नागो धरणो धराधरं विराग-संध्या-तडिदम्बुदो यथा।"
इस प्रकार इस स्तोत्र-काव्यमें प्रबन्धात्मक बीजसूत्र सर्वत्र विद्यमान हैं।
स्तोत्रसाहित्यका निर्माता वही सफल माना जाता है, जो स्तोत्रोंके मध्यमें प्रबन्धात्मक बीजोंकी योजना करता है, इस योजनासे स्तोत्र तो बनते ही हैं, साथ ही उनमें प्रेषणीयता विशेष उत्पन्न होती है। समन्तभदाचार्यने वैदिक मन्त्रोंके समान ही प्रबन्धगर्भित स्तोत्रोंका प्रणयनकर दार्शनिक और काव्यात्मक क्षेत्रमें नये चरणचिन्ह उपस्थित किये हैं।
वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, वसन्ततिलका, रथोद्धता, पथ्यावक्त्र-अनुष्टुप, सुभद्रिका-मालतीमिश्रित, वानवासिका, वेतासीय, शिखरिणी, उदगता एवं आर्यागीति इन तेरह प्रकारके छन्दोंका प्रयोग पाया जाता है। अलंकार-योजनाकी दृष्टिसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्सरन्यास, उदाहरण, दृष्टान्त एवं अन्योक्ति प्रभृति अलंकार उल्लेख्य हैं। अतिशयोक्तिका निम्न उदाहरण ध्यातव्य है-
तव रूपस्य सौन्दर्य दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्।
द्वयक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव वहु-विस्मयः।।
यहाँ भगवान के सौन्दर्यको दो नेत्रोंसे देखने में अतृप्तिका अनुभव करते हुए इन्दने सहत्र नेत्र धारणकर भगवानके रूप-सौन्दर्यका अवलोकन कर आश्चर्य प्राप्त किया है। इस संन्दर्भमें अतिशयोक्ति हैं।
सुखाभिलाषाऽनलदाहमूच्छित मनो निजं मानमयाऽमृत्ताम्बुभिः।
व्यविध्यपस्त्वं विषदाहमोहितं यथा भिषम्मन्त्रगुणैः स्वविग्रहम्।।
जिसप्रकार वैद्य विषदाहसे मुर्चीत हुए अपने शरीरको विषापहारमन्त्रके गुणोंसे उसकी अमोघशक्तियोंसे निर्दिष एवं मुर्चा रहित कर देता है, उसीप्रकार हे शोत्तलजिन ! आपने सांसारिक सुखोंकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूछित हुए अपने आत्माको ज्ञानमय अमृतके सिञ्चनसे मूच्छारहित-शान्त किया है।
स चन्द्रमा भव्यकुमुद्धतीनां विपन्नदोषाभ्रकलखुलेपः।
व्याकोश-याङ-न्याय-मयूखमाल: पूयात्पवित्रो भगवाम्मनो मे।।
यहाँ-'भव्यकुमुदतीनां' और 'दोषाभ्र-कलखु-लेपः' में रूपककी योजना है। इन रूपकोंने भावोंको सहज ग्राह्य तो बनाया ही है, साथ ही चन्द्रप्रभ भगवानके गुणोंका प्रभाव भी दिखलाया है। भव्यकुमुदनियोंको विकसित करनेके लिए चन्द्रप्रभ चन्द्रमा है।
पद्मप्रभः पद्यपलाश-लेश्यः पद्यालयालिजितचारुमूर्ती:।
बभौ भवान् भव्य-पयोरुहाणां पद्माकराणामिव पद्यबन्धुः।।
पद्ममत्रके समान द्रव्यलेश्याके धारक हे पद्मप्रभजिन! आपको सुन्दरमूर्ति पदमालय-लक्ष्मीसे आलिङ्गित रही है और आप भव्यकमलोंको विकसित करनेके लिए उसी तरह भासमान हुए हैं, जिसप्रकार सूर्य कमलसमूहका विकास करता हुआ सुशोभित होता है।
संक्षेपमें स्तोत्रकाव्यमें एकान्ततत्वकी समीक्षापूर्वक स्पाद्वादनयसे अनेकान्तामृततत्वको स्थापना की गयी है।
२. स्तुतिविद्या
जिनशतक और जिनशतकालंकार भी इसके नाम आये हैं। इसमें चित्रकाव्य और बन्धरचनाका अपूर्व कौशल समाहित है। शतककाव्योंमें इसकी गणना की गयी है। सौ पद्योमें किसी एक विषयसे सम्बद्ध रचना लिखना असाधारण बात मानी जातो थी। प्रस्तुत जिनशतकमें चौबीस तीर्थंकरोंकी चित्रबन्धोंमें स्तुति की गयी है। भावपक्ष और कलापक्ष दोनों नैतिक एवं धार्मिक उपदेशके उपस्कारक बनकर आये हैं। समन्तभद्रकी काव्यकला इस स्तोत्रमें आद्यन्त व्याप्त है। मुरजादि चक्रबन्धकी रचनाके कारण चित्र काव्यका उत्कर्ष इस स्तोत्रकाव्यमें पूर्णतया वर्तमान है।
समन्तभद्रकी इस कृतिसे स्पष्ट है कि चित्रकाव्यका विकास माघोत्तरकाल में नहीं हुआ, बल्कि माघ कविसे कई सौ वर्ष पूर्व हो चुका है। चित्र, श्लेष और यमकका समावेश वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता है, अत: यह सम्भव है कि दाक्षिणत्य भाषाओंके विशिष्ट सम्पर्कके कारण समन्तभद्रने चित्र-श्लेष और यमकका पर्याप्त विकास कर उक्त काव्यकी रचना की। इस कृतिमें मुरजबन्ध, अर्धभ्रम, गतप्रत्यागतार्घ, चक्रबन्ध, अनुलोम, प्रतिलोम क्रम एवं सर्वतोभद्र आदि चित्रोंका प्रयोग आया है। एकाक्षर पद्योंको सुन्दरता कलाकी दक्षिसे अत्यन्त प्रशंसनीय है।
कुछ विद्वानोंका इस कृतिको देखकर यह अनुमान है कि जिस कृत्रिम शैलीमें समन्तभद्रने स्तुतिविद्याका प्रमयन किया है वह कृत्रिम शैली ई. सनकी चौथी शताब्दीसे विकसित होती है। अत: कृत्रिम शैलीके कारण यह कृति द्वितीय-तृतीय शतीकी रचना नहीं हो सकती। विचार करनेपर उक्त मत निभ्रन्ति प्रतीत नहीं होता, यतः कृत्रिम शैलीके विकासका मूल कारण आर्यभाषाके साथ द्रविड भाषाका सम्पर्क है। द्राविड़-परिवारकी भाषाओंमें चित्र, श्लेष और चमकको अधिक क्षमता है। अत: समन्तभद्रने दाक्षिणात्य होनेके कारण ही इस शैलीका प्रयोग किया है।
इस स्तोत्रमें कुल ११६ पद्य हैं और अन्तिम पद्यमें "कविकाव्यनामगर्म- चक्रवृत्तम" है। जिसके बाहरके षष्ट वलयमें 'शान्तिवर्मकृतम्' और चतुर्थ वलयमें 'जिनस्तुतिशतम्' की उपलब्धि होती है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकका एक साथ प्रयोग काव्यकलाकी दृष्टिसे श्लाघनीय है। यहाँ उदाहरणार्थ काव्यलिंगको प्रस्तुत किया जा रहा है-
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यच्र्चनं चापि ते
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षि संप्रेक्षते।
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरा नतिपरं सेवेव्दशी येन ते
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृतो तेनैव तेजःपते॥
जिनेन्द्र भगवानकी आराधना करनेवाले मनुष्यकी आत्मा आत्मीय तेजसे जगमगा उठती है। वह सर्वोत्कृष्ट पुरुष गिना आने लगता है। तथा उसके महान पुण्यका बन्ध होता है। यहाँ स्मरण, पूजन, अञ्जलि-बन्धन, कथा-श्रवण, दर्शन आदिका क्रमशः नियोजन होनेसे परिसंख्या-अलंकार है। आचार्यने हेतु-वाक्यों का प्रयोग कर काव्यलिंगकी भी योजना की है। इस प्रकार यह स्तुति-विद्या स्तोत्र-काव्य और दर्शनगुणोंसे युक्त है। और है सविवेक भकि-रचना।
३. आप्तमीमांसा या देवागमस्तोत्र
स्तोत्रके रूपमें तर्क और आगमपरम्पराकी कसौटीपर आप्त-सर्वज्ञदेवकी मीमांसा की गयी है। समन्तभद्र अन्धश्रदालु नहीं हैं, वे श्रद्धाको तर्ककी कसौटीपर कसकर युक्ति-आगमद्वारा आप्तकी विवेचना करते हैं। आप्त विषयक मूल्यांकनमें सर्वज्ञाभाववादी मीमांसक, भावैकान्तवादी सांख्य, एकान्तपर्यायवादी बौद्ध एवं सर्वथा उभयवादी वैशेषिकका तर्कपूर्वक विवेचन करते हए निराकरण किया गया है। प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्साभावका सप्तभंगीन्यायद्वारा समर्थन कर वीरशासनकी महत्ता प्रतिपादित की है। सर्वथा अद्वैतवाद, द्वैतवाद, कर्मद्वैत, फलद्वैत, लोकद्वैत प्रभृतिका निरसन कर अनेकान्तात्मकता सिद्ध की गयी है। इसमें अनेकान्तवादका स्वस्थ स्वरूप विद्यमान है। उदाहरणके लिए-
"द्रव्यपर्यायोरेक्यं तयोरव्यतिरेकतः।
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावत:॥
संज्ञासंख्याविशेषाच्च स्वलक्षनविशेषतः।
प्रयोजनादिभेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा॥"
द्रख्य और पर्याय कथंचित् एक हैं, क्योंकि वे भिन्न उपलब्ध नहीं होते तथा वे कथंचित् अनेक हैं क्योंकि परिणाम, संज्ञा, संख्या, आदिका भेद है। देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदिको सिद्धि अनेकान्तके द्वारा हि होती है। एकान्त वादियोंको समस्त तपस्याओंका अनेकान्तवदके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
इस स्तोत्रमें ११५ पद्य हैं। 'देवागम' पदद्वारा स्तोत्रका आरम्भ होनेके कारण यह 'देवागम' स्तोत्र भी कहा जाता है। समन्तभद्रकी परीक्षाप्रधान दृष्टि इस स्तोत्रकाव्य में समाहित है। कवित्वकी दृष्टिसे यह काव्य बोझिल है। काव्य रस-दर्शनकी चट्टानके भीतर प्रवेश करनेपर ही क्वचित् प्राप्त होता है, अप्रस्तुत विधानका भी अभाव है। जीवन और जगतकी विभिन्न समस्याओंका समाधान इस स्तोत्रकाव्यमें अवश्य वर्तमान है।
४. युक्त्यनुशसन- वीरके सर्वोदय तीर्थका महत्व प्रतिपादित करने के लिए उनकी स्तुति की गयी है। युक्तिपूर्णक महावीरके शासनका मण्डन और विरुद्धमतोंका खण्डन किया गया है। समस्त जिनशासनको केवल १४ पद्योंमें ही समाविष्ट कर दिया है| अर्थगौरवकी दृष्टिसे यह काव्य उत्तम है, 'गागरमें सागर'को भर देनेकी कहावत चरितार्थ होती है। महावीरके तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा है-
"सर्वान्तवत्तद् गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मियोऽनपेक्षम्।
सर्वापदामन्तकरं निरन्सं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव॥"
इसप्रकार महावीरके तीर्थको ही समस्त विपत्तियोंका अन्त करनेवाला सर्वोदय तीर्थ कहा है।
५. रतनकरण्यश्रावकाचार- जीवन और आचारकी व्याख्या इस ग्रंथमें की गयी है। १५० पद्योंमें विस्तारपूर्वक सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक चारित्रका विवेचन करते हुए कुन्दकुन्दके निर्देशानुसार सल्लेखनाको श्रावकके व्रतोंमें स्थान दिया है। अन्तमें श्रावककी एकादश प्रतिमाएँ वर्णित है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवालने समोचीन धर्मशास्त्र- रत्नकरण्डश्रावकाधारको भूमिकामें लिखा है- "स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न केवल जैनमार्गको सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न किया है। (जैन वत्म समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तात् मुहः), किन्तु शुद्धमानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यको नैतिक धरातलपर प्रतिष्ठित करनेके लिए बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके इस दृष्टिकोणमें मानव-मात्रकी रुचि हो सकती है। समन्तभद्रकी दृष्टिमें मनकी साधना हृदयका परिवर्तन सच्ची साधना है। बाह्य आचार तो आडम्बरोंसे भरे भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना है कि मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है (कारिका-३३) किसीने चाहे चाण्डाल योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु यदि उसमें सम्यक् दर्शनका उदय हो गया है तो देवता ऐसे व्यक्तिको देव समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढंके हुए किन्तु अन्तरमें दहकते हुए अंगारकी तरह होता है।"
इस ग्रंथकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-
१. श्रावकके अष्टमूलगुणोंका विवेचन
२. अर्हतपूजनका वैयावृत्यके अन्तर्गत स्थान
३. व्रतोंमें प्रसिद्धि पानेवालोंके नामोल्लेख
४. मोही मुनिको अपेक्षा निर्मोही श्रावककी श्रेष्ठता
५. सम्यकदर्शनसम्पन्न मातंगको देवतुल्य कहकर उदार दृष्टिकोणका उपन्यास।
६.कुन्दकुन्द और उमास्वामीको श्रावकधर्म सम्बन्धी मान्यताओंको आत्मसातकर स्वतन्त्र रूपमें श्रावकधर्मसम्बन्धी ग्रंथका प्रणयन।
इस कृतिमें कर्ताके रूपमी सुमन्त्भद्रका कही भी उपलब्ध नहीं है। टीकाकार प्रभाचन्द्रने इसे समन्तभद्रकृत लिखा है। अत: डाॅ. हीरालाल जैन आप्तमीमांसामें निरूपित आप्तके लक्षणकी शैलीकी अपेक्षा इसकी शैलीमें भिन्नता प्राप्तकर और पार्श्वनाथचरितकी उत्थानिकामें योगीन्द्रकी रचनाके निर्देशको पाकर इसे योगीन्द्रदेवकी रचना मानते हैं। ग्रंथके उपान्त्य श्लोकमें 'बौतकलड’, विद्या' और 'सर्वार्थसिद्धि' शब्दोंको तत्तद् आचार्य और ग्रन्थोंका सूचक मानकर आठवीं-ग्यारहवीं शतीके मध्यकी रचना इसे स्वीकार करते हैं।
अतः डॉ. जैनके मतानुसार यह कृति आप्तमीमांसाके रचयिता स्वामी समन्तभद्रकी नहीं है। भले ही कोई दूसरा समन्तभद्र इसका रचयिता रहा हो। डॉ. साहबने उक्त मन्तव्यको प्रकट करनेके लिए एक निबन्ध अनेकान्त, वर्ष ८, किरण १-३. पृ. २६-३३, ८६-९० और १२५-१३२ में लिखा था, जिसका प्रतिवाद डॉ. प्रो. दरबारीलाल कोठियाने अनेकान्त वर्ष ८ किरण ४-५ में किया है। डॉ. कोठियाने डॉ. जैनके तर्कोका उत्तर देते हुए प्रस्तुत कृतिको आचार्य समन्तभद्रकी ही रचना सिद्ध किया है। मैं इस विवादमें न पड़कर इतना अवश्य कहूँगा कि समन्तभद्रके अन्य ग्रंथोंके समान इस ग्रन्थके भी दो नाम उपलब्ध हैं- १. समीचोन धर्मशास्त्र ओर २. वर्ण्य विषयके अनुसार रत्नकरण्डकश्रावकाचार। स्वामी समन्तभद्रकी यह शेली है कि वे अपने प्रत्येक ग्रन्थके दो नाम रखते हैं. प्रथम नामका निर्देश प्रथम पद्यके प्रारम्भिक वाक्यमें कर देते हैं और दूसरेका निर्देश ग्रंथके वर्ण्य विषयके आधारपर रहता है।
यह निर्विवाद सत्य है कि इस ग्रन्थमें प्रतिपादित विषय बहुत प्राचीन है। श्रुतधर कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुड, प्रवचनसार, दर्शनपाहुड, सीलपाहुड आदिसे विषयको सूत्ररूपमें ग्रहणकर नये रूपमें श्रावकाचारसम्बन्धी सिद्धान्तोंका प्रणयन किया है। अत: विद्वानोंके मध्य मूलगुणसम्बन्धी जो प्रश्न उठाया जाता है उसका समाधान यहाँ सम्भव है। जब समन्तभद्रने श्रावकाचारका प्रणयन नये रूपमें किया, तो उन्होंने बहुत्त-सी ऐसी बातोंको भी इस ग्रंथमें स्थान दिया, जो पहलेसे प्रचलित नहीं थीं। हमारा तो दृढ़ मत है कि तृतीय अध्याय की यह ६६ वीं कारिका प्रक्षिप्त है। पोछेके किसी विद्वान्ने प्रतिलिपि करते समय अहिंसाणुव्रतके विशुद्धयर्थ इस कारिकाको जोड़ दिया है। यहाँसे इसे हटा देनेपर भी ग्रंथके वर्ण्य विषयमें किसीप्रकारकी कमी नहीं आती। यह कारिका एक प्रकारसे विषयका पुनरुक्तीकरण ही करती है। मद्य, मांस, मधु के त्याग तथा पंचाणुव्रतोंके पालनको अष्टमूलगुण कहा गया है। अहिंसाणुव्रत के लक्षणमें संस्कारपूर्वक मन-वचन-काय, कृत, कारित, अनुमोदनारूप व्यापारसे द्वीन्द्रियादि प्राणियोंका घात न करना अहिंसाणुव्रत है। इस परिभाषाके अन्तर्गत मद्य, मांस, मधुका त्याग स्वयमेव समाविष्ट हो जाता है। पंचाणुव्रतोंकी चर्चा तो स्पष्टरूपसे पुनरुक्त है ही। अतएव वर्ण्य-विषयकी दृष्टिसे इस पद्यकी कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि आचार्य समन्तभन्द्रको अष्टमूलगुणोंका निर्देश करना अभीष्ट होता, तो वे इस पद्यको अहिंसाणुव्रतके लक्षणके आस-पास निबद्ध करते। अहिंसादि व्रतोंका पालन करनेवाले व्यक्तियोंके नामोल्लेखके पश्चात इस कारिकाका संयोजन अनुपयोगी जैसा प्रतीत होता है। यदि यह तर्क दिया जाय कि अणुव्रतोंका वर्णन करनेके पश्चात् मूलगुणोंका निर्देश आवश्यक था, तो यह तर्क भी बहुत सबल नहीं है। अणुव्रत और गुणव्रतोंके बीच इस पद्यका स्थान नहीं होना चाहिए। अतएव हमारी दृष्टिसे यह पद्य प्रक्षिप्त है।
अनेक आचार्योंने बताया है कि कोई नदी और समुद्रके स्नानको धर्म समझता है, कोई मिट्टी और पत्थरके स्तूपाकार ढेर बनाकर धर्मको इतिश्री मानता है। कोई पहाडसे कूदकर प्राणान्त कर लेने अथवा अग्निमें शरीरको जला देने में ही कल्याण मानता है । ये सब बातें लोकमूढ़ता है-
"आपगा-सागर-स्नानमुच्चयः सिकताऽश्मनाम्।
गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते।।"
उपयुक्त पद्यमें गतानुगतिक रूपसे अनुसरण किये जानेवाले मूढ़तापूर्ण दृष्टिकोणोंका विवेचन किया है और (१) आपगासागरस्नान, (२) सिकताऽ श्मनामुच्चयः, (३) गिरिपात, (४) अग्निपातको लोकमूढ़ता कहा है। भारतीय संस्कृतिके विकासक्रमका विचार करनेसे अवगत होता है कि उक्त ये चारों प्रथाएँ ई. सन्के पूर्व अत्यधिक रूपमें प्रचलित थीं। उत्तरकालमें इन प्रथाओंमेंसे एक-दोको छोड़कर शेष सभीका लोप हो गया। ऋग्वेदकालमें जीवन तथा जीवन भोगोंके प्रति आसक्तिकी प्रवृत्ति वर्तमान थी। अत: इस युगमें संन्यास और आत्मबलका निर्देश नहीं मिलता। प्रो. हिलब्रैटने दीक्षाविधिमें प्रयुक्त होनेवाले अग्निपातसे अग्निपात द्वारा आत्मबलिका अनुमान किया है। शतपथब्राह्मणमें बताया गया है कि पुरुषमेध गवं सर्वमेध्यत्रमें समस्त सम्पत्तिका त्याग कर साधक मृत्युका वरण करने के लिए बन जाता है। परिव्राजककी क्रियाओंका विवेचन करते हुए जाबालोपनिषदमें विभिन्न रूपोंमें किये जानेवाले आत्मघातोंको धार्मिक रूप दिया गया है-
'वीराध्वाने वा अनाशके वा अपां प्रवेशे बा अग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा।'
स्पष्ट है कि अग्निपात, जलपात और अनशनव्रतद्वारा आत्महत्या करना धार्मिक विधानमें शामिल किया गया है।
हिन्दी विश्वकोषमें आत्मघातोंका निरूपण करते हुए लिखा है कि वैध, अवैध, ज्ञानकृत और अज्ञानकृत ये चार भेद आत्मघातफे हैं। मनु एवं वृद्धगर्गने लिखा है कि जब मनुष्य अत्यन्त वृद्ध हो जाये और चिकित्सा करानेपर भी आरोग्यकी सम्भावना न हो, तो शौचादिक्रियाओंके लुप्त होने की आशंका उत्पन्न होनेसे, उच्च स्थानसे गिरकर, अग्निमें कूदकर, अनशनसे रहकर या जलमें डूबकर प्राण छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्राण छोडनेपर त्रिरात्रका अशौच माना जाता है।
उपर्युक्त सन्दर्भाशसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र द्वारा विवेचित लोक-मूढ़ताएं ब्राह्मण और उपनिषद् काल में प्रचलित थीं। धर्मशास्त्रोंके अशौच प्रकरणमें इन मान्यताओंका समावेश पाया जाता है।
'आपगासागरस्नान' की सांस्कृतिक व्याख्यामें प्रवेश करने पर ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ोंके प्राप्त भग्नवशेषोंमें उपलब्ध हुए स्नानागारोंसे हड़प्पाके सांस्कृतिक जीवनमें जलकी महत्ताका परिचय मिलता है। विद्वानोंने बताया है कि इसका आर्योंके सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। सरोवरों, नदियों और समुद्रोंके जलमें स्नान करनेकी प्रथा तथा सूर्योदयके पूर्व और भोजनके पूर्व स्नान करनेकी विधिपर धार्मिक मोहर इस बातका प्रमाण है कि सिन्धु घाटीकी सभ्यतामें भी स्नानको सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त था। आर्योंके जीवनमें नदियोंका नित्य बहता हुआ निर्मल जल ही उनके लिए स्वर्गकी पवित्रता एवं पावनताका परिचायक था। सिन्धु, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपासा, शत्तद्रु, यमुना, गंगा एवं ब्रह्मापुत्र आदि नदियोंने धार्मिक प्रेरणाके कारण ही आर्योंके जीवनको उर्वर बनाया था। अतएव नदियोंमें स्नान करनेको पवित्र भावनाके साथ उनमें डूबकर आत्मघात करनेकी प्रथा भी धर्मके नामपर ब्राह्मणकालमें प्रचलित थी। जलमात्रमें स्नान करना या असमर्थ अवस्थामें डूबकर प्राणघात करना धार्मिकताका चिह्न था । ई. पूर्व द्वितीय-तृतीय शताब्दीसे लेकर ई. सन प्रथम-द्वितीय शताब्दी तक इस प्रथाका बहुत प्रचार रहा है। जब संन्यासविधि पूर्णतया विकसित हो गयी, और आत्मशोधनके लिए ध्यान, संयमका मूल्य बढ़ गया, तो उक प्रथाका शनैः-शनैः ह्रास होने लगा। स्वामी समन्तभद्रके समय में इस प्रथाका जोर-शोरके साथ प्रचार था। अतः उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें इसकी समीक्षा की है। यहाँ यह स्मरणीय है कि लोक मूढ़ताओंका रूप समयानुसार बदलता रहता है।
धर्मके नामपर स्तूप निर्माणको प्रथाका आरम्भ बौद्धकालसे हुआ है बुद्धके अस्थि-अवशेषको स्तूपके भीतर रखा जाता था और इन स्तूपोंकी धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करनेके लिए पूजा की जाती थी। सम्राट अशोकने तथा उसके उत्तर वर्ती सम्राट् सम्प्रतिने स्तुप और अभिलेखोंका आरम्भ धार्मिक स्मृतिके साथ धर्म-प्रेरणाके लिए कराया। अशोकके नूप में सम्प्रमियरूप पोरन इस प्रकार मिश्रित हो गये हैं कि उनका पृथक्करण सहज सम्भव नहीं है। इसका प्रधान कारण यह है कि धर्म और सदाचारके सामान्य नियम इन दोनों सम्राटोंको समानरूपसे ही अभिप्रेत थे। ये स्तूप ठोस गुम्बदके आकारके होते थे और इनके ऊपर छत्र भी बनाये जाते थे। अशोक निर्मित स्तूपोंमें सांचीका स्तूप अत्यन्त प्रसिद्ध है। कुशाणकालके पूर्व बुद्धकी उपासना इन स्मारक चिन्होंमें प्रयुक्त प्रतीक रूपोंमें ही होती थी। छत्र, पांव, पुष्प, चन्द्र या चक्रके प्रतीकोंमें ही बुद्धकी स्मृति अन्तर्निहित थी। महायान सम्प्रदायके आविर्भावके पश्चात् बुद्ध-प्रतिमाओंके निर्माणकी प्रथाका आरम्भ हुआ।
जब स्तुपनिर्माणका महत्व जनसाधारणमें प्रचलित हुआ, तो स्तूपोंके प्रतिनिषिस्वरूप 'सिकताश्मनामुच्चयः'का प्रचार हुआ। बालू या कंकड़ोंका स्तूपाकार ढेर लगाकर देवकी उपासना होने लगी। यह प्रथा कुषाणकालके पूर्व तक प्रचलित रही। समन्तभद्रके समय में इसका बाहुल्य था। अतएव उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें इस प्रथाकी ओर संकेत किया है। कुषाणकालके पश्चात् कुछ ही शताब्दियोंमें मूर्तिकलाका विकास होनेसे उक्त मान्यता क्षीण हो गयी। अतएव रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें 'सिकताश्मनामुच्चयः'का जो प्रयोग आया है, वह उसको प्राचीनताका सूचक है।
गिरिपातप्रथाका निर्देश समन्तभद्रने किया है। सांस्कृतिकदृष्टिसे इस प्रथाका विकास और प्रसार ई. सन पूर्वकी शताब्दियोंसे ई. सन्की आरम्भिक शताब्दियों तक ही प्राप्त होता है। योग-क्रियाओंको सम्पादित करने में असमर्थ व्यक्ति गिरिपातद्वारा मुक्तिलाभ करता था। अतएव प्राचीन धर्मशास्त्रके लेखकोंने इस प्रथाकी समीक्षा की है। हरिभद्रकी 'समराइचकहा’ के द्वितीय भवमें भी यह प्रथा उल्लिखित है। अतः समन्तभद्रने लोकमूढ़ताका जो वर्णन किया है वह उनकी प्राचीनताका सूचक है।
समन्तभद्ने प्रथम अध्यायकी चौबीसवीं कारिकामें 'पाषण्डि-मूढ़ता' की समीक्षा की है। यह ‘पाषण्डी’ शब्द विचारणीय है। धर्मके अर्थमें इसका प्रयोग प्राचीन साहित्यमें ही उपलब्ध होता है। अशोकके अभिलेखोंके साथ आचार्य कुन्दकुन्दके समयसारमें भी इस शब्दका प्रयोग आया है। कुन्दकुन्दने लिखा है-
"पाखंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि।
चित्त वदंति मुढा लिंगमिणं मोक्खमग्गो ति।।"
"ण वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिहिमयाणि लिंगाणि।"
अशोकने भी गिरिनारके छठे अभिलेखमें 'पाषण्डि' शब्दका प्रयोग धर्म या सम्प्रदायके अर्थ में किया है। लिखा है- 'सब-पासंडापि मे पूजित विविधाय पूजाय' इससे स्पष्ट है कि 'पाषंड-मूढता' का निरूपण समन्तभद्रकी प्राचीनताका द्योतक है। आरम्भमें 'पाषंडी' शब्द पवित्रताके अर्थ में प्रचलित था, पर शनै:- शनै: इस शब्दका अर्थ अपकृर्षित होने लगा और यह आडम्बरपूर्ण जीवन व्यतीत करनेके अर्थमें प्रचलित हुआ।
जहाँ तक हमारा अध्ययन है पाँचवी, छठी शताब्दीके किसी भी साहित्यमें पाषंडीका प्रयोग धर्मके अर्थ में नहीं आया है। अतः समन्तभद्रके समयपर तो इससे प्रकाश पड़ता ही है, साथ ही रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्राचीनतापर भी प्रकाश पड़ता है।
एक अन्य विचारणीय विषय यह भी है कि मूढ़ताओंकी समीक्षा धम्मपद, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। धर्मशास्त्रके निर्माताओंने मूढ़ताओंकी समीक्षा ई. सन पूर्वसे ही आरम्भ कर दी थी। अतः समन्तभद्रको रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें इन मूढ़ताओंकी समीक्षाके लिये धम्मपदादि ग्रंथोंसे भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। समन्तभद्ने इनकी समीक्षा उसो शैलीमें की है जो शैली 'धम्मपद’ में मिलती है। अतः मूढ़ताओंके विवेचनसन्दर्भसे रत्नकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता प्राचीन समन्तभद्र ही सिद्ध होते हैं। 'धम्मपद' में बताया है-
"न नग्गचरिया न जटा न पंका नानासका थण्डिलसायिका वा।
रजोवजल्लं उककुटिकप्पधानं सोधेन्ति मच्चं अवितिण्ण कंखं।"
अर्थात् जिस पुरुषका सन्देह समाप्त नहीं हुआ है उसकी शुद्धि न नंगे रहनेसे, न जटासे, न कीचड़ लपेटनेसे, न उपवास करनेसे, न कठिन भूमि पर शयन करनेसे, न धूल लपेटनेसे और न उकडू बैठनेसे होती है।
लोक-मूढत्ताएँ विकसित होकर पांचवीं- छठी शताब्दीके साहित्यमें आडम्बरपूर्ण जीवनके विश्लेषणके रूपमें आयी हैं। अपभ्रंश साहित्यमें इन लोक-मूढ़ताओंका रूप बाह्याडम्बर या बाह्य वेशके रूप में उपस्थित है।
रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्राचीनताका एक सबल प्रमाण यह भी है कि इस ग्रन्थके कई पद्य मनुस्मृत्तिके वर्तमान संस्करणमें पाये जाते हैं। मनुस्मृतिका वर्तमान संस्करण ई. सन्की दूसरी-तीसरी शतीका है। यद्यपि यह संस्करण भी किसी प्राचीन मनुस्मृतिके आधार पर प्रस्तुत किया गया है, तो भी इसमें द्वितीय और तृतीय शतीकी अनेक रचनाओंके पद्य, वाक्यांश और पदांश उपलब्ध हैं। मनुस्मृति संग्रहग्रंथ है, इसका प्रमाण मनुस्मृतिमें भृगु द्वारा 'प्रोक्त वक्तव्यों’ का पद्यरूपमें निबद्ध करना है। श्रीपाण्डुरंग वामनकाणेने इसका संकलनकाल दूसरी शताब्दी माना है। तुलनाके लिए पद्य प्रस्तुत किये जाते हैं-
सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम।
देवा देवं विदुभंस्मगूढांगारान्तरोजसम्।।
सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिविण्णः।
पञ्चगुरुचरमशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्मः॥
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबद्धयते।
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते॥
इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यम्न चान्यथा।
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्माउँऽसंशया रुचिः॥
इदं शरणमज्ञानमिदमेव विजानताम्।
इदमन्विच्छतांस्वमिदमानन्त्यमिच्छताम्।।
अतएव विषयकी प्राचीनताकी दृष्टिसे रत्नकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता प्राचीन समन्तभद्र ही हैं। मनुस्मृति और रत्नकरण्डकश्रावकाचारके प्रकरणोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि रत्नकरण्डसे ही उक्त पद्य मनुस्मृति में संग्रहीत हैं। पद्योंमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है।
जीवसिद्धि, तत्त्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, प्रमाणपदार्थ, कर्मप्राभृतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य ये रचनाएं उपलब्ध नहीं है। अत: इनके सबन्धमें विवेचन करना संभाव नहीं। इन रचनाओंके केवल निर्देश ही जहाँ-तहाँ मिलते हैं। अतएव अब हम आचार्य समन्तभद्की काव्य-प्रतिमा एवं वैदुष्यपर प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं।
समन्तभद्र अत्यन्त प्रतिभाशाली और स्वसमय, परसमयके ज्ञाता सारस्वत हैं। इन्होंने एकान्तवादियोंका निरसन कर अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा दार्शनिक शैलीमें की है। भाव और अभावरूप विरोधी युगलधार्मोंको लेकर सप्तभंगात्मक वस्तुको सिद्ध किया है। क्रियाभेद, कारकभेद, पुण्य-पापरूप कर्मद्वैत, सुख-दुख-रूप फलद्वैत, इहलोक-परलोकरूप लोकद्वैत, विद्या-अविद्यारूप ज्ञानद्वैत और बन्ध-मोक्षरुप जीवकी शुद्धाशुद्ध अवस्थाओंका चित्रण किया गया है। बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शनोंकी मूल मान्यताओंका अध्ययन कर उनकी यथार्थ समीक्षा समन्तभद्रने की है। हम यहाँ उदाहरणके लिए वैशेषिकोंके परमाणुवादको लेते हैं। वैशेषिकोंमें कोई परमाणुओंमें पाक-अग्नि संयोग होकर द्वयणुकादि अवयवीमें क्रमशः पाक मानते हैं और कोई परमाणुओंमें किसी भी प्रकारकी विकृति न होनेसे उनमें पाक-अग्निसंयोग न मान कर केवल द्वयणुकादिमें पाक स्वीकार करते हैं। जो परमाणुओं में पाक नहीं मानते उनका कहना है कि परमाणु नित्य हैं और इसलिए वे द्वयणुकादि सभी अवस्थाओंमें एकरूप बने रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकारकी अन्यता नहीं होती, अपितु सर्वदा अनन्यता विद्यमान रहती है। इसी मान्यताको आचार्य समन्तभद्रने 'अणुओंका अनन्यतैकान्त' कहा है। इस मान्यतामें दोषोद्घाटन करते हुए बताया है कि यदि अणु द्वयणुकादि संघातदशामें भी उसी प्रकारके बने रहते हैं, जिस प्रकार वे विभागके समय है, तो वे असंहत ही रहेंगे और इस अवस्थामें अवयवीरूप पृथ्वी आदि चारों भूत भ्रान्त हो जायेंगे, जिससे अवयवीरूप कार्य भी भ्रान्त सिद्ध होगा। इस प्रकार वैशेषिकोंके अनन्यतैकान्तकी समीक्षा कर अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा की है।
समन्तभद्रकी कारिकाओंके अवलोकनसे उनका विभिन्न दर्शनोंका पाण्डित्य अभिव्यक्त होता है। प्रमाण, समायाफल, प्रमाणका निम पिच समन्तभद्रने बहुत ही सूक्ष्मतासे किया है। इन्होंने सद्-असद्वादकी तरह द्वेत अद्वैतवाद, शाश्वत-अशाश्वतवाद, वक्तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद, अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-बहिरर्थवाद, देव-पुरुषार्थवाद, पाप-पुण्यवाद और बन्ध-मोक्षकारणवादका विवेचन किया है।
डॉ. दरबारीलाल कोठियाने समन्तभद्र के उपादानोंका निर्देश करते हुए लिखा है कि उन्होंने जैनदर्शनको निम्नलिखित सिद्धान्त प्रदान किये हैं-
१. प्रमाणका स्वपराभासलक्षण
२. प्रमाणके क्रमभावि और अक्रमभावि भेदोंकी परिकल्पना
३. प्रमाणके साक्षात् और परम्परा फलोंका निरूपण
४. प्रमाणका विषय
५. नयका स्वरूप
६. हेतुका स्वरूप
७. स्याद्वादका स्वरूप
८. वाच्यका स्वरूप
९. वाचकका स्वरूप
१०. अभावका वस्तुधर्मनिरूपण एवं भावान्तरकथन
११. तत्वका अनेकान्तरूप प्रतिपादन
१२. अनेकान्तका स्वरूप
१३. अनेकान्तमें भी अनेकान्तकी योजना
१४. जैनदर्शनमें अवस्तुका स्वरूप
१५. स्यात् निपातका स्वरूप
१६. अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि
१७. युक्तियोंसे स्याद्वादकी व्यवस्था
१८. आप्तका तार्किक स्वरूप
१९. वस्तु-द्रव्य-प्रमेयका स्वरूप
काव्य-चमत्कारकी दृष्टिसे भी समन्तभद्र अपने क्षेत्रमें अद्वितीय हैं। इन्होंने चित्र और श्लेष काव्यका प्रारम्भ कर भारवि और माघके लिये काव्य-क्षेत्रका विकास किया है। कवि समन्तभद्रने अपने स्तोत्र-काव्योंमें शब्द और अर्थ इन दोनोंकी गम्भीरताका अपूर्व समन्वयं बनाये रखनेकी सफल चेष्टा की है। शब्द-संघति, अलंकार-वैचित्र्य, कल्पनासम्पत्ति एवं तार्किक प्रतिभाका समवाय एकत्र प्राप्य है। प्रबन्धकाच्य न लिखने पर भी कतिपय पद्योंमें प्रौढ़ प्रबन्धात्माकता पायी जाती है। इतिवृत्तात्मक धार्मिक तथ्योंका समावेश भी काव्य शैलीमें मनोरमरूपमें हुआ है। कविप्रतिभा और दार्शनिकताका मणि-कांचन संयोग श्लाघ्य है। उत्प्रेक्षाद्वारा आराध्य पद्मप्रभका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-
"शरीर-रश्मि-प्रसरः प्रभोस्तै बालार्क-रश्मिन्छविराऽऽलिलेप।
मराऽमराऽकोण सभा प्रभा वा शैलस्य पद्माभमणे: स्वसानुम्।।"
अर्थात् हे प्रभो ! प्रातःकालीन सूर्यकिरणोंकी छविके समान रक्तवर्णकी आभावाले आपके शरीरकी किरणोंके विस्तारने मनुष्य और देवताओंसे भरी हुई समवशरण सभाको इस प्रकार अलिप्त किया है, जैसे पद्मकान्तमणि पर्वतकी प्रभा अपने पाश्वंभागको आलिप्त करती है।
इस पद्यमें पद्मप्रभ तीर्थंकरकी रक्तवर्ण कान्ति द्वारा समवशरणसभाके व्याप्त किये जानेको उत्प्रेक्षा पद्यकान्तमणिके पर्वतकी प्रभासे की गयी है।
कवि समन्तभद्र उपमा-अलंकारके व्यवहारमें भी पटु हैं। उन्होंने भगवान् आदिनाथको अज्ञानान्धकारका विनाश करने के लिए चन्द्रमाका उपमान प्रदान किया है। कुछ पद्यों में प्रयुक्त उपमान नवीन प्रतीत होते हैं। यथा-
"येन प्रणीतं पृथु धर्म-तीर्थ ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम्।
गाङ्ग हृदं चन्दन-पड-शोतं गज-प्रवेका इव घर्मतप्ताः।।''
जिन्होंने उस महान् और ज्येष्ठ धर्मतीर्थका प्रणयन किया है, जिसका आश्रय पाकर भव्यजनं दुःख-सन्तापपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्यके सन्तापसे सन्तप्त हुए बड़े-बड़े हाथी चन्दनलेपके समान शीतल गङ्गाको प्राप्त कर सूर्यके आतापजन्य दुःखको मिटा डालते हैं।
यहाँ गंगाजलका उपमान चन्दनलेप है और धर्मतीर्थका उपमान गंगाजल है। जनका उपमान गज है। इस प्रकार इस पद्यमें संसार-आतापकी शान्तिके लिए धर्मतीर्थका सामर्थ्य विभिन्न उपमानों द्वारा दिखलाया गया है।
चन्द्रप्रभजिनकी स्तुति करते हुए उनको संसारका अद्वितीय चन्द्रमा कहा है तथा उपमा द्वारा आराध्यको रूपाकृतिका मनोरम चित्र अंकित किया है-
चन्द्रप्रभ चन्द्र-मरीचि-गौर चन्द्र द्वितीयं जगतोव कान्तम्।
वन्देऽभिवानद राहतामृषीन्द्र जिनं जित-स्वान्त-कषाय-बन्धम।
चन्द्रकिरणके समान गौरवर्णसे युक्त चन्द्रप्रभजिन जगत्में द्वितीय चन्द्रमाके समान दीप्तिमान हैं, जिन्होंने अपने अन्तःकरणके कषायबन्धनको जीत अकषायपद प्राप्त किया है और जो ऋद्विधारी मुनियोंके स्वामी तथा महात्माओं द्वारा वन्दनीय हैं।
इस पद्यमें 'चन्द्रमरीचिगौर' उपमान है, इस उपमान द्वारा चन्द्रप्रभतीर्थ करके गौरवर्ण शरीरकी आकृतिका सुन्दर अंकन किया है।
चन्द्रप्रभजिनके प्रवचनको सिंहका रूपक और एकान्तवादियोंको मदोन्मत्त गजका रूपक देकर कविने आराध्यके उपदेशकी महत्ता प्रदर्शित की है। इस प्रसंगमें रूपक-अलंकारकी योजना बहुत ही तर्कसंगत है। यथा-
"स्व-पक्ष-सोस्थित्य-मदाऽवलिप्ता वाकसिह-नादेविमदा वभूवुः।
प्रवादिनो यस्य मदार्दगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादैः।।"
जिनके प्रवचनरूप सिंहनादोंको सुनकर अपने मतकी सुस्थित्तिका घमण्ड रखनेवाले प्रवादिजन उसी प्रकार निर्मद हुए हैं, जिस प्रकार मद झरते हुए उन्मत्त हाथी केसरी- सिंहकी गर्जनाको सुनकर निर्मद हो जाते हैं।
चन्दन, चन्द्रकिरण, गंगाजल और मुक्ताओंकी हारयष्टीकी शीतलताका निषेध कर शीतलनाथ तीर्थंकरके वचनोंको आचार्य समन्तभद्रने शीतल सिद्ध किया है। प्रस्तुत सन्दर्भमै व्यतिरेक-अलंकार द्वारा उपमेयमें गुणाधिक्यका आरोप कर उपमानोंमें न्यून गुणका समावेश किया है। शीतलनाथ तीर्थंकरके सद्गुणोंका उत्कर्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुणत्व ही उत्कर्षापकर्षका आधार है। अत: तीर्थंकरकी अमृतवाणीको शीतलताका चरम साधन मानकर उपमानोंके साधारण धर्मसे आधिक्य दिखलाया गया है। वाणीमें शीतलता और माधुर्यके साथ अमृतत्व भी है, जिससे वह चन्दन, चन्द्रकिरण आदिकी अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करने की क्षमता रखती है। यथा-
"न शीतलाश्चन्दमचन्द्ररश्मयो न गाजमम्भो न च हारयष्ट्यः।
यथा मुनेस्तेऽनय! वाक्य-रश्मयःशमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चिताम्॥"
हे अनघ ! निरवद्य निर्दोष श्रीशीतलजिन ! आप जैसे प्रत्यक्षज्ञानी मुनिकी प्रशमजलसे आप्लावित वाक्यरश्मियां संसार-तापको दूर करने के हेतु उतनी शीतल हैं, जितनी न तो चन्द्रकिरणे शीतल हैं, न चन्दन है, न गङ्गाजल श्वीतल है और न मोतियोंकी हारयष्ट्रि ही। तात्पर्य यह है कि शीतलजिनकी अमृतवाणी चन्दन, चन्द्रकिरण, गङ्गाजल और मुक्ताहारष्टिसे अधिक शीतल और सुखप्रद है।
कविताका विषय हृदयकी अनुभूति है। अनुभूतिकी अवस्था में समस्त स्नायुमण्डल तदनुकूल रूप धारण करता है और उच्चरित वाक्यावलिमें अपूर्व प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। अनुभूतिके समयमें हृदयकी प्रधानत: दो अवस्थाएँ होती है। ये अवस्थाएं हैं- १. उल्लास और २. विह्वलता। कवि जब उल्लसित होता है, तो वह गाता है। यही कारण है कि स्तोत्रोंके समय में कविकी तन्मयता चरमसीमाको पहुँच जाती है। आराध्यके चरणोंमें वीतरागताकी प्राप्तिके लिए कवि अपनेको समर्पित कर देता है। भाव जहाँ उसके हृदयको उल्लसित और उद्वेलित करते हैं, वहाँ रमणीय वाक्यावलिके शब्द उसके हृदयको चमत्कारसे भर देते हैं।
चित्रकाव्यमें हृदयकी भावावस्था उतनी द्रवित नहीं होती, जितनी चमत्कारकी योजना होनेसे कोतुहल। अतएव संस्कृतकाव्यमें सर्वप्रथम चित्र, श्लेष और यमकका प्रादुर्भाव हुआ। भावावस्थामें स्थायित्व नहीं रहता है, यतः भाव क्षणभरमें उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, पर चमत्कृत्त दशा अधिक समय तक विद्यमान रहती है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियोंने भी वैदिक मन्त्रोंके प्रयोगमें शब्दरमणीयताको स्थान दिया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक प्रभृति अलंकारोंके साथ श्लेष और यमक भो उपलब्ध हैं।
स्वामी समन्तभदने स्तुतिविद्यामें हृदयको भावावस्थाको अधिक क्षणोंतक बनाये रखने के लिए शब्दोंको रम्यक्रिडाको स्थान दिया है। इसके बिना हृदयमें कौतूहलको स्थिति प्रबल अंगके साथ जागृत नहीं की जा सकती है। सवेदनाओंको शब्दोंकी रम्यताके गर्भसे प्रस्फुटितकर कौतूहल स्थिति तक पहुँचा देना है। आचार्य समन्तभद्रके चित्रबन्ध केवल शाब्दी रमणीयताका ही सृजन नहीं करते हैं, अपितु इनमें वक्रोक्ति और स्वभावोक्तियोंका चमत्कार भी निहित है।
'तकार' व्यज्जन द्वारा निम्नलिखित पद्यका गुम्फन किया है। श्लोकके प्रथमपादमें जो अक्षर हैं, वे ही सब अगले पादोंमें यत्र-तत्र व्यवस्थित हैं। साध्यरूपमें यहाँ शाब्दी क्रीडा नहीं है, अपितु साधनके रूप में है, जिससे शब्दचमत्कार "परिच्छित्ति’ की योजना द्वारा निमित हुआ है।
ततोतित्ता तु तेतीतस्तोतृतोतीतितोतुतः।
ततोतातिततोतोते ततता ते ततोततः।
हे भगवन् ! आपने ज्ञानावरणादि कर्मोको नष्ट कर केवलज्ञानादि विशेषगुणों को प्राप्त किया है, तथा आप परिग्रहहित स्वतन्त्र है। अतः आप पूज्य और सुरक्षित है। आपने ज्ञानावरणादि कर्मोके विस्तृत-अनादिकालिक सम्बन्धको नष्ट कर दिया है। अतः आपका विशालता-प्रभुता स्पष्ट है-आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं।
एक-एक व्यंजनके अक्षरक्रमसे प्रत्येक पादका ग्रंथन कर चित्रालकारकी योजना द्वारा भावाभिव्यक्ति की गयी है। यहाँ शब्दचमत्कारके साथ अर्थ चमत्कार भी प्राप्य है-
येयायायाययेयाय नानाननाननानन।
ममाममाममामामिताततीतिततोतितः।।
हे भगवन् ! आपका मोक्षमार्ग उन्हीं जीवोंको प्राप्त हो सकता है, जो कि पुण्यबन्धके सम्मुख हैं अथवा जिन्होंने पुण्यबन्ध कर लिया है। समवशरणमें आपके चार मुख दिखलाई पड़ते हैं। आप केवलज्ञानसे युक्त हैं तथा ममताभावसे-मोहपरिणामोंसे रहित है, तो भी आप सांसारिक बड़ी-बड़ी व्याधियोंको नष्ट कर देते हैं। हे प्रभो ! मेरे भी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दीजिए।
चन्द्रप्रभ और शीतलजिन स्तुति करते हुए मुजंबन्धोंकी योजनामें व्यतिरेक और श्लेष अलंकारको दिव्य आभाका मिश्रण उपलब्ध होता है-
"प्रकाशयन समुद्भूतस्त्वमुर्धाकलालयः।
विकासयन् समुद्भूतः कुमुदं कमलाप्रियः||"
हे प्रभो ! आप चन्द्ररूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा उदय होते ही आकाशको प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भी समस्त लोकाकाश और अलोकाकाशको प्रकाशित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार मुगलांछनसे युक्त है, उसी प्रकार आप भी मनोहर अर्द्धचन्द्रसे युक्त हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार सोलह कलाओंका आलय-गृह होता है, उसी तरह आप भी केवलज्ञानादि अनेक कलाओंके आलय-स्थान हैं। चन्द्रमा जिस तरह कुमुदों-नीलकुमुदोंको विकसित करता हुआ उदित होता है, उसी तरह आप भी पृथ्वीके समस्त प्रणियोंको आनन्दित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार कमलाप्रिय--कमलतृशात्रु होता है, उसी प्रकार आप भी कमलाप्रिय- केवलज्ञानादि लक्ष्मीके प्रिय है।
श्लेषके समान ही उपर्युक्त पद्यमें व्यतिरेक अलंकार भी है। इस अलंकारके प्रकाशमें चन्द्रमाकी अपेक्षा तीर्थंकर चन्द्रप्रभकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है। चन्द्रप्रभ गुणोंका उत्कर्ष और चन्द्रमामें अपकर्ष दिखलाया गया है।
श्रेयोजिनकी स्तुति में 'अर्द्धभ्रम'का प्रयोग किया है। इसमें औष्ठय वर्णोंका अभाव है, और चतुर्थ पादके समस्त अक्षरोंको अन्य तीन पादोंमें समाहित किया है-
"हरतीज्याहिता तान्ति रक्षार्थायस्य नेदिता।
तीर्थदिश्रेयसे नेताज्यायः श्रेयस्पयस्य हि॥"
कुछ ऐसे भी पद्य हैं, जिन्हें क्रमके साथ विपरीत क्रमसे भी पढ़ा जा सकता है, और विपरीत क्रमसे पढ़नेपर भिन्नार्थक पद्य ही बन जाता है। कविने स्वयं ही अनुलोम-प्रतिलोमक्रमसे श्लोकोंका प्रणयन किया है। यथा-
"रक्षमाक्षर वामेश शमी चारुरुचानुत:।
भो विमोनशनाजोरुनभ्रेन विजरामयः।।"
इसी पद्यको प्रतिलोमक्रमसे पढ़नेपर निम्नलिखित पद्य निर्मित होता है।
"यमराज विनम्रन रजोनाशन भो विभो।
तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर||"
शब्द और अर्थ चमत्कारके साथ नादानुक्रति भी विद्यमान है। विधायक कल्पना द्वारा आराध्यकी शरीराकृतिके साथ गुणोंका समवाय भी अभिव्यक्त हुआ है।
इस प्रकार आचार्य समन्तभद्रने जैनन्यायको तार्किकरूप प्रदान करनेके साथ संस्कृतकाव्यको निम्नलिखित तत्व प्रदान किये हैं-
१. चित्रालंकारका प्रारम्भ
२. श्लेष और यमकों द्वारा काव्यशैलीका उदात्तीकरण
३.शतककाव्यका सूत्रपात
४. स्तवनोंमें बाह्य चित्रणकी अपेक्षा अन्तरंग गुणों एवं अनेकान्तात्मक सिद्धान्तोंकी बहुलता
५. दर्शन और काव्यभावनाका मणि-कांचनसंयोग
आचार्य समन्तभद्रके उक्त काव्यतत्त्वोंका संस्कृतकाव्यतत्वोंपर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। जब संस्कृतकाव्यका प्रणयन मध्यदेशसे स्थानान्तरित हो गुजरात, कश्मीर और दक्षिणभारतमें प्रविष्ट हुआ, तो समन्तभद्रके काव्य सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित हो गये। भारविमें एकाएक चित्र और श्लेषका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, अपितु समन्तभद्रके काव्यसिद्धान्तोंका उनपर प्रभाव है। मलाबार निवासी वासुदेव कविने यमक और श्लेष सम्बन्धी जिन प्रसिद्ध काव्यों की रचना की है, उनके लिए वे शैलीके क्षेत्रम समन्तभद्रके ऋणी हैं। कवि कुज्जर द्वारा लिखित राघवपाण्डवीय पर भी समन्तभद्रकी शैलोका प्रभाव है। अत: संक्षेपमें दर्शन, आचार, तर्क, न्याय आदि क्षेत्रोंम प्रस्तुत किये गये ग्रंथोंकी दृष्टिसे समन्तभद्र ऐसे सारस्वताचार्य है, जिन्होंने कुन्दकुन्दादि आचार्योंके वचनोंको ग्रहण कर, सर्वज्ञकी वाणीको एक नये रूपमें प्रस्तुत किया है।
सारस्वताचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।
सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-
१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।
२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।
३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।
४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।
५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।
६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन ।
७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन ।
Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara_2.
Acharya Shri Samantbhadra Maharaj Ji
#samantbhadramaharaj
15000
Acharya Shri Samantbhadra Maharajji (Prachin)
#samantbhadramaharaj
samantbhadramaharaj
You cannot copy content of this page