हैशटैग
#Gunadharmaharajji

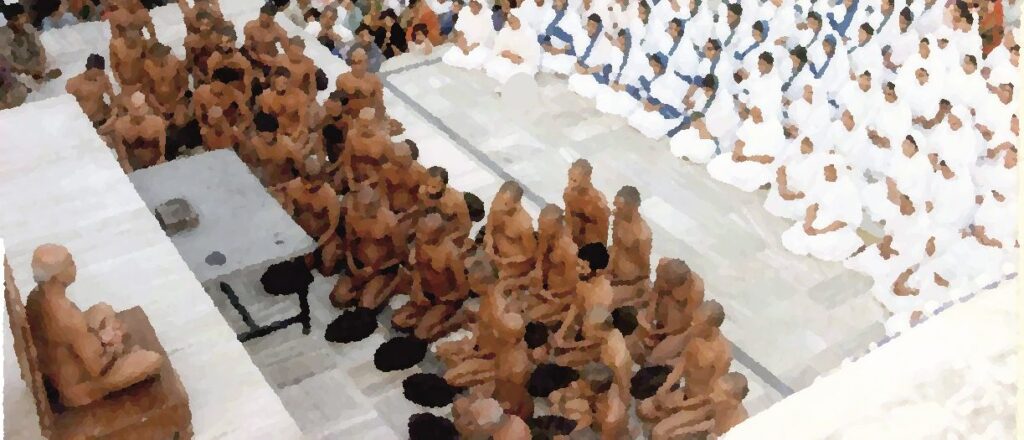
| Title | _hashtag | Year | Chaturmas Status | State | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Muni Shri 108 Sajagsagarji Maharaj | #SajagsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Muni Shri 108 Vibodh Sagarji Maharaj | #VibodhsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Morena |
| Muni Shri 108 Mahat Sagarji Maharaj | #MahatsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Muni Shri 108 Vibhor Sagarji Maharaj | #VibhorsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Muni Shri 108 Sanandsagarji Maharaj | #SanandsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Aryika Shri 105 Sukhadshri Mataji | #SukhadshrijiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Kshullak Shri 105 Shantigupt Ji Maharaj | #ShantiguptjiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Kshullika Shri 105 Dhanyashri Mataji | #DhanyashrijiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Kshullika Shri 105 Thirthshri Mataji | #ThirthshrijiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Acharya Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj | #KunthuSagarJiMaharajAcharyaShriMahavirKirtiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Acharya Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1941 | #SambhavSagarJiMaharaj1941MahavirkirtiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Pulak Sagar Ji Maharaj 1970 | #PulakSagarJiMaharaj1970PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Acharya Shri 108 Saurabh Sagarji Maharaj 1970 | #SaurabhSagarjiMaharaj1970PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttarakhand | Dehradun |
| Acharya Shri 108 Pramukh Sagarji Maharaj-1973 | #PramukhSagarJiMaharaji1973PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Muni Shri 108 Arunsagarji Maharaj-1963 | #ArunsagarJi-1963PuspdantSagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Devband |
| Muni Shri 108 Pragalbh Sagarji Maharaj 1960 | #PragalbhSagarJiMaharaj1960PuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prasang Sagarji Maharaj-1982 | #PrasangSagarJiMaharaj1982PushpadantaSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Hassan |
| Muni Shri 108 Pranam Sagarji Maharaj-1972 | #MuniShriPranamSagarjiMaharaj1972PushpadantaSagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Praneet Sagar Ji Maharaj | #PraneetSagarJiMaharajPuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullak Shri 105 Parv Sagarji Maharaj | #ParvSagarJiMaharajPuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Devas |
| Kshullika Shri 105 Prashantshri Mataji | #PrashantshriMataJiPuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Devas |
| Acharya Shri 108 Siddhant Sagar Ji Maharaj 1966 | #SiddhantSagarJiMaharaj1966SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Acharya Shri 108 Saubhagya Sagar Ji Maharaj 1965 | #SaubhagyaSagarJiMaharaj1965SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Muni Shri 108 Navinandiji Sagar Ji Maharaj 1977 | #NavinandijiSagarJiMaharaj1977SiddhantSagarJi | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Muni Shri 108 Suveer Sagarji Maharaj-1986 | #SuveerSagarJiMaharaj1986SanmatiSagarJi | 2025 | Maharashtra | Amravati | |
| Acharya Shri 108 Subal Sagarji Maharaj 1976 | #SubalSagarJiMaharaj1976AcharyaSriSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Shrestha Sagar Ji Maharaj 1961 | #ShresthaSagarJiMaharaj1961SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Sukumal Sagarji Maharaj | #sukumalsagarjiSanmatisagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Shubhamsagar Ji Maharaj | #shubhamsagarjiSanmatisagarji | 2025 | Rajasthan | Dungarpur | |
| Aryika Shri 105 Samaymati Mataji | #SamaymatijiSanmatiSagarJi1938 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sadaymati Mataji | #SadaymatijiSanmatiSagarJi1938 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Shreyshree Mataji | #ShreyshreejiSanmatiSagarJi1938 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Shubhamati Mataji-1975 | #Shubhamatiji1975SanmatiSagarJi1938 | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Acharya Shri 108 Vivek Sagarji Maharaj-1972 | #VivekSagarJiMaharaj1972SumatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vairagya Sagar Ji Maharaj 1963 | #VairagyaSagarJiMaharaj1963SumatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Sukhadmati Mata Ji 1944 | #SukhadmatiMataJi1944SuvidhiSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Acharya Shri 108 Ativeer Ji Maharaj 1965 | #AtiveerJiMaharaj1965VidyabhushanSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Acharya Shri 108 Gulab Bhushanji Maharaj-1955 | #GulabBhushanjiMaharaj1955VidyabhushanAcharyaSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Mudbadri |
| Elacharya Shri 108 Trilokbhusanji Maharaj (Lalitpur) | #ElacharyaShriTrilokbhusanJiMaharajLalitpurVidyabhusanSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Badagaon |
| Muni Shri 108 Prabhavnabhushanji Maharaj | #PrabhavnabhushanJiVidyabhushanJiMaharaj1975 | 2025 | Delhi | Delhi | |
| Ganini Aryika Shri 105 Shrushtibhushanmati Mataji | #ShrushtibhushanmatijiVidyabhushanSanmatiSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Acharya Shri 108 Pushpadant Sagar Ji Maharaj 1954 | #PushpadantSagarJiMaharaj1954VimalSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Devas |
| Acharya Shri 108 Niranjan Sagar Ji Maharaj | #NiranjanSagarJiMaharajVimalSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Viharsh Sagar Ji Maharaj 1970 | #ViharshSagarJiMaharaj1970ViragsagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Acharya Shri 108 Vimarsh Sagarji-Maharaj-1973 | #VimarshSagarJi1973ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Acharya Shri 108 Vibhav Sagarji Maharaj 1976 | #VibhavSagarJiMaharaj1976ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Acharya Shri 108 Vishad Sagarji Maharaj-1964 | #VishadSagarJiMaharaj1964ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Acharya Shri 108 Pragya Sagarji Maharaj-1978 | #PragyasagarJiMaharaj1978ViragSagarJi | 2025 | Rajasthan | Kota | |
| Acharya Shri 108 Pragysagarji Maharaj 1978 | #PragysagarJiMaharaj1978ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Vijyesh Sagar Ji Maharaj 1978 | #VijyeshSagarJiMaharaj1978ViragSagarJi(Anklikar) | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Muni Shri 108 Vibhaswar Sagar Ji Maharaj 1979 | #VibhaswarSagarJiMaharaj1979ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vidambarsagarji Maharaj-1982 | #MuniShriVidambarsagarJiMaharaj1982ViragSagarJi | 2025 | Maharashtra | Nashik | |
| Muni Shri 108 Visheshsagarji Maharaj-1975 | #MuniShriVisheshsagarJiMaharaj1975ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Satara |
| Muni Shri 108 Vishwamitrasagarji Maharaj (Viragsagarji) | #MuniShriVishwamitrasagarJiMaharajViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vishwasamya Sagarji Maharaj | #VishwasamyasagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhind |
| Muni Shri 108 Viniyog Sagarji Maharaj | #ViniyogsagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalgaon |
| Muni Shri 108 Nirveg Sagarji Maharaj | #NirvegsagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Khandwa |
| Muni Shri 108 Vishwasurya Sagarji Maharaj | #VishwasuryaViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sanavat |
| Aryika Shri 105 Vindhyashri Mataji-1973 | #VindhyashriMaataJi1973ViragSagarjiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Aryika Shri 105 Vishistmati Mata Ji 1979 | #VishistmatiMataJi1979ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vijetashree Mata Ji 1978 | #VijetashreeMataJi1978ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Aryika Shri 105 Vinatshree Mata Ji 1979 | #VinatshreeMataJi1979ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vikaamyashree Mata Ji 1982 | #VikaamyashreeMataJi1982ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Viprabhashree Mata Ji 1982 | #ViprabhashreeMataJi1982ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Viyojnashree Mataji-1979 | #ViyojnashreeMataJi1979ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Viditshree Mata Ji 1986 | #ViditshreeMataJi1986ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vibhaktshree Mataji-1947 | #VibhaktshreeMataJiViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vishisthshree Mataji | #VishisthshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vijitshree Mataji | #VijitshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vigunjanshree Mataji | #VigunjanshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Vijigyasamati Mataji | #VijigyasamatijiViragSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Ailak Shri Viniyogsagarji Maharaj | #ViniyogsagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Madhya Pradesh | Ujjain | |
| Kshullak Shri 105 Videh Sagarji Maharaj (Viragsagarji) | #VidehSagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Kshullika Shri 105 Vipadmashree Mataji | #VipadmashreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Kshullika Shri 105 Vichintanshree Mataji | #VichintanshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullika Shri 105 Visudhrudhshree Mataji | #VisudhrudhshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Kshullika Shri 105 Vipathshree Mataji | #VipathshreejiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Acharya Shri 108 Vibhakt Sagar Ji Maharaj 1969 | #VibhaktSagarJiMaharaj1969VishadSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Bhaktibhartishri Mataji | #BhaktibhartishrijiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Vatsalyabhartishri Mataji | #VatsalyabhartishrijiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Acharya Shri 108 Vipranat Sagar Ji Maharaj 1984 | #VipranatSagarJiMaharaj1984VivekSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Gambhirmati Mataji | #Gambhirmatijisuparshwamatimataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Acharya Shri 108 Tanmay Sagar Ji Maharaj1970 | #TanmaySagarJiMaharaj1970AbhinandanSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Aditya Sagarji Maharaj-1970 | #Adityasagarji1970Abhinandansagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Gurugram |
| Aryika Shri 105 Prasannmati Mata ji 1973 | #PrasannmatiMataji1973AbhinandanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Ajitmati Mataji-(AbhinandanSagarji) | #AjitmatijiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Aryika Shri 105 Abhedmati Mataji | #AbhedmatijiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Aryika Shri 105 Chaityamati Mataji -1967 (AbhinandanSagarji) | #Chaityamatiji1967AbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Suharshmati Mataji | #SuharshmatijiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullak Shri 105 Arham Sagarji Maharaj | #ArhamsagarjiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Acharya Shri 108 Adhyatmanandi Ji Maharaj | #AdhyatmanandijiKanaknandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Kshullak Shri 105 Siddha Sagarji Maharaj (Adityasagarji) | #SiddhasagarjiAdityasagarji1970 | 2025 | Confirmed | Haryana | Gurugram |
| Muni Shri 108 Punyasagarji Maharaj-1965 | #Punyasagarji1965AjitSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Saurabhmati Mataji-1958 | #SaurabhmatiAjitsagarJiMaharaj1926 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Gyanbhushanji Maharaj | #GyanbhushanjiArhadbaliji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Balacharya Shri 108 Siddhesen Ji Maharaj 1943 | #SiddhesenJiMaharaj1943BahubaliJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Raibaug |
| Ganini Aryika Shri 105 Jindevi Mataji 1960 | #GaniniJindeviMataji1960BahubaliJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Khsullika Shri 105 Mangalmati Mataji | #MangalmatijiBahubaliJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Aryika Shri 105 Subhadramati Mataji | #SubhadramatijiBahubaliJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Girnar Sagarji Maharaj (Balyogi Rashtrashant) | #BalyogiRashtrashantGirnarSagarJiMaharajBharatSagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Uddharmati Mataji | #UddharmatijiBharatSagarji1950 | 2025 | Confirmed | xy | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Nandishwarmati Mataji | #NandishwarmatijiBharatSagarji1950 | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Aryika Shri 105 Suprakashmati Mata ji 1965 | #SuprakashmatiMatajiDayaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Acharya Shri 108 Devnandiji Maharaj | #DevNandiJiMaharajKunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Amarkirtiji Maharaj 1974 | #AmarKirtiJiMaharaj1974DevnandiJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Mumbai |
| Muni Shri 108 Amoghkirtiji Maharaj 1980 | #AmoghKirtiJiMaharaj1980DevnandiJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Mumbai |
| Muni Shri 108 Siddhakirtiji Maharaj 1940 | #SiddhakirtijiMaharaj1940Devanandiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Shantikirtiji Maharaj | #ShantikirtijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Darshanshri Mataji | #DarshanshriDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Sanyogshri Mataji | #SanyogshrijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Sushilshri Mataji | #SushilshriDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Supadmamati Mataji | #SupadmamatiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Charitrashri Mataji | #CharitrashriDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Suyogshri Mataji | #SuyogshrijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Amit Sagar Ji Maharaj 1963 | #AmitSagarJiMaharaj1963DharmasagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Shubhmati Mataji 1948 | #ShubhmatiMataji1948DharmSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Suratnamati Mataji (Dharmsagarji) | #SuratnamatijiDharmsagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Dnyesagarji Maharaj | #DnyesagarjiGyanSagarJiMaharaj1957 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Namit Sagarji Maharaj | #NamitsagarjiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Nutanmati Mataji | #NutanmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Nitimati Mataji | #NitimatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Navmati Mataji | #NavmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Nayanmati Mataji | #NayanmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Namrmati Mataji | #NamrmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Kshullika Shri 105 Naychakramati Mataji | #NaychakramatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Kshullika Shri 105 Namanmati Mataji | #NamanmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Kshullika Shri 105 Gyanmoti Mataji | #GyanmotijiGyanBhushanJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Aarshmati Mataji | #AarshmatiMatajiGyanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Acharya Shri 108 Gyatsagarji Maharaj | #GyatsagarjiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Sacchidanand Sagar Ji Maharaj 1973 | #SacchidanandSagarJiMaharaj1973KanaknandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Suvatsalyamati Mataji | #SuvatsalyamatijiKanaknandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Kshullika Shri 105 Bhaktishri Mataji | #BhaktishrijiKanaknandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Acharya Shri 108 Karmvijay Nandiji Maharaj 1958 | #KarmvijayNandijiMaharaj1958KunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Chetanmati Mataji | #ChetanmatiKumudnandiJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Chetannandiji Maharaj | #ChetannandijiKumudnandiJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Shrutsagarji Maharaj 1969 | #ShrutsagarjiMuniraj1969KunthusagarjiMuniraj | 2025 | Confirmed | New Delhi | Green Park |
| Aacharya Shri 108 Kumudnandi Ji Maharaj 1963 | #KumudnandiJiMaharaj1963Kunthusagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Kanaknandiji Maharaj | #KanaknandiJiMaharajKunthusagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Acharya Shri 108 Padmanandiji Maharaj-1955 | #PadmanandijiMaharaj1955GandharacharyaShreeKunthusagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Acharya Shri 108 Vidyanandi Sagar Ji Maharaj 1963 | #VidyanandiSagarJiMaharaj1963KunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Belgaon |
| Acharya Shri 108 Gundhar Nandiji Maharaj | #GundharNandiJiMaharajKunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Niryapakacharya Shri 108 Gunbhadra Nandiji Maharaj-1969 | #GunbhadraNandiMaharaj1969KunthuSagarji | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Muni Shri 108 Dhairyanandi ji Maharaj | #DhairyanandijiMaharajKunthusagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shramannandiji Maharaj | #ShramannandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Pavitramati Mata Ji 1951 | #PavitramatiMataJi1951KunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Aasthashree Mataji-1975 | #AasthashreeMataJi1975KunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Aryika Shri 105 Pawanshree Mata Ji | #PawanshreeMataJiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Sumatishri Mataji | #SumatishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Siddhishri Mataji | #SiddhishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Riddhishri Mataji | #RiddhishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Gunshri Mataji | #GunshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Kshamashri Mataji | #KshamashriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Aryika Shri 105 Kusumshri Mataji | #KusumshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Kirtishri Mataji | #KirtishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Maharashtra | Nashik | |
| Aryika Shri 105 Kshemshri Mataji | #KshemshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Guruwani Mataji | #GuruwaniKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Kundshri Mataji | #KundshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullak Shri 105 Suvidhannandiji Maharaj | #SuvidhannandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullak Shri 105 Suvidya Nandiji Maharaj | #SuvidyanandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullak Shri 105 Shitalnandiji Maharaj | #ShitalnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullak Shri 105 Vardhamannandiji Maharaj | #VardhamannandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullika Shri 105 Sumaitri Mataji | #SumaitriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Kavyashri Mataji | #KavyashriiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Kshullika Shri 105 Chandrashri Mataji | #ChandrashriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullika Shri 105 Chaitanyamati Mataji (Kunthusagarji) | #ChaitanyamatijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Mangal Sagarji Maharaj-2003 | #MangalSagarji2003Mayanksagarji | 2025 | Madhya Pradesh | Shivpuri | |
| Acharya Shri 108 Nirbhay Sagarji Maharaj 1963 | #NirbhaySagarJiMaharaj1963AbhinandanSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Hemdatta Sagarji Maharaj | #HemdattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Sudatta Sagarji Maharaj | #SudattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Shivdatta Sagarji Maharaj | #ShivdattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Gurudatta Sagarji Maharaj | #GurudattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Bhudatta Sagarji Maharaj | #BhudattaSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Ailak Shri 105 Meghdatta Sagarji Maharaj | #MeghdattaSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Kshullak Shri 105 Chandradatta Sagarji Maharaj | #ChandradattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Kshullak Shri 105 Naigam Sagarji Maharaj (Nirbhaysagarji) | #NaigamSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Kshullak Shri 105 Dharmadatta Sagarji Maharaj | #DharmadattaSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Haryana | Gurugram |
| Kshullika Shri 105 Vimohmati Mataji | #VimohmatijiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Vairagyanandiji Maharaj-1974 | #Vairagyanandiji1974PadamNandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Tatvarthnandiji Maharaj | #TatvarthnandijiMaharaj1960Padmanandiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Muni Shri 108 Tatparyanandiji Maharaj | #TatparyanandijiMaharaj1960Padmanandiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Divyshreemati Mataji-1977 | #DivyshreematiMataJi1977PadmnandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vaartikshree Mata Ji 1983 | #VaartikshreeMataJi1983PadmnandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Vyaakhyashree Mata Ji 1979 | #VyaakhyashreeMataJi1979PadmnandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Vijayshree Mataji | #VijayshreejiPadmanandijiMaharaj1955 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Dhairyashree Mataji | #DhairyashreejiPadmanandijiMaharaj1955 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Kshullika Shri 105 Kundanshri Mataji | #KundanshrijiPadmanandijiMaharaj1955 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Ganini Aryika Shri 105 Shreyanshmati Mataji | #ShreyanshmatijiParshvSagarJi1915 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Prabal Sagarji Maharaj 1971 | #PrabalSagarJiMaharaj1971PuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Bharuch |
| Muni Shri 108 Sahajsagarji Maharaj (Prasannasagarji) | #SahajsagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Muni Shri 108 Navpadmasagarji Maharaj | #NavpadmasagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aryika Shri 105 Gyanprabha Mataji | #GyanprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aryika Shri 105 Charitraprabha Mataji | #CharitraprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aryika Shri 105 Punyaprabha Mataji | #PunyaprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullak Shri 105 Naigamsagarji Maharaj (Prasannasagarji) | #NaigamsagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullak Shri 105 Arghsagarji Maharaj | #ArghsagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Darshanprabha Mataji | #DarshanprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Tapaprabha Mataji | #TapaprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Vachanprabha Mataji | #VachanprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Vratprabha Mataji | #VratprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Dharmprabha Mataji | #DharmprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Acharya Shri 108 Prasannrishiji Maharaj | #PrasannrishijiKusagraNandiJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Prabhatchandraji Maharaj | #PrabhatchandrajiPrasannrishiJiMaharaj1981 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Punyamati Mata Ji | #PunyamatiMataJiPrasannrishiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Pujyamati Mataji-1962 | #PujyamatiMataJi1962PrasannrishiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Pulkit Sagar Ji Maharaj(Bhilwara) | #PulkitsagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Pramudit Sagar Ji Maharaj(Jabalpur) | #PramuditSagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Purvang Sagarji Maharaj | #PurvangsagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Ailak Shri 105 Prashmit Sagarji Maharaj | #PrashmitsagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Mohotsav Sagar Ji Maharaj | #mohotsavsagarjimaharajPunyasagarjimaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Muditsagarji Maharaj | #MuditsagarjiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Utsavsagarji Maharaj | #UtsavsagarjiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Harshitmati Mataji | #HarshitmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Pramodmati Mataji-1960 | #PramodmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Parvmati Mataji | #ParvmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Nishchaymati Mataji | #NishchaymatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Nirnaymati Mataji | #NirnaymatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullak Shri 105 Purna Sagarji Maharaj | #PurnasagarjiPunyasagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Balacharya Shri 108 Moksh Sagarji Maharaj-1962 | #BalacharyaShriMokshSagarJiMaharaj1962SambhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Puneet Chaitanya mati Mata ji 1958 | #PuneetChaitanyaMatajiSambhavSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Pavitrasagar Ji Maharaj 1949 | #PavitrasagarJiMaharaj1949SanmatiSagarJi1927 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Niryapak Shraman Muni Shri 108 Dharmsagar Ji Maharaj 1942 | #DharmsagarJiMaharaj1942SanmatiSagarJi1927 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Vidya Sagar Ji Maharaj 1990 | #VidyaSagarJiMaharaj1990SanmatiSagarji(Dakshinwale) | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Siddhantsagar Ji Maharaj 1950 | #SiddhantsagarJiMaharaj1950VardhmansagarJi1951 | 2025 | Madhya Pradesh | Indore | |
| Muni Shri 108 Sulabh Sagarji Maharaj (Saubhagyasagarji) | #SulabhsagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Saubhagyamati Mataji | #SaubhagyamatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullak Shri 105 Shubhlabhsagarji Maharaj | #ShubhlabhsagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullak Shri 105 Shubhkamanasagarji Maharaj | #ShubhkamanasagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullika Shri 105 Shubhmargmati Mataji | #ShubhmargmatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullika Shri 105 Shubhashishmati Mataji | #ShubhashishmatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullika Shri 105 Suaryashri Mataji | #SuaryashrijiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Kshullika Shri 105 Sumargshri Mataji | #SumargshrijiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Kshullika Shri 105 Ashresthmati Mataji | #AshresthmatijiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Acharya Shri 108 Saubhagya Sagarji Maharaj | #SaubhagyasagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Balacharya Shri 108 Suratna Sagar Ji Maharaj-1986 | #BalacharyaShriSuratnJiMaharaj1986SaubhagyaSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Ganini Aryika Shri 105 Shubhmati Mataji | #ShubhmatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Acharya Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 1961 | #SamtaSagarJiMaharaj1961 | 2025 | Rajasthan | Itiwar | |
| Kshullak Shri 105 Suprabhatsagarji Maharaj | #SuprabhatsagarjiShashankSagarjiMaharaj1983 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Sabarkantha |
| Muni Shri 108 Anuman Sagarji Maharaj | #AnumanSagarjiShrutsagarjiMuniraj1969 | 2025 | Uttar Pradesh | Kapilji | |
| Kshullak Shri 105 Aviral Sagarji Maharaj | #Aviral SagarjiShrutsagarjiMuniraj1969 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Shashank Sagarji Maharaj-1983 | #ShashankSagarjiMaharaj1983SiddhantSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Sahajsagar Ji Maharaj 1965 | #SahajsagarJiMaharaj1965SiddhantSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Ganini Aryika Shri 105 Saubhagyamati Mata Ji | #SaubhagyamatiJiSiddhantSagarJiMaharaj1966 | 2025 | Confirmed | Telangana | Hyderabad |
| Gadni Aryika Shri 105 Sangam mati Mata Ji | #SangamMatiMatajiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Ganini Aryika Shri 105 Samatamati Mataji | #SamatamatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Suryamati Mataji | #SuryamatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Siddhantmati Mataji-1951 | #Siddhantmatiji1951SiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Sanskarmati Mataji | #SanskarmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Samarthmati Mataji | #SamarthmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Sakshammati Mataji | #SakshammatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullak Shri 105 Shrutsagarji Maharaj (Siddhantsagarji) | #ShrutsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Sauhardsagarji Maharaj | #SauhardsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Savindrasagarji Maharaj | #SavindrasagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullak Shri 105 Shrifalsagarji Maharaj | #ShrifalsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullak Shri 105 Naigamsagarji Maharaj (Siddhantsagarji) | #NaigamsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Kshullika Shri 105 Suyashmati Mataji | #SuyashmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullika Shri 105 Sunandamati Mataji | #SunandamatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullika Shri 105 Sukaushalmati Mataji | #SukaushalmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Savindramati Mataji | #SavindramatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Sunandamati Mataji-1954 | #SunandamatijiSubaahuSagarJiMaharaj1924 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Subodhmati Mataji-(Subahusagarji) | #SubodhmatijiSubaahuSagarJiMaharaj1924 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Sundar Sagar Ji Maharaj 1976 | #SundarSagarJiMaharaj1976SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Sukaavyamati Mata ji | #SukaavyamatiMatajiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullak Shri 105 Supunya Sagarji Maharaj | #SupunyaSagarjiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sudarshmati Mataji | #SudarshmatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sudharmmati Mataji (Sundarsagarji) | #SudharmmatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sudhanyamati Mataji | #SudhanyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Subhavyamati Mataji | #SubhavyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sutathyamati Mataji | #SutathyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sunamramati Mataji (Sundarsagarji) | #SunamramatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Supathyamati Mataji | #SupathyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sankalpmati Mataji | #SankalpmatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Sushrut Sagar Ji Maharaj 1943 | #SushrutSagarJiMaharaj1943SunilSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuwa |
| Muni Shri 108 Sampujya Sagar Ji Maharaj | #SampujyaSagarJiMaharajSunilSagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Samvigya Sagar Ji Maharaj | #SamvigyaSagarJiMaharajSunilSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuaa |
| Muni Shri 108 Sampragya Sagar Ji Maharaj 2000 | #SampragyaSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Shrutesh Sagarji Maharaj-1983 | #Shruteshsagarji1983Sunilsagarji1977 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuaa |
| Muni Shri 108 Sushrutasagar Ji Maharaj-1992 | #sushrutasagarjiSunilsagarji | 2025 | Madhya Pradesh | Bakshuaa | |
| Muni Shri 108 Sampragyasagar Ji Maharaj-2000 | #sampragyasagarSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Siddharth Sagarji Maharaj | #SiddharthsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Shubham Sagarji Maharaj | #ShubhamsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Dungarpur |
| Muni Shri 108 Suvivek Sagarji Maharaj | #SuviveksagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Suvishuddh Sagarji Maharaj | #SuvishuddhsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sampurnamati Mata ji | #SampurnamatiMatajiSunilSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sampannmati Mata ji 1992 | #SampannmatiMataji1992SunilSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sambalmati Mataji-1995 | #sambalmatiSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sampoornamati Mataji-1990 | #sampoornamatiSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Supragyamati Mataji-1992 | #supragyamati1992Sunilsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Khairwada |
| Aryika Shri 105 Aakashmati Mataji-1957 | #aakashmati1957Sunilsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Adeymati Mataji | #AdeymatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Arshmati Mataji | #ArshmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Anarghmati Mataji | #AnarghmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Khairwada |
| Aryika Shri 105 Suvigyamati Mataji | #SuvigyamatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Sanyyatmati Mataji | #SanyyatmatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Anuprekshamati Mataji | #AnuprekshamatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sutramati Mataji | #SutramatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Sukhadsagarji Maharaj | #SukhadsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Samvruddhasagarji Maharaj | #SamvruddhasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Sampragyasagarji Maharaj | #SampragyasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Santoshsagarji Maharaj | #SantoshsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Santushtsagarji Maharaj | #SantushtsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Vijayantsagarji Maharaj | #VijayantsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Sunishchit Sagarji Maharaj | #SunishchitsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Suprakash Sagarji Maharaj | #SuprakashSagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuaa |
| Kshullak Shri 105 Sankalp Sagarji Maharaj | #SankalpSagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Surajmati Mataji | #SurajmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Suvratmati Mataji | #SuvratmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sugandhmati Mataji | #SugandhmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sambhavmati Mataji | #SambhavmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Samarakshmati Mataji | #SamarakshmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sadvratmati Mataji | #SadvratmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sadbodhmati Mataji | #SadbodhmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Satatmati Mataji | #SatatmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Amohmati Mataji | #AmohmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Atalmati Mataji | #AtalmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Shuddhatmamati Mataji | #ShuddhatmamatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Ajaymati Mataji | #AjaymatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Padmamati Mataji | #PadmamatiMatajiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Saddrushtmati Mataji | #SaddrushtmatiMatajiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sukrutmati Mataji | #SukrutmatijiMatajiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Acharya Shri 108 Sunil Sagarji Maharaj-1977 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sulekhmati Mataji | #SulekhmatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Chintanshree Mata Ji 1981 | #ChintanshreeMataJi1981VairagyanandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sugyanshree Mata Ji 1969 | #SugyanshreeMataJi1969VairagyanandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sohamshree Mataji | #SohamshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samyakshree Mataji | #SamyakshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Jinshree Mataji | #JinshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Krutikashree Mataji | #KrutikashreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Sanwarnandi Maharaj | #SanwarnandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Saukhyashree Mataji | #SaukhyashreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Sadhyamati Mataji | #SadhyamatijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Sahajshree Mataji | #SahajshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Sarvshree Mataji | #SarvshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Samatashree Mataji | #SamatashreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1950 (Vatsalya Viridhi) | #VardhamansagarjiDharmsagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Hitendra Sagarji Maharaj 1977 | #HitendraSagarJiMaharaj1977VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Darshit Sagarji Maharaj 1955 | #DarshitSagarjiMaharaj1955VardhamanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Chintan Sagarji Maharaj 1986 | #ChintanSagarjiMaharaj1986VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Param Sagar Ji Maharaj | #ParamSagarJiMaharajVardhamanSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Agamsagar Ji Maharaj | #AgamsagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Chinmay Sagarji Maharaj | #ChinmaySagarjiVardhamansagarj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Mahayashmati Mataji 1989 | #MahayashmatiMataji1989VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vatsalmati Mataji 1953 | #VatsalmatiMataji1953VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vilokmati Mataji 1961 | #VilokmatiMataji1961VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Divyanshumati Mataji 1947 | #DivyanshumatiMataji1947VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Purnimamati Mataji 1978 | #PurnimamatiMataji1978VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Muditmati Mataji 1938 | #MuditmatiMataji1938VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vichakshanmati Mataji 1963 | #VichakshanmatiMataji1963VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Nirmuktmati Mataji 1958 | #NirmuktmatiMataji1958VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vinamramati Mataji 1966 | #VinamramatiMataji1966VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Darshanamati Mataji 1962 | #DarshanamatiMataji1962VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Deshnamati Mataji 1959 | #DeshnamatiMataji1959VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Nirmohmati Mataji-1962 | #NirmohmatijiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Padmayashamati Mataji-1996 | #PadmayashamatijiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vishwayashmati Mataji-1986 | #VishwayashmatijiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Aryika Shri 105 Divyayashmati Mataji-1996 | #Divyayashmatiji1996VardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Chaityammati Mataji | #ChaityammatijiVardhamansagarji | 2025 | Rajasthan | Tonk | |
| Kshullak Shri 105 Vishalsagarji Maharaj-1959 | #Vishalsagarji1959VardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Nirdosh Sagarji Maharaj-1963 | #NirdoshSagarJiMaharaj1963VardhamanSagarJi(Dakshinwale) | 2025 | Madhya Pradesh | Narsinhpur | |
| Muni Shri 108 Aadisagarji Maharaj | #AadisagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1951 | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Acharya Shri 108 Vasunandiji Maharaj 1967 | #VasunandijiMaharaj1967VidyanandJi | 2025 | Uttar Pradesh | Ahicchatra | |
| Muni Shri 108 Prashmanandji Maharaj-1978 | #PrashmanandJiMaharaj1978VasunandiJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Shivanandji Maharaj-1985 | #ShivanandJiMaharaj1985VasunandiJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Shraddhanandji Maharaj-1987 | #ShraddhanandJiMaharaj1987VasunandiJi | 2025 | Confirmed | Haryana | Sector 16, Faridabad |
| Muni Shri 108 Saiyamanand Ji Maharaj 1959 | #SaiyamanandJiMaharaj1959VasunandiJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Alwar |
| Muni Shri 108 Pavitranand Ji Maharaj 1979 | #PavitranandJiMaharaj1979VasunandiJi | 2025 | Confirmed | Haryana | Sector 16, Faridabad |
| Muni Shri 108 Namisagarji Maharaj (Vasunandiji) | #NamisagarjiVasunandiji | 2025 | Confirmed | Haryana | Rewari |
| Ganini Aryika Shri 105 Gurunandni Mataji-1976 | #GadniGurunandniMataJi1976VasunandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aryika Shri 105 Prabodhnandni Mata Ji 1982 | #PrabodhnandniMataJi1982VasunandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aaryika Shri 105 Prakamyanandani Mata Ji 1995 | #PrakamyanandaniMataJi1995VasunandiJiMaharaj. | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aaryika Shri 105 Prabhanandani Mata Ji 1958 | #PrabhanandaniMataJi1958VasunandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aryika Shri 105 Bramhanandni Mataji-1976 | #BramhanandniMataji1976VasundijiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aryika Shri 105 Shrinandani Mata Ji 1982 | #ShrinandaniMataJi1982VasundijiMaharaj. | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Ailak Shri 105 Vigyansagarji Maharaj | #VigyansagarjiVasunandiji | 2025 | Confirmed | Haryana | Rewari |
| Aryika Shri 105 Gyanmati Mataji 1934 | #GyanmatiMataji1934VeersagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Muni Shri 108 Aavashyak Sagarji Maharaj-1952 | #AavashyakSagarJiMaharaj1952VibhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Adhyyan Sagarji Maharaj-1943 | #AdhyyanSagarJiMaharaj1943VibhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Shudhatm Sagar Ji Maharaj 1995 | #ShudhatmSagarJiMaharaj1995VibhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Muni Shri 108 Sukh Sagarji Maharaj-1958 (Vibhavsagarji) | #sukhsagarji1958Vibhavsagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Siddhatma Sagar Ji Maharaj | #SiddhatmasagarjiVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Omshree Mata Ji 1993 | #OmshreeMataJi1993VibhavSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Sanskriti Shri Mata ji 1974 | #SanskritiShriMataji1974VibhavSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Adyomshree Mataji-1996 | #AdyomshreeVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Subhavsagarji Maharaj-2007 | #SubhavsagarjiVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Samsagarji Maharaj-1960 | #Samsagarji1960Vibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Sanstutishree Mataji | #SanstutishreeVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Safal Sagarji Maharaj | #SafalsagarjiVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aacharya Shri 108 Aarjav Sagar Ji Maharaj 1967 | #AarjavSagarJiMaharaj1967VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Acharya Shri 108 Samay Sagar Ji Maharaj 1958 | #SamaySagarJiMaharaj1958VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Niryapak Muni Shri 108 Sudha Sagar Ji Maharaj 1956 | #SudhaSagarJiMaharaj1956VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Niryapak Muni Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 1962 | #SamtaSagarJiMaharaj1962VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Niryapak Muni Shri 108 Veer Sagar ji Maharaj 1973 | #VeerSagarjiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Niryapak Muni Shri 108 Yog Sagar Ji Maharaj 1986 | #YogSagarJiMaharaj1986VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Niryapak Muni Shri 108 Prasad Sagar Ji Maharaj 1984 | #PrasadSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Maihar |
| Niryapak Muni Shri 108 Abhay Sagarji Maharaj-1960 | #AbhaySagarJiMaharaj1960VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Niryapak Muni Shri 108 Sambhav Sagarji Maharaj-1971 | #SambhavSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Niryapak Muni Shri 108 Niyam Sagar Ji Maharaj 1957 | #NiyamSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Akshay Sagarji Maharaj 1962 | #AkshaySagarJiMaharaj1962VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bareilly |
| Muni Shri 108 Praman Sagarji Maharaj 1967 | #PramanSagarjiMaharaj1967VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Pranamya Sagarji Maharaj 1975 | #PranamyaSagarjiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Nirnay Sagarji Maharaj-1969 | #NirnaySagarJiMaharaj1969VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shajapur |
| Muni Shri 108 Uttam Sagar Ji Maharaj 1960 | #UttamSagarJiMaharaj1960VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sangli |
| Muni Shri 108 Shail Sagarji Maharaj-1986 | #ShailSagarJiMaharaj1986VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Banda |
| Muni Shri 108 Sheetalsagarji Maharaj 1976 | #SheetalsagarjiMaharaj1976VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Maihar |
| Muni Shri 108 Shramanasagarji Maharaj 1981 | #ShramanasagarjiMaharaj1981VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj 1977 | #KunthuSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Sandhansagar Ji Maharaj 1976 | #SandhansagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Nirupamsagarji Maharaj 1978 | #NirupamsagarjiMaharaj1978VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Muni Shri 108 Padm Sagar Ji Maharaj 1963 | #PadmSagarJiMaharaj1963VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Katni |
| Muni Shri 108 Nirveg Sagarji Maharaj-1973 | #NirvegSagarJiMaharajVidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Ajit Sagarji Maharaj-1968 | #AjitSagarJiMaharaj1968VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat Nagar |
| Muni Shri 108 Nirakul Sagarji Maharaj-1982 | #NirakulSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dewas |
| Muni Shri 108 Saumyasagarji Maharaj 1978 | #SaumyasagarjiMaharaj1978VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Agra |
| Muni Shri 108 Niramayasagarji Maharaj 1976 | #NiramayasagarjiMaharaj1976VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Nirogsagarji Maharaj-1976 | #NirogsagarjiMaharaj1976VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Virat Sagarji Maharaj-1974 | #ViratSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Vinamra Sagarji Maharaj-1978 | #VinamraSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Muni Shri 108 Maha Sagarji Maharaj-1973 | #MahaSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chindwara |
| Muni Shri 108 Nishkamp Sagar Ji Maharaj 1982 | #NishkampSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Durlabh Sagar Ji Maharaj 1978 | #DurlabhSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Prabodh Sagar Ji Maharaj 1974 | #PrabodhSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Banda |
| Muni Shri 108 Avichal Sagar Ji Maharaj 1981 | #AvichalSagarJiMaharaj1981VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Jhansi |
| Muni Shri 108 Arah Sagar Ji Maharaj 1976 | #ArahSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sanganer |
| Muni Shri 108 Nirapadasagarji Maharaj 1982 | #NirapadasagarjiMaharaj1982VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shivpuri |
| Muni Shri 108 Nirlobh sagarji Maharaj 1970 | #NirlobhsagarjiMaharaj1970VidyasagarJi | 2025 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | |
| Muni Shri 108 Niradoshsagarji Maharaj 1967 | #NiradoshsagarjiMaharaj1967VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Muni Shri 108 Vimal Sagar Ji Maharaj 1975 | #VimalSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Vishal Sagar Ji Maharaj 1977 | #VishalSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Muni Shri 108 Dhaval Sagar Ji Maharaj 1972 | #DhawalSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi | 2025 | Maharashtra | Dharashiv | |
| Muni Shri 108 Nirmad Sagar Ji Maharaj 1984 | #NirmadSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Pindrai |
| Muni Shri 108 Pujya Sagar Ji Maharaj 1970 | #PujyaSagarJiMaharaj1970VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prashast Sagar Ji Maharaj 1975 | #PrashastSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Vishad Sagar Ji Maharaj 1973 | #VishadSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Dharm Sagar Ji Maharaj 1976 | #DharmSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Muni Shri 108 Prayog Sagar Ji Maharaj 1974 | #PrayogSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Prabhaat Sagar Ji Maharaj 1971 | #PrabhaatSagarJiMaharaj1971VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj 1956 | #ChandraSagarJiMaharaj1956VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Nispaksh Sagar Ji Maharaj 1975 | #NispakshSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Muni Shri 108 Niswarth Sagar Ji Maharaj 1973 | #NiswarthSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Muni Shri 108 Nischal Sagar Ji Maharaj 1972 | #NischalSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Agra |
| Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji Maharaj 1973 | #NirmohSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Nishkaam Sagar Ji Maharaj 1980 | #NishkaamSagarJiMaharaj1980VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Neeraj Sagar Ji Maharaj 1986 | #NeerajSagarJiMaharaj1986VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Pindrai |
| Muni Shri 108 Nissang Sagar Ji Maharaj 1981 | #NissangSagarJiMaharaj1981VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Sanskar Sagar Ji Maharaj 1978 | #SanskarSagarJiMaharaj1978VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Nisprah Sagar Ji Maharaj 1976 | #NisprahSagarJiMaharaj1976VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Muni Shri 108 Nirbhik Sagar Ji Maharaj 1977 | #NirbhikSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Nirag Sagar Ji Maharaj 1982 | #NiragSagarJiMaharaj1982VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat Nagar |
| Muni Shri 108 Nisarg Sagar Ji Maharaj 1977 | #NisargSagarJiMaharaj1977VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Muni Shri 108 Omkaar Sagar Ji Maharaj 1982 | #OmkaarSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Pavitra Sagar Ji Maharaj 1961 | #PavitraSagarJiMaharaj1961VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Muni Shri 108 Nirih Sagar Ji Maharaj 1978 | #NirihSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Abhinandan Sagar Ji Maharaj 1975 | #AbhinandanSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Suparshwa Sagar Ji Maharaj 1955 | #SuparshwaSagarJiMaharaj1955VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Atul Sagar Ji Maharaj 1971 | #AtulSagarJiMaharaj1971VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Nissim Sagar Ji Maharaj 1983 | #NissimSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Shashvat Sagar Ji Maharaj 1957 | #ShashvatSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Mehasana |
| Muni Shri 108 Malli Sagar Ji Maharaj 1972 | #MalliSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Anand Sagar Ji Maharaj 1978 | #AnandSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Bhaav Sagar Ji Maharaj 1976 | #BhaavSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Muni Shri 108 Vineet Sagar Ji Maharaj 1961 | #VineetSagarJiMaharaj1961VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Chandraprabh Sagar Ji Maharaj 1966 | #ChandraprabhSagarJiMaharaj1966VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Aagam Sagar Ji Maharaj 1976 | #AagamSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Jagdalpur |
| Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1980 | #SehajSagarJiMaharaj1980VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1973 | #SubratSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Saral Sagarji Maharaj 1957 | #SaralSagarjiMaharaj1957VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Puran Sagar Ji Maharaj 1975 | #PuranSagarJiMaharaj1975VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Bengaluru |
| Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji Maharaj 1989 | #NirgranthSagarJiMaharaj1989VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Nirbhrant Sagar Ji Maharaj 1987 | #NirbhrantSagarJiMaharaj1987VidyaSagarJi | 2025 | Madhya Pradesh | Jabalpur | |
| Muni Shri 108 Niralas Sagar Ji Maharaj 1983 | #NiralasSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Niraashrav Sagar Ji Maharaj 1981 | #NiraashravSagarJiMaharaj1981VidyaSagarJi | 2025 | Madhya Pradesh | Jabalpur | |
| Muni Shri 108 Nirakar Sagar Ji Maharaj 1985 | #NirakarSagarJiMaharaj1985VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Nishchint Sagar Ji Maharaj 1987 | #NishchintSagarJiMaharaj1987VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Badaut |
| Muni Shri 108 Nirmaan Sagar Ji Maharaj 1971 | #NirmaanSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Nishank Sagar Ji Maharaj 1984 | #NishankSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Niranjan Sagar Ji Maharaj 1983 | #NiranjanSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Nirlep Sagar Ji Maharaj 1990 | #NirlepSagarJiMaharaj1990VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Sukh Sagar Ji Maharaj1963 | #SukhSagarJiMaharaj1963VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Prabuddh Sagar Ji Maharaj1971 | #PrabuddhSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shridham |
| Muni Shri 108 Shreyansh Sagar Ji Maharaj 1967 | #ShreyanshSagarJiMaharaj1967VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Bihar | Bhagalpur |
| Muni Shri 108 Anant Sagar Ji Maharaj1971 | #AnantSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Achal Sagar Ji Maharaj1976 | #AchalSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Banda |
| Muni Shri 108 Pawan Sagar Ji Maharaj 1966 | #PawanSagarJiMaharaj1966VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Vrushabh Sagarji Maharaj (Vidyasagarji) | #VrushabhsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Suvrat Sagarji Maharaj-1973 | #Suvratsagarji1973AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj | 2025 | Madhya Pradesh | Bina | |
| Muni Shri 108 Utkrusth Sagarji Maharaj-1940 | #Utkrusthsagarji1940VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Muni Shri 108 Punitsagarji Maharaj | #PunitsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Muni Shri 108 Samadhisagarji Maharaj | #SamadhisagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Purnamati Mataji-1964 | #PurnmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Agaadhmati Mata Ji 1968 | #AgaadhmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Gurumati Mata Ji 1956 | #GurumatiMataJi1956VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Chintanmati Mata Ji 1968 | #ChintanmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sutramati Mata Ji 1968 | #SutramatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Sheelmati Mata Ji 1972 | #SheelmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Saarmati Mata Ji 1971 | #SaarmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sakarmati Mata Ji 1969 | #SakarmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Somyamati Mata Ji 1972 | #SomyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sushantmati Mata Ji 1965 | #SushantmatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Jagratmati Mata Ji 1968 | #JagratmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Kartavyamati Mata Ji 1972 | #KartavyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Nishkaammati Mataji-1978 | #NishkaammatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalna |
| Aryika Shri 105 Viratmati Mataji-1979 | #ViratimatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalna |
| Aryika Shri 105 Tathamati Mata Ji 1976 | #TathamatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Chaityamati Mata Ji 1970 | #ChaityamatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Puneetmati Mata Ji 1972 | #PuneetmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinhpur |
| Aryika Shri 105 Upshammati Mataji-1979 | #UpshammatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Dhruvmati Mata Ji 1965 | #DhruvmatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalna |
| Aryika Shri 105 Paarmati Mata Ji 1978 | #PaarmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aagatmati Mata Ji 1976 | #AagatmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Shrutmati Mata Ji 1978 | #ShrutmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Pavanmati Mataji-1961 | #Pavanmatiji1961VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sadhnamati Mata Ji 1965 | #SadhnamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Vilakshnamati Mata Ji 1963 | #VilakshnamatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aklankmati Mata Ji 1964 | #AklankmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Niklankmati Mata Ji 1969 | #NiklankmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aagammati Mata Ji 1962 | #AagammatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Swadhyaymati Mata Ji 1962 | #SwadhyaymatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Prashammati Mata Ji 1965 | #PrashammatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Muditmati Mata Ji 1964 | #MuditmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sehajmati Mata Ji 1972 | #SehajmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Saiyammati Mata Ji 1967 | #SaiyammatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Siddhamati Mata Ji 1971 | #SiddhamatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samunnatmati Mata Ji 1974 | #SamunnatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Shastramati Mata Ji 1973 | #ShastramatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Tathyamati Mata Ji 1972 | #TathyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vaatsalyamati Mata Ji 1965 | #VaatsalyamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Pathyamati Mata Ji 1972 | #PathyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sanskarmati Mata Ji 1962 | #SanskarmatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vijitmati Mata Ji 1971 | #VijitmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aaptmati Mata Ji 1976 | #AaptmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Dhavalmati Mata Ji 1976 | #DhavalmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samitimati Mata Ji 1975 | #SamitimatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Mananmati Mata Ji 1982 | #MananmatiMataJi1982VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Mrudumati Mata Ji 1959 | #MradumatiMataJi1959VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Nirnaymati Mata Ji 1958 | #NirnaymatiMataJi1958VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Rijumati Mata Ji 1961 | #RijumatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Saralmati Mata Ji 1966 | #SaralmatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Aseemmati Mata Ji 1976 | #AseemmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Gautammati Mata Ji 1977 | #GautammatiMataJi1977VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Nirvaanmati Mata Ji 1978 | #NirvaanmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Maardavmati Mata Ji 1976 | #MaardavmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Mangalmati Mata Ji 1980 | #MangalmatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Chaaritramati Mata Ji 1979 | #ChaaritramatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Shraddhamati Mata Ji 1982 | #ShraddhamatiMataJi1982VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Utkarshmati Mata Ji 1980 | #UtkarshmatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Tapomati Mataji-1958 | #tapomatimatajividyasagarjimaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Siddhantmati Mataji 1969 | #SiddhantmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinhpur |
| Aryika Shri 105 Namrmati Mataji-1968 | #NamrmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Vinamrmati Mataji-1968 | #VinamrmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Atulmati Mataji-1968 | #AtulmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Anugammati Mataji-1970 | #AnugammatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Uchitmati Mataji-1973 | #UchitmatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vinaymati Mata Ji 1978 | #VinaymatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinhpur |
| Aryika Shri 105 Lakshyamati Mataji-1941 | #LakshyamatiMataJi1941VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Dhyeymati Mataji-1980 | #DhyeymatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aatmmati Mataji-1967 | #AatmmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Saiyatmati Mataji-1974 | #SaiyatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Prashantmati Mata Ji 1961 | #PrashantmatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Vinatmati Mata Ji 1963 | #VinatmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Vishudhmati Mata Ji 1975 | #VishudhmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Shailmati Mata Ji 1968 | #ShailmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Akampmati Mataji-1966 | #AkampmatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Satana |
| Aryika Shri 105 Amulyamati Mataji-1965 | #AmulyamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aaradhyamati Mataji-1972 | #AaradhyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Achintyamati Mataji-1969 | #AchintyamatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Alolyamati Mataji-1968 | #AlolyamatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Anmolmati Mataji-1970 | #AnmolmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aagyamati Mataji-1972 | #AagyammatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Aryika Shri 105 Achalmati Mataji-1973 | #AchalmatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Satana |
| Aryika Shri 105 Bhavnamati Mataji 1966 | #BhavnamatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Balaghat |
| Aryika Shri 105 Sadaymati Mataji-1969 | #SadaymatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Balaghat |
| Aryika Shri 105 Bhaktimati Mataji-1946 | #BhaktimatiMataJi1946VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Balaghat |
| Aryika Shri 105 Satyamati Mataji-1960 | #SatyaMatiMaataJi,1960VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Aryika Shri 105 Gunmati Mataji-1963 | #GunmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samaymati Mataji-1967 | #SamaymatiMaataJi,1967VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Aadarshmati Mataji-1964 | #AadarshmatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Dhaarnamati Mataji-1964 | #DhaarnaMatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Durlabhmati Mataji-1964 | #DurlabhmatiMaataJi1964VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Akhandmati Mataji-1969 | #AkhandmatiMaataJi1969VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Korba |
| Aryika Shri 105 Aalokmati Mataji-1966 | #AalokmatiMaataJi1966VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Apurvmati Mataji-1970 | #ApurvmatiMaataJi1970VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Kushalmati Mataji-1961 | #KushalmatiMataJi1961VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Anantmati Mataji | #AnantMatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Dhrudhmati Mataji-1961 | #Dradhmatiji1961VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Akshaymati Mataji-1967 | #AkshaymatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bhilai |
| Aryika Shri 105 Amandmati Mataji-1969 | #AmandmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Samvarmati Mataji-1969 | #SamvarmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Merumati Mataji-1974 | #MerumatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Nirmadmati Mataji-1976 | #NirmadmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bhilai |
| Aryika Shri 105 Anarghmati Mataji-1975 | #AnarghmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Antarmati Mataji-1967 | #AntarmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Anugrahmati Mataji-1967 | #AnugrahmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Amoortmati Mataji-1968 | #AmoortmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Anupammati Mataji-1968 | #AnupammatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Adhigammati Mataji-1968 | #AdhigammatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Abhedmati Mataji-1971 | #AbhedmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Korba |
| Aryika Shri 105 Nirmalmati Mataji-1963 | #NirmalmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Shuklmati Mataji-1963 | #ShuklmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Samvegmati Mataji | #SamvegmatiMataJiVidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Nirvegmati Mataji-1972 | #NirvegmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Shodhmati Mataji-1964 | #ShodhmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Omkaarmati Mataji-1968 | #OmkaarmatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Shashwatmati Mataji-1972 | #ShashwatmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Sushilmati Mataji-1964 | #SushilmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Susiddhmati Mataji-1970 | #SusiddhmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Udaarmati Mataji-1972 | #UdaarmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Santustmati Mataji-1975 | #SantustmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Nikatmati Mataji-1974 | #NikatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Amitmati Mataji-1972 | #AmitmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Shubhrmati Mataji-1967 | #ShubhrmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Sadhumati Mataji-1967 | #SadhumatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Vishadmati Mataji-1969 | #VishadmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Vipulmati Mataji-1970 | #VipulmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Madhurmati Mataji-1967 | #MadhurmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Satarkmati Mataji-1969 | #SatarkmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Vairagyamati Mata ji1967 | #VairagyamatiMataji1967VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Prasannmati Mataji-1967 | #PrasannmatiMataji1967VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sakalmati Mataji-1966 | #SakalmatiMataji1966VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sheetalmati Mataji-1971 | #SheetalmatiMataji1971VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Upshantmati Mataji-1967 | #UpshantmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Swasthamati Mataji-1961 | #SwasthamatiMataji1961VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Gantavyamati Mataji-1969 | #GantavyamatiMataji1969VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Prithvimati Mataji-1974 | #PrithviymatiMataji1974VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Vineetmati Mata ji 1975 | #VineetmatiMataji1975VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Parmaarthmati Mataji-1983 | #ParmaarthmatiMataji1983VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Dhyanmati Mataji-1978 | #DhyanmatiMataji1978VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Korba |
| Aryika Shri 105 Videhmati Mataji-1970 | #VidehmatiMataji1970VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Aduurmati Mataji-1963 | #AduurmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Swabhavmati Mataji-1972 | #SwabhavmatiMataji1972VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Parammati Mataji-1982 | #ParammatiMataji1982VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Chetanmati Mataji-1986 | #ChetanmatiMataji1986VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Vimalmati Mataji | #VimalmatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Kaivalyamati Mataji-1962 | #KaivalyamatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Nirvanmati Mataji | #NirvanmatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Madhya Pradesh | Chattarpur | |
| Aryika Shri 105 Avaymati Mataji | #AvaymatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Udyotmati Mataji | #UdyotmatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Shwemati Mataji-1970 | #Shwetmatiji1970VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Ailak Shri Dhairya Sagarji Maharaj-1966 | #Dhairyasagarji1966VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Kshullak Shri 105 Sudhar Sagarji Maharaj | #SudharsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Sudhrudh Sagarji Maharaj | #SudhrudhsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Sayyam Sagarji Maharaj | #SayyamsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Ailak Shri 105 Samakit Sagarji Maharaj (Vidyasagarji) | #SamakitsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Veeral Sagarji Maharaj | #VeeralsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Vichar Sagarji Maharaj | #VicharsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Manan Sagarji Maharaj | #ManansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Manthan Sagarji Maharaj | #ManthansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Magan Sagarji Maharaj | #MagansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Nijatma Sagarji Maharaj | #NijatmasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Bihar | Bhagalpur |
| Kshullak Shri 105 Tanmay Sagarji Maharaj | #TanmaysagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Chaitya Sagarji Maharaj | #ChaityasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Gahan Sagarji Maharaj | #GahansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Ailak Shri 105 Kaivalya Sagarji Maharaj | #KaivalyasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Ailak Shri 105 Utsah Sagarji Maharaj | #UtsahsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Apar Sagarji Maharaj | #AparsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Athah Sagarji Maharaj | #AthahsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Sudharm Sagarji Maharaj | #SudharmsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chindwara |
| Kshullak Shri 105 Shwet Sagarji Maharaj | #ShwetsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chindwara |
| Kshullak Shri 105 Vairagya Sagarji Maharaj | #VairagyasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Virat Sagarji Maharaj | #ViratsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Kshullak Shri 105 Nayan Sagarji Maharaj | #NayansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Uttar Pradesh | Baraut | |
| Kshullak Shri 105 Tatwarth Sagarji Maharaj | #TatwarthsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dewas |
| Kshullak Shri 105 Atal Sagarji Maharaj | #AtalsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shajapur |
| Ailak Shri 105 Uchit Sagarji Maharaj | #UchitsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Gambhir Sagarji Maharaj-1961 | #Gambhirsagarji1961AcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Swagat Sagarji Maharaj-1983 | #Swagatsagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Kshullak Shri 105 Aagat Sagarji Maharaj-1986 | #Aagatsagarji1986VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Bhaswat Sagarji Maharaj-1979 | #Bhaswatsagarji1979VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Swastik Sagarji Maharaj-1986 | #Swastiksagarji1986VidyaSagarji1946 | 2025 | Madhya Pradesh | Guna | |
| Kshullak Shri 105 Bharat Sagarji Maharaj-1996 | #Bharatsagarji1996VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Jagrat Sagarji Maharaj-1997 | #Jagratsagarji1997VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Ailak Shri 105 Udyam Sagarji Maharaj-1975 | #Udyamsagarji1975VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Ailak Shri 105 Garistha Sagarji Maharaj-1983 | #Garisthasagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Kshullak Shri 105 Aadar Sagarji Maharaj-1969 | #Aadarsagarji1969VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Samaadar Sagarji Maharaj-1974 | #Samaadarsagarji1974VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Ailak Shri 105 Auchitya Sagarji Maharaj-2000 | #Auchityasagarji2000VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Anunay Sagarji Maharaj-1983 | #Anunaysagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Delhi | Delhi | |
| Kshullak Shri 105 Savinay Sagarji Maharaj-1983 | #Savinaysagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Samanvay Sagarji Maharaj-1982 | #Samanvaysagarji1982VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Hirak Sagarji Maharaj-1988 | #Hiraksagarji1988VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Kshullak Shri 105 Nirdhum Sagarji Maharaj-1995 | #Nirdhumsagarji1995VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Kshullak Shri 105 Varisth Sagarji Maharaj-1982 | #Varisthsagarji1982VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Gaurav Sagarji Maharaj-1985 | #Gauravsagarji1985VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Kshullak Shri 105 Videh Sagarji Maharaj-1990 (Vidyasagarji) | #Videhsagarji1990VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Amapsagarji Maharaj-1993 | #Amapsagarji1993VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Swastiksagarji Maharaj | #SwastiksagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Aadarsagarji Maharaj | #AadarsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Chidrupsagarji Maharaj | #ChidrupsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Swaroopsagarji Maharaj | #SwaroopsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Subhagsagarji Maharaj | #SubhagsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Aagam Sagar Ji Maharaj 1976 | #AagamSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Muni Shri 108 Vishwaharsh Sagarji Maharaj | #VishwaharshSagarjiViharshSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Muni Shri 108 Vichintya Sagar Ji Maharaj 1983 | #VichintyaSagarJiMaharaj1983VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vijay Sagar Ji Maharaj 1972 | #VijaySagarJiMaharaj1972VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vishwarya Sagar Ji Maharaj 1943 | #VishwaryaSagarJiMaharaj1943VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vishwarth Sagar Ji Maharaj 1948 | #VishwarthSagarJiMaharaj1948VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vivrat Sagar Ji Maharaj 1993 | #VivratSagarJiMaharaj1993VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Shamali |
| Muni Shri 108 Visham Sagar Ji Maharaj 1978 | #VishamSagarJiMaharaj1978VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Usmanpur |
| Muni Shri 108 Vishwansh Sagar Ji Maharaj 1961 | #VishwanshSagarJiMaharaj1961VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vigamya Sagar Ji Maharaj 1995 | #VigamyaSagarJiMaharaj1995VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vishwagya Sagarji Maharaj | #VishwagyaSagarjiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Aryika Shri 105 Vidyantshree Mata ji 1987 | #VidyantshreeMataji1987VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vimlantshree Mata Ji 1983 | #VimlantshreeMataJi1983VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vikrantshree Mata Ji 1977 | #VikrantshreeMataJi1977VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vishwantshree Mata Ji 1958 | #VishwantshreeMataJi1958VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vidhyantshree Mata ji 1983 | #VidhyantshreeMataji1983VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vijyantshree Mata Ji 1951 | #VijyantshreeMataJi1951VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vinayantshree Mata Ji 1975 | #VinayantshreeMataJi1975VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Kshullika Shri 105 Viprantshree Mataji | #ViprantshreejiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Kshullika Shri 105 Videhantshree Mataji | #VidehantshreejiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Kshullika Shri 105 Vidikshantshree Mataji | #VidikshantshreejiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Acharya Shri 108 Vinamra Sagarji Maharaj 1963 | #VinamraSagarjiMaharaj1963ViragSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vigya Sagar Ji Maharaj 1976 | #VigyaSagarJiMaharaj1976VinamraSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vinut Sagar Ji Maharaj 1994 | #VinutSagarJiMaharaj1976VinamraSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vishwakund Sagarji Maharaj | #VishwakundSagarjiVinamraSagarjiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vipulshri Mataji-1986 | #VipulshriMataji1986VinamraSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vishramshri Mataji (Banswada) | #VishamshriMataji(Banswada)VinamraSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vimudshri Mata ji 1990 | #VimudshriMataji1990VinamraSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vibhavyamati Mataji | #VibhavyamatijiVinamraSagarjiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Visarvmati Mataji | #VisarvmatijiVinamraSagarjiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Pragyey Sagarji Maharaj | #PragyeySagarjiVipranatSagarJiMaharaj1984 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prabha Sagarji Maharaj | #PrabhaSagarjiVipranatSagarJiMaharaj1984 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Vishuddha Sagar Maharaj 1971 | #VishuddhaSagarMaharaji1971ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Aditya Sagar Ji Maharaj 1986 | #AdityaSagarJiMaharaj1986VishudhSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj 1981 | #SuprabhSagarJiMaharaj1981VishudhSagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Manogya Sagar Ji Maharaj 1948 | #ManogyaSagarJiMaharaj1948VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj 1977 | #PrashamSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1977 | #SubratSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Suyash Sagar Ji Maharaj 1980 | #SuyashSagarJiMaharaj1980VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Anuttar Sagar Ji Maharaj 1977 | #AnuttarSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Anupam Sagar Ji Maharaj 1986 | #AnupamSagarJiMaharaj1986VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhilwara |
| Muni Shri 108 Arijit Sagar Ji Maharaj 1983 | #ArijitSagarJiMaharaj1983VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Nagaland | Dimapur |
| Muni Shri 108 Aastikya Sagarji Maharaj-(Shraman Muni)-1984 | #AastikyaSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalgaon |
| Muni Shri 108 Praneet Sagarji Maharaj-(Shraman Muni)-1984 | #PraneetSagarjiMaharaj1984VishuddhaSagarJi1971 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Aaradhya Sagar Ji Maharaj 1977 | #AaradhyaSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Pranay Sagar Ji Maharaj 1982 | #PranaySagarJiMaharaj1982VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Pranav Sagar Ji Maharaj 1984 | #PranavSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Pranat Sagar Ji Maharaj 1978 | #PranatSagarJiMaharaj1978VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Pranut Sagar Ji Maharaj 1993 | #PranutSagarJiMaharaj1993VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Ujjain |
| Muni Shri 108 Sarvaarth Sagar Ji Maharaj 1991 | #SarvaarthSagarJiMaharaj1991VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Saamya Sagar Ji Maharaj 1989 | #SaamyaSagarJiMaharaj1989VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1979 | #SehajSagarJiMaharaj1979VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Samatva Sagar Ji Maharaj 1984 | #SamatvaSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Saadhya Sagar Ji Maharaj 1987 | #SaadhyaSagarJiMaharaj1987VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sanawat |
| Muni Shri 108 Sankalp Sagar Ji Maharaj 1981 | #SankalpSagarJiMaharaj1981VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jintoor |
| Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj 1996 | #SomyaSagarJiMaharaj1996VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Tikamgadh |
| Muni Shri 108 Saaraswat Sagar Ji Maharaj 1998 | #SaaraswatSagarJiMaharaj1998VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sangli |
| Muni Shri 108 Sadbhaav Sagar Ji Maharaj 1986 | #SadbhaavSagarJiMaharaj1986VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Ratlam |
| Muni Shri 108 Sanjayant Sagar Ji Maharaj 1989 | #SanjayantSagarJiMaharaj1989VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Saiyat Sagar Ji Maharaj 1973 | #SaiyatSagarJiMaharaj1973VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Rawatbhata |
| Muni Shri 108 Sakshya Sagar Ji Maharaj 1979 | #SakshyaSagarJiMaharaj1979VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Silwani |
| Muni Shri 108 Yashodhar Sagar Ji Maharaj | #YashodharSagarJiMaharajVishuddhSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji Maharaj | #NirgranthSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nirvikalp Sagar Ji Maharaj | #NirvikalpSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nivratt Sagar Ji Maharaj | #NivrattSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Silwani |
| Muni Shri 108 Nisang Sagar Ji Maharaj | #NisangSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji Maharaj | #NirmohSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhilwara |
| Muni Shri 108 Yatna Sagarji Maharaj | #YatnasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Yatindra Sagarji Maharaj | #YatindrasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Jayandra Sagarji Maharaj | #JayandrasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Tikamgadh |
| Muni Shri 108 Jitendra Sagarji Maharaj | #JitendrasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Jayant Sagarji Maharaj | #JayantsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sangli |
| Muni Shri 108 Subhag Sagarji Maharaj | #SubhagSagarjiMaharajVishuddhSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Siddha Sagarji Maharaj-2002 | #SiddhaSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Muni (Shraman) Shri 108 Siddharth Sagarji Maharaj-1999 | #SiddharthSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Saharsh Sagarji Maharaj-1999 | #SaharshSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Satyarth Sagarji Maharaj-2000 | #SatyarthSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Sarthak Sagarji Maharaj-1977 | #SarthakSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Sarth Sagarji Maharaj-1995 | #SarthSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Samakit Sagarji Maharaj-2003 | #SamakitSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Kshullak Shri 105 Shrutsagarji Maharaj (Vishuddhasagarjji) | #ShrutsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Ailak Shri Vipramansagarji Maharaj | #VipramansagarjiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Videh Sagarji Maharaj (Viveksagarji) | #VidehsagarjiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Vigunmati Mataji | #VigunmatijiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Shri Sammed Shikharji | ||
| Acharya Shri 108 Yatindra Sagarji Maharaj | #YatindrasagarjiYogendraSagarJiMaharaj1961 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Prasannrishiji Maharaj-1981 | #PrasannrishiJiMaharaj1981KushagranandiJi | 2025 | Madhya Pradesh | Indore | |
| Aryika Shri 105 Kirtivani Mataji | #KirtivanijiKusagraNandiJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Prabhakar Sagarji Maharaj | #PrabhakarsagarjiPramukhSagarJiMaharaji1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Aryika Shri 105 Pritishri Mataji | #PritishriPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Aryika Shri 105 Parikshashri Mataji | #ParikshashriPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullak Shri 105 Parmanandsagarji Maharaj | #ParmanandsagarjiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Paramsadhya Mataji | #ParamsadhyamatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Paramshantaji Mataji | #ParamshantajimatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Paramdivyashri Mataji | #ParamdivyashrimatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Aradhanashri Mataji | #AradhanashriMatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Parmaradhyashri Mataji | #ParmaradhyashriMatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Acharya Shri 108 Namostu Sagar Ji Maharaj 1989 | #NamostuSagarJiMaharaj1989PunyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hapud |
| Aryika Shri 105 Suratnamati Mataji (Punyasagarji) | #SuratnamatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Muni Shri 108 Mahima Sagar Ji Maharaj 1973 | #MahimaSagarJiMaharaj1973VardattSagarJi | 2025 | Maharashtra | Nashik | |
| Muni Shri 108 Achol Sagarji Maharaj | #AcholsagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Agarbh Sagarji Maharaj | #AgarbhsagajiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Abhed Sagarji Maharaj | #AbhedsagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Aganya Sagarji Maharaj | #AganyasagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Akamp Sagarji Maharaj | #AkampsagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Divyasen Ji Maharaj | #DivyasenjiDevsenJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Gadni Aryika Shri 105 Saraswati Mata ji 1961 | #SaraswatiMatajiSubalSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Bagpat |
| Aryika Shri 105 Anantmati Mataji-(Subal Sagarji) | #AnantmatiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Bagpat |
| Aryika Shri 105 Mokshmati Mataji | #MokshmatiMatajiAcharyaShriTirthanandijiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullak Shri 105 Naman Sagarji Maharaj (Tirthanandiji) | #NamanSagarjiAcharyaShriTirthanandijiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Pravar Sagar Ji Maharaj 1980 | #PravarSagar | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Pragyan Sagar Ji Maharaj 1993 | #PragyanSagar | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bundi |
| Muni Shri 108 Prasiddha Sagarji Maharaj | #PrasiddhaSagarjiVinishchaysagarJiMaharaj1973 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bundi |
| Muni Shri 108 Apurva Sagarji Maharaj 1966 | #ApurvaSagarJiMaharaj1966VardhmanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Arpit Sagarji Maharaj 1966 | #ArpitSagarJiMaharaj1966VardhmanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Prabhav Sagarji Maharaj 1944 | #PrabhavSagarjiMaharaj1944VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Mumukshu Sagarji Maharaj | #MumukshuSagarJiMaharajVardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Samarpitmati Mataji | #SamarpitmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 108 Pranatmati Mataji-1961 | #PranatmatiVardhamanSagarJi1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Ratanmati Mataji | #RatanmatijiGambhirmatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Tyagmati Mataji | #TyagmatijiGambhirmatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Dayanshumati Mataji | #DayanshumatijiGambhirmatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Chandnamati Mata Ji 1958 | #ChandnamatiMataJi1958GyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Suvratmati Mataji (Gyanmatiji) | #SuvratmatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Swarnamati Mataji (Gyanmatiji) | #SwarnamatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Sudhrudhmati Mataji-1977 | #Sudhrudhmatiji1977GyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Muditmati Mataji | #MuditmatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Bhaktimati Mataji | #BhaktimatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Kshullak Shri 105 Prashant Sagarji Maharaj | #PrashantSagarjiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Kshullak Shri 105 Jinsagarji Maharaj | #JinsagarjiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Shrutikashree Mata Ji 1979 | #ShrutikashreeMataJi1979KamalshreeMataJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Nikankshashri Mataji (Kshamashrimataji) | #NikankshashrijiKshamashri | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Aryika Shri 105 Devyashmati Mataji 1984 | #DevyashMatiMataJi1984PrashantmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Devagammati Mataji-1983 | #DevagamMatiMataji1983PrashantmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Devardhi Mati Mata ji 1983 | #DevardhiMatiMataji1983PrashantmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Kshullika Shri 105 Sundarmati Mataji | #SundarmatijiSakalmatiMataji1966 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Kshullika Shri 105 Shravanmati Mataji | #ShravanmatijiShreyanshmatiMataji(Pune) | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Garima mati Mata ji | #GarimamatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Suhitmati Mataji | #SuhitmatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Suvegmati Mataji | #SuvegmatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Sugeetmati Mataji | #SugeetmatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Bhavanamati Mataji | #BhavanamatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Vigyanmati Mataji 1963 | #VigyanmatiMataji1963VivekSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Adityamati Mataji 1972 | #AdityamatiMataji1972VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Charanmati Mataji 1980 | #CharanmatiMataji1980VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Karanmati Mataji 1981 | #KaranmatiMataji1981VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Banswara |
| Aryika Shri 105 Sharanmati Mataji-(Vigyanmatiji) | #SharanmatiMatajiVigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Pavitramati Mata ji 1974 | #PavitramatiMataji1974VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Banswara |
| Aryika Shri 105 Suyashmati Mataji 1986 | #SuyashmatiMataji1986VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Uditmati Mataji 1982 | #UditmatiMataji1982VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Chpttorgarh |
| Aryika Shri 105 Varadmati Mataji 1958 | #VaradmatiMataji1958VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Sharadmati Mataji-1977 | #SharadmatiMataji1977VigyanmatiMataJi1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Chpttorgarh |
| Aryika Shri 105 Suveermati Mataji-1987 | #SuveermatiMataji1987VigyanmatiMataJi1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Rajatmati Mataji-1986 | #RajatmatiMataji1986VigyanmatiMataJi1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Chpttorgarh |
| Aryika Shri 105 Suvandanshree Mataji | #SuvandanshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Aryika Shri 105 Sundanshree Mataji | #SundanshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Kshullika Shri 105 Suparvshree Mataji | #SuparvshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Kshullika Shri 105 Suchandanshree Mataji | #SuchandanshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Kshullika Shri 105 Vishalmati Mataji | #VishalmatijiVipulmatiMataJi1970 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Vimalmati Mataji-(Vipulmatiji) | #VimalmatijiVipulmatiMataJi1970 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Vidarshammati Mataji | #VidarshammatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Vikarshmati Mataji | #VikarshmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Kshullika Shri 105 Vishrutmati Mataji | #VishrutmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Kshullika Shri 105 Vipulmati Mataji | #VipulmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Ganini Aryika Shri 105 Vishisthmati Mataji | #VishisthmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Visheshmati Mataji | #VisheshmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Rajasthan | Pratapgadh | |
| Aryika Shri 105 Vibhushanmati Mataji | #VibhushanmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Viditmati Mataji | #ViditmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Vijitmati Mataji | #VijitmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Kshullika Shri 105 Vidushimati Mataji | #VidushimatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Vikhyatmati Mataji | #VikhyatmatijiGarimamatiMataji1972 | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Ganini Aryika Shri 105 Yashasvini Mataji | #GadniYashasviniMataji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Kamalshri Mataji | #KamalshrijiNipunnandiji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sanyogmati Mataji | #SanyogmatijiSangamMatiMataji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Manaswinimati Mataji | #ManaswinimatijiGadniYashasviniMataji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Ganani Pramukh Aryika Shri 105 Vimal Prabha Mata Ji 1951 | #VimalPrabhaMataJi1951VijayamatiMataJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Ganini Aryika Shri 105 Nangmati Mataji | #NangmatijiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Vishnuprabhashree Mataji | #VishnuprabhashreejiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vijayprabhashree Mataji | #VijayprabhashreejiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Vijitprabha Mataji | #VijitprabhajiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Vinatprabha Mataji | #VinatprabhajiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Sugreevmati Mataji | #SugreevmatijiShreyanshmatiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Shradhyeymati Mataji | #ShradhyeymatijiShreyanshmatiji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Ganini Aryika Shri 105 Vigyashree Mataji 1972 | #VigyashreeMataJi1972ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gyeyak Shri Mata ji | #GyeyakShriMataji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gyanshree Mataji | #GyanshreejiVigyashreeMataJi1972 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gnyevyashree Mataji | #GnyevyashreejiVigyashreeMataJi1972 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gyayakshree Mataji | #GyayakshreejiVigyashreeMataJi1972 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Ganini Aryika Shri 105 Vishudhmati Mataji-1949 | #Vishuddhmatimatiji1949NirmalSagarJiMaharaj1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Muni Shri 108 Maun Sagarji Maharaj | #MaunSagarjiBhutbalisagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Susner |
| Muni Shri 108 Muni Sagarji Maharaj | #MuniSagarjiBhutbalisagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Susner |
| Muni Shri 108 Mukti Sagarji Maharaj | #MuktiSagarjiBhutbalisagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Susner |
| Muni Shri 108 Mangalsagar Ji Maharaj | #MangalsagarjiManglanandSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shivpuri |
| Kshullak Shri 105 Priytirth Ji Maharaj | #PriytirthjiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Kshullak Shri 105 Purnatirth Sagarji Maharaj | #PurnatirthsagarjiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Kshullika Shri 105 Shantiprgayashri Mataji | #ShantiprgayashrijiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Kshullika Shri 105 Prayagmati Mataji | #PrayagmatijiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Ailak Tatvarthsagar Ji Maharaj | #TatvarthsagarjiVishalya | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Uditsagarji Maharaj-1949 | #Uditsagarji1949PunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Utsahmati Mataji | #UtsahmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Ganini Aryika Shri 105 Adityashri Mataji | #AdityashrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Nityashri Mataji | #NityashrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Diptishri Mataji | #DiptishrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Dikshashri Mataji | #DikshashrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Maitrishri Mataji | #MaitrishrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Acharya Shri 108 Anekant Sagarji Maharaj 1963 | #AnekantSagarjiMaharaj1963AbhinandanaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Acharya Shri 108 Prasanna Sagarji Maharaj 1970 (Antarmana) | #PrasannaSagarJiMaharaj1970(Antarmana)PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aacharya Shri 108 Gupti Nandi Ji Maharaj 1972 | #GuptiNandiJiMaharaj1972KunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Acharya 108 Shri Bharat Bhushanji Maharaj 1982 | #BharatBhushanJiMaharaj1980DharmabhushanJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Muzzaffarnagar |
| Balacharya Shri 108 Bhadrabahu Sagar Ji Maharaj | #BhadrabahuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Apramit Sagar Ji Maharaj 1984 | #ApramitSagarJiMaharaj1984VishudhSagarji | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Muni Shri 108 Pragyasagar Ji Maharaj - 1972 | #PragyasagarJiMaharaj-1972PuspdantSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Muni Shri 108 Saurabhnandi Ji Maharaj 1991 | #SaurabhnandiJiMaharaj1991VairagyanandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Saiyamnandi Ji Maharaj | #SaiyamnandiJiMaharajVairagyanandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shramannandi Ji Maharaj | #ShramannandiJiMaharajVairagyanandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Amogh Sagar Ji Maharaj 1947 | #AmoghSagarJiMaharaj1947AmitSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Pujya Muni Shri 108 Piyushsagarji Muniraj 1969 | #PujyaPiyushsagarjiMuniraj1969Pushpadantasagarji | 2025 | Confirmed | zzzzz | Indore |
| Muni Shri 108 Shubham Kirti Ji Maharaj | #ShubhamKirtiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Prashantsagar Ji Maharaj 1963 | #PrashantsagarJiMaharaj1963PavitrsagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Prathamanand Ji Maharaj | #PrathamanandJiMaharaj | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Mardav Sagarji Maharaj | #mardavsagarjimaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Subhadra Sagarji Maharaj | #SubhadrasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Vishwavijay Sagarji Maharaj | #VishwavijayViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salambur |
| Muni Shri 108 Vidhruv Sagarji Maharaj | #VidhruvViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vikoshal Sagarji Maharaj | #VikoshalViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Vishwalokesh Sagarji Maharaj | #VishwalokeshViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vinivesh Sagarji Maharaj | #ViniveshViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Prakshal Sagarji Maharaj | #PrakshalViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Parbhani |
| Muni Shri 108 Suyatna Sagarji Maharaj | #SuyatnasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Mumbai |
| Muni Shri 108 Sarvarth Sagarji Maharaj | #SarvarthsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Samakit Sagarji Maharaj | #SamakitsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Prabuddha Sagarji Maharaj-1954 | #PrabuddhaSagarji1954VardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Shrutesh Sagarji Maharaj | #ShruteshsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Madhya Pradesh | Nainagiri | |
| Muni Shri 108 Vimalgupt Sagarji Maharaj | #VimalguptsagarjiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Samantbhadraji Maharaj | #SamantbhadrajiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Shrutdharnandiji Maharaj | #ShrutdharnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Gujarat | Sabarkantha |
| Muni Shri 108 Shantinandiji Maharaj | #ShantinandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Prabhachandnandiji Maharaj | #PrabhachandnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Amarnandiji Maharaj | #AmarnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Shrutkirtiji Maharaj | #ShrutkirtijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Hashendrasagarji Maharaj | #HashendrasagarjiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Sandesh Sagarji Maharaj | #SandeshsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Santosh Sagarji Maharaj | #SantoshsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Muni Shri 108 Shreenandiji Maharaj | #ShreenandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shreekarnandiji Maharaj | #ShreekarnandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vatsanandiji Maharaj | #VatsanandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shubhbahubali Sagarji Maharaj | #ShubhbahubalisagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Shubhkirti Sagarji Maharaj | #ShubhkirtisagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Suvigya Sagarji Maharaj | #SuvigyasagarjiSuvidhiSagarJi1971 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Muni Shri 108 Samay Sagarji Maharaj | #SamaysagarjiSanmatiSagarJiMaharaj1927(Dakshin) | 2025 | Madhya Pradesh | Bhagyaday Tirth, Sagar | |
| Muni Shri 108 Ajitsagar Ji Maharaj | #AjitsagarjiSanmatiSagarJiMaharaj1927(Dakshin) | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Archit Sagarji Maharaj | #ArchitsagarjiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Anant Sagarji Maharaj | #AnantsagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Aaptpramatt Sagarji Maharaj | #AaptpramattsagarjiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Muni Shri 108 Parimalsagarji Maharaj | #ParimalsagarjiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Muni Shri 108 Vilok Sagarji Maharaj | #ViloksagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Morena |
| Muni Shri 108 Sutirth Sagarji Maharaj | #SutirthsagarjiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Yogya Sagarji Maharaj | #YogyasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Pratigyanand Ji Maharaj | #PratigyanandjiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Prabhav Sagarji Maharaj | #PrabhavsagarjiPavitrasagarJiMaharaj1949 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Prabhat Sagarji Maharaj | #PrabhatsagarjiPavitrasagarJiMaharaj1949 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Amitanjaykirti Ji Maharaj | #AmitanjaykirtijiJaykirtiji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Ajitsen Ji Maharaj (Jinsenji) | #AjitsenjiBalacharyaShriJinsenJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Ekatva Sagarji Maharaj (Chaityamatiji) | #EkatvasagarjiChaityamatiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Vigya Shri Mata Ji 1969 | #VigyaShriMataJi1969VishuddhmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Shubh Mati Mata ji 1975 | #ShubhMatiMataji1975SanmatiSagarjiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Garimamati Mata ji 1972 | #GarimamatiMataji1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Banswara |
| Aryika Shri 105 Hemshriji Mataji | #HemshrijiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Aryika Shri 105 Savinaymati Mataji | #SavinaymatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Anubhavmati Mataji | #AnubhavmatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Anuttarmati Mataji | #AnuttarmatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Sakshepmati Mataji | #SakshepmatijiSaubhagyamatiji | 2025 | Confirmed | Telangana | Hyderabad |
| Aryika Shri 105 Shikshamati Mataji | #ShikshamatijiSaubhagyamatiji | 2025 | Confirmed | Telangana | Hyderabad |
| Ailak Shri Vivekanand Sagarji Maharaj | #VivekanandsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat Nagar |
| Ailak Shri Nishchay Sagarji Maharaj | #NishchaysagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Ailak Shri Nijanand Sagarji Maharaj | #NijanandsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Ailak Shri Daya Sagarji Maharaj | #DayasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Ailak Shri Upsham Sagarji Maharaj | #UpshamsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bareilly |
| Ailak Shri 105 Swasti Sagarji Maharaj | #SwastiSagarjiSamanvaySagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prateek Sagarji Maharaj-1980 (Krantiveer) | #PrateekSagarji1980(Krantiveer)PushpaDantaSagarJi | 2025 | Uttar Pradesh | Baghpath | |
| Upadhyay Shri 108 Vishok Sagarji Maharaj 1975 | #VishokSagarjiMaharaj1975ViragsagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Upadhyay Shri 108 Vihasant Sagar Ji Maharaj 1983 | #VihasantSagarJiMaharaj1983ViragSagarJi(Anklikar) | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhind |
| Upadhay Shri 108 Gupti Sagarji Maharaj-1957 | #Guptisagarji1957VidyaSagarji | 2025 | Haryana | Sonipat | |
| Upadhyay Shri 108 Viksant Sagar Ji Maharaj 1985 | #ViksantSagarJiMaharaj1985GanacharyaShriViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Upadhyay Shri 108 Vibhanjan Sagarji Maharaj-1983 | #VibhanjanSagarJiMaharaj1983ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dhaar |
| Upadhyay Shri 108 Vishrutsagar Ji Maharaj 1976 | #VishrutsagarJiMaharaj1976ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Khandwa |
| Upadhyay Shri 108 Urjayant Sagar Ji Maharaj 1977 | #UrjayantSagarJMaharaj1977VimalSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Upadhyay Shri 108 Viranjan Sagarji Maharaj | #ViranjanViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Jayant Sagarji Maharaj | #JayantsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Muni Shri 108 Saaraswat Sagar Ji Maharaj 1998 | #SaaraswatSagarJiMaharaj1998VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj 1996 | #SomyaSagarJiMaharaj1996VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Tikamgarh |
| Acharya Shri 108 Viharsh Sagar Ji Maharaj 1970 | #ViharshSagarJiMaharaj1970ViragsagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Kshullika Shri 105 Sugunmati Mataji | #SugunmatijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Sumanshree Mataji | #SumanshreejiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Utkarsh Sagarji Maharaj | #UtkarshsagarjiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Gujarat | Sabarkantha | |
| Muni Shri 108 Vishwagyeya Sagarji Maharaj | #VishwagyeyajiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dhaar |
| Muni Shri 108 Shuddha Sagarji Maharaj | #ShuddhaSagarJiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Sheel Sagarji Maharaj | #SheelSagarJiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Kshullak Shri 105 Shreysagarji Maharaj | #ShreysagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Shreyashsagarji Maharaj | #ShreyashsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Muni Shri 108 Vishalsagarji Maharaj | #VishalsagarjiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vishubhsagarji Maharaj | #VishubhsagarjiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salambur |
| Muni Shri 108 Vibhorsagarji Maharaj | #VibhorsagarjiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dhar/Indore |
| Kshullak Shri 105 Kshemankar Sagarji Maharaj | #KshemankarsagarjiVibhaktSagarJiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Sumitrasagarji Maharaj | #SumitrasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Savimalsagarji Maharaj | #SavimalsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Suratsagarji Maharaj | #SuratsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Saksham Sagarji Maharaj | #SakshamsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Dungarpur |
| Aryika Shri 105 Aarshmati Mataji-(Gyanmatiji) | #AarshmatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Badauth |
| Aryika Shri 105 Prashantnandini Mataji | #PrashantnandinijiVasunandijiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Acharya Shri 108 Vinischay Sagarji Maharaj-1973 | #VinischayaSagarJiMaharaj1973ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Muni Shri 108 Paay Sagarji Maharaj-1969 | #PaaySagarJiMaharaj1969VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Senki Gatta |
| Aryika Shri 105 Amoghmati Mataji | #AmoghmatijiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Aryika Shri 105 Arpanmati Mataji | #ArpanmatijiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Aryika Shri 105 Anshmati Mataji | #AnshmatijiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Kshullak Shri 105 Samyayog Sagarji Maharaj | #SamyayogSagarjiVishuddhaSagarMaharajji1971 | 2025 | Confirmed | Nagaland | Dimapur |
| Kshullak Shri 105 Paramyog Sagarji Maharaj | #ParamyogSagarjiVishuddhaSagarMaharajji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Ratlam |
| Muni Shri 108 Vishwaksh Sagarji Maharaj-(Vidyasagarji) | #VishwakshSagarjiAcharyaShriVidyasagarjiMaharaj | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Praneetsagarji Maharaj | #PraneetsagarjiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Dhyey Sagarji Maharaj | #DhyeySagarjiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Bhuvan Sagarji Maharaj | #BhuvanSagarjiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Prekshamati Mataji-1955 | #PrekshamatijiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Jineshmati Mataji-1945 | #Jineshmatiji1945Vardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Ailak Shri 105 Harsh Sagarji Maharaj | #HarshSagarjiVardhamansagarjiDharmsagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Kshullak Shri 105 Praptisagarji Maharaj-1956 | #Praptisagarji1956Vardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Vivarjit Sagarji Maharaj-1951 | #VivarjitSagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Niyogsagarji Maharaj | #NiyogsagarjiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Harshendrasagarji Maharaj | #HarshendrasagarjiPunyasagarji1965 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
श्रुतधराचार्यों की परंपरामें सर्वप्रथम आचार्य गुणधरका नाम आता है। गुणधर और धरसेन दोनों ही श्रुत-प्रतिष्ठापकके रूपमें प्रसिद्ध हैं। गुणधर आचार्य धरसेनकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी थे। गणधरको 'पञ्चमपूर्वगत पेज्जदोसपाहुड' का ज्ञान प्राप्त था और धरसेनको 'पूर्वगत कम्मपयडिपाहुड' का। इतना ही नहीं, किन्तु गुणधरको 'पेज्जदोसपाहुड’ के अतिरिक्त 'महाकम्मपयडिपाहुड' का भी ज्ञान प्राप्त था, जिसका समर्थन 'कसायपाहुड’ से होता है । 'कसायपाहुड' में बन्ध, संक्रमण, उदय और उदीरणा से पृथक् अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार 'महाकम्मपयडिपाहुड’ के चौबीस अनुयोगद्वारों में से क्रमशः षष्ठ, द्वादश और दशम अनुयोगद्वारोंसे संबद्ध हैं। 'महाफम्मपयडिपाहुड' का चौबीसवाँ अल्पबहुत्व नामक अनुयोगद्वार भी 'कसायपाहुड' के सभी अधिकारोंमें व्याप्त है । अतः स्पष्ट है कि आचार्य गुणधर 'महाकम्मपयडिपाहुड’ के ज्ञाता होने के साथ 'पेज्जदोसपाहुड' के ज्ञाता और 'कसायपाहुड' के रूपमें उसके उपसंहारकर्ता भी थे। पर 'छक्खडागम’ की धवला-टोकाके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात नहीं होता कि धरसेन 'पेज्ज दोसपाहुड' के ज्ञाता थे। अतएव आचार्य गुणधरको दिगंबर परंपरामें लिखित रूपमें प्राप्त श्रुतका प्रथम श्रुतकार माना जा सकता है। धरसेनने किसी ग्रंथकी रचना नहीं की। जबकि गुणधरने 'पेज्जदोसपाहुड' की रचना की है। जयघवलाके मंगलाचरणके पश्चसे ज्ञात होता है कि आचार्य गुणधरने कसायपाहुडका गाथाओं द्वारा व्याख्यान किया है।
जैणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जलं अणंतत्थं।
माहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे ॥ ६ ॥
इसके अनन्तर आचार्य वीरसेनने लिखा है - ज्ञानप्रवादपूर्वके निर्मल दसवें वस्तु अधिकारके तृतीय कसायपाहुडरूपी समुद्रके जलसमूहसे प्रक्षालित मति ज्ञानरूपी नेत्रवारी एवं त्रिभुवन-प्रत्यक्षज्ञानकर्ता गणधर भट्टारक हैं और उनके द्वारा उपदिष्ट गाथाओंमें सम्पूर्ण कसायपाहुडका अर्थ समाविष्ट है। आचार्य वीरसेनने उसी संदर्भ में आगे लिखा है कि तीसरा कषायनाभूत महासमुद्रके तुल्य है और आचार्य गुणधर उसके पारगामी हैं।
वीरसेनाचार्यके उक्त कथनसे यह ध्वनित होता है कि आचार्य गुणधर पूर्व विदोंकी परम्परा में सम्मिलित थे, किन्तु धरसेन पूर्वविद् होते हुए भी पूर्वविदोंकी परम्परामें नहीं थे। एक अन्य प्रमाण यह भी है कि धरसेनकी अपेक्षा गुणधर अपने विषयके पूर्ण ज्ञाता थे। अतः यह माना जा सकता है कि गुणधर ऐसे समय में हुए थे जब पूवों के आंशिक ज्ञानमें उतनी कमी नहीं आयी थो, जितनी कमी धरसेनके समयमें आ गयी थी । अतएव गुणधर धरसेनके पूर्ववर्ती हैं।
आचार्य गुणधरके समयके सम्बन्धमें विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इनका समय धरसेनके पूर्व है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लोहार्य तकको गुरु परम्पराके पश्चात् विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हदत्त इन चार आचार्यो का उल्लेख किया गया है। ये सभी आचार्य अंगों और पूर्वों के एकदेशज्ञाता थे। इनके पश्चात् अर्हद्वीलिका नाम आया है। अर्हद्वीलि बड़े भारी संघनायक थे। इन्हें पूर्वदेशके पुण्ड्वर्धनपूरका निवासी कहा गया है। इन्होंने पञ्चवर्षीय युगप्रतिक्रमणके समय बड़ा भारो एक यति-सम्मेलन किया, जिसमें सौ योजन तकके यति सम्मिलित हुए। इन यत्तियोंको भावनाओंसे अर्हद्वीलिने ज्ञात किया कि अब पक्षपातका समय आ गया है। अतएव इन्होंने नन्दि, वीर, अपराजित, देव, पञ्चस्तूप, सेन, भद्र, गुणधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामोंसे भिन्न-भिन्न संघ स्थापित किये, जिससे परस्परमें धर्मवात्सल्यभाव वृद्धिंगत हो सके।
संघके उक्त नामोंसे यह स्पष्ट होता है कि गुणधरसंघ आचार्य गुणधरके नाम पर ही था । अतः गुणधरका समय अर्हद्वीलिके समकालीन या उनसे भी पूर्व होना चाहिए। इन्द्रनन्दिको गुणधर और धरसेनका पूर्व या उत्तरवर्तीय ज्ञात नहीं है। अतएव उन्होंने स्वयं अपनो असमर्थता व्यक्त करते हुए लिखा है-
गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरकमोऽस्माभिः ।
न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात् ।। १५१ ।।
अर्थात् गुणधर और धरसेनको पूर्वापर गुरुपरम्परा हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि इसका वृत्तान्त न तो हमें किसी आगम में मिला और न किसी मुनिने ही बतलाया।
स्पष्ट है कि इन्द्रनन्दिके समय तक आचार्य गुणधर और धरसेनका पूर्वापर वत्तित्व स्मृत्तिके गर्भ में विलीन हो चुका था। पर इतना स्पष्ट है कि अर्हद्वीलि द्वारा स्थापित संघोंमें गुणधरसंघका नाम आया है। नन्दिसंघको प्राकृत पट्टावली में अर्हद्वीलिका समय वीर निर्वाण सं. ५६५ अथवा वि. सं. ९५ है। यह स्पष्ट है कि गुणधर अर्हद्वीलिके पूर्ववर्ती है; पर कितने पूर्ववर्ती हैं, यह निर्णयात्मक रूपसे नहीं कहा जा सकता। याद गणधरको परम्पराको ख्याति प्राप्त करने में सौ वर्षका समय मान लिया जाय तो 'छक्खंडागम' प्रवचनकर्ता घरसेनाचार्य से 'कसायपाहुड' के प्रणेता गुणवराचार्यका समय लगभग दो सौ वर्ष पूर्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आचार्य गुणधरका समय विक्रम संवत पूर्व प्रथम शताब्दी सिद्ध होता है।
हमारा यह अनुमान केवल कल्पना पर आधृत नहीं है। अर्हद्वीलिके समय तक गुणधरके इतने अनुयायी यति हो चुके थे कि उनके नामपर उन्हें संघकी स्थापना करनी पड़ी। अतएव अर्हद्वीलिको अन्य संघोंके समान गुणधर संघका भी मान्यता देनी पड़ी। प्रसिद्धि प्राप्त करते और अनुयायो बनानेमें कमसे कम सौ वर्षका समय तो लग ही सकता है। अतः गुणधरका समय धरसेनसे कमसे कम दो सौ वर्ष पूर्व अवश्य होना चाहिये।
इनके गुरु आदिके सम्बन्धमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। गुणधरने इस ग्रन्थकी रचना कर आचार्य नागहस्ति और आर्यमक्षुको इसका व्याख्यान किया था। अतएव इनका समय उक्त आचार्योंसे पूर्व है। छक्खंडागमके सूत्रों के अध्ययनसे भी यह अवगत होता है कि 'पेज्जदोसपाहुड' का प्रभाव इसके सूत्रों पर है। भाषाका दृष्टिसे भा छक्खंडागमकी भाषा कसायपाहुडकी भाषाकी अपेक्षा अर्वाचीन है। अतः गुणधरका समय वि. पू. प्रथम शताब्दी मानना गर्वथा उचित है! जयधवलाकारने लिखा है- "पुणो ताओ चेव सुत्तगाहाओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणीओ अज्जमं खुणागहत्थीणं गत्ताओ। पुणो नेसि दोण्हं पि पादमूले असोदिसदमाहाणं गुणहर मुहकमलविणिग्गयाणमार्थ सम्मं सोङ्गण जयीवसहभडारएण पचयणवच्छलेण चुन्नीसुतं कयं।'
अर्थात् गुणधराचायके द्वारा १८० गाथाओं में कसायपाहुड़का उपसंहार कर दिये जाने पर वे हा सुनगाथाएँ आचार्यपरम्परासे आती हुई आयमंक्षु और नागहस्तिको प्राप्त हुई। पश्चात उन दोनों ही आचार्या के पादमलमें बैठकर गुणधराचार्यके मुखकमलसे निकली हुई उन १८० गाथाओंके अर्थको भले प्रकारसे श्रवण करके प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित हो यतिवृषभ भट्टारकने उनपर चूणिसूत्रोंकी रचना की। इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि आचार्य गुणधरने महान विषयको संक्षेपमें प्रस्तुत कर सूत्रप्रणालीका प्रवर्तन किया। गुणधर दिगम्बर परम्पराके सबसे पहले सूत्रकार हैं।
गणघराचार्यने 'कसायपाहुड', जिसका दूसरा नाम 'पेज्जदोसपाहुड' भी है, को रचना की है। १६००० पद प्रमाण कसायपाहुडके विषयको संक्षेपमें एकसौ अस्सी गाथाओंमें ही उपसंहृत कर दिया है।
'पेज्ज' शब्दका अर्थ राग है। यतः यह ग्रन्थ राग और द्वेषका निरूपण करता है। क्रोधादि कषायोंको रागद्वेष परिणति और उनकी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेशबन्ध सम्बन्धी विशेषताओंका विवेचन ही इस ग्रन्थका मूल वर्ण्य विषय है। यह ग्रन्थ सूत्रशेलीमें निबद्ध है| गुणधरने गहन और विस्तृत विषधको अत्यन्त संक्षेपमें प्रस्तुत कर सूत्रपरम्पराका आरंभ किया है। उन्होंने अपने ग्रंथके निरूपणकी प्रतिज्ञा करते हुए गाथाओंको सुनगाहा कहा है-
गाहासदे असीदे अत्ये पण्णरसधा विहतम्मि |
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्यम्मि ॥२॥
स्पष्ट है 'कसायपाहुड' की शैली गाथासूत्र शैली है। प्रश्न यह है कि इन गाथाओंको सूत्रगाथा कहा जाय अथवा नहीं? विचार करनेसे ज्ञात होता है कि 'कसायपाहुड' की गाथाओं में सूत्रशैलीके सभी लक्षण समाहित हैं। इस ग्रन्थकी जयधवला-टीकामें आचार्य वीरसेनने आगमदृष्टिसे सूत्रशैलीका लक्षण बतलाते हुए लिखा है- सुत्तं
गणहरकहियं तहेय पत्तेयबुद्धकहियं च।
सुदकेवलिणा कहियं अभिष्णदसपुब्धिकहियं च।।
अर्थात् जो गणघर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्नदसपूर्वियों द्वारा कहा जाय यह सूत्र है।
अब यहाँ प्रश्न यह है कि गुणधर भट्टारक न तो गणधर हैं, न प्रत्येकबुद्ध हैं, न श्रुतकेवली हैं और न अभिन्नदशपूर्शी हैं। अत: पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार इनके द्वारा रचित गाथाओंको सूत्र कैसे माना जाय? इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य वीरसेनने लिखा है कि आगमद्रुष्टिसे सूत्र न होने पर भी शैलीकी दृष्टि से ये सभी गाथाएँ सूत्र है- 'इदि वयणादो णेदाओ गाहाओ सुत्तं गणहर-पत्तेयबुद्ध-सुदकेवलि-अभिण्णदसपुब्बीसु गुणहरभद्धारयस्स अभावादो; ण, णिड्डोसापकावर सहेउपमानेहि सुत्तेण ससित्तमस्थि त्ति सुत्तत्तुवलंभादो।' अर्थात् गुणधर भट्टारकको माथाएं निर्दोष, अल्पाक्षर एवं सहेतुक होनेके कारण सूत्रके समान हैं।
सूत्रशब्दका वास्तविक अर्थ बाजपद है। तीर्थंकरके मुखसे निस्सत बोज पदोंको सूत्र कहा जाता है और इस सूत्रके द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सूत्र सम कहलाता है-
'इदि वयणादा तिस्थयरवयणचिणिगयबीजपदं सुतं । तेण सुत्तेण समं धट्टीद उप्पज्जादि त्ति गणहरदेवम्मि द्विदसुदणाणं सुतसम'।
बन्धन अनुयोगद्वारमें सूत्रका अर्थ श्रुतकेवली या द्वादशांगरूप शब्दागम लिया गया है और श्रुतकेवली के समान श्रुतज्ञानको भी सूत्रसम कहा है; पर कृतिअनुयोगद्वारमें जो सूत्रको परिभाषा बतलाया गयी है उसके अनुसार द्वादशांगका सूत्रागममें अन्तर्भाव न होकर ग्रन्यागममें अन्तर्भाव होता है। यतः कृतिअनुयोगद्वारमें गणधर द्वारा रचे गये द्रव्यश्रुतको ग्रन्थागम कहा है।
आचार्य वीरसेनका अभिमत है कि सूत्रको समग्र परिभाषा जिनेन्द्र द्वारा कथीत अर्थपदोंमें ही पायी जाती है, गणधरदेवके द्वारा ग्रंथित द्वादशांगमें नहीं। इस विवेचनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि गुणपर आचार्य द्वारा विरचित 'कमायपाहुड’ में आगमसम्मत सूत्रकी परिभाषा घटित नहीं होती; पर सूत्रशैलीके समस्त लक्षण इसमें समाहित हैं। प्राचार्य वीरसेनने जयधवलामें 'कसायपाहुड' को सूत्रग्रन्थ सिद्ध करते हुए लिखा है-
"एवं सञ्चं पि सुत्तलक्षणं जिणवयणकमलविष्णिग्गय अथ्यपदाणं चेव संभवङ्, ण गणहरमुहविणिरायगंथरयणाए, तत्थ महापरिमाण तुवलंभादो; ण; सच्च (सुत्त) सारिच्छमस्सिदूण तत्थ वि सुत्तत्तं पडी विरोहाभावादो।"
अर्थात् सूत्रका सम्पूर्ण लक्षण तो जिनदेवके मुखकमलसे निस्सृत अर्थपदों में ही संभव है, गणधरकै मुखकमलसे निकली हुई रचनामें नहीं; क्योंकि गणधर की रचनाओंमें महापरिमाण माना जाता है। इतना होनेपर भी गणधरके वचन भी सूत्रके समान होनेके कारण सूत्र कहलाते हैं। अतः उनकी ग्रंथरचनामें भी सूत्रत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है। गणधरवचन भी बीजपदोंके समान सूत्र रूप है। अतएव गुणधर भट्टारककी रचना ‘कसायपाहुड़’ में सूत्रशैलीके सभी प्रमुख लक्षण घटित होते हैं। यहाँ विश्लेषण करनेपर निम्नलिखित सूत्रलक्षण उपलब्ध है-
१. अर्थमत्ता
२. अल्पाक्षरता
३. असंदिग्धता
४. निर्दोषता
५. हेतुमत्तता
६. सारयुक्तता
७. सोपस्कारता
८. अनवद्यता
९. प्रामाणिकता
स्पष्ट है कि कसायपाहुडकी गाथाओंकी शैली सूत्रशैली है। इस ग्रंथमें १८० + ५३ = २३३ गाथाएँ हैं। इनमें १२ गाथाएँ सम्बन्धज्ञापक हैं, छ: गाथाएं अधपरिमाणका निर्देश करती हैं और ३५ गाथाएँ संक्रमणवृतिसे सम्बद्ध हैं। जयधवलाके अनुसार ये समस्त २३३ गाथाएँ आचार्य गणधर द्वारा विरचित हैं। यहाँ यह शंका स्वभावतः उत्पन्न होती है कि जब ग्रन्थमें २२३ गाथाएँ थीं, तो ग्रन्थके आदिमें गुणधराचार्यने १८० गाथाओंका ही क्यों निर्देश किया? आचार्य वीरसेनने इस शंकाका समाधान करते हुए बताया है कि १५ अधिकारों में विभक्त होनेवाली गाथाओंको संख्या १८० रहने के कारण गुणधराचार्यने १८० गाथाओंकी संख्या निर्दिष्ट की है। सम्बन्ध-गायाएँ तथा अज्ञापरिमाण निर्देशक गाथाएँ इन १५ अधिकारोंमें सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। अतः उनकी संख्या छोड़ दी गयी है।
आचार्य वीरसेनने पुनः शंका उपस्थित की है कि संक्रमण सम्बन्धी ३५ गाथाएं बन्धक नामक अधिकारमें समाविष्ट हो सकती हैं, तब क्यों उनकी गणना उपस्थित नहीं की? इस शंकाका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रारंभके पांच अर्थाधिकारों में केवल तीन ही गाथाएं हैं और उन तीन गाथाओंसे निबद्ध हुए पांच अधिकारों से बन्धक नामक अधिकारसे ही उक्त ३५ गाथाएँ सम्बद्ध हैं। अतः इन ३५ गाथाओंको १८० गाथाओंकी संख्यामें सम्मिलित करना कोई महत्वकी बात नहीं है। हमारा अनुमान है कि जिन ५३ गाथाओंकी गणना आचार्य गुणधरने नहीं की है वे गाथाएं संभवत: नागहस्तिद्वारा विरचित होनी चाहिए। हमारे इस अनुमानकी पुष्टि जयधवलासे भी होती है। जयधवलामें मतान्तरसे उक्त ५३ गाथाओंको नागहस्तिकृत माना है।
एक बात यह भी विचारणीय है कि सम्बन्धनिर्देशक १२ गाथाओं और अद्धापरिमाणनिर्देशक छ: गाथाओं पर यत्तिवृषभके चूर्णिसूत्र भी उपलब्ध नहीं हैं। यदि ये गाथाएँ गुणधर भट्टारक द्वारा विरचित होती तो यतिवृषभ इनपर अवश्य ही चूणिसूत्र लिखते। दूसरी बात यह कि संक्रमणसे सम्बद्ध ३५ गाथाओं मेंसे १३ गाथाएँ शिवशर्म रचित कर्मप्रकृतिमें भी पायी जाती हैं। यह सत्य है कि उक्त तथ्योंसे ५३ गाथाओंके रचयिता नामहस्ति सिद्ध नहीं होते, पर इसमें आशंका नहीं कि उक्त ५३ गाथाएँ गुणधर भट्टारक द्वारा विरचित नहीं। यद्यपि आचार्य वीरसेनने व्याख्याकारोंके मतोंको स्वीकार नहीं किया है तो भी समीक्षाकी दृष्टिसे ५३ गाथाओंको गुणधर भट्टारक द्वारा विरचित नहीं माना जा सकता है। रचनाशेलीकी दुष्टिसे १८० गाथाओंकी अपेक्षा ५३ गाथाओंकी शैली भिन्न प्रतीत होती है। एक अनुमान यह भी है कि आचार्य गुणधरने १८० गाथाओंको १५ अधिकारोंमें विभक्त करनेवाली प्रतिज्ञा नहीं की है। उनकी प्रतिज्ञा तो यह होनी चाहिए थी कि सोलह हजार पद प्रमाण कषायप्रामृतको एक-सो अस्सी गाथाओंमें संक्षिप्त करता हूँ। वस्तुत: गुणधराचार्य कषाय प्राभूतको उपसंहत करनेके लिए प्रवृत्त हुए थे, स्वरचित गाथाओंको अधिकारोंमें विभक्त करनेके लिए नहीं।
'सस्तेदा गाहाओ'; 'एदाओ सुत्त गाहाओं' आदि पदोंसे यह ध्वनित होता है कि इन गाथाओंकी रचनासे पूर्व मूलगाथाओं और भाष्यगाथाओंकी रचना हो चुकी थी। अन्यथा अमुक गाथासूत्र है, इस प्रकारका कथन संभव ही नहीं था। अतएव व्याख्याकारोंके, 'गाहासदे असीदे’ प्रतिज्ञावाक्य नागहस्तिका है, इस अभिमतको सर्वथा उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता है।
कसायपाहुडमें १५ अधिकार हैं जो निम्न प्रकार है-
१. प्रकृति-विभक्ति अधिकार
२. स्थिति-विभक्ति अधिकार
३. अनुभाग-विमति अधिकार
४. प्रदेश-विभक्ति-झीणाझीण-स्थित्यन्तिक
५. बंधक अधिकार
६. वेदक अधिकार
७. उपयोग अधिकार
८. चतुःस्थान अधिकार
९. व्यंजन अधिकार
१०. दर्शनमोहोपशमना अधिकार
११. दर्शनमोहक्षपणा अधिकार
१२. संयमासंगमलब्धि अधिकार
१३. संयमलब्धि अधिकार
१४. चारित्रमोहोपशमना
१५. चारित्रमोहक्षपणा
१. प्रकृति-विभक्ति- अधिकारका अन्य नाम 'पेज्जदोस-विभक्ती' है। यतः कषाय पेज्ज- राग या देषरूप होती है। चूर्णिसूत्रोंमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंका विभाजन राग और द्वेषमें किया है। नैगम और संग्रहनयकी दृष्टिसे क्रोध और मान द्वेषरूप हैं तथा माया और लोभ रागरूप हैं। व्यवहारनय मायाको भी द्वेषरूप मानता है। यतः लोकमें मायाचारीकी निन्दा होती है। ऋजुसूत्रनय कोधको द्वेषरूप तथा लोभको रागरूप मानता है। मान और माया न तो रागरूप है और न द्वेषरूप ही; क्योंकि मान क्रोधोत्पत्तिके द्वारा द्वेषरूप है तथा माया लोभोत्पत्तिके कारण रागस्प है स्वयं नहीं। अत: इस परम्पराका व्यवहार ऋजुसूत्रनयकी सीमामें नहीं आता। तीनों शब्दनय चारों कषायोंको द्वेषरूप मानते हैं क्योंकि उनसे कर्मों का आनंद होता है। राग और दोषोंका विवेचना हादा अनुहारों में किया गण है एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भागाभागातुगम और अल्पबहुत्वानुगम।
२. स्थिति-विभक्ति-आत्माकी शक्तियोंको आवृत्त करनेवाला कर्म कहलाता है। यह पुद्गलरूप होता है। इस लोकमें सूक्ष्म कर्मपुद्गलस्कन्ध भरे हुए हैं जो इस जीवकी कायिक, वाचनिक और मानसिक प्रवृत्तिके साथ आकृष्ट होकर स्वतः आत्मासे बद्ध हो जाते हैं। कर्मपरमाणुओंको आकृष्ट करनेका कार्य योग द्वारा होता है। यह योग मन, वचन, काय रूप है। इस योगकी जैसी शुभाशुभ या तीव्र-मन्दरूप परिणति होती है उसीप्रकार कर्मों का आस्रव होता है। कषायके कारण कर्मों में स्थिति और अनुभाग उत्पन्न होते हैं। जब कर्म अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदयमें आते हैं तो इष्ट या अनिष्ट फल प्राप्त होता है। इसप्रकार जीव पूर्वबद्ध कर्मके उदयसे क्रोधादि कषाय करता है और उससे नवीन कर्मका बन्ध करता है। कर्मसे कषाय और कषायसे कर्मबन्धकी परम्परा अनादि है।
कर्मबन्धके चार भेद हैं- १. प्रकृतिबन्ध, २. स्थितिबन्ध, ३. अनुभाग बन्ध, ४. प्रदेशबन्ध। कर्मोंमें ज्ञान-दर्शनादिको रोकने और सुख-दुःखादि देनेका जो स्वभाव पड़ता है उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कर्म बन्धनेपर कितने समय तक आत्माके साथ बद्ध रहेंगे उस समयकी मर्यादाका नाम स्थितिबन्ध है। कर्म तीव्र या मन्द जैसा फल दें उस फलदानकी शक्तिका पड़ना अनुभागबन्ध है। कर्मपरमाणुओंकी संख्याके परिमाणका नाम प्रदेशबन्ध है। प्रकृति और प्रदेशनन्ध योग- मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे होते हैं। तथा स्थिति और अनु भागबन्ध कषायसे होते हैं । . स्थिति-विभक्तिनामक इस द्वित्तीय अधिकारमें स्थितिबन्ध के साथ प्रकृति बन्धका भी कथन सम्मिलित है। प्रकृति और स्थितिबन्धका एक जीवको अपेक्षा कथन स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंको अठेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्वकी दृष्टिसे किया है। कसायपाहुडमें मोहनीयकर्मका वर्णन विशेष रूपसे आया है। इस अधिकारमें प्रकृत्ति-विभक्ति के दो भेद किये हैं। प्रथम भेद मूलप्रकृति मोहनीयकर्म है और द्वितीय भेद उत्तरप्रकृतिमें मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ ग्रहण की गई हैं। इसप्रकार विभिन्न अनुयोगों द्वारा स्थिति-विभक्तिमें चौदह मार्गणाओंका आश्रय लेकर मोहनीयके २८ भेदोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बतलायो गई है। अद्धाच्छेद, सर्वविक्ति, नोसर्व विभक्ति, उत्कृष्टविक्ति, अनुत्तकृष्टविभक्ति, जयन्यविभक्ति, अजघन्मविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति आदिका कथन किया है।
३. अनुभाग-विभक्ति- अधिकारमें कर्मोंको फलदार-शक्तिका विवेचन किया गया है। आचार्यने यहां उस अनुभागका विचार किया है जो बन्धसे लेकर सत्ताके रूपमें रहता है। वह जितना बन्धकालमें हुआ उतना भी हो सकता है और होनाधिक भी संभव है। उसके दो भेद हैं- १. मूलप्रकृति-अनुभाग विभक्ति और २. उत्तरप्रकृति-अनुभागविभक्ति । इस सबका वर्णन संक्षेपमें किया है। इस अधिकारमें संज्ञाके दो भेद किये हैं- १. घातिसंज्ञा और २. स्थानसंज्ञा। मोहनीयकर्म की घातिसंज्ञा है क्योंकि वह जीवके गुणोंका घातक है। घातीके दो भेद हैं- सर्वघाती औः देशघाती। मोहनीवर उत्क्रुस्त अनुभाग सर्वघाती है और अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघातो और देशघाती दोनों प्रकारका है। इसी तरह जघन्य अनुभाग और अजघन्य अनुभाग देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकारका है। स्थान अनुभागके चार प्रकार है- एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक । इस प्रकार अनुभागनवभक्तिमें अनुभागके विभिन्न भेद-प्रभेदोंका कथन किया है।
४. प्रदेश-विभक्ति- कर्मों का बन्ध होनेपर तत्काल बन्धको प्राप्त कर्मों को जो द्रव्य मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। इसके दो भेद हैं- प्रथम बन्धके समय प्राप्त द्रव्य और द्वितीय बन्ध होकर सत्तामें स्थित द्रव्य| कसायपाहूडमें इस द्वितीयका हो निरूपण आया है। मोहनीय कर्मको लेकर स्वामित्व, काल, अन्तर, भंगविचय आदि दुष्टियोंसे विचार किया है। अनुभागके दो प्रकार है - जीवभागाभाग और प्रदेशभागाभाग। पहले की चर्चामें कहा है कि उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्ति बाले जीव सब जीवों के अनन्तमें भाग प्रमाण है। और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्ति बाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग प्रमाण है। इस प्रकार इस प्रदेश-विभक्ति अधिकारमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण प्रति कर्मों को स्थितियोंका भी विचार किया गया है।
५. बंधक - अधिकारमें कर्मवर्गणाओंका, मिथ्यात्व, अविरति आदिके निमित्तसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारके कर्मरूप परिणमनका कथन आया है। इस अधिकारमें बन्ध और संक्रम इन दो विषयोंका व्याख्यान किया है। गुणधर भट्टारकने इस बन्धक अधिकारमें संक्रमका भी अन्तर्भाव किया है। बन्धके दो भेद बताये है- १. अकर्मबन्ध और २. कर्मबन्ध| जो कार्माणवर्गणाएं कर्मरूप परिणत नहीं हैं उनका कर्मरूप परिणत होना अकर्म बन्ध है और कर्मरूप परिणत पुद्गलस्कन्धोंका एक कर्मसे अपने सजातीय अन्य कर्मरूप परिणमन करना कर्मबन्ध है। यह द्वितीय कर्मबन्ध भेद ही संक्रमरूप है। यही कारण है कि इस बन्धके अधिकारमें बन्ध और संक्रम इन दोनोंका समावेश हो जाता है। आचार्यने 'कदि पयडीओ बन्धदि' आदि २३ संख्यक गाथामें इस अधिकारका वर्णन किया है।
६. वेदक अधिकार- इस अधिकारमें बताया है कि यह संसारी जीव मोह नीयकर्म और उसके अवान्तर भेदोंका कहाँ कितने काल तक सान्तर या निरन्तर किस रूपमें वेदन करता है। इस अधिकारके दो भेद है- उदय और उदोरणा। उदीरणा सामान्यतः उदयविशेष ही है। किन्तु इन दोनोंमें अन्तर यह है कि कर्मों का जो यथाकाल फलविपाक होता है उसकी उदयसंज्ञा है और जिन कर्मों का उदयकाल प्राप्त नहीं हुआ उनको उपायविशेषसे पचाना उदोरणा है। इस अधिकारको गुणधरने चार गाथासूत्रोंमें निबद्ध किया है। यहाँ उदोरणा, उदय और कारणभूत बाह्य सामग्रीका निर्देश किया गया है। प्रथम पाद द्वारा उदीरणा सुचित की गयी है। द्वितीय पाद द्वारा विस्तार सहित उदय सूचित किया है और शेष दो पादों द्वारा उदयावलीके भीतर प्रविष्ट हुई उदय प्रकृत्तियों और अनुदयप्रकृतियोंको ग्रहण कर प्रवेशसंज्ञावाले अर्थाधिकारका सूचन किया है। गाथाके पूर्वाद्धका स्पष्टीकरण करनेके पश्चात् उत्तरार्द्ध में बताया है कि क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलोंको निमित्त कर कर्मों का उदय और उदौरणारूप फलत्रिपाक होता है। यहाँ क्षेत्रपदसे नरकादिगतियोंका क्षेत्र, भवपदसे एक इन्द्रियादि पर्यायोंका, कालपदसे बसन्त, ग्रीष्म और वर्षा आदिका एवं पुद्गल पदसे ग्रंथ, ताम्बूल, वस्त्र, आभरण आदि पुद्गलोंका ग्रहण किया है।
उदीरणाके समग्र विवेचनके पश्चात् गाथाके उत्तरार्द्ध में उदयका कथन किया है। उदीरणाके मूल प्रकृति उदोरणा और उत्तरप्रकृति उदोरणा ये दो भेद किये गये हैं। उत्तरवर्ती टोकाकारोंने १७ अनुयोगनारोंका आश्रय लेकर उदीरणाओंका विस्तृत विवेचन किया है।
वेदक अधिकारकी दूसरी गाथाका दूसरा पाद है 'को व केय अणुभागे' अर्थात् कौन जीव किस अनुभागमें मिथ्यात्व आदि कर्मों का प्रवेशक है। गाथासूत्रके इस पादको व्याख्या चूर्णिसूत्रकार और टीकाकारोंने विस्तारपूर्वक की है।"
७. उपयोगाधिकार में जीवके क्रोध, मान, मायादिरूप परिणामोंको उपयोग कहा है। इस अधिकार में चारों कषायोंके उपयोगका वर्णन किया गया है। और बतलाया है कि एक जीवके एक कायका उदय कितने काल तक रहता है और किस गत्तिके जीवके कौन-सी कषाय बारबार उदयमें आती है। एक भवमें एक कषायका उदय कितने बार होता है और एक कषायका उदय कितने भवों तक रहता है। जितने जीय वर्तमान समयमें जिस कषायसे उपयुक्त हैं क्या वे उतने ही पहले उसी कवायसे उपयुक्त थे? और आगे भी क्या उपयुक्त रहेंगे? आदि कषायविषयक सासष्य बातोंका विवेचन इस अधिकारमें किया है।
८. चतुःस्थान अधिकार- वातियाकर्मों की फलदानशक्तिका विवरण लता, दारू, अस्थि और शेलरूप उपमा देकर किया गया है। इन्हें क्रमशः एक स्थान, द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुःस्थान भी कहा गया है।
इस प्रस्तुत अधिकारके नामकरणका कारण भी उक्त चार स्थानोंका रहना हो है। उपमाओं द्वारा क्रोधको पाषाणरेखाके समान, पृथ्वीरेखाके समान, बालुरेखाके समान और जलरेखाके समान बसाया है। जिस प्रकार जलमें खिंची हुई रेखा तुरंत मिट जाती है और बालू, पृथ्वी और पाषाणपर खिंची गई रेखाएँ उत्तरोत्तर अधिक समयमें मिटती है, उसी प्रकार हीनाधिक कालकी अपेक्षासे क्रोधके भी चार स्थान है। इसी क्रमसे मान, माया और लोभके भी चार-चार स्थानोंका निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त चारों कषायोंके सोलह स्थानोंमेंसे कौन-सा स्थान किस स्थानसे अधिक होता है और कोन किससे हीन होता है, कोन स्थान सर्वघाती है, कोन स्थान देशघाती है? आदिका विचार किया गया है।
९. व्यजन अधिकार- व्यञ्जनका अर्थ पर्यायवाधी शब्द है। इस अधिकार में क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों हो कषायोंके पर्यायवाचक शब्दोंका प्रतिपादन किया गया है। क्रोधके पर्याय रोष ,अक्षमा, कलह, विवाद आदि बतलाये हैं। मानके पर्याय, मान, मद, दर्प, स्तम्भ, परिभव तथा मायाके, माया, निकृति, वंचना, सातियोग और अनऋजुता आदि बतलाये गये हैं। लोभके पर्यायोंमें लोभ, राग, निदान, प्रेयस्, मळ आदि बतलाये गये हैं। इस प्रकार विभिन्न पर्यायवाची शब्दों द्वारा कषायविषयोंपर विचार-विमर्श किया गया है।
१०. दर्शनमोहोपशमनाधिकार-जिस कर्मके उदयमें आनेपर जीवको अपने स्वरूपका दर्शन- साक्षात्कार और यथार्थ प्रतीति न हो उसे दर्शनमोहकर्म कहते हैं। इस कर्मके परमाणुओंका एक अन्तर्मुहसके लिए अभाव करने या उपशान्त रूप अवस्थाके करनेको उपशम कहते हैं। इस दर्शनमोहके उपशमनकी अवस्था में जीवको अपने वास्तविक स्वरूपका एक अन्तमुहूर्तके लिए साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कारकी स्थितिमें जो उसे आनन्द प्राप्त होता है वह अनिर्वच नीय है। दर्शनमोहके उपशमन करने वाले जीदके परिणाम कैसे होते हैं, उसके कौन सा योग होता, कौन-सा उपयोग रहता है। कौन-सी कषाय होती है और कौन-सी लेश्या, आदि बातोंका निरूपण करते हुए उन परिणाम विशेषोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। दर्शनमोहके उपशमको चारों गतियोंके ही जीव कर सकते हैं, पर उन्हे संज्ञी, पन्चेन्द्रिय और पर्याप्तक होना चाहिए। इस अधिकारके अन्तमें प्रथमोपशम-सम्यक्त्वीके विशिष्ट कार्यों और अवस्थाओंका वर्णन भी आया है।
११. दर्शनमोक्षपणा अधिकार- दर्शनमोहकी उपशम अवस्था अन्त मुहूर्त तक ही रहती है। इसके पश्चात् वह समाप्त हो जाती है| और जीव पुनः आत्मदर्शनसे वंचित हो जाता है। आत्मसाक्षात्कार सर्वदा बना रहे, इसके लिए दर्शन मोहका क्षय आवश्यक है। इसके लिये जिन प्रमुख बातोंकी आवश्यकता होती है उन सबका विवेचन इस अधिकार में किया गया है। दर्शनमोहके क्षयका प्रारम्भ कर्मभूमिमें उत्पन्न मनुष्य ही कर सकता है और इसकी पूर्णता चारों गतियों में की जा सकती है। दर्शनमोहके क्षपणका काल अन्तर्मुहूर्त है। इस क्षपर्णावयाके समाप्त होनेके पूर्व हो यदि उस मनुष्यको मृत्यु हो जाय तो वह अपनी आयुबन्धके अनुसार यथासंभव चारों ही गतियों में उत्पन्न हो सकता है। दर्शनमोहके क्षपणका प्रारम्भ करने वाला मनुष्य अधिक से अधिक तीन भव और धारण करके मुक्तिलाभ करता है। इस अधिकारमें दर्शनमोहक क्षपणकी प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी साधन-सामग्रीका निरूपण किया गया है।
१२. संयमासंयमलब्धि अधिकार- आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होते ही जीव मिथ्यास्वरूप पंकसे निकलकर निर्मल सरोवरमें स्नान कर आनन्दमें निमग्न हो जाता है। उसको विचारधारा सांसारिक विषयवासनासे दूर हो संयमासंयमकी प्राप्तिकी ओर अग्रसर होती है। शास्त्रीय परिभाषाके अनुसार अप्रत्याख्यानावरणकषायके उदयके अभावसे देशसंयमको प्राप्त करने वाले जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उसे संयमासंयमलब्धि कहते हैं। इसके निमित्तसे जोव श्रावकके व्रतोंको धारण करने में समर्थ होता है। इस अधिकारमें संयमासंयमलब्धिके लिये आवश्यक साधन-सामग्रियोंका विस्तार पूर्वक कथन किया है।
१३. संयमलब्धि अधिकार- प्रत्याख्यानावरणकषायके अभाव होनेपर आत्मामें संयमलब्धि प्रकट होती है, जिसके द्वारा आत्माकी प्रवृत्ति हिंसादि पाँच पापोंसे दूर होकर अहिंसादि महाव्रतोंके धारण और पालनकी होती है। संयमासंयम अधिकारकी गाथा ही इस अधिकारको गाथा है। संयमके प्राप्त कर लेनेपर भी कषायके उदयानुसार जो परिणामोंका उतार-चढ़ाव होता है उसका प्ररूपण अल्पबहुत्त्व आदि भेदों द्वारा किया गया है। इस लब्धिका वर्णन चूणिसूत्रकारने अधःकरण और अपूर्वकरणके विवेचन द्वारा किया है, जो अध्यात्म प्रेमी उपशमसम्यक्त्वके साथ संघमासंयम धारण करते हैं उनके तीनों करण होते हैं, पर जो वेदकसम्यकदृष्टि संयमासंयमको धारण करते हैं उनके दो ही करण होते हैं। संयमको धारण करनेके लिये आवश्यक सामग्रीका भी कथन किया गया है।
१४. चारित्रमोहोपशमनाधिकार- इस अधिकारमें प्रथम आठ गाथाएँ आती हैं। पहली गाथाके द्वारा उपशमना कितने प्रकारकी होती है, किस-किस कर्मका उपशम होता है आदि प्रश्न किये गये हैं। दूसरी गाथाके द्वारा निरुद्ध चारित्रमोहप्रकृतिको स्थितिके कितने भागका उपशम करता है, कितने भागका संक्रमण करता है और कितने भागका उदीरणा करता है इत्यादि प्रश्नोंकी अव तारणा की गयी है। तीसरी गाथाके द्वारा चारित्रमोहनीयका उपशम कितने कालमें किया जाता है उसो उपशमित प्रकृतिको उदोरणा-संक्रमण कितने काल तक करता है इत्यादि प्रश्न किये गये हैं। चौथी गाथाके द्वारा आठ करणोंमेंसे उपशामकके कब, किस करणसे व्युछित्ति होती है या नहीं इत्यादि प्रश्नोंका अव तार किया गया है। इस प्रकार चार गाथाओंके द्वारा उपशामकके और शेष चार गाथाओंके द्वारा उपशामकके पतनके सम्बन्ध में प्रश्न किये गये हैं।
१५. चारित्रमोहक्षपणाधिकार- यह अन्तिम अधिकार बहुत विस्तृत है। इसमें चारित्रमोहनीयकर्मके क्षयका वर्णन विस्तारसे किया है। यहां यह ध्यातव्य है कि चारित्रमोहनीयका क्षय अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करपके बिना संभव नहीं है। इस अधिकारमें २८ मूलगाथाएँ हैं ओर ८६ भाष्यगाथाएँ हैं। इस प्रकार कुल ११४ गाथाओंमें यह अधिकार व्याप्त है। इनमेंसे चार सूत्रमाथाएँ अधःप्रवृत्तिकरणके अन्तिम समयसे प्रतिबद्ध हैं। इनके आधारपर चूणिसूत्रों और जयधवलामें योग और कषायोंको उत्तरोत्तर विशद्धिका चित्रण किया गया है। आशय यह है कि चारित्रमोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंका क्षय किस क्रमसे होता है और किस-किस प्रकृतिक क्षय होनेपर कहाँपर कितना स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्व रहता है इत्यादि बातोंका वर्णन इस अधिकारमें आया है। ध्यान और कषायक्षयको प्रक्रिया भी इस अधिकारमें वर्णित है।
बायपावना को नीदर महावीरकी आरातीय परम्परासे प्राप्त हुआ है| वीरसेनाचार्य ने जयधवला-टीकामें लिखा है- "एदम्हादो विउलगिरिमत्ययस्थवड्डमाणदिवायरादो विणिग्यमिय गोदम लोहज्ज-जंबुसामियादि-आइरियपरंपराए आगंतूण गुणहराइरियं पाविय गाहास रूवेण परिणामय" अर्यातविपुलाचलके शिखरपर विराजमान वर्धमान दिवाकरसे प्रकट होकर गौतम, लोहाचार्य, जम्बूस्वामी आदिकी आचार्यपरम्परासे आकर गुणधरको 'कम्मपडिपाहुड' का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने गाथारूपमें इस ज्ञान का प्रतिपादन किया | स्पष्ट है कि आचार्य गुणधरको केलियोंकी परम्परासे ज्ञान प्रास हुआ था| आचार्य गुणधर सूत्ररचनाशैलीके प्रकाण्ड विद्वान् हैं । धवला टीकामें आचार्य वीरसेनने उन्हें वाचक कहा है और वाचकका अर्थ पूर्वविद लिया है। अतएव इनकी रचना-प्रतिभा मंजुल अर्थको संक्षेपमें प्रस्तुत करनेकी थी। वस्तुतः आचार्य गुणधर 'कम्मपडिपाहुड' के ज्ञाता होनेके साथ ही अत्यन्त प्रतिभाशाली और विषविशेषज विद्वान थे। इनके कसायपाहुडकी प्रत्येक गाथाके एक-एक पदको लेकर एक-एक अधिकारका रचा जाना तथा तीन गाथाओंका पाँच अधिकारोंमें निबद्ध होना ही इनकी प्रतिभाकी गंभीरता और अनन्त अर्थगर्भित अभीव्यक्तीको सूचित करता है। वेदक अधिकारकी जो ज सकामेदिय' (गाथाङ्क ६२) गाथाके द्वारा चारों प्रकारके बन्ध, चारों प्रकारके संक्रमण, चारों प्रकारके उदय, चारों प्रकारकी उदीरणा और चारों प्रकारके सत्वसम्बन्धी अल्पबहुत्वकी सूचना निश्चयतः उसके गाम्भीर्य और अनन्तार्थभित्वकी साक्षी है। अर्थबहुलताकी दृष्टि से गुणधरकी शैली अत्यन्त गंभीर है। गुणधरके इस ग्रंथपर यदि चूर्णिसूत्र न लिखे जाते तो उनका अर्थ पश्चादवर्ती व्यक्ति योंके लिये दुर्बोध हो जाता।
आचार्य शिवशर्मके 'कम्मपयडि' और 'सतक' नामक दो ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। इन दोनों ग्रंथोका उद्गम स्थान 'महाकम्मपडिपाहुड' है। 'कम्म पयडी के साथ जब हम गुणधरके 'कषायपाहुड' की तुलना करते हैं तो हमें इन दोनोंमें मौलिक अन्तर प्रतीत होता है। कम्मापयडिमें महाकम्मपडिपाहुडके चौबीस अनुयोगद्वारोंका समावेश नहीं है। किन्तु बन्धन, उदय और संक्रमणादि कुछ अनुयोगद्वार ही प्राप्त हैं। गुणधरने अपने 'कषायपाहुड' में समस्त 'पेज्जदोषपाहुड' का उपसंहार किया है। अतः यह स्पष्ट है कि 'कम्मपयडि की रचना शिवशर्मने गुणधरके पश्चात् ही की है। 'कम्मपयडि' और 'सतक’ इन दोनों ग्रंथोके अन्त में अपनी अल्पज्ञना प्रकट करते हुए शिवशर्मने दृष्टिवादके ज्ञाता आचार्यों से उसे शुद्ध कर लेनेकी प्रार्थना की है। वस्तुत: 'कम्मपयडि' एक संग्रह ग्रंथ है क्योंकि उसमें विभिन्न स्थानोंपर आई हुई प्राचीन गाथाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। कम्मपयडिकी चूणिमें उसके कर्ताने उसे 'कम्पयडिसंग्रहिणी' नाम दिया है। इसी प्रकार 'सतक' चुर्णीमें भी उसे संग्रह-ग्रन्थ कहा है। गुणधरकी यह रचना मौलिक है तथा कर्म-शिद्धान्तको बीजरूप में प्रस्तुत करती है।
कषायपाहुड कम्मपडिसे पूर्ववर्ती है। कम्मपर्याडके संक्रमकरणमें कषाय पाहुड़के संक्रमअर्थाअधिकारको १३ गाथाएँ साधारण पाठभेदके साथ अनुक्रमसे ज्यों-की-त्यों उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार कम्मपयडिके उपशमकरणमें कषाय पाहुडके दर्शनमोहोपशमना अर्थाधिकारकी चार गाथाएँ कुछ पाठभेदके साथ पायी जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य गुणधर केवली और श्रुतकेवलियोंके अनन्सर पहले पूर्वविद हैं, जिन्होंने 'महाकम्मपयडिपाहुड' का संक्षेपमें उपसंहार किया। महान् अर्थको अल्पाक्षरोंमें निबद्ध करनेकी प्रतिभा उनमें विद्यमान थी। यही कारण है कि कसायपाहुडका उत्तरकालीन सभी वाङ्मयपर प्रभाव है।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------श्रुतधराचार्यसे अभिप्राय हमारा उन आचार्यों से है, जिन्होंने सिद्धान्त, साहित्य, कमराहिम, बायाससाहित्यका साथ दिगम्बर आचार्यों के चारित्र और गुणोंका जोबन में निर्वाह करते हुए किया है। यों तो प्रथमानुयोग, करणा नुयोग, चरणानुयोग और ध्यानुयोगका पूर्व परम्पराके भाधारपर प्रन्धरूपमें प्रणयन करनेका कार्य सभी आचार्य करते रहे हैं, पर केवली और श्रुत केवलियोंकी परम्पराको प्राप्त कर जो अंग या पूर्वो के एकदेशशाता आचार्य हुए हैं उनका इतिवृत्त श्रुतधर आचार्यों को परम्पराके अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायगा | अतएव इन आचार्यों में गुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवाल, यति वृषम, उच्चारणाचार्य, आयमंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, गृपिच्छाचार्य और बप्पदेवकी गणना की जा सकती है ।
श्रुतघराचार्य युगसंस्थापक और युगान्तरकारी आचार्य है। इन्होंने प्रतिभाके कोण होनेपर नष्ट होतो हुई श्रुतपरम्पराको मूर्त रूप देनेका कार्य किया है। यदि श्रतधर आचार्य इस प्रकारका प्रयास नहीं करते तो आज जो जिनवाणी अवशिष्ट है, वह दिखलायी नहीं पड़ती। श्रुतधराचार्य दिगम्बर आचार्यों के मूलगुण और उत्तरगुणों से युक्त थे और परम्पराको जीवित रखनेको दृष्टिसे वे ग्रन्थ-प्रणयनमें संलग्न रहते थे 1 श्रुतकी यह परम्परा अर्थश्रुत और द्रव्यश्रुतके रूपमें ई. सन् पूर्वकी शताब्दियोंसे आरम्भ होकर ई० सनकी चतुर्थ पंचम शताब्दी तक चलती रही है ।अतएव श्रुतघर परम्परामें कर्मसिद्धान्त, लोका. नुयोग एवं सूत्र रूपमें ऐसा निबद साहित्य, जिसपर उत्तरकालमें टीकाएँ, विव त्तियाँ एवं भाष्य लिखे गये हैं, का निरूपण समाविष्ट रहेगा।
#Gunadharmaharajji
आचार्य श्री १०८ गुणधर महाराजजी
| Name | Phone/Mobile 1 | Which Sangh/Maharaji/Aryika Ji you are associated with |
|---|---|---|
| Sangh Common Number | +919844033717 | #VardhamanSagarJiMaharaj1950DharmSagarJi |
| Hemal Jain | +918690943133 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi |
| Abhi Bantu | +919575455473 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi |
| Purnima Didi | +918552998307 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi |
| Varna Manish Bhai | +919352199164 | #KanaknandiJiMaharajKunthusagarji |
| Ankit Test | +919730016352 | #AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj |
| Santosh Khule | +919850774639 | #PavitrasagarJiMaharaj1949SanmatiSagarJi1927 |
| Madhok Shaha | +919928058345 | #KanaknandiJiMaharajKunthusagarji |
| Siddharth jain Baddu | +917987281995 | #AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj, #VishalSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi |
| Akshay Adadande | +919765069127 | #AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj, #NiyamSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi |
| Mayur Jain | +918484845108 | #SundarSagarJiMaharaj1976SanmatiSagarJi, #VibhavSagarJiMaharaj1976ViragSagarJi, #PrabhavsagarjiPavitrasagarJiMaharaj1949, #MayanksagarjiRayansagarJiMaharaj1955 |
शशांक शहा
Shashank Shaha
| Title | _hashtag | Year | Chaturmas Status | State | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Muni Shri 108 Sajagsagarji Maharaj | #SajagsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Muni Shri 108 Vibodh Sagarji Maharaj | #VibodhsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Morena |
| Muni Shri 108 Mahat Sagarji Maharaj | #MahatsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Muni Shri 108 Vibhor Sagarji Maharaj | #VibhorsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Muni Shri 108 Sanandsagarji Maharaj | #SanandsagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Aryika Shri 105 Sukhadshri Mataji | #SukhadshrijiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Kshullak Shri 105 Shantigupt Ji Maharaj | #ShantiguptjiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Kshullika Shri 105 Dhanyashri Mataji | #DhanyashrijiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Kshullika Shri 105 Thirthshri Mataji | #ThirthshrijiGuptiNandiJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Acharya Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj | #KunthuSagarJiMaharajAcharyaShriMahavirKirtiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Acharya Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1941 | #SambhavSagarJiMaharaj1941MahavirkirtiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Pulak Sagar Ji Maharaj 1970 | #PulakSagarJiMaharaj1970PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Acharya Shri 108 Saurabh Sagarji Maharaj 1970 | #SaurabhSagarjiMaharaj1970PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttarakhand | Dehradun |
| Acharya Shri 108 Pramukh Sagarji Maharaj-1973 | #PramukhSagarJiMaharaji1973PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Muni Shri 108 Arunsagarji Maharaj-1963 | #ArunsagarJi-1963PuspdantSagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Devband |
| Muni Shri 108 Pragalbh Sagarji Maharaj 1960 | #PragalbhSagarJiMaharaj1960PuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prasang Sagarji Maharaj-1982 | #PrasangSagarJiMaharaj1982PushpadantaSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Hassan |
| Muni Shri 108 Pranam Sagarji Maharaj-1972 | #MuniShriPranamSagarjiMaharaj1972PushpadantaSagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Praneet Sagar Ji Maharaj | #PraneetSagarJiMaharajPuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullak Shri 105 Parv Sagarji Maharaj | #ParvSagarJiMaharajPuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Devas |
| Kshullika Shri 105 Prashantshri Mataji | #PrashantshriMataJiPuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Devas |
| Acharya Shri 108 Siddhant Sagar Ji Maharaj 1966 | #SiddhantSagarJiMaharaj1966SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Acharya Shri 108 Saubhagya Sagar Ji Maharaj 1965 | #SaubhagyaSagarJiMaharaj1965SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Muni Shri 108 Navinandiji Sagar Ji Maharaj 1977 | #NavinandijiSagarJiMaharaj1977SiddhantSagarJi | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Muni Shri 108 Suveer Sagarji Maharaj-1986 | #SuveerSagarJiMaharaj1986SanmatiSagarJi | 2025 | Maharashtra | Amravati | |
| Acharya Shri 108 Subal Sagarji Maharaj 1976 | #SubalSagarJiMaharaj1976AcharyaSriSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Shrestha Sagar Ji Maharaj 1961 | #ShresthaSagarJiMaharaj1961SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Sukumal Sagarji Maharaj | #sukumalsagarjiSanmatisagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Shubhamsagar Ji Maharaj | #shubhamsagarjiSanmatisagarji | 2025 | Rajasthan | Dungarpur | |
| Aryika Shri 105 Samaymati Mataji | #SamaymatijiSanmatiSagarJi1938 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sadaymati Mataji | #SadaymatijiSanmatiSagarJi1938 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Shreyshree Mataji | #ShreyshreejiSanmatiSagarJi1938 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Shubhamati Mataji-1975 | #Shubhamatiji1975SanmatiSagarJi1938 | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Acharya Shri 108 Vivek Sagarji Maharaj-1972 | #VivekSagarJiMaharaj1972SumatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vairagya Sagar Ji Maharaj 1963 | #VairagyaSagarJiMaharaj1963SumatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Sukhadmati Mata Ji 1944 | #SukhadmatiMataJi1944SuvidhiSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Acharya Shri 108 Ativeer Ji Maharaj 1965 | #AtiveerJiMaharaj1965VidyabhushanSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Acharya Shri 108 Gulab Bhushanji Maharaj-1955 | #GulabBhushanjiMaharaj1955VidyabhushanAcharyaSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Mudbadri |
| Elacharya Shri 108 Trilokbhusanji Maharaj (Lalitpur) | #ElacharyaShriTrilokbhusanJiMaharajLalitpurVidyabhusanSanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Badagaon |
| Muni Shri 108 Prabhavnabhushanji Maharaj | #PrabhavnabhushanJiVidyabhushanJiMaharaj1975 | 2025 | Delhi | Delhi | |
| Ganini Aryika Shri 105 Shrushtibhushanmati Mataji | #ShrushtibhushanmatijiVidyabhushanSanmatiSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Acharya Shri 108 Pushpadant Sagar Ji Maharaj 1954 | #PushpadantSagarJiMaharaj1954VimalSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Devas |
| Acharya Shri 108 Niranjan Sagar Ji Maharaj | #NiranjanSagarJiMaharajVimalSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Viharsh Sagar Ji Maharaj 1970 | #ViharshSagarJiMaharaj1970ViragsagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Acharya Shri 108 Vimarsh Sagarji-Maharaj-1973 | #VimarshSagarJi1973ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Acharya Shri 108 Vibhav Sagarji Maharaj 1976 | #VibhavSagarJiMaharaj1976ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Acharya Shri 108 Vishad Sagarji Maharaj-1964 | #VishadSagarJiMaharaj1964ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Acharya Shri 108 Pragya Sagarji Maharaj-1978 | #PragyasagarJiMaharaj1978ViragSagarJi | 2025 | Rajasthan | Kota | |
| Acharya Shri 108 Pragysagarji Maharaj 1978 | #PragysagarJiMaharaj1978ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Vijyesh Sagar Ji Maharaj 1978 | #VijyeshSagarJiMaharaj1978ViragSagarJi(Anklikar) | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Muni Shri 108 Vibhaswar Sagar Ji Maharaj 1979 | #VibhaswarSagarJiMaharaj1979ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vidambarsagarji Maharaj-1982 | #MuniShriVidambarsagarJiMaharaj1982ViragSagarJi | 2025 | Maharashtra | Nashik | |
| Muni Shri 108 Visheshsagarji Maharaj-1975 | #MuniShriVisheshsagarJiMaharaj1975ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Satara |
| Muni Shri 108 Vishwamitrasagarji Maharaj (Viragsagarji) | #MuniShriVishwamitrasagarJiMaharajViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vishwasamya Sagarji Maharaj | #VishwasamyasagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhind |
| Muni Shri 108 Viniyog Sagarji Maharaj | #ViniyogsagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalgaon |
| Muni Shri 108 Nirveg Sagarji Maharaj | #NirvegsagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Khandwa |
| Muni Shri 108 Vishwasurya Sagarji Maharaj | #VishwasuryaViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sanavat |
| Aryika Shri 105 Vindhyashri Mataji-1973 | #VindhyashriMaataJi1973ViragSagarjiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Aryika Shri 105 Vishistmati Mata Ji 1979 | #VishistmatiMataJi1979ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vijetashree Mata Ji 1978 | #VijetashreeMataJi1978ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Aryika Shri 105 Vinatshree Mata Ji 1979 | #VinatshreeMataJi1979ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vikaamyashree Mata Ji 1982 | #VikaamyashreeMataJi1982ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Viprabhashree Mata Ji 1982 | #ViprabhashreeMataJi1982ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Viyojnashree Mataji-1979 | #ViyojnashreeMataJi1979ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Viditshree Mata Ji 1986 | #ViditshreeMataJi1986ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vibhaktshree Mataji-1947 | #VibhaktshreeMataJiViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vishisthshree Mataji | #VishisthshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vijitshree Mataji | #VijitshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Aryika Shri 105 Vigunjanshree Mataji | #VigunjanshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Vijigyasamati Mataji | #VijigyasamatijiViragSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Ailak Shri Viniyogsagarji Maharaj | #ViniyogsagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Madhya Pradesh | Ujjain | |
| Kshullak Shri 105 Videh Sagarji Maharaj (Viragsagarji) | #VidehSagarjiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Kshullika Shri 105 Vipadmashree Mataji | #VipadmashreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Kshullika Shri 105 Vichintanshree Mataji | #VichintanshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullika Shri 105 Visudhrudhshree Mataji | #VisudhrudhshreeViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Kshullika Shri 105 Vipathshree Mataji | #VipathshreejiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgarh |
| Acharya Shri 108 Vibhakt Sagar Ji Maharaj 1969 | #VibhaktSagarJiMaharaj1969VishadSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Bhaktibhartishri Mataji | #BhaktibhartishrijiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Vatsalyabhartishri Mataji | #VatsalyabhartishrijiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Acharya Shri 108 Vipranat Sagar Ji Maharaj 1984 | #VipranatSagarJiMaharaj1984VivekSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Gambhirmati Mataji | #Gambhirmatijisuparshwamatimataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Acharya Shri 108 Tanmay Sagar Ji Maharaj1970 | #TanmaySagarJiMaharaj1970AbhinandanSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Aditya Sagarji Maharaj-1970 | #Adityasagarji1970Abhinandansagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Gurugram |
| Aryika Shri 105 Prasannmati Mata ji 1973 | #PrasannmatiMataji1973AbhinandanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Ajitmati Mataji-(AbhinandanSagarji) | #AjitmatijiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Aryika Shri 105 Abhedmati Mataji | #AbhedmatijiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Aryika Shri 105 Chaityamati Mataji -1967 (AbhinandanSagarji) | #Chaityamatiji1967AbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Suharshmati Mataji | #SuharshmatijiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullak Shri 105 Arham Sagarji Maharaj | #ArhamsagarjiAbhinandanSagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Acharya Shri 108 Adhyatmanandi Ji Maharaj | #AdhyatmanandijiKanaknandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Kshullak Shri 105 Siddha Sagarji Maharaj (Adityasagarji) | #SiddhasagarjiAdityasagarji1970 | 2025 | Confirmed | Haryana | Gurugram |
| Muni Shri 108 Punyasagarji Maharaj-1965 | #Punyasagarji1965AjitSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Saurabhmati Mataji-1958 | #SaurabhmatiAjitsagarJiMaharaj1926 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Gyanbhushanji Maharaj | #GyanbhushanjiArhadbaliji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Balacharya Shri 108 Siddhesen Ji Maharaj 1943 | #SiddhesenJiMaharaj1943BahubaliJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Raibaug |
| Ganini Aryika Shri 105 Jindevi Mataji 1960 | #GaniniJindeviMataji1960BahubaliJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Khsullika Shri 105 Mangalmati Mataji | #MangalmatijiBahubaliJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Aryika Shri 105 Subhadramati Mataji | #SubhadramatijiBahubaliJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Girnar Sagarji Maharaj (Balyogi Rashtrashant) | #BalyogiRashtrashantGirnarSagarJiMaharajBharatSagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Uddharmati Mataji | #UddharmatijiBharatSagarji1950 | 2025 | Confirmed | xy | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Nandishwarmati Mataji | #NandishwarmatijiBharatSagarji1950 | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Aryika Shri 105 Suprakashmati Mata ji 1965 | #SuprakashmatiMatajiDayaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Acharya Shri 108 Devnandiji Maharaj | #DevNandiJiMaharajKunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Amarkirtiji Maharaj 1974 | #AmarKirtiJiMaharaj1974DevnandiJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Mumbai |
| Muni Shri 108 Amoghkirtiji Maharaj 1980 | #AmoghKirtiJiMaharaj1980DevnandiJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Mumbai |
| Muni Shri 108 Siddhakirtiji Maharaj 1940 | #SiddhakirtijiMaharaj1940Devanandiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Shantikirtiji Maharaj | #ShantikirtijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Darshanshri Mataji | #DarshanshriDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Sanyogshri Mataji | #SanyogshrijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Sushilshri Mataji | #SushilshriDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Supadmamati Mataji | #SupadmamatiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Charitrashri Mataji | #CharitrashriDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Suyogshri Mataji | #SuyogshrijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Amit Sagar Ji Maharaj 1963 | #AmitSagarJiMaharaj1963DharmasagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Shubhmati Mataji 1948 | #ShubhmatiMataji1948DharmSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Suratnamati Mataji (Dharmsagarji) | #SuratnamatijiDharmsagarJiMaharaj1942 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Dnyesagarji Maharaj | #DnyesagarjiGyanSagarJiMaharaj1957 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Namit Sagarji Maharaj | #NamitsagarjiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Nutanmati Mataji | #NutanmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Nitimati Mataji | #NitimatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Navmati Mataji | #NavmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Aryika Shri 105 Nayanmati Mataji | #NayanmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Namrmati Mataji | #NamrmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Kshullika Shri 105 Naychakramati Mataji | #NaychakramatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Kshullika Shri 105 Namanmati Mataji | #NamanmatijiGundharNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Kshullika Shri 105 Gyanmoti Mataji | #GyanmotijiGyanBhushanJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Aarshmati Mataji | #AarshmatiMatajiGyanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Acharya Shri 108 Gyatsagarji Maharaj | #GyatsagarjiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Sacchidanand Sagar Ji Maharaj 1973 | #SacchidanandSagarJiMaharaj1973KanaknandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Suvatsalyamati Mataji | #SuvatsalyamatijiKanaknandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Kshullika Shri 105 Bhaktishri Mataji | #BhaktishrijiKanaknandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Acharya Shri 108 Karmvijay Nandiji Maharaj 1958 | #KarmvijayNandijiMaharaj1958KunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Chetanmati Mataji | #ChetanmatiKumudnandiJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Chetannandiji Maharaj | #ChetannandijiKumudnandiJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Shrutsagarji Maharaj 1969 | #ShrutsagarjiMuniraj1969KunthusagarjiMuniraj | 2025 | Confirmed | New Delhi | Green Park |
| Aacharya Shri 108 Kumudnandi Ji Maharaj 1963 | #KumudnandiJiMaharaj1963Kunthusagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Kanaknandiji Maharaj | #KanaknandiJiMaharajKunthusagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Acharya Shri 108 Padmanandiji Maharaj-1955 | #PadmanandijiMaharaj1955GandharacharyaShreeKunthusagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Acharya Shri 108 Vidyanandi Sagar Ji Maharaj 1963 | #VidyanandiSagarJiMaharaj1963KunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Belgaon |
| Acharya Shri 108 Gundhar Nandiji Maharaj | #GundharNandiJiMaharajKunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Varoor |
| Niryapakacharya Shri 108 Gunbhadra Nandiji Maharaj-1969 | #GunbhadraNandiMaharaj1969KunthuSagarji | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Muni Shri 108 Dhairyanandi ji Maharaj | #DhairyanandijiMaharajKunthusagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shramannandiji Maharaj | #ShramannandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Pavitramati Mata Ji 1951 | #PavitramatiMataJi1951KunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Aasthashree Mataji-1975 | #AasthashreeMataJi1975KunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Aryika Shri 105 Pawanshree Mata Ji | #PawanshreeMataJiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Sumatishri Mataji | #SumatishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Siddhishri Mataji | #SiddhishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Riddhishri Mataji | #RiddhishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Gunshri Mataji | #GunshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Kshamashri Mataji | #KshamashriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Aryika Shri 105 Kusumshri Mataji | #KusumshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Kirtishri Mataji | #KirtishriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Maharashtra | Nashik | |
| Aryika Shri 105 Kshemshri Mataji | #KshemshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Guruwani Mataji | #GuruwaniKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Aryika Shri 105 Kundshri Mataji | #KundshriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullak Shri 105 Suvidhannandiji Maharaj | #SuvidhannandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullak Shri 105 Suvidya Nandiji Maharaj | #SuvidyanandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullak Shri 105 Shitalnandiji Maharaj | #ShitalnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullak Shri 105 Vardhamannandiji Maharaj | #VardhamannandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullika Shri 105 Sumaitri Mataji | #SumaitriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Kavyashri Mataji | #KavyashriiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Kshullika Shri 105 Chandrashri Mataji | #ChandrashriKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Kshullika Shri 105 Chaitanyamati Mataji (Kunthusagarji) | #ChaitanyamatijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Mangal Sagarji Maharaj-2003 | #MangalSagarji2003Mayanksagarji | 2025 | Madhya Pradesh | Shivpuri | |
| Acharya Shri 108 Nirbhay Sagarji Maharaj 1963 | #NirbhaySagarJiMaharaj1963AbhinandanSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Hemdatta Sagarji Maharaj | #HemdattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Sudatta Sagarji Maharaj | #SudattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Shivdatta Sagarji Maharaj | #ShivdattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Gurudatta Sagarji Maharaj | #GurudattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Muni Shri 108 Bhudatta Sagarji Maharaj | #BhudattaSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Ailak Shri 105 Meghdatta Sagarji Maharaj | #MeghdattaSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Kshullak Shri 105 Chandradatta Sagarji Maharaj | #ChandradattasagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| Kshullak Shri 105 Naigam Sagarji Maharaj (Nirbhaysagarji) | #NaigamSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Kshullak Shri 105 Dharmadatta Sagarji Maharaj | #DharmadattaSagarjiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Haryana | Gurugram |
| Kshullika Shri 105 Vimohmati Mataji | #VimohmatijiNirbhaySagarJiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Vairagyanandiji Maharaj-1974 | #Vairagyanandiji1974PadamNandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Tatvarthnandiji Maharaj | #TatvarthnandijiMaharaj1960Padmanandiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Muni Shri 108 Tatparyanandiji Maharaj | #TatparyanandijiMaharaj1960Padmanandiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Divyshreemati Mataji-1977 | #DivyshreematiMataJi1977PadmnandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vaartikshree Mata Ji 1983 | #VaartikshreeMataJi1983PadmnandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Vyaakhyashree Mata Ji 1979 | #VyaakhyashreeMataJi1979PadmnandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Vijayshree Mataji | #VijayshreejiPadmanandijiMaharaj1955 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Aryika Shri 105 Dhairyashree Mataji | #DhairyashreejiPadmanandijiMaharaj1955 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Kshullika Shri 105 Kundanshri Mataji | #KundanshrijiPadmanandijiMaharaj1955 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Phaltan |
| Ganini Aryika Shri 105 Shreyanshmati Mataji | #ShreyanshmatijiParshvSagarJi1915 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Prabal Sagarji Maharaj 1971 | #PrabalSagarJiMaharaj1971PuspdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Bharuch |
| Muni Shri 108 Sahajsagarji Maharaj (Prasannasagarji) | #SahajsagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Muni Shri 108 Navpadmasagarji Maharaj | #NavpadmasagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aryika Shri 105 Gyanprabha Mataji | #GyanprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aryika Shri 105 Charitraprabha Mataji | #CharitraprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aryika Shri 105 Punyaprabha Mataji | #PunyaprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullak Shri 105 Naigamsagarji Maharaj (Prasannasagarji) | #NaigamsagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullak Shri 105 Arghsagarji Maharaj | #ArghsagarjijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Darshanprabha Mataji | #DarshanprabhajiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Tapaprabha Mataji | #TapaprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Vachanprabha Mataji | #VachanprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Vratprabha Mataji | #VratprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Kshullika Shri 105 Dharmprabha Mataji | #DharmprabhamatijiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Acharya Shri 108 Prasannrishiji Maharaj | #PrasannrishijiKusagraNandiJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Prabhatchandraji Maharaj | #PrabhatchandrajiPrasannrishiJiMaharaj1981 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Punyamati Mata Ji | #PunyamatiMataJiPrasannrishiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Pujyamati Mataji-1962 | #PujyamatiMataJi1962PrasannrishiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Pulkit Sagar Ji Maharaj(Bhilwara) | #PulkitsagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Pramudit Sagar Ji Maharaj(Jabalpur) | #PramuditSagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Purvang Sagarji Maharaj | #PurvangsagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Ailak Shri 105 Prashmit Sagarji Maharaj | #PrashmitsagarjiPulaksagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Mohotsav Sagar Ji Maharaj | #mohotsavsagarjimaharajPunyasagarjimaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Muditsagarji Maharaj | #MuditsagarjiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Utsavsagarji Maharaj | #UtsavsagarjiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Harshitmati Mataji | #HarshitmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Pramodmati Mataji-1960 | #PramodmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Parvmati Mataji | #ParvmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Nishchaymati Mataji | #NishchaymatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Nirnaymati Mataji | #NirnaymatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Kshullak Shri 105 Purna Sagarji Maharaj | #PurnasagarjiPunyasagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Balacharya Shri 108 Moksh Sagarji Maharaj-1962 | #BalacharyaShriMokshSagarJiMaharaj1962SambhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Puneet Chaitanya mati Mata ji 1958 | #PuneetChaitanyaMatajiSambhavSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Pavitrasagar Ji Maharaj 1949 | #PavitrasagarJiMaharaj1949SanmatiSagarJi1927 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Niryapak Shraman Muni Shri 108 Dharmsagar Ji Maharaj 1942 | #DharmsagarJiMaharaj1942SanmatiSagarJi1927 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Vidya Sagar Ji Maharaj 1990 | #VidyaSagarJiMaharaj1990SanmatiSagarji(Dakshinwale) | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Siddhantsagar Ji Maharaj 1950 | #SiddhantsagarJiMaharaj1950VardhmansagarJi1951 | 2025 | Madhya Pradesh | Indore | |
| Muni Shri 108 Sulabh Sagarji Maharaj (Saubhagyasagarji) | #SulabhsagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Saubhagyamati Mataji | #SaubhagyamatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullak Shri 105 Shubhlabhsagarji Maharaj | #ShubhlabhsagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullak Shri 105 Shubhkamanasagarji Maharaj | #ShubhkamanasagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullika Shri 105 Shubhmargmati Mataji | #ShubhmargmatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullika Shri 105 Shubhashishmati Mataji | #ShubhashishmatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Kshullika Shri 105 Suaryashri Mataji | #SuaryashrijiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Kshullika Shri 105 Sumargshri Mataji | #SumargshrijiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Kshullika Shri 105 Ashresthmati Mataji | #AshresthmatijiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Itawa |
| Acharya Shri 108 Saubhagya Sagarji Maharaj | #SaubhagyasagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Balacharya Shri 108 Suratna Sagar Ji Maharaj-1986 | #BalacharyaShriSuratnJiMaharaj1986SaubhagyaSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Ganini Aryika Shri 105 Shubhmati Mataji | #ShubhmatijiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Acharya Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 1961 | #SamtaSagarJiMaharaj1961 | 2025 | Rajasthan | Itiwar | |
| Kshullak Shri 105 Suprabhatsagarji Maharaj | #SuprabhatsagarjiShashankSagarjiMaharaj1983 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Sabarkantha |
| Muni Shri 108 Anuman Sagarji Maharaj | #AnumanSagarjiShrutsagarjiMuniraj1969 | 2025 | Uttar Pradesh | Kapilji | |
| Kshullak Shri 105 Aviral Sagarji Maharaj | #Aviral SagarjiShrutsagarjiMuniraj1969 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Shashank Sagarji Maharaj-1983 | #ShashankSagarjiMaharaj1983SiddhantSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Sahajsagar Ji Maharaj 1965 | #SahajsagarJiMaharaj1965SiddhantSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Ganini Aryika Shri 105 Saubhagyamati Mata Ji | #SaubhagyamatiJiSiddhantSagarJiMaharaj1966 | 2025 | Confirmed | Telangana | Hyderabad |
| Gadni Aryika Shri 105 Sangam mati Mata Ji | #SangamMatiMatajiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Ganini Aryika Shri 105 Samatamati Mataji | #SamatamatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Suryamati Mataji | #SuryamatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Siddhantmati Mataji-1951 | #Siddhantmatiji1951SiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Sanskarmati Mataji | #SanskarmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Samarthmati Mataji | #SamarthmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Sakshammati Mataji | #SakshammatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullak Shri 105 Shrutsagarji Maharaj (Siddhantsagarji) | #ShrutsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Sauhardsagarji Maharaj | #SauhardsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Savindrasagarji Maharaj | #SavindrasagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullak Shri 105 Shrifalsagarji Maharaj | #ShrifalsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullak Shri 105 Naigamsagarji Maharaj (Siddhantsagarji) | #NaigamsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Kshullika Shri 105 Suyashmati Mataji | #SuyashmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullika Shri 105 Sunandamati Mataji | #SunandamatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Kshullika Shri 105 Sukaushalmati Mataji | #SukaushalmatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Savindramati Mataji | #SavindramatiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Aryika Shri 105 Sunandamati Mataji-1954 | #SunandamatijiSubaahuSagarJiMaharaj1924 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Subodhmati Mataji-(Subahusagarji) | #SubodhmatijiSubaahuSagarJiMaharaj1924 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Acharya Shri 108 Sundar Sagar Ji Maharaj 1976 | #SundarSagarJiMaharaj1976SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Sukaavyamati Mata ji | #SukaavyamatiMatajiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullak Shri 105 Supunya Sagarji Maharaj | #SupunyaSagarjiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sudarshmati Mataji | #SudarshmatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sudharmmati Mataji (Sundarsagarji) | #SudharmmatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sudhanyamati Mataji | #SudhanyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Subhavyamati Mataji | #SubhavyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sutathyamati Mataji | #SutathyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sunamramati Mataji (Sundarsagarji) | #SunamramatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Supathyamati Mataji | #SupathyamatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Kshullika Shri 105 Sankalpmati Mataji | #SankalpmatijiSundarSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Sushrut Sagar Ji Maharaj 1943 | #SushrutSagarJiMaharaj1943SunilSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuwa |
| Muni Shri 108 Sampujya Sagar Ji Maharaj | #SampujyaSagarJiMaharajSunilSagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Samvigya Sagar Ji Maharaj | #SamvigyaSagarJiMaharajSunilSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuaa |
| Muni Shri 108 Sampragya Sagar Ji Maharaj 2000 | #SampragyaSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Shrutesh Sagarji Maharaj-1983 | #Shruteshsagarji1983Sunilsagarji1977 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuaa |
| Muni Shri 108 Sushrutasagar Ji Maharaj-1992 | #sushrutasagarjiSunilsagarji | 2025 | Madhya Pradesh | Bakshuaa | |
| Muni Shri 108 Sampragyasagar Ji Maharaj-2000 | #sampragyasagarSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Siddharth Sagarji Maharaj | #SiddharthsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Shubham Sagarji Maharaj | #ShubhamsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Dungarpur |
| Muni Shri 108 Suvivek Sagarji Maharaj | #SuviveksagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Suvishuddh Sagarji Maharaj | #SuvishuddhsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sampurnamati Mata ji | #SampurnamatiMatajiSunilSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sampannmati Mata ji 1992 | #SampannmatiMataji1992SunilSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sambalmati Mataji-1995 | #sambalmatiSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sampoornamati Mataji-1990 | #sampoornamatiSunilsagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Supragyamati Mataji-1992 | #supragyamati1992Sunilsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Khairwada |
| Aryika Shri 105 Aakashmati Mataji-1957 | #aakashmati1957Sunilsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Adeymati Mataji | #AdeymatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Arshmati Mataji | #ArshmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Anarghmati Mataji | #AnarghmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Khairwada |
| Aryika Shri 105 Suvigyamati Mataji | #SuvigyamatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Sanyyatmati Mataji | #SanyyatmatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Anuprekshamati Mataji | #AnuprekshamatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sutramati Mataji | #SutramatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Sukhadsagarji Maharaj | #SukhadsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Samvruddhasagarji Maharaj | #SamvruddhasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Sampragyasagarji Maharaj | #SampragyasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Santoshsagarji Maharaj | #SantoshsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Santushtsagarji Maharaj | #SantushtsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Vijayantsagarji Maharaj | #VijayantsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Sunishchit Sagarji Maharaj | #SunishchitsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Suprakash Sagarji Maharaj | #SuprakashSagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bakshuaa |
| Kshullak Shri 105 Sankalp Sagarji Maharaj | #SankalpSagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Surajmati Mataji | #SurajmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Suvratmati Mataji | #SuvratmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sugandhmati Mataji | #SugandhmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sambhavmati Mataji | #SambhavmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Samarakshmati Mataji | #SamarakshmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sadvratmati Mataji | #SadvratmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sadbodhmati Mataji | #SadbodhmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Satatmati Mataji | #SatatmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Amohmati Mataji | #AmohmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Atalmati Mataji | #AtalmatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Shuddhatmamati Mataji | #ShuddhatmamatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Ajaymati Mataji | #AjaymatiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Padmamati Mataji | #PadmamatiMatajiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Saddrushtmati Mataji | #SaddrushtmatiMatajiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullika Shri 105 Sukrutmati Mataji | #SukrutmatijiMatajiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Acharya Shri 108 Sunil Sagarji Maharaj-1977 | #SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Sulekhmati Mataji | #SulekhmatijiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Aryika Shri 105 Chintanshree Mata Ji 1981 | #ChintanshreeMataJi1981VairagyanandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sugyanshree Mata Ji 1969 | #SugyanshreeMataJi1969VairagyanandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sohamshree Mataji | #SohamshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samyakshree Mataji | #SamyakshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Jinshree Mataji | #JinshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Krutikashree Mataji | #KrutikashreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Sanwarnandi Maharaj | #SanwarnandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Saukhyashree Mataji | #SaukhyashreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Sadhyamati Mataji | #SadhyamatijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Sahajshree Mataji | #SahajshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Sarvshree Mataji | #SarvshreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Samatashree Mataji | #SamatashreejiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1950 (Vatsalya Viridhi) | #VardhamansagarjiDharmsagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Hitendra Sagarji Maharaj 1977 | #HitendraSagarJiMaharaj1977VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Darshit Sagarji Maharaj 1955 | #DarshitSagarjiMaharaj1955VardhamanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Chintan Sagarji Maharaj 1986 | #ChintanSagarjiMaharaj1986VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Param Sagar Ji Maharaj | #ParamSagarJiMaharajVardhamanSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Agamsagar Ji Maharaj | #AgamsagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Chinmay Sagarji Maharaj | #ChinmaySagarjiVardhamansagarj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Mahayashmati Mataji 1989 | #MahayashmatiMataji1989VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vatsalmati Mataji 1953 | #VatsalmatiMataji1953VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vilokmati Mataji 1961 | #VilokmatiMataji1961VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Divyanshumati Mataji 1947 | #DivyanshumatiMataji1947VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Purnimamati Mataji 1978 | #PurnimamatiMataji1978VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Muditmati Mataji 1938 | #MuditmatiMataji1938VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vichakshanmati Mataji 1963 | #VichakshanmatiMataji1963VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Nirmuktmati Mataji 1958 | #NirmuktmatiMataji1958VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vinamramati Mataji 1966 | #VinamramatiMataji1966VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Darshanamati Mataji 1962 | #DarshanamatiMataji1962VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Deshnamati Mataji 1959 | #DeshnamatiMataji1959VardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Nirmohmati Mataji-1962 | #NirmohmatijiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Padmayashamati Mataji-1996 | #PadmayashamatijiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Vishwayashmati Mataji-1986 | #VishwayashmatijiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Aryika Shri 105 Divyayashmati Mataji-1996 | #Divyayashmatiji1996VardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Chaityammati Mataji | #ChaityammatijiVardhamansagarji | 2025 | Rajasthan | Tonk | |
| Kshullak Shri 105 Vishalsagarji Maharaj-1959 | #Vishalsagarji1959VardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Nirdosh Sagarji Maharaj-1963 | #NirdoshSagarJiMaharaj1963VardhamanSagarJi(Dakshinwale) | 2025 | Madhya Pradesh | Narsinhpur | |
| Muni Shri 108 Aadisagarji Maharaj | #AadisagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1951 | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Acharya Shri 108 Vasunandiji Maharaj 1967 | #VasunandijiMaharaj1967VidyanandJi | 2025 | Uttar Pradesh | Ahicchatra | |
| Muni Shri 108 Prashmanandji Maharaj-1978 | #PrashmanandJiMaharaj1978VasunandiJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Shivanandji Maharaj-1985 | #ShivanandJiMaharaj1985VasunandiJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Shraddhanandji Maharaj-1987 | #ShraddhanandJiMaharaj1987VasunandiJi | 2025 | Confirmed | Haryana | Sector 16, Faridabad |
| Muni Shri 108 Saiyamanand Ji Maharaj 1959 | #SaiyamanandJiMaharaj1959VasunandiJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Alwar |
| Muni Shri 108 Pavitranand Ji Maharaj 1979 | #PavitranandJiMaharaj1979VasunandiJi | 2025 | Confirmed | Haryana | Sector 16, Faridabad |
| Muni Shri 108 Namisagarji Maharaj (Vasunandiji) | #NamisagarjiVasunandiji | 2025 | Confirmed | Haryana | Rewari |
| Ganini Aryika Shri 105 Gurunandni Mataji-1976 | #GadniGurunandniMataJi1976VasunandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aryika Shri 105 Prabodhnandni Mata Ji 1982 | #PrabodhnandniMataJi1982VasunandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aaryika Shri 105 Prakamyanandani Mata Ji 1995 | #PrakamyanandaniMataJi1995VasunandiJiMaharaj. | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aaryika Shri 105 Prabhanandani Mata Ji 1958 | #PrabhanandaniMataJi1958VasunandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aryika Shri 105 Bramhanandni Mataji-1976 | #BramhanandniMataji1976VasundijiMaharaj | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Aryika Shri 105 Shrinandani Mata Ji 1982 | #ShrinandaniMataJi1982VasundijiMaharaj. | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | |
| Ailak Shri 105 Vigyansagarji Maharaj | #VigyansagarjiVasunandiji | 2025 | Confirmed | Haryana | Rewari |
| Aryika Shri 105 Gyanmati Mataji 1934 | #GyanmatiMataji1934VeersagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Muni Shri 108 Aavashyak Sagarji Maharaj-1952 | #AavashyakSagarJiMaharaj1952VibhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Adhyyan Sagarji Maharaj-1943 | #AdhyyanSagarJiMaharaj1943VibhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Shudhatm Sagar Ji Maharaj 1995 | #ShudhatmSagarJiMaharaj1995VibhavSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Muni Shri 108 Sukh Sagarji Maharaj-1958 (Vibhavsagarji) | #sukhsagarji1958Vibhavsagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Siddhatma Sagar Ji Maharaj | #SiddhatmasagarjiVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Omshree Mata Ji 1993 | #OmshreeMataJi1993VibhavSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Sanskriti Shri Mata ji 1974 | #SanskritiShriMataji1974VibhavSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Adyomshree Mataji-1996 | #AdyomshreeVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Subhavsagarji Maharaj-2007 | #SubhavsagarjiVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Samsagarji Maharaj-1960 | #Samsagarji1960Vibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Sanstutishree Mataji | #SanstutishreeVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Safal Sagarji Maharaj | #SafalsagarjiVibhavsagarji1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aacharya Shri 108 Aarjav Sagar Ji Maharaj 1967 | #AarjavSagarJiMaharaj1967VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seore |
| Acharya Shri 108 Samay Sagar Ji Maharaj 1958 | #SamaySagarJiMaharaj1958VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Niryapak Muni Shri 108 Sudha Sagar Ji Maharaj 1956 | #SudhaSagarJiMaharaj1956VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Niryapak Muni Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 1962 | #SamtaSagarJiMaharaj1962VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Niryapak Muni Shri 108 Veer Sagar ji Maharaj 1973 | #VeerSagarjiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Niryapak Muni Shri 108 Yog Sagar Ji Maharaj 1986 | #YogSagarJiMaharaj1986VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Niryapak Muni Shri 108 Prasad Sagar Ji Maharaj 1984 | #PrasadSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Maihar |
| Niryapak Muni Shri 108 Abhay Sagarji Maharaj-1960 | #AbhaySagarJiMaharaj1960VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Niryapak Muni Shri 108 Sambhav Sagarji Maharaj-1971 | #SambhavSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Niryapak Muni Shri 108 Niyam Sagar Ji Maharaj 1957 | #NiyamSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Akshay Sagarji Maharaj 1962 | #AkshaySagarJiMaharaj1962VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bareilly |
| Muni Shri 108 Praman Sagarji Maharaj 1967 | #PramanSagarjiMaharaj1967VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Pranamya Sagarji Maharaj 1975 | #PranamyaSagarjiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Nirnay Sagarji Maharaj-1969 | #NirnaySagarJiMaharaj1969VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shajapur |
| Muni Shri 108 Uttam Sagar Ji Maharaj 1960 | #UttamSagarJiMaharaj1960VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sangli |
| Muni Shri 108 Shail Sagarji Maharaj-1986 | #ShailSagarJiMaharaj1986VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Banda |
| Muni Shri 108 Sheetalsagarji Maharaj 1976 | #SheetalsagarjiMaharaj1976VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Maihar |
| Muni Shri 108 Shramanasagarji Maharaj 1981 | #ShramanasagarjiMaharaj1981VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj 1977 | #KunthuSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Sandhansagar Ji Maharaj 1976 | #SandhansagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Nirupamsagarji Maharaj 1978 | #NirupamsagarjiMaharaj1978VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Muni Shri 108 Padm Sagar Ji Maharaj 1963 | #PadmSagarJiMaharaj1963VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Katni |
| Muni Shri 108 Nirveg Sagarji Maharaj-1973 | #NirvegSagarJiMaharajVidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Ajit Sagarji Maharaj-1968 | #AjitSagarJiMaharaj1968VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat Nagar |
| Muni Shri 108 Nirakul Sagarji Maharaj-1982 | #NirakulSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dewas |
| Muni Shri 108 Saumyasagarji Maharaj 1978 | #SaumyasagarjiMaharaj1978VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Agra |
| Muni Shri 108 Niramayasagarji Maharaj 1976 | #NiramayasagarjiMaharaj1976VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Nirogsagarji Maharaj-1976 | #NirogsagarjiMaharaj1976VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Virat Sagarji Maharaj-1974 | #ViratSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Vinamra Sagarji Maharaj-1978 | #VinamraSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Muni Shri 108 Maha Sagarji Maharaj-1973 | #MahaSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chindwara |
| Muni Shri 108 Nishkamp Sagar Ji Maharaj 1982 | #NishkampSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Durlabh Sagar Ji Maharaj 1978 | #DurlabhSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Prabodh Sagar Ji Maharaj 1974 | #PrabodhSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Banda |
| Muni Shri 108 Avichal Sagar Ji Maharaj 1981 | #AvichalSagarJiMaharaj1981VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Jhansi |
| Muni Shri 108 Arah Sagar Ji Maharaj 1976 | #ArahSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sanganer |
| Muni Shri 108 Nirapadasagarji Maharaj 1982 | #NirapadasagarjiMaharaj1982VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shivpuri |
| Muni Shri 108 Nirlobh sagarji Maharaj 1970 | #NirlobhsagarjiMaharaj1970VidyasagarJi | 2025 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | |
| Muni Shri 108 Niradoshsagarji Maharaj 1967 | #NiradoshsagarjiMaharaj1967VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Muni Shri 108 Vimal Sagar Ji Maharaj 1975 | #VimalSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Vishal Sagar Ji Maharaj 1977 | #VishalSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Muni Shri 108 Dhaval Sagar Ji Maharaj 1972 | #DhawalSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi | 2025 | Maharashtra | Dharashiv | |
| Muni Shri 108 Nirmad Sagar Ji Maharaj 1984 | #NirmadSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Pindrai |
| Muni Shri 108 Pujya Sagar Ji Maharaj 1970 | #PujyaSagarJiMaharaj1970VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prashast Sagar Ji Maharaj 1975 | #PrashastSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Vishad Sagar Ji Maharaj 1973 | #VishadSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Dharm Sagar Ji Maharaj 1976 | #DharmSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Muni Shri 108 Prayog Sagar Ji Maharaj 1974 | #PrayogSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Prabhaat Sagar Ji Maharaj 1971 | #PrabhaatSagarJiMaharaj1971VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj 1956 | #ChandraSagarJiMaharaj1956VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Nispaksh Sagar Ji Maharaj 1975 | #NispakshSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Muni Shri 108 Niswarth Sagar Ji Maharaj 1973 | #NiswarthSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Muni Shri 108 Nischal Sagar Ji Maharaj 1972 | #NischalSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Agra |
| Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji Maharaj 1973 | #NirmohSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Nishkaam Sagar Ji Maharaj 1980 | #NishkaamSagarJiMaharaj1980VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Neeraj Sagar Ji Maharaj 1986 | #NeerajSagarJiMaharaj1986VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Pindrai |
| Muni Shri 108 Nissang Sagar Ji Maharaj 1981 | #NissangSagarJiMaharaj1981VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Sanskar Sagar Ji Maharaj 1978 | #SanskarSagarJiMaharaj1978VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Nisprah Sagar Ji Maharaj 1976 | #NisprahSagarJiMaharaj1976VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Muni Shri 108 Nirbhik Sagar Ji Maharaj 1977 | #NirbhikSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Muni Shri 108 Nirag Sagar Ji Maharaj 1982 | #NiragSagarJiMaharaj1982VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat Nagar |
| Muni Shri 108 Nisarg Sagar Ji Maharaj 1977 | #NisargSagarJiMaharaj1977VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Muni Shri 108 Omkaar Sagar Ji Maharaj 1982 | #OmkaarSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Pavitra Sagar Ji Maharaj 1961 | #PavitraSagarJiMaharaj1961VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Muni Shri 108 Nirih Sagar Ji Maharaj 1978 | #NirihSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Abhinandan Sagar Ji Maharaj 1975 | #AbhinandanSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Suparshwa Sagar Ji Maharaj 1955 | #SuparshwaSagarJiMaharaj1955VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Atul Sagar Ji Maharaj 1971 | #AtulSagarJiMaharaj1971VidyaSagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Nissim Sagar Ji Maharaj 1983 | #NissimSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Shashvat Sagar Ji Maharaj 1957 | #ShashvatSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Gujarat | Mehasana |
| Muni Shri 108 Malli Sagar Ji Maharaj 1972 | #MalliSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Anand Sagar Ji Maharaj 1978 | #AnandSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Bhaav Sagar Ji Maharaj 1976 | #BhaavSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Muni Shri 108 Vineet Sagar Ji Maharaj 1961 | #VineetSagarJiMaharaj1961VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Chandraprabh Sagar Ji Maharaj 1966 | #ChandraprabhSagarJiMaharaj1966VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Aagam Sagar Ji Maharaj 1976 | #AagamSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Jagdalpur |
| Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1980 | #SehajSagarJiMaharaj1980VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1973 | #SubratSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Saral Sagarji Maharaj 1957 | #SaralSagarjiMaharaj1957VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Muni Shri 108 Puran Sagar Ji Maharaj 1975 | #PuranSagarJiMaharaj1975VidyasagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Bengaluru |
| Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji Maharaj 1989 | #NirgranthSagarJiMaharaj1989VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Nirbhrant Sagar Ji Maharaj 1987 | #NirbhrantSagarJiMaharaj1987VidyaSagarJi | 2025 | Madhya Pradesh | Jabalpur | |
| Muni Shri 108 Niralas Sagar Ji Maharaj 1983 | #NiralasSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Niraashrav Sagar Ji Maharaj 1981 | #NiraashravSagarJiMaharaj1981VidyaSagarJi | 2025 | Madhya Pradesh | Jabalpur | |
| Muni Shri 108 Nirakar Sagar Ji Maharaj 1985 | #NirakarSagarJiMaharaj1985VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Nishchint Sagar Ji Maharaj 1987 | #NishchintSagarJiMaharaj1987VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Badaut |
| Muni Shri 108 Nirmaan Sagar Ji Maharaj 1971 | #NirmaanSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Nishank Sagar Ji Maharaj 1984 | #NishankSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Niranjan Sagar Ji Maharaj 1983 | #NiranjanSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Nirlep Sagar Ji Maharaj 1990 | #NirlepSagarJiMaharaj1990VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Muni Shri 108 Sukh Sagar Ji Maharaj1963 | #SukhSagarJiMaharaj1963VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Prabuddh Sagar Ji Maharaj1971 | #PrabuddhSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shridham |
| Muni Shri 108 Shreyansh Sagar Ji Maharaj 1967 | #ShreyanshSagarJiMaharaj1967VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Bihar | Bhagalpur |
| Muni Shri 108 Anant Sagar Ji Maharaj1971 | #AnantSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Achal Sagar Ji Maharaj1976 | #AchalSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Banda |
| Muni Shri 108 Pawan Sagar Ji Maharaj 1966 | #PawanSagarJiMaharaj1966VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Vrushabh Sagarji Maharaj (Vidyasagarji) | #VrushabhsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Suvrat Sagarji Maharaj-1973 | #Suvratsagarji1973AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj | 2025 | Madhya Pradesh | Bina | |
| Muni Shri 108 Utkrusth Sagarji Maharaj-1940 | #Utkrusthsagarji1940VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Muni Shri 108 Punitsagarji Maharaj | #PunitsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Muni Shri 108 Samadhisagarji Maharaj | #SamadhisagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Purnamati Mataji-1964 | #PurnmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Agaadhmati Mata Ji 1968 | #AgaadhmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Gurumati Mata Ji 1956 | #GurumatiMataJi1956VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Chintanmati Mata Ji 1968 | #ChintanmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sutramati Mata Ji 1968 | #SutramatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Sheelmati Mata Ji 1972 | #SheelmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Saarmati Mata Ji 1971 | #SaarmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sakarmati Mata Ji 1969 | #SakarmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Somyamati Mata Ji 1972 | #SomyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sushantmati Mata Ji 1965 | #SushantmatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Jagratmati Mata Ji 1968 | #JagratmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Kartavyamati Mata Ji 1972 | #KartavyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Nishkaammati Mataji-1978 | #NishkaammatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalna |
| Aryika Shri 105 Viratmati Mataji-1979 | #ViratimatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalna |
| Aryika Shri 105 Tathamati Mata Ji 1976 | #TathamatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Chaityamati Mata Ji 1970 | #ChaityamatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Puneetmati Mata Ji 1972 | #PuneetmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinhpur |
| Aryika Shri 105 Upshammati Mataji-1979 | #UpshammatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Dhruvmati Mata Ji 1965 | #DhruvmatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalna |
| Aryika Shri 105 Paarmati Mata Ji 1978 | #PaarmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aagatmati Mata Ji 1976 | #AagatmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Shrutmati Mata Ji 1978 | #ShrutmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Pavanmati Mataji-1961 | #Pavanmatiji1961VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sadhnamati Mata Ji 1965 | #SadhnamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Vilakshnamati Mata Ji 1963 | #VilakshnamatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aklankmati Mata Ji 1964 | #AklankmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Niklankmati Mata Ji 1969 | #NiklankmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aagammati Mata Ji 1962 | #AagammatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Swadhyaymati Mata Ji 1962 | #SwadhyaymatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Prashammati Mata Ji 1965 | #PrashammatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Muditmati Mata Ji 1964 | #MuditmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sehajmati Mata Ji 1972 | #SehajmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Saiyammati Mata Ji 1967 | #SaiyammatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Siddhamati Mata Ji 1971 | #SiddhamatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samunnatmati Mata Ji 1974 | #SamunnatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Shastramati Mata Ji 1973 | #ShastramatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Tathyamati Mata Ji 1972 | #TathyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vaatsalyamati Mata Ji 1965 | #VaatsalyamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Pathyamati Mata Ji 1972 | #PathyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sanskarmati Mata Ji 1962 | #SanskarmatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vijitmati Mata Ji 1971 | #VijitmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aaptmati Mata Ji 1976 | #AaptmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Dhavalmati Mata Ji 1976 | #DhavalmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samitimati Mata Ji 1975 | #SamitimatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Mananmati Mata Ji 1982 | #MananmatiMataJi1982VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Mrudumati Mata Ji 1959 | #MradumatiMataJi1959VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Nirnaymati Mata Ji 1958 | #NirnaymatiMataJi1958VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Rijumati Mata Ji 1961 | #RijumatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Saralmati Mata Ji 1966 | #SaralmatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Aseemmati Mata Ji 1976 | #AseemmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Gautammati Mata Ji 1977 | #GautammatiMataJi1977VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Nirvaanmati Mata Ji 1978 | #NirvaanmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Maardavmati Mata Ji 1976 | #MaardavmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Mangalmati Mata Ji 1980 | #MangalmatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Chaaritramati Mata Ji 1979 | #ChaaritramatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Shraddhamati Mata Ji 1982 | #ShraddhamatiMataJi1982VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Utkarshmati Mata Ji 1980 | #UtkarshmatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chattarpur |
| Aryika Shri 105 Tapomati Mataji-1958 | #tapomatimatajividyasagarjimaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Siddhantmati Mataji 1969 | #SiddhantmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinhpur |
| Aryika Shri 105 Namrmati Mataji-1968 | #NamrmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Vinamrmati Mataji-1968 | #VinamrmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Atulmati Mataji-1968 | #AtulmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Anugammati Mataji-1970 | #AnugammatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Uchitmati Mataji-1973 | #UchitmatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Vinaymati Mata Ji 1978 | #VinaymatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinhpur |
| Aryika Shri 105 Lakshyamati Mataji-1941 | #LakshyamatiMataJi1941VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Dhyeymati Mataji-1980 | #DhyeymatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aatmmati Mataji-1967 | #AatmmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Saiyatmati Mataji-1974 | #SaiyatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Prashantmati Mata Ji 1961 | #PrashantmatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Vinatmati Mata Ji 1963 | #VinatmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Vishudhmati Mata Ji 1975 | #VishudhmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Aryika Shri 105 Shailmati Mata Ji 1968 | #ShailmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Akampmati Mataji-1966 | #AkampmatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Satana |
| Aryika Shri 105 Amulyamati Mataji-1965 | #AmulyamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aaradhyamati Mataji-1972 | #AaradhyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Achintyamati Mataji-1969 | #AchintyamatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Alolyamati Mataji-1968 | #AlolyamatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Anmolmati Mataji-1970 | #AnmolmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Aagyamati Mataji-1972 | #AagyammatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Aryika Shri 105 Achalmati Mataji-1973 | #AchalmatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Satana |
| Aryika Shri 105 Bhavnamati Mataji 1966 | #BhavnamatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Balaghat |
| Aryika Shri 105 Sadaymati Mataji-1969 | #SadaymatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Balaghat |
| Aryika Shri 105 Bhaktimati Mataji-1946 | #BhaktimatiMataJi1946VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Balaghat |
| Aryika Shri 105 Satyamati Mataji-1960 | #SatyaMatiMaataJi,1960VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Aryika Shri 105 Gunmati Mataji-1963 | #GunmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Samaymati Mataji-1967 | #SamaymatiMaataJi,1967VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Aadarshmati Mataji-1964 | #AadarshmatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Dhaarnamati Mataji-1964 | #DhaarnaMatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Durlabhmati Mataji-1964 | #DurlabhmatiMaataJi1964VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Akhandmati Mataji-1969 | #AkhandmatiMaataJi1969VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Korba |
| Aryika Shri 105 Aalokmati Mataji-1966 | #AalokmatiMaataJi1966VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Apurvmati Mataji-1970 | #ApurvmatiMaataJi1970VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Kushalmati Mataji-1961 | #KushalmatiMataJi1961VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Anantmati Mataji | #AnantMatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Dhrudhmati Mataji-1961 | #Dradhmatiji1961VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Akshaymati Mataji-1967 | #AkshaymatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bhilai |
| Aryika Shri 105 Amandmati Mataji-1969 | #AmandmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Samvarmati Mataji-1969 | #SamvarmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Merumati Mataji-1974 | #MerumatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Nirmadmati Mataji-1976 | #NirmadmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bhilai |
| Aryika Shri 105 Anarghmati Mataji-1975 | #AnarghmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Antarmati Mataji-1967 | #AntarmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Anugrahmati Mataji-1967 | #AnugrahmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Amoortmati Mataji-1968 | #AmoortmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Anupammati Mataji-1968 | #AnupammatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Adhigammati Mataji-1968 | #AdhigammatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Abhedmati Mataji-1971 | #AbhedmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Korba |
| Aryika Shri 105 Nirmalmati Mataji-1963 | #NirmalmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Shuklmati Mataji-1963 | #ShuklmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Samvegmati Mataji | #SamvegmatiMataJiVidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Nirvegmati Mataji-1972 | #NirvegmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Shodhmati Mataji-1964 | #ShodhmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Omkaarmati Mataji-1968 | #OmkaarmatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Shashwatmati Mataji-1972 | #ShashwatmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Sushilmati Mataji-1964 | #SushilmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Susiddhmati Mataji-1970 | #SusiddhmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Udaarmati Mataji-1972 | #UdaarmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Santustmati Mataji-1975 | #SantustmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Nikatmati Mataji-1974 | #NikatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Amitmati Mataji-1972 | #AmitmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Narsinghpur |
| Aryika Shri 105 Shubhrmati Mataji-1967 | #ShubhrmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Sadhumati Mataji-1967 | #SadhumatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Vishadmati Mataji-1969 | #VishadmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Vipulmati Mataji-1970 | #VipulmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Madhurmati Mataji-1967 | #MadhurmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Satarkmati Mataji-1969 | #SatarkmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Vairagyamati Mata ji1967 | #VairagyamatiMataji1967VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Prasannmati Mataji-1967 | #PrasannmatiMataji1967VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sakalmati Mataji-1966 | #SakalmatiMataji1966VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sheetalmati Mataji-1971 | #SheetalmatiMataji1971VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Aryika Shri 105 Upshantmati Mataji-1967 | #UpshantmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Swasthamati Mataji-1961 | #SwasthamatiMataji1961VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Bilaspur |
| Aryika Shri 105 Gantavyamati Mataji-1969 | #GantavyamatiMataji1969VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Prithvimati Mataji-1974 | #PrithviymatiMataji1974VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Durg |
| Aryika Shri 105 Vineetmati Mata ji 1975 | #VineetmatiMataji1975VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Parmaarthmati Mataji-1983 | #ParmaarthmatiMataji1983VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Dhyanmati Mataji-1978 | #DhyanmatiMataji1978VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Korba |
| Aryika Shri 105 Videhmati Mataji-1970 | #VidehmatiMataji1970VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Aryika Shri 105 Aduurmati Mataji-1963 | #AduurmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Swabhavmati Mataji-1972 | #SwabhavmatiMataji1972VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Parammati Mataji-1982 | #ParammatiMataji1982VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Chetanmati Mataji-1986 | #ChetanmatiMataji1986VidyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Seoni |
| Aryika Shri 105 Vimalmati Mataji | #VimalmatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Kaivalyamati Mataji-1962 | #KaivalyamatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Aryika Shri 105 Nirvanmati Mataji | #NirvanmatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Madhya Pradesh | Chattarpur | |
| Aryika Shri 105 Avaymati Mataji | #AvaymatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Udyotmati Mataji | #UdyotmatijiAcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Raipur |
| Aryika Shri 105 Shwemati Mataji-1970 | #Shwetmatiji1970VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
| Ailak Shri Dhairya Sagarji Maharaj-1966 | #Dhairyasagarji1966VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Kshullak Shri 105 Sudhar Sagarji Maharaj | #SudharsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Sudhrudh Sagarji Maharaj | #SudhrudhsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Sayyam Sagarji Maharaj | #SayyamsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Ailak Shri 105 Samakit Sagarji Maharaj (Vidyasagarji) | #SamakitsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Veeral Sagarji Maharaj | #VeeralsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Vichar Sagarji Maharaj | #VicharsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Manan Sagarji Maharaj | #ManansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Manthan Sagarji Maharaj | #ManthansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Magan Sagarji Maharaj | #MagansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Dharashiv |
| Kshullak Shri 105 Nijatma Sagarji Maharaj | #NijatmasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Bihar | Bhagalpur |
| Kshullak Shri 105 Tanmay Sagarji Maharaj | #TanmaysagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Chaitya Sagarji Maharaj | #ChaityasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Gahan Sagarji Maharaj | #GahansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Ailak Shri 105 Kaivalya Sagarji Maharaj | #KaivalyasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Ailak Shri 105 Utsah Sagarji Maharaj | #UtsahsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Apar Sagarji Maharaj | #AparsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Athah Sagarji Maharaj | #AthahsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Sudharm Sagarji Maharaj | #SudharmsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chindwara |
| Kshullak Shri 105 Shwet Sagarji Maharaj | #ShwetsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Chindwara |
| Kshullak Shri 105 Vairagya Sagarji Maharaj | #VairagyasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Virat Sagarji Maharaj | #ViratsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Kshullak Shri 105 Nayan Sagarji Maharaj | #NayansagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Uttar Pradesh | Baraut | |
| Kshullak Shri 105 Tatwarth Sagarji Maharaj | #TatwarthsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dewas |
| Kshullak Shri 105 Atal Sagarji Maharaj | #AtalsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shajapur |
| Ailak Shri 105 Uchit Sagarji Maharaj | #UchitsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Gambhir Sagarji Maharaj-1961 | #Gambhirsagarji1961AcharyaShriVidyasagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Swagat Sagarji Maharaj-1983 | #Swagatsagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Kshullak Shri 105 Aagat Sagarji Maharaj-1986 | #Aagatsagarji1986VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Bhaswat Sagarji Maharaj-1979 | #Bhaswatsagarji1979VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Swastik Sagarji Maharaj-1986 | #Swastiksagarji1986VidyaSagarji1946 | 2025 | Madhya Pradesh | Guna | |
| Kshullak Shri 105 Bharat Sagarji Maharaj-1996 | #Bharatsagarji1996VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Jagrat Sagarji Maharaj-1997 | #Jagratsagarji1997VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Ailak Shri 105 Udyam Sagarji Maharaj-1975 | #Udyamsagarji1975VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Ailak Shri 105 Garistha Sagarji Maharaj-1983 | #Garisthasagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Kshullak Shri 105 Aadar Sagarji Maharaj-1969 | #Aadarsagarji1969VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Samaadar Sagarji Maharaj-1974 | #Samaadarsagarji1974VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Ailak Shri 105 Auchitya Sagarji Maharaj-2000 | #Auchityasagarji2000VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Anunay Sagarji Maharaj-1983 | #Anunaysagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Delhi | Delhi | |
| Kshullak Shri 105 Savinay Sagarji Maharaj-1983 | #Savinaysagarji1983VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Samanvay Sagarji Maharaj-1982 | #Samanvaysagarji1982VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Hirak Sagarji Maharaj-1988 | #Hiraksagarji1988VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bagidaura |
| Kshullak Shri 105 Nirdhum Sagarji Maharaj-1995 | #Nirdhumsagarji1995VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Kshullak Shri 105 Varisth Sagarji Maharaj-1982 | #Varisthsagarji1982VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Gaurav Sagarji Maharaj-1985 | #Gauravsagarji1985VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Vidisha |
| Kshullak Shri 105 Videh Sagarji Maharaj-1990 (Vidyasagarji) | #Videhsagarji1990VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Ailak Shri 105 Amapsagarji Maharaj-1993 | #Amapsagarji1993VidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kshullak Shri 105 Swastiksagarji Maharaj | #SwastiksagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Guna |
| Kshullak Shri 105 Aadarsagarji Maharaj | #AadarsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Chidrupsagarji Maharaj | #ChidrupsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Swaroopsagarji Maharaj | #SwaroopsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Kshullak Shri 105 Subhagsagarji Maharaj | #SubhagsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Aagam Sagar Ji Maharaj 1976 | #AagamSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Chhattisgarh | Bastar |
| Muni Shri 108 Vishwaharsh Sagarji Maharaj | #VishwaharshSagarjiViharshSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Muni Shri 108 Vichintya Sagar Ji Maharaj 1983 | #VichintyaSagarJiMaharaj1983VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vijay Sagar Ji Maharaj 1972 | #VijaySagarJiMaharaj1972VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vishwarya Sagar Ji Maharaj 1943 | #VishwaryaSagarJiMaharaj1943VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vishwarth Sagar Ji Maharaj 1948 | #VishwarthSagarJiMaharaj1948VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vivrat Sagar Ji Maharaj 1993 | #VivratSagarJiMaharaj1993VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Shamali |
| Muni Shri 108 Visham Sagar Ji Maharaj 1978 | #VishamSagarJiMaharaj1978VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Usmanpur |
| Muni Shri 108 Vishwansh Sagar Ji Maharaj 1961 | #VishwanshSagarJiMaharaj1961VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vigamya Sagar Ji Maharaj 1995 | #VigamyaSagarJiMaharaj1995VimarshSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Muni Shri 108 Vishwagya Sagarji Maharaj | #VishwagyaSagarjiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Aryika Shri 105 Vidyantshree Mata ji 1987 | #VidyantshreeMataji1987VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vimlantshree Mata Ji 1983 | #VimlantshreeMataJi1983VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vikrantshree Mata Ji 1977 | #VikrantshreeMataJi1977VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vishwantshree Mata Ji 1958 | #VishwantshreeMataJi1958VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vidhyantshree Mata ji 1983 | #VidhyantshreeMataji1983VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vijyantshree Mata Ji 1951 | #VijyantshreeMataJi1951VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Aryika Shri 105 Vinayantshree Mata Ji 1975 | #VinayantshreeMataJi1975VimarshSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Kshullika Shri 105 Viprantshree Mataji | #ViprantshreejiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Kshullika Shri 105 Videhantshree Mataji | #VidehantshreejiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Kshullika Shri 105 Vidikshantshree Mataji | #VidikshantshreejiVimarshSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| Acharya Shri 108 Vinamra Sagarji Maharaj 1963 | #VinamraSagarjiMaharaj1963ViragSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vigya Sagar Ji Maharaj 1976 | #VigyaSagarJiMaharaj1976VinamraSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vinut Sagar Ji Maharaj 1994 | #VinutSagarJiMaharaj1976VinamraSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vishwakund Sagarji Maharaj | #VishwakundSagarjiVinamraSagarjiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vipulshri Mataji-1986 | #VipulshriMataji1986VinamraSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vishramshri Mataji (Banswada) | #VishamshriMataji(Banswada)VinamraSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vimudshri Mata ji 1990 | #VimudshriMataji1990VinamraSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vibhavyamati Mataji | #VibhavyamatijiVinamraSagarjiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Visarvmati Mataji | #VisarvmatijiVinamraSagarjiMaharaj1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Pragyey Sagarji Maharaj | #PragyeySagarjiVipranatSagarJiMaharaj1984 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prabha Sagarji Maharaj | #PrabhaSagarjiVipranatSagarJiMaharaj1984 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Vishuddha Sagar Maharaj 1971 | #VishuddhaSagarMaharaji1971ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Aditya Sagar Ji Maharaj 1986 | #AdityaSagarJiMaharaj1986VishudhSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj 1981 | #SuprabhSagarJiMaharaj1981VishudhSagarji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Manogya Sagar Ji Maharaj 1948 | #ManogyaSagarJiMaharaj1948VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj 1977 | #PrashamSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1977 | #SubratSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Suyash Sagar Ji Maharaj 1980 | #SuyashSagarJiMaharaj1980VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Anuttar Sagar Ji Maharaj 1977 | #AnuttarSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Anupam Sagar Ji Maharaj 1986 | #AnupamSagarJiMaharaj1986VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhilwara |
| Muni Shri 108 Arijit Sagar Ji Maharaj 1983 | #ArijitSagarJiMaharaj1983VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Nagaland | Dimapur |
| Muni Shri 108 Aastikya Sagarji Maharaj-(Shraman Muni)-1984 | #AastikyaSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jalgaon |
| Muni Shri 108 Praneet Sagarji Maharaj-(Shraman Muni)-1984 | #PraneetSagarjiMaharaj1984VishuddhaSagarJi1971 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Aaradhya Sagar Ji Maharaj 1977 | #AaradhyaSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Pranay Sagar Ji Maharaj 1982 | #PranaySagarJiMaharaj1982VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Pranav Sagar Ji Maharaj 1984 | #PranavSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Pranat Sagar Ji Maharaj 1978 | #PranatSagarJiMaharaj1978VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Pranut Sagar Ji Maharaj 1993 | #PranutSagarJiMaharaj1993VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Ujjain |
| Muni Shri 108 Sarvaarth Sagar Ji Maharaj 1991 | #SarvaarthSagarJiMaharaj1991VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Saamya Sagar Ji Maharaj 1989 | #SaamyaSagarJiMaharaj1989VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1979 | #SehajSagarJiMaharaj1979VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Samatva Sagar Ji Maharaj 1984 | #SamatvaSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Saadhya Sagar Ji Maharaj 1987 | #SaadhyaSagarJiMaharaj1987VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sanawat |
| Muni Shri 108 Sankalp Sagar Ji Maharaj 1981 | #SankalpSagarJiMaharaj1981VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Jintoor |
| Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj 1996 | #SomyaSagarJiMaharaj1996VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Tikamgadh |
| Muni Shri 108 Saaraswat Sagar Ji Maharaj 1998 | #SaaraswatSagarJiMaharaj1998VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sangli |
| Muni Shri 108 Sadbhaav Sagar Ji Maharaj 1986 | #SadbhaavSagarJiMaharaj1986VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Ratlam |
| Muni Shri 108 Sanjayant Sagar Ji Maharaj 1989 | #SanjayantSagarJiMaharaj1989VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Saiyat Sagar Ji Maharaj 1973 | #SaiyatSagarJiMaharaj1973VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Rawatbhata |
| Muni Shri 108 Sakshya Sagar Ji Maharaj 1979 | #SakshyaSagarJiMaharaj1979VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Silwani |
| Muni Shri 108 Yashodhar Sagar Ji Maharaj | #YashodharSagarJiMaharajVishuddhSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji Maharaj | #NirgranthSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nirvikalp Sagar Ji Maharaj | #NirvikalpSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nivratt Sagar Ji Maharaj | #NivrattSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Silwani |
| Muni Shri 108 Nisang Sagar Ji Maharaj | #NisangSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji Maharaj | #NirmohSagarjiVishuddhSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhilwara |
| Muni Shri 108 Yatna Sagarji Maharaj | #YatnasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Yatindra Sagarji Maharaj | #YatindrasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Jayandra Sagarji Maharaj | #JayandrasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Tikamgadh |
| Muni Shri 108 Jitendra Sagarji Maharaj | #JitendrasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Jayant Sagarji Maharaj | #JayantsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sangli |
| Muni Shri 108 Subhag Sagarji Maharaj | #SubhagSagarjiMaharajVishuddhSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Siddha Sagarji Maharaj-2002 | #SiddhaSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Muni (Shraman) Shri 108 Siddharth Sagarji Maharaj-1999 | #SiddharthSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Saharsh Sagarji Maharaj-1999 | #SaharshSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Satyarth Sagarji Maharaj-2000 | #SatyarthSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Sarthak Sagarji Maharaj-1977 | #SarthakSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Sarth Sagarji Maharaj-1995 | #SarthSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni (Shraman) Shri 108 Samakit Sagarji Maharaj-2003 | #SamakitSagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Kshullak Shri 105 Shrutsagarji Maharaj (Vishuddhasagarjji) | #ShrutsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Ailak Shri Vipramansagarji Maharaj | #VipramansagarjiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullak Shri 105 Videh Sagarji Maharaj (Viveksagarji) | #VidehsagarjiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Vigunmati Mataji | #VigunmatijiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Shri Sammed Shikharji | ||
| Acharya Shri 108 Yatindra Sagarji Maharaj | #YatindrasagarjiYogendraSagarJiMaharaj1961 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Acharya Shri 108 Prasannrishiji Maharaj-1981 | #PrasannrishiJiMaharaj1981KushagranandiJi | 2025 | Madhya Pradesh | Indore | |
| Aryika Shri 105 Kirtivani Mataji | #KirtivanijiKusagraNandiJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Prabhakar Sagarji Maharaj | #PrabhakarsagarjiPramukhSagarJiMaharaji1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Aryika Shri 105 Pritishri Mataji | #PritishriPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Aryika Shri 105 Parikshashri Mataji | #ParikshashriPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullak Shri 105 Parmanandsagarji Maharaj | #ParmanandsagarjiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Paramsadhya Mataji | #ParamsadhyamatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Paramshantaji Mataji | #ParamshantajimatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Paramdivyashri Mataji | #ParamdivyashrimatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Aradhanashri Mataji | #AradhanashriMatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Kshullika Shri 105 Parmaradhyashri Mataji | #ParmaradhyashriMatajiPramukhSagarJi1973 | 2025 | Confirmed | West Bengal | Kolkatta |
| Acharya Shri 108 Namostu Sagar Ji Maharaj 1989 | #NamostuSagarJiMaharaj1989PunyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hapud |
| Aryika Shri 105 Suratnamati Mataji (Punyasagarji) | #SuratnamatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji | |
| Muni Shri 108 Mahima Sagar Ji Maharaj 1973 | #MahimaSagarJiMaharaj1973VardattSagarJi | 2025 | Maharashtra | Nashik | |
| Muni Shri 108 Achol Sagarji Maharaj | #AcholsagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Agarbh Sagarji Maharaj | #AgarbhsagajiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Abhed Sagarji Maharaj | #AbhedsagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Aganya Sagarji Maharaj | #AganyasagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Akamp Sagarji Maharaj | #AkampsagarjiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Muni Shri 108 Divyasen Ji Maharaj | #DivyasenjiDevsenJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Gadni Aryika Shri 105 Saraswati Mata ji 1961 | #SaraswatiMatajiSubalSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Bagpat |
| Aryika Shri 105 Anantmati Mataji-(Subal Sagarji) | #AnantmatiSubalSagarJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Bagpat |
| Aryika Shri 105 Mokshmati Mataji | #MokshmatiMatajiAcharyaShriTirthanandijiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullak Shri 105 Naman Sagarji Maharaj (Tirthanandiji) | #NamanSagarjiAcharyaShriTirthanandijiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Pravar Sagar Ji Maharaj 1980 | #PravarSagar | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Pragyan Sagar Ji Maharaj 1993 | #PragyanSagar | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bundi |
| Muni Shri 108 Prasiddha Sagarji Maharaj | #PrasiddhaSagarjiVinishchaysagarJiMaharaj1973 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bundi |
| Muni Shri 108 Apurva Sagarji Maharaj 1966 | #ApurvaSagarJiMaharaj1966VardhmanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Arpit Sagarji Maharaj 1966 | #ArpitSagarJiMaharaj1966VardhmanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Prabhav Sagarji Maharaj 1944 | #PrabhavSagarjiMaharaj1944VardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Mumukshu Sagarji Maharaj | #MumukshuSagarJiMaharajVardhmaanSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Samarpitmati Mataji | #SamarpitmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 108 Pranatmati Mataji-1961 | #PranatmatiVardhamanSagarJi1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Ratanmati Mataji | #RatanmatijiGambhirmatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Tyagmati Mataji | #TyagmatijiGambhirmatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Dayanshumati Mataji | #DayanshumatijiGambhirmatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Chandnamati Mata Ji 1958 | #ChandnamatiMataJi1958GyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Suvratmati Mataji (Gyanmatiji) | #SuvratmatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Swarnamati Mataji (Gyanmatiji) | #SwarnamatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Sudhrudhmati Mataji-1977 | #Sudhrudhmatiji1977GyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Muditmati Mataji | #MuditmatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Bhaktimati Mataji | #BhaktimatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Kshullak Shri 105 Prashant Sagarji Maharaj | #PrashantSagarjiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Kshullak Shri 105 Jinsagarji Maharaj | #JinsagarjiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| Aryika Shri 105 Shrutikashree Mata Ji 1979 | #ShrutikashreeMataJi1979KamalshreeMataJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Kshullika Shri 105 Nikankshashri Mataji (Kshamashrimataji) | #NikankshashrijiKshamashri | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Uoon |
| Aryika Shri 105 Devyashmati Mataji 1984 | #DevyashMatiMataJi1984PrashantmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Devagammati Mataji-1983 | #DevagamMatiMataji1983PrashantmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Devardhi Mati Mata ji 1983 | #DevardhiMatiMataji1983PrashantmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Kshullika Shri 105 Sundarmati Mataji | #SundarmatijiSakalmatiMataji1966 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Kshullika Shri 105 Shravanmati Mataji | #ShravanmatijiShreyanshmatiMataji(Pune) | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Garima mati Mata ji | #GarimamatiMataji | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Aryika Shri 105 Suhitmati Mataji | #SuhitmatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Suvegmati Mataji | #SuvegmatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Sugeetmati Mataji | #SugeetmatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Bhavanamati Mataji | #BhavanamatijiSuprakashmatiMataji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Vigyanmati Mataji 1963 | #VigyanmatiMataji1963VivekSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Adityamati Mataji 1972 | #AdityamatiMataji1972VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Charanmati Mataji 1980 | #CharanmatiMataji1980VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Karanmati Mataji 1981 | #KaranmatiMataji1981VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Banswara |
| Aryika Shri 105 Sharanmati Mataji-(Vigyanmatiji) | #SharanmatiMatajiVigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Pavitramati Mata ji 1974 | #PavitramatiMataji1974VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Banswara |
| Aryika Shri 105 Suyashmati Mataji 1986 | #SuyashmatiMataji1986VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Uditmati Mataji 1982 | #UditmatiMataji1982VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Chpttorgarh |
| Aryika Shri 105 Varadmati Mataji 1958 | #VaradmatiMataji1958VigyanmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Sharadmati Mataji-1977 | #SharadmatiMataji1977VigyanmatiMataJi1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Chpttorgarh |
| Aryika Shri 105 Suveermati Mataji-1987 | #SuveermatiMataji1987VigyanmatiMataJi1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Partapur |
| Aryika Shri 105 Rajatmati Mataji-1986 | #RajatmatiMataji1986VigyanmatiMataJi1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Chpttorgarh |
| Aryika Shri 105 Suvandanshree Mataji | #SuvandanshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Aryika Shri 105 Sundanshree Mataji | #SundanshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Kshullika Shri 105 Suparvshree Mataji | #SuparvshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Kshullika Shri 105 Suchandanshree Mataji | #SuchandanshreejiVindhyashriMaataJi1973 | 2025 | Confirmed | Tamilnadu | Suleha |
| Kshullika Shri 105 Vishalmati Mataji | #VishalmatijiVipulmatiMataJi1970 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Vimalmati Mataji-(Vipulmatiji) | #VimalmatijiVipulmatiMataJi1970 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Vidarshammati Mataji | #VidarshammatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Vikarshmati Mataji | #VikarshmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Kshullika Shri 105 Vishrutmati Mataji | #VishrutmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Kshullika Shri 105 Vipulmati Mataji | #VipulmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Ganini Aryika Shri 105 Vishisthmati Mataji | #VishisthmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Visheshmati Mataji | #VisheshmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Rajasthan | Pratapgadh | |
| Aryika Shri 105 Vibhushanmati Mataji | #VibhushanmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Viditmati Mataji | #ViditmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Vijitmati Mataji | #VijitmatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Kshullika Shri 105 Vidushimati Mataji | #VidushimatiVishudhmatiMataJi1975 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Pratapgadh |
| Aryika Shri 105 Vikhyatmati Mataji | #VikhyatmatijiGarimamatiMataji1972 | 2025 | Confirmed | Assam | Dispur |
| Ganini Aryika Shri 105 Yashasvini Mataji | #GadniYashasviniMataji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Kamalshri Mataji | #KamalshrijiNipunnandiji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Sanyogmati Mataji | #SanyogmatijiSangamMatiMataji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Manaswinimati Mataji | #ManaswinimatijiGadniYashasviniMataji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Ganani Pramukh Aryika Shri 105 Vimal Prabha Mata Ji 1951 | #VimalPrabhaMataJi1951VijayamatiMataJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Ganini Aryika Shri 105 Nangmati Mataji | #NangmatijiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Aryika Shri 105 Vishnuprabhashree Mataji | #VishnuprabhashreejiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Vijayprabhashree Mataji | #VijayprabhashreejiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Vijitprabha Mataji | #VijitprabhajiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullika Shri 105 Vinatprabha Mataji | #VinatprabhajiVimalPrabhaMataJi1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Aryika Shri 105 Sugreevmati Mataji | #SugreevmatijiShreyanshmatiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Shradhyeymati Mataji | #ShradhyeymatijiShreyanshmatiji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Ganini Aryika Shri 105 Vigyashree Mataji 1972 | #VigyashreeMataJi1972ViragsagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gyeyak Shri Mata ji | #GyeyakShriMataji | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gyanshree Mataji | #GyanshreejiVigyashreeMataJi1972 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gnyevyashree Mataji | #GnyevyashreejiVigyashreeMataJi1972 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Aryika Shri 105 Gyayakshree Mataji | #GyayakshreejiVigyashreeMataJi1972 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Hastinapur |
| Ganini Aryika Shri 105 Vishudhmati Mataji-1949 | #Vishuddhmatimatiji1949NirmalSagarJiMaharaj1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Muni Shri 108 Maun Sagarji Maharaj | #MaunSagarjiBhutbalisagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Susner |
| Muni Shri 108 Muni Sagarji Maharaj | #MuniSagarjiBhutbalisagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Susner |
| Muni Shri 108 Mukti Sagarji Maharaj | #MuktiSagarjiBhutbalisagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Susner |
| Muni Shri 108 Mangalsagar Ji Maharaj | #MangalsagarjiManglanandSagarji | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Shivpuri |
| Kshullak Shri 105 Priytirth Ji Maharaj | #PriytirthjiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Kshullak Shri 105 Purnatirth Sagarji Maharaj | #PurnatirthsagarjiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Kshullika Shri 105 Shantiprgayashri Mataji | #ShantiprgayashrijiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Kshullika Shri 105 Prayagmati Mataji | #PrayagmatijiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Ailak Tatvarthsagar Ji Maharaj | #TatvarthsagarjiVishalya | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Uditsagarji Maharaj-1949 | #Uditsagarji1949PunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Aryika Shri 105 Utsahmati Mataji | #UtsahmatiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Ganini Aryika Shri 105 Adityashri Mataji | #AdityashrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Nityashri Mataji | #NityashrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Diptishri Mataji | #DiptishrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Dikshashri Mataji | #DikshashrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Aryika Shri 105 Maitrishri Mataji | #MaitrishrijiGunbhadraNandiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Karnataka | Chikkamagaluru |
| Acharya Shri 108 Anekant Sagarji Maharaj 1963 | #AnekantSagarjiMaharaj1963AbhinandanaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Ichalkaranji |
| Acharya Shri 108 Prasanna Sagarji Maharaj 1970 (Antarmana) | #PrasannaSagarJiMaharaj1970(Antarmana)PushpdantSagarJi | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Aacharya Shri 108 Gupti Nandi Ji Maharaj 1972 | #GuptiNandiJiMaharaj1972KunthuSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Acharya 108 Shri Bharat Bhushanji Maharaj 1982 | #BharatBhushanJiMaharaj1980DharmabhushanJi | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Muzzaffarnagar |
| Balacharya Shri 108 Bhadrabahu Sagar Ji Maharaj | #BhadrabahuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Apramit Sagar Ji Maharaj 1984 | #ApramitSagarJiMaharaj1984VishudhSagarji | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Muni Shri 108 Pragyasagar Ji Maharaj - 1972 | #PragyasagarJiMaharaj-1972PuspdantSagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Muni Shri 108 Saurabhnandi Ji Maharaj 1991 | #SaurabhnandiJiMaharaj1991VairagyanandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Saiyamnandi Ji Maharaj | #SaiyamnandiJiMaharajVairagyanandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shramannandi Ji Maharaj | #ShramannandiJiMaharajVairagyanandiJi | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Amogh Sagar Ji Maharaj 1947 | #AmoghSagarJiMaharaj1947AmitSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Pujya Muni Shri 108 Piyushsagarji Muniraj 1969 | #PujyaPiyushsagarjiMuniraj1969Pushpadantasagarji | 2025 | Confirmed | zzzzz | Indore |
| Muni Shri 108 Shubham Kirti Ji Maharaj | #ShubhamKirtiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Prashantsagar Ji Maharaj 1963 | #PrashantsagarJiMaharaj1963PavitrsagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Prathamanand Ji Maharaj | #PrathamanandJiMaharaj | 2025 | Confirmed | New Delhi | New Delhi |
| Muni Shri 108 Mardav Sagarji Maharaj | #mardavsagarjimaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Subhadra Sagarji Maharaj | #SubhadrasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Vishwavijay Sagarji Maharaj | #VishwavijayViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salambur |
| Muni Shri 108 Vidhruv Sagarji Maharaj | #VidhruvViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vikoshal Sagarji Maharaj | #VikoshalViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Muni Shri 108 Vishwalokesh Sagarji Maharaj | #VishwalokeshViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vinivesh Sagarji Maharaj | #ViniveshViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Prakshal Sagarji Maharaj | #PrakshalViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Parbhani |
| Muni Shri 108 Suyatna Sagarji Maharaj | #SuyatnasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Mumbai |
| Muni Shri 108 Sarvarth Sagarji Maharaj | #SarvarthsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Samakit Sagarji Maharaj | #SamakitsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Prabuddha Sagarji Maharaj-1954 | #PrabuddhaSagarji1954VardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Shrutesh Sagarji Maharaj | #ShruteshsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Madhya Pradesh | Nainagiri | |
| Muni Shri 108 Vimalgupt Sagarji Maharaj | #VimalguptsagarjiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Pune |
| Muni Shri 108 Samantbhadraji Maharaj | #SamantbhadrajiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Shrutdharnandiji Maharaj | #ShrutdharnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Gujarat | Sabarkantha |
| Muni Shri 108 Shantinandiji Maharaj | #ShantinandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Prabhachandnandiji Maharaj | #PrabhachandnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Amarnandiji Maharaj | #AmarnandijiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kunthugiri |
| Muni Shri 108 Shrutkirtiji Maharaj | #ShrutkirtijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Hashendrasagarji Maharaj | #HashendrasagarjiPunyaSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Sandesh Sagarji Maharaj | #SandeshsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Muni Shri 108 Santosh Sagarji Maharaj | #SantoshsagarjiSiddhantSagarJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bela Ji |
| Muni Shri 108 Shreenandiji Maharaj | #ShreenandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shreekarnandiji Maharaj | #ShreekarnandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Vatsanandiji Maharaj | #VatsanandijiVairagyanandiji1974 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Shubhbahubali Sagarji Maharaj | #ShubhbahubalisagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Shubhkirti Sagarji Maharaj | #ShubhkirtisagarjiSaubhagyaSagarJiMaharaj1965 | 2025 | Confirmed | New Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Suvigya Sagarji Maharaj | #SuvigyasagarjiSuvidhiSagarJi1971 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Bhiluda |
| Muni Shri 108 Samay Sagarji Maharaj | #SamaysagarjiSanmatiSagarJiMaharaj1927(Dakshin) | 2025 | Madhya Pradesh | Bhagyaday Tirth, Sagar | |
| Muni Shri 108 Ajitsagar Ji Maharaj | #AjitsagarjiSanmatiSagarJiMaharaj1927(Dakshin) | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat |
| Muni Shri 108 Archit Sagarji Maharaj | #ArchitsagarjiVivekSagarJiMaharaj1972 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Anant Sagarji Maharaj | #AnantsagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1951 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Muni Shri 108 Aaptpramatt Sagarji Maharaj | #AaptpramattsagarjiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Muni Shri 108 Parimalsagarji Maharaj | #ParimalsagarjiPrasannaSagarJiMaharaj1970 | 2025 | Confirmed | Delhi | Muradnagar |
| Muni Shri 108 Vilok Sagarji Maharaj | #ViloksagarjiAarjavSagarJiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Morena |
| Muni Shri 108 Sutirth Sagarji Maharaj | #SutirthsagarjiSaubhagyasagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Yogya Sagarji Maharaj | #YogyasagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Damoh |
| Muni Shri 108 Pratigyanand Ji Maharaj | #PratigyanandjiPragyasagarJiMaharaj-1972 | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Prabhav Sagarji Maharaj | #PrabhavsagarjiPavitrasagarJiMaharaj1949 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Prabhat Sagarji Maharaj | #PrabhatsagarjiPavitrasagarJiMaharaj1949 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Hingoli |
| Muni Shri 108 Amitanjaykirti Ji Maharaj | #AmitanjaykirtijiJaykirtiji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Ajitsen Ji Maharaj (Jinsenji) | #AjitsenjiBalacharyaShriJinsenJiMaharaj1976 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Ekatva Sagarji Maharaj (Chaityamatiji) | #EkatvasagarjiChaityamatiji | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Aryika Shri 105 Vigya Shri Mata Ji 1969 | #VigyaShriMataJi1969VishuddhmatiMataJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| Aryika Shri 105 Shubh Mati Mata ji 1975 | #ShubhMatiMataji1975SanmatiSagarjiMaharaj | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Garimamati Mata ji 1972 | #GarimamatiMataji1972 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Banswara |
| Aryika Shri 105 Hemshriji Mataji | #HemshrijiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Aryika Shri 105 Savinaymati Mataji | #SavinaymatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Mandla |
| Aryika Shri 105 Anubhavmati Mataji | #AnubhavmatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Aryika Shri 105 Anuttarmati Mataji | #AnuttarmatiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Chattisgarh | Akaltara |
| Aryika Shri 105 Sakshepmati Mataji | #SakshepmatijiSaubhagyamatiji | 2025 | Confirmed | Telangana | Hyderabad |
| Aryika Shri 105 Shikshamati Mataji | #ShikshamatijiSaubhagyamatiji | 2025 | Confirmed | Telangana | Hyderabad |
| Ailak Shri Vivekanand Sagarji Maharaj | #VivekanandsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Surat Nagar |
| Ailak Shri Nishchay Sagarji Maharaj | #NishchaysagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Ailak Shri Nijanand Sagarji Maharaj | #NijanandsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji/ Hazaribaug |
| Ailak Shri Daya Sagarji Maharaj | #DayasagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Gwalior |
| Ailak Shri Upsham Sagarji Maharaj | #UpshamsagarjiVidyaSagarji1946 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bareilly |
| Ailak Shri 105 Swasti Sagarji Maharaj | #SwastiSagarjiSamanvaySagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Prateek Sagarji Maharaj-1980 (Krantiveer) | #PrateekSagarji1980(Krantiveer)PushpaDantaSagarJi | 2025 | Uttar Pradesh | Baghpath | |
| Upadhyay Shri 108 Vishok Sagarji Maharaj 1975 | #VishokSagarjiMaharaj1975ViragsagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Upadhyay Shri 108 Vihasant Sagar Ji Maharaj 1983 | #VihasantSagarJiMaharaj1983ViragSagarJi(Anklikar) | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Bhind |
| Upadhay Shri 108 Gupti Sagarji Maharaj-1957 | #Guptisagarji1957VidyaSagarji | 2025 | Haryana | Sonipat | |
| Upadhyay Shri 108 Viksant Sagar Ji Maharaj 1985 | #ViksantSagarJiMaharaj1985GanacharyaShriViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jhalawar |
| Upadhyay Shri 108 Vibhanjan Sagarji Maharaj-1983 | #VibhanjanSagarJiMaharaj1983ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dhaar |
| Upadhyay Shri 108 Vishrutsagar Ji Maharaj 1976 | #VishrutsagarJiMaharaj1976ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Khandwa |
| Upadhyay Shri 108 Urjayant Sagar Ji Maharaj 1977 | #UrjayantSagarJMaharaj1977VimalSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Upadhyay Shri 108 Viranjan Sagarji Maharaj | #ViranjanViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Sambhajinagar |
| Muni Shri 108 Jayant Sagarji Maharaj | #JayantsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Muni Shri 108 Saaraswat Sagar Ji Maharaj 1998 | #SaaraswatSagarJiMaharaj1998VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Kolhapur |
| Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj 1996 | #SomyaSagarJiMaharaj1996VishuddhaSagarJi | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Tikamgarh |
| Acharya Shri 108 Viharsh Sagar Ji Maharaj 1970 | #ViharshSagarJiMaharaj1970ViragsagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salumbar |
| Kshullika Shri 105 Sugunmati Mataji | #SugunmatijiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Kshullika Shri 105 Sumanshree Mataji | #SumanshreejiDevNandiJiMaharaj | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nashik |
| Muni Shri 108 Utkarsh Sagarji Maharaj | #UtkarshsagarjiKunthuSagarJiMaharaj | 2025 | Gujarat | Sabarkantha | |
| Muni Shri 108 Vishwagyeya Sagarji Maharaj | #VishwagyeyajiViragSagarji1963 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dhaar |
| Muni Shri 108 Shuddha Sagarji Maharaj | #ShuddhaSagarJiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Maharashtra | Nagpur |
| Muni Shri 108 Sheel Sagarji Maharaj | #SheelSagarJiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Sagar |
| Kshullak Shri 105 Shreysagarji Maharaj | #ShreysagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Shreyashsagarji Maharaj | #ShreyashsagarjiVishuddhaSagarMaharaji1971 | 2025 | Rajasthan | Jaipur | |
| Muni Shri 108 Vishalsagarji Maharaj | #VishalsagarjiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Muni Shri 108 Vishubhsagarji Maharaj | #VishubhsagarjiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Salambur |
| Muni Shri 108 Vibhorsagarji Maharaj | #VibhorsagarjiVishadSagarJiMaharaj1964 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Dhar/Indore |
| Kshullak Shri 105 Kshemankar Sagarji Maharaj | #KshemankarsagarjiVibhaktSagarJiMaharaj1969 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Indore |
| Kshullak Shri 105 Sumitrasagarji Maharaj | #SumitrasagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Savimalsagarji Maharaj | #SavimalsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Kshullak Shri 105 Suratsagarji Maharaj | #SuratsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Gujarat | Ahmedabad |
| Muni Shri 108 Saksham Sagarji Maharaj | #SakshamsagarjiSunilSagarJi1977 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Dungarpur |
| Aryika Shri 105 Aarshmati Mataji-(Gyanmatiji) | #AarshmatijiGyanmatiMataji1934 | 2025 | Confirmed | Uttar Pradesh | Badauth |
| Aryika Shri 105 Prashantnandini Mataji | #PrashantnandinijiVasunandijiMaharaj1967 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Jaipur |
| Acharya Shri 108 Vinischay Sagarji Maharaj-1973 | #VinischayaSagarJiMaharaj1973ViragSagarJi | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Kota |
| Muni Shri 108 Paay Sagarji Maharaj-1969 | #PaaySagarJiMaharaj1969VidyaSagarJi | 2025 | Confirmed | Karnataka | Senki Gatta |
| Aryika Shri 105 Amoghmati Mataji | #AmoghmatijiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Aryika Shri 105 Arpanmati Mataji | #ArpanmatijiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Aryika Shri 105 Anshmati Mataji | #AnshmatijiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Haryana | Ranila |
| Kshullak Shri 105 Samyayog Sagarji Maharaj | #SamyayogSagarjiVishuddhaSagarMaharajji1971 | 2025 | Confirmed | Nagaland | Dimapur |
| Kshullak Shri 105 Paramyog Sagarji Maharaj | #ParamyogSagarjiVishuddhaSagarMaharajji1971 | 2025 | Confirmed | Madhya Pradesh | Ratlam |
| Muni Shri 108 Vishwaksh Sagarji Maharaj-(Vidyasagarji) | #VishwakshSagarjiAcharyaShriVidyasagarjiMaharaj | 2025 | Confirmed | Delhi | Delhi |
| Muni Shri 108 Praneetsagarji Maharaj | #PraneetsagarjiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Dhyey Sagarji Maharaj | #DhyeySagarjiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Bhuvan Sagarji Maharaj | #BhuvanSagarjiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Prekshamati Mataji-1955 | #PrekshamatijiVardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Aryika Shri 105 Jineshmati Mataji-1945 | #Jineshmatiji1945Vardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Ailak Shri 105 Harsh Sagarji Maharaj | #HarshSagarjiVardhamansagarjiDharmsagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Kshullak Shri 105 Praptisagarji Maharaj-1956 | #Praptisagarji1956Vardhamansagarji | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Tonk |
| Muni Shri 108 Vivarjit Sagarji Maharaj-1951 | #VivarjitSagarjiVardhamanSagarJiMaharaj1950 | 2025 | Confirmed | Rajasthan | Udaipur |
| Muni Shri 108 Niyogsagarji Maharaj | #NiyogsagarjiDnyesagarji | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
| Muni Shri 108 Harshendrasagarji Maharaj | #HarshendrasagarjiPunyasagarji1965 | 2025 | Confirmed | Jharkhand | Shri Sammed Shikharji |
श्रुतधराचार्यों की परंपरामें सर्वप्रथम आचार्य गुणधरका नाम आता है। गुणधर और धरसेन दोनों ही श्रुत-प्रतिष्ठापकके रूपमें प्रसिद्ध हैं। गुणधर आचार्य धरसेनकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी थे। गणधरको 'पञ्चमपूर्वगत पेज्जदोसपाहुड' का ज्ञान प्राप्त था और धरसेनको 'पूर्वगत कम्मपयडिपाहुड' का। इतना ही नहीं, किन्तु गुणधरको 'पेज्जदोसपाहुड’ के अतिरिक्त 'महाकम्मपयडिपाहुड' का भी ज्ञान प्राप्त था, जिसका समर्थन 'कसायपाहुड’ से होता है । 'कसायपाहुड' में बन्ध, संक्रमण, उदय और उदीरणा से पृथक् अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार 'महाकम्मपयडिपाहुड’ के चौबीस अनुयोगद्वारों में से क्रमशः षष्ठ, द्वादश और दशम अनुयोगद्वारोंसे संबद्ध हैं। 'महाफम्मपयडिपाहुड' का चौबीसवाँ अल्पबहुत्व नामक अनुयोगद्वार भी 'कसायपाहुड' के सभी अधिकारोंमें व्याप्त है । अतः स्पष्ट है कि आचार्य गुणधर 'महाकम्मपयडिपाहुड’ के ज्ञाता होने के साथ 'पेज्जदोसपाहुड' के ज्ञाता और 'कसायपाहुड' के रूपमें उसके उपसंहारकर्ता भी थे। पर 'छक्खडागम’ की धवला-टोकाके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात नहीं होता कि धरसेन 'पेज्ज दोसपाहुड' के ज्ञाता थे। अतएव आचार्य गुणधरको दिगंबर परंपरामें लिखित रूपमें प्राप्त श्रुतका प्रथम श्रुतकार माना जा सकता है। धरसेनने किसी ग्रंथकी रचना नहीं की। जबकि गुणधरने 'पेज्जदोसपाहुड' की रचना की है। जयघवलाके मंगलाचरणके पश्चसे ज्ञात होता है कि आचार्य गुणधरने कसायपाहुडका गाथाओं द्वारा व्याख्यान किया है।
जैणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जलं अणंतत्थं।
माहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे ॥ ६ ॥
इसके अनन्तर आचार्य वीरसेनने लिखा है - ज्ञानप्रवादपूर्वके निर्मल दसवें वस्तु अधिकारके तृतीय कसायपाहुडरूपी समुद्रके जलसमूहसे प्रक्षालित मति ज्ञानरूपी नेत्रवारी एवं त्रिभुवन-प्रत्यक्षज्ञानकर्ता गणधर भट्टारक हैं और उनके द्वारा उपदिष्ट गाथाओंमें सम्पूर्ण कसायपाहुडका अर्थ समाविष्ट है। आचार्य वीरसेनने उसी संदर्भ में आगे लिखा है कि तीसरा कषायनाभूत महासमुद्रके तुल्य है और आचार्य गुणधर उसके पारगामी हैं।
वीरसेनाचार्यके उक्त कथनसे यह ध्वनित होता है कि आचार्य गुणधर पूर्व विदोंकी परम्परा में सम्मिलित थे, किन्तु धरसेन पूर्वविद् होते हुए भी पूर्वविदोंकी परम्परामें नहीं थे। एक अन्य प्रमाण यह भी है कि धरसेनकी अपेक्षा गुणधर अपने विषयके पूर्ण ज्ञाता थे। अतः यह माना जा सकता है कि गुणधर ऐसे समय में हुए थे जब पूवों के आंशिक ज्ञानमें उतनी कमी नहीं आयी थो, जितनी कमी धरसेनके समयमें आ गयी थी । अतएव गुणधर धरसेनके पूर्ववर्ती हैं।
आचार्य गुणधरके समयके सम्बन्धमें विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इनका समय धरसेनके पूर्व है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लोहार्य तकको गुरु परम्पराके पश्चात् विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हदत्त इन चार आचार्यो का उल्लेख किया गया है। ये सभी आचार्य अंगों और पूर्वों के एकदेशज्ञाता थे। इनके पश्चात् अर्हद्वीलिका नाम आया है। अर्हद्वीलि बड़े भारी संघनायक थे। इन्हें पूर्वदेशके पुण्ड्वर्धनपूरका निवासी कहा गया है। इन्होंने पञ्चवर्षीय युगप्रतिक्रमणके समय बड़ा भारो एक यति-सम्मेलन किया, जिसमें सौ योजन तकके यति सम्मिलित हुए। इन यत्तियोंको भावनाओंसे अर्हद्वीलिने ज्ञात किया कि अब पक्षपातका समय आ गया है। अतएव इन्होंने नन्दि, वीर, अपराजित, देव, पञ्चस्तूप, सेन, भद्र, गुणधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामोंसे भिन्न-भिन्न संघ स्थापित किये, जिससे परस्परमें धर्मवात्सल्यभाव वृद्धिंगत हो सके।
संघके उक्त नामोंसे यह स्पष्ट होता है कि गुणधरसंघ आचार्य गुणधरके नाम पर ही था । अतः गुणधरका समय अर्हद्वीलिके समकालीन या उनसे भी पूर्व होना चाहिए। इन्द्रनन्दिको गुणधर और धरसेनका पूर्व या उत्तरवर्तीय ज्ञात नहीं है। अतएव उन्होंने स्वयं अपनो असमर्थता व्यक्त करते हुए लिखा है-
गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरकमोऽस्माभिः ।
न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात् ।। १५१ ।।
अर्थात् गुणधर और धरसेनको पूर्वापर गुरुपरम्परा हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि इसका वृत्तान्त न तो हमें किसी आगम में मिला और न किसी मुनिने ही बतलाया।
स्पष्ट है कि इन्द्रनन्दिके समय तक आचार्य गुणधर और धरसेनका पूर्वापर वत्तित्व स्मृत्तिके गर्भ में विलीन हो चुका था। पर इतना स्पष्ट है कि अर्हद्वीलि द्वारा स्थापित संघोंमें गुणधरसंघका नाम आया है। नन्दिसंघको प्राकृत पट्टावली में अर्हद्वीलिका समय वीर निर्वाण सं. ५६५ अथवा वि. सं. ९५ है। यह स्पष्ट है कि गुणधर अर्हद्वीलिके पूर्ववर्ती है; पर कितने पूर्ववर्ती हैं, यह निर्णयात्मक रूपसे नहीं कहा जा सकता। याद गणधरको परम्पराको ख्याति प्राप्त करने में सौ वर्षका समय मान लिया जाय तो 'छक्खंडागम' प्रवचनकर्ता घरसेनाचार्य से 'कसायपाहुड' के प्रणेता गुणवराचार्यका समय लगभग दो सौ वर्ष पूर्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आचार्य गुणधरका समय विक्रम संवत पूर्व प्रथम शताब्दी सिद्ध होता है।
हमारा यह अनुमान केवल कल्पना पर आधृत नहीं है। अर्हद्वीलिके समय तक गुणधरके इतने अनुयायी यति हो चुके थे कि उनके नामपर उन्हें संघकी स्थापना करनी पड़ी। अतएव अर्हद्वीलिको अन्य संघोंके समान गुणधर संघका भी मान्यता देनी पड़ी। प्रसिद्धि प्राप्त करते और अनुयायो बनानेमें कमसे कम सौ वर्षका समय तो लग ही सकता है। अतः गुणधरका समय धरसेनसे कमसे कम दो सौ वर्ष पूर्व अवश्य होना चाहिये।
इनके गुरु आदिके सम्बन्धमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। गुणधरने इस ग्रन्थकी रचना कर आचार्य नागहस्ति और आर्यमक्षुको इसका व्याख्यान किया था। अतएव इनका समय उक्त आचार्योंसे पूर्व है। छक्खंडागमके सूत्रों के अध्ययनसे भी यह अवगत होता है कि 'पेज्जदोसपाहुड' का प्रभाव इसके सूत्रों पर है। भाषाका दृष्टिसे भा छक्खंडागमकी भाषा कसायपाहुडकी भाषाकी अपेक्षा अर्वाचीन है। अतः गुणधरका समय वि. पू. प्रथम शताब्दी मानना गर्वथा उचित है! जयधवलाकारने लिखा है- "पुणो ताओ चेव सुत्तगाहाओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणीओ अज्जमं खुणागहत्थीणं गत्ताओ। पुणो नेसि दोण्हं पि पादमूले असोदिसदमाहाणं गुणहर मुहकमलविणिग्गयाणमार्थ सम्मं सोङ्गण जयीवसहभडारएण पचयणवच्छलेण चुन्नीसुतं कयं।'
अर्थात् गुणधराचायके द्वारा १८० गाथाओं में कसायपाहुड़का उपसंहार कर दिये जाने पर वे हा सुनगाथाएँ आचार्यपरम्परासे आती हुई आयमंक्षु और नागहस्तिको प्राप्त हुई। पश्चात उन दोनों ही आचार्या के पादमलमें बैठकर गुणधराचार्यके मुखकमलसे निकली हुई उन १८० गाथाओंके अर्थको भले प्रकारसे श्रवण करके प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित हो यतिवृषभ भट्टारकने उनपर चूणिसूत्रोंकी रचना की। इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि आचार्य गुणधरने महान विषयको संक्षेपमें प्रस्तुत कर सूत्रप्रणालीका प्रवर्तन किया। गुणधर दिगम्बर परम्पराके सबसे पहले सूत्रकार हैं।
गणघराचार्यने 'कसायपाहुड', जिसका दूसरा नाम 'पेज्जदोसपाहुड' भी है, को रचना की है। १६००० पद प्रमाण कसायपाहुडके विषयको संक्षेपमें एकसौ अस्सी गाथाओंमें ही उपसंहृत कर दिया है।
'पेज्ज' शब्दका अर्थ राग है। यतः यह ग्रन्थ राग और द्वेषका निरूपण करता है। क्रोधादि कषायोंको रागद्वेष परिणति और उनकी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेशबन्ध सम्बन्धी विशेषताओंका विवेचन ही इस ग्रन्थका मूल वर्ण्य विषय है। यह ग्रन्थ सूत्रशेलीमें निबद्ध है| गुणधरने गहन और विस्तृत विषधको अत्यन्त संक्षेपमें प्रस्तुत कर सूत्रपरम्पराका आरंभ किया है। उन्होंने अपने ग्रंथके निरूपणकी प्रतिज्ञा करते हुए गाथाओंको सुनगाहा कहा है-
गाहासदे असीदे अत्ये पण्णरसधा विहतम्मि |
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्यम्मि ॥२॥
स्पष्ट है 'कसायपाहुड' की शैली गाथासूत्र शैली है। प्रश्न यह है कि इन गाथाओंको सूत्रगाथा कहा जाय अथवा नहीं? विचार करनेसे ज्ञात होता है कि 'कसायपाहुड' की गाथाओं में सूत्रशैलीके सभी लक्षण समाहित हैं। इस ग्रन्थकी जयधवला-टीकामें आचार्य वीरसेनने आगमदृष्टिसे सूत्रशैलीका लक्षण बतलाते हुए लिखा है- सुत्तं
गणहरकहियं तहेय पत्तेयबुद्धकहियं च।
सुदकेवलिणा कहियं अभिष्णदसपुब्धिकहियं च।।
अर्थात् जो गणघर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्नदसपूर्वियों द्वारा कहा जाय यह सूत्र है।
अब यहाँ प्रश्न यह है कि गुणधर भट्टारक न तो गणधर हैं, न प्रत्येकबुद्ध हैं, न श्रुतकेवली हैं और न अभिन्नदशपूर्शी हैं। अत: पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार इनके द्वारा रचित गाथाओंको सूत्र कैसे माना जाय? इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य वीरसेनने लिखा है कि आगमद्रुष्टिसे सूत्र न होने पर भी शैलीकी दृष्टि से ये सभी गाथाएँ सूत्र है- 'इदि वयणादो णेदाओ गाहाओ सुत्तं गणहर-पत्तेयबुद्ध-सुदकेवलि-अभिण्णदसपुब्बीसु गुणहरभद्धारयस्स अभावादो; ण, णिड्डोसापकावर सहेउपमानेहि सुत्तेण ससित्तमस्थि त्ति सुत्तत्तुवलंभादो।' अर्थात् गुणधर भट्टारकको माथाएं निर्दोष, अल्पाक्षर एवं सहेतुक होनेके कारण सूत्रके समान हैं।
सूत्रशब्दका वास्तविक अर्थ बाजपद है। तीर्थंकरके मुखसे निस्सत बोज पदोंको सूत्र कहा जाता है और इस सूत्रके द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सूत्र सम कहलाता है-
'इदि वयणादा तिस्थयरवयणचिणिगयबीजपदं सुतं । तेण सुत्तेण समं धट्टीद उप्पज्जादि त्ति गणहरदेवम्मि द्विदसुदणाणं सुतसम'।
बन्धन अनुयोगद्वारमें सूत्रका अर्थ श्रुतकेवली या द्वादशांगरूप शब्दागम लिया गया है और श्रुतकेवली के समान श्रुतज्ञानको भी सूत्रसम कहा है; पर कृतिअनुयोगद्वारमें जो सूत्रको परिभाषा बतलाया गयी है उसके अनुसार द्वादशांगका सूत्रागममें अन्तर्भाव न होकर ग्रन्यागममें अन्तर्भाव होता है। यतः कृतिअनुयोगद्वारमें गणधर द्वारा रचे गये द्रव्यश्रुतको ग्रन्थागम कहा है।
आचार्य वीरसेनका अभिमत है कि सूत्रको समग्र परिभाषा जिनेन्द्र द्वारा कथीत अर्थपदोंमें ही पायी जाती है, गणधरदेवके द्वारा ग्रंथित द्वादशांगमें नहीं। इस विवेचनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि गुणपर आचार्य द्वारा विरचित 'कमायपाहुड’ में आगमसम्मत सूत्रकी परिभाषा घटित नहीं होती; पर सूत्रशैलीके समस्त लक्षण इसमें समाहित हैं। प्राचार्य वीरसेनने जयधवलामें 'कसायपाहुड' को सूत्रग्रन्थ सिद्ध करते हुए लिखा है-
"एवं सञ्चं पि सुत्तलक्षणं जिणवयणकमलविष्णिग्गय अथ्यपदाणं चेव संभवङ्, ण गणहरमुहविणिरायगंथरयणाए, तत्थ महापरिमाण तुवलंभादो; ण; सच्च (सुत्त) सारिच्छमस्सिदूण तत्थ वि सुत्तत्तं पडी विरोहाभावादो।"
अर्थात् सूत्रका सम्पूर्ण लक्षण तो जिनदेवके मुखकमलसे निस्सृत अर्थपदों में ही संभव है, गणधरकै मुखकमलसे निकली हुई रचनामें नहीं; क्योंकि गणधर की रचनाओंमें महापरिमाण माना जाता है। इतना होनेपर भी गणधरके वचन भी सूत्रके समान होनेके कारण सूत्र कहलाते हैं। अतः उनकी ग्रंथरचनामें भी सूत्रत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है। गणधरवचन भी बीजपदोंके समान सूत्र रूप है। अतएव गुणधर भट्टारककी रचना ‘कसायपाहुड़’ में सूत्रशैलीके सभी प्रमुख लक्षण घटित होते हैं। यहाँ विश्लेषण करनेपर निम्नलिखित सूत्रलक्षण उपलब्ध है-
१. अर्थमत्ता
२. अल्पाक्षरता
३. असंदिग्धता
४. निर्दोषता
५. हेतुमत्तता
६. सारयुक्तता
७. सोपस्कारता
८. अनवद्यता
९. प्रामाणिकता
स्पष्ट है कि कसायपाहुडकी गाथाओंकी शैली सूत्रशैली है। इस ग्रंथमें १८० + ५३ = २३३ गाथाएँ हैं। इनमें १२ गाथाएँ सम्बन्धज्ञापक हैं, छ: गाथाएं अधपरिमाणका निर्देश करती हैं और ३५ गाथाएँ संक्रमणवृतिसे सम्बद्ध हैं। जयधवलाके अनुसार ये समस्त २३३ गाथाएँ आचार्य गणधर द्वारा विरचित हैं। यहाँ यह शंका स्वभावतः उत्पन्न होती है कि जब ग्रन्थमें २२३ गाथाएँ थीं, तो ग्रन्थके आदिमें गुणधराचार्यने १८० गाथाओंका ही क्यों निर्देश किया? आचार्य वीरसेनने इस शंकाका समाधान करते हुए बताया है कि १५ अधिकारों में विभक्त होनेवाली गाथाओंको संख्या १८० रहने के कारण गुणधराचार्यने १८० गाथाओंकी संख्या निर्दिष्ट की है। सम्बन्ध-गायाएँ तथा अज्ञापरिमाण निर्देशक गाथाएँ इन १५ अधिकारोंमें सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। अतः उनकी संख्या छोड़ दी गयी है।
आचार्य वीरसेनने पुनः शंका उपस्थित की है कि संक्रमण सम्बन्धी ३५ गाथाएं बन्धक नामक अधिकारमें समाविष्ट हो सकती हैं, तब क्यों उनकी गणना उपस्थित नहीं की? इस शंकाका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रारंभके पांच अर्थाधिकारों में केवल तीन ही गाथाएं हैं और उन तीन गाथाओंसे निबद्ध हुए पांच अधिकारों से बन्धक नामक अधिकारसे ही उक्त ३५ गाथाएँ सम्बद्ध हैं। अतः इन ३५ गाथाओंको १८० गाथाओंकी संख्यामें सम्मिलित करना कोई महत्वकी बात नहीं है। हमारा अनुमान है कि जिन ५३ गाथाओंकी गणना आचार्य गुणधरने नहीं की है वे गाथाएं संभवत: नागहस्तिद्वारा विरचित होनी चाहिए। हमारे इस अनुमानकी पुष्टि जयधवलासे भी होती है। जयधवलामें मतान्तरसे उक्त ५३ गाथाओंको नागहस्तिकृत माना है।
एक बात यह भी विचारणीय है कि सम्बन्धनिर्देशक १२ गाथाओं और अद्धापरिमाणनिर्देशक छ: गाथाओं पर यत्तिवृषभके चूर्णिसूत्र भी उपलब्ध नहीं हैं। यदि ये गाथाएँ गुणधर भट्टारक द्वारा विरचित होती तो यतिवृषभ इनपर अवश्य ही चूणिसूत्र लिखते। दूसरी बात यह कि संक्रमणसे सम्बद्ध ३५ गाथाओं मेंसे १३ गाथाएँ शिवशर्म रचित कर्मप्रकृतिमें भी पायी जाती हैं। यह सत्य है कि उक्त तथ्योंसे ५३ गाथाओंके रचयिता नामहस्ति सिद्ध नहीं होते, पर इसमें आशंका नहीं कि उक्त ५३ गाथाएँ गुणधर भट्टारक द्वारा विरचित नहीं। यद्यपि आचार्य वीरसेनने व्याख्याकारोंके मतोंको स्वीकार नहीं किया है तो भी समीक्षाकी दृष्टिसे ५३ गाथाओंको गुणधर भट्टारक द्वारा विरचित नहीं माना जा सकता है। रचनाशेलीकी दुष्टिसे १८० गाथाओंकी अपेक्षा ५३ गाथाओंकी शैली भिन्न प्रतीत होती है। एक अनुमान यह भी है कि आचार्य गुणधरने १८० गाथाओंको १५ अधिकारोंमें विभक्त करनेवाली प्रतिज्ञा नहीं की है। उनकी प्रतिज्ञा तो यह होनी चाहिए थी कि सोलह हजार पद प्रमाण कषायप्रामृतको एक-सो अस्सी गाथाओंमें संक्षिप्त करता हूँ। वस्तुत: गुणधराचार्य कषाय प्राभूतको उपसंहत करनेके लिए प्रवृत्त हुए थे, स्वरचित गाथाओंको अधिकारोंमें विभक्त करनेके लिए नहीं।
'सस्तेदा गाहाओ'; 'एदाओ सुत्त गाहाओं' आदि पदोंसे यह ध्वनित होता है कि इन गाथाओंकी रचनासे पूर्व मूलगाथाओं और भाष्यगाथाओंकी रचना हो चुकी थी। अन्यथा अमुक गाथासूत्र है, इस प्रकारका कथन संभव ही नहीं था। अतएव व्याख्याकारोंके, 'गाहासदे असीदे’ प्रतिज्ञावाक्य नागहस्तिका है, इस अभिमतको सर्वथा उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता है।
कसायपाहुडमें १५ अधिकार हैं जो निम्न प्रकार है-
१. प्रकृति-विभक्ति अधिकार
२. स्थिति-विभक्ति अधिकार
३. अनुभाग-विमति अधिकार
४. प्रदेश-विभक्ति-झीणाझीण-स्थित्यन्तिक
५. बंधक अधिकार
६. वेदक अधिकार
७. उपयोग अधिकार
८. चतुःस्थान अधिकार
९. व्यंजन अधिकार
१०. दर्शनमोहोपशमना अधिकार
११. दर्शनमोहक्षपणा अधिकार
१२. संयमासंगमलब्धि अधिकार
१३. संयमलब्धि अधिकार
१४. चारित्रमोहोपशमना
१५. चारित्रमोहक्षपणा
१. प्रकृति-विभक्ति- अधिकारका अन्य नाम 'पेज्जदोस-विभक्ती' है। यतः कषाय पेज्ज- राग या देषरूप होती है। चूर्णिसूत्रोंमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंका विभाजन राग और द्वेषमें किया है। नैगम और संग्रहनयकी दृष्टिसे क्रोध और मान द्वेषरूप हैं तथा माया और लोभ रागरूप हैं। व्यवहारनय मायाको भी द्वेषरूप मानता है। यतः लोकमें मायाचारीकी निन्दा होती है। ऋजुसूत्रनय कोधको द्वेषरूप तथा लोभको रागरूप मानता है। मान और माया न तो रागरूप है और न द्वेषरूप ही; क्योंकि मान क्रोधोत्पत्तिके द्वारा द्वेषरूप है तथा माया लोभोत्पत्तिके कारण रागस्प है स्वयं नहीं। अत: इस परम्पराका व्यवहार ऋजुसूत्रनयकी सीमामें नहीं आता। तीनों शब्दनय चारों कषायोंको द्वेषरूप मानते हैं क्योंकि उनसे कर्मों का आनंद होता है। राग और दोषोंका विवेचना हादा अनुहारों में किया गण है एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भागाभागातुगम और अल्पबहुत्वानुगम।
२. स्थिति-विभक्ति-आत्माकी शक्तियोंको आवृत्त करनेवाला कर्म कहलाता है। यह पुद्गलरूप होता है। इस लोकमें सूक्ष्म कर्मपुद्गलस्कन्ध भरे हुए हैं जो इस जीवकी कायिक, वाचनिक और मानसिक प्रवृत्तिके साथ आकृष्ट होकर स्वतः आत्मासे बद्ध हो जाते हैं। कर्मपरमाणुओंको आकृष्ट करनेका कार्य योग द्वारा होता है। यह योग मन, वचन, काय रूप है। इस योगकी जैसी शुभाशुभ या तीव्र-मन्दरूप परिणति होती है उसीप्रकार कर्मों का आस्रव होता है। कषायके कारण कर्मों में स्थिति और अनुभाग उत्पन्न होते हैं। जब कर्म अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदयमें आते हैं तो इष्ट या अनिष्ट फल प्राप्त होता है। इसप्रकार जीव पूर्वबद्ध कर्मके उदयसे क्रोधादि कषाय करता है और उससे नवीन कर्मका बन्ध करता है। कर्मसे कषाय और कषायसे कर्मबन्धकी परम्परा अनादि है।
कर्मबन्धके चार भेद हैं- १. प्रकृतिबन्ध, २. स्थितिबन्ध, ३. अनुभाग बन्ध, ४. प्रदेशबन्ध। कर्मोंमें ज्ञान-दर्शनादिको रोकने और सुख-दुःखादि देनेका जो स्वभाव पड़ता है उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कर्म बन्धनेपर कितने समय तक आत्माके साथ बद्ध रहेंगे उस समयकी मर्यादाका नाम स्थितिबन्ध है। कर्म तीव्र या मन्द जैसा फल दें उस फलदानकी शक्तिका पड़ना अनुभागबन्ध है। कर्मपरमाणुओंकी संख्याके परिमाणका नाम प्रदेशबन्ध है। प्रकृति और प्रदेशनन्ध योग- मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे होते हैं। तथा स्थिति और अनु भागबन्ध कषायसे होते हैं । . स्थिति-विभक्तिनामक इस द्वित्तीय अधिकारमें स्थितिबन्ध के साथ प्रकृति बन्धका भी कथन सम्मिलित है। प्रकृति और स्थितिबन्धका एक जीवको अपेक्षा कथन स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंको अठेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्वकी दृष्टिसे किया है। कसायपाहुडमें मोहनीयकर्मका वर्णन विशेष रूपसे आया है। इस अधिकारमें प्रकृत्ति-विभक्ति के दो भेद किये हैं। प्रथम भेद मूलप्रकृति मोहनीयकर्म है और द्वितीय भेद उत्तरप्रकृतिमें मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ ग्रहण की गई हैं। इसप्रकार विभिन्न अनुयोगों द्वारा स्थिति-विभक्तिमें चौदह मार्गणाओंका आश्रय लेकर मोहनीयके २८ भेदोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बतलायो गई है। अद्धाच्छेद, सर्वविक्ति, नोसर्व विभक्ति, उत्कृष्टविक्ति, अनुत्तकृष्टविभक्ति, जयन्यविभक्ति, अजघन्मविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति आदिका कथन किया है।
३. अनुभाग-विभक्ति- अधिकारमें कर्मोंको फलदार-शक्तिका विवेचन किया गया है। आचार्यने यहां उस अनुभागका विचार किया है जो बन्धसे लेकर सत्ताके रूपमें रहता है। वह जितना बन्धकालमें हुआ उतना भी हो सकता है और होनाधिक भी संभव है। उसके दो भेद हैं- १. मूलप्रकृति-अनुभाग विभक्ति और २. उत्तरप्रकृति-अनुभागविभक्ति । इस सबका वर्णन संक्षेपमें किया है। इस अधिकारमें संज्ञाके दो भेद किये हैं- १. घातिसंज्ञा और २. स्थानसंज्ञा। मोहनीयकर्म की घातिसंज्ञा है क्योंकि वह जीवके गुणोंका घातक है। घातीके दो भेद हैं- सर्वघाती औः देशघाती। मोहनीवर उत्क्रुस्त अनुभाग सर्वघाती है और अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघातो और देशघाती दोनों प्रकारका है। इसी तरह जघन्य अनुभाग और अजघन्य अनुभाग देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकारका है। स्थान अनुभागके चार प्रकार है- एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक । इस प्रकार अनुभागनवभक्तिमें अनुभागके विभिन्न भेद-प्रभेदोंका कथन किया है।
४. प्रदेश-विभक्ति- कर्मों का बन्ध होनेपर तत्काल बन्धको प्राप्त कर्मों को जो द्रव्य मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। इसके दो भेद हैं- प्रथम बन्धके समय प्राप्त द्रव्य और द्वितीय बन्ध होकर सत्तामें स्थित द्रव्य| कसायपाहूडमें इस द्वितीयका हो निरूपण आया है। मोहनीय कर्मको लेकर स्वामित्व, काल, अन्तर, भंगविचय आदि दुष्टियोंसे विचार किया है। अनुभागके दो प्रकार है - जीवभागाभाग और प्रदेशभागाभाग। पहले की चर्चामें कहा है कि उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्ति बाले जीव सब जीवों के अनन्तमें भाग प्रमाण है। और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्ति बाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग प्रमाण है। इस प्रकार इस प्रदेश-विभक्ति अधिकारमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण प्रति कर्मों को स्थितियोंका भी विचार किया गया है।
५. बंधक - अधिकारमें कर्मवर्गणाओंका, मिथ्यात्व, अविरति आदिके निमित्तसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारके कर्मरूप परिणमनका कथन आया है। इस अधिकारमें बन्ध और संक्रम इन दो विषयोंका व्याख्यान किया है। गुणधर भट्टारकने इस बन्धक अधिकारमें संक्रमका भी अन्तर्भाव किया है। बन्धके दो भेद बताये है- १. अकर्मबन्ध और २. कर्मबन्ध| जो कार्माणवर्गणाएं कर्मरूप परिणत नहीं हैं उनका कर्मरूप परिणत होना अकर्म बन्ध है और कर्मरूप परिणत पुद्गलस्कन्धोंका एक कर्मसे अपने सजातीय अन्य कर्मरूप परिणमन करना कर्मबन्ध है। यह द्वितीय कर्मबन्ध भेद ही संक्रमरूप है। यही कारण है कि इस बन्धके अधिकारमें बन्ध और संक्रम इन दोनोंका समावेश हो जाता है। आचार्यने 'कदि पयडीओ बन्धदि' आदि २३ संख्यक गाथामें इस अधिकारका वर्णन किया है।
६. वेदक अधिकार- इस अधिकारमें बताया है कि यह संसारी जीव मोह नीयकर्म और उसके अवान्तर भेदोंका कहाँ कितने काल तक सान्तर या निरन्तर किस रूपमें वेदन करता है। इस अधिकारके दो भेद है- उदय और उदोरणा। उदीरणा सामान्यतः उदयविशेष ही है। किन्तु इन दोनोंमें अन्तर यह है कि कर्मों का जो यथाकाल फलविपाक होता है उसकी उदयसंज्ञा है और जिन कर्मों का उदयकाल प्राप्त नहीं हुआ उनको उपायविशेषसे पचाना उदोरणा है। इस अधिकारको गुणधरने चार गाथासूत्रोंमें निबद्ध किया है। यहाँ उदोरणा, उदय और कारणभूत बाह्य सामग्रीका निर्देश किया गया है। प्रथम पाद द्वारा उदीरणा सुचित की गयी है। द्वितीय पाद द्वारा विस्तार सहित उदय सूचित किया है और शेष दो पादों द्वारा उदयावलीके भीतर प्रविष्ट हुई उदय प्रकृत्तियों और अनुदयप्रकृतियोंको ग्रहण कर प्रवेशसंज्ञावाले अर्थाधिकारका सूचन किया है। गाथाके पूर्वाद्धका स्पष्टीकरण करनेके पश्चात् उत्तरार्द्ध में बताया है कि क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलोंको निमित्त कर कर्मों का उदय और उदौरणारूप फलत्रिपाक होता है। यहाँ क्षेत्रपदसे नरकादिगतियोंका क्षेत्र, भवपदसे एक इन्द्रियादि पर्यायोंका, कालपदसे बसन्त, ग्रीष्म और वर्षा आदिका एवं पुद्गल पदसे ग्रंथ, ताम्बूल, वस्त्र, आभरण आदि पुद्गलोंका ग्रहण किया है।
उदीरणाके समग्र विवेचनके पश्चात् गाथाके उत्तरार्द्ध में उदयका कथन किया है। उदीरणाके मूल प्रकृति उदोरणा और उत्तरप्रकृति उदोरणा ये दो भेद किये गये हैं। उत्तरवर्ती टोकाकारोंने १७ अनुयोगनारोंका आश्रय लेकर उदीरणाओंका विस्तृत विवेचन किया है।
वेदक अधिकारकी दूसरी गाथाका दूसरा पाद है 'को व केय अणुभागे' अर्थात् कौन जीव किस अनुभागमें मिथ्यात्व आदि कर्मों का प्रवेशक है। गाथासूत्रके इस पादको व्याख्या चूर्णिसूत्रकार और टीकाकारोंने विस्तारपूर्वक की है।"
७. उपयोगाधिकार में जीवके क्रोध, मान, मायादिरूप परिणामोंको उपयोग कहा है। इस अधिकार में चारों कषायोंके उपयोगका वर्णन किया गया है। और बतलाया है कि एक जीवके एक कायका उदय कितने काल तक रहता है और किस गत्तिके जीवके कौन-सी कषाय बारबार उदयमें आती है। एक भवमें एक कषायका उदय कितने बार होता है और एक कषायका उदय कितने भवों तक रहता है। जितने जीय वर्तमान समयमें जिस कषायसे उपयुक्त हैं क्या वे उतने ही पहले उसी कवायसे उपयुक्त थे? और आगे भी क्या उपयुक्त रहेंगे? आदि कषायविषयक सासष्य बातोंका विवेचन इस अधिकारमें किया है।
८. चतुःस्थान अधिकार- वातियाकर्मों की फलदानशक्तिका विवरण लता, दारू, अस्थि और शेलरूप उपमा देकर किया गया है। इन्हें क्रमशः एक स्थान, द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुःस्थान भी कहा गया है।
इस प्रस्तुत अधिकारके नामकरणका कारण भी उक्त चार स्थानोंका रहना हो है। उपमाओं द्वारा क्रोधको पाषाणरेखाके समान, पृथ्वीरेखाके समान, बालुरेखाके समान और जलरेखाके समान बसाया है। जिस प्रकार जलमें खिंची हुई रेखा तुरंत मिट जाती है और बालू, पृथ्वी और पाषाणपर खिंची गई रेखाएँ उत्तरोत्तर अधिक समयमें मिटती है, उसी प्रकार हीनाधिक कालकी अपेक्षासे क्रोधके भी चार स्थान है। इसी क्रमसे मान, माया और लोभके भी चार-चार स्थानोंका निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त चारों कषायोंके सोलह स्थानोंमेंसे कौन-सा स्थान किस स्थानसे अधिक होता है और कोन किससे हीन होता है, कोन स्थान सर्वघाती है, कोन स्थान देशघाती है? आदिका विचार किया गया है।
९. व्यजन अधिकार- व्यञ्जनका अर्थ पर्यायवाधी शब्द है। इस अधिकार में क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों हो कषायोंके पर्यायवाचक शब्दोंका प्रतिपादन किया गया है। क्रोधके पर्याय रोष ,अक्षमा, कलह, विवाद आदि बतलाये हैं। मानके पर्याय, मान, मद, दर्प, स्तम्भ, परिभव तथा मायाके, माया, निकृति, वंचना, सातियोग और अनऋजुता आदि बतलाये गये हैं। लोभके पर्यायोंमें लोभ, राग, निदान, प्रेयस्, मळ आदि बतलाये गये हैं। इस प्रकार विभिन्न पर्यायवाची शब्दों द्वारा कषायविषयोंपर विचार-विमर्श किया गया है।
१०. दर्शनमोहोपशमनाधिकार-जिस कर्मके उदयमें आनेपर जीवको अपने स्वरूपका दर्शन- साक्षात्कार और यथार्थ प्रतीति न हो उसे दर्शनमोहकर्म कहते हैं। इस कर्मके परमाणुओंका एक अन्तर्मुहसके लिए अभाव करने या उपशान्त रूप अवस्थाके करनेको उपशम कहते हैं। इस दर्शनमोहके उपशमनकी अवस्था में जीवको अपने वास्तविक स्वरूपका एक अन्तमुहूर्तके लिए साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कारकी स्थितिमें जो उसे आनन्द प्राप्त होता है वह अनिर्वच नीय है। दर्शनमोहके उपशमन करने वाले जीदके परिणाम कैसे होते हैं, उसके कौन सा योग होता, कौन-सा उपयोग रहता है। कौन-सी कषाय होती है और कौन-सी लेश्या, आदि बातोंका निरूपण करते हुए उन परिणाम विशेषोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। दर्शनमोहके उपशमको चारों गतियोंके ही जीव कर सकते हैं, पर उन्हे संज्ञी, पन्चेन्द्रिय और पर्याप्तक होना चाहिए। इस अधिकारके अन्तमें प्रथमोपशम-सम्यक्त्वीके विशिष्ट कार्यों और अवस्थाओंका वर्णन भी आया है।
११. दर्शनमोक्षपणा अधिकार- दर्शनमोहकी उपशम अवस्था अन्त मुहूर्त तक ही रहती है। इसके पश्चात् वह समाप्त हो जाती है| और जीव पुनः आत्मदर्शनसे वंचित हो जाता है। आत्मसाक्षात्कार सर्वदा बना रहे, इसके लिए दर्शन मोहका क्षय आवश्यक है। इसके लिये जिन प्रमुख बातोंकी आवश्यकता होती है उन सबका विवेचन इस अधिकार में किया गया है। दर्शनमोहके क्षयका प्रारम्भ कर्मभूमिमें उत्पन्न मनुष्य ही कर सकता है और इसकी पूर्णता चारों गतियों में की जा सकती है। दर्शनमोहके क्षपणका काल अन्तर्मुहूर्त है। इस क्षपर्णावयाके समाप्त होनेके पूर्व हो यदि उस मनुष्यको मृत्यु हो जाय तो वह अपनी आयुबन्धके अनुसार यथासंभव चारों ही गतियों में उत्पन्न हो सकता है। दर्शनमोहके क्षपणका प्रारम्भ करने वाला मनुष्य अधिक से अधिक तीन भव और धारण करके मुक्तिलाभ करता है। इस अधिकारमें दर्शनमोहक क्षपणकी प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी साधन-सामग्रीका निरूपण किया गया है।
१२. संयमासंयमलब्धि अधिकार- आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होते ही जीव मिथ्यास्वरूप पंकसे निकलकर निर्मल सरोवरमें स्नान कर आनन्दमें निमग्न हो जाता है। उसको विचारधारा सांसारिक विषयवासनासे दूर हो संयमासंयमकी प्राप्तिकी ओर अग्रसर होती है। शास्त्रीय परिभाषाके अनुसार अप्रत्याख्यानावरणकषायके उदयके अभावसे देशसंयमको प्राप्त करने वाले जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उसे संयमासंयमलब्धि कहते हैं। इसके निमित्तसे जोव श्रावकके व्रतोंको धारण करने में समर्थ होता है। इस अधिकारमें संयमासंयमलब्धिके लिये आवश्यक साधन-सामग्रियोंका विस्तार पूर्वक कथन किया है।
१३. संयमलब्धि अधिकार- प्रत्याख्यानावरणकषायके अभाव होनेपर आत्मामें संयमलब्धि प्रकट होती है, जिसके द्वारा आत्माकी प्रवृत्ति हिंसादि पाँच पापोंसे दूर होकर अहिंसादि महाव्रतोंके धारण और पालनकी होती है। संयमासंयम अधिकारकी गाथा ही इस अधिकारको गाथा है। संयमके प्राप्त कर लेनेपर भी कषायके उदयानुसार जो परिणामोंका उतार-चढ़ाव होता है उसका प्ररूपण अल्पबहुत्त्व आदि भेदों द्वारा किया गया है। इस लब्धिका वर्णन चूणिसूत्रकारने अधःकरण और अपूर्वकरणके विवेचन द्वारा किया है, जो अध्यात्म प्रेमी उपशमसम्यक्त्वके साथ संघमासंयम धारण करते हैं उनके तीनों करण होते हैं, पर जो वेदकसम्यकदृष्टि संयमासंयमको धारण करते हैं उनके दो ही करण होते हैं। संयमको धारण करनेके लिये आवश्यक सामग्रीका भी कथन किया गया है।
१४. चारित्रमोहोपशमनाधिकार- इस अधिकारमें प्रथम आठ गाथाएँ आती हैं। पहली गाथाके द्वारा उपशमना कितने प्रकारकी होती है, किस-किस कर्मका उपशम होता है आदि प्रश्न किये गये हैं। दूसरी गाथाके द्वारा निरुद्ध चारित्रमोहप्रकृतिको स्थितिके कितने भागका उपशम करता है, कितने भागका संक्रमण करता है और कितने भागका उदीरणा करता है इत्यादि प्रश्नोंकी अव तारणा की गयी है। तीसरी गाथाके द्वारा चारित्रमोहनीयका उपशम कितने कालमें किया जाता है उसो उपशमित प्रकृतिको उदोरणा-संक्रमण कितने काल तक करता है इत्यादि प्रश्न किये गये हैं। चौथी गाथाके द्वारा आठ करणोंमेंसे उपशामकके कब, किस करणसे व्युछित्ति होती है या नहीं इत्यादि प्रश्नोंका अव तार किया गया है। इस प्रकार चार गाथाओंके द्वारा उपशामकके और शेष चार गाथाओंके द्वारा उपशामकके पतनके सम्बन्ध में प्रश्न किये गये हैं।
१५. चारित्रमोहक्षपणाधिकार- यह अन्तिम अधिकार बहुत विस्तृत है। इसमें चारित्रमोहनीयकर्मके क्षयका वर्णन विस्तारसे किया है। यहां यह ध्यातव्य है कि चारित्रमोहनीयका क्षय अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करपके बिना संभव नहीं है। इस अधिकारमें २८ मूलगाथाएँ हैं ओर ८६ भाष्यगाथाएँ हैं। इस प्रकार कुल ११४ गाथाओंमें यह अधिकार व्याप्त है। इनमेंसे चार सूत्रमाथाएँ अधःप्रवृत्तिकरणके अन्तिम समयसे प्रतिबद्ध हैं। इनके आधारपर चूणिसूत्रों और जयधवलामें योग और कषायोंको उत्तरोत्तर विशद्धिका चित्रण किया गया है। आशय यह है कि चारित्रमोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंका क्षय किस क्रमसे होता है और किस-किस प्रकृतिक क्षय होनेपर कहाँपर कितना स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्व रहता है इत्यादि बातोंका वर्णन इस अधिकारमें आया है। ध्यान और कषायक्षयको प्रक्रिया भी इस अधिकारमें वर्णित है।
बायपावना को नीदर महावीरकी आरातीय परम्परासे प्राप्त हुआ है| वीरसेनाचार्य ने जयधवला-टीकामें लिखा है- "एदम्हादो विउलगिरिमत्ययस्थवड्डमाणदिवायरादो विणिग्यमिय गोदम लोहज्ज-जंबुसामियादि-आइरियपरंपराए आगंतूण गुणहराइरियं पाविय गाहास रूवेण परिणामय" अर्यातविपुलाचलके शिखरपर विराजमान वर्धमान दिवाकरसे प्रकट होकर गौतम, लोहाचार्य, जम्बूस्वामी आदिकी आचार्यपरम्परासे आकर गुणधरको 'कम्मपडिपाहुड' का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने गाथारूपमें इस ज्ञान का प्रतिपादन किया | स्पष्ट है कि आचार्य गुणधरको केलियोंकी परम्परासे ज्ञान प्रास हुआ था| आचार्य गुणधर सूत्ररचनाशैलीके प्रकाण्ड विद्वान् हैं । धवला टीकामें आचार्य वीरसेनने उन्हें वाचक कहा है और वाचकका अर्थ पूर्वविद लिया है। अतएव इनकी रचना-प्रतिभा मंजुल अर्थको संक्षेपमें प्रस्तुत करनेकी थी। वस्तुतः आचार्य गुणधर 'कम्मपडिपाहुड' के ज्ञाता होनेके साथ ही अत्यन्त प्रतिभाशाली और विषविशेषज विद्वान थे। इनके कसायपाहुडकी प्रत्येक गाथाके एक-एक पदको लेकर एक-एक अधिकारका रचा जाना तथा तीन गाथाओंका पाँच अधिकारोंमें निबद्ध होना ही इनकी प्रतिभाकी गंभीरता और अनन्त अर्थगर्भित अभीव्यक्तीको सूचित करता है। वेदक अधिकारकी जो ज सकामेदिय' (गाथाङ्क ६२) गाथाके द्वारा चारों प्रकारके बन्ध, चारों प्रकारके संक्रमण, चारों प्रकारके उदय, चारों प्रकारकी उदीरणा और चारों प्रकारके सत्वसम्बन्धी अल्पबहुत्वकी सूचना निश्चयतः उसके गाम्भीर्य और अनन्तार्थभित्वकी साक्षी है। अर्थबहुलताकी दृष्टि से गुणधरकी शैली अत्यन्त गंभीर है। गुणधरके इस ग्रंथपर यदि चूर्णिसूत्र न लिखे जाते तो उनका अर्थ पश्चादवर्ती व्यक्ति योंके लिये दुर्बोध हो जाता।
आचार्य शिवशर्मके 'कम्मपयडि' और 'सतक' नामक दो ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। इन दोनों ग्रंथोका उद्गम स्थान 'महाकम्मपडिपाहुड' है। 'कम्म पयडी के साथ जब हम गुणधरके 'कषायपाहुड' की तुलना करते हैं तो हमें इन दोनोंमें मौलिक अन्तर प्रतीत होता है। कम्मापयडिमें महाकम्मपडिपाहुडके चौबीस अनुयोगद्वारोंका समावेश नहीं है। किन्तु बन्धन, उदय और संक्रमणादि कुछ अनुयोगद्वार ही प्राप्त हैं। गुणधरने अपने 'कषायपाहुड' में समस्त 'पेज्जदोषपाहुड' का उपसंहार किया है। अतः यह स्पष्ट है कि 'कम्मपयडि की रचना शिवशर्मने गुणधरके पश्चात् ही की है। 'कम्मपयडि' और 'सतक’ इन दोनों ग्रंथोके अन्त में अपनी अल्पज्ञना प्रकट करते हुए शिवशर्मने दृष्टिवादके ज्ञाता आचार्यों से उसे शुद्ध कर लेनेकी प्रार्थना की है। वस्तुत: 'कम्मपयडि' एक संग्रह ग्रंथ है क्योंकि उसमें विभिन्न स्थानोंपर आई हुई प्राचीन गाथाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। कम्मपयडिकी चूणिमें उसके कर्ताने उसे 'कम्पयडिसंग्रहिणी' नाम दिया है। इसी प्रकार 'सतक' चुर्णीमें भी उसे संग्रह-ग्रन्थ कहा है। गुणधरकी यह रचना मौलिक है तथा कर्म-शिद्धान्तको बीजरूप में प्रस्तुत करती है।
कषायपाहुड कम्मपडिसे पूर्ववर्ती है। कम्मपर्याडके संक्रमकरणमें कषाय पाहुड़के संक्रमअर्थाअधिकारको १३ गाथाएँ साधारण पाठभेदके साथ अनुक्रमसे ज्यों-की-त्यों उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार कम्मपयडिके उपशमकरणमें कषाय पाहुडके दर्शनमोहोपशमना अर्थाधिकारकी चार गाथाएँ कुछ पाठभेदके साथ पायी जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य गुणधर केवली और श्रुतकेवलियोंके अनन्सर पहले पूर्वविद हैं, जिन्होंने 'महाकम्मपयडिपाहुड' का संक्षेपमें उपसंहार किया। महान् अर्थको अल्पाक्षरोंमें निबद्ध करनेकी प्रतिभा उनमें विद्यमान थी। यही कारण है कि कसायपाहुडका उत्तरकालीन सभी वाङ्मयपर प्रभाव है।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------श्रुतधराचार्यसे अभिप्राय हमारा उन आचार्यों से है, जिन्होंने सिद्धान्त, साहित्य, कमराहिम, बायाससाहित्यका साथ दिगम्बर आचार्यों के चारित्र और गुणोंका जोबन में निर्वाह करते हुए किया है। यों तो प्रथमानुयोग, करणा नुयोग, चरणानुयोग और ध्यानुयोगका पूर्व परम्पराके भाधारपर प्रन्धरूपमें प्रणयन करनेका कार्य सभी आचार्य करते रहे हैं, पर केवली और श्रुत केवलियोंकी परम्पराको प्राप्त कर जो अंग या पूर्वो के एकदेशशाता आचार्य हुए हैं उनका इतिवृत्त श्रुतधर आचार्यों को परम्पराके अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायगा | अतएव इन आचार्यों में गुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवाल, यति वृषम, उच्चारणाचार्य, आयमंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, गृपिच्छाचार्य और बप्पदेवकी गणना की जा सकती है ।
श्रुतघराचार्य युगसंस्थापक और युगान्तरकारी आचार्य है। इन्होंने प्रतिभाके कोण होनेपर नष्ट होतो हुई श्रुतपरम्पराको मूर्त रूप देनेका कार्य किया है। यदि श्रतधर आचार्य इस प्रकारका प्रयास नहीं करते तो आज जो जिनवाणी अवशिष्ट है, वह दिखलायी नहीं पड़ती। श्रुतधराचार्य दिगम्बर आचार्यों के मूलगुण और उत्तरगुणों से युक्त थे और परम्पराको जीवित रखनेको दृष्टिसे वे ग्रन्थ-प्रणयनमें संलग्न रहते थे 1 श्रुतकी यह परम्परा अर्थश्रुत और द्रव्यश्रुतके रूपमें ई. सन् पूर्वकी शताब्दियोंसे आरम्भ होकर ई० सनकी चतुर्थ पंचम शताब्दी तक चलती रही है ।अतएव श्रुतघर परम्परामें कर्मसिद्धान्त, लोका. नुयोग एवं सूत्र रूपमें ऐसा निबद साहित्य, जिसपर उत्तरकालमें टीकाएँ, विव त्तियाँ एवं भाष्य लिखे गये हैं, का निरूपण समाविष्ट रहेगा।
Acharya Gunadhar
Shashank Shaha
#Gunadharmaharajji
15000
Acharya Shri 108 Gunadhar MaharajJi
#Gunadharmaharajji
Gunadharmaharajji
You cannot copy content of this page